अंतर्राष्ट्रीय संबंध
बांग्लादेश की राजनीतिक उथल-पुथल और भारत पर इसका प्रभाव
प्रिलिम्स के लिये:मुद्रास्फीति, यूरोपियन यूनियन, भारत-बांग्लादेश संबंध, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971, अखौरा-अगरतला रेल संपर्क मेन्स के लिये:भारत-बांग्लादेश संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा भारत से जुड़े समझौते और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते। |
स्रोत: द हिंदू
चर्चा में क्यों?
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा दक्षिण एशियाई भू-राजनीति में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ है। विरोध प्रदर्शनों के बीच देश छोड़कर भारत में शरण लेने के बाद बांग्लादेश की स्थिरता और भारत के साथ उसके संबंधों पर सवाल उठने लगे हैं।
- इस उथल-पुथल के न केवल बांग्लादेश के लिये बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु भी दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।
बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति क्या है?
- विरोध प्रदर्शन और अशांति: बांग्लादेश में नौकरी कोटा के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन जारी है, जो सत्तावादी नीतियों और विपक्ष के दमन से प्रेरित है, जिसके कारण काफी अशांति पैदा हो गई है, जो वर्ष 2008 में शेख हसीना के कार्यकाल के बाद से सबसे बड़ी अशांति है।
- आर्थिक चुनौतियाँ: शेख हसीना के जाने से कोविड-19 महामारी से देश की आर्थिक सुधार को लेकर चिंताएँ पैदा हो गई हैं, जो पहले से ही बढ़ती मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन से प्रभावित है।
- राजनीतिक परिदृश्य: बांग्लादेश की सेना अंतरिम सरकार बनाने के लिए तैयार है, जो स्थिति की अस्थिरता को दर्शाता है। कट्टरपंथी इस्लामी ताकतों की संभावित वापसी बांग्लादेश के धर्मनिरपेक्ष शासन को खतरे में डाल सकती है।
- निर्यात प्रवाह में व्यवधान: बांग्लादेश का कपड़ा क्षेत्र, जो इसके निर्यात राजस्व में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है, बड़े व्यवधानों का सामना कर रहा है। चल रही अशांति के कारण आपूर्ति शृंखलाएँ टूट गई हैं, जिससे माल की आवाजाही और उत्पादन कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं।
- बांग्लादेश वैश्विक वस्त्र उद्योग, कपड़ों के वैश्विक व्यापार का 7.9% हिस्सा है। देश का 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर का परिधान क्षेत्र, जिसमें चार मिलियन से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, इसके व्यापारिक निर्यात का 85% से अधिक प्रतिनिधित्व करता है।
- बांग्लादेश में अनिश्चितता के कारण अंतरराष्ट्रीय क्रेता अपने आपूर्ति स्रोतों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप भारत सहित वैकल्पिक बाज़ारों में ऑर्डर का स्थानांतरण हो सकता है।
- अगर भारत, बांग्लादेश से विस्थापित ऑर्डर का एक हिस्सा हासिल कर लेता है तो उसे काफी फायदा हो सकता है। उद्योग विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर बांग्लादेश के कपड़ा निर्यात का 10-11% तिरुपुर जैसे भारतीय केंद्रों को पुनर्निर्देशित किया जाता है तो भारत को मासिक कारोबार में 300-400 मिलियन अमरीकी डॉलर का अतिरिक्त लाभ हो सकता है।
बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है?
- एक साझेदार की हानि: भारत ने शेख हसीना के रूप में एक महत्त्वपूर्ण साझेदार खो दिया है, जो आतंकवाद का मुकाबला करने और द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने में आवश्यक भूमिका निभा रही थी।
- हसीना के नेतृत्व में भारत को सुरक्षा मामलों पर बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिला, लेकिन राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव के कारण अब यह संबंध खतरे में है।
- वित्त वर्ष 2023-24 में भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय व्यापार 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिससे बांग्लादेश उपमहाद्वीप में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बन गया। हसीना के प्रशासन के तहत दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता (South Asian Free Trade Area- SAFTA) समझौते के तहत अधिकांश टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्रदान की गई थी।
- उनके प्रशासन के प्रति भारत का समर्थन अब एक दायित्व बन गया है, क्योंकि उनकी अलोकप्रियता और विवादास्पद शासन भारत की क्षेत्रीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है।
- हसीना के नेतृत्व में भारत को सुरक्षा मामलों पर बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिला, लेकिन राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव के कारण अब यह संबंध खतरे में है।
- पश्चिमी देशों की जाँच और संभावित प्रतिक्रिया: हसीना को भारत के समर्थन ने पश्चिमी सहयोगियों, खास तौर पर अमेरिका के साथ टकराव पैदा किया है, जिसने उनकी अलोकतांत्रिक गतिविधियों की आलोचना की है। अब अलोकप्रिय नेता का समर्थन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संतुलित करना भारत के लिये चुनौती है।
- हसीना की बढ़ती अलोकप्रियता के कारण भारत को बांग्लादेशी नागरिकों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, जो भारत को अपदस्थ नेता का सहयोगी मानते हैं। यह स्थिति भारत-बांग्लादेश संबंधों को प्रभावित कर सकती है।
भारत के लिये बांग्लादेश का महत्त्व
- यह देश व्यापार और परिवहन के लिये एक महत्त्वपूर्ण गलियारे के रूप में कार्य करता है, जो पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँच को सुविधाजनक बनाता है।
- क्षेत्रीय सुरक्षा के लिये एक स्थिर और मैत्रीपूर्ण बांग्लादेश आवश्यक है। आतंकवाद-रोधी, सीमा सुरक्षा तथा अन्य सुरक्षा मामलों पर सहयोग दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है।
- यह आर्थिक संबंध भारत की विदेश व्यापार नीति के लक्ष्यों का समर्थन करता है तथा 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के उसके लक्ष्य में योगदान देता है।
- भारत और बांग्लादेश के बीच सक्रिय सहयोग बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation- BIMSTEC) और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (South Asian Association for Regional Cooperation- SAARC) जैसे क्षेत्रीय मंचों की सफलता हेतु महत्त्वपूर्ण है।
नई व्यवस्था के साथ जुड़ने में भारत के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?
- अनिश्चित राजनीतिक वातावरण: नई सरकार की प्रकृति, चाहे उसका नेतृत्व विपक्षी दल करें या सेना, भारत के सामरिक हितों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालेगी।
- भारत के प्रति कम मैत्रीपूर्ण रवैया रखने वाला नया प्रशासन भारत विरोधी उग्रवादी समूहों को फिर से सक्रिय कर सकता है, जिससे सीमाओं पर पहले से ही तनावपूर्ण सुरक्षा स्थिति और भी तनावपूर्ण हो सकती है।
- यदि इस्लामी चरमपंथ बढ़ता है तो हिंदू अल्पसंख्यकों को अधिक जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। भारत को क्षेत्रीय तनाव से बचने के लिये हिंदू शरणार्थियों के लिये नागरिकता के वादों पर सावधानीपूर्वक कार्य करना चाहिये।
- क्षेत्रीय भू-राजनीति: बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता चीन को इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर प्रदान कर सकती है।
- भारत को सतर्क रहना चाहिये क्योंकि बीजिंग नई सरकार को आकर्षक सौदे दे सकता है, ठीक उसी तरह जैसे उसने श्रीलंका और मालदीव में शासन परिवर्तनों का लाभ उठाया है।
- भारत को यह सुनिश्चित करने के लिये रणनीतिक साझेदारियों में शामिल होना होगा कि उग्रवादी तत्त्वों को बढ़ावा न मिले और बांग्लादेश की आर्थिक स्थिरता बनी रहे।।
- बांग्लादेश में उथल-पुथल ऐसे समय में आई है जब भारत कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान के साथ तनाव, म्याँमार में अस्थिरता, नेपाल के साथ तनावपूर्ण संबंध, अफगानिस्तान और मालदीव में तालिबान द्वारा सत्ता पर कब्ज़ा करना शामिल है।
- भारतीय निवेश पर प्रभाव: राजनीतिक उथल-पुथल के कारण बांग्लादेश में भारतीय व्यवसायों और निवेशों को अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में व्यवधान और भुगतान में देरी इन निवेशों की लाभप्रदता और स्थिरता को प्रभावित कर सकती है।
- यह अशांति बांग्लादेश में भारतीय स्वामित्व वाली कपड़ा निर्माण इकाइयों को प्रभावित करेगी। बांग्लादेश में लगभग 25% कपड़ा इकाइयाँ भारतीय कंपनियों के स्वामित्व में हैं। संभावना है कि मौजूदा अस्थिरता के कारण ये इकाइयाँ अपना परिचालन वापस भारत में स्थानांतरित कर सकती हैं।
- अक्तूबर 2023 में संभावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के बारे में चर्चा शुरू होने के साथ ही उम्मीदें बढ़ गई हैं कि इससे भारत में बांग्लादेश के निर्यात में 297% और भारत के निर्यात में 172% तक की वृद्धि हो सकती है।
- हालाँकि, राजनीतिक अस्थिरता इन वार्ताओं के भविष्य के बारे में संदेह पैदा करती है और मौजूदा व्यापार प्रवाह को बाधित कर सकती है।
- बुनियादी ढाँचे और कनेक्टिविटी की चिंताएँ: भारत-बांग्लादेश संबंधों को मज़बूत करने में बुनियादी ढाँचे और कनेक्टिविटी की अहम भूमिका रही है। भारत ने वर्ष 2016 से सड़क, रेल और बंदरगाह परियोजनाओं के लिये 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है, जिसमें अखौरा-अगरतला रेल लिंक एवं खुलना-मोंगला पोर्ट रेल लाइन शामिल है।
- हालाँकि, मौजूदा अशांति इन महत्त्वपूर्ण संपर्कों को खतरे में डालती है, जिससे भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापार और पहुँच बाधित हो सकती है और पहले के समझौते खतरे में पड़ सकते हैं।
- संतुलन: भारत को लोकतांत्रिक ताकतों का समर्थन करने और क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संबंधों को प्रबंधित करने के बीच संतुलन बनाना चाहिये।
- चुनौती यह होगी कि बांग्लादेश में मज़बूत राजनयिक उपस्थिति बनाए रखते हुए आंतरिक विवादों में उलझने से बचा जाए।
भारत को अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाने के लिये क्या करना चाहिये?
- नए गठबंधन बनाना: भारत एक सतर्क दृष्टिकोण बनाए हुए है, बांग्लादेश में स्थिति पर बारीकी से नज़र रखते हुए "प्रतीक्षा करें और देखें" की रणनीति अपना रहा है। इसमें क्षेत्रीय स्थिरता पर विकास और उनके संभावित प्रभावों का आकलन करना शामिल है।
- इसके अलावा, भारत को बांग्लादेश में विभिन्न राजनीतिक गुटों के साथ जुड़ना चाहिये, ताकि अधिक समावेशी संबंध विकसित हो सकें। भारत को एक लचीली रणनीति विकसित करनी चाहिये जो बांग्लादेश में विकसित हो रहे राजनीतिक परिदृश्य को समायोजित कर सके।
- भारत के बारे में किसी भी नकारात्मक धारणा का मुकाबला करने के लिये बांग्लादेशी समाज के व्यापक स्पेक्ट्रम के साथ जुड़ना महत्त्वपूर्ण होगा। भारत को वर्ष 1971 की मुक्ति कथा से आगे बढ़ने की ज़रूरत है।
- सुरक्षा उपायों को बढ़ाना: भारत को संभावित स्पिलओवर प्रभावों को कम करने और स्थिरता बनाए रखने के लिये सीमा पर तथा महत्त्वपूर्ण बांग्लादेशी प्रवासी आबादी वाले क्षेत्रों में अपने सुरक्षा उपायों को और मज़बूत करना चाहिये।
- डिजिटल कनेक्टिविटी कॉरिडोर: डिजिटल कनेक्टिविटी कॉरिडोर विकसित करने से व्यापार, तकनीकी आदान-प्रदान और ई-कॉमर्स को बढ़ावा मिल सकता है।
- नए राजनीतिक माहौल के मद्देनजर बांग्लादेश के साथ FTA की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना।
- भू-राजनीतिक पैंतरेबाजी: भारत को यह अनुमान लगाना चाहिये कि पाकिस्तान और चीन बांग्लादेश की स्थिति से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे।
- इन जोखिमों को कम करने के लिये अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों सहित अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग करना महत्त्वपूर्ण होगा।
- भारत को बांग्लादेश के आर्थिक स्थिरीकरण और चरमपंथी प्रभावों का मुकाबला करने के लिये यूएई और सऊदी अरब जैसे खाड़ी भागीदारों के साथ कार्य करना चाहिये। यह सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और बांग्लादेश को अपने पारंपरिक सहयोगियों से दूर जाने से रोकने में मदद कर सकता है।
|
दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत के पड़ोसी देशों में लगातार राजनीतिक अस्थिरता के क्या परिणाम हैं? बांग्लादेश में हाल की राजनीतिक अस्थिरता के आलोक में चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये। |
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)मेन्स:प्रश्न. नियंत्रण रेखा (LoC) सहित म्याँमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमाओं पर आंतरिक सुरक्षा खतरों तथा सीमा पार अपराधों का विश्लेषण कीजिये। इस संबंध में विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा निभाई गई भूमिका पर भी चर्चा कीजिये। (2018) |


भारतीय अर्थव्यवस्था
अवसंरचना परियोजनाओं को सरकार द्वारा प्रोत्साहन
प्रिलिम्स के लिये:अवसंरचना परियोजना, पूंजीगत व्यय, डिजिटल डिवाइड, निवेश मॉडल के प्रकार, साइबर सुरक्षा, डिजिटल और सामाजिक अवसंरचना, डिजिटल इंडिया मुख्य परीक्षा के लिये:अवसंरचना विकास के लिये सरकारी पहल, भारत में अवसंरचना विकास की चुनौतियाँ, भारत में अवसंरचना विकास के लिये उठाए जा सकने वाले कदम। |
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
चर्चा में क्यों?
हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत आठ राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
- इन परियोजनाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 4.42 करोड़ दैनिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
स्वीकृत आठ राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाएँ कौन-सी हैं?
|
कॉरिडोर परियोजनाएँ |
निवेश मॉडल |
|
बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) |
|
हाइब्रिड ऐन्युइटी मॉडल (HAM) |
|
इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) मॉडल |
PPP मॉडल के विभिन्न प्रकार क्या हैं?
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership- PPP) मॉडल: PPP सार्वजनिक परिसंपत्तियों और/या सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान के लिये सरकार एवं निजी क्षेत्र के बीच एक व्यवस्था है। PPP बड़े पैमाने पर सरकारी परियोजनाओं, जैसे कि सड़क, पुल या अस्पताल को निजी वित्तपोषण से आपूर्ति करने की अनुमति देता है।
- PPP मॉडल के प्रकार:
|
मॉडल |
विवरण |
|
निर्माण-संचालन-हस्तांतरण (BOT) |
एक निजी भागीदार डिज़ाइन करता है, बनाता है, संचालित (अनुबंधित अवधि के दौरान) करता है, और सुविधा को सार्वजनिक क्षेत्र में वापस स्थानांतरित करता है। निजी क्षेत्र उपयोगकर्त्ताओं से राजस्व एकत्र करते हुए परियोजना का वित्तपोषण, निर्माण और रखरखाव करता है। NHAI द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएँ BOT मॉडल का एक प्रमुख उदाहरण हैं। |
|
बिल्ड-ओन-ऑपरेट (BOO) |
इस मॉडल में, नवनिर्मित सुविधा का स्वामित्व निजी पक्ष के पास होता है। पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर, सार्वजनिक क्षेत्र का भागीदार परियोजना द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को ‘खरीदने’ के लिये सहमत होता है। |
|
बिल्ड-ओन-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOOT) |
BOT के इस प्रकार में, समझौता की गई समयावधि के बाद, परियोजना को सरकार या निजी ऑपरेटर को हस्तांतरित कर दिया जाता है। BOOT मॉडल का प्रयोग राजमार्गों और बंदरगाहों के विकास के लिये किया जाता है। |
|
बिल्ड-ओन-लीज़-ट्रांसफर (BOLT) |
इस दृष्टिकोण में, सरकार एक निजी इकाई को एक सुविधा बनाने (और संभवतः इसे डिज़ाइन करने), सुविधा का स्वामित्व लेने, सार्वजनिक क्षेत्र को सुविधा पट्टे पर देने और पुनः पट्टे की अवधि के अंत में सुविधा का स्वामित्व सरकार को हस्तांतरित करने की रियायत देती है। |
|
डिज़ाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट (DBFO) |
|
|
लीज़-डेवलप-ऑपरेट (LDO) |
सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नव निर्मित अवसंरचना सुविधा का स्वामित्व बरकरार रखती है और निजी प्रमोटर के साथ लीज़ समझौते के अनुसार भुगतान प्राप्त करती है। इसका पालन अधिकतर हवाई अड्डे की अवसंरचना विकास में किया जाता है। |
|
हाइब्रिड ऐन्युटी मॉडल (HAM) |
यह EPC और BOT-ऐन्युटी मॉडल का मिश्रण है। डिज़ाइन के अनुसार, सरकार पहले पाँच वर्षों में वार्षिक भुगतान (ऐन्युटी) के माध्यम से परियोजना लागत का 40% योगदान देगी। शेष भुगतान निर्मित परिसंपत्तियों और डेवलपर के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। |
|
इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) मॉडल |
इस मॉडल के तहत, सरकार सामग्री की खरीद और निर्माण सहित सभी लागतों को वहन करती है। निजी क्षेत्र की भागीदारी इंजीनियरिंग विशेषज्ञता प्रदान करने तक सीमित है। इस मॉडल की एक प्रमुख चुनौती सरकार पर उच्च वित्तीय बोझ है। |
अवसंरचना विकास के लिये सरकार का रोडमैप क्या है?
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) पर ध्यान: सरकार ने PPP निवेश मॉडल के माध्यम से परियोजना विकास पर ज़ोर दिया है।
- यह मॉडल निजी भागीदारों को निवेश जोखिम उठाने और राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव का प्रबंधन करने की अनुमति देता है।
- रियायत समझौतों में संशोधन: सरकार ने निजी निवेशकों के लिये इसे और अधिक आकर्षक बनाने हेतु मॉडल रियायत समझौते में संशोधन किया है, जिसमें उदार मुआवज़ा (Liberal compensation), विस्तारित रियायत अवधि व समापन भुगतान शामिल हैं।
- पहले की रियायत समझौता प्रणाली में निश्चित मुआवज़ा, छोटी रियायत अवधि, कम समापन भुगतान और सख्त नियामक निरीक्षण शामिल थे, जिससे यह निजी निवेशकों के लिये कम आकर्षक हो गया था।
- निर्माण सहायता की शुरूआत: एक नवीन 'निर्माण सहायता' तंत्र भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को भौतिक प्रगति के आधार पर दस किस्तों में कुल परियोजना लागत का 40% तक भुगतान करने में सक्षम करेगा, जिससे निजी डेवलपर्स के लिये वित्तीय व्यवहार्यता में वृद्धि होगी।
- इससे पहले NHAI केवल इक्विटी सहायता प्रदान करता था, जिसके परिणामस्वरूप नकदी प्रवाह की चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं क्योंकि डेवलपर्स को परियोजना पूरी होने से पहले अपनी स्वयं की निधि पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता था।
- हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं का आर्थिक प्रभाव: इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी में सुधार तथा परिवहन लागत में कमी द्वारा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना है (विशेष रूप से पश्चिम बंगाल एवं पूर्वोत्तर राज्यों में)।
- भारत में राजमार्ग निर्माण के क्षेत्र में प्रगति:
- राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई वर्ष 2013-14 के 0.91 लाख किमी. से बढ़कर वर्ष 2024 में 1.46 लाख किमी. हो गई है।
- राष्ट्रीय राजमार्गों का औसत वार्षिक निर्माण वर्ष 2004-14 के लगभग 4,000 किमी. से लगभग 2.4 गुना बढ़कर वर्ष 2014-24 में लगभग 9,600 किमी. हो गया है।
- निजी निवेश सहित राष्ट्रीय राजमार्गों में कुल पूंजी निवेश वर्ष 2013-14 के 50,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर वर्ष 2023-24 में लगभग 3.1 लाख करोड़ रुपए हो गया है।
- सरकार ने सुसंगत मानकों, उपयोगकर्त्ता सुविधा और रसद/लॉजिस्टिक्स दक्षता पर ध्यान केंद्रित करते हुए कॉरिडोर-आधारित राजमार्ग अवसंरचना विकास दृष्टिकोण अपनाया है।
संबंधित बुनियादी अवसंरचना विकास योजनाएँ
- पीएम गति शक्ति योजना: इसका उद्देश्य बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है, जिसमें ज़मीनी स्तर पर कार्यों में तेज़ी लाना, लागत बचाना और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करना है।
- भारतमाला योजना: यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) के तहत शुरू किया गया एक व्यापक कार्यक्रम है।
- भारतमाला के प्रथम चरण की घोषणा वर्ष 2017 में की गई थी और इसे वर्ष 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब इसकी समयसीमा बढ़ाकर वर्ष 2027-28 तक कर दी गई है।
- इसमें पहले से निर्मित बुनियादी अवसंरचना की बढ़ी हुई प्रभावशीलता, बहुविध एकीकरण, निर्बाध आवागमन के लिये बुनियादी अवसंरचना की कमियों को दूर करने एवं राष्ट्रीय व आर्थिक कॉरिडोर को एकीकृत करने पर केंद्रित है।
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP): यह पूरे देश में विश्व स्तरीय आधारिक संरचना उपलब्ध कराने तथा सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिये सामाजिक एवं आर्थिक बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं का एक समूह है।
- सागरमाला परियोजना: इसे वर्ष 2015 में स्वीकृति दी गई थी जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण, मशीनीकरण और कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से भारत की 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ बंदरगाह की बुनियादी अवसंरचना का विकास करना है।
- उड़े देश का आम नागरिक (UDAN): इस योजना का उद्देश्य भारत के दूरस्थ और स्थानीय क्षेत्रों में हवाई संपर्क में सुधार करना, आम लोगों को सस्ती दरों पर हवाई यात्रा करने में सक्षम बनाना और विमानन क्षेत्र में रोज़गार सृजन करना है।
भारत में बुनियादी अवसंरचना विकास की चुनौतियाँ क्या हैं?
- भौतिक अवसंरचना: भारत को भौतिक अवसंरचना के निर्माण में भूमि अधिग्रहण सहित कई महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें अक्सर जटिल पुनर्वास और मुआवजे के मुद्दे शामिल होते हैं।
- इसके अतिरिक्त, सीमित सरकारी संसाधनों तथा आर्थिक एवं नियामक बाधाओं के कारण निजी निवेश में बाधा उत्पन्न होने के कारण ऐसी बड़े पैमाने की परियोजनाओं का वित्तपोषण कठिन है।
- इसके अलावा, जटिल बुनियादी अवसंरचना के विकास के लिये आवश्यक प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता का भी अभाव है।
- राजनीतिक और विनियामक जोखिम: इसमें परियोजना चक्र के दौरान आवश्यक विभिन्न अनुमोदन, सामुदायिक विरोध, विनियमों में परिवर्तन और अनुबंध शर्तों का उल्लंघन शामिल हैं।
- भारत में, संविदात्मक समझौतों के तहत सरकारी भुगतान से इंकार करने से भविष्य के निवेश निर्णयों पर असर पड़ने की संभावना देखी जाती है।
- भौगोलिक चुनौतियाँ: भारत की विविध स्थलाकृति जिसमें पहाड़, नदियाँ और तटीय क्षेत्र शामिल हैं, अद्वितीय इंजीनियरिंग चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं। इसके अतिरिक्त, चक्रवात और बाढ़ जैसी चरम मौसम की स्थितियाँ परियोजनाओं को बाधित कर सकती हैं तथा लागत बढ़ा सकती हैं।
- भ्रष्टाचार और अकुशलता: नौकरशाही की लालफीताशाही, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी अक्सर परियोजनाओं में देरी, लागत में वृद्धि तथा परियोजनाओं की खराब गुणवत्ता का कारण बनती है।
- नीतिगत असंगतियाँ: परस्पर विरोधी नीतियाँ और विनियमन अक्सर निवेशकों व डेवलपर्स के लिये अनिश्चित वातावरण बनाते हैं, जिससे निजी भागीदारी हतोत्साहित होती है।
- डिजिटल डिवाइड: भारत को अपनी डिजिटल बुनियादी अवसंरचना को विकसित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और इंटरनेट तक सीमित पहुँच के कारण डिजिटल डिवाइड काफी अधिक है।
- प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग से साइबर सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ भी उत्पन्न होती हैं, जिसके लिये मज़बूत विनियमन और बुनियादी अवसंरचना की आवश्यकता होती है।
- इसके अतिरिक्त, डिजिटल अवसंरचना क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के बीच मानकीकरण और समन्वय का अभाव उपयोगकर्त्ता के अनुभव को बाधित कर सकता है साथ ही विकास एवं नवाचार को बाधित कर सकता है।
भारत में बुनियादी अवसंरचना विकास हेतु क्या कदम उठाए जा सकते हैं?
- सामाजिक बुनियादी अवसंरचना में निवेश:
- शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे सामाजिक बुनियादी अवसंरचना में निवेश से कार्यबल की उत्पादकता बढ़ सकती है, मृत्यु दर एवं कुपोषण की दर कम हो सकती है, सामाजिक गतिशीलता बढ़ सकती है तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।
- ये निवेश अधिक मज़बूत, अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था और समग्र विकास को समर्थन प्रदान करते हैं।
- शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे सामाजिक बुनियादी अवसंरचना में निवेश से कार्यबल की उत्पादकता बढ़ सकती है, मृत्यु दर एवं कुपोषण की दर कम हो सकती है, सामाजिक गतिशीलता बढ़ सकती है तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) में वृद्धि:
- सरकार बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण, डिज़ाइन, निर्माण और संचालन के लिये निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी कर सकती है।
- बेहतर परियोजना नियोजन और कार्यान्वयन:
- सरकार परियोजना नियोजन एवं कार्यान्वयन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजनाएँ समय पर और बजट के भीतर पूरी हो जाएं।
- नवीन वित्तपोषण समाधानों का कार्यान्वयन:
- सरकार बुनियादी अवसंरचना के विकास के लिये अतिरिक्त धन जुटाने हेतु बुनियादी अवसंरचना बाॅण्ड जैसे नवीन वित्तपोषण समाधानों पर विचार कर सकती है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को प्रोत्साहित करना:
- सरकार नियमों को आसान बना सकती है और बुनियादी अवसंरचना के विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिये अनुकूल वातावरण प्रदान कर सकती है।
- मानव पूंजी का निर्माण:
- बुनियादी अवसंरचना के विकास को आगे बढ़ाने के लिये सरकार को रोज़गार प्रशिक्षण और प्रशिक्षुता में निवेश के माध्यम से मानव पूंजी के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करनी चाहिये, बुनियादी अवसंरचना के अनुसंधान एवं नवाचार का समर्थन करना चाहिये तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिये। इन पहलों का समर्थन करने वाली प्रमुख योजनाओं में स्किल इंडिया, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) शामिल हैं।
- प्रभावी विनियमन:
- सरकार बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी नियम स्थापित और लागू कर सकती है।
- विनियमन सामग्री की गुणवत्ता और कार्यकुशलता के लिये मानक स्थापित कर सकते हैं। वे परियोजना में शामिल जनता और श्रमिकों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये अग्नि सुरक्षा, निकासी योजनाओं एवं पहुँच मानकों सहित सुरक्षा आवश्यकताओं को भी अनिवार्य कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र निरीक्षण और परीक्षण से बुनियादी अवसंरचना के उपयोग में आने से पहले किसी भी समस्या की पहचान करने तथा उसका समाधान करने में सहायता मिल सकती है।
- सरकार बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी नियम स्थापित और लागू कर सकती है।
|
दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में बुनियादी अवसंरचना के विकास में क्या बाधाएँ हैं और इसके समाधान के लिये क्या कदम उठाए जा सकते हैं? |
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्स:प्रश्न 1. 'राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढाँचा कोष' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017)
नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (d) प्रश्न 2. भारत में ‘पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर’ पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? (2020) (a) डिजिटल सुरक्षा अवसंरचना उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न. अधिक तीव्र और समावेशी आर्थिक विकास के लिये बुनियादी अवसंरचना में निवेश आवश्यक है।” भारत के अनुभव के आलोक में चर्चा कीजिये। (2021) |

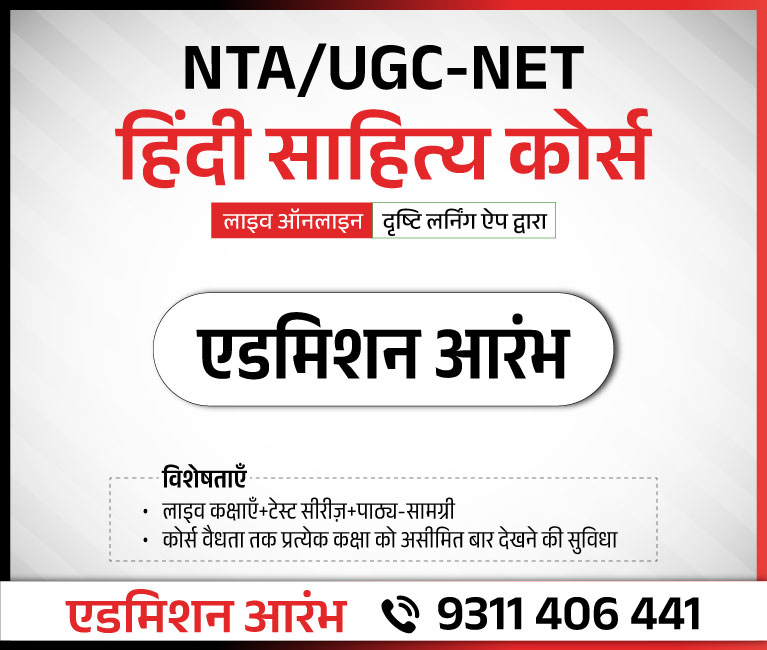
शासन व्यवस्था
MCD एल्डरमैन को मनोनीत करने का LG का अधिकार
प्रिलिम्स के लिये:लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG), एल्डरमैन, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957, स्थानीय सरकार, वार्ड समिति, स्थायी समिति, अनुच्छेद 239AA, मंत्रिपरिषद, 69वाँ संशोधन अधिनियम, 1991, उद्देश्यपूर्ण निर्माण, संघवाद मेन्स के लिये:नई दिल्ली का शासन मॉडल और निर्वाचित विधानसभा तथा LG के बीच सत्ता का संघर्ष। |
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
चर्चा में क्यों?
सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने कहा कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद से परामर्श किये बिना दिल्ली नगर निगम (MCD) में "एल्डरमैन" को नामित कर सकते हैं।
MCD एल्डरमैन के नामांकन पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया?
- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (DMC अधिनियम) की धारा 3, दिल्ली के LG को मंत्रिपरिषद से परामर्श किये बिना एल्डरमैन को नामित करने की “स्पष्ट” शक्ति प्रदान करती है।
- अपना निर्णय देने के लिये सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ 2023 के पाँच न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय पर भरोसा किया।
- वर्ष 2023 में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जब बात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की हो तो संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार होगा।
- इस मामले में 'स्थानीय सरकार' के संबंध में कानून बनाना शामिल होगा, जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है और DMC अधिनियम 1957 से संबंधित है।
एल्डरमैन के नामांकन में क्या मुद्दे थे?
- संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239AA में यह प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री को विधानसभा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों में उपराज्यपाल को “सहायता तथा सलाह” देनी चाहिये, सिवाय तब जब उपराज्यपाल को कानून के अनुसार विवेकानुसार कार्य करना हो।
- दिल्ली विधानसभा को 'सार्वजनिक व्यवस्था', 'पुलिस' और 'भूमि' को छोड़कर अधिकांश विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है।
- एल्डरमैन नामांकन: 3 जनवरी, 2023 को दिल्ली LG ने DMC अधिनियम, 1957 की धारा 3 के तहत 10 एल्डरमैन नामित किये।
- कानूनी चुनौती: दिल्ली सरकार ने नामांकन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।
- दिल्ली सरकार ने दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ, 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि LG को राज्य और समवर्ती सूची के तहत मामलों के लिये मंत्रिपरिषद की सहायता तथा सलाह का पालन करना चाहिये।
- LG का तर्क: दिल्ली LG ने तर्क दिया कि DMC अधिनियम, 1957 उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना एल्डरमैन को नामित करने की शक्ति प्रदान करता है।
MCD में एल्डरमैन का पद क्या है?
- एल्डरमैन के बारे में: एल्डरमैन किसी नगर परिषद या नगर निकाय के सदस्य को संदर्भित करता है।
- यह मूल रूप से एक कबीले या जनजाति के बुजुर्गों को संदर्भित करता था और जल्द ही यह राजा के वाइसराय के लिये एक शब्द बन गया। बाद में यह एक अधिक विशिष्ट शीर्षक "एक काउंटी के मुख्य मजिस्ट्रेट" को दर्शाता है, जिसमें नागरिक तथा सैन्य दोनों कर्तव्य होते हैं।
- एल्डरमैन से नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव की अपेक्षा की जाती है, जिनका कार्य सार्वजनिक महत्त्व के निर्णय लेने में सदन की सहायता करना होता है।
- एल्डरमैन की भूमिका: दिल्ली नगर निगम (DMC) अधिनियम, 1957 के तहत दिल्ली को 12 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में एक 'वार्ड समिति' है जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधि और मनोनीत एल्डरमैन शामिल हैं।
- नामांकन: दिल्ली के उपराज्यपाल 10 एल्डरमैन को नामांकित कर सकते हैं जिनकी आयु कम-से-कम 25 वर्ष हो तथा जिन्हें नगरपालिका प्रशासन में अनुभव हो।
- मतदान का अधिकार: एल्डरमैन MCD की बैठकों में मतदान नहीं करते हैं, लेकिन वार्ड समितियों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहाँ वे मतदान कर सकते हैं और MCD स्थायी समिति के चुनाव में खड़े हो सकते हैं।
- स्थायी समिति: यह समिति, जिसमें एल्डरमैन शामिल हैं, MCD के कार्यों का प्रबंधन करती है और 5 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंध, बजट संशोधन और अधिकारियों की नियुक्ति जैसे निर्णयों के लिये आवश्यक है।
- एल्डरमैन के बिना, स्थायी समिति का गठन नहीं किया जा सकता है, जिससे MCD के प्रमुख कार्य रुक जाते हैं।
दिल्ली का शासन मॉडल क्या है?
- 69वें संशोधन अधिनियम, 1991 ने अनुच्छेद 239AA जोड़ा, जिसने दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) कर दिया, जिसका प्रशासन LG द्वारा किया जाएगा, जो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है।
- 'सहायता और सलाह' नियम केवल उन मामलों पर लागू होता है, जहाँ दिल्ली विधानसभा के पास अधिकार है, जिसमें राज्य और समवर्ती सूची के विषय शामिल हैं। यह सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि पर लागू नहीं होता है।
- साथ ही, अनुच्छेद 239AA, LG को मंत्रिपरिषद के साथ 'किसी भी मामले' पर मतभेद को राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार देता है।
- दिल्ली के शासन मॉडल पर न्यायपालिका की राय: दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ, 2018 में, सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिये।
- उद्देश्यपूर्ण निर्माण: न्यायालय ने उद्देश्यपूर्ण निर्माण के नियम का उपयोग करते हुए कहा कि 69वें संशोधन अधिनियम, 1991 के पीछे के उद्देश्य अनुच्छेद 239AA की व्याख्या का मार्गदर्शन करेंगे।
- इसका अर्थ है कि अनुच्छेद 239AA संघवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों को शामिल करता है, जो दिल्ली को अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में एक विशिष्ट दर्जा देता है।
- LG को सहायता और सलाह पर कार्य करना होगा: न्यायालय ने घोषणा की कि LG मंत्रिपरिषद की “सहायता और सलाह” से बंधे हैं, यह देखते हुए कि दिल्ली विधानसभा के पास समवर्ती सूची में शामिल सभी विषयों और राज्य सूची में तीन बहिष्कृत विषयों (सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि) को छोड़कर सभी पर कानून बनाने की शक्ति है।
- LG को मंत्रिपरिषद की “सहायता और सलाह” पर कार्य करना चाहिए, सिवाय इसके कि जब वह किसी मामले को अंतिम निर्णय के लिये राष्ट्रपति के पास भेजता है।
- कोई भी मामला प्रत्येक मामला नहीं होता: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि LG केवल असामान्य मामलों में ही किसी मामले को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, न कि मंत्रिपरिषद के साथ प्रत्येक असहमति के लिये।
- LG एक सुविधाकर्त्ता के रूप में: LG निर्वाचित मंत्रिपरिषद के विरोधी के रूप में कार्य करने के बजाय एक समन्वयक के रूप में कार्य करेगा।
- नई दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता: साथ ही, न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि संवैधानिक योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता।
- उद्देश्यपूर्ण निर्माण: न्यायालय ने उद्देश्यपूर्ण निर्माण के नियम का उपयोग करते हुए कहा कि 69वें संशोधन अधिनियम, 1991 के पीछे के उद्देश्य अनुच्छेद 239AA की व्याख्या का मार्गदर्शन करेंगे।
निष्कर्ष
सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि दिल्ली का शासन संवैधानिक विश्वास और सहयोग पर निर्भर करता है। सहायकता के सिद्धांत के लिये सुव्यवस्थित स्थानीय सरकारों की आवश्यकता होती है, इसलिये भारत को जकार्ता, सियोल, लंदन व पेरिस जैसे वैश्विक मेगासिटीज़ के उदाहरण का अनुसरण करते हुए शहर की सरकारों को अधिक शक्ति प्रदान करनी चाहिये।
|
दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के मुख्य बिंदु क्या हैं और किन मुद्दों ने दिल्ली के निर्वाचित प्रतिनिधियों और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच संघर्ष का कारण बना है? स्पष्ट कीजिये। |
69वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1991
UPSC यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)मेन्सप्रश्न. 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के उन अत्यावश्यक तत्त्वों और विषमताओं, यदि कोई हों, पर चर्चा कीजिये, जिन्होंने दिल्ली के प्रशासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों और उप-राज्यपाल के बीच हाल में समाचारों में आए मतभेदों को उत्पन्न कर दिया है। क्या आपके विचार में इससे भारतीय परिसंघीय राजनीति के प्रकार्यण में एक नई प्रवृत्ति का उदय होगा? (2016) प्रश्न. क्या उच्चतम न्यायालय का निर्णय (जुलाई 2018) दिल्ली के उप-राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच राजनैतिक कशमकश को निपटा सकता है? परीक्षण कीजिये। (2018) |
भारतीय राजव्यवस्था
वक्फ अधिनियम, 1995 में प्रस्तावित संशोधन
प्रिलिम्स के लिये:वक्फ अधिनियम, 1995, वक्फ बोर्ड, केंद्रीय वक्फ परिषद (CWC), धर्म की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक, संपत्ति की बंदोबस्ती, शैक्षणिक संस्थान मेन्स के लिये:वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 और संबंधित चिंताएँ |
स्रोत : बिजनेस स्टैण्डर्ड
चर्चा में क्यों ?
संसद वक्फ बोर्ड के कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लक्ष्य के साथ वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करने के लिये वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करने वाली है।
- यह वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्ति को कम करने के लिये वक्फ अधिनियम, 1995 के कुछ प्रावधानों को हटाने का प्रयास करता है, जो वर्तमान में उन्हें आवश्यक जाँच के बिना किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने की अनुमति देता है।
वक्फ अधिनियम (संशोधन विधेयक), 2024 में मुख्य संशोधन क्या हैं?
- पारदर्शिता: विधेयक में मौजूदा वक्फ अधिनियम में लगभग 40 संशोधनों की रूपरेखा दी गई है, जिसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये वक्फ बोर्डों को सभी संपत्ति दावों हेतु अनिवार्य सत्यापन से गुजरना होगा।
- लिंग विविधता: वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 9 और 14 में संशोधन किया जाएगा ताकि वक्फ बोर्ड की संरचना और कार्यप्रणाली को संशोधित किया जा सके, जिसमें महिला प्रतिनिधियों को शामिल करना भी शामिल है।
- संशोधित सत्यापन प्रक्रियाएँ: विवादों को सुलझाने और दुरुपयोग को रोकने के लिये वक्फ संपत्तियों के लिए नई सत्यापन प्रक्रियाएँ शुरू की जाएंगी, तथा ज़िला मजिस्ट्रेट संभवतः इन संपत्तियों की देख-रेख करेंगे।
- सीमित शक्ति: ये संशोधन वक्फ बोर्डों (Waqf Boards) की अनियंत्रित शक्तियों के बारे में चिंताओं का जवाब देते हैं, जिसके कारण व्यापक भूमि पर वक्फ का दावा किया जा रहा है, जिससे विवाद और दुरुपयोग के दावे हो रहे हैं।
- उदाहरण के लिये सितंबर 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने पूरे थिरुचेंदुरई गाँव पर दावा किया, जो मुख्य रूप से हिंदू बहुल है।
वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन की आलोचना क्यों की गई?
- शक्तियों में कमी: यह वक्फ बोर्डों के अधिकारों को सीमित करता है, जिससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन की उनकी क्षमता प्रभावित होती है।
- अल्पसंख्यक अधिकारों की चिंता: आलोचकों को चिंता है कि इससे उन मुस्लिम समुदायों के हितों को नुकसान पहुँच सकता है जो इन संपत्तियों का उपयोग धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिये करते हैं।
- सरकारी नियंत्रण में वृद्धि: ज़िला मजिस्ट्रेटों की भागीदारी और अधिक निगरानी से नौकरशाही का अत्यधिक हस्तक्षेप हो सकता है।
- धार्मिक स्वतंत्रता में बाधा: वक्फ संपत्तियों की देखरेख में ज़िला मजिस्ट्रेटों और अन्य सरकारी अधिकारियों की भागीदारी को धार्मिक स्वायत्तता पर अतिक्रमण के रूप में देखा जा सकता है।
- संभावित विवाद: ज़िला मजिस्ट्रेटों की भागीदारी जैसी नई सत्यापन प्रक्रियाएँ अधिक विवाद और जटिलताएँ उत्पन्न कर सकती हैं।
वक्फ अधिनियम, 1995 क्या है?
- पृष्ठभूमि: वक्फ अधिनियम को पहली बार वर्ष 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया था।
- बाद में इसे निरस्त कर दिया गया और वर्ष 1995 में एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया गया, जिसने वक्फ बोर्डों को और अधिक अधिकार दिये गए।
- वर्ष 2013 में, अधिनियम में संशोधन करके वक्फ बोर्ड को संपत्ति को 'वक्फ संपत्ति' के रूप में नामित करने के लिये व्यापक अधिकार दिये गए।
- वक्फ: यह मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिये चल या अचल संपत्तियों का स्थायी समर्पण है।
- इसका तात्पर्य है कि मुस्लिम द्वारा संपत्ति, चाहे वह चल हो या अचल, मूर्त या अमूर्त, ईश्वर को इस आधार पर दान करना ताकि अंतरण से जरूरतमंदों को लाभ हो सके।
- वक्फ से होने वाली आय आमतौर पर शैक्षणिक संस्थानों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों और आश्रय गृहों को निधि देती है।
- भारत में वक्फ को वक्फ अधिनियम, 1995 द्वारा विनियमित किया जाता है।
- वक्फ का प्रबंधन:
- एक सर्वेक्षण आयुक्त स्थानीय जाँच करके, गवाहों को बुलाकर और सार्वजनिक दस्तावेज़ों की मांग करके वक्फ के रूप में घोषित सभी संपत्तियों को सूचीबद्ध करता है।
- वक्फ का प्रबंधन एक मुतवली/मुतवल्ली द्वारा किया जाता है, जो पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है।
- भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत स्थापित ट्रस्ट जो व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं और बोर्ड द्वारा जिनका विघटन किया जा सकता है, के विपरीत वक्फ के उद्देश्य विशेष रूप से धार्मिक एवं धर्मार्थ उपयोगों के लिये होते हैं तथा इन्हें स्थायी माना जाता है।
- वक्फ या तो सार्वजनिक (जो धर्मार्थ उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं) हो सकते हैं, या निजी (जो संपत्ति के स्वामी के प्रत्यक्ष वंशजों को लाभ पहुँचाते हैं) हो सकते हैं।
- वक्फ के गठन के लिये व्यक्ति का शांत चित्त का होना चाहिये और संपत्ति का वैध स्वामित्व होना चाहिये। दिलचस्प बात यह है कि वक्फ के संस्थापक, जिन्हें वक्फ के रूप में जाना जाता है, को मुस्लिम होने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि वे इस्लामी सिद्धांतों में विश्वास करते हैं।
- वक्फ बोर्ड:
- वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई है जो संपत्ति अर्जित करने, उसे रखने और हस्तांतरित करने में सक्षम है। यह मुकदमा करने और न्यायालय में मुकदमा किये जाने दोनों में सक्षम है।
- यह वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है, खोई हुई संपत्तियों को वापस प्राप्त करता है और बिक्री, उपहार, बंधक ऋण या गिरवी कर्ज, विनिमय या पट्टे के माध्यम से अचल वक्फ संपत्तियों के हस्तांतरण को मंजूरी देता है, जिसमें बोर्ड के कम से कम दो-तिहाई सदस्य लेनदेन के पक्ष में मतदान करते हैं।
- वर्ष 1964 में स्थापित केंद्रीय वक्फ परिषद (CWC) पूरे भारत में राज्य स्तरीय वक्फ बोर्डों की देखरेख और सलाह देती है।
- वक्फ संपत्तियाँ: वक्फ बोर्ड को भारत में रेलवे और रक्षा विभाग के बाद तीसरा सबसे बड़ा भूमिधारक कहा जाता है।
- वर्तमान में 8 लाख एकड़ में फैली 8,72,292 पंजीकृत वक्फ संपत्तियाँ हैं। इन संपत्तियों से 200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है।
- एक बार जब किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाता है तो वह अहस्तांतरणीय हो जाती है और ईश्वर के प्रति एक धर्मार्थ कार्य के रूप में स्थायी रूप से सुरक्षित रहती है, जो अनिवार्य रूप से ईश्वर को स्वामित्व हस्तांतरित कर देती है।
निष्कर्ष
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ाता है। शासन, जवाबदेही और संपत्ति के उपयोग में सुधार करके यह वक्फ बोर्डों को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि लाभ लक्षित समुदायों तक पहुँचे। इस संशोधन का उद्देश्य सामाजिक कल्याण एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए वक्फ की अखंडता को बनाए रखना है, जिससे संभावित रूप से अधिक विश्वास और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा मिलेगा।
|
दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. धार्मिक अल्पसंख्यकों के मामलों के प्रबंधन में राज्य के हस्तक्षेप का डर प्रतीत होता है। क्या आप इससे सहमत हैं? वक्फ अधिनियम, 1995 में प्रस्तावित संशोधनों के आलोक में चर्चा कीजिये। |
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)मेन्स:प्रश्न. धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल से कैसे भिन्न है? चर्चा कीजिये। (2018) |





-min.jpg)