छत्तीसगढ़ Switch to English
प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों का उद्घाटन किया
चर्चा में क्यों?
प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, निर्माण कार्य का शुभारंभ किया और लोकार्पण किया।
मुख्य बिंदु
- विकास पहल:
- प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की प्रगति में तेज़ी लाने के उद्देश्य से कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की।
- इन पहलों में वंचितों के लिये आवास, शिक्षा, परिवहन और ऊर्जा क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढाँचे और बेहतर कनेक्टिविटी शामिल हैं।
- इन परियोजनाओं से न केवल जन सुविधाएँ बढ़ेंगी बल्कि रोज़गार के अवसर भी सृजित होंगे।
- उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत तीन लाख गरीब परिवारों के मकान के सपने पूरे होने पर प्रकाश डाला।
- किसानों को समर्थन देना और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करना:
- उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों और महिलाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई तथा पिछले वादों को पूरा करना सुनिश्चित किया।
- उन्होंने धान किसानों को दो वर्षों के लंबित बोनस के भुगतान तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के साथ धान की खरीद की घोषणा की।
- छत्तीसगढ़ की 25वीं वर्षगाँठ: "अटल निर्माण वर्ष"
- छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करते ही प्रधानमंत्री ने 2025 को "अटल निर्माण वर्ष" के रूप में घोषित किया, जो अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को समर्पित होगा।
- उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि नव-प्रवर्तित बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ राज्य की समृद्धि के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुरूप हैं।
- जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे का विस्तार:
- उन्होंने दूरदराज़ के आदिवासी क्षेत्रों में संपर्क, परिवहन और सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ाने में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला।
- उन्होंने नई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया और छत्तीसगढ़ के रेल नेटवर्क के पूर्ण विद्युतीकरण का शुभारंभ किया।
- उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक सेवाओं को वंचित समुदायों तक पहुँचाने के लिये सरकार की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया।
- छत्तीसगढ़ के ऊर्जा क्षेत्र को मज़बूत बनाना:
- प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड की सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण-III (9,790 करोड़ रुपए) और छत्तीसगढ़ की पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना (15,800 करोड़ रुपए) की आधारशिला रखी।
- उन्होंने पावरग्रिड (560 करोड़ रुपए) के तहत तीन विद्युत पारेषण परियोजनाएँ राष्ट्र को समर्पित कीं।
- इन पहलों का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करना है।
- नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ईंधन पहल को आगे बढ़ाना:
- प्रधानमंत्री ने कई ज़िलों में भारत पेट्रोलियम की सिटी गैस वितरण परियोजना (1,285 करोड़ रुपए) का शुभारंभ किया।
- उन्होंने ईंधन आपूर्ति दक्षता में सुधार के लिये हिंदुस्तान पेट्रोलियम की विशाख-रायपुर पाइपलाइन परियोजना (2,210 करोड़ रुपए) का भी उद्घाटन किया।
- उन्होंने 'प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा मुफ्त बिजली योजना' की शुरुआत की, जिससे घरों में सौर ऊर्जा उत्पन्न करने और बिजली की लागत को खत्म करने की सुविधा मिली।
- सड़क और रेलवे संपर्क बढ़ाना:
- प्रधानमंत्री ने सात रेलवे परियोजनाओं (108 किमी) की आधारशिला रखी और तीन पूर्ण हो चुकी रेलवे परियोजनाओं (111 किमी) का उद्घाटन किया, जिनकी कुल लागत 2,690 करोड़ रुपए है।
- उन्होंने जनजातीय और औद्योगिक क्षेत्रों में सम्पर्क सुधारने तथा आर्थिक और सामाजिक एकीकरण को मज़बूत करने के लिये कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया।
- शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना:
- प्रधानमंत्री ने 29 ज़िलों में 130 पीएम श्री स्कूलों का उद्घाटन किया, जिससे शिक्षा के बुनियादी ढाँचे में वृद्धि हुई।
- उन्होंने शिक्षा कार्यक्रमों की वास्तविक समय पर निगरानी के लिये रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) का शुभारंभ किया।
- ऐतिहासिक उपेक्षा को संबोधित करना और नक्सलवाद का सामना करना:
- उन्होंने आदिवासी समुदायों को समर्थन देने के लिये स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत और पीएम जन औषधि केंद्र जैसी पहल पर ज़ोर दिया।
- उन्होंने 7,000 आदिवासी गाँवों के उत्थान के लिये 80,000 करोड़ रुपए आवंटित करते हुए "धरती आबा जनजाति उत्कर्ष अभियान" की घोषणा की।
- उन्होंने "प्रधानमंत्री जनमन योजना" की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य 2,000 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह बस्तियों में बुनियादी ढाँचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना था।
प्रधानमंत्री जनमन योजना
- परिचय:
- लॉन्च: प्रधानमंत्री जनमन योजना को 15 नवंबर, 2023 को लॉन्च किया गया था, इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
- यह पहल भारत के वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में घोषित प्रधानमंत्री-PVTG विकास मिशन को आगे बढ़ाती है।
- उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य व्यापक विकास हस्तक्षेप प्रदान करके विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है।
- लाभार्थी: इस योजना का लक्ष्य 18 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) के 75 PVTG समुदायों को लाभार्थी बनाना है।
- नोडल मंत्रालय: जनजातीय कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय है जो 9 मंत्रालयों/विभागों और संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से योजना के कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार है।
पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना
- यह पर्याप्त वित्तीय सब्सिडी प्रदान करके और इनस्टॉलेशन में सुविधा सुनिश्चित करके सोलर रूफटॉप सिस्टम को अपनाने को बढ़ावा देने के लिये एक केंद्रीय योजना है।
- उद्देश्य: इसका लक्ष्य भारत में एक करोड़ परिवारों को मुफ्त विद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराना है, जो रूफटॉप सोलर पैनल वाली बिजली इकाइयाँ स्थापित करना चाहते हैं।
- परिवारों को प्रत्येक महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकेगी।
- कार्यान्वयन एजेंसियाँ: योजना का क्रियान्वयन दो स्तरों पर किया जाएगा।
- राष्ट्रीय स्तर: राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (NPIA) द्वारा प्रबंधित।
- राज्य स्तर: राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (SIA) द्वारा प्रबंधित, जो संबंधित राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों की वितरण उपयोगिताएँ (डिस्कॉम) या विद्युत/ऊर्जा विभाग हैं।
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान
- मूल रूप से PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PM-JUGA) नाम से आरंभ हुई यह योजना 63,000 अनुसूचित जनजाति बहुल गाँवों में मौज़ूदा योजनाओं को लागू करने के लिये एक व्यापक योजना है।
- धरती आबा का तात्पर्य झारखंड के 19वीं सदी के आदिवासी नेता और उपनिवेशवाद विरोधी प्रतीक बिरसा मुंडा से है।
- इस पहल का उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न 17 मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में महत्त्वपूर्ण अंतराल को दूर करना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)
- वर्ष 2016 में शुरू की गई PMAY-G का उद्देश्य समाज के सबसे गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराना है।
- यह सुनिश्चित करने के लिये कि सहायता सबसे अधिक पात्र लोगों तक पहुँचे, प्राप्तकर्त्ताओं का चयन एक कठोर तीन-चरणीय सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिसमें सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011, ग्राम सभा की मंजूरी और जियो-टैगिंग शामिल है।
- PMAY-G के अंतर्गत लाभार्थियों को प्राप्त होगा:
- वित्तीय सहायता: मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपए तथा पूर्वोत्तर राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों सहित पहाड़ी राज्यों में 1.30 लाख रुपए।
- शौचालयों हेतु अतिरिक्त सहायता: स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना या किसी अन्य समर्पित वित्त पोषण स्रोत जैसी योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिये 12,000 रुपए।
- रोज़गार सहायता: आवास निर्माण के लिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के माध्यम से लाभार्थियों के लिये 90/95 व्यक्ति-दिवस अकुशल मज़दूरी रोज़गार का अनिवार्य प्रावधान।
- बुनियादी सुविधाएँ: प्रासंगिक योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से पानी, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) और बिजली कनेक्शन तक पहुँच।
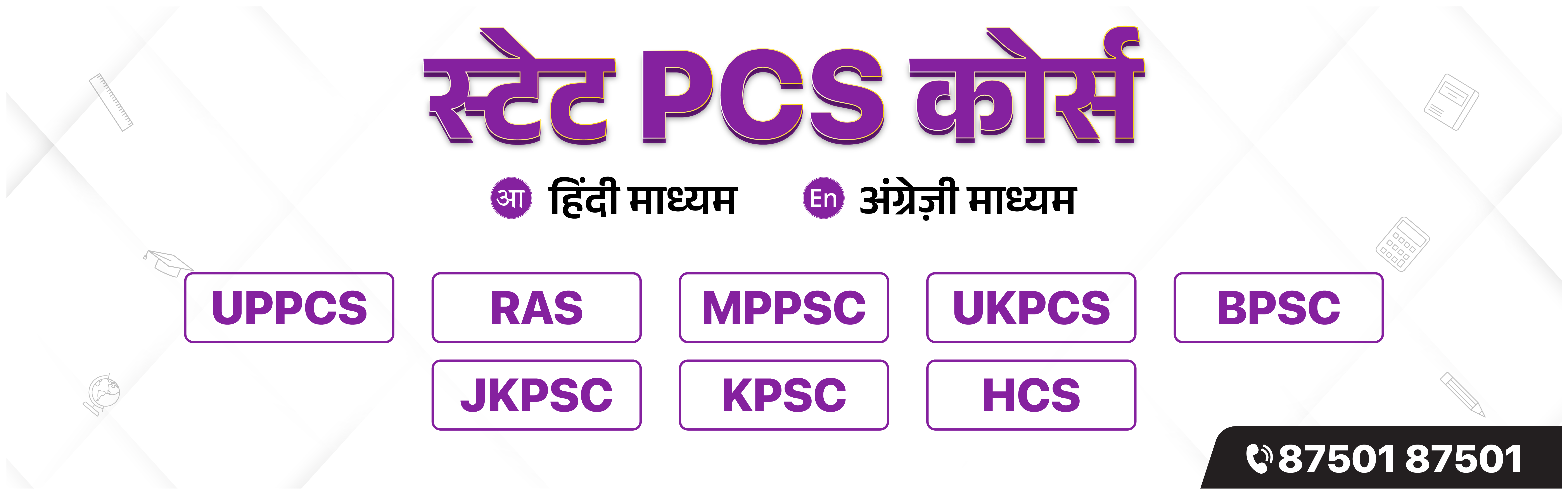
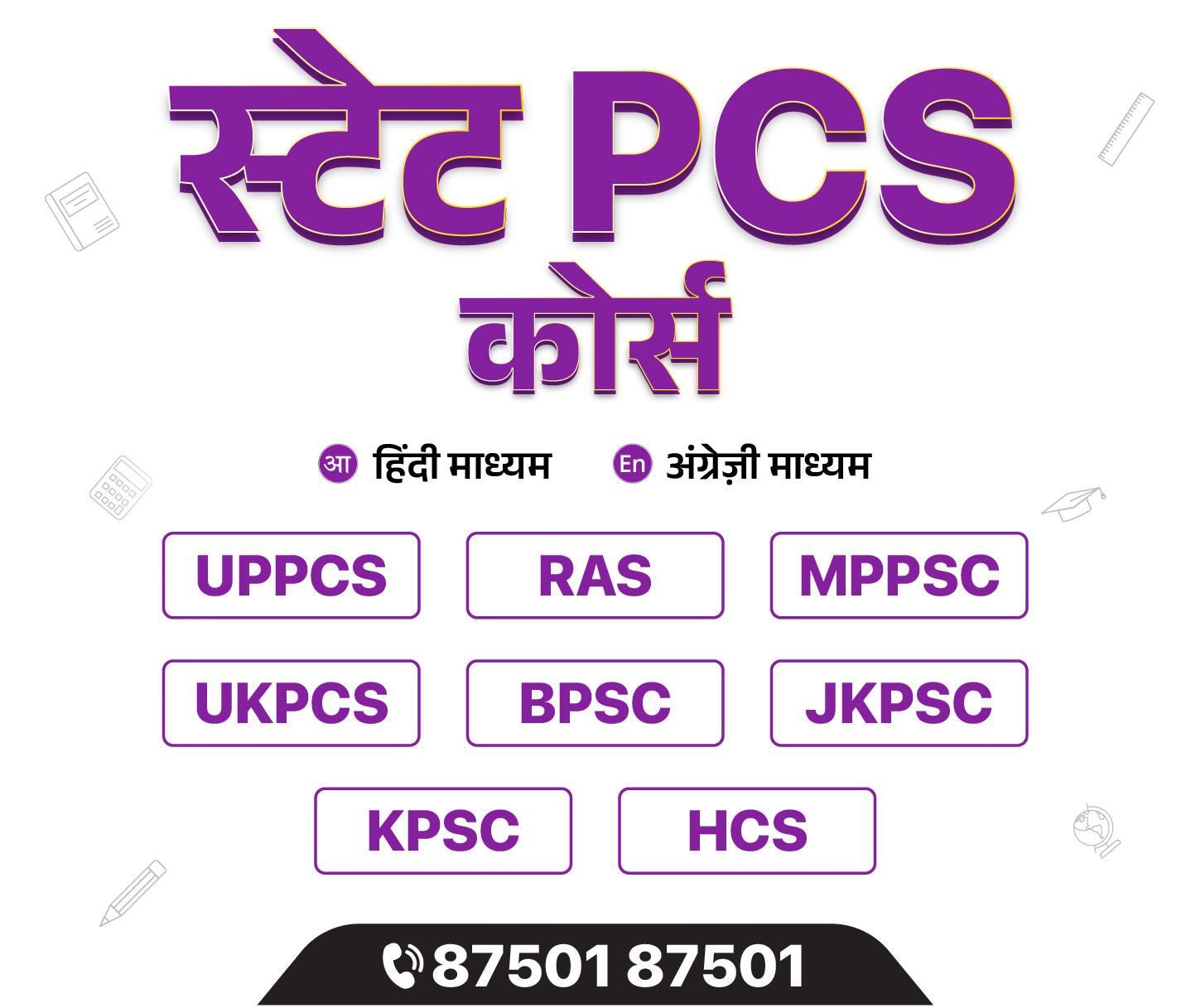
छत्तीसगढ़ Switch to English
वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित ज़िले
चर्चा में क्यों?
केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित ज़िलों की संख्या 12 से घटकर छह हो गई है, जो माओवाद मुक्त राष्ट्र की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। उन्होंने 31 मार्च 2026 तक देश से माओवाद को खत्म करने की सरकार की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की।
मुख्य बिंदु
- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ज़िलों में कमी:
- वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित ज़िलों की संख्या 12 से घटकर मात्र 6 रह गई है।
- केंद्र सरकार नक्सलवाद के खिलाफ सख्त रुख और केंद्रित विकास के माध्यम से भारत को सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिये प्रतिबद्ध है।
- तीव्र माओवादी विरोधी अभियान:
- छत्तीसगढ़ में उग्रवाद विरोधी अभियानों में तेज़ी देखी गई है।
- वर्ष 2024 में 219 माओवादियों का सफाया किया गया, जबकि 2023 में 22 और 2022 में 30 माओवादियों का सफाया किया गया, जो आतंकवाद विरोधी प्रयासों में तीव्र वृद्धि को दर्शाता है।
- बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागाँव और सुकमा सहित प्रमुख माओवादी गढ़ उग्रवाद का केंद्र बने हुए हैं।
- माओवादियों के ठिकानों और किलेबंदी को ध्वस्त करने के लिये "लाल गलियारे" में हज़ारों सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है।
- सरकार की बहुआयामी रणनीति:
- केंद्र सरकार का लक्ष्य निरंतर सैन्य कार्रवाई और सामाजिक-आर्थिक विकास के माध्यम से 31 मार्च 2026 तक माओवाद का उन्मूलन करना है।
- उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों और अन्य विकासात्मक पहलों सहित बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं।
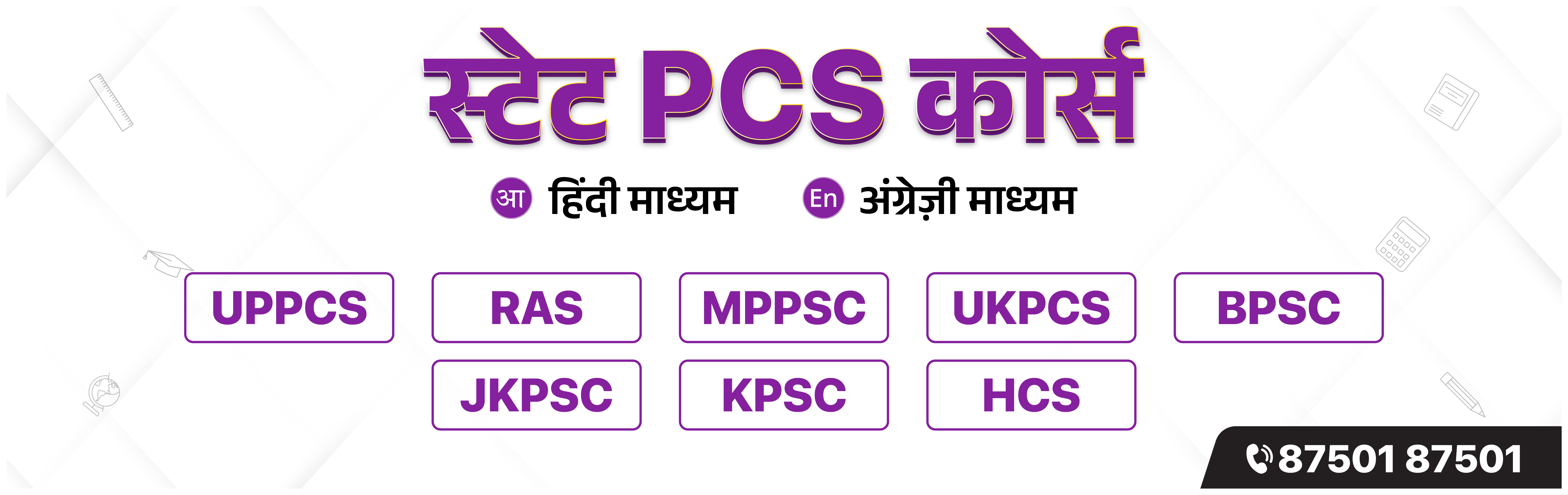
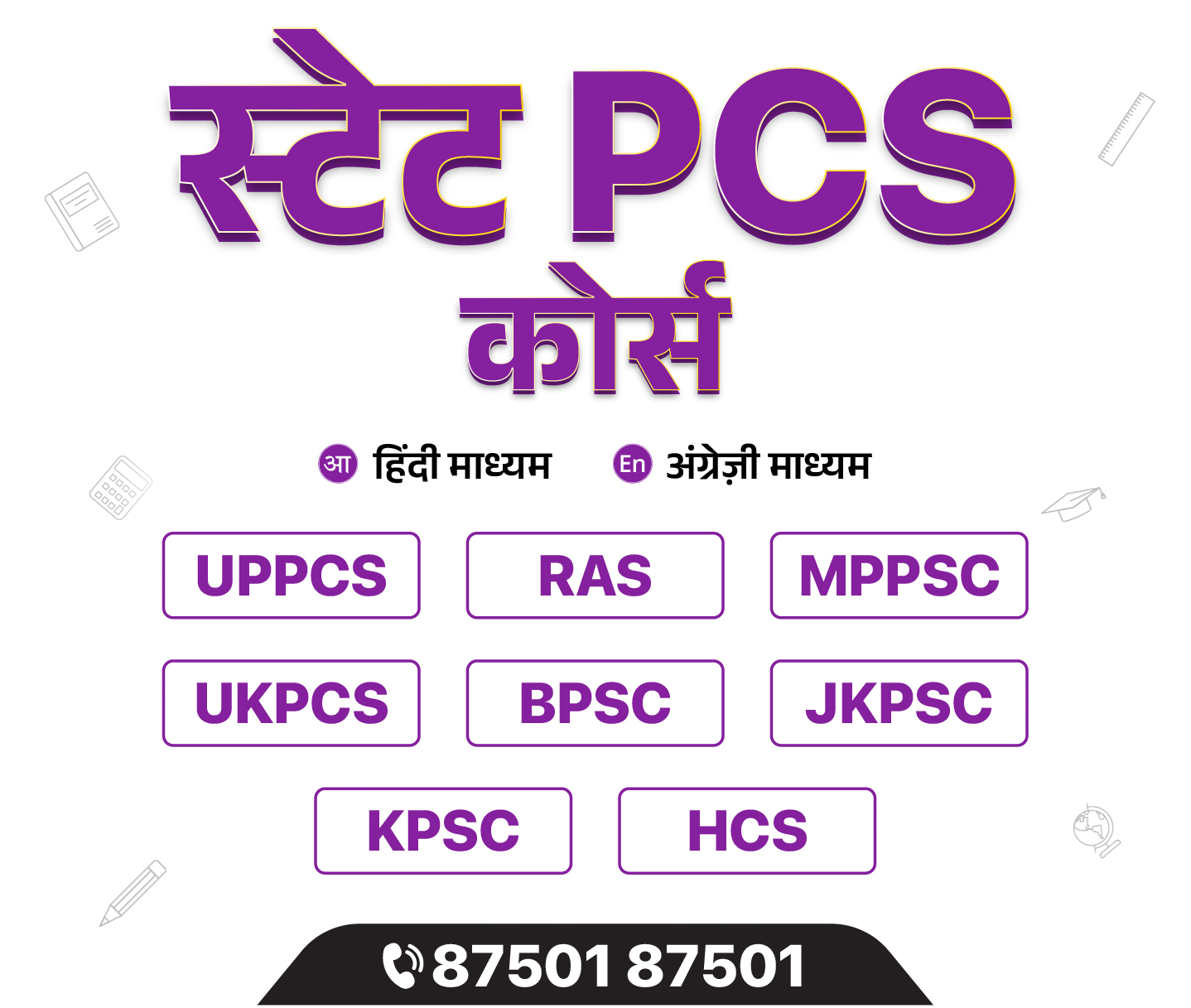
झारखंड Switch to English
झारखंड में NAFLD के लिये अभियान
चर्चा में क्यों?
राँची झारखंड का पहला ज़िला बनने जा रहा है, जो नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) की जाँच और प्रबंधन के लिये बड़े पैमाने पर अभियान लागू करेगा।
मुख्य बिंदु
- उद्देश्य और कार्यान्वयन:
- राँची में राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (NP-NCD) के अंतर्गत NAFLD के लिये झारखंड का पहला बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग और प्रबंधन अभियान शुरू किया जाएगा।
- यह पहल फैटी लीवर रोग के बढ़ते बोझ से निपटने के लिये शीघ्र पहचान, क्षमता निर्माण और स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने पर केंद्रित है।
- शुभारंभ और महत्त्व:
- यह अभियान 19 अप्रैल 2025 को विश्व लिवर दिवस पर शुरू किया जाएगा।
- दो-चरणीय कार्यान्वयन:
- चरण 1 (अप्रैल-जून 2025):
- उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को लक्षित करता है - जो मोटापे, मधुमेह और उच्च रक्तचाप से ग्रस्त हैं।
- इसमें 30,000 सामान्य जनसंख्या सदस्यों की स्क्रीनिंग शामिल है।
- चरण 2 (जुलाई-नवंबर 2025):
- राँची ज़िले में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्कों के लिये स्क्रीनिंग का विस्तार किया गया।
- यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान (ILBS), नई दिल्ली तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
- चरण 1 (अप्रैल-जून 2025):
- मोबाइल स्क्रीनिंग वैन:
- फाइब्रो-स्कैन तकनीक से लैस अत्याधुनिक मोबाइल वैन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क जाँच करेंगी।
- प्रत्येक वैन की लागत 1 करोड़ रुपए है और यह उन्नत लिवर स्क्रीनिंग विधियों के माध्यम से सटीक निदान सुनिश्चित करती है।
- स्वास्थ्य पर प्रभाव और शीघ्र पता लगाने की आवश्यकता:
- राँची में लगभग 50% ओपीडी मरीज लीवर से संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं।
- औसतन प्रतिदिन 25 रोगियों का निदान किया जाता है, जिनमें से पाँच को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता होती है।
- पिछले वर्ष, यकृत रोग से संबंधित पाँच मौतें दर्ज की गईं, जिससे शीघ्र हस्तक्षेप की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ा।
- डाटा संग्रहण और निगरानी:
- स्क्रीनिंग डाटा को एक ट्रैकिंग सिस्टम में तब तक दर्ज किया जाएगा जब तक कि राष्ट्रीय एनसीडी पोर्टल NAFLD-विशिष्ट रिकॉर्ड को एकीकृत नहीं कर देता।
- कार्यक्रम का उद्देश्य रेफरल प्रणाली को मज़बूत करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मरीजों को विशेष चिकित्सा देखभाल प्राप्त हो।
- यह पहल राँची को NAFLD प्रबंधन में अग्रणी बनाती है तथा राष्ट्रव्यापी यकृत रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिये एक उदाहरण स्थापित करती है।
नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग
- परिचय: NAFLD एक ऐसी स्थिति है जिसमें शराब के बिना भी लिवर में वसा का संग्रहण हो जाता है।
- इसमें दो प्रकार शामिल हैं: नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर (NAFL) और नॉन-अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस (NASH)।
- NAFLD के प्रकार
- NAFL: इसमें लिवर में वसा का निर्माण होने के साथ सूजन या क्षति न्यूनतम या शून्य होती है।
- इससे आमतौर पर लिवर संबंधी जटिलताएँ नहीं होती हैं लेकिन यकृत में वृद्धि के साथ असुविधा हो सकती है।
- NASH: इसमें वसा का निर्माण तथा लिवर की सूजन दोनों ही शामिल हैं, जिससे लिवर क्षतिग्रस्त होने के साथ फाइब्रोसिस (ऐसी स्थिति जिसमें लिवर में स्कार ऊतक की अधिकता हो जाती है) एवं संभावित रूप से सिरोसिस (ऐसी स्थिति जिससे लिवर कैंसर के जोखिम में वृद्धि होती है) की समस्या हो सकती है।
- लक्षण और कारण: NAFLD अक्सर लक्षणहीन होता है लेकिन मोटापा, मेटाबोलिक सिंड्रोम (चयापचय संबंधी असामान्यताओं का समूह) एवं टाइप 2 मधुमेह जैसी स्थितियाँ इसके जोखिम को बढ़ा देती हैं।
- निदान: NAFLD का निदान चिकित्सा इतिहास, शारीरिक परीक्षण और NAFL एवं NASH के बीच अंतर करने के लिये रक्त परीक्षण, इमेजिंग तथा यकृत बायोप्सी जैसे परीक्षणों के माध्यम से किया जाता है।
- उपचार: वजन कम करना, NAFLD के प्रबंधन के लिये महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वसा, सूजन एवं लिवर फाइब्रोसिस (ऐसी स्थिति जिसमें लिवर में स्कार ऊतक की अधिकता हो जाती है) की स्थिति को रोका जा सकता है।
- रोकथाम: स्वस्थ आहार और वजन में संतुलन बनाए रखने से NAFLD को रोकने या प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। प्रभावित लोगों के लिये स्वस्थ आहार और वजन घटाने की सलाह दी जाती है।
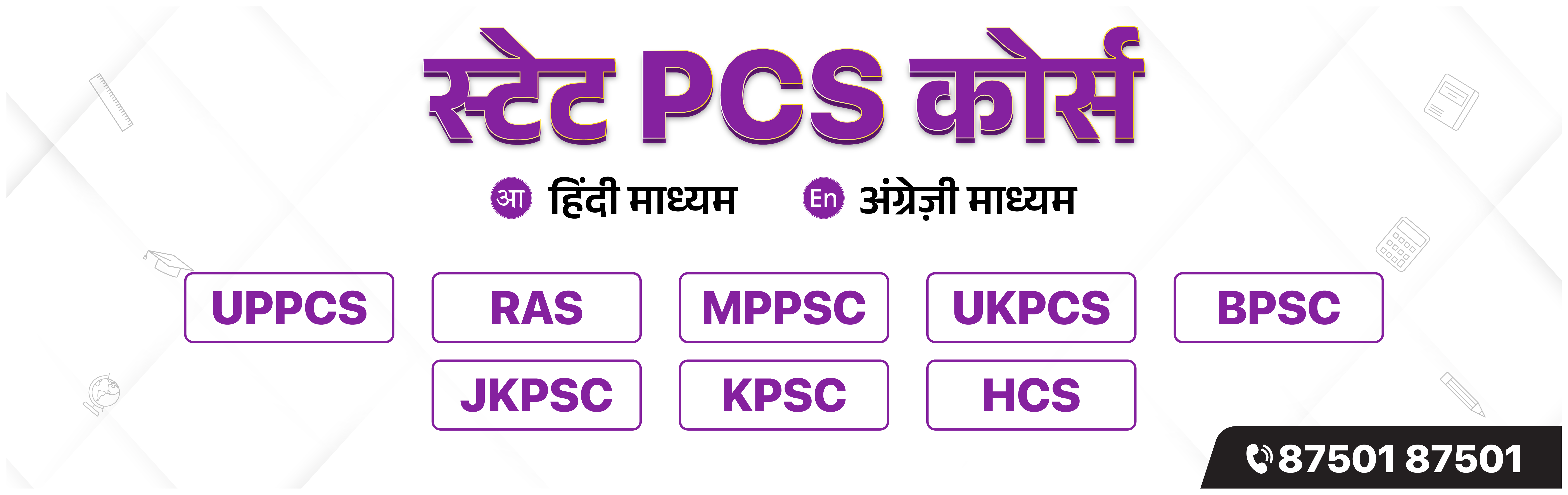

उत्तर प्रदेश Switch to English
टेककृति 2025
चर्चा में क्यों?
- 27 से 30 मार्च, 2025 तक उत्तर प्रदेश के कानपुर में एशिया के सबसे बड़े अंतर-महाविद्यालय तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव ‘टेककृति’ का आयोजन किया गया।
मुख्य बिंदु
- संबोधन और थीम:
- इस उत्सव का उद्घाटन CDS जनरल अनिल चौहान द्वारा किया गया।
- उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों की उन्नति और आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला तथा भविष्य के युद्धों की चुनौती के रूप में साइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम टेक्नोलॉजी और संज्ञानात्मक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया।
- इस वर्ष के महोत्सव का विषय था "पंता रेई" (सब कुछ प्रवाहित होता है)।
- रक्षककृति: रक्षा एक्सपो
- एक विशेष रक्षा प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें भविष्य की सैन्य तकनीकों का प्रदर्शन किया गया।
- इस प्रदर्शनी में AI-आधारित युद्ध प्रणालियाँ, स्वायत्त ड्रोन और स्वदेशी रक्षा नवाचारों को प्रस्तुत किया गया।
- ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में कदम बढ़ाने और विदेशी रक्षा निर्भरता को कम करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पुनः उजागर किया गया।
- टेककृति महोत्सव
- यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर का वार्षिक तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1995 में हुई थी।
- इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में प्रेरित करना है, ताकि वे नई सोच और विचारधारा के साथ आगे बढ़ सकें।
- वर्ष 2000 में, महोत्सव में स्टार्टअप्स, उद्यमशीलता और कार्यशालाओं को भी शामिल किया गया, जिसके परिणामस्वरूप यह महोत्सव एक व्यापक और विविधतापूर्ण तकनीकी उत्सव बन गया।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
- परिचय:
- AI का आशय कंप्यूटर या कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट के ऐसे कार्य करने की क्षमता से है जो आमतौर पर मनुष्यों द्वारा किये जाते हैं क्योंकि ऐसे कार्यों के निष्पादन हेतु मानव बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है।
- हालाँकि अभी ऐसी कोई AI प्रणाली नहीं है, जो एक सामान्य मानव द्वारा किये जा सकने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर सके, हालाँकि कुछ AI मनुष्यों द्वारा किये जाने वाले कुछ विशिष्ट कार्यों को करने में सक्षम हो सकते हैं।
- विशेषताएँ और घटक:
- डीप लर्निंग (DL) तकनीक बड़ी मात्रा में असंरचित डाटा जैसे- टेक्स्ट, चित्र या वीडियो के माध्यम से ऑटोमेटिक लर्निंग को सक्षम बनाती है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता की आदर्श विशेषता इसकी युक्तिसंगत कार्रवाई करने की क्षमता है जिसमें एक विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। मशीन लर्निंग (ML), AI का ही एक प्रकार है।
- डीप लर्निंग (DL) तकनीक बड़ी मात्रा में असंरचित डाटा जैसे- टेक्स्ट, चित्र या वीडियो के माध्यम से ऑटोमेटिक लर्निंग को सक्षम बनाती है।
AI के प्रकार:
|
क्षमताओं के आधार पर |
विवरण |
|
दुर्बल Al या संकीर्ण Al |
इस Al को शतरंज खेलने, चेहरे पहचानने या सिफ़ारिशें करने जैसे विशिष्ट कार्यों के लिये डिज़ाइन किया गया है। उदाहरणों में सिरी, वॉटसन, AlphaGo शामिल हैं। |
|
जनरल Al |
तर्कशक्ति, लर्निंग और प्लानिंग सहित किसी भी बौद्धिक कार्य को करने की क्षमता जो मनुष्य कर सकता है। कोई मौजूदा उदाहरण नहीं है, लेकिन शोधकर्त्ता इस पर कार्य कर रहे हैं। |
|
सुपर Al |
काल्पनिक Al जो मानव बुद्धि से बढ़कर है, रचनात्मकता, आत्म-जागरूकता और भावना जैसी संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले कार्यों में उत्कृष्ट है। कोई वर्तमान उदाहरण नहीं, केवल भविष्य की संभावनाएँ। |

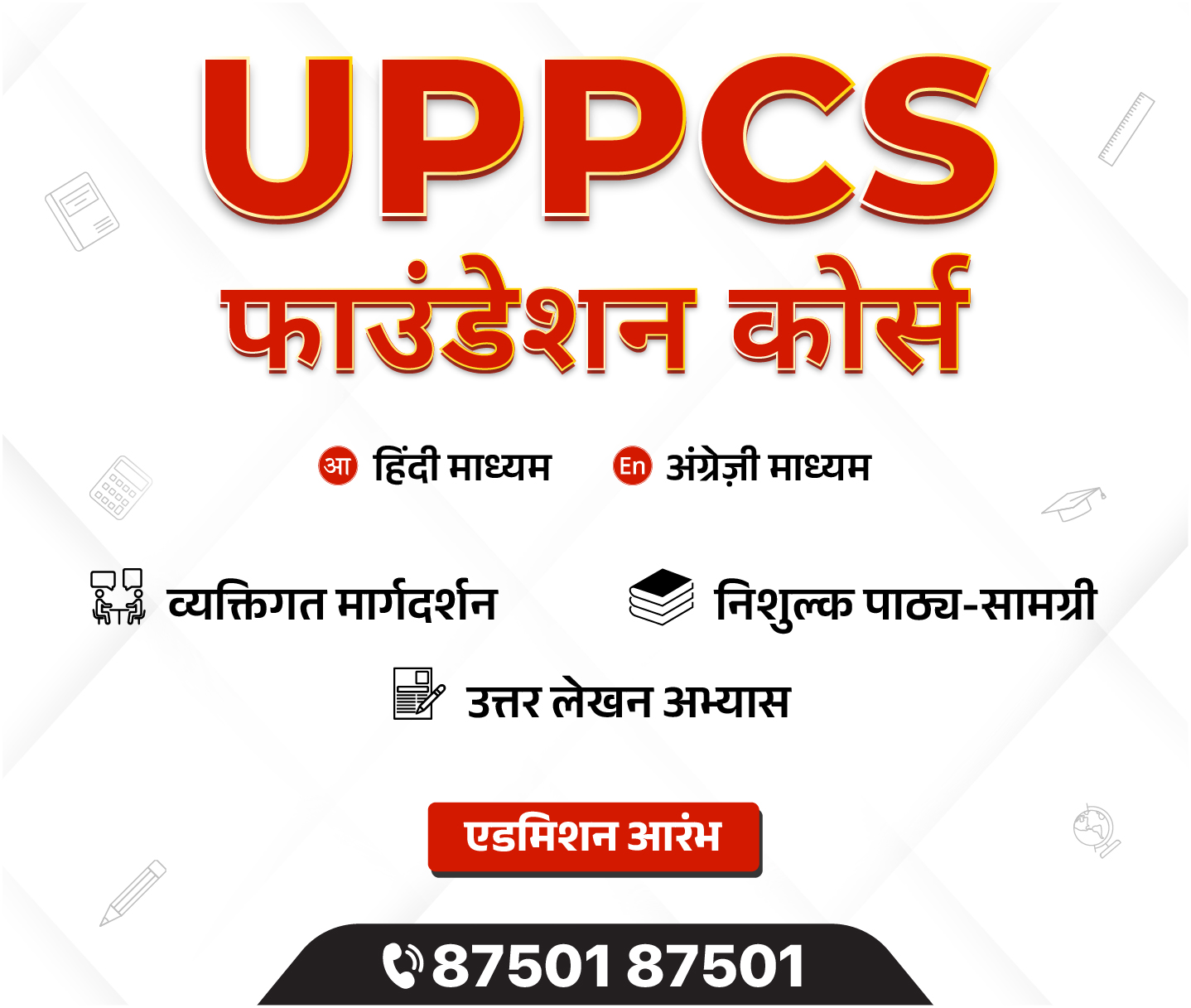
उत्तर प्रदेश Switch to English
अहेतुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिस साँप
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिज़र्व में एक दुर्लभ साँप, अहेतुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिस (लंबी थूथन वाला बेल साँप) खोजा गया।
मुख्य बिंदु
- साँप के बारे में:
- इसकी खोज दुधवा टाइगर रिज़र्व के पलिया डिवीजन में गैंडों के शिफ्टिंग अभियान के दौरान की गई थी।
- इससे पहले यह साँप केवल बिहार के पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व के जंगलों में पाया गया था।
- विशेषताएँ:
-
इसका शरीर लंबा, पतला और हरा या भूरा रंग का होता है, जो इसे अन्य साँपों से अलग करता है।
-
इसकी लंबी नाक (रोस्ट्रल) भी इसकी पहचान का एक प्रमुख संकेत है।
-
यह मुख्य रूप से पेड़ों पर रहता है और आसानी से शाखाओं तथा पत्तियों के बीच छिप सकता है।
-
यह हल्का जहरीला होता है, जिसका जहर इंसान के लिये अधिक खतरनाक नहीं होता।
-
- परिवार: कोलुब्रिडे
दुधवा टाइगर रिज़र्व के बारे में
- यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर-खीरी ज़िले में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में सबसे अच्छे प्राकृतिक जंगलों और घास के मैदानों का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह रिज़र्व अपनी समृद्ध जैवविविधता के लिये जाना जाता है, जिसमें बंगाल टाइगर, भारतीय गैंडा, दलदली हिरण, तेंदुआ और पक्षियों की कई प्रजातियाँ सहित विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव हैं।
- इस तराई आर्क लैंडस्केप (TAL) के अंतर्गत तीन महत्त्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं :
- दुधवा राष्ट्रीय उद्यान
- किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य
- कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य
- तीनों संरक्षित क्षेत्रों को राज्य में रॉयल बंगाल टाइगर के अंतिम व्यवहार्य घर होने के नाते प्रोजेक्ट टाइगर (Project Tiger) के तहत दुधवा टाइगर रिज़र्व के रूप में संयुक्त रूप से गठित किया गया है।
- दुधवा नेशनल पार्क और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को वर्ष 1987 में तथा कतर्निया वन्यजीव अभयारण्य को वर्ष 2000 में दुधवा टाइगर रिज़र्व में शामिल किया गया था।

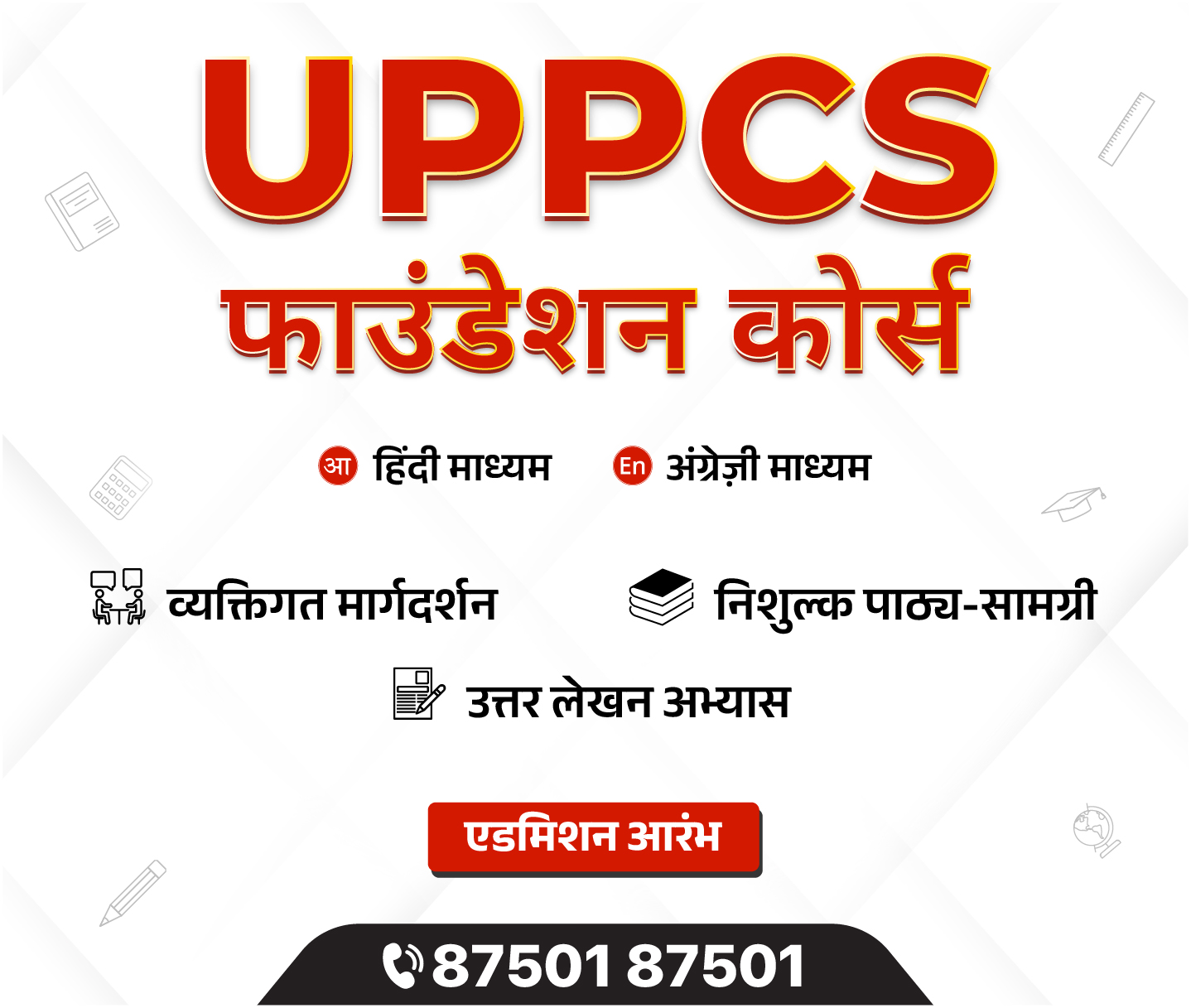
उत्तर प्रदेश Switch to English
भारत-नेपाल साहित्य महोत्सव
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश के वृंदावन (मथुरा) में तीन दिवसीय भारत-नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया।
मुख्य बिंदु
- उत्सव के बारे में:
- यह आयोजन उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की सहायक संस्था गीता शोध संस्थान और क्रांति धरा साहित्य अकादमी, मेरठ द्वारा आयोजित किया गया।
- इस महोत्सव में भारत और नेपाल के 180 से अधिक साहित्यकार, लेखक, पत्रकार और शिक्षाविद् शामिल हुए।
- इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहित और संवर्द्धित करना था।
- महत्त्व:
- साहित्य और संस्कृति के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन मिला।
- भारत और नेपाल के साहित्यकारों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिला।
- पारंपरिक और समकालीन साहित्य को एक नई दिशा मिली।
भारत -नेपाल संबंध
- पड़ोसी के रूप में भारत और नेपाल मित्रता एवं सहयोग के अनूठे संबंधों को साझा करते हैं, जिसकी विशेषता एक खुली सीमा, दोनों देशों के लोगों के बीच रिश्तेदारी तथा मज़बूत सांस्कृतिक संबंध है।
- नेपाल के व्यापारिक व्यापार में लगभग दो-तिहाई तथा सेवाओं के व्यापार में लगभग एक-तिहाई योगदान भारत का है।
- बटालियन स्तर पर संयुक्त सैन्य अभ्यास, 'सूर्य किरण', भारत तथा नेपाल दोनों देशों में क्रमिक आधार आयोजित किया जाता है।
- भारत तराई क्षेत्र में 10 सड़कों को उन्नत करके, जोगबनी-विराटनगर तथा जयनगर-बर्दीबास में सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करके एवं बीरगंज, विराटनगर, भैरहवा व नेपालगंज जैसे प्रमुख स्थानों पर एकीकृत चेक पोस्ट स्थापित करके नेपाल की मुख्य रूप से सहायता की।
- भारत ने काठमांडू-वाराणसी, लुंबिनी-बोधगया और जनकपुर-अयोध्या को जोड़ने के लिये तीन सिस्टर-सिटी समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं।

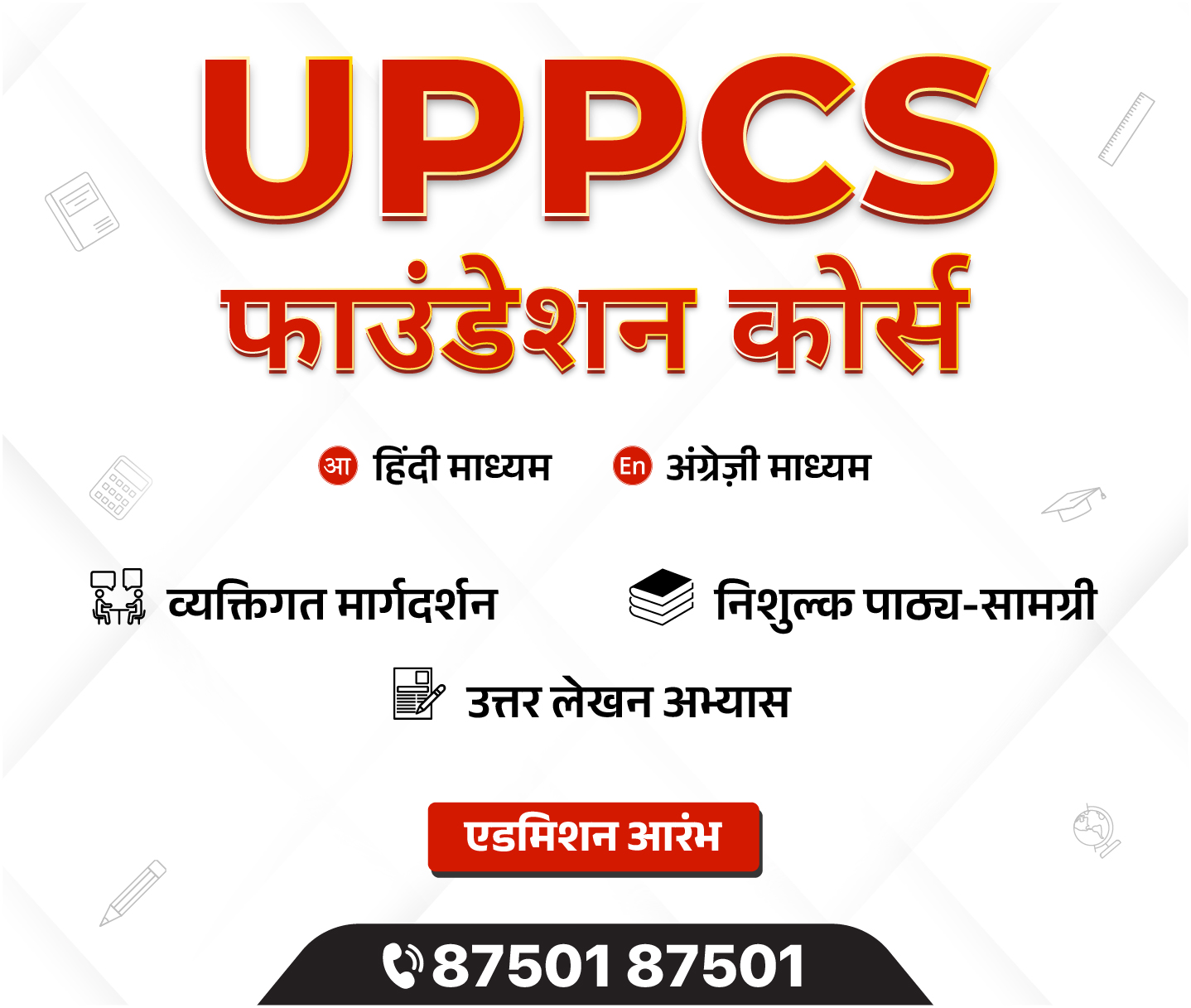
राजस्थान Switch to English
राजस्थान उच्च न्यायालय में नए न्यायाधीश नियुक्त
चर्चा में क्यों?
राजस्थान उच्च न्यायालय में चार नए न्यायधीशों की नियुक्ति की गई, जिससे अब न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है।
मुख्य बिंदु
- न्यायधीशों के बारे में:
- न्यायालय में आयोजित औपचारिक समारोह में मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ने उन्हें शपथ दिलाई।
- नए न्यायधीशों में जयपुर से आनंद शर्मा और जोधपुर से सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित और संदीप शाह का नाम शामिल हैं।
- उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति:
- संविधान का अनुच्छेद 217: यह कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी।
- मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है।
- परामर्श प्रक्रिया: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है जिसमें CJI और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
- यह प्रस्ताव दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है।
- सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो केंद्रीय कानून मंत्री को प्रस्ताव राज्यपाल को भेजने की सलाह देता है।
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इस नीति के आधार पर की जाती है कि राज्य का मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य से बाहर का होगा।
- संविधान का अनुच्छेद 217: यह कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी।
राजस्थान उच्च न्यायालय
- राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 के तहत की गई थी।
- वर्तमान में इस न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 50 है, जबकि मार्च 2025 तक कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 38 है।
- राजस्थान के एकीकरण से पहले, राज्य की विभिन्न इकाइयों में पाँच अलग-अलग उच्च न्यायालय कार्यरत थे। राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 ने इन विभिन्न न्यायालयों को समाप्त कर पूरे राज्य के लिये एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान किया।
- शुरुआत में राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय जयपुर में था और इसका उद्घाटन राजप्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह ने 29 अगस्त 1949 को किया।
- बाद में, 1956 में राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के बाद, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसे जोधपुर में स्थानांतरित कर दिया गया।
- राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कमला कांत वर्मा थे।


राजस्थान Switch to English
राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय AI रोबोटिक्स संस्थान
चर्चा में क्यों?
1 अप्रैल 2025 को निम्स (NIMS) विश्वविद्यालय जयपुर में प्रदेश के पहले "डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, एवं साइबरनेटिक्स संस्थान का उद्घाटन किया गया।
मुख्य बिंदु
- संस्थान के बारे में:
- यह संस्थान 'राइजिंग राजस्थान' पहल के तहत राजस्थान सरकार और निम्स विश्वविद्यालय के बीच हुए समझौते का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।
- उद्देश्य:
- इसका प्रमुख उद्देश्य राजस्थान को डिजिटल नवाचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का वैश्विक केंद्र बनाना है।
- संस्थान में 15 अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी, जिनमें 500 से अधिक उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटर शामिल होंगे।
- इसके अलावा, इस संस्थान को इंडो-पैसिफिक यूरोपीयन हब फॉर डिजिटल पार्टनरशिप (INPACE) के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, जो भारत और यूरोप के बीच डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देगा।
- यह संस्थान यूरोपीय संघ (EU) और अन्य वैश्विक संगठनों के साथ मिलकर AI, रोबोटिक्स और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करेगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
- परिचय:
- AI का आशय कंप्यूटर या कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट के ऐसे कार्य करने की क्षमता से है जो आमतौर पर मनुष्यों द्वारा किये जाते हैं क्योंकि ऐसे कार्यों के निष्पादन हेतु मानव बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है।
- हालाँकि अभी ऐसी कोई AI प्रणाली नहीं है जो एक सामान्य मानव द्वारा किये जा सकने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर सके, हालाँकि कुछ AI मनुष्यों द्वारा किये जाने वाले कुछ विशिष्ट कार्यों को करने में सक्षम हो सकते हैं।
- विशेषताएँ और घटक:
- डीप लर्निंग (DL) तकनीक बड़ी मात्रा में असंरचित डाटा जैसे- टेक्स्ट, चित्र या वीडियो के माध्यम से ऑटोमेटिक लर्निंग को सक्षम बनाती है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता की आदर्श विशेषता इसकी युक्तिसंगत कार्रवाई करने की क्षमता है जिसमें एक विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। मशीन लर्निंग (ML), AI का ही एक प्रकार है।
यूरोपीय संघ
- स्थापना: द्वितीय विश्व युद्ध (1939-45) के बाद वर्ष 1951 में छह देशों (बेल्जियम, फ्राँस, जर्मनी, इटली, लक्जमबर्ग और नीदरलैंड) द्वारा इसकी स्थापना की गई।
- वर्तमान सदस्य देश: वर्तमान में इसमें 27 देश (ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस गणराज्य, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्राँस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन) शामिल हैं।
- ब्रिटेन 1973 में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ और वर्ष 2020 में इससे अलग हो गया (ब्रेक्सिट)।
- जनसांख्यिकी: यूरोपीय संघ में, जर्मनी की जनसंख्या सबसे अधिक है और फ्राँस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है जबकि सबसे छोटा देश माल्टा है।
- खुली सीमाएँ: साइप्रस और आयरलैंड के अतिरिक्त शेंगेन क्षेत्र में यूरोपीय संघ के अधिकांश सदस्यों के मुक्त आवागमन की अनुमति है।
- चार गैर-यूरोपीय संघ देश (आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिकटेंस्टीन) भी शेंगेन का हिस्सा हैं।
- एकल बाज़ार: यूरोपीय संघ के भीतर माल, सेवाओं, पूंजी और लोगों का स्वतंत्र आवागमन होता है।
- जलवायु लक्ष्य: इसने वर्ष 2050 तक जलवायु-तटस्थ होने और वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में 55% की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।



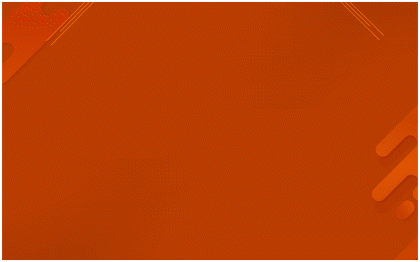


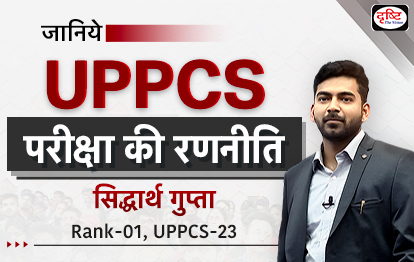
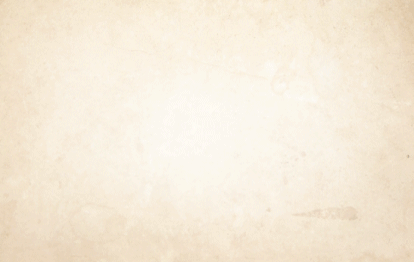
.jpg)
.jpg)
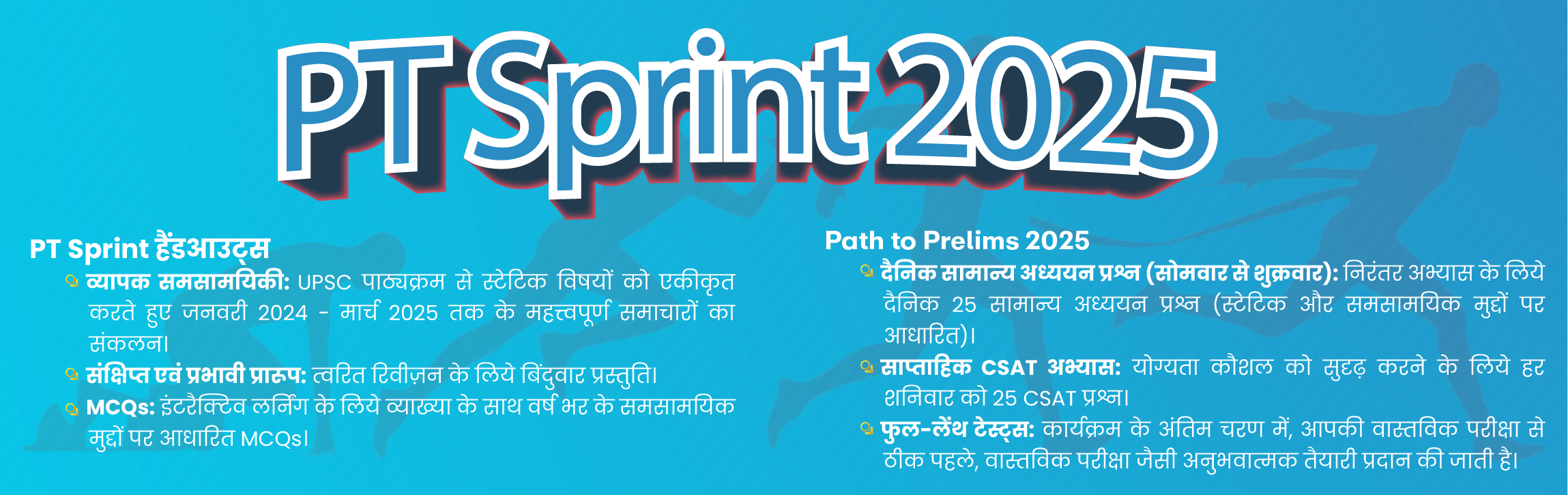
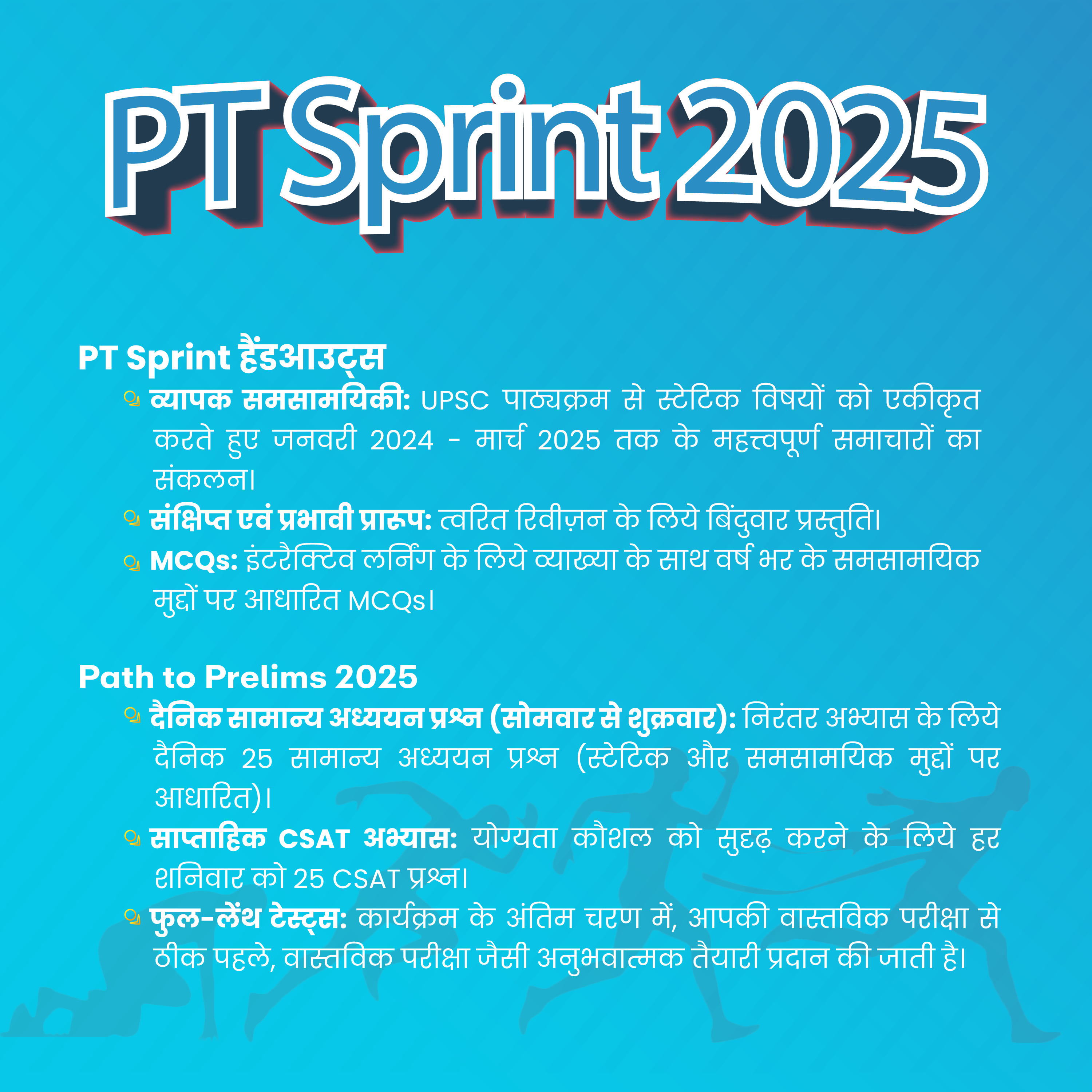

%201.jpeg)
.jpg)


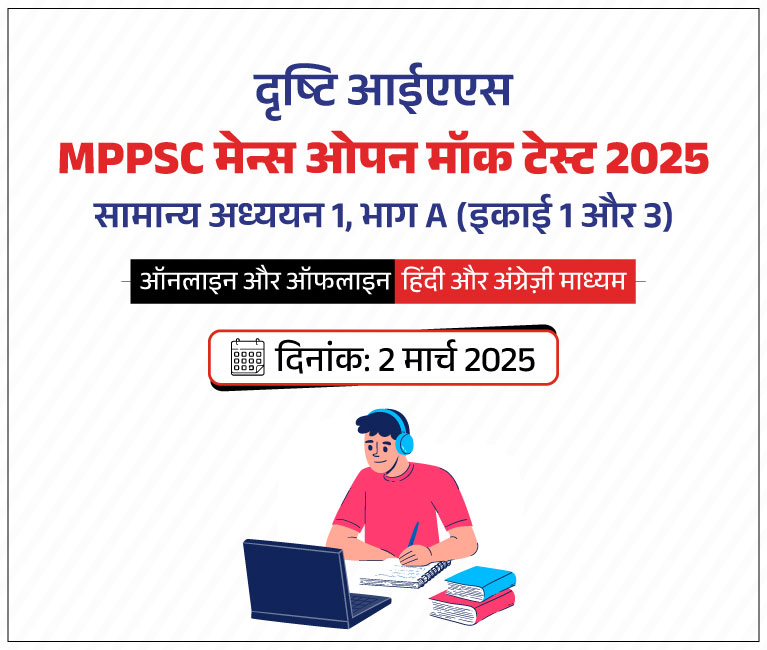
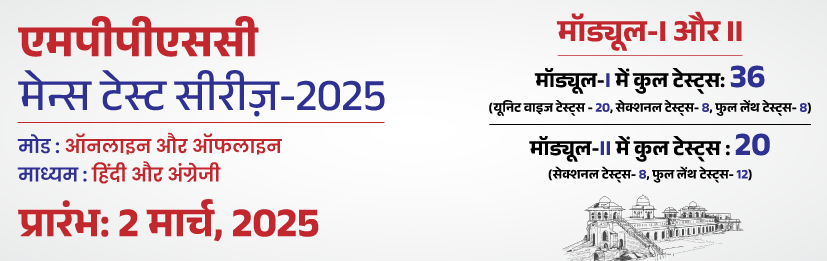

%20MPPCS%202025%20Desktop%20H.jpg)
%20MPPCS%202025%20Mobile%20H%20(1).jpg)

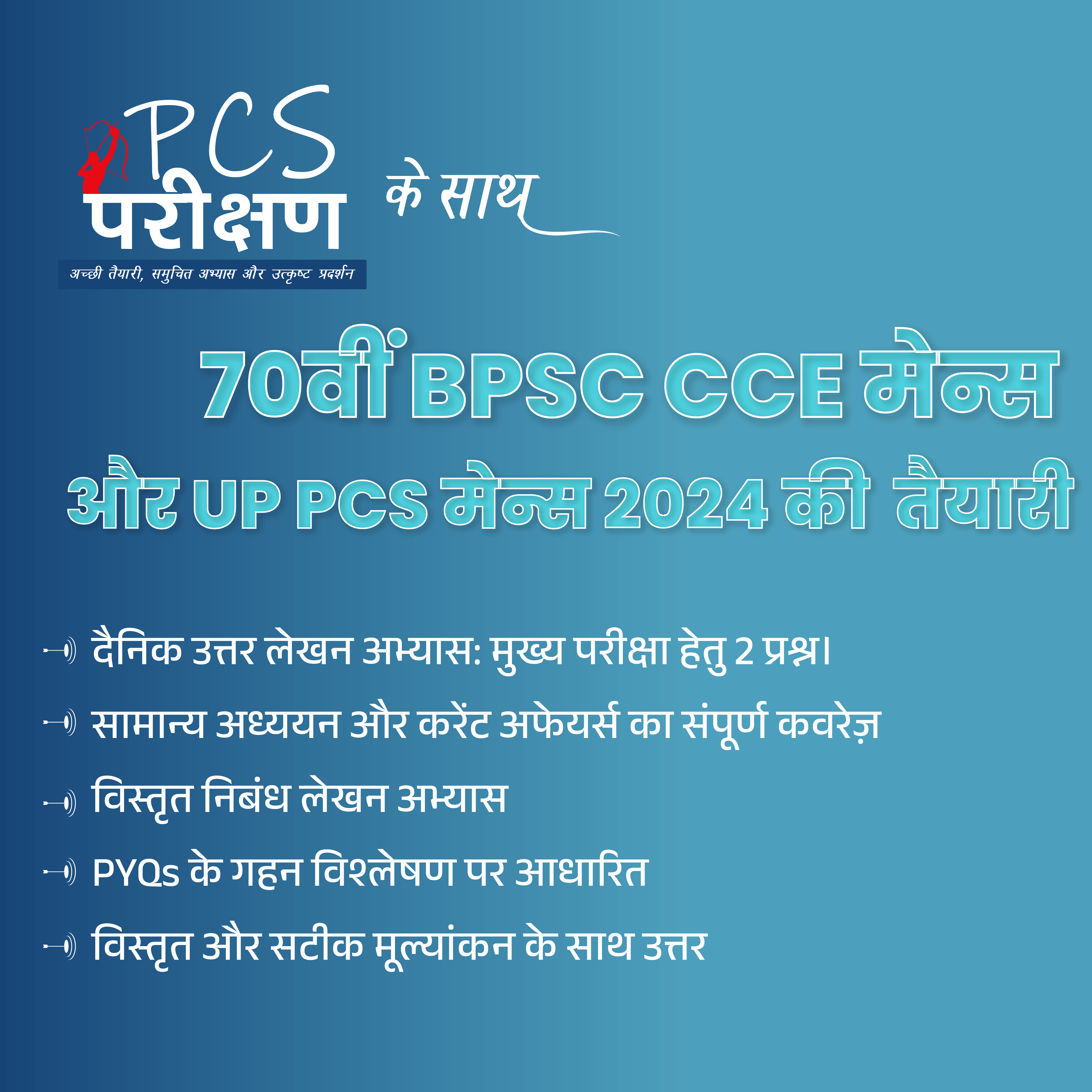


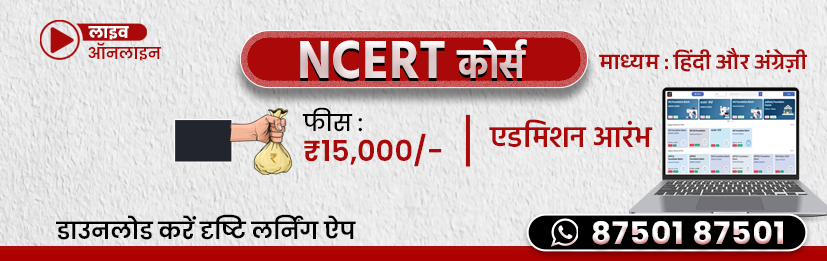
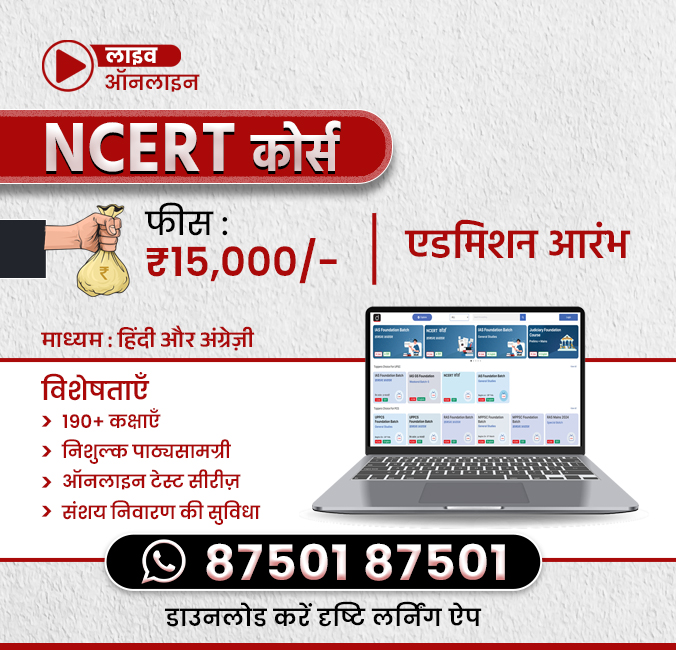

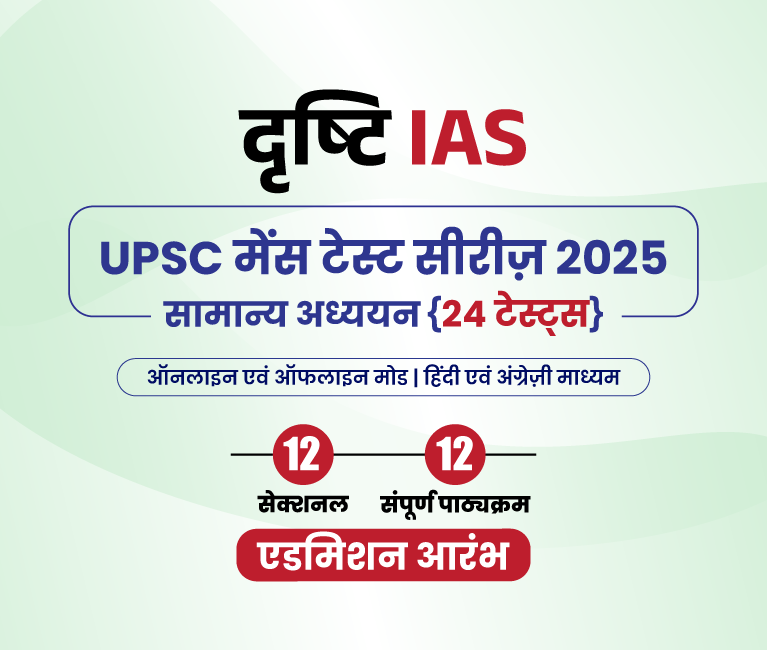
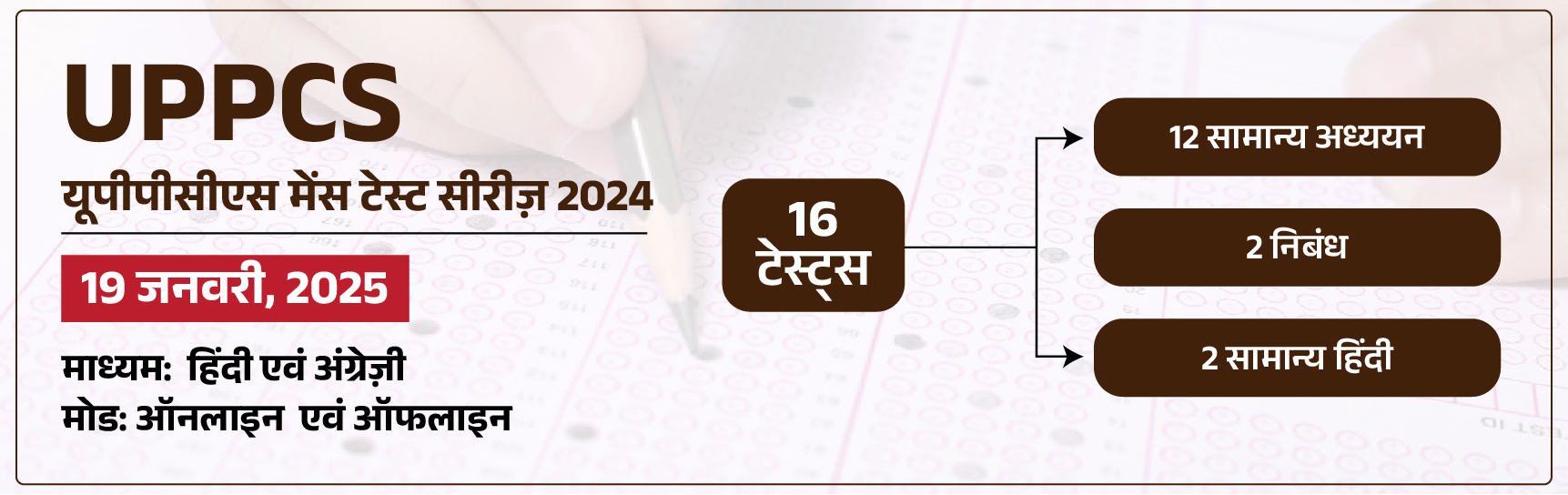
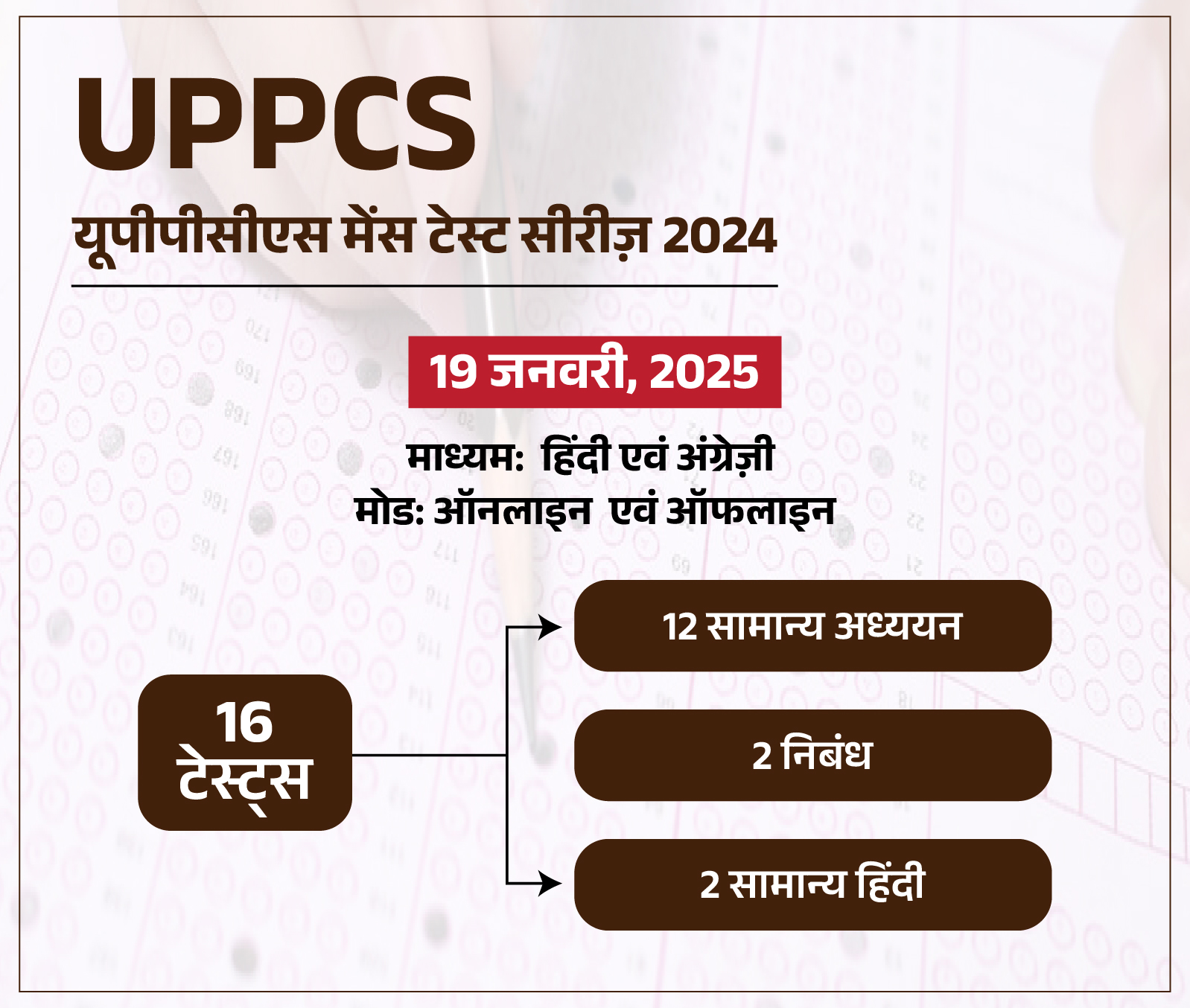



 PCS परीक्षण
PCS परीक्षण



