छत्तीसगढ़ Switch to English
अनुच्छेद 21 का उल्लंघन
चर्चा में क्यों?
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि कोई भी महिला को कौमार्य परीक्षण के लिये मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, जो उसके जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है।
मुख्य बिंदु
- मामले की पृष्ठभूमि:
- एक याचिकाकर्त्ता ने अपनी पत्नी के लिये कौमार्य परीक्षण की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उसकी पत्नी अवैध संबंध में है।
- उन्होंने पारिवारिक अदालत के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया था।
- कौमार्य परीक्षण पर न्यायालय का रुख:
- उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी भी महिला को कौमार्य परीक्षण के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता।
- इसमें कहा गया कि इस तरह का परीक्षण अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, जो सम्मान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
- कौमार्य परीक्षण की अनुमति देना मौलिक अधिकारों, प्राकृतिक न्याय और महिला की गरिमा का उल्लंघन होगा।
- उच्च न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण और अपरिवर्तनीय है।
अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण
- किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
- यह मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति, नागरिक और विदेशियों को समान रूप से उपलब्ध है।
- अनुच्छेद 21 दो अधिकार प्रदान करता है:
- जीवन का अधिकार
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार को 'मौलिक अधिकारों का हृदय' बताया है। इसका तात्पर्य यह है कि यह अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध प्रदान किया गया है।
- यहाँ राज्य में सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, विधायिका आदि भी शामिल हैं।
- जीवन का अधिकार सिर्फ़ जीवित रहने के अधिकार के बारे में नहीं है। इसमें गरिमा और अर्थ के साथ पूर्ण जीवन जीने की क्षमता भी शामिल है।
- केस कानून:
- ए.के. गोपालन केस (1950): 1950 के दशक तक अनुच्छेद 21 का दायरा सीमित था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान में 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' शब्द ने अमेरिकी 'उचित प्रक्रिया' के बजाय व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ब्रिटिश अवधारणा को मूर्त रूप दिया है।
- मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978): इस मामले ने गोपालन मामले के फैसले को पलट दिया। अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचार का दायरा बहुत व्यापक है, जिसमें कई अधिकार शामिल हैं, जिनमें से कुछ अनुच्छेद 19 के तहत सन्निहित हैं, इस प्रकार उन्हें 'अतिरिक्त सुरक्षा' दी गई है। न्यायालय ने यह भी माना कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आने वाले कानून को अनुच्छेद 19 के तहत आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहिये।
- इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से वंचित करने के लिये कानून के तहत कोई भी प्रक्रिया अनुचित, अविवेकपूर्ण या मनमानी नहीं होनी चाहिये।
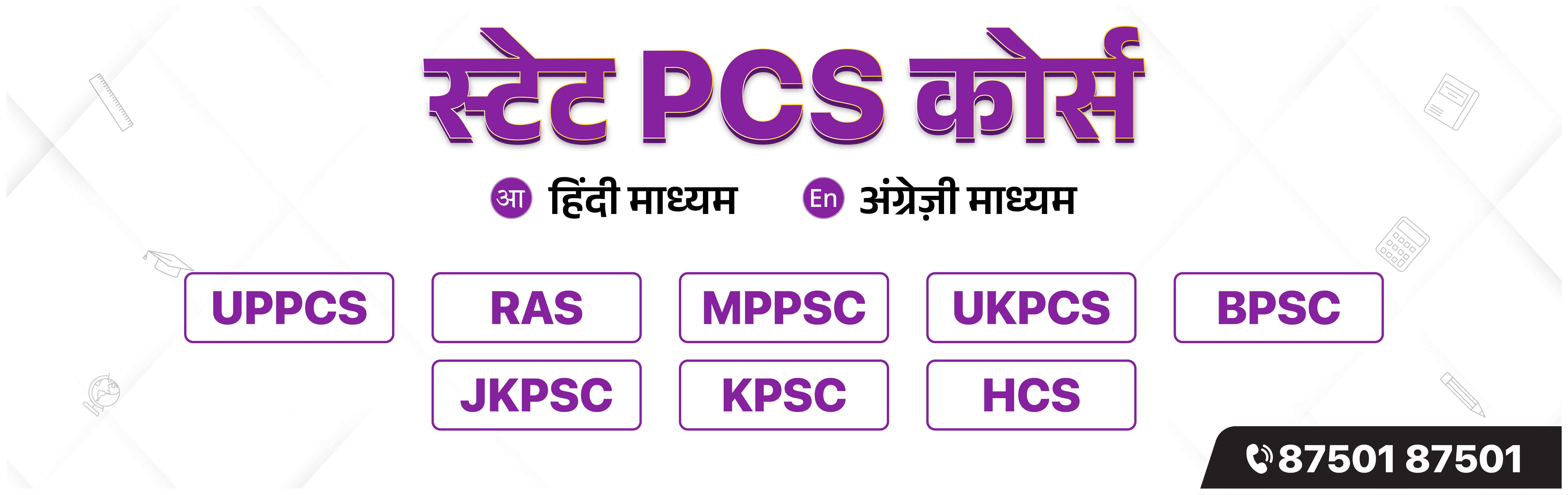
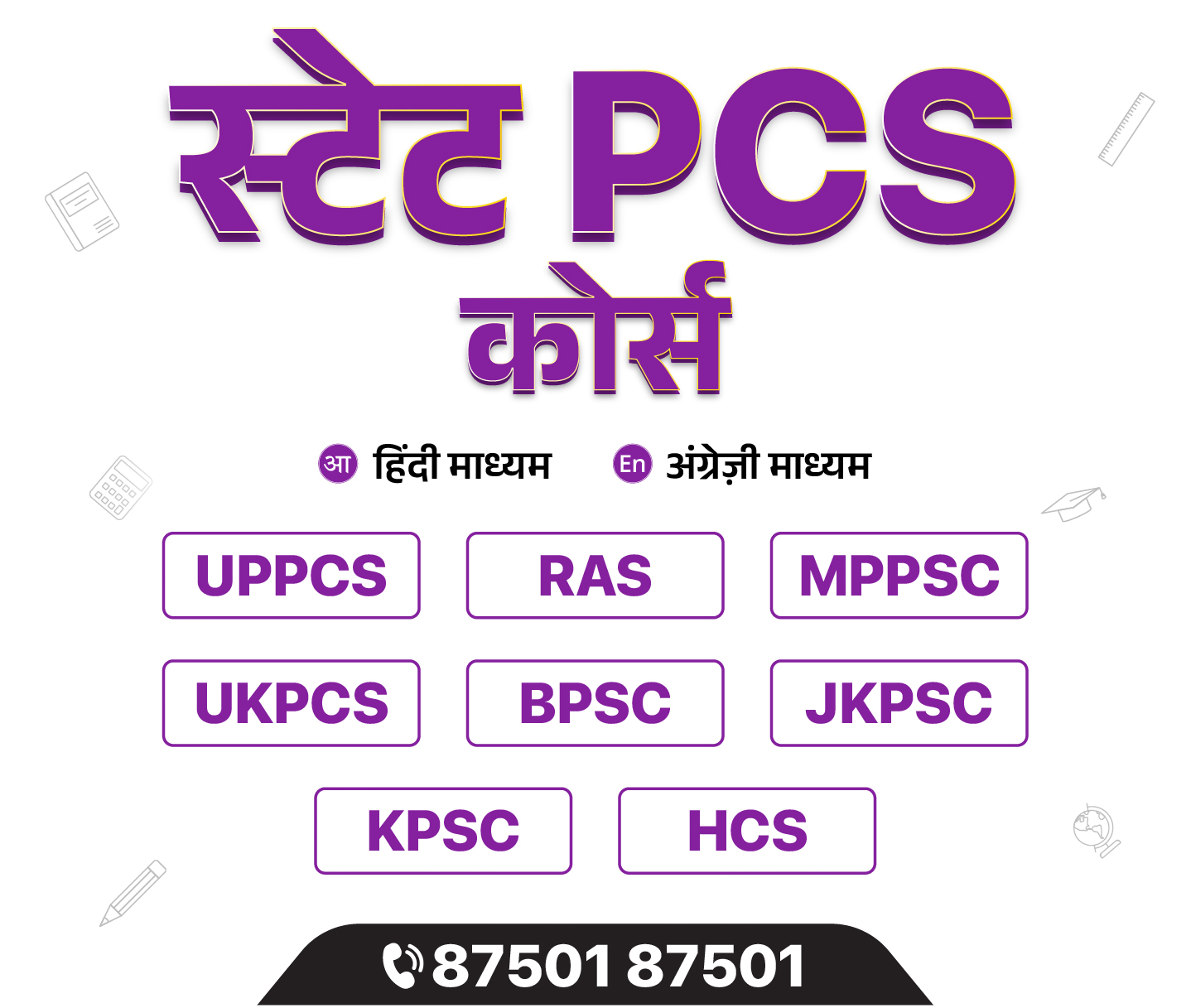
उत्तराखंड Switch to English
उत्तराखंड में 18 स्थानों के नाम बदले गए
चर्चा में क्यों?
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर ज़िलों में स्थित 18 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की।
मुख्य बिंदु
- नाम परिवर्तन के पीछे उद्देश्य:
- मुख्यमंत्री ने कहा कि नाम बदलने की पहल का उद्देश्य जनभावना का सम्मान करना तथा भारतीय संस्कृति और विरासत को संरक्षित करना है।
- उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि नए नाम भारतीय संस्कृति में योगदान देने वाले महान व्यक्तियों को सम्मानित करके लोगों को प्रेरित करेंगे।
- पुनः नामित स्थान:
- हरिद्वार ज़िले में:
- औरंगज़ेबपुर (भगवानपुर ब्लॉक) → शिवाजी नगर
- गाज़ीवाली (बहादराबाद ब्लॉक) → आर्य नगर
- चाँदपुर (बहादराबाद ब्लॉक) → ज्योतिबा फुले नगर
- मोहम्मदपुर जाट (नारसन ब्लॉक) → मोहनपुर जाट
- खानपुर कुरसाली (नारसन ब्लॉक) → अंबेडकर नगर
- इदिरिसपुर (खानपुर ब्लॉक) → नंदपुर
- खानपुर (खानपुर ब्लॉक) → श्री कृष्णपुर
- अकबरपुर फज़लपुर (रुड़की) → विजय नगर
- देहरादून में:
- मियाँवाला → रामजीवाला
- पीरवाला → केसरी नगर
- चाँदपुर खुर्द → पृथ्वीराज नगर
- अब्दुलपुर → दक्ष नगर
- नैनीताल में:
- नवाबी रोड → अटल मार्ग
- पनचक्की से IIT रोड → गुरु गोवलकर मार्ग
- उधम सिंह नगर में:
- सुल्तानपुर पट्टी नगर पंचायत → कौशल्यापुरी
- हरिद्वार ज़िले में:
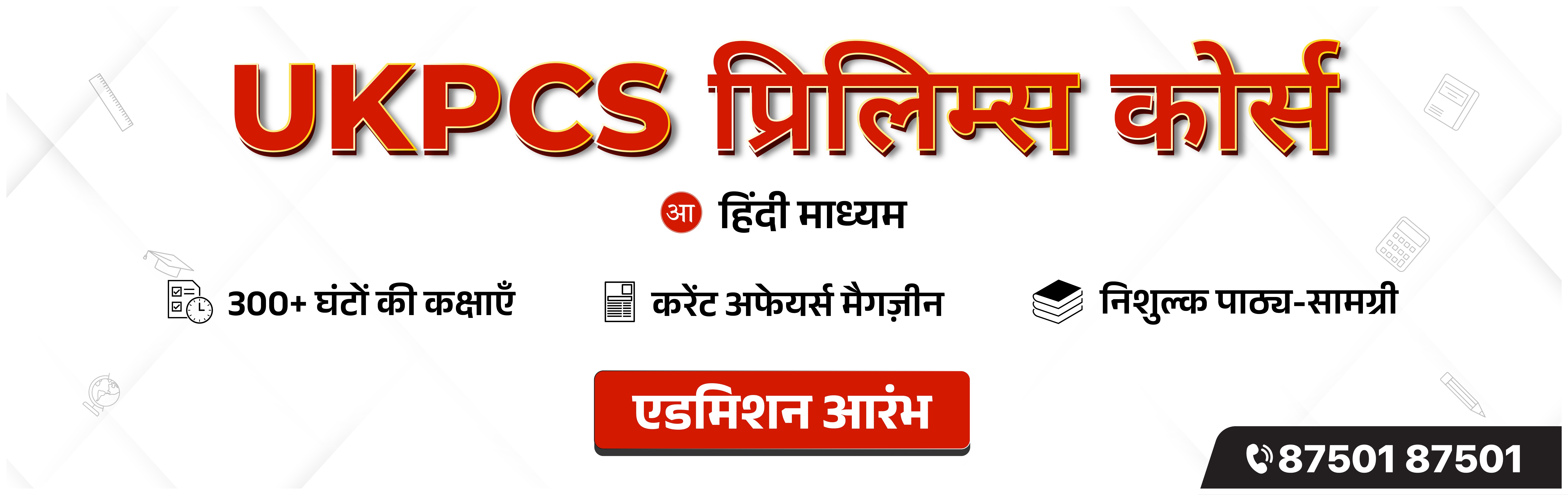

छत्तीसगढ़ Switch to English
सरहुल महोत्सव
चर्चा में क्यों?
1 अप्रैल 2025 को झारखंड और छोटे नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों ने सरहुल त्योहार के साथ नए साल और वसंत के आगमन का उत्सव मनाया।
मुख्य बिंदु
- प्रकृति और साल वृक्ष की पूजा:
- आदिवासी साल वृक्षों (शोरिया रोबस्टा) की पूजा करते हैं, उनका मानना है कि ये सरना माँ का निवास स्थान है, जो गाँवों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाती हैं।
- सरहुल, जिसका अर्थ है "साल वृक्ष की पूजा", सबसे पूजनीय आदिवासी त्योहारों में से एक है, जो सूर्य और पृथ्वी के मिलन का प्रतीक है।
- पाहन (गाँव का पुजारी) सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि उसकी पत्नी (पाहेन) पृथ्वी का प्रतीक है।
- इस पवित्र मिलन को जीवन को बनाए रखने के लिये आवश्यक माना जाता है, क्योंकि यह सूर्य की किरणों का मिट्टी से मिलकर विकास को सक्षम बनाता है।
- आदिवासी सरहुल अनुष्ठान पूरा करने के बाद ही अपने खेतों की जुताई, फसल बोना और वन उपज एकत्र करना शुरू करते हैं।
- यह त्योहार उरांव, मुंडा, संथाल, खड़िया और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, जिनमें से प्रत्येक की अलग-अलग परंपराएँ हैं।
- सरहुल का विकास और इसका राजनीतिक महत्त्व:
- 1960 के दशक में आदिवासी नेता बाबा कार्तिक उरांव ने सामाजिक न्याय और आदिवासी पहचान संरक्षण की वकालत करते हुए राँची में सरहुल उत्सव शुरू किया।
- पिछले 60 वर्षों में यह उत्सव सरहुल का एक महत्त्वपूर्ण पहलू बन गया है तथा राँची में सिरम टोली सरना स्थल एक प्रमुख सभा स्थल बन गया है।
- यह त्योहार राजनीतिक रूप से भी महत्त्वपूर्ण हो गया है तथा आदिवासी पहचान को विकसित करने के लिये एक मंच के रूप में कार्य कर रहा है।
साल वृक्ष
- परिचय:
- शोरिया रोबस्टा या साल वृक्ष, डिप्टेरोकार्पेसी परिवार का एक वृक्ष प्रजाति है।
- यह वृक्ष भारत, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत और हिमालयी क्षेत्रों का मूल निवासी है।
- विवरण:
- यह 40 मीटर तक ऊँचा हो सकता है तथा इसके तने का व्यास 2 मीटर होता है।
- पत्तियाँ 10-25 सेमी लंबी और 5-15 सेमी चौड़ी होती हैं।
- आर्द्र क्षेत्रों में साल सदाबहार होता है; शुष्क क्षेत्रों में यह शुष्क ऋतु में पर्णपाती होता है, जिसके अधिकांश पत्ते फरवरी से अप्रैल तक गिर जाते हैं तथा अप्रैल और मई में पुनः पत्ते निकल आते हैं।
- साल के वृक्ष को मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड सहित उत्तरी भारत में सखुआ के नाम से भी जाना जाता है।
- यह दो भारतीय राज्यों– छत्तीसगढ़ और झारखंड का राज्य वृक्ष है।

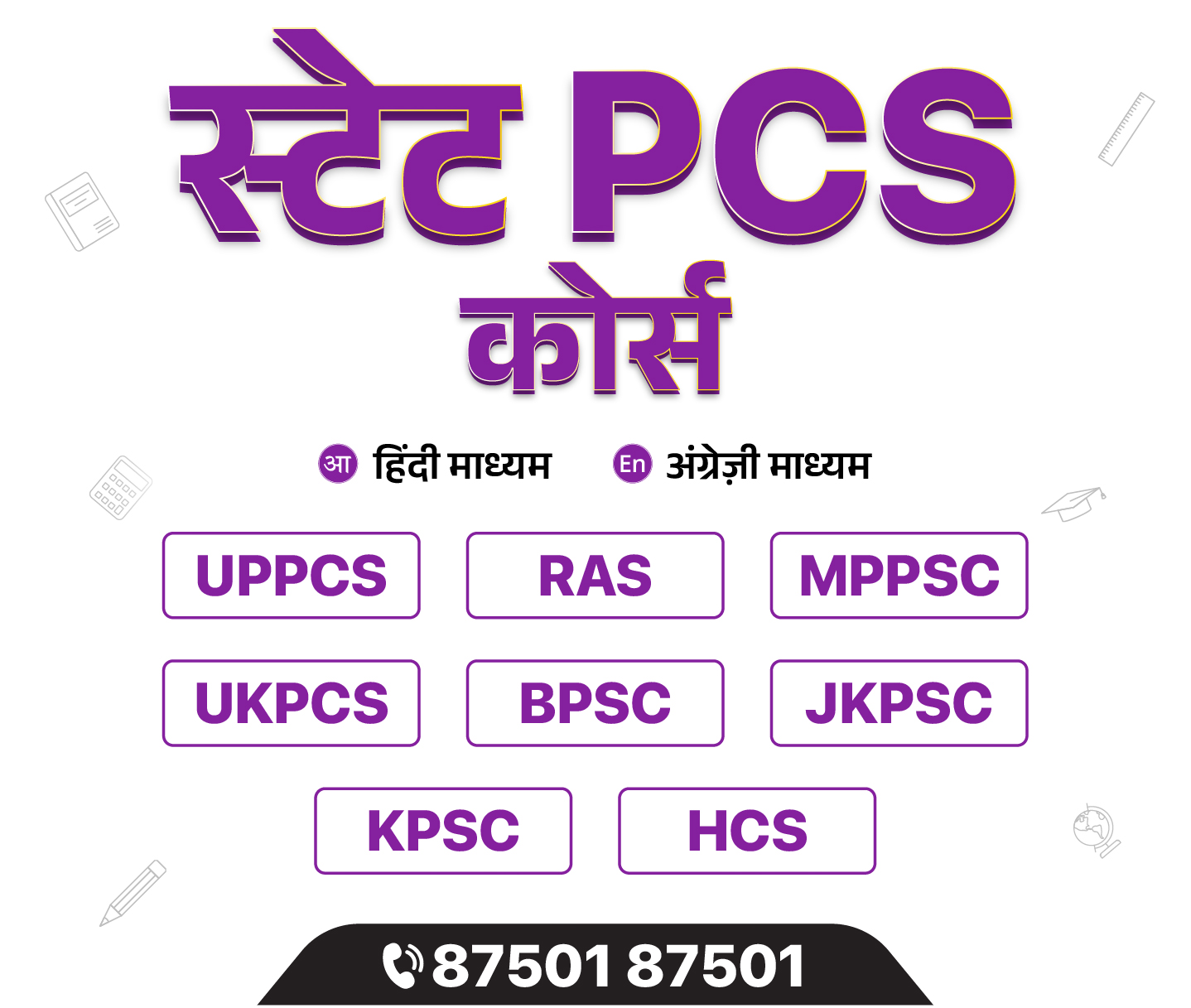
उत्तर प्रदेश Switch to English
एग्रीवोल्टेइक परियोजना
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश ‘एग्रीवोल्टेइक’ परियोजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
मुख्य बिंदु
- एग्रीवोल्टेइक प्रणाली
- एग्रीवोल्टाइक प्रणाली, जिसे कृषि-वोल्टीय प्रणाली या "सौर-खेती" भी कहा जाता है, एक नई तकनीक है जिसमें किसान अपनी फसलों के उत्पादन के साथ-साथ बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं।
- इस प्रणाली में फोटो-वोल्टाइक (PV) तकनीक का उपयोग करके कृषि योग्य भूमि पर सौर पैनल स्थापित किये जाते हैं।
- यह तकनीक पहली बार वर्ष 1981 में एडॉल्फ गोएट्ज़बर्गर और आर्मिन ज़ास्ट्रो द्वारा पेश की गई थी। 2004 में जापान में इसका प्रोटोटाइप विकसित किया गया और कई परीक्षणों के बाद 2022 में पूर्वी अफ्रीका में इसे लागू किया गया।
- वर्तमान में भारत, अमेरिका, फ्राँस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है।
- हालांकि, भारत में यह तकनीक अभी अपने प्रारंभिक चरण में है।
- लाभ
- बढ़ती ऊर्जा की मांग और खाद्य सुरक्षा की समस्याओं का समाधान।
- सौर पैनल से फसलों की वाष्पन दर कम और जल का बेहतर उपयोग।
- सौर पैनल से फसलों को उच्च तापमान और UV किरणों से सुरक्षा।
- सौर ऊर्जा से बिजली की लागत में कमी और किसानों की आय में वृद्धि।
- बारिश का पानी सौर पैनल से एकत्र और सिंचाई के लिये उपयोग।
- चुनौतियाँ
- यह एक भूमि-आधारित प्रणाली है, जिसमें प्रति मेगावाट उत्पादन के लिये लगभग दो हेक्टेयर ज़मीन की आवश्यकता होती है।
- बरसाती मौसम में जब आकाश में बादल होते हैं, तब यह प्रणाली उतनी प्रभावी नहीं रहती है और किसानों को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है।
- सौर पैनल से उत्पन्न छाया कभी-कभी पौधों में पीड़क का कारण बन सकती है, जिससे फसलों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
- एडीबी से अनुदान:
- वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने “उत्तर प्रदेश में एग्रीवोल्टेइक परियोजनाओं का प्रदर्शन” शीर्षक वाले राज्य सरकार के तकनीकी सहायता प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
- इसके तहत एशियाई विकास बैंक (ADB) से 0.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹4.15 करोड़) की तकनीकी सहायता स्वीकृत हुई है।
- उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जिसे ADB से इस प्रकार की आर्थिक सहायता मिली है।
- महत्त्व
- इस परियोजना के तहत एक ही ज़मीन पर कृषि उत्पादन के साथ सौर ऊर्जा का भी उत्पादन होता है।
- इससे किसानों को अतिरिक्त आय मिलेगी, ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा और सतत् विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- यह पहल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण और सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।
एशियाई विकास बैंक क्या है?
- परिचय: ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।
- ADB सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान एवं इक्विटी निवेश प्रदान करके अपने सदस्यों तथा भागीदारों की सहायता करता है।
- मुख्यालय: मनीला, फिलीपींस
- सदस्य: वर्तमान में इसके 68 सदस्य हैं जिनमें से 49 एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के भीतर और 19 अन्य क्षेत्रों से हैं।
- ADB और भारत: भारत ADB का संस्थापक सदस्य और बैंक का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है।
- ADB की रणनीति 2030 और देश की साझेदारी रणनीति, 2023-2027 के अनुरूप मज़बूत, जलवायु लचीले एवं समावेशी विकास के लिये भारत की प्राथमिकताओं का समर्थन करता है।

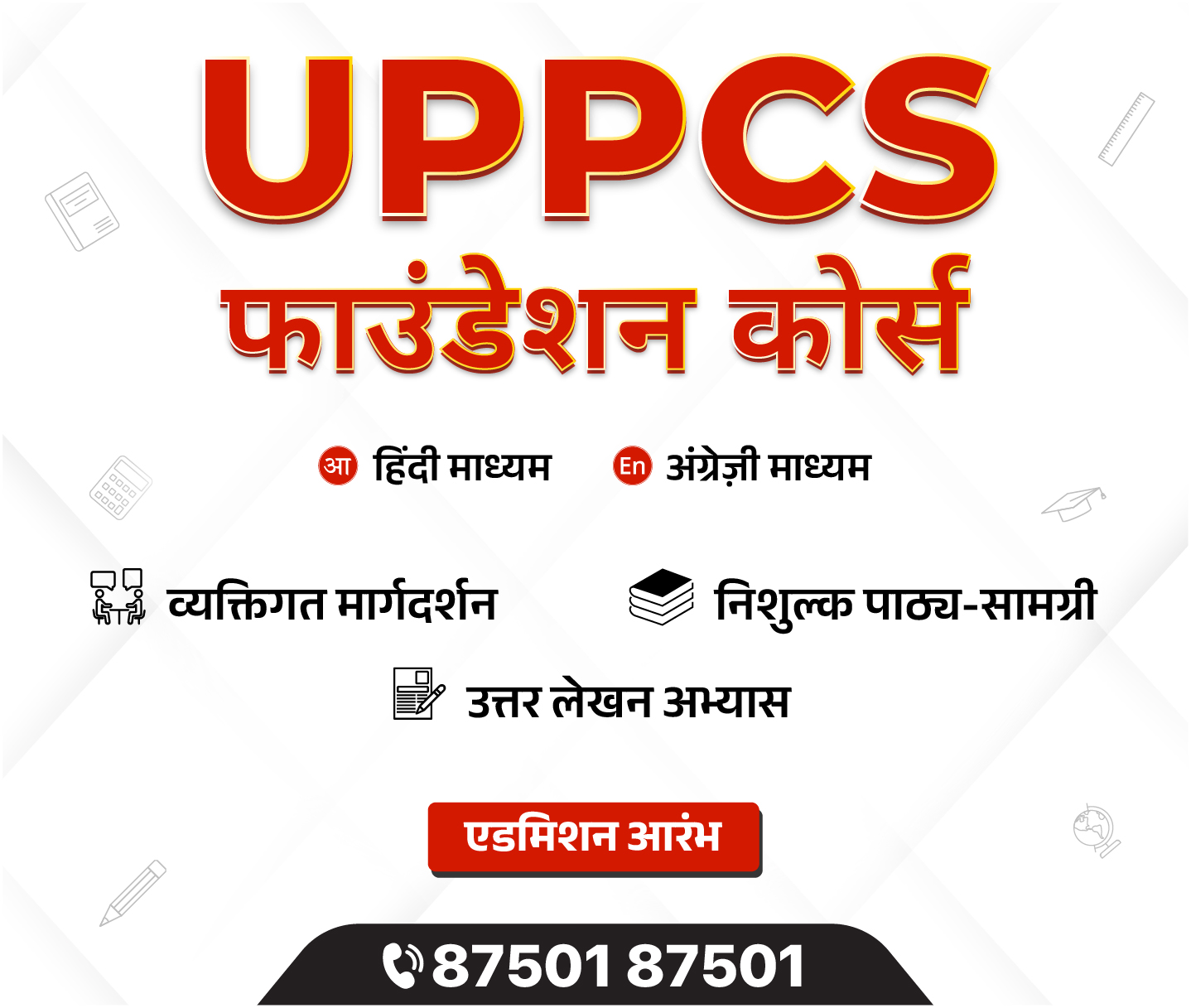
उत्तर प्रदेश Switch to English
उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन में 10 गुना वृद्धि
चर्चा में क्यों?
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि पिछले 8 वर्षों में राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन में 10 गुना वृद्धि हुई है।
मुख्य बिंदु
- मुद्दे के बारे में:
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) ने वर्तमान सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह जानकारी दी।
- वर्ष 2017 में राज्य में सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 288 मेगावाट थी, जो 2025 में बढ़कर 2653 मेगावाट हो गई है।
- उत्तर प्रदेश के सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रयास:
- सौर ऊर्जा नीति – 2022:
- 5 वर्षों में 22 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य।
- यह नीति भविष्य में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से बनाई गई है।
- बुंदेलखंड में सौर ऊर्जा पार्क:
- बुंदेलखंड क्षेत्र में 4,000 मेगावाट क्षमता का सौर पार्क विकसित किया जा रहा है।
- चित्रकूट, बाँदा और अन्य क्षेत्रों में 800 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का विकास।
- रूफटॉप और फ्लोटिंग सोलर प्लांट:
- 508 मेगावाट सोलर रूफटॉप परियोजनाएँ घरों की छतों पर स्थापित की जा चुकी हैं।
- उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत प्रदेशवासियों को सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
- सोलर रूफटॉप इंस्टालेशन में गुजरात और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है।
- औरया के दिबियापुर में प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है और ललितपुर में 1 गीगावॉट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है
- सौर ऊर्जा नीति – 2022:
सौर ऊर्जा के बारे में:
- सौर ऊर्जा, जिसे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, एक स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा स्रोत है। यह सौर प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपयोग की जाती है, जो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है:
- सौर तापीय: इसमें सूर्य की ऊष्मा का उपयोग पानी को गर्म करने के लिये किया जाता है।
- सौर फोटोवोल्टिक (पीवी): इसमें सूर्य की किरणों को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिये फोटोवोल्टिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है।
- सौर ऊर्जा का उपयोग:
- सौर प्रौद्योगिकियाँ मापनीय और लचीली होती हैं, जो पूरे शहर को सौर फार्मों के माध्यम से बिजली प्रदान कर सकती हैं।
- विकेंद्रीकृत प्रणालियों के द्वारा दूरदराज़ क्षेत्रों में भी बिजली की आपूर्ति की जा सकती है।
- छतों पर सौर पैनल लगाकर घरों और वाणिज्यिक भवनों को ऊर्जा प्रदान की जा सकती है।
- उदाहरण: कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक ऐसा उदाहरण है जहाँ सौर ऊर्जा का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है।
- सौर ऊर्जा के महत्त्व:
- जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी।
- कार्बन उत्सर्जन को कम करना।
- वायु गुणवत्ता में सुधार।
- ऊर्जा तक पहुँच और सुरक्षा को बढ़ावा देना।
उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण
- उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 1983 में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की थी, जो एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में कार्यरत था।
- बाद में इस संस्था का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) रखा गया।
- यह अभिकरण प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये स्टेट नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है।

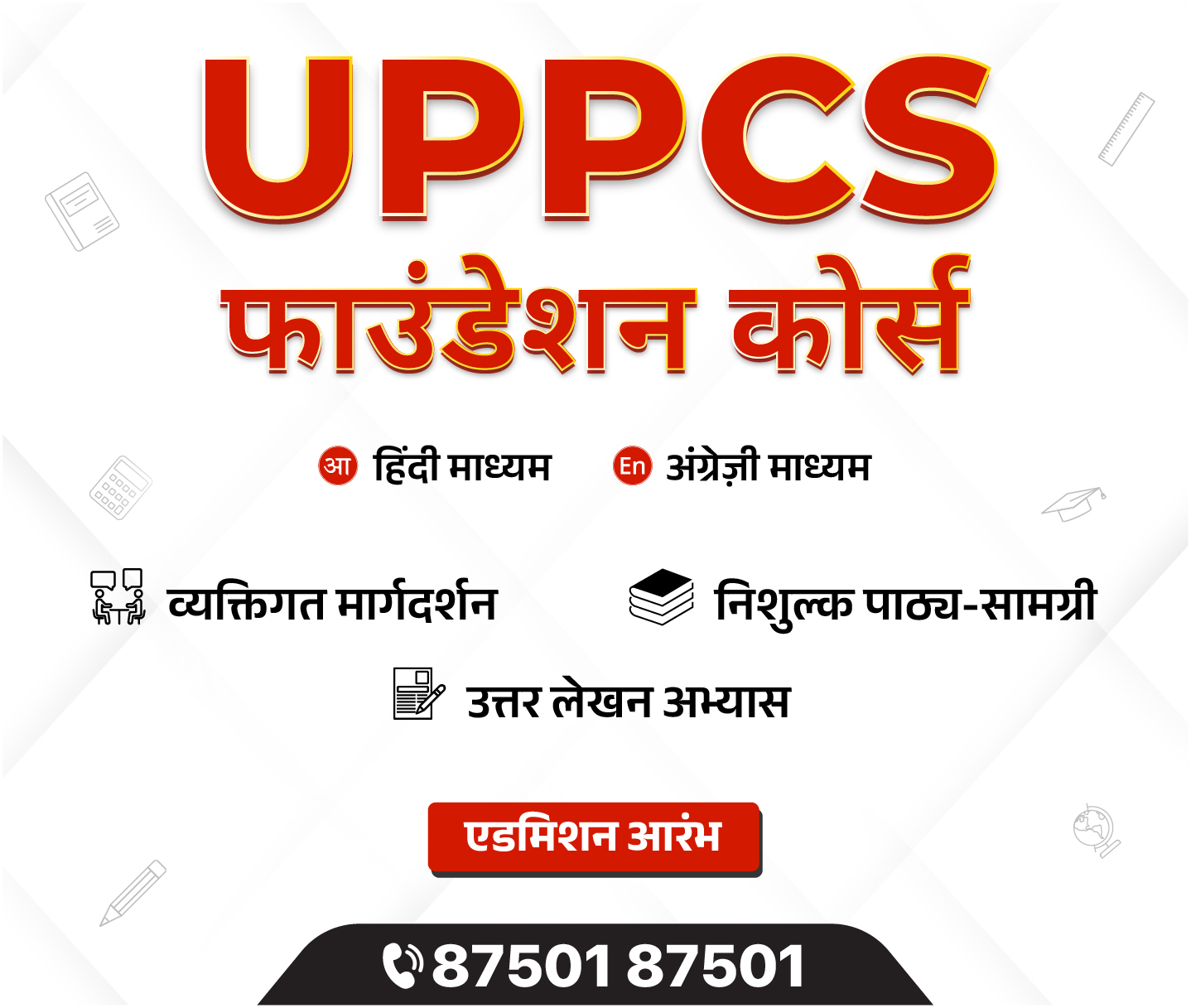
बिहार Switch to English
सेपक टकरा विश्व कप 2025
चर्चा में क्यों?
बिहार के पटना में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारत ने स्वर्ण पदक जीता।
मुख्य बिंदु
- पदकों के बारे में:
- भारतीय पुरुष रेगु टीम ने बिहार सेपक टकरा विश्व कप 2025 के फाइनल में जापान को हराकर यह स्वर्ण पदक जीता।
- यह पहली बार है जब भारत ने सेपक टकरा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है।
- भारतीय दल ने कुल सात पदक जीते।
- स्वर्ण पदक: पुरुष टीम ने रेगु श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता।
- रजत पदक: महिला युगल टीम ने रजत पदक जीता।
- कांस्य पदक:
- पुरुष युगल टीम
- महिला रेगु टीम
- मिश्रित क्वाड टीम
- महिला क्वाड टीम
- पुरुष क्वाड टीम
- इस विश्व कप में कुल आठ देशों ने पदक जीते। पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा, जबकि थाईलैंड चार पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा।
- सेपक टकरा विश्व कप 2025
-
यह प्रतियोगिता 20 से 25 मार्च 2025 तक पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुई।
-
सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सेपक टकरा महासंघ (ISTAF) द्वारा किया गया, जबकि इसकी मेज़बानी भारतीय सेपक टकरा महासंघ ने की।
- इस विश्व कप में विश्व के 20 देशों ने भाग लिया जिसमें 300 से अधिक खिलाड़ी और प्रशिक्षक शामिल थे।
- यह ISTAF विश्व कप का पाँचवाँ संस्करण था।
-
सेपक टकरा
- सेपक टकरा एक पारंपरिक मलेशियाई खेल है, जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में अत्यंत लोकप्रिय है।
- यह खेल फुटबॉल और वॉलीबॉल का संयोजन है और भारत में इसे किक वॉलीबॉल के नाम से भी जाना जाता है।
- भारत में 1980 के दशक में इसे नागपुर, महाराष्ट्र में पहली बार प्रस्तुत किया गया था।
सेपक टकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया
- सेपक टकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन 1982 में दिल्ली एशियाई खेलों की पूर्व संध्या पर हुआ था।
- यह फेडरेशन भारत में सेपक टकरा खेल के संचालन की प्रमुख संस्था है।
- मुख्यालय: नई दिल्ली
इंटरनेशनल सेपक टकरा फेडरेशन (ISTAF)
- इंटरनेशनल सेपक टकरा फेडरेशन (ISTAF) की स्थापना 1982 में हुई थी।
- यह सेपक टकरा खेल की विश्वस्तरीय शासी संस्था है।
- मुख्यालय: बैंकॉक, थाईलैंड


राजस्थान Switch to English
राजस्थान दिवस
चर्चा में क्यों?
हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च के बजाए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाने की घोषणा की है।
मुख्य बिंदु
- वर्षों पुरानी मांग:
- वर्ष 1992 में गठित नववर्ष समारोह समिति ने राजस्थान सरकार से वर्षों से यह मांग की थी कि राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च की बजाय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (नव संवत्सर) पर मनाया जाए। समिति ने तर्क दिया कि स्थापना दिवस का वास्तविक महत्त्व इस तथ्य में निहित है कि राजस्थान की स्थापना इसी दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार शुभ समय पर हुई थी।
- चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का महत्त्व:
-
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वर्ष का वह दिन होता है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण चक्र पूरा करती है, जिससे दिन और रात बराबर होते हैं।
-
यह संतुलन और नई शुरुआत का प्रतीक है।
-
- राजस्थान की स्थापना
- 14 जनवरी, 1949 को उदयपुर की एक सार्वजनिक सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर रियासतों के सैद्धांतिक रूप से विलय की घोषणा की थी।
- सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर में 30 मार्च, 1949 को एक समारोह में वृहद् राजस्थान का उद्घाटन किया था, इसलिये राजस्थान दिवस हर वर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है।
- आज़ादी के वक्त राजस्थान में कुल 22 रियासतें थी। वर्तमान राजस्थान में तत्कालीन 19 देसी रियासतों में राजाओं का शासन हुआ करता था। जबकि, तीन रियासतों (नीमराना, लव और कुशालगढ़) में चीफशिप थी। यहाँ के अजमेर-मेरवाड़ा प्रांत पर ब्रिटिश शासकों का राज था।
- भारत सरकार ने अफज़ल अली के नेतृत्व में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर ब्रिटिश शासित अजमेर-मेरवाड़ा प्रांत का 1 नवंबर, 1956 को राजस्थान में विलय कर लिया।
- इस दौरान ही मध्य प्रदेश की मंदसौर तहसील के गाँव सुनेलटप्पा को भी राजस्थान में शामिल किया गया। जबकि, राजस्थान के झालावाड़ ज़िले के गाँव सिरोंज को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया।
- भारत सरकार की गठित राव समिति की सिफारिशों के आधार पर 7 सितंबर, 1949 को जयपुर को राजस्थान राज्य की राजधानी बनाया गया।
- राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल तीन लाख 42 हज़ार 239 वर्ग किलोमीटर है। यह देश का 1/10 भूभाग है।


राजस्थान Switch to English
राजस्थान को टीबी उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार
चर्चा में क्यों?
24 मार्च, 2025 को विश्व टीबी दिवस के अवसर पर राजस्थान को टीबी उन्मूलन की दिशा में किये गए विशेष प्रयासों के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
मुख्य बिंदु
- मुद्दे के बारे में:
- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राजस्थान को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में देशभर में तीसरा स्थान प्राप्त करने पर यह पुरस्कार प्रदान किया।
- टीबी मुक्त भारत अभियान और टीबी मुक्त ग्राम पंचायत जैसी पहलों को साकार करने में राजस्थान ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
- प्रमुख शासन सचिव ने जानकारी दी कि टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत वर्ष 2024 में राजस्थान की 3,355 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया, जबकि 2023 में यह संख्या 586 थी।
- इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत राजस्थान में अब तक 19,000 से अधिक निक्षय मित्र (समुदाय समर्थक) जोड़े जा चुके हैं।
प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान:
- परिचय:
- यह वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन की दिशा में देश की प्रगति में तेज़ी लाने के लिये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) की एक पहल है।
- उद्देश्य:
- टीबी रोगियों के उपचार परिणामों में सुधार के लिये अतिरिक्त रोगी सहायता प्रदान करना।
- 2025 तक टीबी को समाप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने में समुदाय की भागीदारी बढ़ाना।
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility-CSR) गतिविधियों का लाभ उठाना।
- घटक:
- नि-क्षय मित्र पहल: यह टीबी के इलाज के लिये अतिरिक्त निदान, पोषण और व्यावसायिक सहायता सुनिश्चित करता है।
- नि-क्षय मित्र (दाता) सरकारी प्रयासों के पूरक के लिये टीबी के खिलाफ प्रतिक्रिया में तेज़ी लाने हेतु स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये (व्यक्तिगत दाता के लिये), ब्लॉक/शहरी वार्डों/ज़िलों/राज्यों के स्तर पर सहायता करते हैं।
- नि-क्षय डिजिटल पोर्टल: यह टीबी से पीड़ित व्यक्तियों के लिये सामुदायिक सहायता के लिये एक मंच प्रदान करेगा।
- नि-क्षय मित्र पहल: यह टीबी के इलाज के लिये अतिरिक्त निदान, पोषण और व्यावसायिक सहायता सुनिश्चित करता है।
- ‘क्षय रोग’ (TB)
- परिचय: टीबी या क्षय रोग ‘माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस’ नामक जीवाणु के कारण होता है,
- यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है।
- यह एक इलाज योग्य और साध्य रोग है।
- संचरण: टीबी रोग हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जब ‘पल्मोनरी टीबी’ से पीड़ित कोई व्यक्ति खाँसता, छींकता या थूकता है, तो वह टीबी के कीटाणुओं को हवा में फैला देता है।
- लक्षण: ‘पल्मोनरी टीबी’ के सामान्य लक्षणों में बलगम, कई बार खून के साथ खाँसी और सीने में दर्द, कमज़ोरी, वज़न कम होना, बुखार और रात को पसीना आना शामिल है।
- वैक्सीन: बैसिल कैलमेट-गुएरिन (BCG) टीबी रोग के लिये एक टीका है।
- परिचय: टीबी या क्षय रोग ‘माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस’ नामक जीवाणु के कारण होता है,



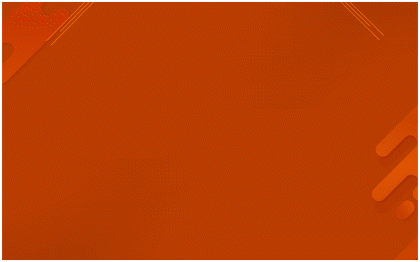


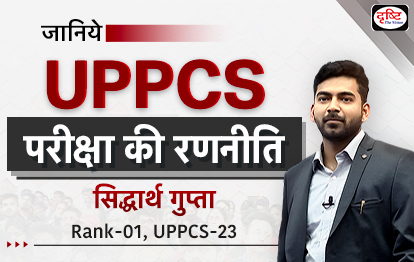
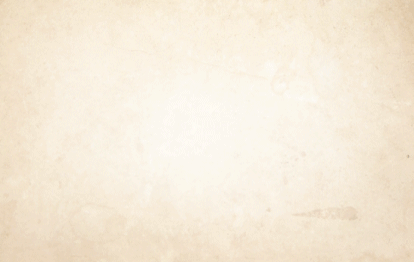
.jpg)
.jpg)
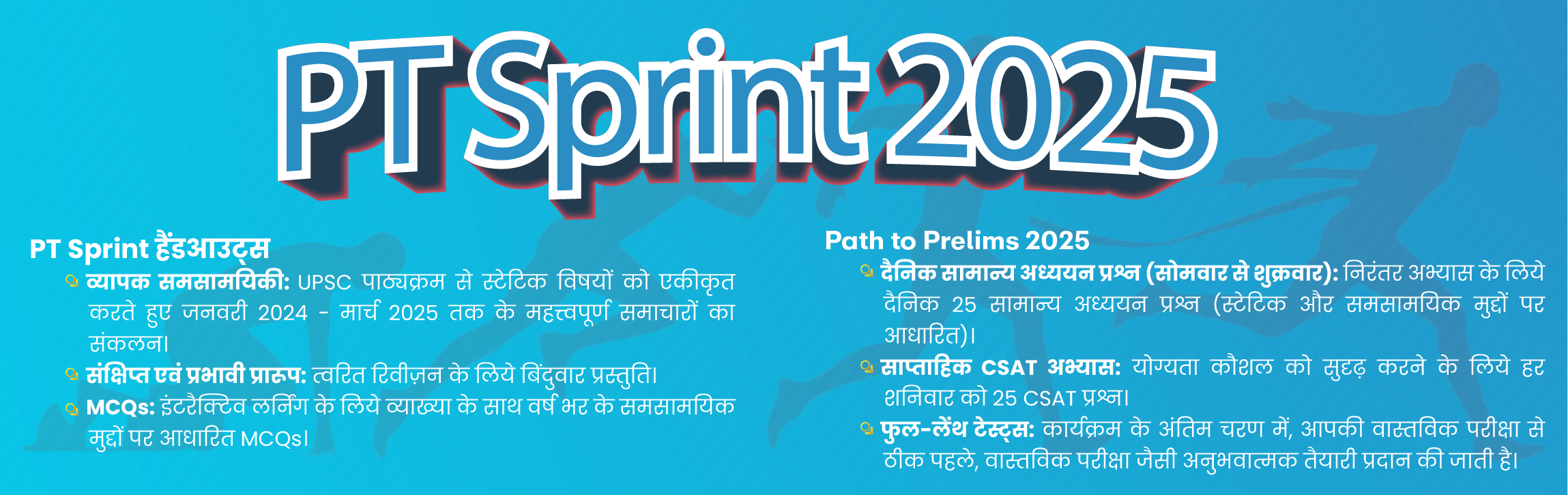
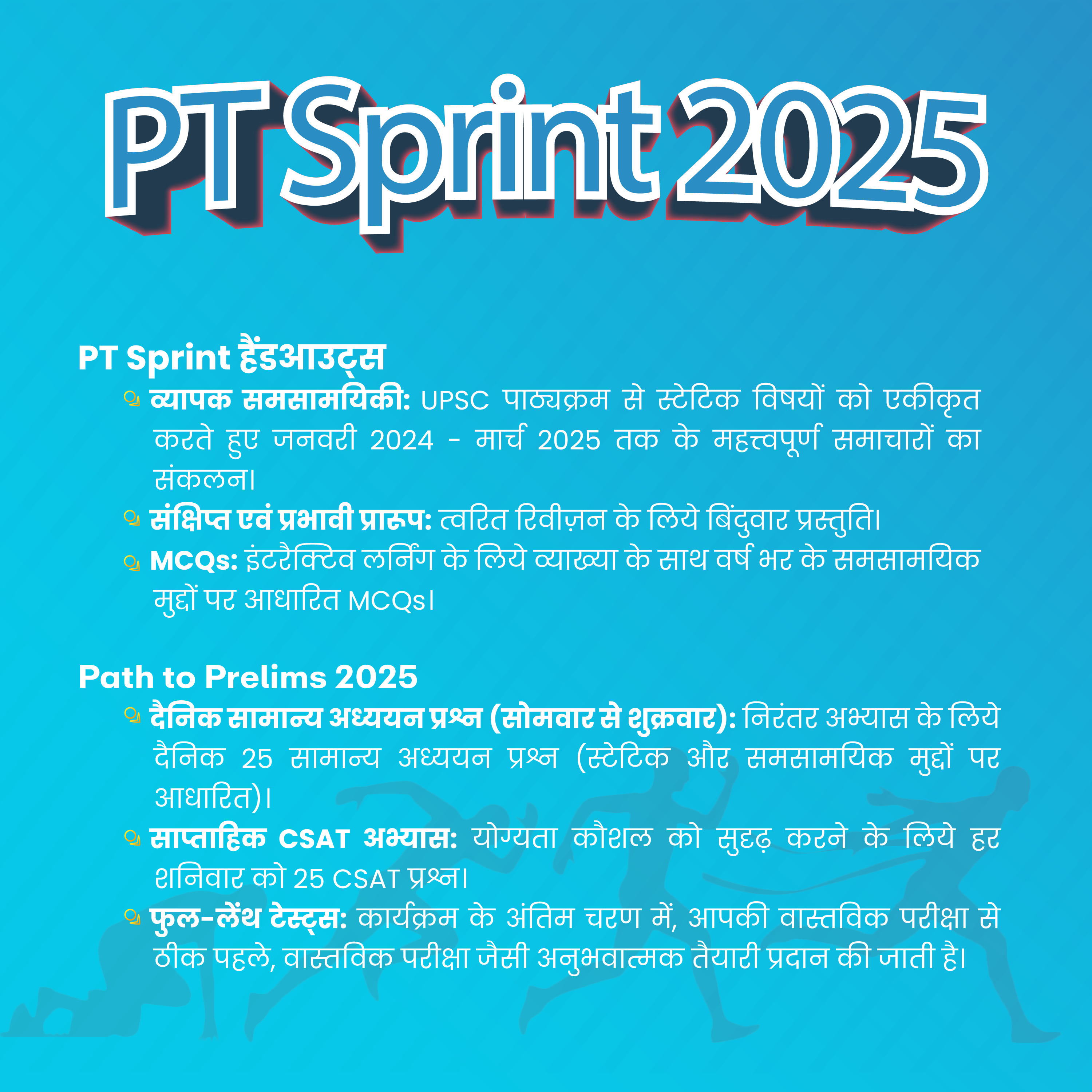

%201.jpeg)
.jpg)


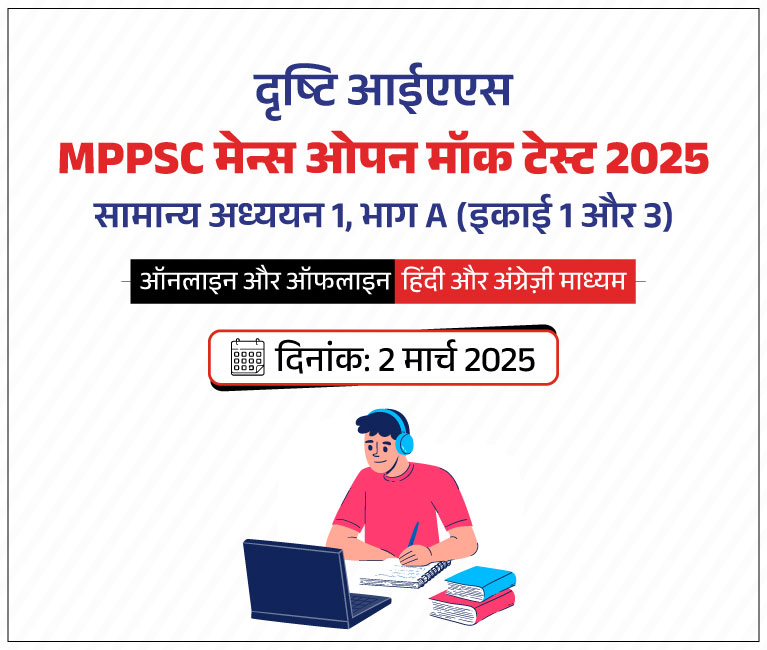
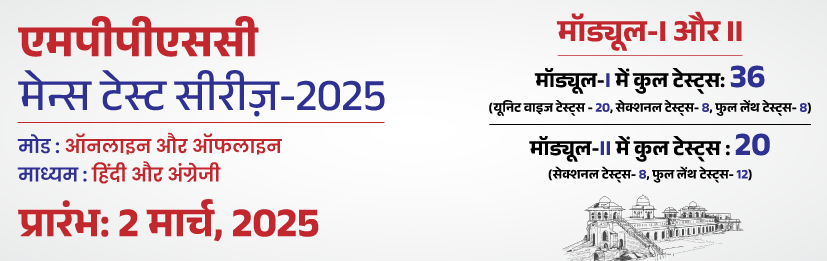

%20MPPCS%202025%20Desktop%20H.jpg)
%20MPPCS%202025%20Mobile%20H%20(1).jpg)

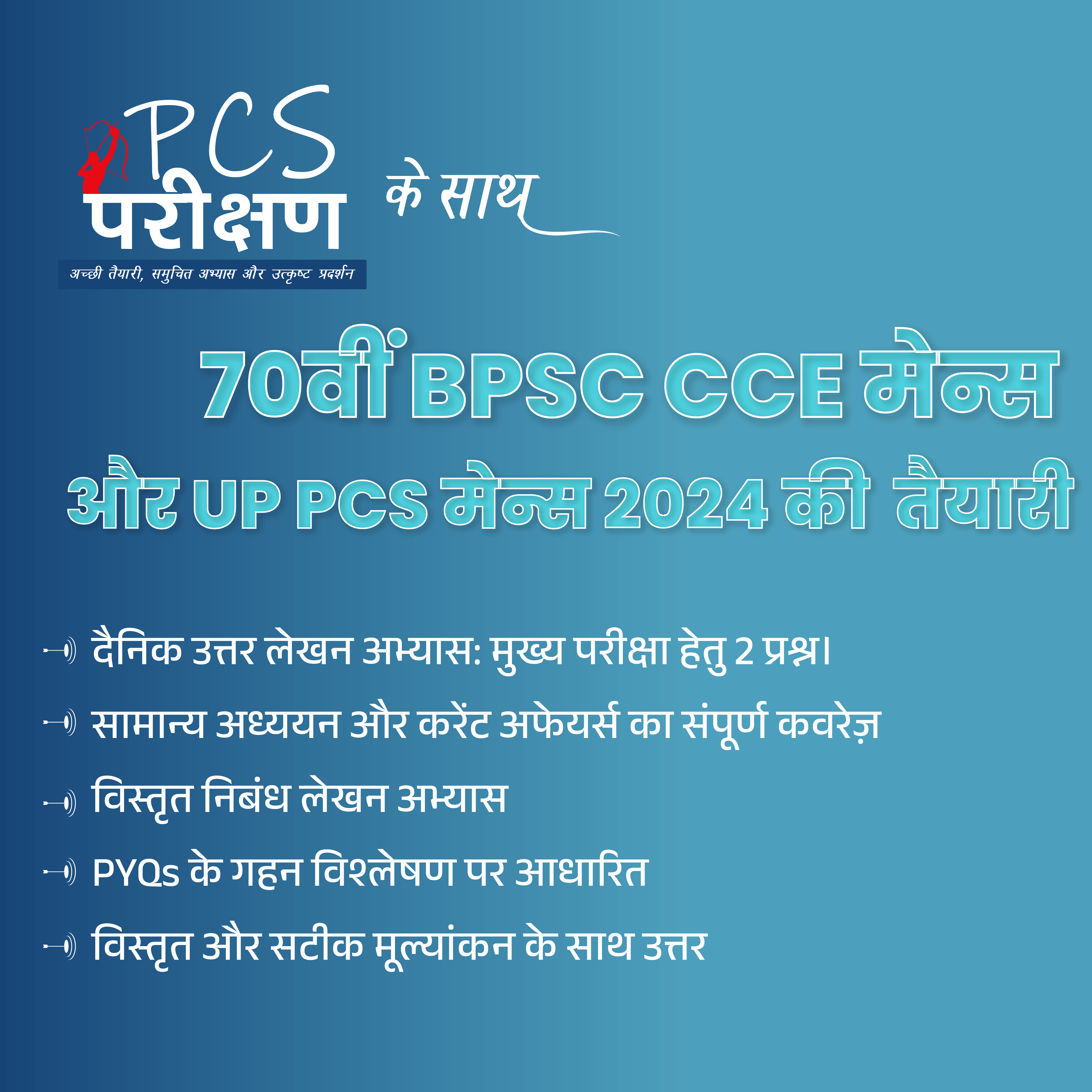


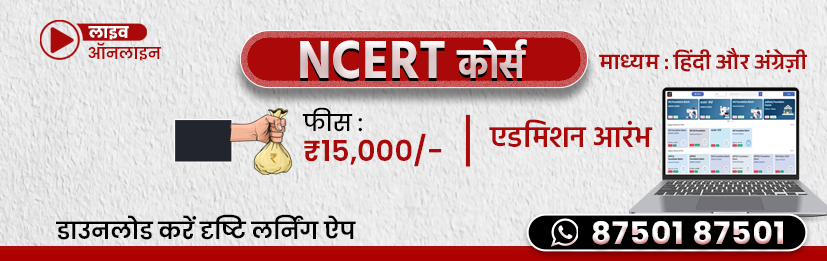
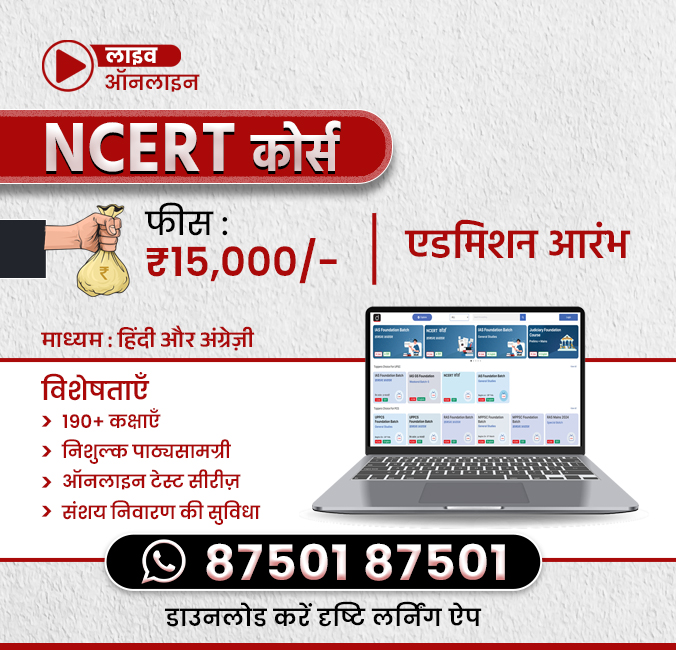

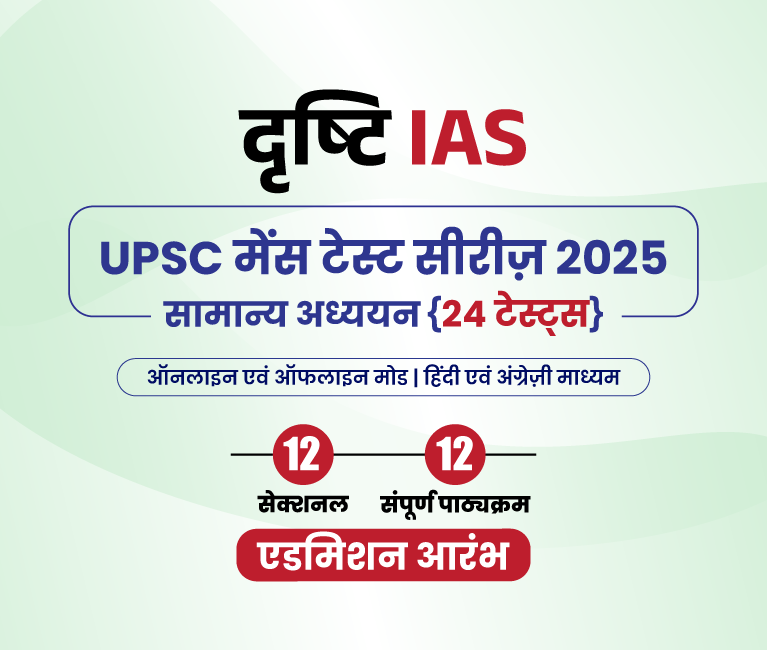
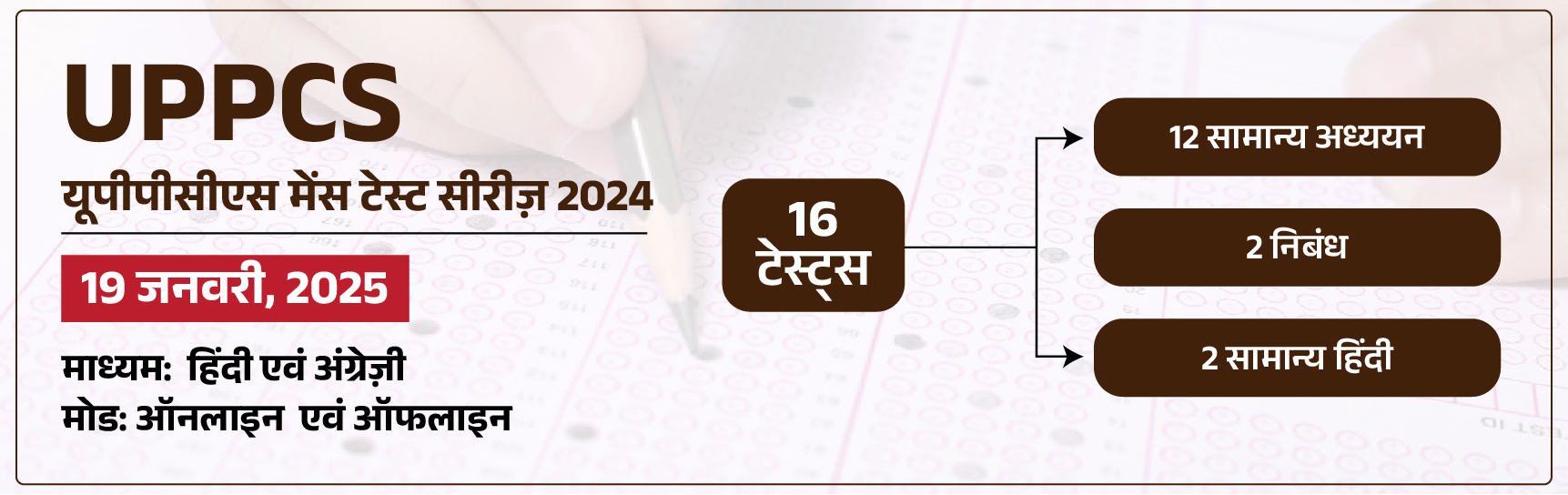
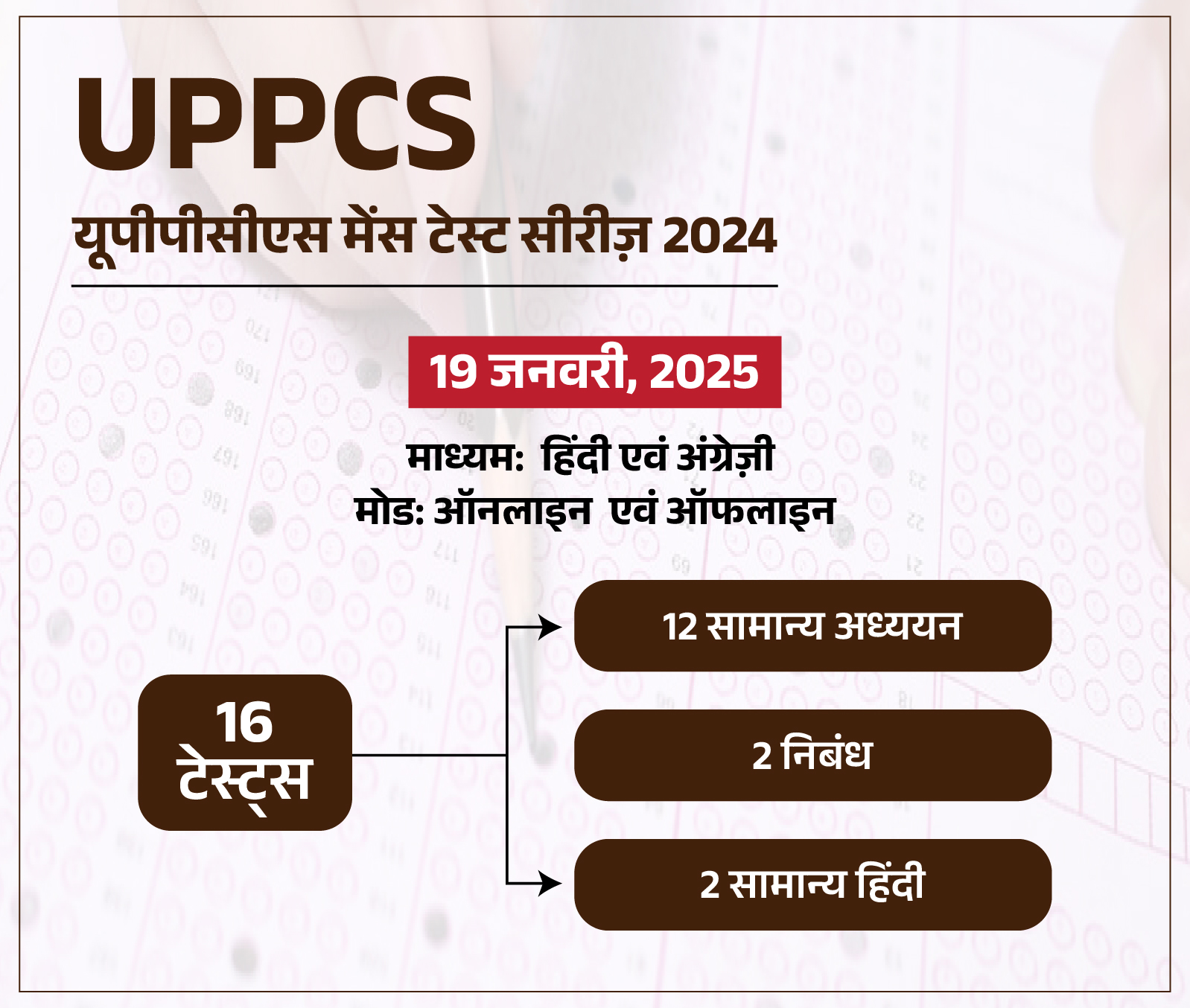



 PCS परीक्षण
PCS परीक्षण



