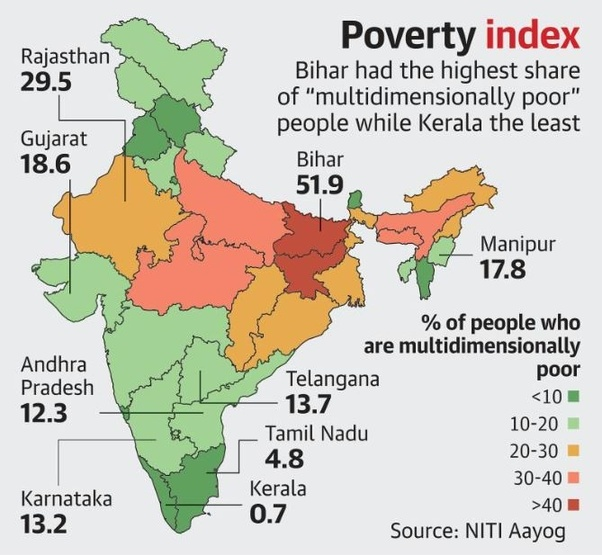दक्षिण भारतीय राज्यों की आर्थिक गतिशीलता
प्रिलिम्स के लिये:सकल राज्य घरेलू उत्पाद, LPG सुधार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, शिशु मृत्यु दर, भारतमाला परियोजना मेन्स के लिये:भारत में आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असमानताएँ, राज्य की अर्थव्यवस्थाओं में सुधार |
स्रोत: द हिंदू
चर्चा में क्यों?
मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंथा नागेश्वरन ने दक्षिण भारतीय राज्यों से अपने आर्थिक प्रदर्शन को वैश्विक मानकों के अनुरूप करने का आग्रह करने के साथ उनकी मज़बूती और सुधार के क्षेत्रों पर प्रकाश डाला। मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंथा नागेश्वरन ने इस बात पर बल दिया कि दक्षिण भारतीय राज्यों को अपने आर्थिक प्रदर्शन को अन्य भारतीय राज्यों के बजाय वैश्विक मानकों के आधार पर मापना चाहिये। उन्होंने इस क्षेत्र की आर्थिक मज़बूती के साथ सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डाला।
दक्षिण भारत के राज्यों का आर्थिक योगदान क्या है?
- आर्थिक योगदान: दक्षिण भारत के राज्यों का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 30% योगदान है, वित्त वर्ष 2024-25 में महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु और कर्नाटक सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) वृद्धि में अग्रणी रहे।
- उच्च संवृद्धि दर: वास्तविक अर्थों में दक्षिण भारत के राज्यों में 6.3% वार्षिक GSDP वृद्धि दर्ज की गई, जबकि शेष भारत में यह 5% है।
- यहाँ प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 5% से अधिक की दर से बढ़ रहा है जबकि शेष भारत में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 4.2% है।
- विनिर्माण एवं निवेश: कुल कारखानों का 37.4% और संचालित कारखानों का 37% दक्षिण भारत में स्थित हैं।
- भारत के कुल स्थायी पूंजी निवेश का 25.6% इसी क्षेत्र से संबंधित है।
- भारत का 33% विनिर्माण कार्यबल दक्षिण भारत से संबंधित है।
दक्षिणी राज्य शेष भारत से बेहतर प्रदर्शन क्यों करते हैं?
- ऐतिहासिक स्थिरता: उत्तर भारत के बार-बार होने वाले विदेशी आक्रमणों के विपरीत, दक्षिण भारत की सापेक्षिक स्थिरता ने विजयनगर, काँचीपुरम, मदुरै, महाबलीपुरम, कोच्चि और कोझीकोड जैसे प्रमुख व्यापार केंद्रों के साथ लगातार आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास को सक्षम बनाया।
- औपनिवेशिक लाभ: 18वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिण में मद्रास और बॉम्बे प्रमुख प्रेसीडेंसी शहर बन गए थे जबकि उत्तर में केवल एक (कलकत्ता) ही था।
- दक्षिण में पुर्तगाली और फ्राँसीसी प्रभाव से प्रारंभिक व्यापार तथा शहरी विकास को और भी बढ़ावा मिला।
- आर्थिक विकास: LPG सुधारों के बाद आर्थिक विकास में दक्षिणी राज्यों ने उत्तरी राज्यों को पीछे छोड़ दिया, जिससे अधिक यहाँ औद्योगिक निवेश और FDI आकर्षित हुआ।
- कर्नाटक और तमिलनाडु ऑटोमोबाइल, वस्त्र और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) उद्योगों के केंद्र बन गए, जबकि तेलंगाना एक जैव प्रौद्योगिकी और फार्मास्युटिकल केंद्र के रूप में उभरा (इसका वैश्विक वैक्सीन उत्पादन में 1/3 का योगदान है)।
- महाराष्ट्र, गुजरात और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विकास के बावजूद अन्य क्षेत्रों में असमान विकास हुआ है। दक्षिणी राज्यों के विपरीत, उत्तरी राज्यों में प्रमुख शहरी केंद्रों का अभाव है।
- पूर्वोत्तर में कई प्रमुख चुनौतियाँ (जिसमें भीड़भाड़ वाली सड़कें तथा सीमित संपर्क शामिल है) बनी हुई हैं, जो व्यापार और विकास में बाधक हैं।
- कृषि उत्पादकता: तमिलनाडु और कर्नाटक ने आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाया तथा नकदी फसलों, बागवानी और जलीय कृषि में विविधता लायी।
- उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे उत्तरी राज्य गेहूँ और चावल जैसी पारंपरिक फसलों पर बहुत अधिक निर्भर थे, जिसके कारण उत्पादकता में स्थिरता आ गई।
- शासन: तेलंगाना और कर्नाटक ने IT और ई-गवर्नेंस सुधार लागू किये जिससे उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला।
- हालाँकि, भूमि, श्रम और उद्योग में देरी से हुए सुधारों के कारण मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, नोएडा और गुरुग्राम जैसे शहरों ने दक्षिणी शहरों की तुलना में काफी विलंब से आर्थिक विकास हासिल किया।
- सामाजिक विकास: स्वतंत्रता के समय दक्षिणी राज्य अविकसित थे। नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि ने बाद में विकास के लिये बेहतर संसाधन आवंटन को सक्षम किया।
- केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में साक्षरता दर उच्च है। दक्षिण में बेहतर स्कूली बुनियादी ढाँचे और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के कारण शेष भारत की तुलना में तुलनात्मक रूप से अधिक कुशल कार्यबल उपलब्ध हुआ।
- तमिलनाडु ने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका निभाई, जिससे स्कूल में नामांकन बढ़ा, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने अंग्रेज़ी माध्यम शिक्षा के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया है।
- भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर (96.2%) के साथ केरल ने अत्यधिक कुशल कार्यबल विकसित किया है।
- उत्तरी राज्यों में खराब प्रदर्शन का कारण शिक्षा और बुनियादी ढाँचे में अपर्याप्त निवेश है, जो राजनीतिक उपेक्षा से प्रेरित है।
- केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में साक्षरता दर उच्च है। दक्षिण में बेहतर स्कूली बुनियादी ढाँचे और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के कारण शेष भारत की तुलना में तुलनात्मक रूप से अधिक कुशल कार्यबल उपलब्ध हुआ।
- स्वास्थ्य और सामाजिक संकेतक: दक्षिणी राज्य स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्ट हैं, केरल में सबसे अच्छा बुनियादी ढाँचा है और मध्य प्रदेश (46) की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम (प्रति 1,000 जन्म पर 6) है।
- दक्षिणी भारत में मातृ मृत्यु अनुपात राष्ट्रीय औसत (वर्ष 2020 में 103) से कम है।
- प्राकृतिक कारक: बंदरगाहों की निकटता से व्यापार, निर्यात और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है (चेन्नई, कोच्चि, विशाखापत्तनम)।
- मध्यम जलवायु उत्तर में चरम मौसम की तुलना में कृषि, पर्यटन और जीवन स्थितियों को बेहतर बनाती है।
दक्षिणी राज्यों की आर्थिक वृद्धि के संबंध में चिंताएँ क्या हैं?
- विनिर्माण में उत्पादकता अंतर: दक्षिणी क्षेत्र कुल विनिर्माण उत्पादन में केवल 26% का योगदान देता है। मज़बूत कार्यबल के बावजूद विनिर्माण में निम्न उत्पादकता और दक्षता को दर्शाता है।
- कौशल विकास की कमियाँ: इस क्षेत्र में कौशल स्तर 2 कार्यबल (मध्यवर्ती कौशल) मज़बूत है, लेकिन कौशल स्तर 3 और 4 (AI, इंजीनियरिंग और उच्च तकनीक क्षेत्रों में उन्नत पेशेवर कौशल) में पिछड़ा हुआ है।
- उच्च शिक्षा और अनुसंधान में अपर्याप्त निवेश उच्च मूल्य वाले उद्योगों में नवाचार और रोज़गार सृजन को सीमित करता है।
- दक्षिणी राज्यों में घटती जनसांख्यिकी (युवा) और बेहतर अवसरों की तलाश में प्रवास के कारण स्थिति और नाजुक हो रही है, श्रमिकों की कमी का खतरा बढ़ रहा है, जिससे विकास को बनाए रखने के लिये समावेशी प्रवासी नीति की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जा रहा है।
- बुनियादी ढाँचा: शहरी भीड़भाड़ और ऊर्जा संबंधी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिये बेहतर औद्योगिक गलियारों, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और डिजिटल बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता है।
- क्षेत्रीय असमानताएँ: तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्य आर्थिक विकास में अग्रणी हैं, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे अन्य राज्यों में औद्योगिकीकरण धीमा है।
- आर्थिक अवसरों और बुनियादी ढाँचे के मामले में ग्रामीण क्षेत्र अभी भी शहरी केंद्रों से पीछे हैं।
- जलवायु परिवर्तन: दक्षिणी भारत जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, यहाँ अक्सर सूखा, चक्रवात और चरम मौसम की घटनाएँ होती हैं। कृषि और तटीय अर्थव्यवस्थाएँ विशेष रूप से जोखिम में हैं।
- नीतिगत मुद्दे: कई राज्य केंद्र सरकार से वित्तीय हस्तांतरण पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जिससे उनकी राजकोषीय स्वायत्तता कम हो रही है तथा राज्य ऋण अनुपात में वृद्धि से राज्यों पर बोझ बढ़ रहा है।
आगे की राह:
- वैश्विक बेंचमार्किंग: भारत की "सिलिकॉन वैली" बेंगलुरू, प्रौद्योगिकी के मामले में कैलिफोर्निया की तर्ज पर विकास कर रही है, इसलिये दक्षिणी राज्यों को वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा के लिये प्रयास करना पड़ा।
- उत्पादकता में वृद्धि: कार्यबल की भागीदारी को आउटपुट के साथ संरेखित करने के लिये विनिर्माण उत्पादकता में सुधार करना। कौशल उन्नयन में निवेश करना, विशेष रूप से उच्च-मूल्य विनिर्माण में और उद्योग 4.0 अपनाने को प्रोत्साहित करना।
- बुनियादी ढाँचे में सुधार: वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिये भारतमाला परियोजना के माध्यम से औद्योगिक गलियारों, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और डिजिटल बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना।
- संतुलित विकास के लिये उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम आर्थिक क्षेत्रों को जोड़ने वाले औद्योगिक गलियारों का विस्तार करना।
- पर्यटन संभावना: दक्षिणी राज्यों की समृद्ध मंदिर विरासत का लाभ उठाना तथा सतत् तटीय पर्यटन को बढ़ावा देना।
- राजस्व वृद्धि को मज़बूत करना: GST के माध्यम से कर संग्रह में वृद्धि करना तथा स्थायी राजकोषीय स्थिति के लिये उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI) को बढ़ावा देना।
- समावेशी विकास: स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) और क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) के माध्यम से कम औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करके क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना।
- उत्तरी राज्य मानव विकास को बढ़ावा देने के लिये केरल के स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा मॉडल को अपना सकते हैं, जिससे बदले में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- क्षेत्रीय संपर्क और व्यापार को बढ़ाने के लिये गंगा और यमुना जैसी प्रमुख नदियों के किनारे अंतर्देशीय जलमार्गों का निर्माण एवं विस्तार करना।
|
दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: दक्षिणी राज्यों के आर्थिक परिदृश्य पर सामाजिक विकास संकेतकों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिये। |
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2015))
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) |
एयरो इंडिया 2025 में भारत-ब्रिटेन समझौता
प्रिलिम्स के लिये:MANPADs, एडवांस्ड शॉर्ट-रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (ASRAAM), अपतटीय पवन ऊर्जा, विद्युत क्षेत्रक सुधार, इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन (ITAR), कोंकण शक्ति, अभ्यास कोबरा वाॅरियर, अजेय वाॅरियर, विश्व बैंक, ग्रीन ग्रिड पहल, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेज़िलियेंट आइलैंड स्टेट्स, COP26। मेन्स के लिये:रक्षा और हरित ऊर्जा के संबंध में भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) के बीच संबंध। |
स्रोत: बिज़नेस स्टैण्डर्ड
चर्चा में क्यों?
भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) ने रक्षा संबंधों को मज़बूत करने के लिये एयरो इंडिया 2025 में कई रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किये।
- एक अन्य घटनाक्रम में चौथी भारत-ब्रिटेन ऊर्जा वार्ता आयोजित हुई जिसमें धारणीय, लचीले और समावेशी ऊर्जा भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया गया।
भारत-ब्रिटेन संबंधों से संबंधित हाल की घटनाएँ क्या हैं?
- रक्षा:
- रक्षा साझेदारी-भारत (DP-I): इसका उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मज़बूत और सुव्यवस्थित करना है।
- रक्षा विनिर्माण: दोनों देशों ने लेज़र बीम राइडिंग MANPADs (LBRM) की आपूर्ति के लिये एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये, जिसकी शुरुआत हाई वेलोसिटी मिसाइलों (STARStreak) एवं लांचरों की प्रारंभिक डिलीवरी से हुई।
- दोनों देशों की कंपनियों द्वारा हल्की बहुउद्देशीय मिसाइलों (LMMs) का उत्पादन करने से भारतीय उद्योग ब्रिटेन की वैश्विक आपूर्ति शृंखला में शामिल हो जाएंगे।
- दोनों देश लड़ाकू विमानों को सुसज्जित करने एवं वैश्विक निर्यात को समर्थन देने के लिये हैदराबाद में भारत की पहली एडवांस्ड शॉर्ट-रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (ASRAAM) असेंबली एवं परीक्षण केंद्र स्थापित करेंगे।
- विद्युत प्रणोदन प्रणाली: दोनों देशों ने भारत के अगली पीढ़ी के लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक (LPD) बेड़े के लिये एक एकीकृत पूर्ण विद्युत प्रणोदन (IFEP) प्रणाली विकसित करने पर सहमति व्यक्त की, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक LPD वितरण करना है।
- ऊर्जा:
- ASPIRE चरण-2: भारत-ब्रिटेन एक्सेलरेटिंग स्मार्ट पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया (ASPIRE) कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू हुआ।
- ASPIRE प्रोग्राम, एक UK-भारत पहल, 24/7 विद्युत् आपूर्ति का समर्थन करता है, तथा औद्योगिक ऊर्जा दक्षता और डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देता है।
- विंड टास्कफोर्स: दोनों ने पारिस्थितिकी तंत्र, आपूर्ति शृंखला और वित्तपोषण को बढ़ाने के लिये अपतटीय पवन ऊर्जा को मज़बूत करने हेतु UK-भारत अपतटीय विंड टास्कफोर्स का गठन किया।
- दोनों ने त्वरित जलवायु परिवर्तन के लिये UK भागीदारी (UKPACT) के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम को जारी रखने की घोषणा की।
- UK PACT भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को निम्न-कार्बन, सतत् विकास की ओर बढ़ने में सहायता करता है।
- दोनों ने त्वरित जलवायु परिवर्तन के लिये UK भागीदारी (UKPACT) के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम को जारी रखने की घोषणा की।
- ASPIRE चरण-2: भारत-ब्रिटेन एक्सेलरेटिंग स्मार्ट पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया (ASPIRE) कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू हुआ।
ब्रिटेन भारत की रक्षा को कैसे मज़बूत कर सकता है?
- नई रक्षा प्रौद्योगिकियाँ: भारत-UK 2030 रोडमैप के तहत, UK जेट इंजन विकास और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सहित महत्त्वपूर्ण तकनीक प्रदान करता है।
- आत्मनिर्भरता: अगली पीढ़ी की रक्षा सेनाओं का सह-विकास करके 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' का समर्थन करता है।
- सामरिक सैन्य उपस्थिति: संयुक्त प्रशिक्षण के लिये हिंद महासागर में एक तटीय प्रतिक्रिया समूह की स्थापना करना, जिसके अड्डे ओमान, नेपाल, ब्रुनेई, डिएगो गार्सिया और सिंगापुर में होंगे।
ब्रिटेन भारत के हरित परिवर्तन का समर्थन कैसे कर सकता है?
- निवेश: ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल के माध्यम से हरित परियोजनाओं के लिये 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा विश्व बैंक की 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की गारंटी।
- अपतटीय पवन: ब्रिटेन की विशेषज्ञता भारत के वर्ष 2030 तक 30 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी।
- सामुदायिक ऊर्जा: भारतीय सौर, जल और जलवायु परियोजनाओं में 67 मिलियन यूरो का निवेश किया गया, जिससे 413 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ी और 1.14 मिलियन टन उत्सर्जन में कमी आई।
- स्वच्छ ऊर्जा पहल: ब्रिटेन का स्वच्छ ऊर्जा विकास कार्यक्रम भारत के 1.8 ट्रिलियन पाउंड के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में व्यापार विस्तार का समर्थन करता है।
- वैश्विक सहयोग: भारत-ब्रिटेन ने COP26 में हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की, जिसमें भारत ग्लासगो ब्रेकथ्रू और ज़ीरो EV घोषणा में शामिल हुआ।
भारत-ब्रिटेन संबंधों के संबंध में मुख्य बिंदु क्या हैं?
- व्यापारिक संबंध: भारत वर्ष 2024 में ब्रिटेन का 11वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था और द्विपक्षीय व्यापार 42 बिलियन पाउंड का था।
- द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिये वर्ष 2005 में भारत-ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (JETCO) की स्थापना की गई थी।
- निवेश: भारत वर्ष 2022-23 में UK का दूसरा सबसे बड़ा FDI स्रोत था।
- UK भारत का छठा सबसे बड़ा निवेशक है, जिसका FDI (अप्रैल 2000 - मार्च 2023) में 33.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कुल प्रवाह में 5.34% का योगदान देता है।
- रक्षा सहयोग: कोंकण शक्ति पहला भारत-ब्रिटेन त्रि-सेवा अभ्यास था, जिसने रक्षा संबंधों को मज़बूत किया। भारत अभ्यास कोबरा वारियर (वायु अभ्यास) में शामिल हुआ, जबकि अजय वारियर ने सेना के सहयोग को बढ़ावा दिया।
- शिक्षा: शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता पर जुलाई 2022 में हस्ताक्षर किये गए, जिससे शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- वर्ष 2022-23 में ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्रों का नामांकन 185,000 तक पहुँच गया है।
- लोगों के बीच संबंध: प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी (MMP) पर मई 2021 में हस्ताक्षर किये गए, जिससे भारत और UK के बीच पेशेवरों की आवाजाही सुगम हो सकेगी।
- G-20 बाली शिखर सम्मेलन में घोषित यंग प्रोफेशनल्स स्कीम (YPS) दोनों देशों के स्नातकों (18-30) को दो वर्ष तक रहने और कार्य करने की अनुमति प्रदान करती है।
निष्कर्ष
भारत और यूके प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, निवेश और सहयोगात्मक पहलों के माध्यम से रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा में अपनी रणनीतिक साझेदारी को गति प्रदान कर रहे हैं। अपतटीय पवन, विद्युत गतिशीलता और रक्षा विनिर्माण में उनके संयुक्त प्रयास भारत के आत्मनिर्भरता लक्ष्यों के अनुरूप हैं, जो वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए पारस्परिक आर्थिक लाभ सुनिश्चित करते हैं।
|
दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्त्व का विश्लेषण कीजिये। |
UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. हमने ब्रिटिश मॉडल के आधार पर संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन हमारा मॉडल उस मॉडल से कैसे अलग है?( 2021)
नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न: भारत और ब्रिटेन की न्यायिक व्यवस्था हाल के दिनों में अभिसरण के साथ-साथ अलग-अलग होती दिख रही है। न्यायिक प्रथाओं के संदर्भ में दोनों देशों के बीच अभिसरण एवं विचलन के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिये। (मुख्य परीक्षा, 2020) प्रश्न: भारत-प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की महत्त्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना नई त्रि-राष्ट्र साझेदारी AUKUS का उद्देश्य है। क्या यह इस क्षेत्र में मौजूदा साझेदारी का स्थान लेने जा रहा है? वर्तमान परिदृश्य में, AUKUS की शक्ति और प्रभाव की विवेचना कीजिये। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिये।) प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के पक्षकारों के सम्मेलन (COP) के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई प्रतिबद्धताएँ क्या हैं? (2021) |
प्रतिस्पर्द्धी और सहकारी संघवाद
प्रिलिम्स के लिये:प्रतिस्पर्द्धी और सहकारी संघवाद, वित्त आयोग (FC), वस्तु एवं सेवा कर (GST), सातवीं अनुसूची, अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, NMM, IIPDF, B-READY कार्यक्रम, GST परिषद। मेन्स के लिये:भारतीय अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने में प्रतिस्पर्द्धी और सहकारी संघवाद की भूमिका। |
स्रोत: बिज़नेस लाइन
चर्चा में क्यों?
सरकार ने प्रतिस्पर्द्धी एवं सहकारी संघवाद तथा इसके लाभों को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न पहलों पर ज़ोर दिया है।
प्रतिस्पर्द्धी एवं सहकारी संघवाद क्या है?
- प्रतिस्पर्द्धी संघवाद:
- परिचय: यह निवेश आकर्षित करने, शासन में सुधार करने और सेवाओं को बढ़ाने के लिये क्षैतिज (राज्य-राज्य) और ऊर्ध्वाधर (केंद्र-राज्य) प्रतिस्पर्द्धा की एक प्रणाली है।
- कार्यान्वयन: 15 वें वित्त आयोग (FC) ने राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिये कर और राजकोषीय प्रयास जैसे संकेतक पेश किये हैं, जो धन आवंटन निर्धारित करते हैं।
- राज्य-स्तरीय सुधार: केंद्रीय योजनाओं के साथ-साथ संचालित होने वाली राज्य-विशिष्ट कल्याणकारी योजनाओं के उदाहरणों में शामिल हैं:
- रायथु बंधु (तेलंगाना): किसानों के लिये प्रत्यक्ष आय सहायता योजना।
- कालिया (ओडिशा): यह केंद्रीय PM किसान योजना की पूरक किसान सहायता योजना है।
- वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन: वैश्विक निवेश आकर्षित करने पर केंद्रित।
- सहकारी संघवाद:
- विषय में: यह प्रभावी शासन, संतुलित विकास और साझा सर्वोत्तम प्रथाओं के लिये केंद्र-राज्य सहयोग को बढ़ावा देता है।
- कार्यान्वयन: वित्त आयोग का प्रदर्शन-आधारित निधि आवंटन राज्यों को राष्ट्रीय सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
- प्रमुख उदाहरणों में वस्तु एवं सेवा कर (GST), आयुष्मान भारत और PM-किसान शामिल हैं, जिनमें केंद्र-राज्य सहयोग की आवश्यकता होती है।
- अखिल भारतीय सेवाएँ (IAS और IPS) राज्यों में एक समान शासन संरचना को सक्षम बनाती हैं।
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 ने क्षेत्रीय सहयोग के लिये पाँच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की, जिससे अंतर-राज्यीय मुद्दों पर चर्चा में सुविधा हुई।
- संवैधानिक प्रावधान:
- सातवीं अनुसूची: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची प्रभावी शासन के लिये केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों को विभाजित करती है।
- फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज (अनुच्छेद 261): यह राज्यों में सार्वजनिक कृत्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों की मान्यता सुनिश्चित करता है, तथा कानूनी और प्रशासनिक एकरूपता को बढ़ावा देता है।
- अंतर्राज्यीय परिषद (ISC): अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित ISC अंतर-सरकारी विवादों को सुलझाती है और सरकारिया आयोग की सिफारिशों के अनुसार 28 मई 1990 को इसे एक स्थायी निकाय बना दिया गया।
- अंतर-राज्यीय जल विवाद (अनुच्छेद 262): संसद को अंतर्राज्यीय जल विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार है।
प्रतिस्पर्द्धी और सहकारी संघवाद के क्या लाभ हैं?
- प्रतिस्पर्द्धी संघवाद:
- आर्थिक दक्षता: यह राज्यों को उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियाँ तैयार करने की अनुमति देता है, जिससे निवेश, रोज़गार सृजन और समग्र आर्थिक विकास में वृद्धि होती है।
- नीतिगत नवप्रवर्तन: राज्य शासन मॉडल, विनियामक ढाँचे और सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालियों के साथ प्रयोग करके प्रतिस्पर्द्धा करते हैं, जिससे नवीन नीति समाधान और सर्वोत्तम प्रथाओं का विकास होता है।
- राजकोषीय अनुशासन: यह राजकोषीय अनुशासन को मज़बूत करता है, क्योंकि राज्यों को व्यवसायों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिये व्यय प्रबंधन के साथ राजस्व सृजन को संतुलित करना चाहिये, जिससे ज़िम्मेदार राजकोषीय नीतियाँ सुनिश्चित हो सकें।
- सार्वजनिक सेवा की गुणवत्ता: राज्यों के बीच प्रतिस्पर्द्धा उन्हें कुशल श्रमिकों और व्यवसायों को बनाए रखने के लिये बुनियादी ढाँचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक सेवाओं जैसी सार्वजनिक सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिये प्रेरित करती है।
- सहकारी संघवाद:
- संतुलित क्षेत्रीय विकास: यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और राज्यों में समान विकास सुनिश्चित करने में मदद करता है।
- संसाधन साझाकरण को सुगम बनाना: बुनियादी ढाँचे, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में संयुक्त पहल से संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित होता है तथा प्रयासों के अनावश्यक दोहराव को रोका जा सकता है।
प्रतिस्पर्द्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न पहल क्या हैं?
- प्रतिस्पर्द्धी संघवाद:
- निवेश अनुकूलता सूचकांक (IFI): राज्यों के निवेश आकर्षण का आकलन करने के लिये एक पारदर्शी बेंचमार्क प्रदान करने हेतु IFI को वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा।
- सार्वजनिक रैंकिंग और रैंकिंग को वित्तीय पहुँच से जोड़ने से प्रतिष्ठा संबंधी प्रोत्साहन, शासन को बढ़ाने के लिये चुनावी और आर्थिक दबाव उत्पन्न होगा।
- PPP प्रोजेक्ट पाइपलाइन: बजट 2025-26 में मंत्रालयों और राज्यों को तीन वर्षीय PPP परियोजनाओं की योजना बनाने की आवश्यकता है, जिससे बुनियादी ढाँचे के लिये निजी क्षेत्र के निवेश को कुशलतापूर्वक आकर्षित करने के लिये प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा मिलेगा।
- व्यवसाय सुधार कार्य योजना (BRAP): BRAP रैंकिंग और कार्यान्वयन के माध्यम से राज्य स्तरीय व्यवसाय सुधारों को आगे बढ़ाती है।
- वर्ष 2024 BRAP अनुपालन में कमी, गैर-अपराधीकरण और विश्व बैंक के B-READY कार्यक्रम के साथ संरेखण पर ज़ोर देगा।
- वित्त आयोग (FC): FC शासन, राजकोषीय अनुशासन और आर्थिक प्रदर्शन को प्रोत्साहित करते हुए न्यायसंगत वित्तीय वितरण सुनिश्चित करके सहकारी और प्रतिस्पर्द्धी संघवाद को बढ़ावा देता है।
- निवेश अनुकूलता सूचकांक (IFI): राज्यों के निवेश आकर्षण का आकलन करने के लिये एक पारदर्शी बेंचमार्क प्रदान करने हेतु IFI को वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा।
- सहकारी संघवाद:
- राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन (NMM): NMM व्यापार करने में आसानी, बुनियादी ढाँचे और निवेश आकर्षण में राज्य प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के लिये एक एकीकृत नीति ढाँचा, कार्यान्वयन रोडमैप और शासन तंत्र प्रदान करता है।
- भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (IIPDF): IIPDF वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि सभी वित्तीय क्षमता वाले राज्य राष्ट्रीय अवसंरचना विकास में समान रूप से योगदान कर सकें।
भारत में प्रतिस्पर्द्धी और सहकारी संघवाद में क्या चुनौतियाँ हैं?
- प्रतिस्पर्द्धी संघवाद:
- अर्द्ध-संघवाद: संघ अवशिष्ट सूची और समवर्ती सूची में वरीयता के माध्यम से अधिक विधायी शक्तियाँ रखता है, जो अक्सर राज्य प्राधिकरण को दरकिनार कर देता है तथा परस्पर विरोधी संघवाद का निर्माण करता है।
- कराधान विवाद: संवैधानिक प्रावधानों के कारण, जो केंद्र को धन के आवंटन पर अधिक अधिकार प्रदान करते हैं, अधिकांश कर विवादों का निपटारा उसके पक्ष में हुआ है।
- GST से राज्य की कराधान शक्तियाँ कम होने के साथ चुंगी, विलासिता और मनोरंजन कर समाप्त हुए हैं।
- अनियंत्रित प्रतिस्पर्द्धा: भारत में सब्सिडी में प्रतिस्पर्द्धा देखी जाती है। राज्य बहुत अधिक सब्सिडी के माध्यम से एक-दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं जबकि नौकरशाही बाधाओं से सुधार अप्रभावी बने रहते हैं।
- अनियंत्रित प्रतिस्पर्द्धा के क्रम में अत्यधिक कर छूट, राजकोषीय कुप्रबंधन एवं सब्सिडी पर निर्भरता बढ़ने से स्थिरता को खतरा हो सकता है।
- वित्त आयोग और GST परिषद के बीच टकराव: अनुच्छेद 269A(1) के तहत GST परिषद को अंतर-राज्यीय व्यापार के लिये कर-साझाकरण की सिफारिश करने का अधिकार मिलता है, लेकिन अनुच्छेद 270(1A) और 270(2) में कहा गया है कि GST कानूनों के तहत लगाए गए करों को वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार साझा किया जाएगा, न कि GST परिषद के अनुसार।
- इससे सहकारी संघवाद (GST) और प्रतिस्पर्द्धी संघवाद (FC) दोनों में असंतुलन पैदा होता है।
- सहकारी संघवाद:
- केंद्रीय कर राजस्व का असमान वितरण: पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों का तर्क है कि समान वित्तपोषण से आर्थिक असमानताओं की अनदेखी होती है तथा वे विकास और निवेश के लिये विशेष वित्तीय सहायता की मांग करते हैं।
- बेहतर बुनियादी ढाँचे, कुशल श्रम एवं पूंजी के कारण धनी राज्यों में अधिक निवेश आकर्षित होता है जबकि कमज़ोर राज्य इसमें पीछे रह जाते हैं।
- केंद्रीय कर राजस्व का असमान वितरण: पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों का तर्क है कि समान वित्तपोषण से आर्थिक असमानताओं की अनदेखी होती है तथा वे विकास और निवेश के लिये विशेष वित्तीय सहायता की मांग करते हैं।
आगे की राह
- नीति आयोग की भूमिका का विस्तार करना: नीति आयोग को सूक्ष्म स्तर पर योजना बनाने को प्राथमिकता देनी चाहिये तथा क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिये राज्यों के साथ सहयोग करना चाहिये।
- राज्य, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियाँ बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिये नीति आयोग के अनुरूप अपनी संस्थाएँ स्थापित कर सकते हैं।
- ISC को मज़बूत करना: कराधान, संसाधन-साझाकरण और शासन संबंधी विवादों को सुलझाने के लिये ISC को एक स्थायी निकाय बनाना चाहिये। WTO दायित्वों, संधियों और अंतर-राज्य व्यापार में राज्यों का दृष्टिकोण शामिल किया जाना चाहिये।
- आर्थिक असमानताओं का समाधान करना: नीतियों को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिये कि राज्यों की विशिष्ट आर्थिक शक्तियों और कमज़ोरियों पर विचार किया जा सके।
- उदाहरण के लिये, झारखंड को खनन एवं विनिर्माण निवेश आकर्षित करना चाहिये जबकि केरल को उच्च स्तरीय सेवा उद्योग पर बल देना चाहिये।
- परिषदों को मज़बूत करना: कर-साझाकरण संबंधी विवादों से बचने के लिये वित्त आयोग एवं GST परिषद की स्पष्ट भूमिका की आवश्यकता है। इसके साथ ही न्यायपालिका को केंद्र-राज्य संबंधों में निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिये।
- FC द्वारा सशर्त अनुदान ढाँचे को लागू करके अनावश्यक मुफ्त सुविधाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है।
|
दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत में प्रतिस्पर्द्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिये नीतिगत उपाय बताइये। |
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs)मेन्सप्रश्न: आपके विचार में सहयोग, स्पर्द्धा एवं संघर्ष ने भारत में संघीय व्यवस्था को किस सीमा तक आकार दिया है? अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिये कुछ हालिया उदाहरण उद्धृत कीजिये। (2020) |