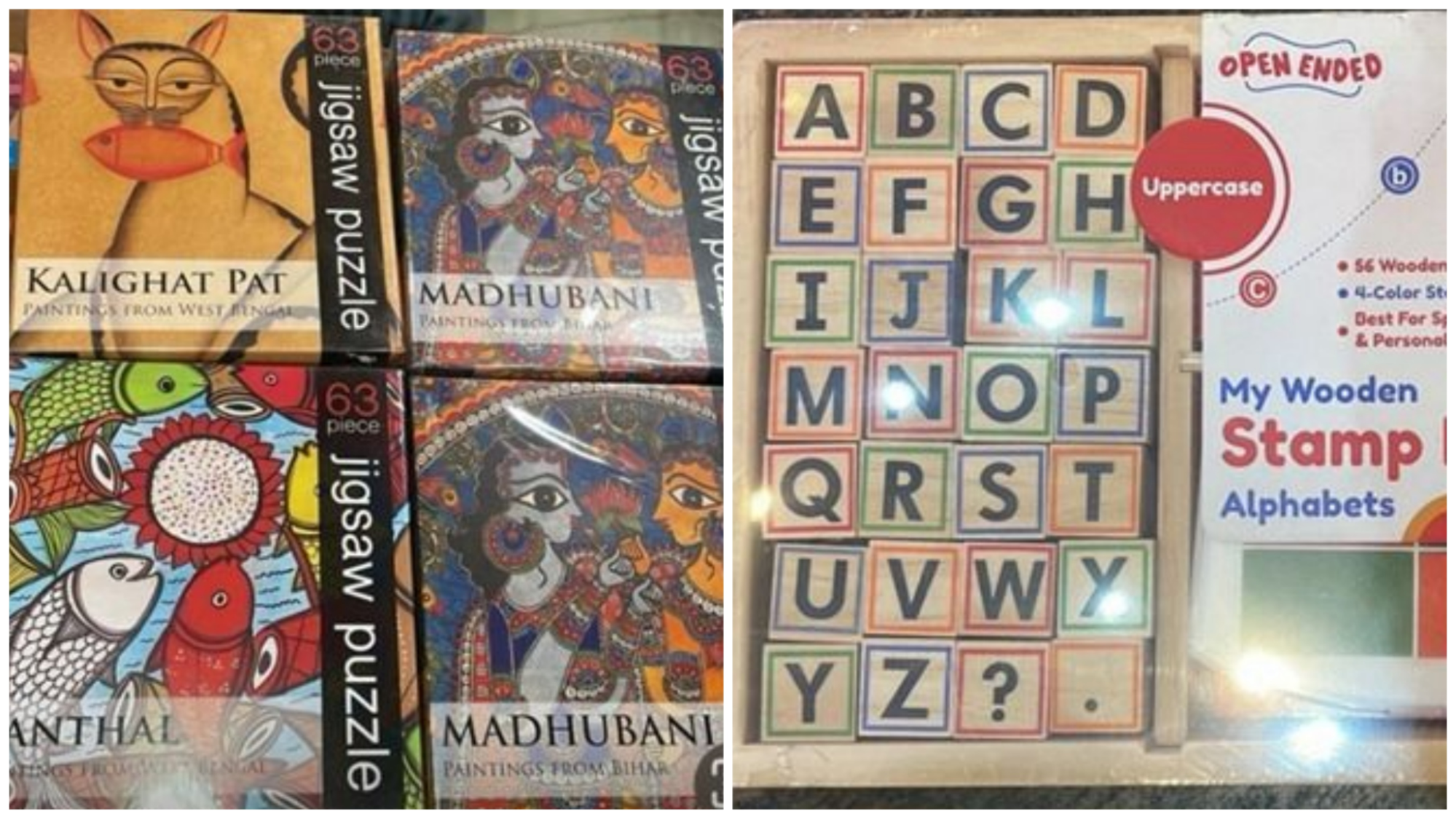उत्तर प्रदेश Switch to English
महाकुंभ में योजनाओं की प्रदर्शनी
चर्चा में क्यों?
हाल ही में महाकुंभ मेला में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित महत्त्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रदर्शनी आयोजित की गई।
मुख्य बिंदु
- प्रदर्शनी के बारे में:
- यह प्रदर्शनी महाकुंभ मेला में ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार एवं ग्रामीण विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित की गई।
- इसमें विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के बदलते परिवेश को उकेरने का प्रयास किया गया है।
- इनमें महत्त्वपूर्ण योजनाएँ निम्नलिखित हैं:
- मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्य जैसे अमृत-सरोवर, सोक पिट, रेन वाटर हर्वेस्टिंग, नालियों का निर्माण, वृक्षारोपण, पंचायत भवन आदि कराए गए। इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्र का स्वरूप बदला और विकास हुआ।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सरस हाट के माध्यम से महिलाओं के उत्पादों को प्रमोट कर उनकी आजीविका को संवर्धित किया गया। बीसी सखी और ड्रोन सखी जैसे कार्यक्रमों से महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुधार दिखाया गया।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मॉडल आवासों से ग्रामीण क्षेत्रों में आवास का बदलता स्वरूप और हर परिवार को अपना पक्का मकान देने का लक्ष्य पूरा किया गया।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 250 से अधिक आबादी वाली ग्रामीण क्षेत्रों को सभी मौसमों में चलने योग्य सड़कों से जोड़ा गया है।
- एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन प्रणाली
-
स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण
-
मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अमृत-सरोवर, सोख्ता गड्ढा, वर्षा जल संचयन, नालियों का निर्माण, वृक्षारोपण आदि विभिन्न विकास कार्य कराए गए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर बदल गई और विकास को बढ़ावा मिला।
सरस हाट के बारे में:
- यह सामान्य रूप से ग्रामीण भारत और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के जीवन को बदलने का एक कार्यक्रम है।
- मेले के दौरान, ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों और कारीगरों को शिक्षित करने के लिये उत्पाद पैकेजिंग और डिजाइन, संचार कौशल, सोशल मीडिया प्रचार और बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग पर कार्यशालाएँ आयोजित की जाएंगी।
आयोजक:
- यह ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) द्वारा पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी (CAPART) की उन्नति परिषद द्वारा आयोजित एक पहल है।
- CAPART ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है, जो सरकार और गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के बीच इंटरफेस के लिये है जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं।
उद्देश्य:
- ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को एक मंच पर लाना ताकि वे अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकें, अपने उत्पाद बेच सकें और थोक खरीदारों के साथ संबंध बनाने में उनकी मदद कर सकें।
- सरस आजीविका मेले में भागीदारी के माध्यम से, इन ग्रामीण स्वयं सहायता समूह महिलाओं को शहरी ग्राहकों की मांग और रुचि को समझने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर महत्त्वपूर्ण अनुभव प्राप्त होगा।
कुंभ मेले के बारे में
- वर्ष 2025 में महाकुंभ मेला प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आध्यात्मिक शुद्धि, सांस्कृतिक उत्सव एवं एकता के प्रतीक के रूप में लाखों तीर्थयात्री प्रतिदिन आ रहें।
- 'कुंभ' शब्द की उत्पत्ति 'कुंभक' (अमरता के अमृत का पवित्र घड़ा) धातु से हुई है।
- यह तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है जिसके दौरान प्रतिभागी पवित्र नदी में स्नान या डुबकी लगाते हैं। यह समागम 4 अलग-अलग जगहों पर होता है, अर्थात्:
- हरिद्वार में गंगा के तट पर।
- उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर।
- नासिक में गोदावरी (दक्षिण गंगा) के तट पर।
- प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक अदृश्य सरस्वती के संगम पर
कुंभ के विभिन्न प्रकार:
- कुंभ मेला 12 वर्षों में 4 बार मनाया जाता है।
- हरिद्वार और प्रयागराज में अर्द्धकुंभ मेला हर छठे वर्ष आयोजित किया जाता है।
- महाकुंभ मेला 144 वर्षों (12 'पूर्ण कुंभ मेलों' के बाद) के बाद प्रयाग में मनाया जाता है।
- प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ (जनवरी-फरवरी) महीने में माघ कुंभ मनाया जाता है।
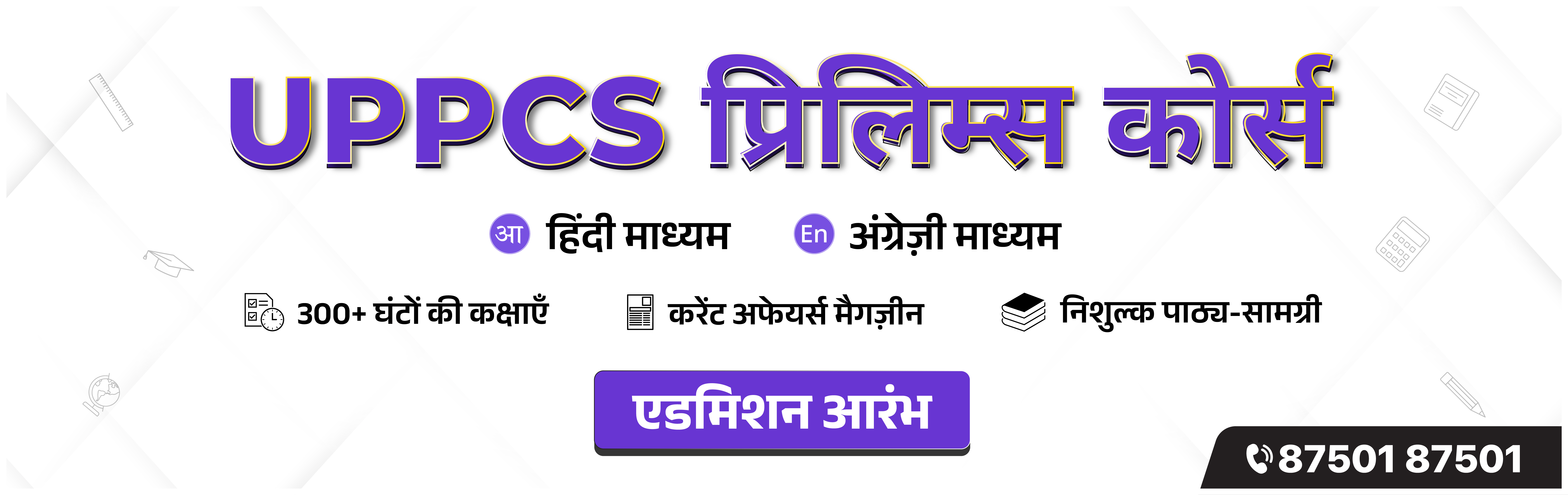

उत्तर प्रदेश Switch to English
हिंडन नदी
चर्चा में क्यों ?
हाल ही में गाज़ियाबाद में हिंडन नदी में भारी मात्रा में गाद और धार्मिक सामग्री डाल दी गई है, जो पहले से ही प्रदूषित नदी को और अधिक प्रदूषित कर रहा है।
मुख्य बिंदु
- उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने नदी के प्रदूषित होने का कारण कुप्रबंधन और पानी की गुणवत्त्ता पर ध्यान न देना तथा अनेक अनुपचारित नालों का नदी में गिरना बताया है।
- घुलित ऑक्सीजन (DO) 1.43 से 4.22 मिलीग्राम/लीटर के बीच है, जबकि जलीय जीवन के लिये न्यूनतम DO 4 मिलीग्राम/लीटर होना चाहिये।
- कुल कोलीफॉर्म का स्तर 260,000 से 380,000 MPN/100ML तक है, जबकि मानक सीमा 1,000 MPN/100 ML है।
- उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) ने नदी की जल गुणवत्ता को 'ई' श्रेणी में रखा, जिसका अर्थ है कि पानी सिर्फ सिंचाई, औद्योगिक शीतलन और नियंत्रित अपशिष्ट निपटान के लिये उपयुक्त है।
- वर्ष 2015 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने हिंडन नदी को "मृत नदी" घोषित कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि इसमें प्रदूषण का स्तर अत्यधिक है, विभिन्न भागों में यह स्नान के लिये अनुपयुक्त है।
हिंडन नदी के बारे में:
- यह नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में० लगभग 400 किमी. तक बहती हुई नोएडा में यमुना नदी में मिल जाती है।
- अतः यह यमुना नदी की एक सहायक नदी है।
- यह एक मानसून पोषित नदी है।
- इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 7,083 वर्ग किमी. है।
- काली (पश्चिम) नदी और कृष्णी नदी हिंडन नदी की मुख्य सहायक नदियाँ हैं।
- इसी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, जो 2500 ईसा पूर्व तक पुराने हैं।
- गाज़ियाबाद और नोएडा इस नदी के किनारे पर ही स्थित हैं।

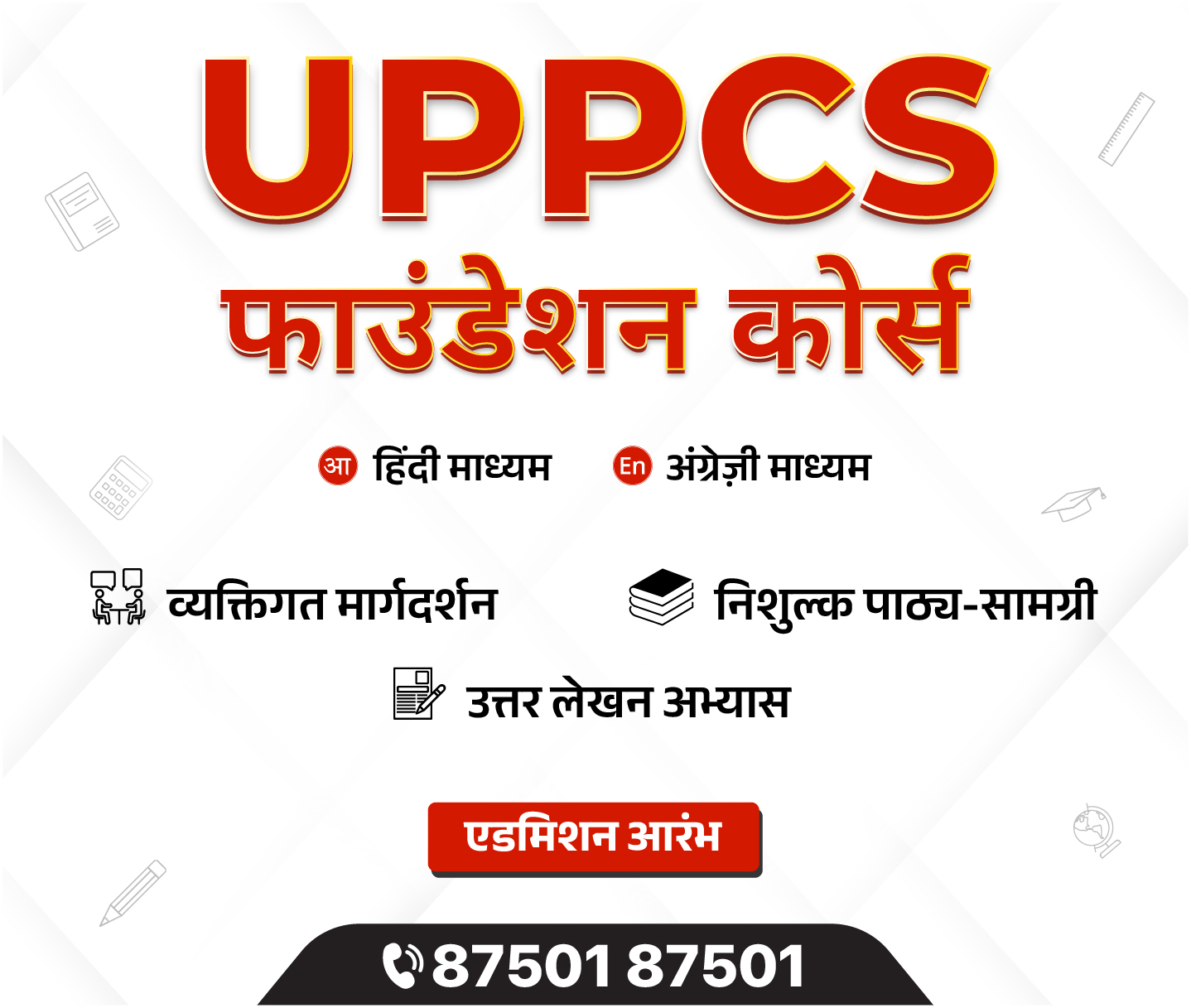
राजस्थान Switch to English
क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन
चर्चा में क्यों?
17 फरवरी 2025 को जयपुर में संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया।
मुख्य बिंदु
- सम्मेलन के बारे में:
- यह सम्मेलन गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से आयोजित किया गया।
- अतिथि: मुख्य अतिथि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जबकि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में मौजूद रहे।
- इस सम्मेलन में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से लगभग 3000 लोगों ने भाग लिया।
- सरकारी कामकाज़ में हिंदी के अधिकाधिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को सम्मानित भी किया गया।
- उद्देश्य: इस सम्मलेन का उद्देश्य सरकारी विभागों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना था।
हिंदी भाषा के बारे में:
- परिचय:
- हिंदी एक इंडो-आर्यन भाषा है, जो मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाती है। यह भारतीय संविधान के अनुसार भारत की प्रमुख राजभाषा है और यह भारतीय समाज, संस्कृति और साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है।
- यह दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और यूनेस्को महा सम्मेलन की दस आधिकारिक भाषाओं में से एक है।
- इतिहास: हिंदी का विकास संस्कृत से हुआ है और इसे भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन काल से बोला जाता है। समय के साथ, हिंदी ने फारसी, अरबी और अंग्रेज़ी भाषाओं से भी शब्द ग्रहण किये हैं, विशेषकर मुग़ल साम्राज्य और ब्रिटिश शासन के दौरान।
- लिपि: हिंदी की लिपि देवनागरी है, जो संस्कृत की लिपि से विकसित हुई है। इसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। देवनागरी लिपि का उपयोग न केवल हिंदी बल्कि कई अन्य भारतीय भाषाओं के लिये भी होता है।
- भाषायी विविधता: हिंदी भाषा में कई बोलियाँ हैं, जैसे कि अवधी, भोजपुरी, ब्रज, हरियाणवी, मारवाड़ी आदि।
- विस्तार: हिंदी न केवल भारत में, बल्कि नेपाल, पाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, फिजी और अन्य देशों में भी बोली जाती है।
- संविधान में स्थान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके अलावा, हिंदी को आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक माना गया है।


हरियाणा Switch to English
पराली जलाना
चर्चा में क्यों?
जनवरी 2025 में प्रकाशित एक अध्ययन में, जो क्षेत्र माप, वायु द्रव्यमान प्रक्षेप पथ और रासायनिक परिवहन मॉडल पर आधारित था, पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं और दिल्ली-एनसीआर में पीएम 2.5 सांद्रता के बीच कोई रैखिक सहसंबंध नहीं पाया गया।
प्रमुख बिंदु
- पराली जलाने का सीमित प्रभाव:
- शोधकर्त्ताओं ने पाया कि पंजाब और हरियाणा में फसल अवशेष जलाने से दिल्ली-एनसीआर में पीएम 2.5 का केवल 14% ही उत्सर्जन होता है, जिससे यह प्रदूषण का एक नगण्य प्राथमिक स्रोत बन जाता है।
- वर्ष 2015 से 2023 तक पराली जलाने की घटनाओं में 50% की गिरावट के बावजूद, दिल्ली-एनसीआर में पीएम 2.5 की सांद्रता काफी स्थिर रही, जो अन्य प्रमुख प्रदूषण स्रोतों का संकेत है।
- वायु प्रदूषण पर वैज्ञानिक अवलोकन:
- रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमैनिटी एंड नेचर (RIHN), क्योटो के शोधकर्त्ताओं ने पुष्टि की है कि दिल्ली-एनसीआर में पीएम 2.5 में बदलाव पंजाब और हरियाणा में आग की संख्या से सीधे संबंधित नहीं है।
- नवंबर के बाद पराली जलाना काफी हद तक बंद हो जाता है, फिर भी स्थिर हवाओं, कम ऊँचाइयों और विपरीत स्थितियों के कारण दिल्ली-एनसीआर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 2016 से हर सर्दियों में "बहुत खराब" से "गंभीर" श्रेणी में रहता है।
- प्रदूषण स्रोतों पर मुख्य निष्कर्ष:
- वर्ष 2023 में, दिल्ली-एनसीआर में रात में CO की सांद्रता दिन की तुलना में 67% अधिक होगी, जबकि 2022 में यह 48% होगी, जबकि पंजाब और हरियाणा में केवल पराली जलाने की अवधि के दौरान ही दिन-रात में स्पष्ट भिन्नता दिखाई देगी।
- यहाँ तक कि फसल अवशेष जलाने के चरम मौसम (अक्तूबर-नवंबर) के दौरान भी, स्थानीय औद्योगिक और मानव जनित स्रोत पराली जलाने की तुलना में PM2.5 में अधिक योगदान करते हैं।
- ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ( GRAP) चरण III और IV अवधि के दौरान, परिवहन और निर्माण पर सख्त नियंत्रण से पीएम 2.5 के स्तर में काफी कमी आई, लेकिन प्रतिबंध हटने के बाद प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ गया।
- दिल्ली-एनसीआर में पीएम 2.5 के प्रमुख योगदानकर्त्ता:
- परिवहन क्षेत्र – 30%
- स्थानीय बायोमास जलाना – 23%
- निर्माण एवं सड़क की धूल – 10%
- पाककला और उद्योग – 5-7%
- बेहिसाब स्रोत – 10%
- पराली जलाना – 13% (केवल अक्तूबर-नवंबर में)
- ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ( GRAP)
- के बारे में:
- GRAP में आपातकालीन उपाय शामिल हैं, जो दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में विशिष्ट सीमा तक पहुँचने के बाद वायु गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिये तैयार किये गए हैं।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2017 में GRAP को अधिसूचित किया।
- एनसीआर एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) GRAP को क्रियान्वित करता है।
- कार्यान्वयन: इसे चार चरणों में कार्यान्वित किया जाता है:
- GRAP की प्रकृति वृद्धिशील है, इसलिये जब वायु गुणवत्ता 'खराब' से 'अत्यंत खराब' हो जाती है, तो दोनों धाराओं के अंतर्गत सूचीबद्ध उपायों का पालन करना होता है।
कणिकीय पदार्थ (PM)
- पार्टिकुलेट मैटर या पीएम, हवा में निलंबित अत्यंत छोटे कणों और तरल बूंदों के जटिल मिश्रण को संदर्भित करता है। ये कण कई आकारों में आते हैं और सैकड़ों अलग-अलग यौगिकों से बने हो सकते हैं।
- पी.एम.10 (मोटे कण) - 10 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण।
- पी.एम.2.5 (सूक्ष्म कण) - 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण।
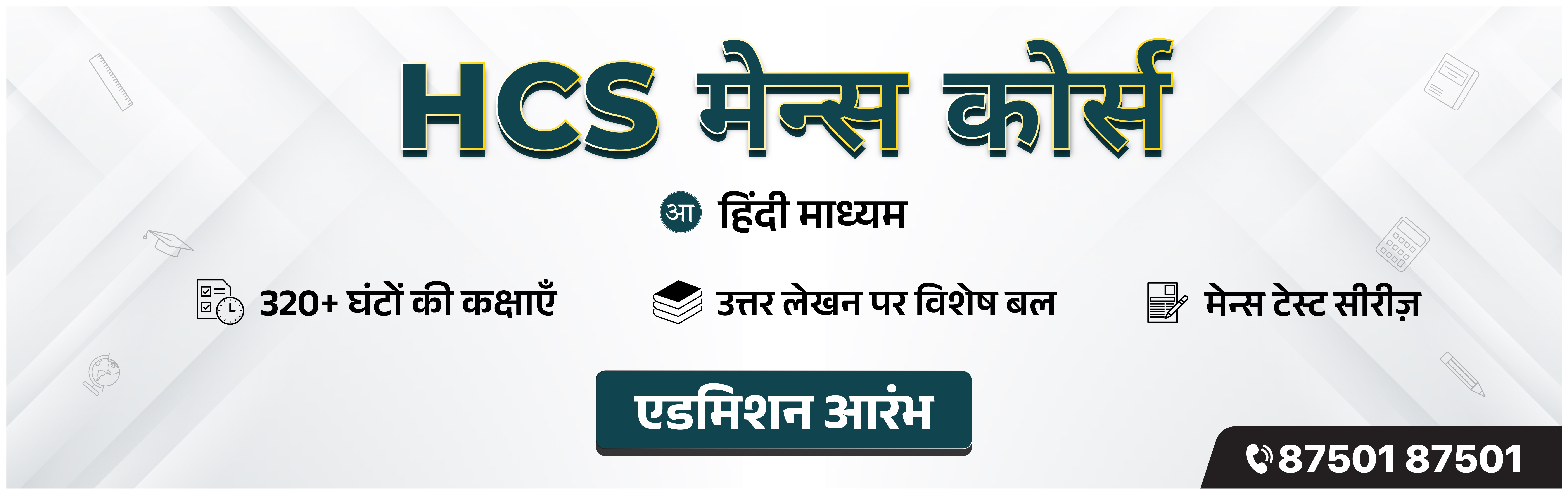

हरियाणा Switch to English
RuTAG स्मार्ट विलेज सेंटर
चर्चा में क्यों?
हाल ही में हरियाणा के सोनीपत के मंडौरा गाँव में ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्रवाई समूह (RuTAG) स्मार्ट ग्राम केंद्र (RSVC का शुभारंभ किया गया।
प्रमुख बिंदु
- RSVC के बारे में:
- RuTAG स्मार्ट विलेज सेंटर (RSVC) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़मर्रा की चुनौतियों को हल करने के लिये अभिनव समाधान प्रस्तुत करना है, जैसे पशु हस्तक्षेप को रोकना, जैविक खेती को बढ़ावा देना और बेकरी उत्पादन जैसे छोटे व्यवसायों का समर्थन करना।
- यह केंद्र किसानों, कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों को सीधे उनके दरवाज़े तक प्रौद्योगिकी समाधान उपलब्ध कराकर लाभान्वित करेगा।
- तकनीकी समाधान:
- प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के तहत विकसित, RSVC खेती के लिये उपग्रह डेटा, जल निगरानी किट, सौर ऊर्जा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स अनुप्रयोग और जैविक उर्वरक जैसी प्रौद्योगिकियों को पेश करेगा।
- इस पहल में दिव्यांग व्यक्तियों के लिये सहायक प्रौद्योगिकियाँ और वित्तीय समावेशन ऐप भी शामिल हैं, जिससे सभी के लिये आधुनिक प्रगति तक पहुँच सुनिश्चित होगी।
- यह उन्नत कृषि पद्धतियों, अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा समाधान और वहनीय आवास नवाचारों के साथ ग्रामीण चुनौतियों का समाधान करेगा।
- किसानों को उन्नत कटाई-पश्चात प्रौद्योगिकियों से लाभ मिलेगा और केंद्र नागरिक-केंद्रित ऐप्स के माध्यम से सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करेगा।
- इस पहल से बाज़ार तक पहुँच में सुधार होने से स्थानीय कारीगरों और किसानों की आय भी बढ़ेगी।
- यह केंद्र IIT मद्रास और सहायक प्रौद्योगिकी फाउंडेशन जैसे संस्थानों के साथ मिलकर बेकरी, ब्रेड बनाने और वित्तीय साक्षरता सहित विभिन्न कौशलों में व्यावहारिक समाधान और प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
- सरकारी एवं संस्थागत सहायता:
- यह पहल ग्रामीण कल्याण को बढ़ाने के लिये ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन और श्रम मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करती है।
- भारत भर में RSVC का विस्तार करने की योजना है तथा 20 और केंद्रों का विकास किया जा रहा है।
- " टेकप्रिन्योर्स" कार्यक्रम महिलाओं को अपने समुदायों में इन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिये सशक्त करेगा, जिससे स्थायित्व और दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित होगी।
ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्य समूह (RuTAG)
- RuTAG वर्ष 2004 से प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) कार्यालय की एक पहल है।
- इसकी संकल्पना ग्रामीण क्षेत्रों के लिये उच्च स्तर के विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप और समर्थन प्रदान करने के तंत्र के रूप में की गई थी।
- इस पहल के तहत, हस्तक्षेपों को मुख्य रूप से मांग-संचालित बनाया गया है, जिसमें जमीनी स्तर पर प्रौद्योगिकी अंतराल को पाटने, प्रौद्योगिकी को उन्नत करने और नवीन परियोजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण और प्रदर्शन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।


उत्तर प्रदेश Switch to English
उच्च न्यायालय के न्यायधीश को हटाना
चर्चा में क्यों?
हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विवादित बयान के बाद उन्हे पद से हटाने के लिये 55 सदस्यों की ओर से हस्ताक्षरित महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया गया है।
मुख्य बिंदु
- मुद्दे के बारे में:
- न्यायाधीश ने विगत वर्ष दिसंबर में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में कथित तौर पर कुछ सांप्रदायिक टिप्पणियाँ की थीं।
- राज्यसभा में विपक्ष के 55 सांसदों ने न्यायाधीश जाँच अधिनियम, 1968 के तहत न्यायाधीश को उनके कथित कदाचार के लिये न्यायाधीश के पद से हटाने के लिये प्रस्ताव पेश करने हेतु नोटिस दिया है।
- न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया:
- अनुच्छेद 124 और 218 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा “सिद्ध दुर्व्यवहार ” या “अक्षमता” के आधार पर हटाया जा सकता है।
- हटाने के लिये संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है:
- सदन की कुल सदस्यता का बहुमत।
- उसी सत्र में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई का विशेष बहुमत।
- संविधान में “सिद्ध कदाचार” और “अक्षमता” शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या के अनुसार दुर्व्यवहार में जानबूझकर किया गया कदाचार, भ्रष्टाचार, निष्ठा की कमी या नैतिक अधमता शामिल है।
- अक्षमता से तात्पर्य न्यायिक कार्यों में बाधा डालने वाली शारीरिक या मानसिक स्थिति से है।
- न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 के अंतर्गत प्रक्रिया:
- प्रस्ताव की सूचना:
- गठित जाँच समिति:
- यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो न्यायाधीशों और एक प्रतिष्ठित न्यायविद सहित तीन सदस्यीय समिति गठित की जाती है।
- समिति आरोपों की जाँच करती है:
- यदि न्यायाधीश को दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो प्रस्ताव निरस्त हो जाता है।
- यदि दोषी पाया जाता है तो समिति की रिपोर्ट मतदान के लिये संसद में भेजी जाती है।
- संसदीय अनुमोदन:
- राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश को हटाने के लिये दोनों सदनों को विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा।

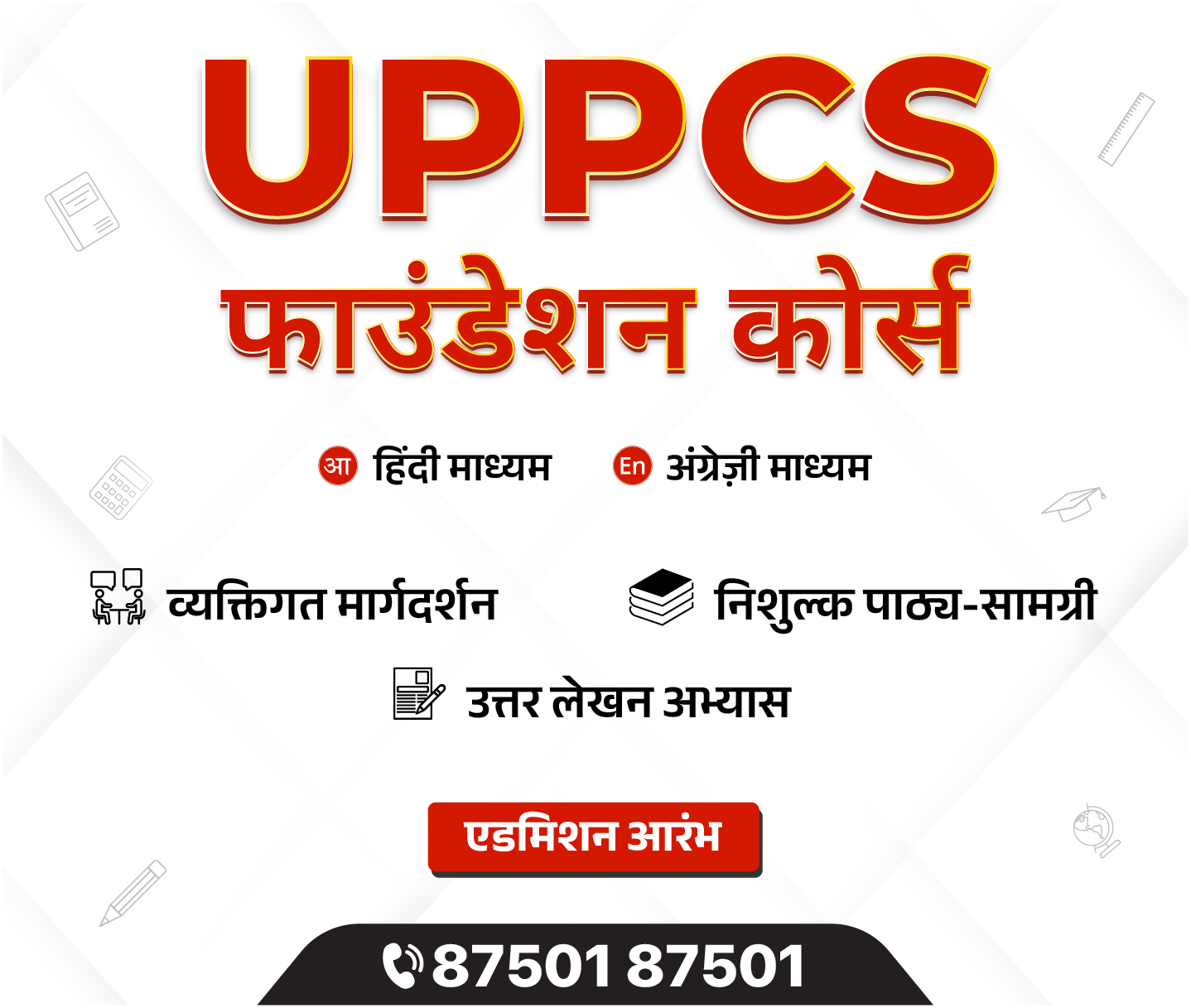
उत्तराखंड Switch to English
14वाँ मध्य कैरियर पाठ्यक्रम (चरण III)
चर्चा में क्यों?
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), भारत ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में 14वें मध्य कैरियर पाठ्यक्रम (चरण III) के भाग के रूप में भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारियों के लिये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।
प्रमुख बिंदु
- आईएफएस अधिकारियों का महत्त्व:
- NHRC के अध्यक्ष ने देश की प्राकृतिक विरासत की सुरक्षा में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया। उन्होंने विकास आवश्यकताओं और संरक्षण प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाने की उनकी जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला।
- उन्होंने अधिकारियों के लिये वन कानून के ऐतिहासिक संदर्भ, वन प्रबंधन में उभरती चुनौतियों तथा कानून, नीति और प्रवर्तन के बीच संबंधों को समझने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया ताकि वे अपने कर्त्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें।
- वन कानून का ऐतिहासिक विकास:
- अध्यक्ष ने ब्रिटिश काल से लेकर वर्तमान तक वन कानून के ऐतिहासिक विकास पर भी चर्चा की। विकास और संरक्षण के बीच बदलते संतुलन पर भी प्रकाश डाला गया।
- वन भूमि अधिग्रहण पर 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रभाव की जाँच की गई, जिसके परिणामस्वरूप अंततः वन संरक्षण अधिनियम 2023 में संशोधन किया गया।
- वन संरक्षण पर न्यायिक प्रभाव:
- अध्यक्ष ने वन संरक्षण को आकार देने में न्यायालयों की भूमिका पर ज़ोर दिया, उन्होंने वर्ष 1995 के ऐतिहासिक टी. एन. गोदावर्मन मामले का हवाला दिया। इस मामले ने वन क्षेत्र पर लकड़ी उद्योग के हानिकारक प्रभावों को कम किया।
- मज़बूत कानूनों और प्रभावी प्रवर्तन तंत्रों के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया तथा यह भी कहा गया कि 'निरंतर आदेश' के माध्यम से न्यायालय की निरंतर भागीदारी, विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने में लगातार आने वाली चुनौतियों को उजागर करती है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
- के बारे में:
- यह व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं द्वारा गारंटीकृत अधिकार, जिन्हें भारतीय न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सकता है।
- स्थापना:
- 12 अक्तूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित।
- मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 और मानव अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित।
- मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और संरक्षण देने के लिये अपनाए गए पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप इसकी स्थापना की गई।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी
- यह भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक वन सेवा प्रशिक्षण संस्थान है, जिसे मूलतः भारतीय वन महाविद्यालय के रूप में जाना जाता था, जिसकी स्थापना वर्ष 1938 में वरिष्ठ वन अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये की गई थी।
- यह वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के न्यू फॉरेस्ट परिसर में स्थित है।

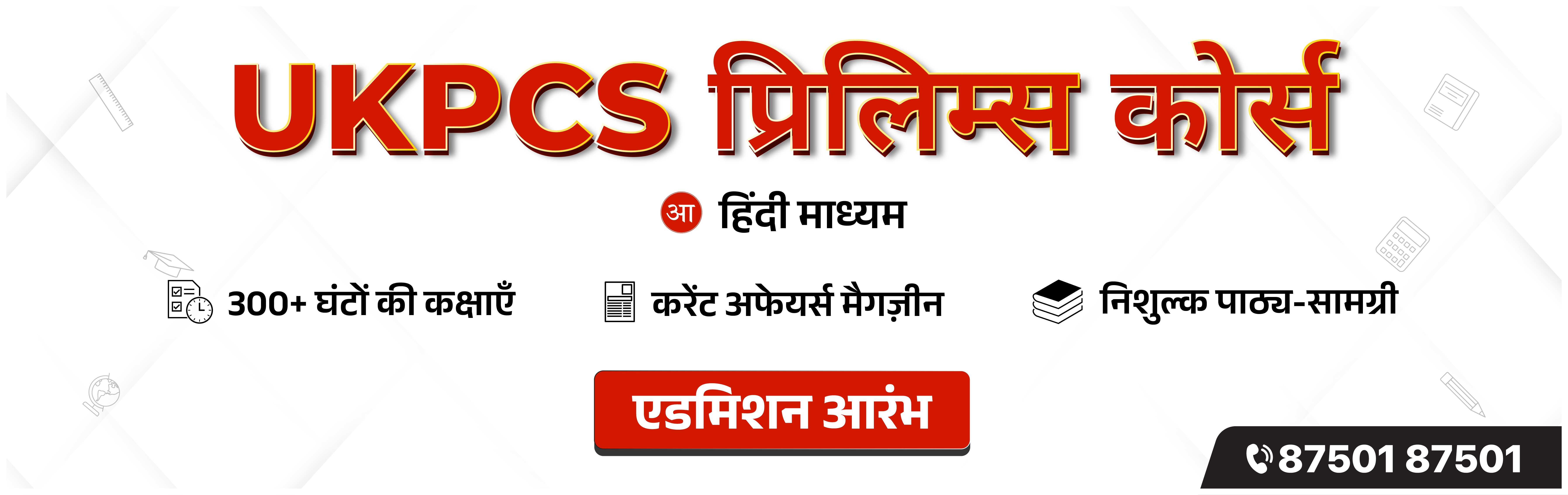
बिहार Switch to English
मधुबनी चित्रकला
चर्चा में क्यों?
यूरोपीय देश की दो दिवसीय यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने फ्राँस में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस के बच्चों को भारतीय लोक कला पर आधारित एक लकड़ी का रेलवे खिलौना सेट और एक जिग्सॉ पहेली उपहार में दीं।
मुख्य बिंदु
- उपहारों के बारे में
- लकड़ी का रेलवे खिलौना:
- प्राकृतिक लकड़ी से तैयार और पर्यावरण के अनुकूल वनस्पति रंगों से रंगा गया यह खिलौना बच्चों की सुरक्षा और पर्यावरण के प्रति जागरूकता सुनिश्चित करता है। इस लकड़ी के रेलवे खिलौने को "एक कालातीत क्लासिक" बताया गया, जो पुरानी यादों को स्थिरता के साथ जोड़ता है।
- जिग्सॉ पहेली:
- इसमें पश्चिम बंगाल की कालीघाट कला, संथाल जनजाति की संथाल पेंटिंग और बिहार की मधुबनी पेंटिंग जैसी विभिन्न लोक चित्रकला शैलियों को शामिल करके भारत की समृद्ध कला विरासत को दर्शाया गया है।
- लकड़ी का वर्णमाला सेट:
-
यह एक टिकाऊ, सुरक्षित और आकर्षक शिक्षण उपकरण है, जो कौशल और संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाता है।
-
- लकड़ी का रेलवे खिलौना:
मधुबनी कला
- उत्पत्ति: मधुबनी चित्रकला की उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई है।
- यह चित्रकला सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध भारतीय कला रूपों में से एक है, जिसका नेपाल में भी अभ्यास किया जाता है।
- मधुबनी कला के निशान भारतीय महाकाव्य रामायण में भी देखे जा सकते हैं।
- इसे मिथिला या मधुबनी कला के नाम से भी जाना जाता है।
- विशेषताएँ: ये चित्र अपने आदिवासी रूपांकनों और चमकीले मिट्टी के रंगों के उपयोग के कारण लोकप्रिय हैं।
- परंपरागत रूप से गाँव की महिलाएँ अपनी भावनाओं, आशाओं और विचारों के प्रदर्शन के रूप में अपने घरों की दीवारों पर ये चित्र बनाती थीं।
- आज मांग को पूरा करने के लिये पुरुष भी इसमें शामिल हो गए हैं।
- शैली: इसमें ज्यामितीय पैटर्न, पुष्प, पशु और पक्षी रूपांकन शामिल हैं।
- रंग: चित्रों में इस्तेमाल किये जाने वाले रंग पौधों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त प्राकृतिक अर्क से बने होते हैं। उदाहरण के लिये: काला रंग गाय के गोबर में कालिख मिलाकर बनाया जाता है; नीला रंग नील से; सफेद रंग चावल के पाउडर से; नारंगी रंग पलाश के फूलों से बनाया जाता है, आदि।


हरियाणा Switch to English
हरियाणा राज्य सूचना आयोग में लंबित मामले
चर्चा में क्यों?
सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मिले जवाब के अनुसार, हरियाणा राज्य सूचना आयोग 7,000 से अधिक अपील मामलों का लंबित निपटारा कर रहा है। अधिकारियों को सूचना देने में देरी के लिये राज्य लोक सूचना अधिकारियों पर लगाए गए जुर्माने के रूप में 2.84 करोड़ रुपए अभी भी वसूलने हैं।
प्रमुख बिंदु
- लंबित अपील मामले:
- जनवरी 2024 में मुख्य सूचना आयुक्त और सात राज्य सूचना आयुक्तों के समक्ष 8,340 अपील मामले लंबित थे।
- दिसंबर 2024 तक यह संख्या घटकर 7,216 हो गई तथा एक वर्ष में केवल लगभग 1,000 मामले ही सुलझाए गए।
- सीमित जागरूकता अभियान:
- RTI के जवाब के अनुसार, 2005 से अब तक केवल पाँच कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं, जिनमें 896 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिनमें से अंतिम कार्यशाला 2011 में पंचकूला में आयोजित की गई थी।
- जुर्माना और वसूली का विवरण:
- पिछले 20 वर्षों में आयोग ने सूचना उपलब्ध कराने में देरी के 3,611 मामलों में 5.86 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
- हालाँकि, अब तक केवल 2.84 करोड़ रुपए ही वसूले जा सके हैं।
- आयोग ने समय पर सूचना उपलब्ध न कराने के कारण 1,974 मामलों में 92 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
- पिछले 20 वर्षों में आयोग ने सूचना उपलब्ध कराने में देरी के 3,611 मामलों में 5.86 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम
- के बारे में:
- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी सूचना के लिये नागरिकों के अनुरोधों पर समय पर प्रतिक्रिया देने का प्रावधान करता है।
- सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज़ में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना तथा हमारे लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में लोगों के लिये काम करने योग्य बनाना है।
- सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019:
- इसमें प्रावधान किया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त (केंद्र और राज्य दोनों के) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक पद पर बने रहेंगे। इस संशोधन से पहले उनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित था।
- इसमें प्रावधान किया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त (केन्द्र तथा राज्य के) के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
- इसने मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के वेतन में कटौती से संबंधित प्रावधानों को हटा दिया, जो उनकी पिछली सरकारी सेवा के दौरान प्राप्त पेंशन या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के कारण होता था।
- RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 की आलोचना इस आधार पर की गई कि यह कानून को कमज़ोर करता है और केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ देता है।
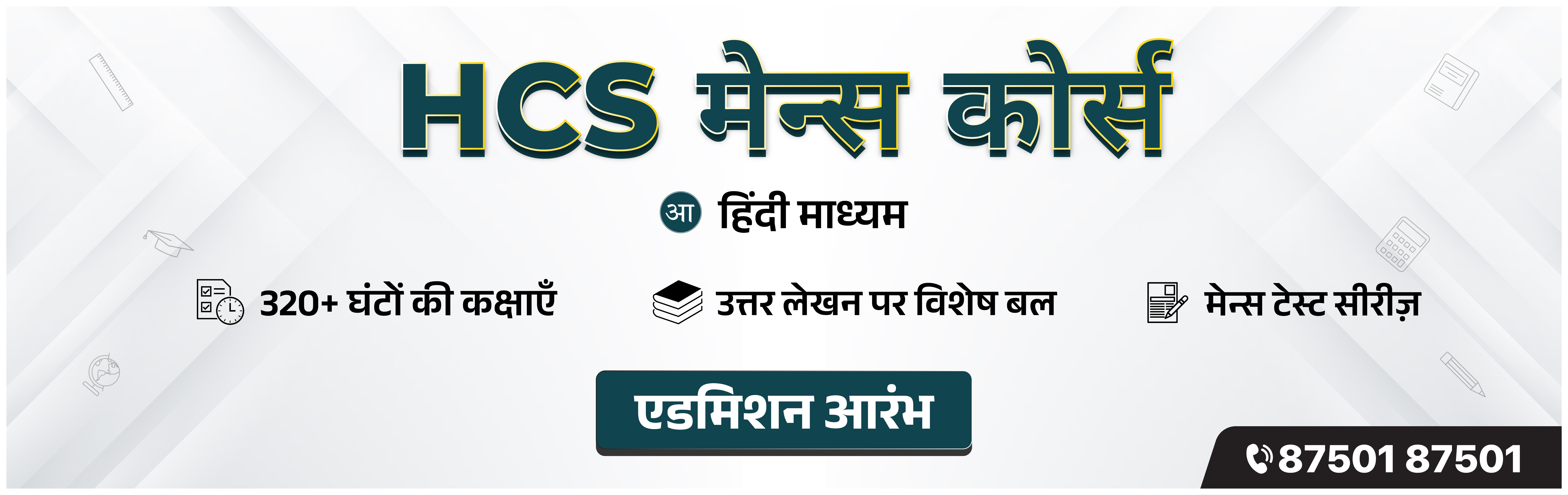


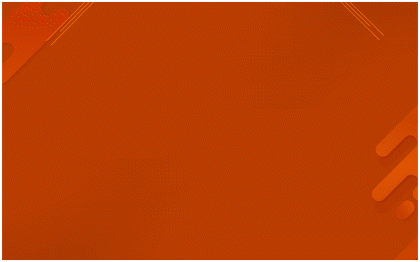


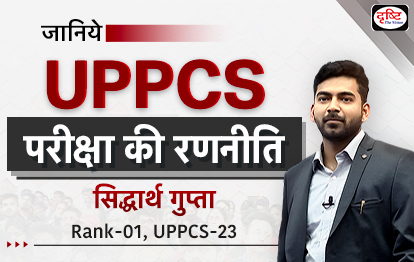
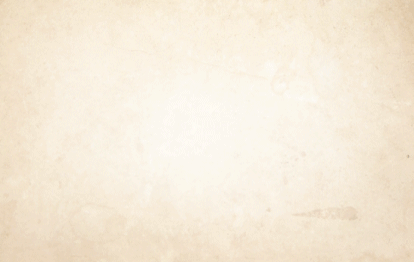
.jpg)
.jpg)
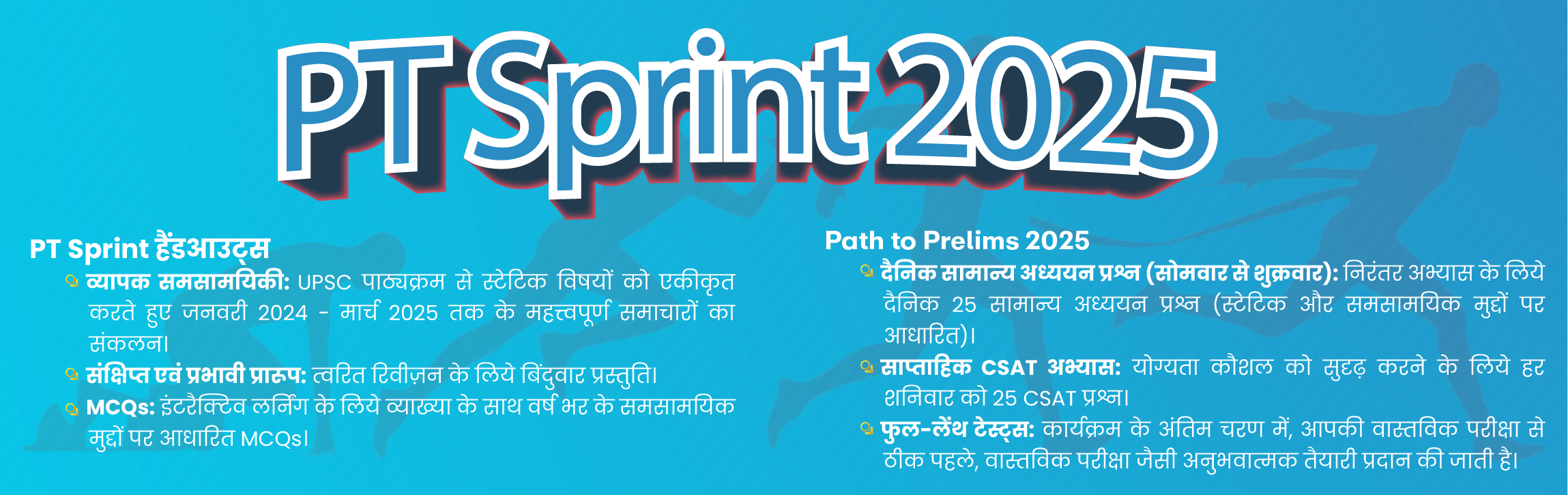
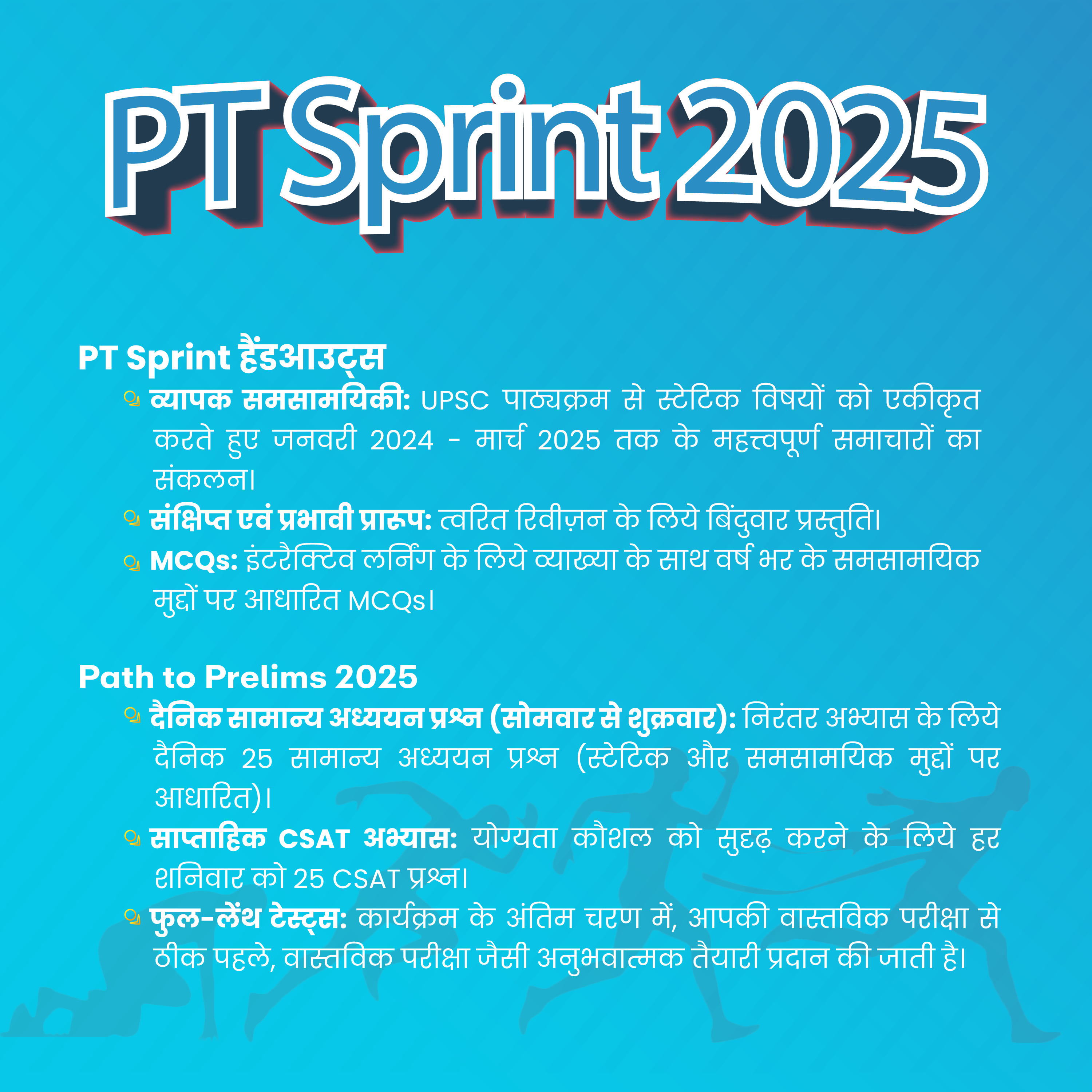

%201.jpeg)
.jpg)


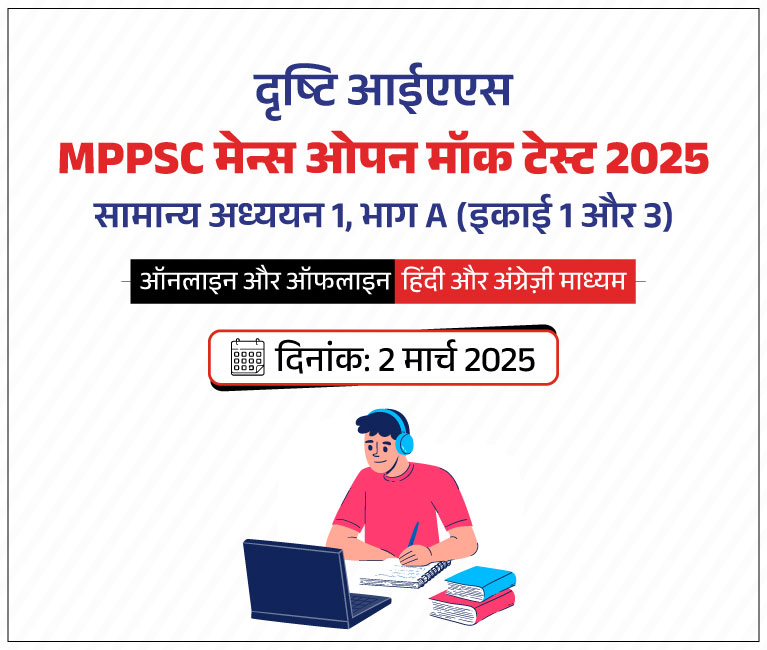
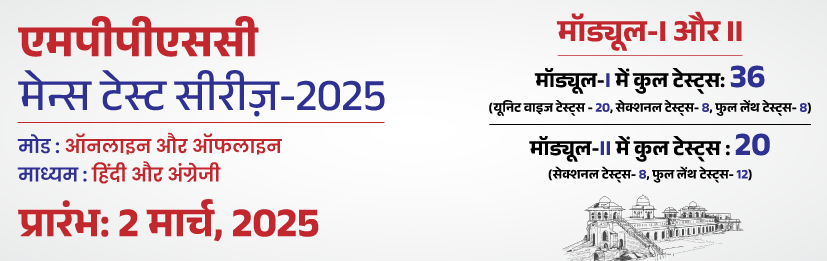

%20MPPCS%202025%20Desktop%20H.jpg)
%20MPPCS%202025%20Mobile%20H%20(1).jpg)

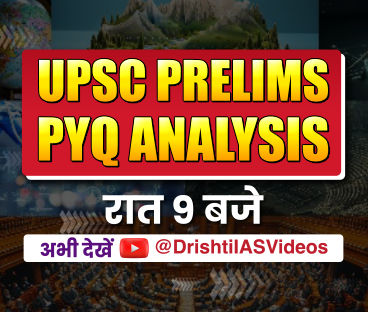

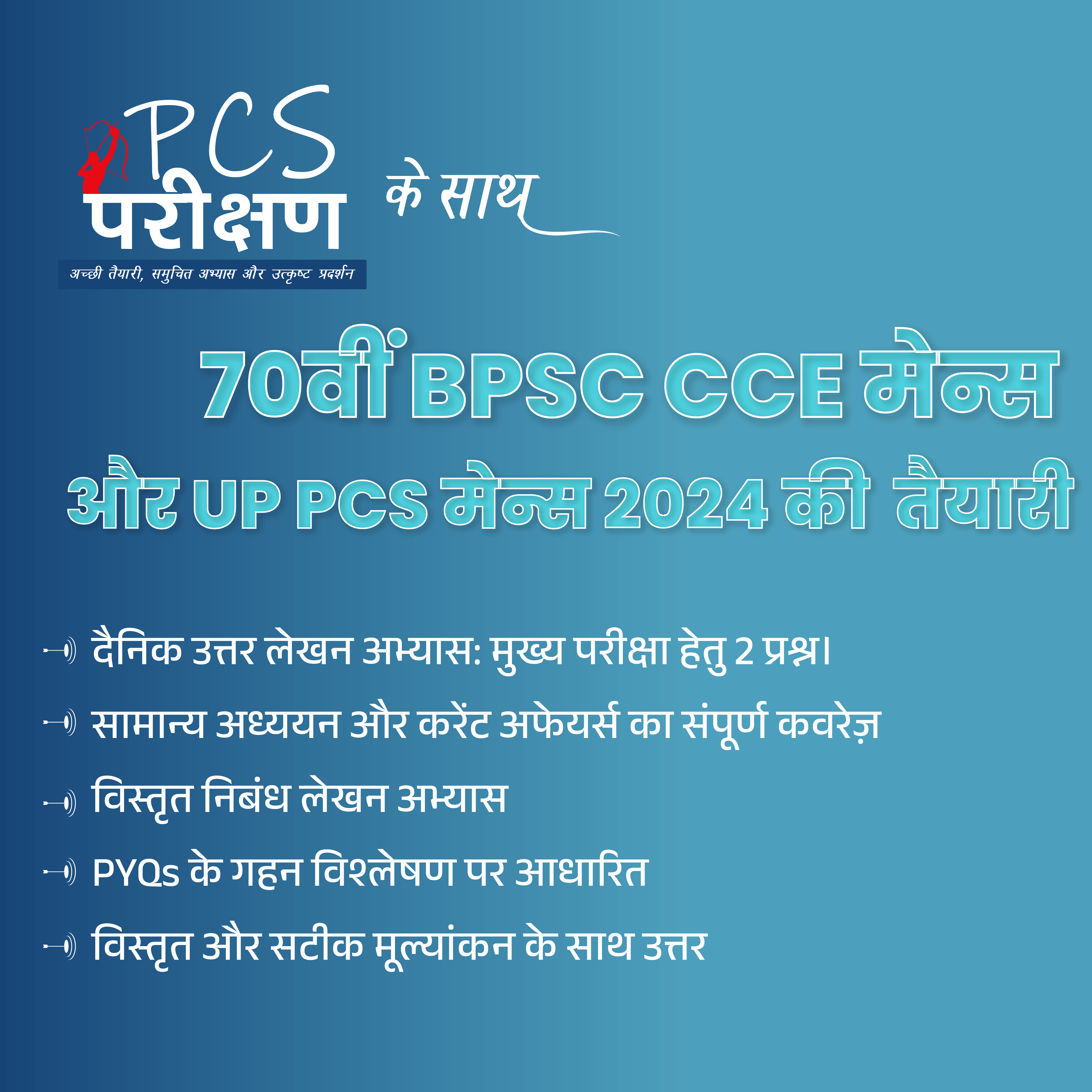


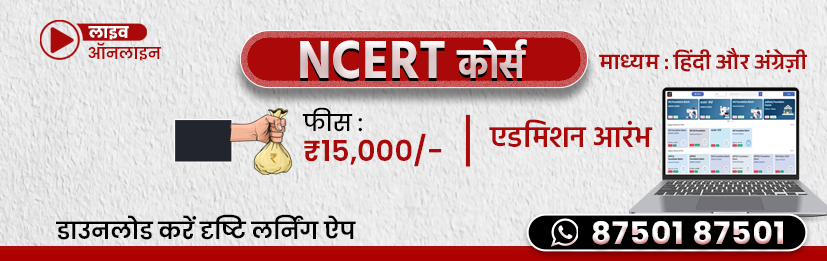
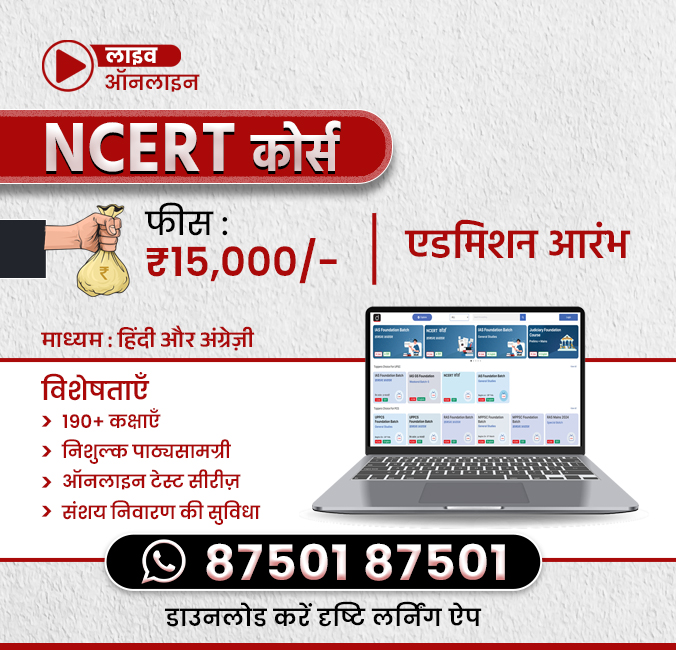

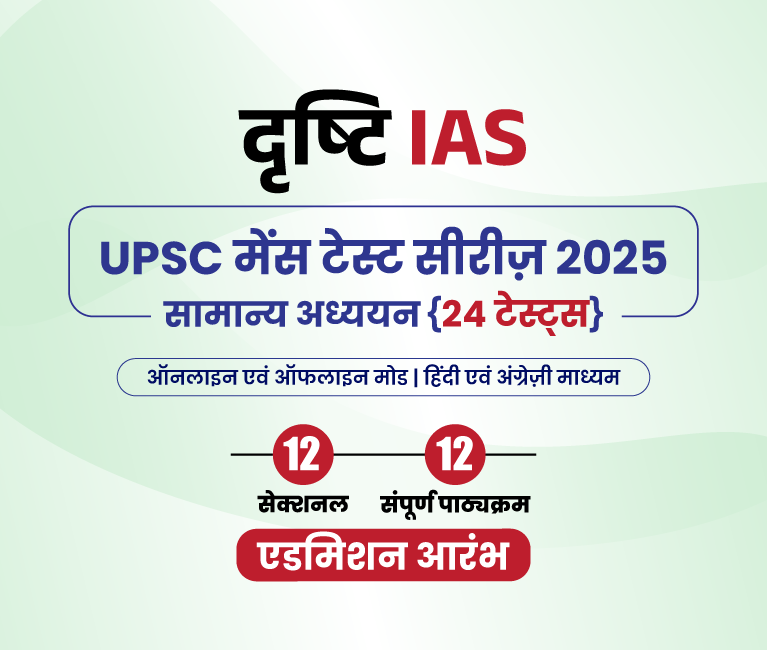
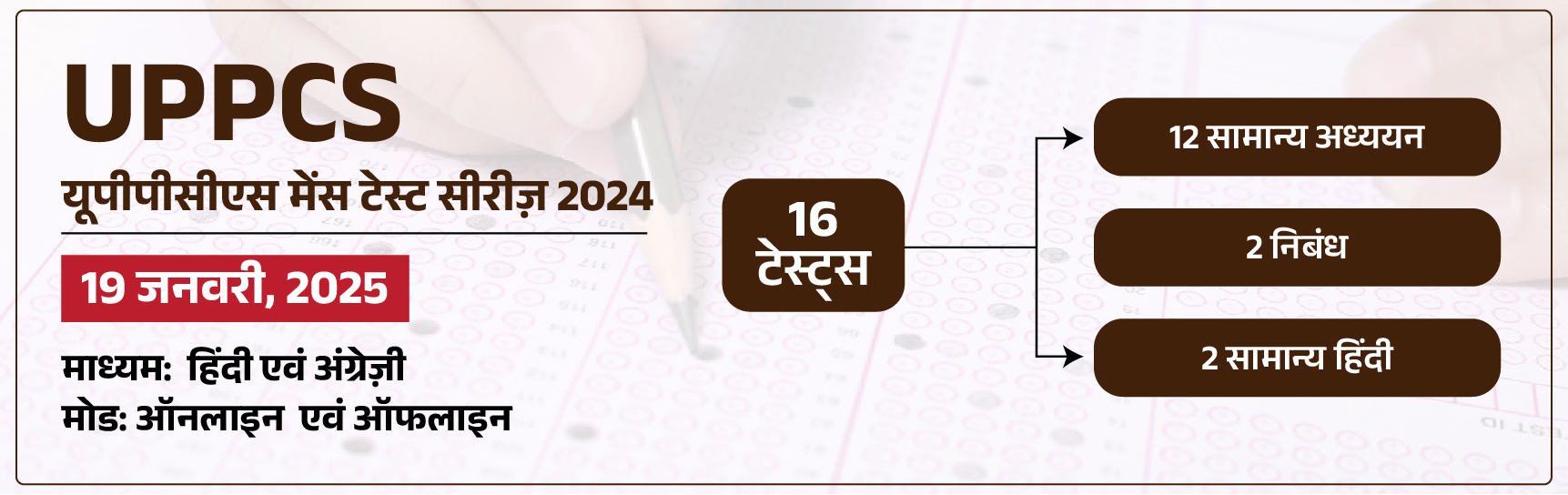
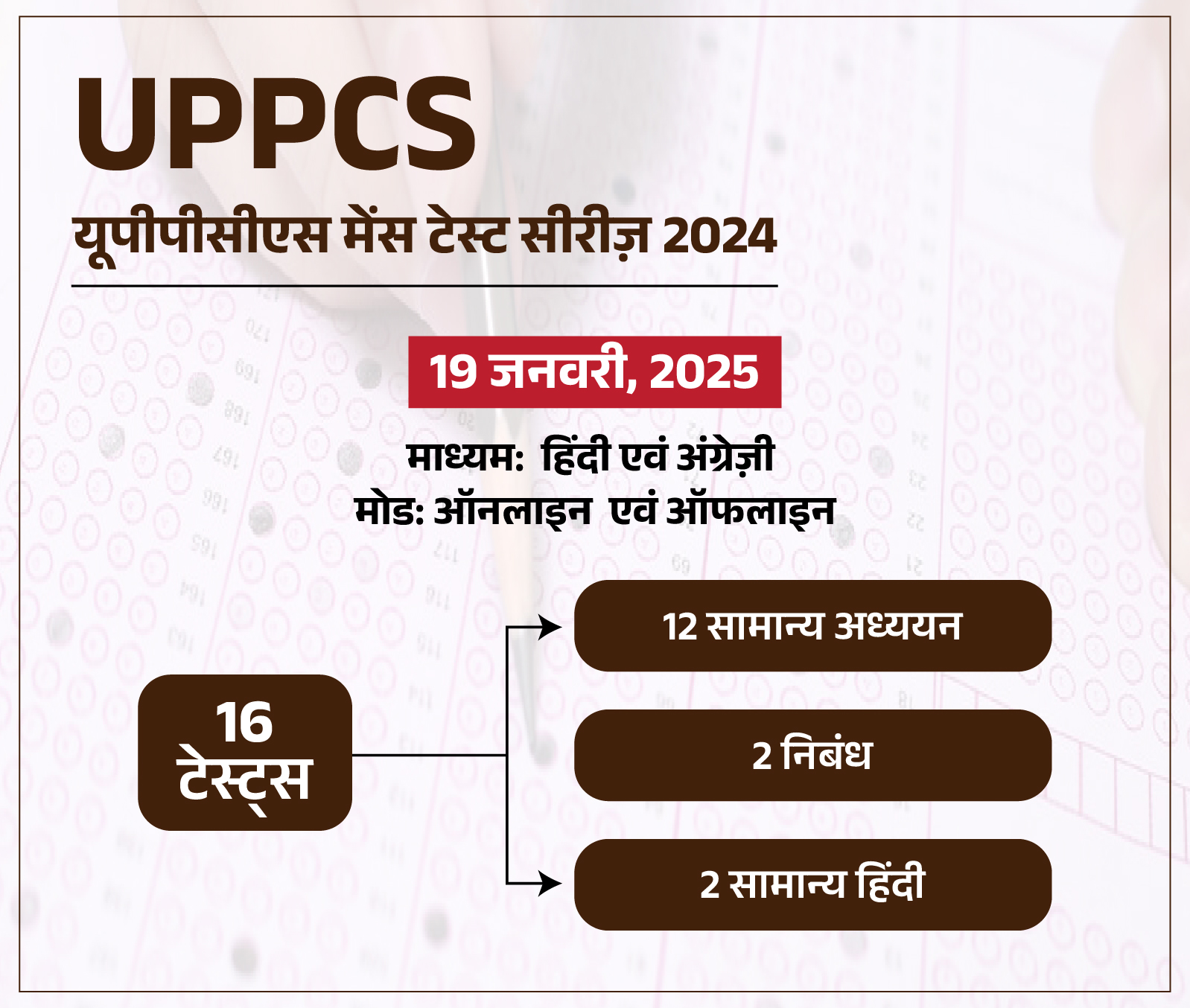



 PCS परीक्षण
PCS परीक्षण