हरियाणा Switch to English
पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन
चर्चा में क्यों?
23 फरवरी 2025 को पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह को सम्मानित करने के लिये पगड़ी संभाल दिवस मनाया।
मुख्य बिंदु
- अजीत सिंह के बारे में:
- जन्म और प्रारंभिक जीवन: अजीत सिंह का जन्म 23 फरवरी, 1881 को खटकर कलां गाँव, पंजाब (अब शहीद भगत सिंह नगर ज़िले का हिस्सा) में हुआ था।
- स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी: वह एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे और उन्होंने अपने भतीजे भगत सिंह को प्रेरित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- निर्वासन और संघर्ष: पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन में उनकी भूमिका के कारण, अंग्रेज़ो ने उन्हें निशाना बनाया और 1909 से 1947 तक निर्वासन में रहने के लिये मजबूर किया।
- वापसी और मृत्यु: वे मार्च 1947 में भारत लौट आए लेकिन 15 अगस्त 1947 को डलहौज़ी में अस्वस्थता के कारण उनकी मृत्यु हो गई। यह वही दिन था जब भारत स्वतंत्र हुआ था।
- पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन:
- प्रारंभ और अर्थ: अजीत सिंह ने वर्ष 1907 में अंग्रेज़ो द्वारा लगाए गए तीन दमनकारी कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन शुरू किया।
- "पगड़ी संभाल जट्टा" वाक्यांश का अर्थ है "अपनी पगड़ी का ध्यान रखना, हे किसान", जो आत्म-सम्मान और सम्मान का प्रतीक है।
- दमनकारी कानून:
- पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम, 1900 - किसानों के भूमि बेचने या गिरवी रखने के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया, जिससे ज़मींदारों और साहूकारों को लाभ हुआ।
- पंजाब भूमि उपनिवेशीकरण अधिनियम, 1906 - चिनाब कॉलोनी (अब पाकिस्तान में) में किसानों के उत्तराधिकारियों के बजाए अंग्रेज़ो को भूमि स्वामित्व हस्तांतरित कर दिया गया।
- दोआब बारी अधिनियम, 1907 - किसानों से भूमि स्वामित्व के अधिकार छीन लिये गए तथा उन्हें ठेका मज़दूर बना दिया गया।
- अतिरिक्त बोझ: अंग्रेज़ो ने कृषि भूमि और सिंचाई जल पर भी कर बढ़ा दिया, जिससे छोटे किसानों पर व्यापक ऋण और भूमि हानि बढ़ गई।
- आंदोलन का प्रभाव:
- बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन: इस आंदोलन के कारण बड़े पैमाने पर किसानों ने अन्यायपूर्ण कानूनों को निरस्त करने की मांग की।
- भारत माता सोसाइटी का गठन: अजीत सिंह और किशन सिंह (भगत सिंह के पिता) ने भारत माता सोसाइटी की स्थापना की, जो किसानों का समर्थन करने वाला एक क्रांतिकारी समूह था।
- नारा: राष्ट्रवादी कवि बांके दयाल ने "पगड़ी संभाल जट्टा" का नारा गढ़ा, जो अवज्ञा का प्रतीक बन गया।
- ब्रिटिश प्रतिक्रिया: बढ़ते दबाव के कारण ब्रिटिशों ने कुछ दमनकारी धाराएँ वापस ले लीं।
- भविष्य के आंदोलनों पर प्रभाव: इस आंदोलन ने भविष्य के विद्रोहों की नींव रखी तथा गदर आंदोलन और भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रेरित किया।
- गिरफ्तारी और निर्वासन: मई 1907 में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर लिया गया और बर्मा (अब म्यांमार) निर्वासित कर दिया गया, लेकिन जनता के दबाव के कारण नवंबर 1907 में उन्हें रिहा कर दिया गया।
- बाद में अजीत सिंह फारस, तुर्की, ब्राज़ील, जर्मनी और इटली चले गए और लाला हरदयाल और मैडम कामा जैसे क्रांतिकारियों के साथ काम किया।
- पगड़ी संभाल दिवस:
- किसान वर्ष 2021 से 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस के रूप में मना रहे हैं, जो अजीत सिंह की जयंती के साथ मेल खाता है।
- वर्ष 2021 किसान विरोध प्रदर्शन: दिल्ली सीमा पर विरोध प्रदर्शन के दौरान, किसानों ने तीन कृषि कानूनों (अब समाप्त) को निरस्त करने की मांग करते हुए पगड़ी संभाल दिवस मनाया।
- 2024 विरोध प्रदर्शन: 13 फरवरी, 2024 से किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी और अन्य अधिकारों की मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
झारखंड Switch to English
मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा
चर्चा में क्यों?
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के सचिव ने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दिल्ली और झारखंड में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों की समीक्षा के लिये एक उच्च स्तरीय बैठक का नेतृत्व किया।
मुख्य बिंदु
- प्रमुख मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा:
- बैठक में 17 महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित 21 मुद्दों की समीक्षा की गई, जिनमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत 9 परियोजनाएँ शामिल थीं।
- सभी परियोजनाओं की कुल लागत 13,501 करोड़ रुपए से अधिक हो गई।
- वाराणसी-राँची-कोलकाता एक्सप्रेसवे परियोजना, जिसकी कीमत 9,623.72 करोड़ रुपए है, मुख्य फोकस थी। इस परियोजना में छह पैकेजों में सात मुद्दे शामिल थे।
- रणनीतिक स्थानों पर नए एनआईटी पर ध्यान केंद्रित:
- बैठक में रणनीतिक स्थानों पर नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) स्थापित करने की सरकार की योजना पर ज़ोर दिया गया।
- इन NIT का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा में क्षेत्रीय असमानताओं को पाटना तथा कुशल इंजीनियरों और तकनीकी पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करना है।
- शैक्षणिक क्षेत्र के अलावा, ये संस्थान नवाचार, अनुसंधान और उद्योग सहयोग को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी गति देंगे।
- वाराणसी-राँची-कोलकाता एक्सप्रेसवे परियोजना:
- यह एक्सप्रेसवे भारत माला योजना के तहत एक प्रमुख परियोजना है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाएगी।
- इससे व्यापार और माल ढुलाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे उन उद्योगों को लाभ होगा जो समुद्री व्यापार के लिये कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों पर निर्भर हैं।
- कुशल परियोजना निगरानी के प्रति प्रतिबद्धता:
- सचिव ने परियोजना निगरानी के लिये संस्थागत ढाँचे को मज़बूत करने के लिये सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- उन्होंने अधिकारियों को लंबित परियोजना मुद्दों के समाधान में सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया।
- उन्होंने निजी समर्थकों से परियोजना के त्वरित कार्यान्वयन के लिये परियोजना निगरानी समूह (PMG) तंत्र (PMG पोर्टल) का उपयोग करने का आग्रह किया।
- PMG तंत्र केंद्र सरकार, राज्य प्राधिकरणों और निजी हितधारकों के बीच सहयोग के माध्यम से चिंताओं का कुशल और समय पर समाधान सुनिश्चित करता है।
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT)
- स्थापना:
- उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग की स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी तथा वर्ष 2000 में औद्योगिक विकास विभाग को इसमें मिला दिया गया।
- यह अपने वर्तमान स्वरूप में 27 जनवरी 2019 को अस्तित्व में आया, जब पूर्ववर्ती औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग का नाम बदलकर उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) कर दिया गया।
- उद्देश्य:
- यह विभाग राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिये प्रोत्साहन एवं विकासात्मक उपायों के निर्माण एवं कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार है।
- यह देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने के लिये भी ज़िम्मेदार है।
- यह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
छत्तीसगढ़ Switch to English
नक्सलवाद का अंत
चर्चा में क्यों?
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका ने घोषणा की कि राज्य में नक्सलवाद समाप्ति के कगार पर है।
मुख्य बिंदु
- माओवाद उन्मूलन के लिये सरकार की रणनीति:
- बजट सत्र के पहले दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सरकार की रणनीतिक सोच, सुरक्षा बलों की बहादुरी और जनता के सहयोग के कारण छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्ति की ओर है।
- सरकार ने क्षेत्र पर नियंत्रण के प्रयास तेज़ कर दिये हैं, जिसके परिणामस्वरूप पिछले 14 महीनों में 300 से अधिक नक्सलियों का सफाया हो गया है।
- इसके अतिरिक्त, 972 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जबकि सुरक्षा बलों ने 1,183 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है।
- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्धियाँ:
- पहली बार माओवाद प्रभावित 26 गाँवों में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया।
- सुकमा के पेंटाचिमाली, केरलापेन्डा, दुलेड़, सुन्नम गुडा और पुवर्ती सहित कई गाँवों ने पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में भाग लिया।
- दंतेवाड़ा ज़िले के पोटाली गाँव में 19 वर्षों के बाद स्वास्थ्य केंद्र का संचालन फिर से शुरू हुआ।
- अन्य विकासात्मक उपाय:
- राज्यपाल के 59-सूत्रीय संबोधन में निम्नलिखित प्रमुख पहल शामिल थीं:
- गरीबों के लिये आवास योजना का कार्यान्वयन।
- वनोपज संग्रहण कार्यक्रमों का विस्तार।
- आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये औद्योगीकरण को बढ़ावा देना।
- राज्यपाल के 59-सूत्रीय संबोधन में निम्नलिखित प्रमुख पहल शामिल थीं:
नक्सलवाद
- परिचय:
- नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गाँव से हुई है।
- इसकी शुरुआत स्थानीय जमींदारों के खिलाफ विद्रोह के रूप में हुई, जिन्होंने भूमि विवाद को लेकर एक किसान की पिटाई की थी।
- यह आंदोलन जल्द ही पूर्वी भारत के छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे अल्प विकसित क्षेत्रों में फैल गया।
- वामपंथी उग्रवादियों (LWE) को दुनिया भर में माओवादी और भारत में नक्सलवादी के नाम से जाना जाता है।
- उद्देश्य:
- वे सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत सरकार को उखाड़ फेंकने और माओवादी सिद्धांतों पर आधारित साम्यवादी राज्य की स्थापना की वकालत करते हैं।
- वे राज्य को दमनकारी, शोषक और शासक अभिजात वर्ग के हितों की सेवा करने वाला मानते हैं तथा सशस्त्र संघर्ष और जनयुद्ध के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक शिकायतों को दूर करना चाहते हैं।
उत्तर प्रदेश Switch to English
सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी
चर्चा में क्यों?
किसानों की आय बढ़ाने और फसल की बर्बादी को कम करने के उद्देश्य से IIT कानपुर ने एक नई सौर निर्जलीकरण तकनीक (Solar Dehydration Technology) विकसित की है।
मुख्य बिंदु
- उद्देश्य:
- यह तकनीक फलों और सब्ज़ियों को सौर ऊर्जा के माध्यम से सुखाने की सुविधा प्रदान करती है। यह एक कुशल और टिकाऊ तरीका है।
- इसका उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना और फसल की बर्बादी को कम करना है।
- किसान इस तकनीक का उपयोग करके अपनी फसलों को लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं और उचित मूल्य मिलने पर उन्हें बेच सकते हैं।
- लाभ:
- सोलर डिहाइड्रेशन एक पर्यावरण अनुकूल तरीका है, जो ऊर्जा की बचत करता है और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।
- सौर ऊर्जा का उपयोग करने से परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता कम होती है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम:
- इस पहल के तहत हाल ही में 30 किसानों को सोलर डिहाइड्रेशन तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया है। किसानों को टमाटर के प्री-ट्रीटमेंट और सोलर ड्राईिंग की लाइव डेमोंस्ट्रेशन दी गई, जिससे वे इस तकनीक को अपनी खेती में लागू कर सकेंगे।
- अन्य संस्थाओं का सहयोग:
- इस प्रोजेक्ट में NABARD का महत्त्वपूर्ण सहयोग रहा है।
- इसके साथ ही, CSJM विश्वविद्यालय के फूड प्रोसेसिंग विभाग के साथ मिलकर इस तकनीक के लिये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) और गुणवत्ता प्रोटोकॉल तैयार किये गए हैं।
नाबार्ड (NABARD)
- नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिये एक शीर्ष बैंक है।
- इसकी स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिशों के आधार पर संसद के एक अधिनियम द्वारा 12 जुलाई, 1982 को की गई थी।
- इसका कार्य कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों के संवर्द्धन और विकास के लिये ऋण प्रवाह को उपलब्ध कराना है।
- इसके साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य संबद्ध आर्थिक क्रियाओं को समर्थन प्रदान कर गाँवों का सतत् विकास करना है।
उत्तर प्रदेश Switch to English
गंगा जल की शुद्धता
चर्चा में क्यों?
हाल ही में महाकुंभ 2025 में गंगा जल की शुद्धता को लेकर संदेह दूर करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी की।
मुख्य बिंदु
मुद्दे के बारे में:
- गंगा जल की शुद्धता का दावा:
- उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी कर एक वैज्ञानिक के हवाले से महाकुंभ में गंगा जल की शुद्धता के बारे में ‘संदेह को दूर’ करने का प्रयास किया और कहा कि नदी का जल ‘क्षारीय जल की तरह’ शुद्ध है।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के संदर्भ में यह विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें महाकुंभ में गंगा जल की गुणवत्ता पर संदेह जताया गया था।
- CPCB की रिपोर्ट:
- CPCB की रिपोर्ट में कहा गया था कि महाकुंभ की शुरुआत में संगम पर पानी की जैविक ऑक्सीजन मांग (BOD) 3.94 मिलीग्राम प्रति लीटर थी।
- 14 जनवरी को यह 2.28 मिलीग्राम प्रति लीटर और 15 जनवरी को घटकर 1 मिलीग्राम प्रति लीटर हो गई।
- हालाँकि 24 जनवरी को BOD बढ़कर 4.08 मिलीग्राम प्रति लीटर हो गई और 29 जनवरी को यह 3.26 मिलीग्राम प्रति लीटर दर्ज की गई।
- डॉ. अजय कुमार सोनकर का शोध:
- पद्मश्री डॉ. अजय कुमार सोनकर ने गंगा जल की पवित्रता को साबित करने के लिये वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ संदेह को खारिज किया।
- उन्होंने महाकुंभ के विभिन्न प्रमुख स्नान घाटों से पानी के नमूने एकत्र किये और उनकी सूक्ष्म जाँच की।
- उन्होंने पाया कि करोड़ों श्रद्धालुओं के स्नान के बावजूद गंगा जल में बैक्टीरिया की वृद्धि नहीं हुई।
- पानी के Ph स्तर में भी कोई गिरावट नहीं देखी गई।
- प्राकृतिक वायरस की उपस्थिति:
- गंगा जल में 1,100 प्रकार के प्राकृतिक वायरस, जिसे "बैक्टीरियोफेज" कहा जाता है, होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करते हैं।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB):
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 को किया गया।
- इसके पश्चात् केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ व कार्य सौंपे गए।
- यह बोर्ड पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी उपलब्ध कराता है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्यों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत वर्णित किया गया है।
जैविक ऑक्सीजन मांग (Biological Oxygen Demand-BOD):
- ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिये आवश्यक होती है, वह BOD कहलाती है।
- जल प्रदूषण की मात्रा को BOD के माध्यम से मापा जाता है। परंतु BOD के माध्यम से केवल जैव अपघटक का पता चलता है साथ ही यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसलिये BOD को प्रदूषण मापन में प्रयोग नहीं किया जाता है।
- गौरतलब है कि उच्च स्तर के BOD का मतलब पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा को विघटित करने हेतु अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।
बिहार Switch to English
नालंदा में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन
चर्चा में क्यों?
बिहार के मुख्यमंत्री ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान नालंदा में 820.72 करोड़ रुपए की कुल 263 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
मुख्य बिंदु
प्रमुख उद्घाटन और शिलान्यास
- इन विकास परियोजनाओं में 361.66 करोड़ रुपए की 177 परियोजनाओं का उद्घाटन और 459.05 करोड़ रुपए की 86 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। जिनमें प्रमुख परियोजनाएँ निम्नलिखित हैं:
- तालाब और पुस्तकालय का उद्घाटन: इस दौरान उन्होंने सिलाव प्रखंड के नानंद गाँव में अमृत सरोवर योजना के तहत बने तालाब, सुंदर पार्क और वातानुकूलित डिजिटल पुस्तकालय का उद्घाटन किया।
- सामाजिक उत्थान पार्क: ₹19-22 लाख की लागत से निर्मित, इसे स्वच्छ बनाए रखने के निर्देश
- प्रधानमंत्री आवास योजना: के तहत 12 महादलित परिवारों को नवनिर्मित मकान सौंपे (बिजली, पानी और बागवानी सुविधा सहित)
- जीविका दीदियों को आर्थिक सहयोग प्रदान
- राजगीर कुंड परिसर: नवनिर्मित यात्री विश्राम भवन का उद्घाटन
- बेनार-सकसोहरा मार्ग: चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण करना
- मत्स्य हैचरी: निरीक्षण किया
- स्थानीय खेल मैदान: निरीक्षण, खिलाड़ियों को ब्लेजर बॉल और खेल किट प्रदान की
- सामाजिक भवन, वर्क शेड और चाइल्ड वेलफेयर स्कीम के लाभार्थियों से संवाद
- भावी परियोजनाएँ
- राजगीर में डायनासोर पार्क का निर्माण
- पंचाने सिंचाई योजना: जीर्णोद्धार और विकास
- सरमेरा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना
नालंदा ज़िला
- परिचय
- नालंदा बिहार का एक प्रमुख ज़िला है जिसका मुख्यालय बिहार शरीफ है। इसका क्षेत्रफल 2,355 वर्ग किलोमीटर (909 वर्ग मील) है।
- एतिहासिक महत्त्व
- नालंदा अपने प्राचीन इतिहास के लिये विश्व प्रसिद्ध है।
- यहाँ विश्व के सबसे पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी स्थित हैं।
- बुद्ध और महावीर कई बार नालंदा में ठहरे थे।
- महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी (नालंदा) में की थी।
- बुद्ध के प्रमुख शिष्य शारिपुत्र का जन्म नालंदा में हुआ था।
- प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ एक वर्ष बिताया था।
- पर्यटन स्थल
- नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष
- नालंदा संग्रहालय
- ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल
- राजगीर (गर्म पानी के झरने – ब्रह्मकुण्ड, सरस्वती कुण्ड, लंगटे कुण्ड)
- पावापुरी (महावीर का निर्वाण स्थल)
- बोधगया एवं गया (बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र)
- प्रमुख नदियाँ
- फल्गु
- मोहने
बिहार Switch to English
भारतीय नकली नोट की छपाई
चर्चा में क्यों?
21 फरवरी 2025 को राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने भारतीय मुद्रा के जाली नोटों (FICN) की छपाई में संलिप्त सात मॉड्यूल को गिरफ्तार किया गया।
मुख्य बिंदु
- मुद्दे के बारे में
- नकली भारतीय मुद्रा नोट (FICN) छापने और सिक्योरिटी पेपर के आयात में संलिप्त मॉड्यूल के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए, राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु और बिहार में 11 स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया।
- इस कार्रवाई में FICN की छपाई में सक्रिय सात मॉड्यूल को गिरफ्तार किया गया।
- इससे पहले भी 8 फरवरी, 2025 को, डीआरआई ने गाज़ीपुर और बेंगलुरु में ‘RBI’ और ‘इंडिया’ (‘सिक्योरिटी पेपर्स’) शब्दों वाले एम्बेडेड सुरक्षा धागे वाले कागज़ के आयातक पाए गए दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था।
- टीम ने 50 रुपए और 100 रुपए के मूल्यवर्ग के नकली नोट और कई मशीनरी/उपकरण ज़ब्त किये हैं।
- नकली मुद्रा का प्रभाव
- अर्थव्यवस्था को नुकसान
- नकली मुद्रा के प्रसार से महंगाई बढ़ सकती थी और आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती थी।
- असली और नकली मुद्रा के मिश्रण से बैंकिंग सिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है।
- अपराध का बढ़ना
- नकली नोटों का इस्तेमाल काले धन और अवैध गतिविधियों में किया जाता है, जिसे आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं।
- नकली नोटों का कारोबार सीमा पार तस्करी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़ा होता है।
- अर्थव्यवस्था को नुकसान
राजस्व खुफिया निदेशालय:
- यह भारत की एक प्रमुख तस्करी विरोधी खुफिया, जाँच एवं संचालन एजेंसी है।
- इसके आलावा इस एजेंसी द्वारा ड्रग्स, सोना, हीरे, इलेक्ट्रॉनिक्स, विदेशी मुद्रा, और नकली भारतीय मुद्रा सहित वस्तुओं की तस्करी पर रोक लगाने का कार्य किया जाता है।
- राजस्व खुफिया निदेशालय, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों और सीमा शुल्क के तहत कार्य करता है।
बिहार Switch to English
महिलाओं की सहायता हेतु सुरक्षा अधिकारी नियुक्त
चर्चा में क्यों?
बिहार सरकार ने घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को अधिक प्रभावी ढंग से सहायता प्रदान करने के लिये राज्य में 140 पूर्णकालिक 'संरक्षण अधिकारी' नियुक्त करने का निर्णय लिया है।
मुख्य बिंदु
- मुद्दे के बारे में:
- समाज कल्याण विभाग ने एक अलग संवर्ग बनाने का निर्णय किया है जिसके तहत उपमंडल, ज़िला और राज्य स्तर पर सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किये जाएंगे।
- उद्देश्य:
- घरेलू हिंसा के बढ़ते मामलों से प्रभावी ढंग से निपटना।
- महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करना।
- नियुक्ति का स्तर:
- उपमंडल, ज़िला और राज्य स्तर पर सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किये जाएंगे।
- कुल 140 सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किये जाएंगे:
- 101 उपमंडल स्तर पर
- 38 ज़िला स्तर पर
- 1 राज्य स्तरीय सुरक्षा अधिकारी।
- सुरक्षा अधिकारी की ज़िम्मेदारियाँ:
- महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत महिला के अधिकारों की सुरक्षा करना।
- मजिस्ट्रेट को उनके कार्यों में सहायता करना।
- पीड़ित महिला की शारीरिक चोटों का चिकित्सकीय परीक्षण करवाना और रिपोर्ट संबंधित थाने तथा मजिस्ट्रेट को भेजना।
- घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 20 के तहत आर्थिक राहत आदेश का पालन सुनिश्चित करना।
घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (Domestic Violence Act, 2005)
परिचय
- यह महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को रोकने और उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण कानून है।
उद्देश्य
- इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं को उनके घरों में या किसी अन्य निजी स्थान पर होने वाली हिंसा से बचाना है और उन्हें उनके अधिकारों का संरक्षण प्रदान करना है।
घरेलू हिंसा के विभिन्न प्रकार: अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा के विभिन्न प्रकार की हिंसाओं को शामिल किया गया है:
- शारीरिक हिंसा:
- इसमें महिला को शारीरिक रूप से चोट पहुँचाना शामिल है।
- उदाहरण: थप्पड़ मारना, धक्का देना, पीटना आदि।
- यौन हिंसा:
- इसमें महिला के साथ यौन उत्पीड़न या बलात्कार करना आदि कुकृत्य शामिल हैं।
- उदाहरण: जबरन संभोग, अन्य यौन अपराध।
- भावनात्मक दुरुपयोग:
- इसमें महिला की मानसिक स्थिति और आत्म-सम्मान को नुकसान पहुँचाना शामिल है।
- उदाहरण: अपमान करना, विश्वासघात करना, डराना-धमकाना, या महिला को मानसिक रूप से कमज़ोर महसूस कराना।
- सामाजिक और आर्थिक नियंत्रण:
- इसमें महिला को उसके परिवार और दोस्तों से अलग करना, उसे सामाजिक रूप से अकेला करना, या उसे अपनी इच्छा के खिलाफ सीमित करना शामिल है।

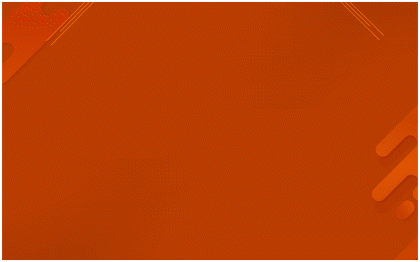


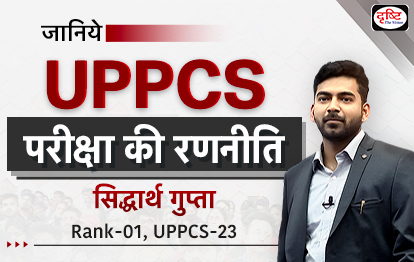
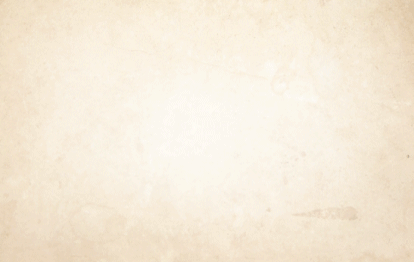
.jpg)
.jpg)
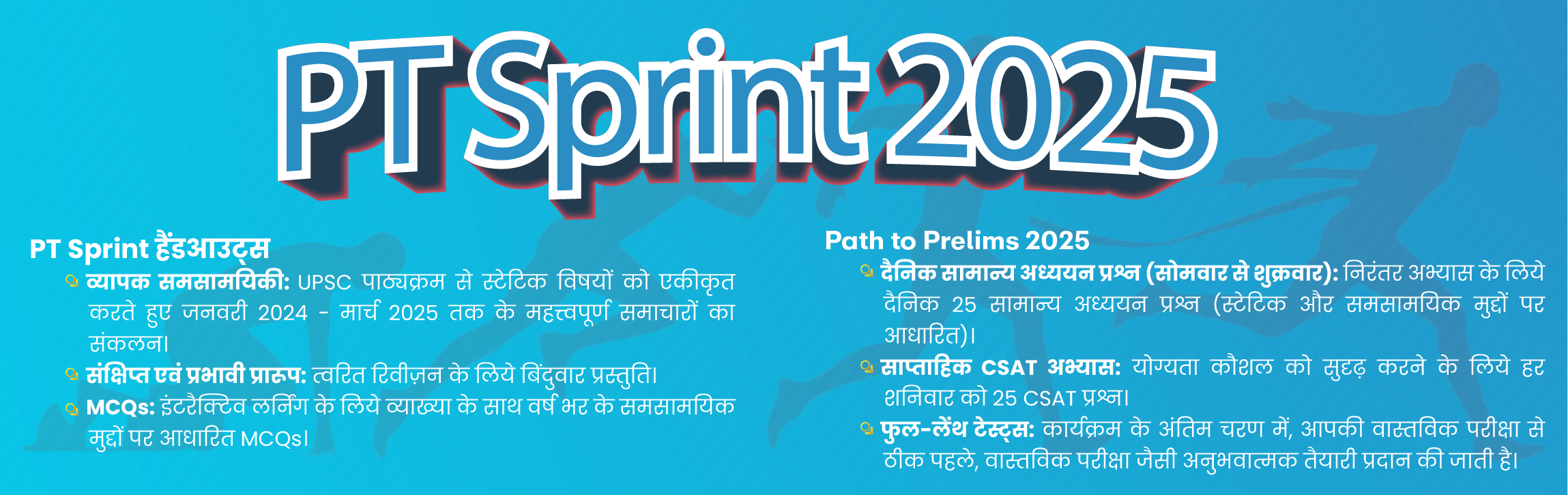
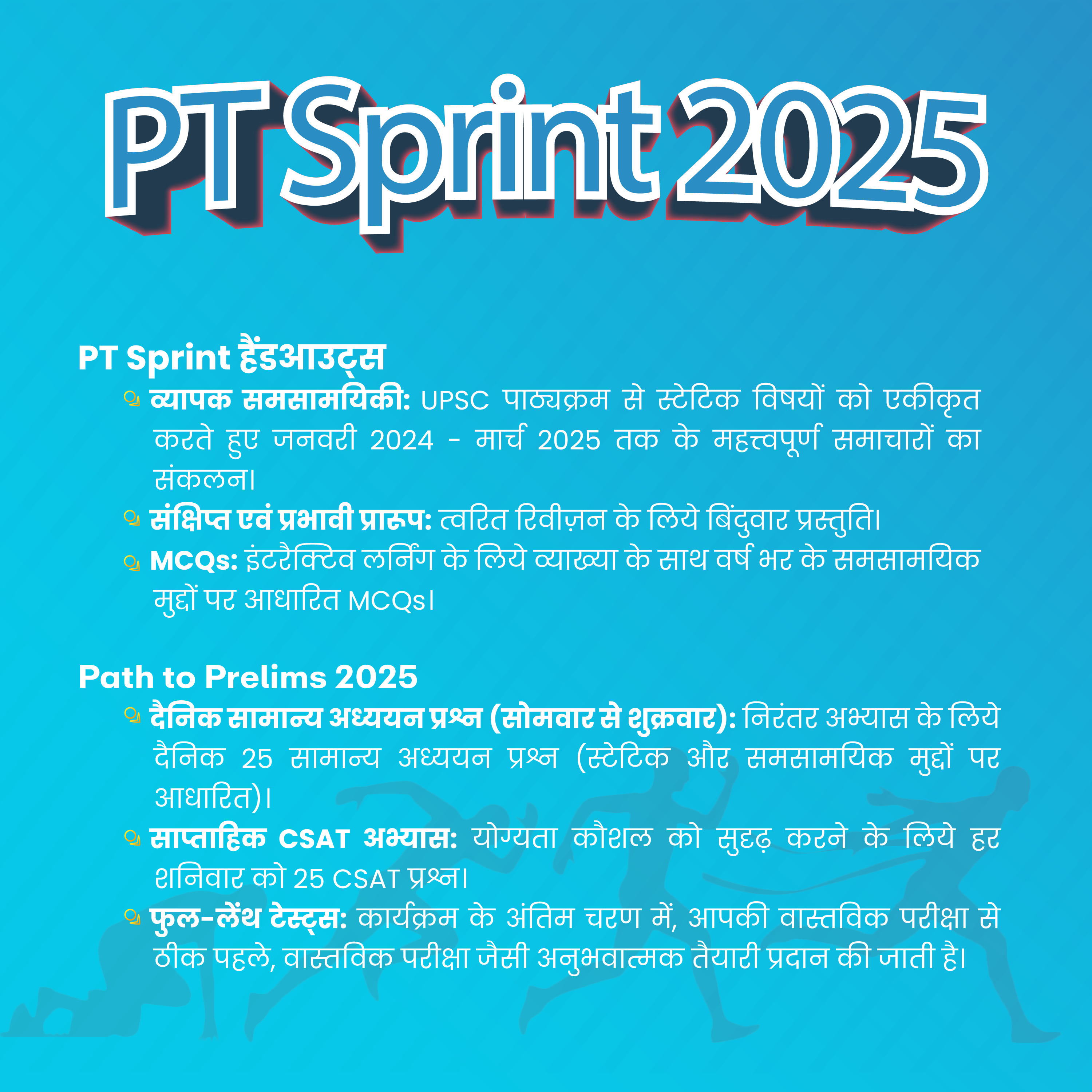

%201.jpeg)
.jpg)


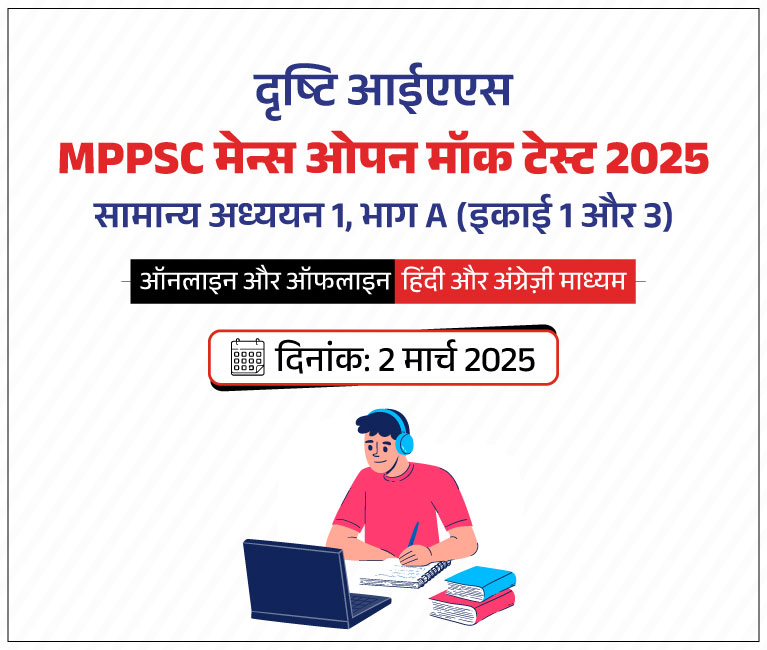
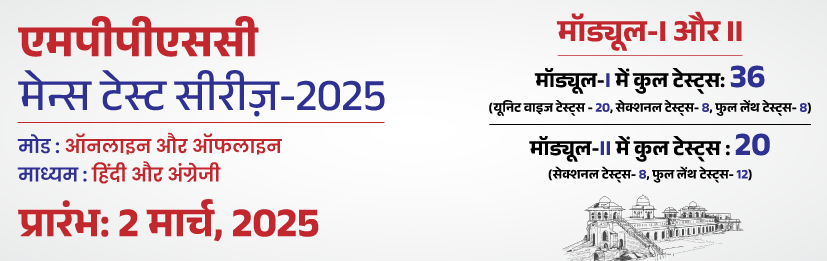

%20MPPCS%202025%20Desktop%20H.jpg)
%20MPPCS%202025%20Mobile%20H%20(1).jpg)

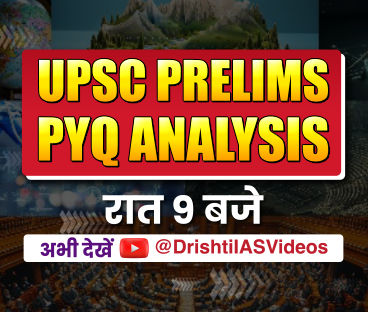

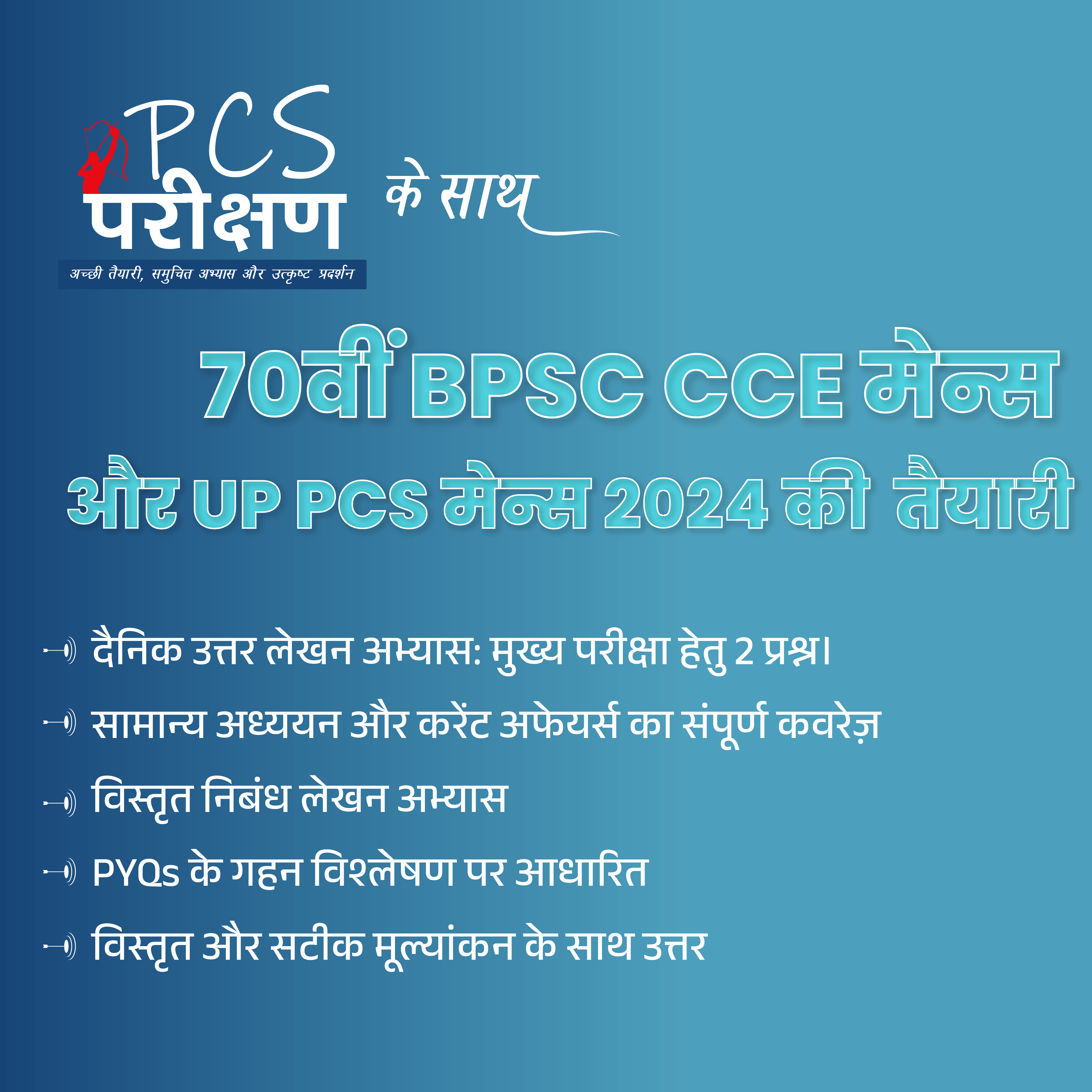


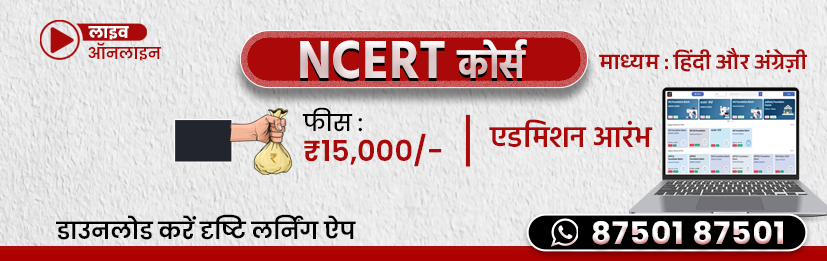
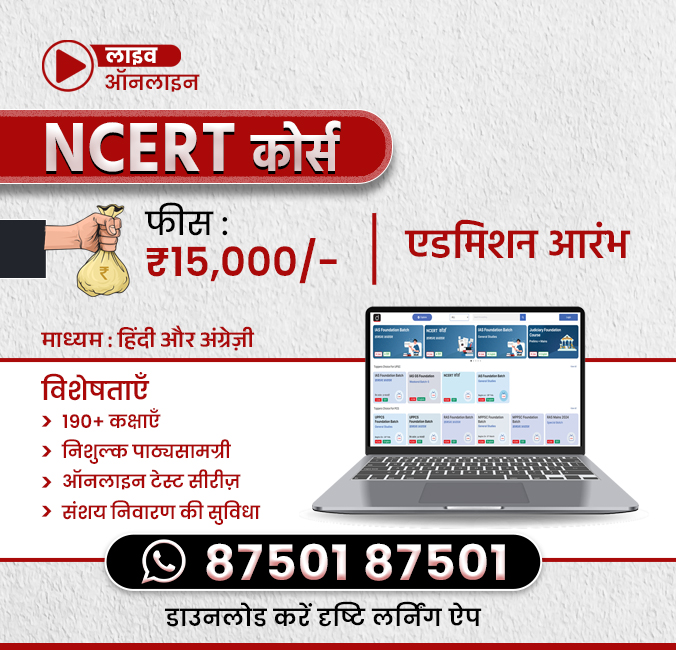

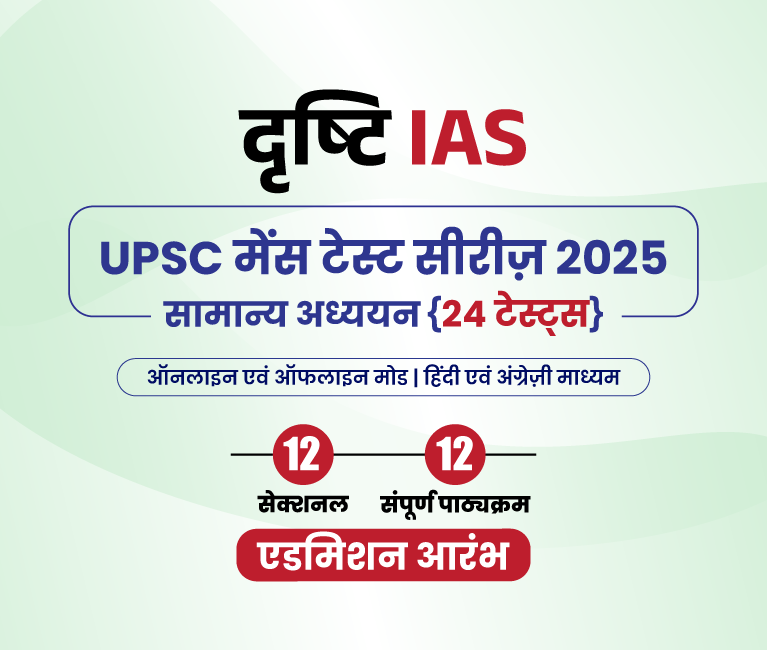
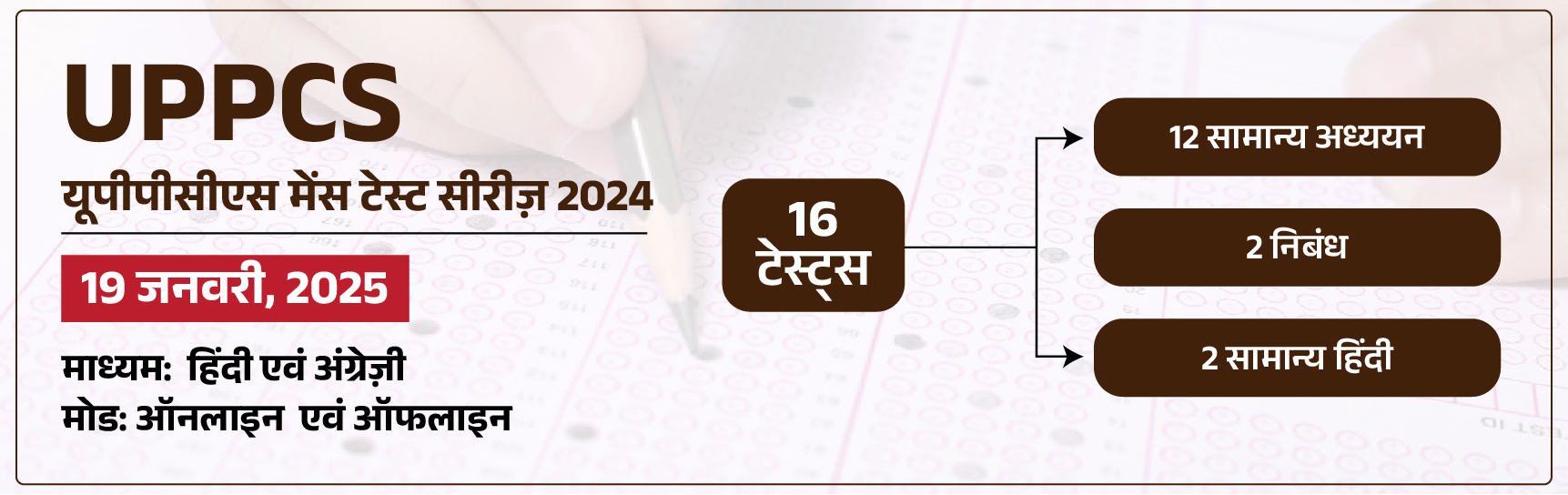
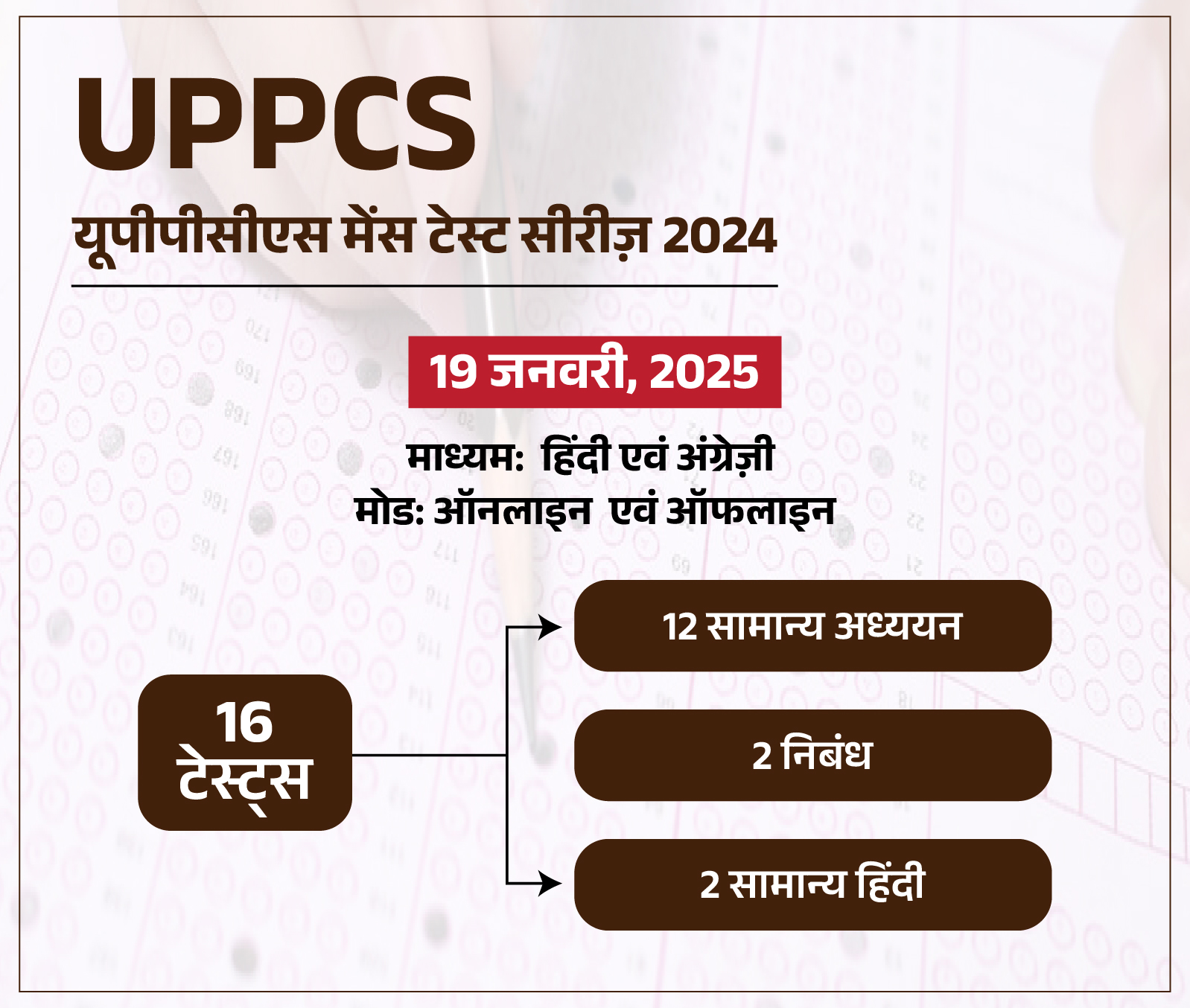



 PCS परीक्षण
PCS परीक्षण


