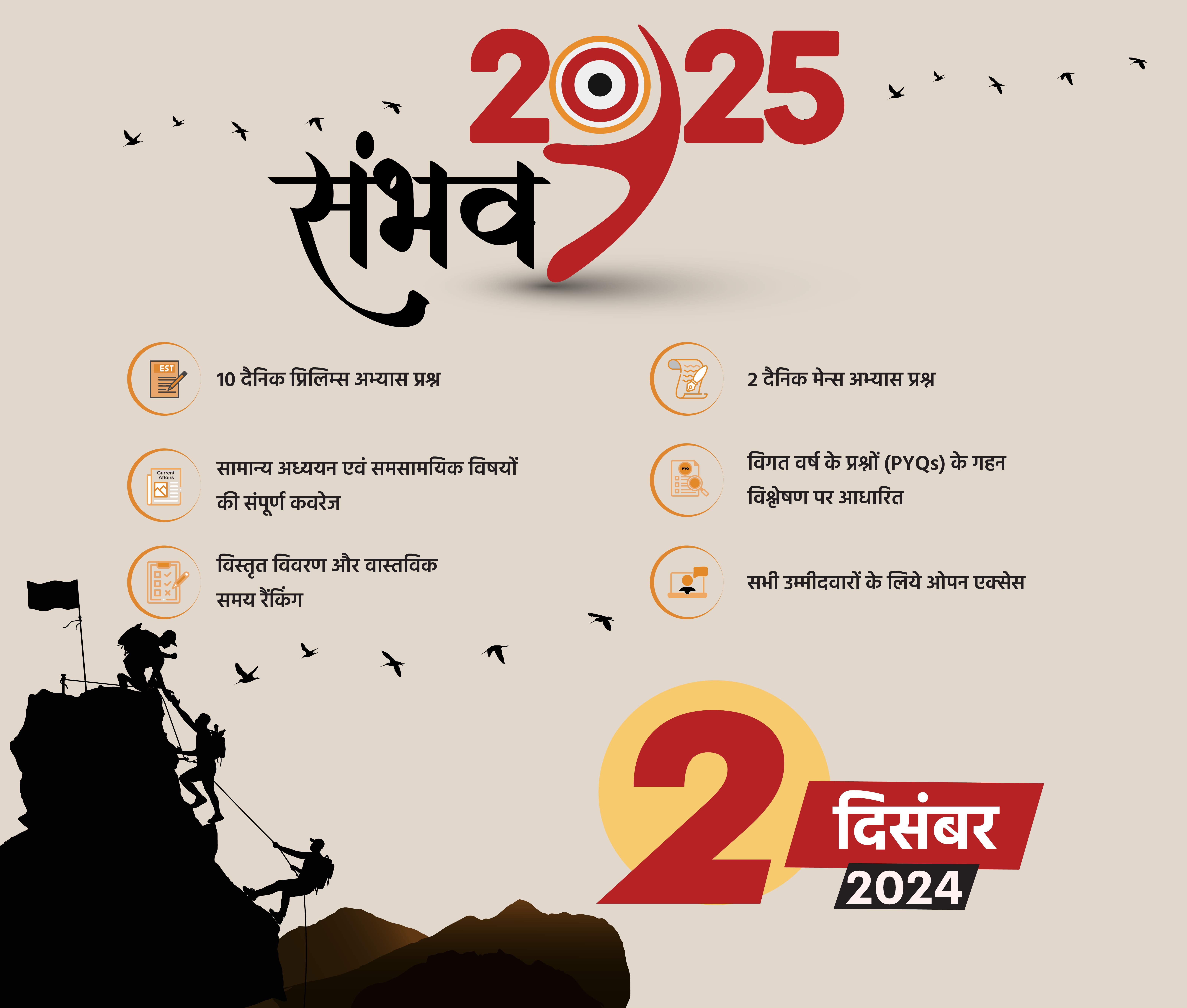आंतरिक सुरक्षा
बदलती युद्ध शैलियाँ और सैन्य क्षेत्र में भारत की प्रगति
प्रिलिम्स के लिये:चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, क्वांटम कंप्यूटिंग, मेक इन इंडिया, एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, सृजन पोर्टल, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मेन्स के लिये:भारत का रक्षा आधुनिकीकरण और क्षमताएँ, 21वीं सदी का युद्ध |
स्रोत: द हिंदू
चर्चा में क्यों?
एयरो इंडिया 2025 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने तकनीकी उन्नति से परे भारतीय सेना के समग्र परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया।
एयरो इंडिया
- रक्षा मंत्रालय के रक्षा प्रदर्शनी संगठन द्वारा आयोजित एयरो इंडिया, भारत की प्रमुख द्विवार्षिक एयरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी है, जो बेंगलुरु के येलहांका वायु सेना स्टेशन में आयोजित की जाती है।
- एयरो इंडिया में वैश्विक एयरो विक्रेता के साथ भारतीय वायु सेना द्वारा कलात्मक प्रदर्शन किया जाता है; इसे पहली बार वर्ष 1996 में आयोजित किया गया था।
21वीं सदी में युद्धकला का किस प्रकार विकास हो रहा है?
- बहु-आयामी संघर्ष: युद्ध अब भूमि, समुद्र और वायु से परे साइबरस्पेस, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम और बाह्य अंतरिक्ष तक विस्तारित हो गया है।
- मानवरहित प्लेटफाॅर्मों और स्वायत्त हथियारों के उदय से यह पुनः परिभाषित हो रहा है।
- गैर-संपर्क युद्ध का उदय: सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री, साइबर हमले और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध (EW) से प्रत्यक्ष युद्ध में कमी आई है।
- लंबी दूरी की मिसाइलों, ड्रोनों और AI-संचालित प्रणालियों के उपयोग से शत्रुओं को सीधे टकराव के बिना हमला करने की अनुमति मिलती है।
- युद्ध में प्रौद्योगिकियाँ: अमेरिका, चीन और रूस क्वांटम कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और हाइपरसोनिक हथियारों में सबसे आगे हैं जिससे युद्ध रणनीतियों में बदलाव आने से संभावित रूप से मशीन-बनाम-मशीन युद्ध हो सकता है।
- इसके अतिरिक्त, छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों और स्वायत्त हथियार प्रणालियों की भी भविष्य के युद्धों में प्रमुख भूमिका रहने का अनुमान है।
- हालाँकि, इन प्रौद्योगिकियों का सटीक प्रभाव अनिश्चित बना हुआ है, जिसके लिये अनुकूलनीय सैन्य रणनीतियों की आवश्यकता है।
- सतत् एवं अतार्किक युद्ध: पहले युद्ध सीमित होते थे तथा इसके बाद राजनीतिक वार्ता होती थी।
- वर्तमान में संघर्ष लंबे समय तक चलने वाले, संकर प्रकृति के (जिसमें पारंपरिक युद्ध, साइबर ऑपरेशन और सूचना आधारित युद्ध शामिल हैं) हो गए हैं तथा तकनीकी विषमता (विभिन्न देशों के बीच तकनीकी क्षमताओं का असमान वितरण) से प्रेरित हो गए हैं।
भारतीय सैन्य क्षेत्र में समग्र परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है?
- सुरक्षा संबंधी उभरती चुनौतियाँ: भारत को चीन और पाकिस्तान से दो मोर्चों पर खतरा है, जिसमें लगातार सीमा तनाव (जैसे, पूर्वी लद्दाख, डोकलाम) और जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान का परोक्षी युद्ध शामिल है।
- चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) सहित उनके रणनीतिक सहयोग से दो मोर्चों पर युद्ध का खतरा बढ़ गया है।
- हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी के कारण भारत को अपनी समुद्री शक्ति और क्षेत्र-बाह्य आकस्मिकता (OOAC) संचालन को मज़बूत करने की आवश्यकता है।
- संरचनात्मक और सैद्धांतिक सीमाएँ: भारत की रक्षा प्रणाली को संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें रक्षा नियोजन में भारतीय सेना का प्रभुत्व और 1.4 मिलियन से अधिक की विशाल स्थायी सेना शामिल है, जिससे बजट पर दबाव पड़ता है और आधुनिकीकरण में बाधा आती है।
- भारत की सैद्धांतिक सीमाएँ, खतरों के प्रति प्रतिक्रियात्मक अनुक्रियाओं (जैसे, कारगिल युद्ध, मुंबई 26/11) द्वारा चिह्नित, बढ़ी हुई सुरक्षा के लिये अग्रसक्रिय निवारण और अद्यतन परिचालन सिद्धांतों की आवश्यकता को उजागर करती हैं।
- आधुनिकीकरण की कमियाँ: भारत का रक्षा भंडार अप्रचलित हो गया है, जिससे परिचालन दक्षता प्रभावित हो रही है। आधुनिक प्रगति के बावजूद भारतीय सेना अभी भी 1980 के दशक के T-72 टैंक (40 वर्ष से अधिक पुराने) और बोफोर्स हॉवित्जर का इस्तेमाल करती है।
- 'मेक इन इंडिया' पहल के बावजूद, भारत विश्व का सबसे बड़ा आयुध आयातक देश है (2019 से 2023 तक वैश्विक आयात का 9.8%) और उन्नत हथियारों के लिये रूस, फ्राँस और अमेरिका पर निर्भर है।
- ऐसा तेजस लड़ाकू विमानों और भविष्य के पैदल सेना के लड़ाकू यानों जैसे आधुनिक उपकरणों को शामिल करने में देरी के कारण है।
- भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना के बीच तालमेल के अभाव से एकीकृत वायु-भूमि-समुद्र युद्ध और अभियान रणनीतियों में बाधा उत्पन्न होती है।
- बजटीय बाधाएँ: भारत का 2025-26 का रक्षा बजट 78.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो वर्ष 2023 में चीन के 236 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में बहुत कम है।
- वर्ष 2001 से भारत के रक्षा क्षेत्र ने केवल 5,077 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित किया है, जबकि FDI सीमा में स्वचालित मार्ग से 74% और सरकारी मार्ग से 100% का विस्तार कर दिया गया है।
- रक्षा बजट के एक बड़े हिस्से का व्यय मानव शक्ति लागत (वेतन और पेंशन) में होता है, जिससे पूंजी अधिग्रहण के लिये बहुत कम शेष बचता है। रक्षा आवश्यकताओं और वित्तीय बाधाओं के बीच संतुलन बनाना भारत के लिये चुनौती बना हुआ है।
सैन्य क्षेत्र के आधुनिकीकरण में भारत की प्रगति
- मेक इन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में, भारत ने प्रमुख रक्षा प्रणालियों जैसे धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम, एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम (ATAGS), मुख्य युद्धक टैंक (MBT) अर्जुन, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस, पाँचवीं पीढ़ी (5G) लड़ाकू विमान, पनडुब्बियाँ, फ्रिगेट, कोरवेट और हाल ही में कमीशन किया गया आईएनएस विक्रांत विकसित किया है, जो देश की बढ़ती रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करता है।
- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 से रक्षा उत्पादन वर्ष 2023-24 में 1.27 लाख करोड़ रुपए हुआ, जिसका लक्ष्य वर्ष 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए है, जिससे भारत वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित हो जाएगा।
- भारत का रक्षा निर्यात वर्ष 2013-14 में 686 करोड़ रुपए था जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 21,083 करोड़ रुपए हो गया, जो एक दशक में 30 गुना वृद्धि है।
- औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है, और iDEX योजना स्टार्टअप एवं एमएसएमई को रक्षा क्षेत्र में नवाचार करने के लिये प्रोत्साहित करती है। SRIJAN पोर्टल स्वदेशीकरण ( "मेक" प्रक्रिया ) में सहायता करता है, जबकि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारे क्षेत्रीय विनिर्माण को बढ़ावा देते हैं।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास अब बेहतर सहयोग के लिये निजी क्षेत्र के लिये खुले है।
उभरते युद्ध रुझानों का अनुसरण करने के लिये भारत क्या कदम उठा सकता है?
- स्वदेशी रक्षा नवाचार: अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकियों के विकास के लिये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन प्रौद्योगिकी क्लस्टरों, निजी रक्षा स्टार्टअप्स एवं शिक्षाविदों के लिये वित्त पोषण में वृद्धि।
- रक्षा में प्रौद्योगिकी: एआई-संचालित स्वायत्त ड्रोन, निर्णय लेने वाली प्रणालियाँ और साइबर युद्ध उपकरणों को तीव्रता से एकीकृत करने की आवश्यकता है। क्वांटम संचार एवं क्रिप्टोग्राफी भारत की सामरिक सैन्य संपत्तियों को सुरक्षित करेगी।
- एकीकृत कमान संरचना से रणनीतिक समन्वय और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
- साइबर और विद्युत चुम्बकीय युद्ध बल: डिजिटल युद्ध के खतरों का मुकाबला करने के लिये समर्पित साइबर और विद्युत चुम्बकीय कमांड की स्थापना करना और सामरिक लाभ के लिये NavIC उपग्रह निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं का विस्तार करना।
- सैन्य प्रशिक्षण एवं रणनीति: AI, रोबोटिक्स एवं असममित युद्ध रणनीतियों को शामिल करने के लिये सैन्य प्रशिक्षण को संशोधित करना। अमेरिका, इज़रायल और फ्राँस जैसी वैश्विक तकनीक-संचालित सेनाओं के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करना।
- भारत की वैश्विक रक्षा स्थिति को बढ़ाना: पश्चिमी सैन्य मानकों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने के लिये स्वदेशी रक्षा उत्पादन और नवाचार में निवेश की आवश्यकता है।
- उभरते उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) और क्वाड सैन्य सिद्धांतों के साथ तालमेल बिठाने से भारत को वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के लिये तैयार होने में मदद मिलेगी।
- भविष्य के लिये तैयार सैन्य रणनीति: भारत की भविष्य के लिये तैयार सैन्य रणनीति में भूमि, समुद्र, वायु, साइबर और अंतरिक्ष क्षमताओं का संतुलन होना चाहिये। नियोजित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) का लाभ उठाने से अंतरिक्ष निगरानी और संचार में वृद्धि होगी।
- आगे बने रहने के लिये, भारत को उभरते खतरों के लिये तैयार रहना होगा, जिनमें "रोबोट युद्ध", "ड्रोन युद्ध", "स्वायत्त वाहन मुठभेड़" और "मशीनीकृत संघर्ष" शामिल हैं।
निष्कर्ष
भारत के रक्षा परिवर्तन के लिये एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सामरिक अनुकूलनशीलता के साथ प्रौद्योगिकीय प्रगति को संतुलित किया जाए तथा उभरते युद्ध रुझानों के साथ तालमेल बिठाया जाए, जिससे भारत अपनी वैश्विक रक्षा स्थिति को बढ़ा सके तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सके।
|
दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: आधुनिक युद्ध एक बहु-क्षेत्रीय संघर्ष में बदल रहा है। मुख्य मुद्दों और उन बदलावों पर चर्चा कीजिये जो भारतीय सेना को नए खतरों से निपटने के लिये करने की आवश्यकता है।। |
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, वित्त वर्ष के प्रश्न (PYQs)प्रिलिम्सप्रश्न. कभी-कभी समाचारों में उल्लिखित "टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस (THAAD)" क्या है? (2018) (a) इज़रायल की एक रडार प्रणाली उत्तर: (c) प्रश्न. भारतीय रक्षा के संदर्भ में 'ध्रुव' क्या है? (2008) (a) विमान ले जाने वाला युद्धपोत उत्तर: (c) मेन्सप्रश्न :रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अब उदार बनाया जाना तय है: इससे भारतीय रक्षा और अर्थव्यवस्था पर अल्पावधि और दीर्घावधि में क्या प्रभाव पड़ने की उम्मीद है? (2014) |

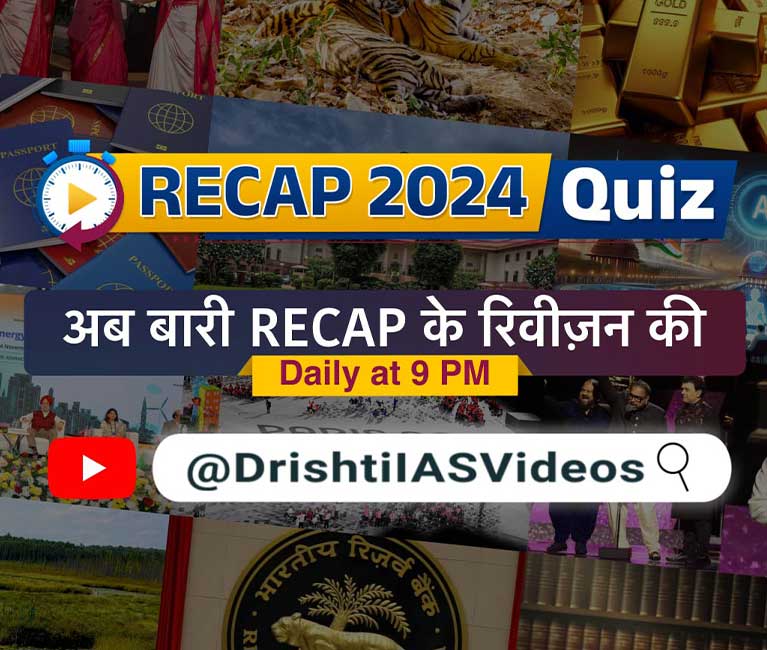
भारतीय इतिहास
स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती
प्रारंभिक परीक्षा के लिये:महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती, आर्य समाज मुख्य परीक्षा के लिये :महर्षि दयानंद सरस्वती और उनका योगदान, महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व, आर्य समाज के मार्गदर्शक सिद्धांत। |
स्रोत: पी.आई.बी
प्रधानमंत्री ने 12 फरवरी 2025 को स्वामी दयानंद सरस्वती (1824-1883) की 201 वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वे एक महान विचारक, प्रखर राष्ट्रवादी और आर्य समाज के संस्थापक थे।
महर्षि दयानंद सरस्वती कौन थे?
- परिचय:
- महर्षि दयानंद सरस्वती, 19 वीं सदी के एक प्रमुख समाज सुधारक, दार्शनिक और धार्मिक नेता थे।
- जन्म एवं प्रारंभिक जीवन:
- उनका जन्म 12 फरवरी, 1824 को गुजरात के टंकारा में एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम मूल शंकर तिवारी था। उनके माता-पिता यशोदाबाई और लालजी तिवारी समर्पित हिंदू थे।
- छोटी उम्र में ही उनमें आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति गहरी रुचि विकसित हो गई और उन्होंने मूर्ति पूजा, अनुष्ठानों और अंधविश्वासों पर प्रश्न उठाए।
- 19 वर्ष की उम्र में सांसारिक जीवन त्यागकर, वे सत्य की खोज में लगभग 15 वर्षों (1845-1860) तक एक तपस्वी के रूप में भ्रमण करते रहे।
- उन्होंने मथुरा में स्वामी विरजानंद से शिक्षा प्राप्त की, जिन्होंने उन्हें हिंदू धर्म से भ्रष्ट प्रथाओं को समाप्त करने तथा वेदों के सच्चे अर्थ को पुनर्स्थापित करने के लिये काम करने का आग्रह किया।
- दर्शन और सामाजिक सुधार:
- उन्होंने मूर्ति पूजा, अस्पृश्यता, जाति-आधारित भेदभाव, बहुविवा, बाल विवाह और लैंगिक असमानता का विरोध किया।
- वह एक वर्गविहीन और जातिविहीन समाज में विश्वास करते थे जहाँ जाति जन्म के बजाय योग्यता पर आधारित होती थी।
- उन्होंने महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, दलित वर्गों के उत्थान, पुनः धर्म परिवर्तन के लिये शुद्धि आंदोलन तथा सती प्रथा और बाल विवाह उन्मूलन की पुरज़ोर वकालत की।
- उन्होंने "वेदों की ओर लौटो" पर ज़ोर देते हुए तर्क दिया कि सच्चा हिंदू धर्म वेदों में निहित है, जो तर्कसंगतता, समानता और सामाजिक न्याय को कायम रखते हैं।
- उनके विचार उनकी मौलिक कृति सत्यार्थ प्रकाश में संकलित हैं, जिसमें उन्होंने भ्रूण हत्या और दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों की आलोचना की तथा वैदिक ज्ञान की वकालत की।
- शैक्षिक योगदान:
- उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली का विरोध करते हुए आधुनिक, वैज्ञानिक तथा वैदिक शिक्षा की वकालत की।
- वर्ष 1886 में इन्होने गुरुकुलों, बालिका गुरुकुलों और दयानंद एंग्लो-वैदिक (DAV) स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना को प्रेरित किया, जिसमें महात्मा हंसराज के नेतृत्व में लाहौर में पहला DAV स्कूल स्थापित किया गया।
- राष्ट्रवादी आंदोलन में भूमिका:
- वह वर्ष 1876 में "स्वराज" का आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिसका प्रभाव बाद के नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी पर पड़ा।
- उन्होंने स्वदेशी (आर्थिक आत्मनिर्भरता) अपनाने एवं गौरक्षा के साथ हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में बढ़ावा दिया।
- विरासत:
- स्वामी दयानंद सरस्वती को सामाजिक-धार्मिक सुधार के प्रयासों के कारण समाज के रूढ़िवादी वर्गों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। हालाँकि, उन्होंने आर्य समाज और DAV स्कूलों जैसी संस्थाओं के माध्यम से एक स्थायी विरासत छोड़ी, जिसका समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।
आर्य समाज क्या है?
- परिचय:
- आर्य समाज (कुलीनों का समाज) एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसके तहत वेदों को ज्ञान एवं सत्य के अंतिम स्रोत के रूप में बढ़ावा दिया गया।
- इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ष 1875 में की थी।
- मूल मान्यता और सिद्धांत:
- वेदों की प्रधानता पर ज़ोर दिया गया है तथा मूर्ति पूजा, पुरोहिती अनुष्ठान, पशु बलि, सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों को अस्वीकार किया गया।
- कर्म (कर्मों का नियम), संसार (पुनर्जन्म का चक्र) और गाय की पवित्रता पर बल दिया गया।
- वैदिक अग्नि अनुष्ठान (हवन/यज्ञ) और संस्कारों को बढ़ावा दिया गया।
- सामाजिक सुधार और योगदान:
- महिला शिक्षा, अंतर्जातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया।
- स्कूल, अनाथालय और विधवा आश्रम स्थापित किये गये।
- अकाल राहत और चिकित्सा सहायता में महत्त्वपूर्ण निभाई।
- अन्य धर्मों को अपनाने वाले लोगों को पुनः धर्मांतरित करने के लिये शुद्धि आंदोलन का नेतृत्व किया।
|
प्रश्न. 19वीं शताब्दी के प्रमुख सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन कौन-से थे? |
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सी घटना सबसे पहले हुई? (2018) (a) स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। उत्तर: (b) |

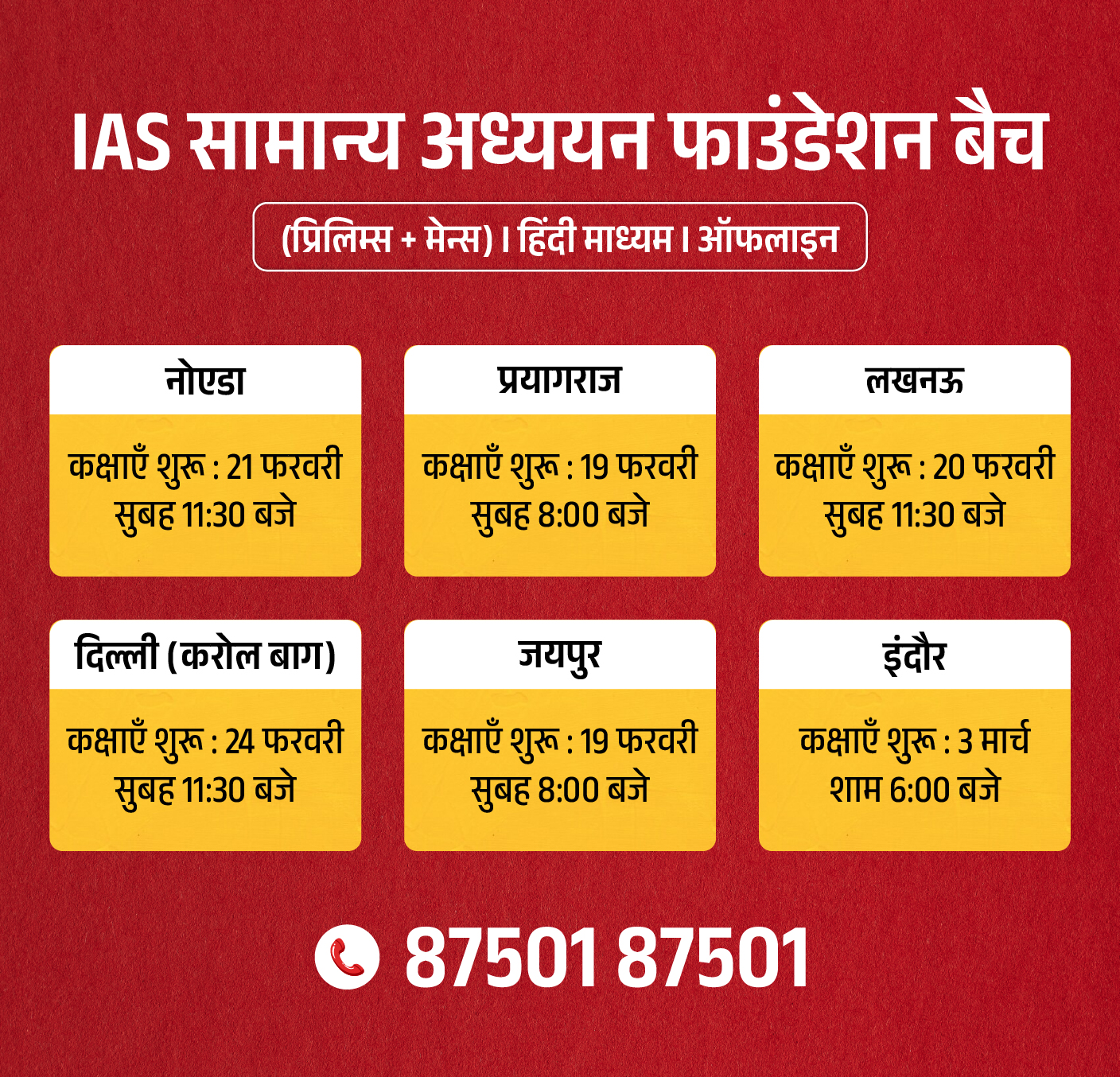
शासन व्यवस्था
भारत में वैवाहिक बलात्कार
प्रिलिम्स के लिये:उच्च न्यायालय (HC), सर्वोच्च न्यायालय (SC), BNS, धारा 377, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005, अनुच्छेद 14 (समानता), 15 (गैर-भेदभाव), और 21 (जीवन और गरिमा का अधिकार), POCSO अधिनियम, 2012। मेन्स के लिये:भारत में वैवाहिक बलात्कार की कानूनी और न्यायिक स्थिति। वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने पर चर्चा। |
स्रोत: बिज़नेस स्टैंडर्ड
चर्चा में क्यों?
गोरखनाथ शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले, 2019 में, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (HC) ने निर्णय दिया कि यदि पत्नी 15 वर्ष से अधिक उम्र की है, तो पति पर सहमति के बिना भी, उसके साथ बलात्कार या अप्राकृतिक यौन संबंध का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।
- यह IPC की धारा 375 के तहत अपवाद 2 पर निर्भर करता है, जो पति को बलात्कार के आरोप से छूट देता है यदि पत्नी 15 वर्ष से कम नहीं है।
- एक अन्य घटनाक्रम में, सर्वोच्च न्यायालय (SC) वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसका समर्थन महिला अधिकार कार्यकर्त्ताओं द्वारा किया जा रहा है।
वैवाहिक बलात्कार क्या है?
- परिचय: वैवाहिक बलात्कार एक प्रकार की अंतरंग साथी हिंसा है जिसमें पति-पत्नी के बीच जबरन यौन संबंध या यौन उत्पीड़न शामिल होता है। यह भारत में अपराध नहीं है।
- हालाँकि, यदि कोई दंपत्ति विवाहित है, लेकिन अलग-अलग रह रहे हैं, तो यदि उसकी पत्नी यौन संबंध के लिये सहमति नहीं देती है, तो पति बलात्कार का दोषी है।
- विधिक दृष्टिकोण:
- IPC: धारा 375 (2) में कहा गया है कि एक पुरुष और उसकी पत्नी, जो 15 वर्ष से कम उम्र की नहीं है, के बीच यौन संबंध या यौन क्रिया बलात्कार नहीं है।
- BNS ने वैवाहिक बलात्कार के मामलों में पतियों के लिये प्रतिरक्षा बरकरार रखी है, लेकिन इंडिपेंडेंट थॉट बनाम UoI केस, 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करते हुए सहमति की उम्र 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है।
- घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005: यद्यपि वैवाहिक बलात्कार कोई अपराध नहीं है, फिर भी एक महिला यौन दुर्व्यवहार, अपमान या गरिमा के उल्लंघन के लिये घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत राहत की मांग कर सकती है।
- IPC: धारा 375 (2) में कहा गया है कि एक पुरुष और उसकी पत्नी, जो 15 वर्ष से कम उम्र की नहीं है, के बीच यौन संबंध या यौन क्रिया बलात्कार नहीं है।
- वैवाहिक बलात्कार पर न्यायिक निर्णय:
- इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूओआई केस, 2017: सर्वोच्च न्यायालय ने 15-18 वर्ष की आयु की पत्नियों के लिये भारतीय दंड संहिता की धारा 375 (BNS की धारा 63) के अपवाद 2 को खारिज कर दिया, जिसके तहत नाबालिग पत्नियों (18 वर्ष से कम) के साथ संभोग को बलात्कार माना गया था।।
- इसने इस अपवाद को मनमाना और असंवैधानिक करार दिया, जो अनुच्छेद 14 (समानता) , 15 (गैर-भेदभाव) और 21 (जीवन और सम्मान का अधिकार) का उल्लंघन करता है ।
- न्यायालय ने निर्णय दिया कि पोक्सो अधिनियम, 2012 भारतीय दंड संहिता से अधिक प्रभावी है, जो नाबालिग (18 वर्ष से कम) के साथ यौन संबंध को बलात्कार बनाता है, भले ही वह विवाहित हो।
- के.एस. पुट्टस्वामी केस, 2017: इसमें गोपनीयता के आंतरिक भाग के रूप में व्यक्तियों के लिये यौन स्वायत्तता के महत्त्व पर बल दिया गया ।
- इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूओआई केस, 2017: सर्वोच्च न्यायालय ने 15-18 वर्ष की आयु की पत्नियों के लिये भारतीय दंड संहिता की धारा 375 (BNS की धारा 63) के अपवाद 2 को खारिज कर दिया, जिसके तहत नाबालिग पत्नियों (18 वर्ष से कम) के साथ संभोग को बलात्कार माना गया था।।
- अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय:
- वर्ष 2023 में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि नाबालिग पत्नी के साथ सहमति से बनाया गया यौन संबंध बलात्कार है, और ऐसे मामलों में सहमति के बचाव को खारिज कर दिया।
- वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बलात्कार नहीं है और ऐसे मामलों में पत्नी की सहमति अप्रासंगिक है ।
- अप्राकृतिक यौन संबंध पर न्यायिक निर्णय:
- नवतेज सिंह जौहर केस, 2018: सर्वोच्च न्यायालय ने सहमति से समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए आईपीसी की धारा 377 को आंशिक रूप से निरस्त कर दिया।
- सरकार का रुख: गृह मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि यद्यपि पति अपनी पत्नी की सहमति का उल्लंघन नहीं कर सकता, लेकिन इसे "बलात्कार" कहना अत्यधिक कठोर और असंगत है।
वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के पक्ष और विपक्ष में तर्क क्या हैं?
|
अपराधीकरण के लिये |
अपराधीकरण के विरुद्ध |
|
स्वायत्तता का उल्लंघन: हर व्यक्ति को यौन संबंध बनाने से इंकार करने का अधिकार है, यहाँ तक कि विवाह के बाद भी। नवतेज जौहर मामले, 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने यौन स्वायत्तता को बनाए रखा और इसे विवाह के बाद तक बढ़ाया जाना चाहिये। |
विवाह को खतरा: अपराधीकरण से वैवाहिक संबंध अस्थिर हो सकते हैं। |
|
सर्वोच्च न्यायालय निर्णय: इंडिपेंडेंट थॉट केस, 2017 ने नाबालिगों के लिये वैवाहिक बलात्कार को मान्यता दी, जिससे सहमति को बल मिला। |
मौजूदा कानून पर्याप्त : घरेलू हिंसा कानून पहले से ही यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करते हैं। |
|
कानून के समक्ष समानता : पतियों को छूट देना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है (अनुच्छेद 14, 15, 21)। |
संभावित दुरुपयोग: तलाक और हिरासत के मामलों में झूठे आरोप लग सकते हैं । |
|
POCSO एवं बाल संरक्षण: नाबालिगों के साथ गैर-सहमति से यौन संबंध अपराध है; यह विवाहित वयस्कों पर भी लागू होना चाहिये। |
सामाजिक एवं सांस्कृतिक मानदंड: पारंपरिक रूप से विवाह में यौन संबंध शामिल होते हैं, जिससे विधिक परिवर्तन जटिल हो जाता है। |
|
कानूनी विरोधाभास: धारा 377 को हटाने के बावजूद BNS में पतियों के लिये प्रतिरक्षा को बनाए रखा गया है। |
विधायी क्षेत्र: सरकार का तर्क है कि इस संबंध में न्यायालय को नहीं, बल्कि विधायिका को निर्णय लेना चाहिये। |
विश्व स्तर पर वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण
- 77 देशों में वैवाहिक बलात्कार को स्पष्ट रूप से अपराध घोषित किया गया है, 74 देशों में सामान्य प्रावधानों के तहत पति-पत्नी के विरुद्ध मामले चलाने की अनुमति दी गई है तथा 34 देशों में इसे अपराधमुक्त कर दिया गया है या इसमें छूट दी गई है।
- वैवाहिक बलात्कार 50 अमेरिकी राज्यों, 3 ऑस्ट्रेलियाई राज्यों, न्यूज़ीलैंड, कनाडा, इजरायल, फ्राँस , स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, सोवियत संघ, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया तथा कई अन्य देशों में अवैध है।
- ब्रिटेन (जहाँ से IPC काफी हद तक प्रेरित है) ने वर्ष 1991 में वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को हटा दिया था।
वैवाहिक बलात्कार को रोकने के लिये क्या किया जा सकता है?
- जया जेटली समिति की सिफारिशें: लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाने और गैर-सहमति वाले यौन संबंध (वैवाहिक बलात्कार) के जोखिम को कम करने के लिये महिलाओं के लिये विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष की जाए।
- विधायी सुधार: वैवाहिक बलात्कार से छूट को हटाने के लिये BNS में संशोधन करना चाहिये तथा वैवाहिक सहमति को विधिक आवश्यकता के रूप में मान्यता देनी चाहिये।
- वैकल्पिक कानूनी ढाँचा: घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 का विस्तार करके इसमें वैवाहिक यौन उत्पीडन को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिये, तथा दंडात्मक आदेश और मुआवज़े जैसे मज़बूत नागरिक उपचारों की पेशकश की जानी चाहिये।
- वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ: भारत ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के कानूनों का अध्ययन कर सकता है ताकि सांस्कृतिक रूप से अनुकूल वैवाहिक बलात्कार कानून विकसित किया जा सके, जो सामाजिक-सांस्कृतिक वास्तविकताओं पर विचार करते हुए वैश्विक मानवाधिकारों के साथ संरेखित हो।
निष्कर्ष
वैवाहिक बलात्कार पर चर्चा व्यक्तिगत स्वायत्तता, विधिक समानता और सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों के बीच भेद प्रकट करती है। विभिन्न देशों ने इसे अपराध घोषित कर दिया है, भारत में पतियों के लिये कानूनी प्रतिरक्षा बरकरार है। यहाँ न्यायिक फैसले सहमति और गरिमा पर ज़ोर देते हैं, लेकिन विधायी अनिच्छा बनी हुई है। इस मुद्दे पर विधिक स्पष्टता की आवश्यकता है, जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों को सामाजिक चिंताओं के साथ संतुलित किये जाने की आवश्यकता है।
|
दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। |
UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)मेन्सQ. महिलाएँ जिन समस्याओं का सार्वजानिक एवं निज़ी दोनों स्थलों का सामना कर रही हैं, क्या राष्ट्रीय महिला आयोग उनका समाधान निकालने की रणनीति बनाने में सफल रहा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिये। (2017) Q. हमें देश में महिलाओं के प्रति यौन उत्पीडन के बढ़ते हुए दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं। इस कुकृत्य के विरुद्ध विद्यमान विधिक उपबंधों के होते हुए भी ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस संकट से निपटने के लिये कुछ नवाचारी उपाय सुझाइये। (2014) |