मध्य प्रदेश Switch to English
प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार
चर्चा में क्यों?
भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस (21 अप्रैल 2025) के अवसर पर मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग को "साइबर तहसील पहल" के लिये प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार-2023 से सम्मानित किया।
मुख्य बिंदु
- साइबर तहसील पहल के बारे में:
- यह पहल प्रदेश में भूमि नामांतरण सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल, प्रभावी और नागरिकों के अनुकूल बनाने में सफल रही है।
- एकीकृत प्रणाली से न्यायालयों का प्रबंधन और प्रकरणों का निपटारा त्वरित और निष्पक्ष होता है।
- इस पहल से पारदर्शिता बढ़ी है और नागरिक अब अपने नामांतरण मामले की स्थिति को रिजल्ट्स और कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम (RCMS) पोर्टल के माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं।
- राज्य में 1 लाख 50 हज़ार से अधिक प्रकरणों का निपटारा किया जा चुका है।
- तहसील कार्यालयों पर नामांतरण प्रकरणों के कार्यभार में 25 प्रतिशत तक की कमी आई है।
- रियल-टाइम अपडेट, वेब GIS, संपदा और सारा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के एकीकरण से प्रक्रिया और सुगम हो गई है।
- इस पहल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है और अन्य राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड ने इसे अपनाने में रुचि दिखाई है।
वेब GIS
- यह इंटरनेट के माध्यम से भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) के उपयोग को संदर्भित करता है, जो ऑनलाइन भौगोलिक डाटा को साझा करने, दृश्य प्रस्तुत करने और विश्लेषण करने की अनुमति देता है।
- यह उपयोगकर्त्ताओं को मानचित्रों और स्थानिक डाटा के साथ दूरस्थ रूप से इंटरएक्ट करने और उसे एक्सेस करने में सक्षम बनाता है, जिससे सहयोग और जानकारी के व्यापक प्रसार को बढ़ावा मिलता है।
राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस
- परिचय
- यह हर साल 21 अप्रैल को पूरे भारत में मनाया जाता है। यह दिन उन सभी अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिये समर्पित है, जो देश के विभिन्न सार्वजनिक विभागों में काम करते हुए भारत की प्रशासनिक प्रणाली को मज़बूती से चलाते हैं। साथ ही, यह दिन सिविल सेवकों को यह याद दिलाने का भी कार्य करता है कि उनकी प्राथमिक ज़िम्मेदारी देश के नागरिकों की सेवा करना है।
- सिविल सेवक, विशेष रूप से उच्च प्रशासनिक पदों पर कार्यरत, नीतिगत निर्णयों को निर्धारित करने और उन्हें लागू करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। IAS, IPS और अन्य उच्च पदों पर नियुक्त अधिकारी नागरिकों से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिये अक्सर ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं।
- यह हर साल 21 अप्रैल को पूरे भारत में मनाया जाता है। यह दिन उन सभी अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिये समर्पित है, जो देश के विभिन्न सार्वजनिक विभागों में काम करते हुए भारत की प्रशासनिक प्रणाली को मज़बूती से चलाते हैं। साथ ही, यह दिन सिविल सेवकों को यह याद दिलाने का भी कार्य करता है कि उनकी प्राथमिक ज़िम्मेदारी देश के नागरिकों की सेवा करना है।
- उद्देश्य
- भारत सरकार सिविल सेवा दिवस का आयोजन हर वर्ष इस उद्देश्य से करती है, ताकि सिविल सेवक अपनी सेवा के प्रति फिर से समर्पित हो सकें और सार्वजनिक सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पुनः नवीनीकरण कर सकें।
- इस दिन का चयन इसलिये किया गया था क्योंकि 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने दिल्ली के मेटकाफ हाउस में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से संवाद करते हुए उन्हें 'भारत का स्टील फ्रेम' कहा था।
- यह शब्द इस बात को रेखांकित करता है कि सिविल सेवक प्रशासनिक व्यवस्था के मज़बूत स्तंभ होते हैं।


राजस्थान Switch to English
पोकरण में सोलर प्रोजेक्ट
चर्चा में क्यों?
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा जैसलमेर के पोकरण में 1.3 गीगावॉट पीक पावर क्षमता वाले सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया।
मुख्य बिंदु
- सोलर प्रोजेक्ट के बारे में:
- यह परियोजना पूरी तरह से मेड-इन-इंडिया मोड्यूल्स द्वारा बनाई गई है, जिसमें 90% सोलर मोड्यूल्स जयपुर स्थित रीन्यू कंपनी द्वारा निर्मित हैं।
- उद्देश्य: इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन बढ़ाना और पर्यावरण को कार्बन उत्सर्जन से बचाना है।
- विद्युत उत्पादन: इस परियोजना से सालाना लगभग 2490 मिलियन युनिट्स विद्युत का उत्पादन होगा, जो लगभग 5 लाख परिवारों की विद्युत जरूरतों को पूरा करेगा।कार्बन उत्सर्जन में कमी: परियोजना से 2.3 मिलियन टन कार्बन
- डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण में योगदान मिलेगा।भौगोलिक अवस्थिति: यह परियोजना राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में स्थित है और लगभग 3500 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है। यह क्षेत्र सोलर ऊर्जा के लिये उपयुक्त परिस्थितियाँ प्रदान करता है, जिससे परियोजना की सफलता की संभावना और बढ़ जाती है।
- ऊर्जा क्षेत्र में विकास: इस परियोजना के माध्यम से भविष्य में ऊर्जा की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ ही, ऊर्जा क्षेत्र में तेज़ी से विकास की संभावना है।
मेक इन इंडिया पहल:
- परिचय:
- वर्ष 2014 में लॉन्च किये गए मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य देश को एक अग्रणी वैश्विक विनिर्माण और निवेश गंतव्य में बदलना है।
- इसका नेतृत्त्व उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है।
- यह पहल दुनिया भर के संभावित निवेशकों और भागीदारों को 'न्यू इंडिया' की विकास गाथा में भाग लेने हेतु एक खुला निमंत्रण है।
- उद्देश्य:
- विनिर्माण क्षेत्र की संवृद्धि दर को बढ़ाकर 12-14% प्रतिवर्ष करना।
- वर्ष 2022 तक (संशोधित तिथि 2025) विनिर्माण से संबंधित 100 मिलियन अतिरिक्त रोज़गार सृजित करना।
- वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ाकर 25% करना।
सौर ऊर्जा
- परिचय
- सौर तापीय ऊर्जा (Solar Thermal Energy): इसमें सूरज की किरणों को ऊष्मा में बदलकर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। यह ऊर्जा गर्म पानी तैयार करने, तापमान नियंत्रित करने या उद्योगों में उपयोग की जाती है।
- सौर विद्युत ऊर्जा (Solar Photovoltaic Energy): इसमें सौर पैनल्स (Photovoltaic Cells) का उपयोग करके सूर्य प्रकश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह ऊर्जा घरों, उद्योगों और अन्य क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति के लिये उपयोग की जाती है।
- यह वह ऊर्जा है, जो सूर्य से प्राप्त होती है। यह एक नवीकरणीय और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है, जो पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे प्रचुर और स्थायी ऊर्जा स्रोतों में से एक है।
- सौर ऊर्जा का उपयोग मुख्यतः दो तरीकों से किया जाता है:
- सौर ऊर्जा के लाभ:
- यह एक नवीकरणीय ऊर्जा है, अर्थात यह हमेशा उपलब्ध रहती है।
- पर्यावरणीय प्रभाव कम है, क्योंकि यह प्रदूषण नहीं करती।
- यह स्थायी स्रोत है, जिससे लंबे समय तक ऊर्जा मिलती है।
- ऊर्जा संकट के समाधान के रूप में काम करती है, विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ विद्युत आपूर्ति सीमित होती है।


झारखंड Switch to English
झारखंड में भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य
चर्चा में क्यों?
झारखंड के लातेहार ज़िले में स्थित महुआदानर भेड़िया अभयारण्य भारत का पहला और एकमात्र भेड़ियों को समर्पित अभयारण्य है।
मुख्य बिंदु
- अभयारण्य के बारे में:
- यह सरना धर्म का पालन करने वाले जनजातीय समुदायों के निवास वाले क्षेत्र में स्थित है।
- 80% से अधिक स्थानीय आबादी सरना कोड का पालन करती है, जो एक प्रकृति-पूजक धर्म है जिसमें वनों, नदियों और प्राकृतिक तत्त्वों का सम्मान किया जाता है।
- भेड़िया संरक्षण का समर्थन करने वाली पारंपरिक मान्यताएँ:
- एक उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रथा है, जिसमें शीतकाल (नवंबर से फरवरी) के दौरान साल के जंगलों में मौसमी रूप से जाने से बचते है। यह प्रथा साल वृक्ष के पवित्र खिलने के मौसम से मेल खाती है।
- यह सांस्कृतिक प्रथा कम-से-कम मानवीय व्यवधान की अवधि का निर्माण करती है, जो भेड़ियों के महत्त्वपूर्ण प्रजनन और मांद बनाने के मौसम के साथ पूरी तरह से संरेखित होती है।
- वैज्ञानिक अनुसंधान से प्राप्त अंतर्दृष्टि:
- नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन, जिसका शीर्षक था "पारिस्थितिक और सांस्कृतिक कारकों को ध्यान में रखते हुए महुआडानर वुल्फ अभयारण्य के आदिवासी परिदृश्यों में भारतीय ग्रे भेड़ियों द्वारा मांद स्थल का चयन", ने इस बात की जाँच की कि भेड़िये इस अद्वितीय सांस्कृतिक-पारिस्थितिक व्यवस्था में मांद स्थल का चयन कैसे करते हैं।
- शोधकर्त्ताओं ने परिकल्पना की कि भेड़िये शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों को अपने मांद के लिये पसंद करेंगे, साथ ही सांस्कृतिक रूप से लगाए गए मानव परिहार क्षेत्रों से भी लाभान्वित होंगे।
- भारतीय भेड़ियों का भविष्य:
- भारतीय भूरे भेड़ियों और अन्य कम ज्ञात मांसाहारी प्रजातियों का भविष्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण और पारंपरिक ज्ञान के संयोजन पर निर्भर कर सकता है।
- संरक्षण रणनीतियों को महज कानूनी ढाँचे से आगे बढ़कर सांस्कृतिक मूल्यों को शामिल करना होगा, जिन्होंने लंबे समय से पारिस्थितिकी तंत्र को प्राकृतिक रूप से सुरक्षित रखा है।
इंडियन ग्रे वुल्फ
- भारतीय ग्रे वुल्फ (Canis lupus pallipes) ग्रे वुल्फ की एक उप-प्रजाति है जो दक्षिण-पश्चिम एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है।
- यह छोटे झुंड में रहता है और अन्य भेड़िया उप-प्रजातियों की तुलना में कम मुखर होता है।
- यह मुख्यतः रात्रिचर है, जो शाम से सुबह तक शिकार करता है।
- प्राकृतिक वास: यह भारत की झाड़ियों, घास के मैदानों और अर्द्ध-शुष्क कृषि-पारिस्थितिक तंत्र में एक शीर्ष शिकारी है। गर्म तापमान वाले क्षेत्रों में पनपता है। गर्म तापमान वाले क्षेत्रों में पनपता है।
- संरक्षण की स्थिति:
- IUCN: लुप्तप्राय (भारत में संख्या: 2,000 - 3,000)।
- CITES: परिशिष्ट I
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची I
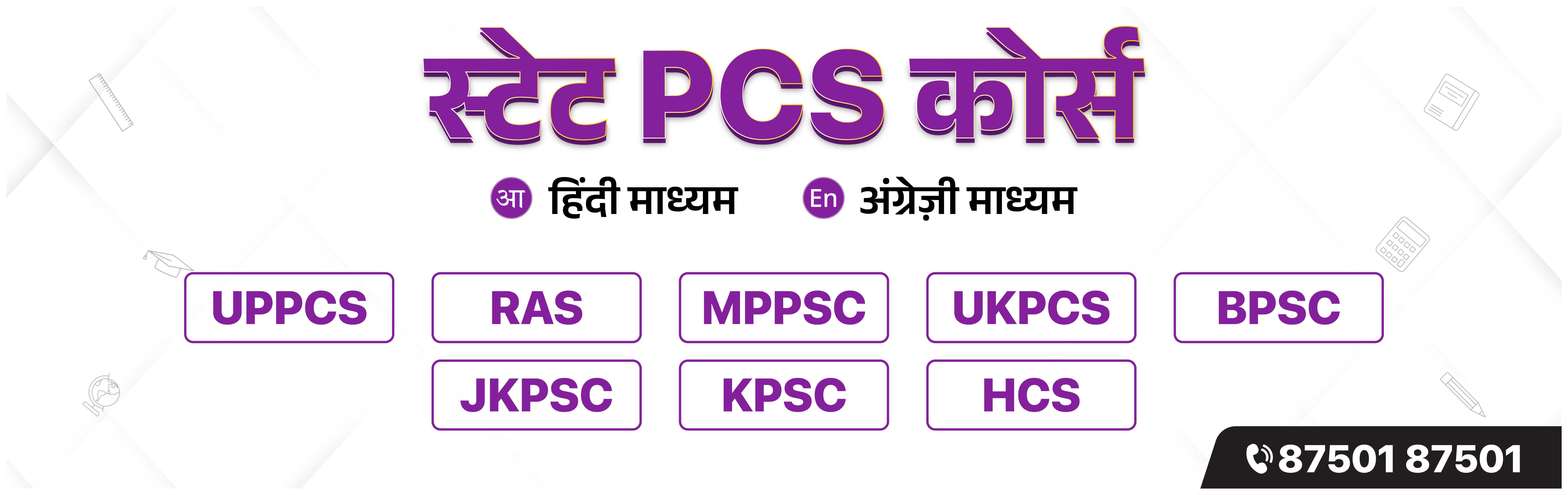
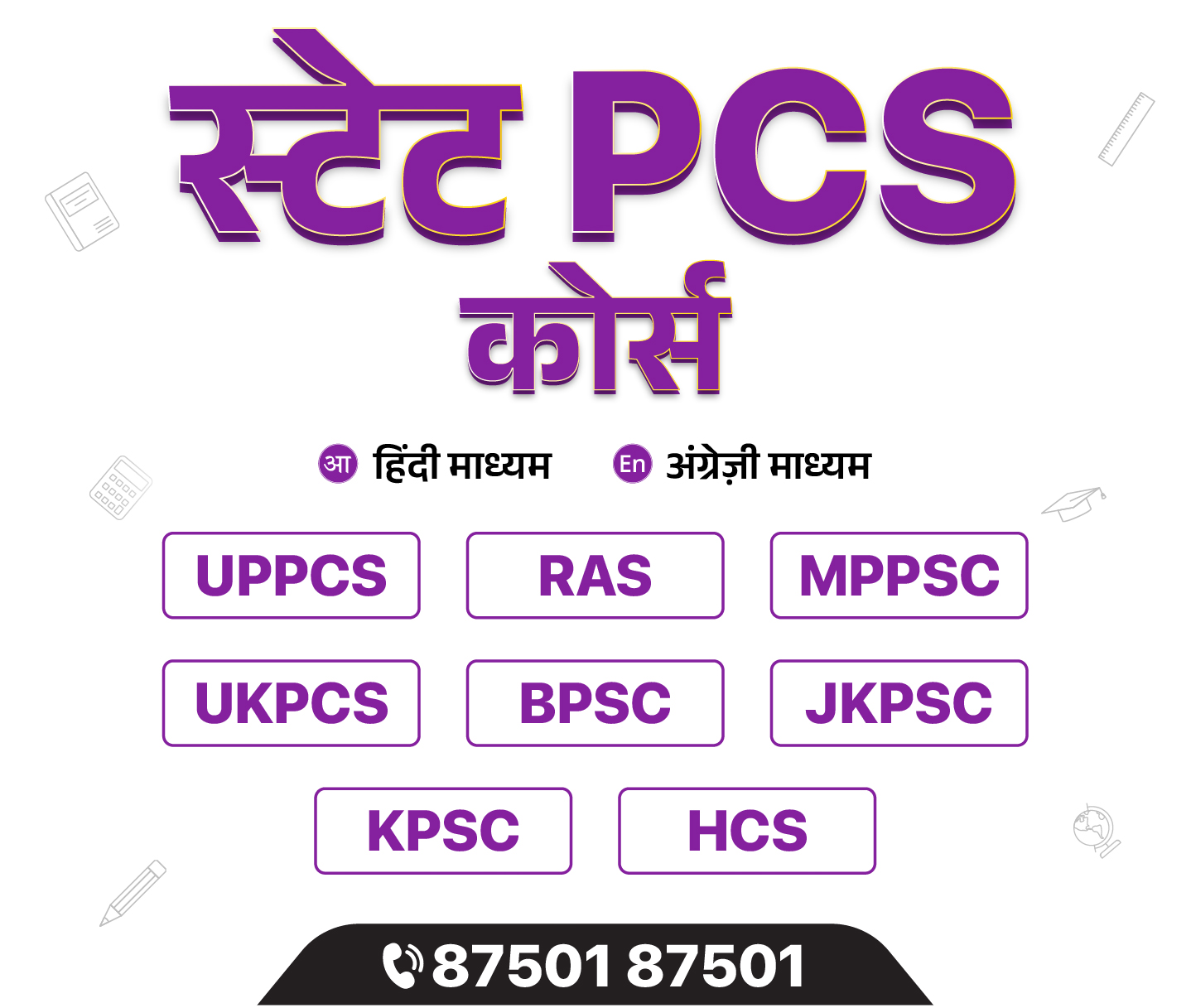
उत्तर प्रदेश Switch to English
उत्तर प्रदेश में इको-पर्यटन
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिये बाँधों और जलाशयों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है।
मुख्य बिंदु
- पहल के बारे में:
- इस पहल के तहत चित्रकूट, महोबा, सोनभद्र, हमीरपुर, झाँसी, सिद्धार्थनगर और बाँदा ज़िलों के सात प्रमुख बाँधों और झीलों पर बुनियादी ढाँचे का निर्माण किया जाएगा।
- इन स्थानों पर जल और साहसिक क्रीड़ा गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का सहयोग सुनिश्चित किया गया है।
- जिन जलाशयों और बाँधों को चुना गया है, उनमें शामिल हैं:
- गुंता बाँध (चित्रकूट)
- अर्जुन डैम (महोबा)
- धंधरौल डैम (सोनभद्र)
- मौदहा डैम (हमीरपुर)
- गढ़मऊ झील (झाँसी)
- मझौली सागर (सिद्धार्थनगर)
- नवाब टैंक (बाँदा)
- सरकार का उद्देश्य इन जलाशयों के प्राकृतिक सौंदर्य को आधुनिक पर्यटन सुविधाओं जैसे रिसॉर्ट, बोटिंग, वाटर स्पोर्ट्स, ट्रैकिंग और कैंपिंग के माध्यम से और भी आकर्षक बनाना है।
- इस योजना से स्थानीय स्तर पर रोज़गार सृजन और आर्थिक विकास को मज़बूती मिलेगी।
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग इन परियोजनाओं के लिये तकनीकी सहायता और आवश्यक अनुमतियाँ देगा, साथ ही बाँधों की सुरक्षा और संरचना को सुरक्षित रखने के मानकों का पालन सुनिश्चित करेगा।
- जल क्रीड़ा गतिविधियों के दौरान पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा।
इको टूरिज्म
- परिचय
- इको टूरिज्म पर्यटन का एक ऐसा रूप है, जो पर्यावरण के अनुकूल, सतत और प्राकृतिक क्षेत्रों पर केंद्रित होता है। इसमें प्राकृतिक क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, वर्षावनों आदि का इस तरह से भ्रमण किया जाता है कि वहाँ की जैवविविधता और संस्कृति को कोई क्षति न पहुँचे।
- उद्देश्य
- इसका उद्देश्य संरक्षण प्रयासों का समर्थन करते हुए, स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ पहुँचाना और आगंतुकों को प्रकृति के प्रति जागरूक करना है।
- इको टूरिज्म के प्रकार:
- इको टूरिज्म का वैश्विक परिप्रेक्ष्य:
- संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) ने इको टूरिज्म को सतत विकास के साधन के रूप में मान्यता दी है।

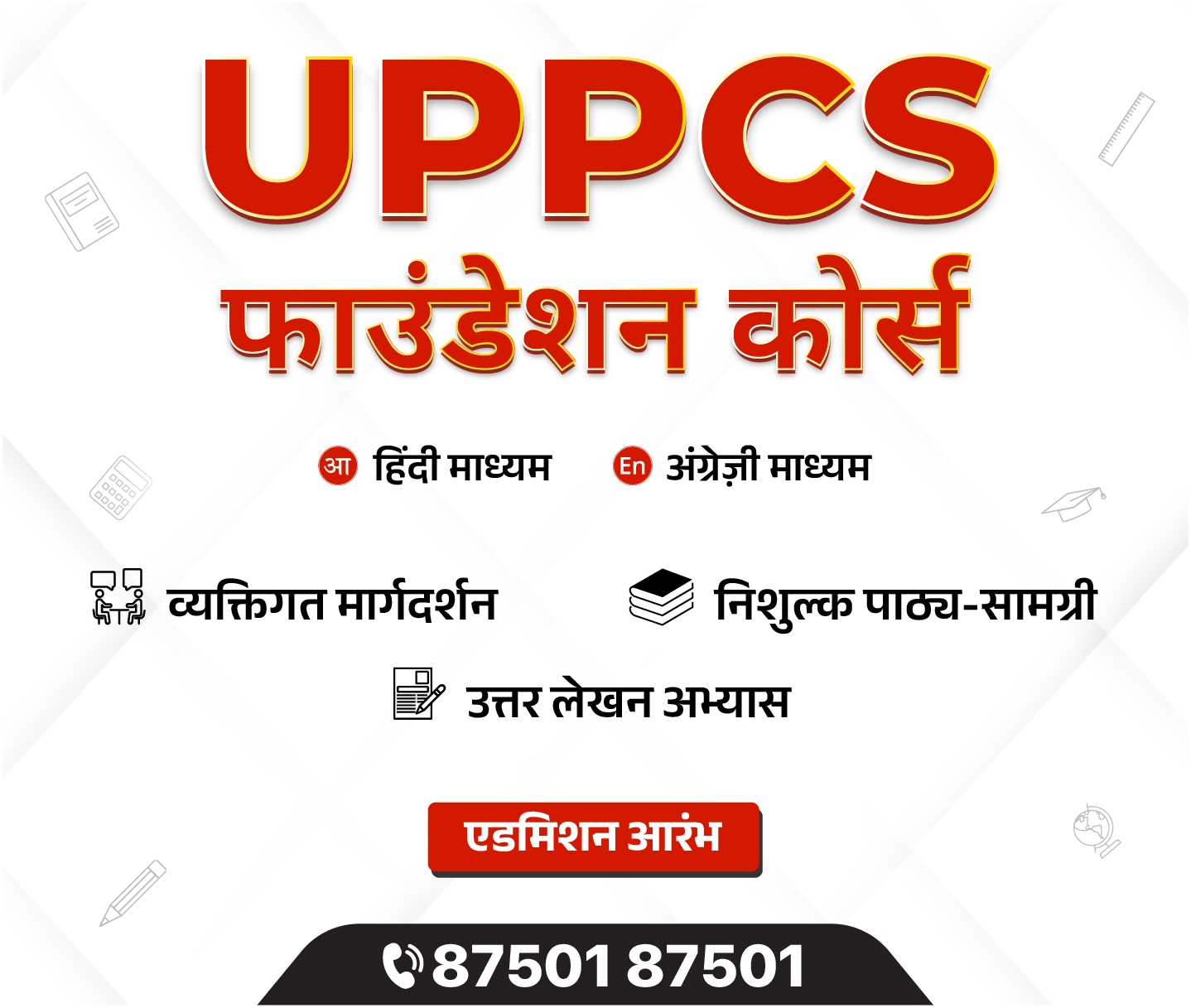
उत्तर प्रदेश Switch to English
कान्हा गौशाला
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश के आगरा नगर निगम की कान्हा गोशाला में दो मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिससे यह प्रदेश की पहली ऐसी गोशाला बन जाएगी जो बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग करेगी।
मुख्य बिंदु
- कान्हा गोशाला के बारे में:
- यह परियोजना नगर निगम द्वारा वर्ष 2025 तक हरित भविष्य के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए म्यूनिसिपल बॉण्ड योजना के तहत क्रियान्वित की जा रही है।
- इससे न केवल गोशाला की ऊर्जा आवश्यकताएँ स्वच्छ स्रोत से पूरी होंगी, बल्कि पर्यावरणीय संरक्षण को भी मज़बूती मिलेगी।
- गोशाला में पहले से ही 100 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं, जो स्वच्छ ऊर्जा का उदाहरण हैं।
- गोशाला में गोबर से गोकाष्ठ बनाया जा रहा है, जिसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों और अंतिम संस्कार में लकड़ी के विकल्प के रूप में किया जा रहा है। इससे वनों की कटाई को रोकने और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल रही है।
- यह परियोजना नगर निगम द्वारा वर्ष 2025 तक हरित भविष्य के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए म्यूनिसिपल बॉण्ड योजना के तहत क्रियान्वित की जा रही है।
- अस्थिति
- गोशाला ऐसी भूमि पर स्थित है, जहाँ मिट्टी बंजर और भूजल खारा है। इसके बावजूद, यहाँ मियावाकी तकनीक द्वारा 5000 वर्ग मीटर क्षेत्र में घना जंगल विकसित किया गया है, जो जैवविविधता को बढ़ावा देता है और एक प्राकृतिक ऑक्सीजन ज़ोन के रूप में कार्य करता है।
- यह गोशाला अब ऊर्जा, हरियाली और नवाचार का एक प्रमुख मॉडल बन चुकी है।
नगर निगम बॉण्ड
- यह वे ऋण उपकरण हैं, जो शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) द्वारा बुनियादी ढाँचे और विकास परियोजनाओं के लिये निधि जुटाने के उद्देश्य से जारी किये जाते हैं।
- लाभ: सरकारी निधियों पर निर्भरता कम करना, वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाना, निजी निवेश को आकर्षित करना और दीर्घकालिक शहरी वित्तपोषण को सक्षम बनाना।
- चुनौतियाँ: राज्य अनुदानों पर भारी निर्भरता (वित्त वर्ष 24 में राजस्व का 38%) के कारण कम निर्गम। पुणे, अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और लखनऊ जैसे कुछ ही शहरों ने बॉण्ड जारी किये हैं।
- व्यय पैटर्न (वित्त वर्ष 2018-2025): नगरपालिकाओं द्वारा बॉण्ड के माध्यम से जुटाई गई अधिकांश धनराशि शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज के लिये आवंटित की गई, इसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा और नदी विकास का स्थान रहा।
मियावाकी वृक्षारोपण विधि:
- मियावाकी पद्यति के प्रणेता जापानी वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी (Akira Miyawaki) हैं। इस पद्यति से बहुत कम समय में जंगलों को घने जंगलों में परिवर्तित किया जा सकता है।
- यह कार्यविधि 1970 के दशक में विकसित की गई थी, जिसका मूल उद्देश्य भूमि के एक छोटे से टुकड़े के भीतर हरित आवरण को सघन बनाना था।
- इस कार्यविधि में पेड़ स्वयं अपना विकास करते हैं और तीन वर्ष के भीतर वे अपनी पूरी लंबाई तक बढ़ जाते हैं।
- मियावाकी पद्धति में उपयोग किये जाने वाले पौधे ज़्यादातर आत्मनिर्भर होते हैं और उन्हें खाद एवं जल देने जैसे नियमित रख-रखाव की आवश्यकता नहीं होती है।
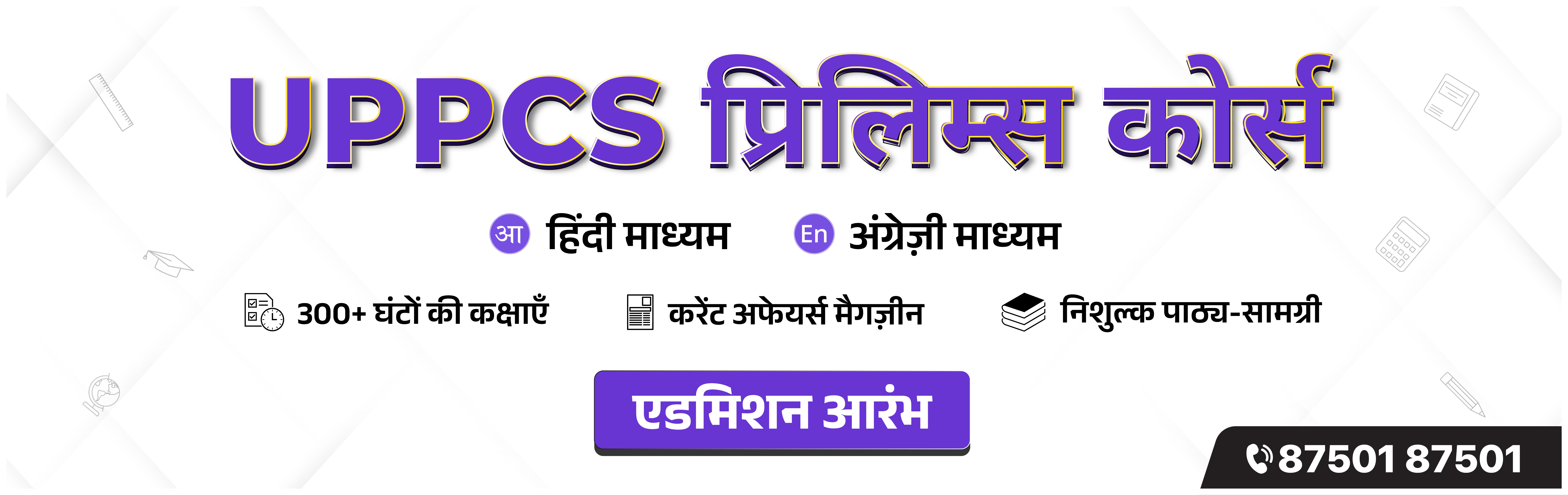


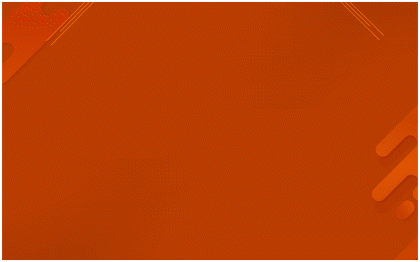


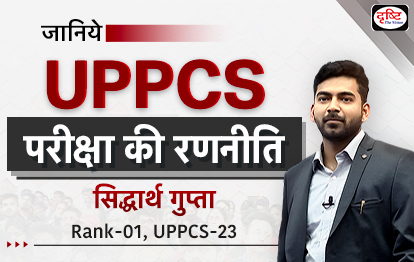
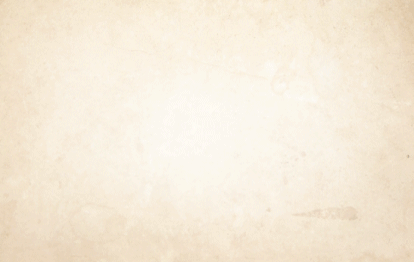

.jpg)
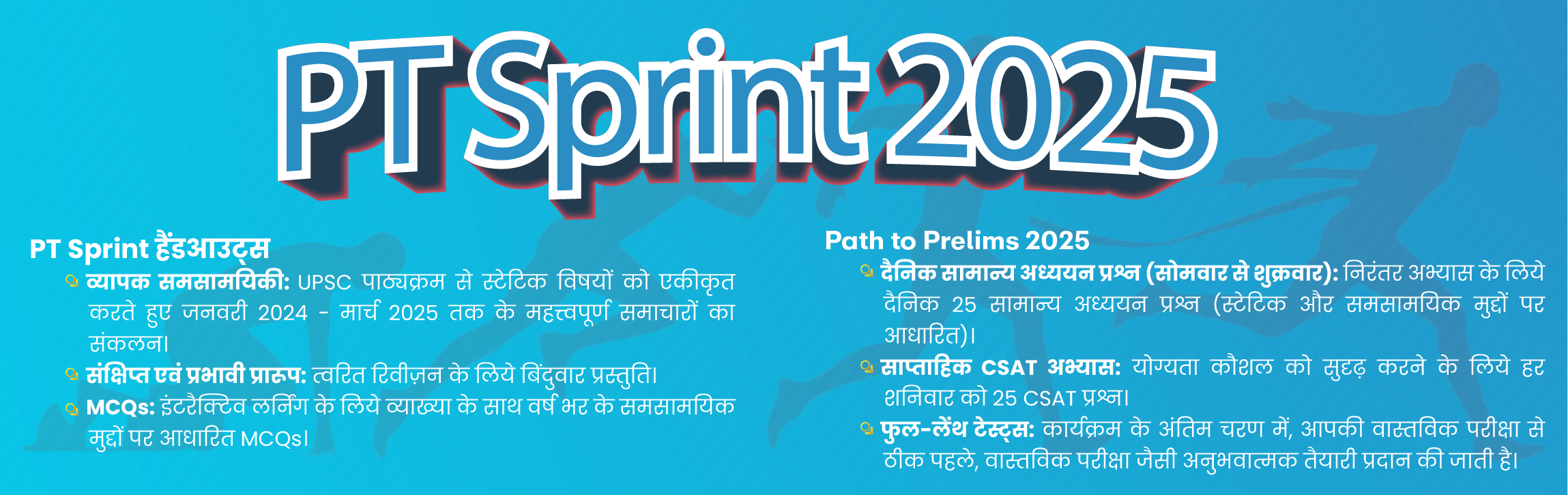
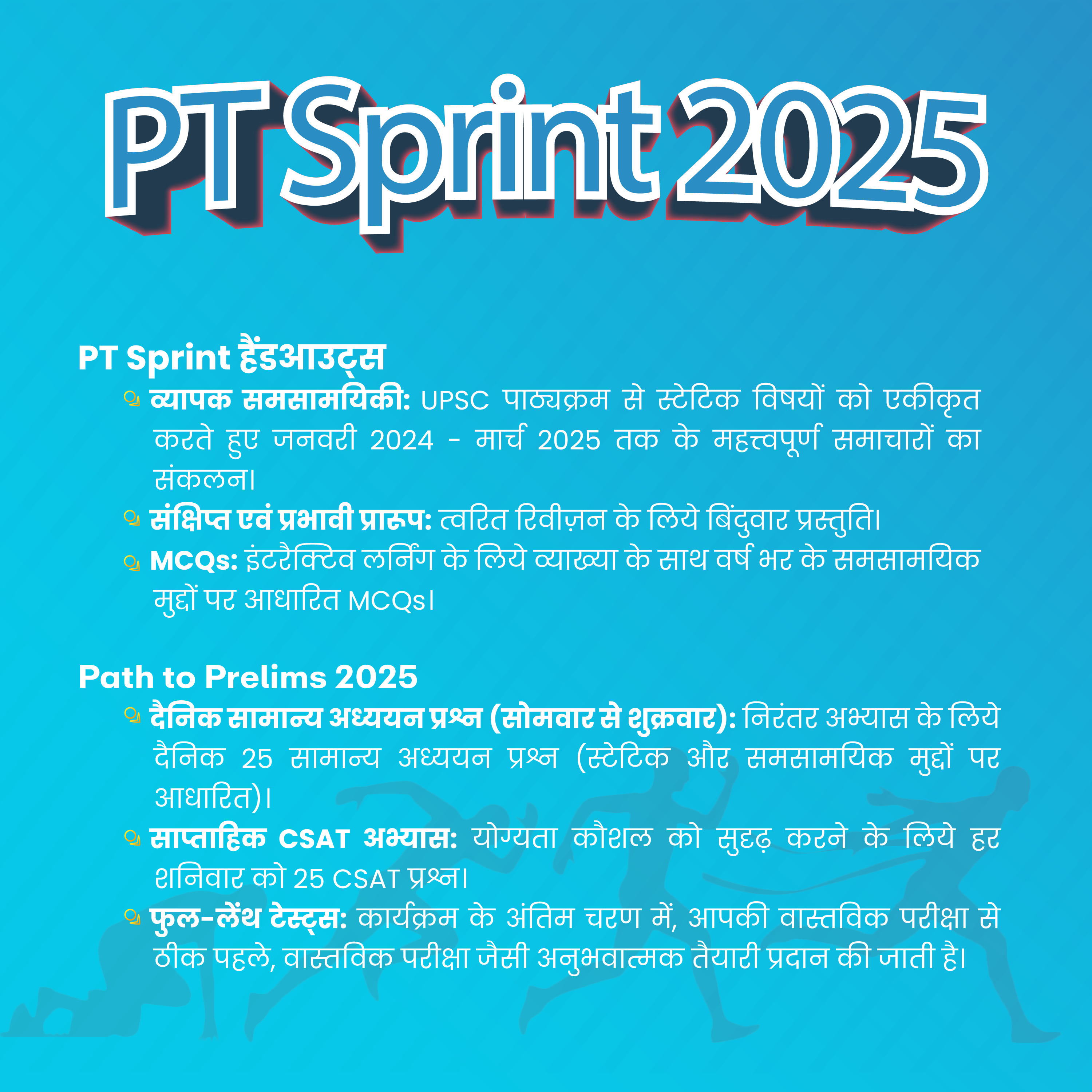

%201.jpeg)
.jpg)


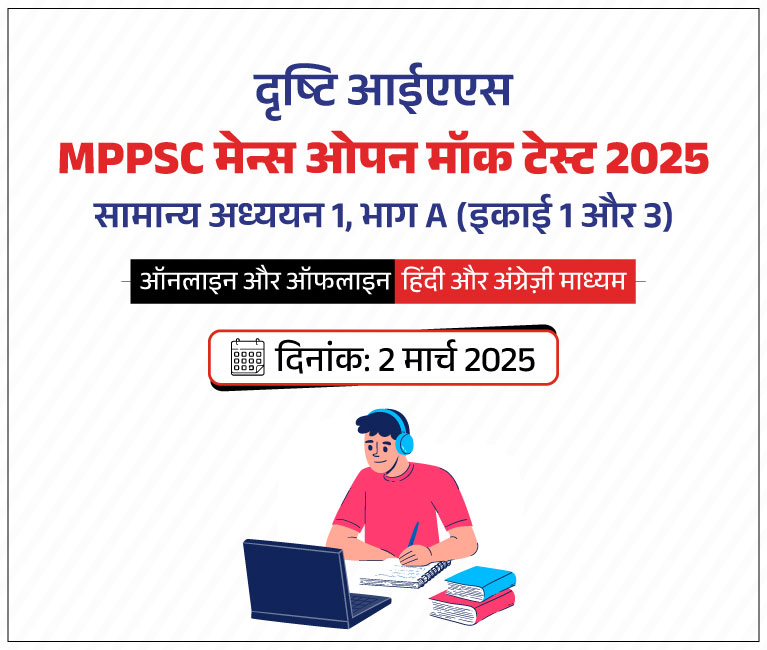
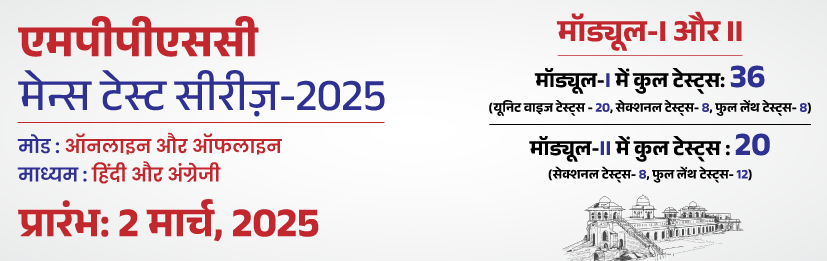

%20MPPCS%202025%20Desktop%20H.jpg)
%20MPPCS%202025%20Mobile%20H%20(1).jpg)

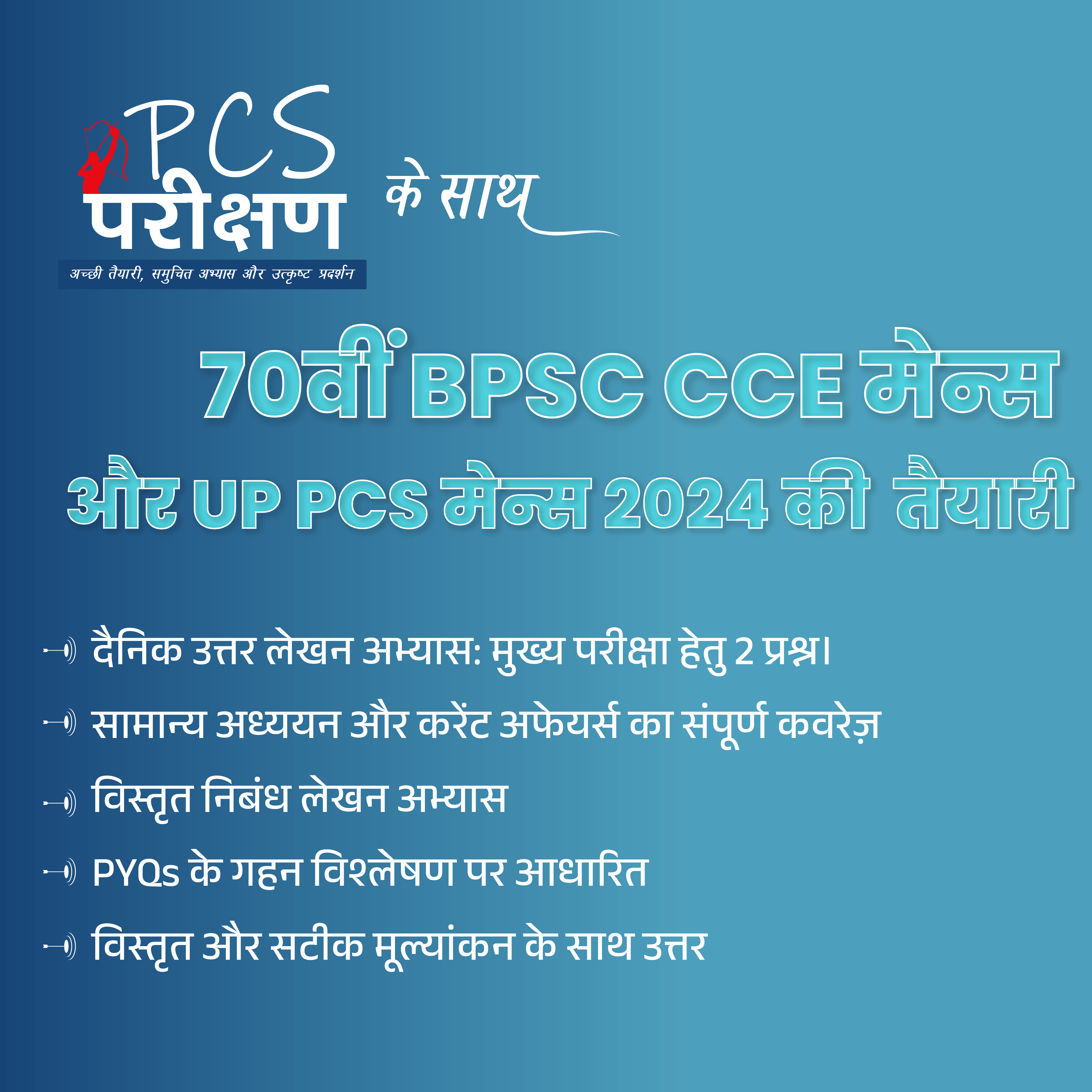


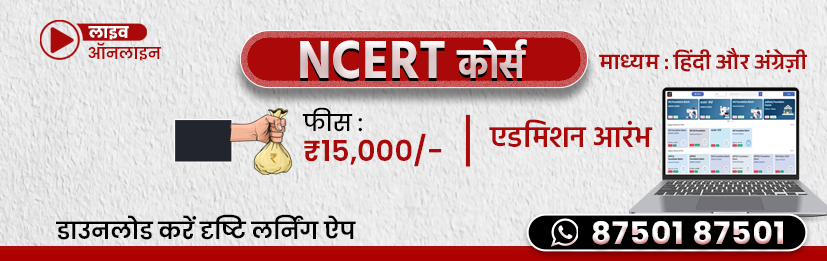
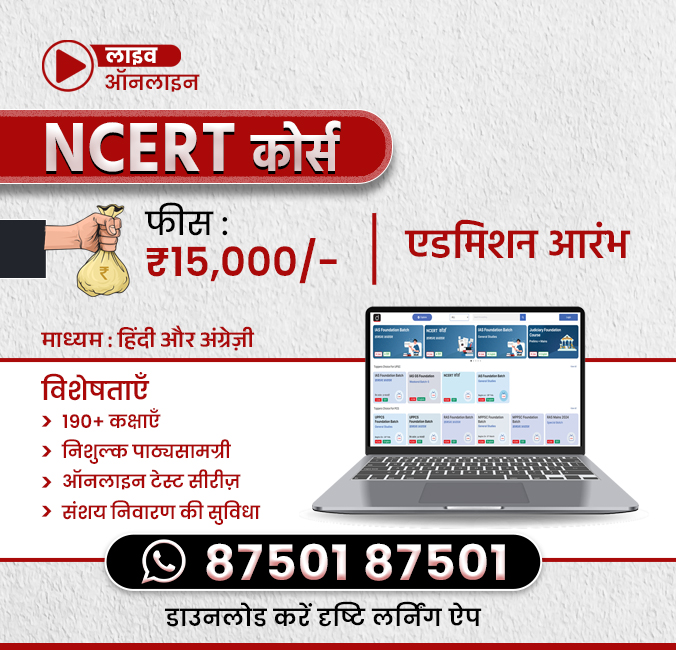

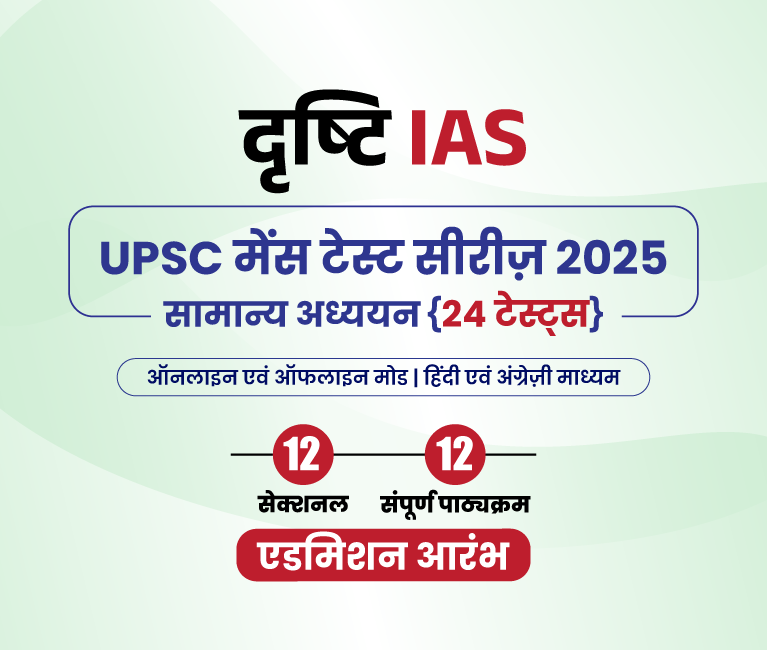
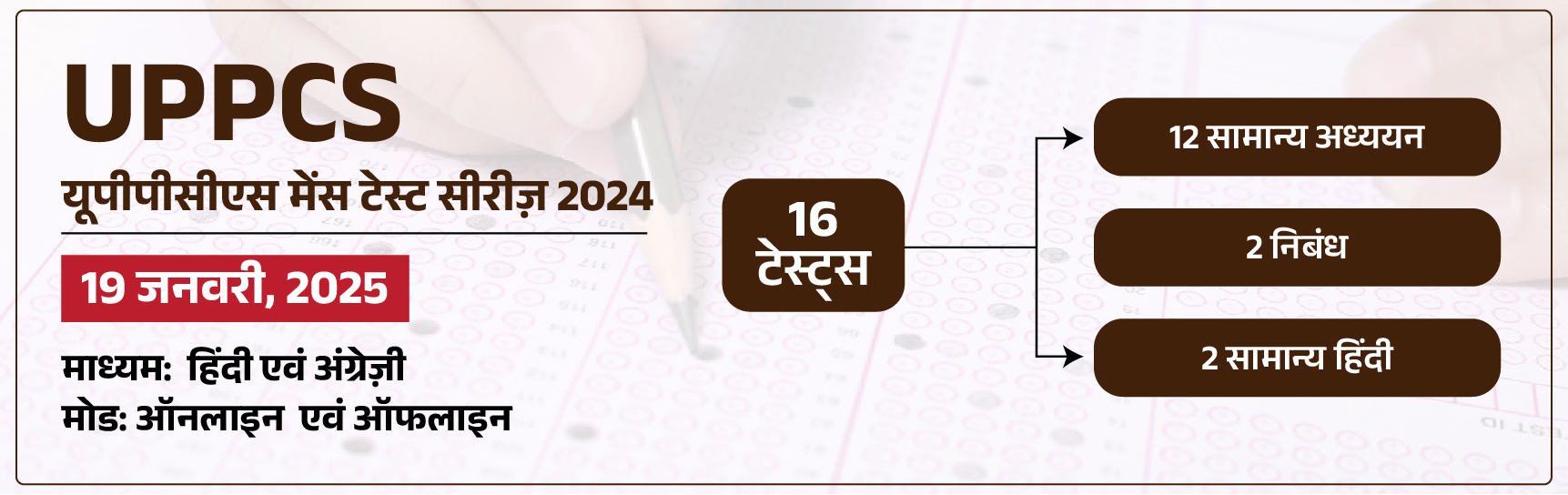
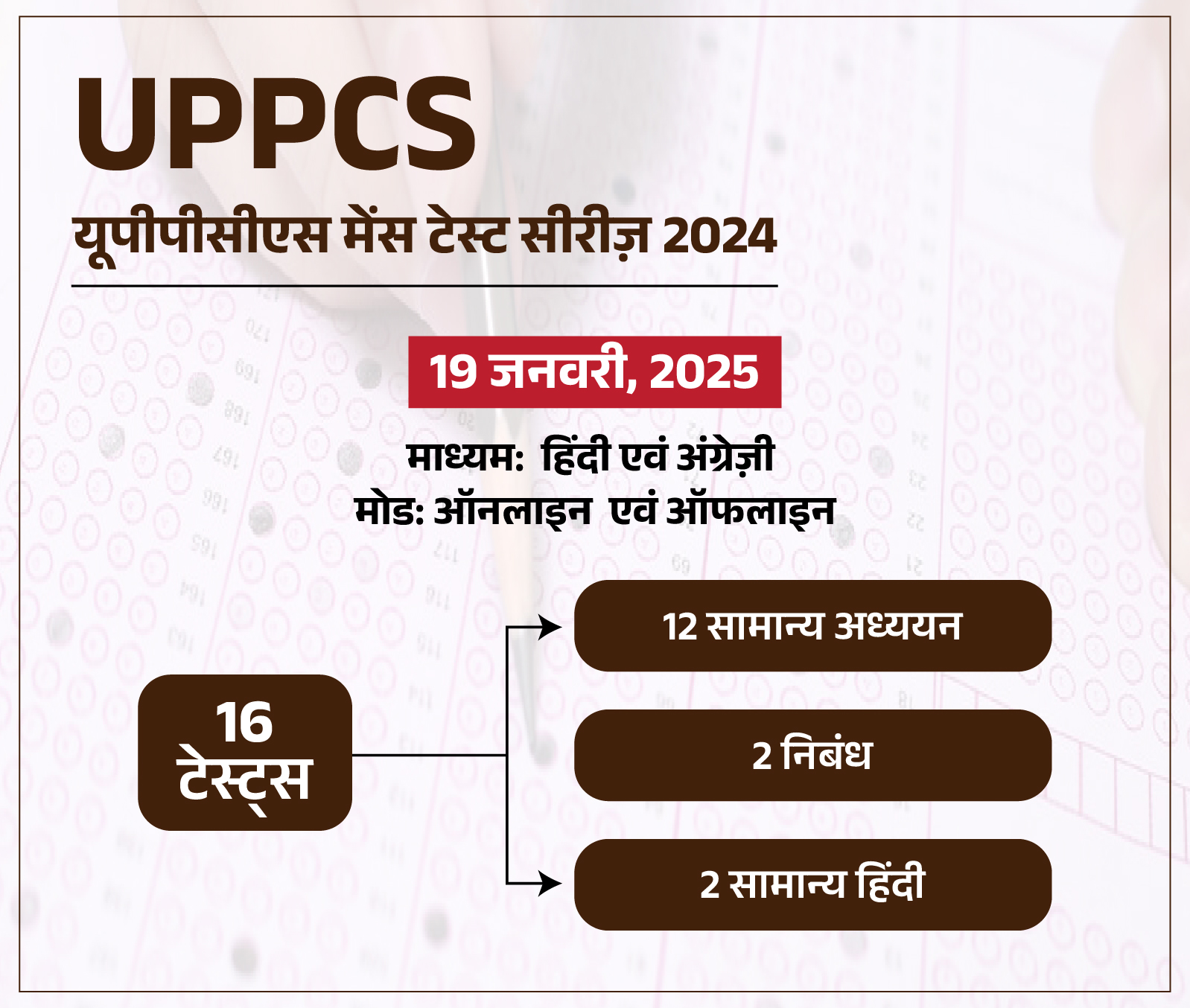



 PCS परीक्षण
PCS परीक्षण


