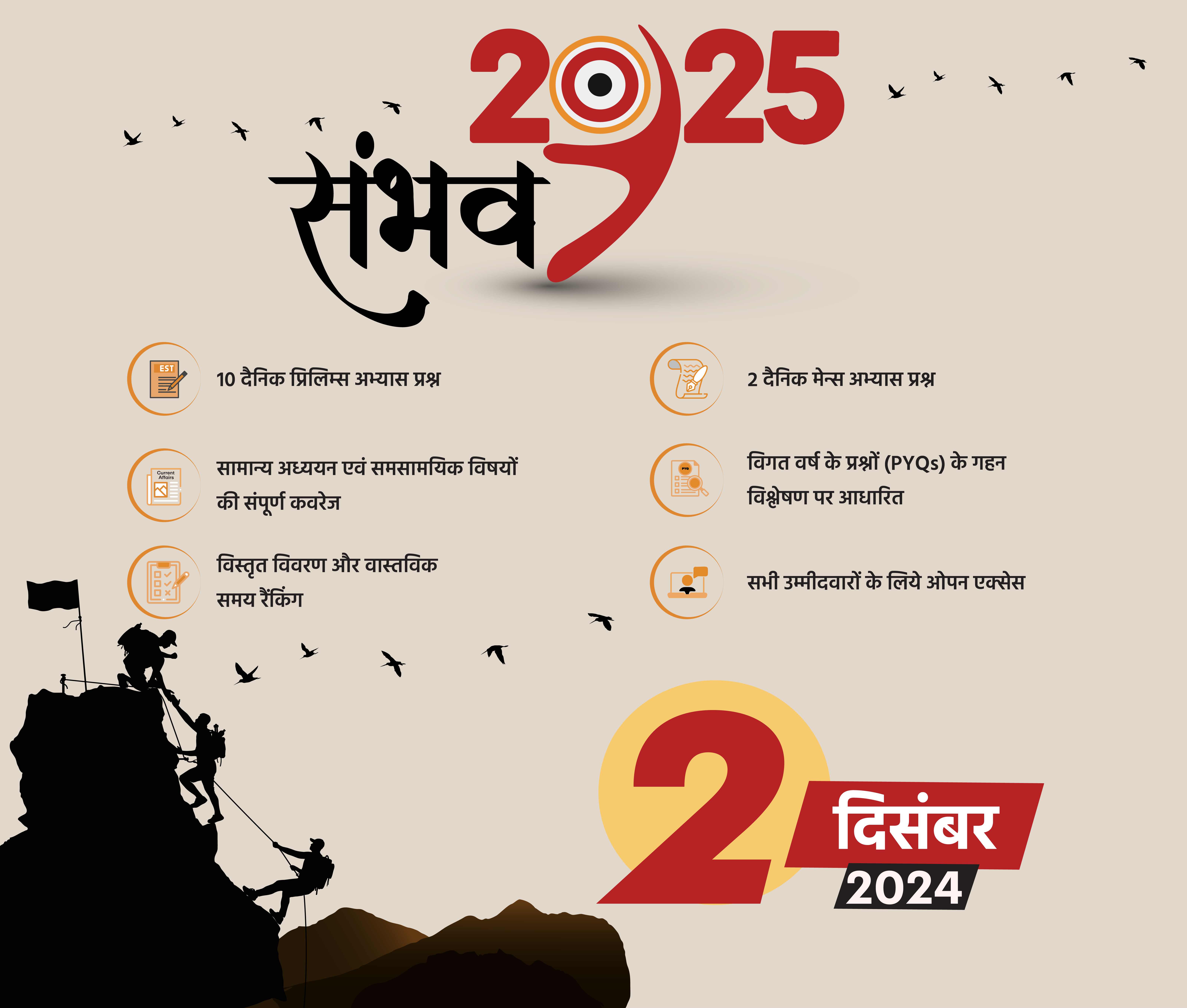भारतीय राजव्यवस्था
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन
प्रारंभिक परीक्षा:राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356, कुकी-ज़ो-मार और मैतेई, अनुच्छेद 355, राज्यपाल, साधारण बहुमत, 44वाँ संशोधन अधिनियम 1978, राष्ट्रीय आपातकाल, निर्वाचन आयोग, राज्य समेकित निधि मुख्य परीक्षा:राष्ट्रपति शासन और न्यायिक व्याख्या से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। |
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
चर्चा में क्यों?
केंद्र ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया है साथ ही मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद राज्य विधानसभा को भंग कर दिया है।
मणिपुर में हो रहे संघर्ष को सुलझाने में राष्ट्रपति शासन किस प्रकार सहायक हो सकता है?
- प्रशासन की तटस्थता: केंद्रीय प्रशासन जातीय हिंसा से निपटने में पक्षपातपूर्ण रवैये के आरोपों को हटा देगा, तथा कुकी-ज़ो-मार और मैतेई दोनों समुदायों को संरक्षित करेगा।
- राज्यपाल की निगरानी में केंद्रीय बल जातिगत हिंसा को रोक सकते हैं तथा राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रख सकते हैं।
- चुनावी स्थिरता: शासन के क्षरण को रोकने के लिये सत्तारूढ़ दल के आंतरिक विवादों को समाप्त करती है।
- पुनर्वास: 20 माह से अधिक समय से शिविरों में रह रहे 60,000 विस्थापित लोगों के लिये उचित राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करना।
और पढ़ें... मणिपुर में अशांति का कारण क्या था?
राष्ट्रपति शासन क्या है?
- राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य सरकार और उसकी विधानसभा को भंग करने से है, जिससे राज्य केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ जाता है।
- यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया गया है।
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुसार कार्य करे।
- यदि कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में विफल रहती है तो केंद्र अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाकर हस्तक्षेप कर सकता है।
- राष्ट्रपति शासन को राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है।
उद्घोषणा के आधार:
- अनुच्छेद 356 : यदि राष्ट्रपति को लगता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर सकती तो वह राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ऐसा निम्न आधारों पर किया जा सकता है:
- राज्यपाल की सिफारिश पर
- राष्ट्रपति के विवेक पर, राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी।
- अनुच्छेद 365: यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता है कि उसकी सरकार संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर सकती।
- संसदीय अनुमोदन: राष्ट्रपति शासन की घोषणा को दो माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिये।
- यदि राष्ट्रपति शासन की घोषणा लोकसभा के भंग होने पर की जाती है, या यदि लोकसभा बिना किसी अनुमोदन के दो महीने के भीतर भंग हो जाती है, तो यह लोकसभा के पुनः आहूत होने के 30 दिन बाद तक वैध रहती है, बशर्ते कि इस अवधि के दौरान राज्य सभा इसे अनुमोदित कर दे।
- राष्ट्रपति शासन को मंजूरी देने या बढ़ाने के लिये संसद में साधारण बहुमत (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत) की आवश्यकता होती है।
- अवधि: राष्ट्रपति शासन प्रारंभ में छह महीने तक रहता है, जिसे हर छह महीने में संसद की मंजूरी से 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
- 44वाँ संशोधन अधिनियम, 1978 राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष से अधिक बढ़ाने की अनुमति केवल तभी देता है जब:
- राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत में या राज्य के किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता है।
- चुनाव आयोग द्वारा प्रमाणित किया गया है कि कठिनाइयों के कारण राज्य विधानसभा के चुनाव नहीं कराए जा सकते।
- राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिये बढ़ाने हेतु संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिये 67वाँ संशोधन अधिनियम, 1990 और 68वाँ संशोधन अधिनियम, 1991 पंजाब में उग्रवाद के दौरान राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष से अधिक अवधि हेतु बढ़ाने के लिये लागू किया गया था।
- प्रभाव: राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राष्ट्रपति को असाधारण शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं।
- कार्यकारी शक्तियाँ: राज्य के कार्यों का कार्यान्वयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता हैं। राज्यपाल उनकी ओर से प्रशासन का कार्य करते हैं, तथा मुख्य सचिव और नियुक्त सलाहकार उनकी सहायता करते हैं।
- विधायी शक्तियाँ: राज्य विधानमंडल को निलंबित या भंग कर दिया जाता है, तथा संसद अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है या राष्ट्रपति या किसी निर्दिष्ट निकाय को कानून बनाने का अधिकार सौंपती है।
- राष्ट्रपति शासन के दौरान बनाए गए कानून तब तक लागू रहते हैं जब तक कि राज्य विधानमंडल द्वारा उन्हें निरस्त नहीं कर दिया जाता।
- वित्तीय नियंत्रण: राष्ट्रपति राज्य समेकित निधि से व्यय को अधिकृत कर सकता है जब तक कि उसे संसद द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए।
- निरसन: राष्ट्रपति, संसदीय अनुमोदन के बिना भी किसी भी समय राष्ट्रपति शासन को निरस्त कर सकते हैं।
राष्ट्रपति शासन लगाने पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख क्या है?
- एस.आर. बोम्मई केस, 1994: सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 356 न्यायिक समीक्षा के अधीन है, और राज्य सरकार की बर्खास्तगी राज्यपाल की राय पर नहीं, बल्कि फ्लोर टेस्ट के आधार पर होनी चाहिये।
- सर्बानंद सोनोवाल केस, 2005: अनुच्छेद 355 का दायरा बढ़ा दिया गया, जिससे संघ को राज्य शासन और संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिये व्यापक कार्रवाई करने में सक्षम बनाया गया।
- रामेश्वर प्रसाद केस, 2006: सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा को बिना शक्ति परीक्षण के भंग करने की निंदा की तथा अनुच्छेद 356 के राजनीतिक दुरुपयोग की आलोचना की।
- अनुच्छेद 356 का उपयोग दलबदल जैसी सामाजिक बुराइयों से निपटने के लिए नहीं किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 361 के तहत अभिरक्षा न्यायालय को कार्यवाही की वैधता की समीक्षा करने से नहीं रोका गया है।
और पढ़ें: अनुच्छेद 356 का उचित और अनुचित उपयोग
राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में क्या सिफारिशें हैं?
- सरकारिया आयोग (1987): इसने अनुच्छेद 356 का संयमित प्रयोग करने की सिफारिश की तथा कहा कि इसका प्रयोग केवल अंतिम उपाय (जब राज्य की संवैधानिक विफलता को हल करने के लिए सभी विकल्प विफल हो जाएँ) के रूप में किया जाना चाहिये।
- पुंछी आयोग (2010): इसने अनुच्छेद 355 और 356 के तहत "स्थानीय आपातकालीन प्रावधानों" का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत किसी ज़िले या उसके कुछ हिस्सों में 3 महीने तक के लिए राज्यपाल शासन की अनुमति दी गई।
- राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग (NCRWC, 2000): इसने कहा कि अनुच्छेद 356 को हटाया नहीं जाना चाहिये बल्कि इसका प्रयोग संयम से तथा केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिये।
- यदि चुनाव नहीं हो सकते तो आपातकाल के बिना भी राष्ट्रपति शासन जारी रह सकता है। अनुच्छेद 356 में तदनुसार संशोधन किया जाना चाहिये।
- अंतर-राज्यीय परिषद (अनुच्छेद 263): राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने वाली राज्यपाल की रिपोर्ट विस्तृत एवं व्याख्यात्मक होनी चाहिये।
- राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले संबंधित राज्य को चेतावनी दी जानी चाहिये।
- राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी देने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी।
और पढ़ें: सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग, वेंकटचलैया आयोग (NCRWC)
निष्कर्ष
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने का उद्देश्य तटस्थ शासन सुनिश्चित करने के साथ कानून और व्यवस्था बनाए रखने एवं राजनीतिक संवाद को सुविधाजनक बनाकर स्थिरता बहाल करना है। हालाँकि, पिछले न्यायिक फैसलों और आयोग की सिफारिशों में राजनीतिक दुरुपयोग को रोकने तथा संघवाद को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 356 के सतर्क एवं कम उपयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
|
दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों तथा न्यायिक व्याख्याओं पर चर्चा कीजिये। |
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न: यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शत्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, तो (2018) (a) उस राज्य की विधानसभा स्वत: भंग हो जाती है। उत्तर: (b) मेन्सQ. भारत के राष्ट्रपति द्वारा किन परिस्थितियों में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? जब ऐसी घोषणा लागू रहती है तो इसके क्या परिणाम होते हैं? (2018) |

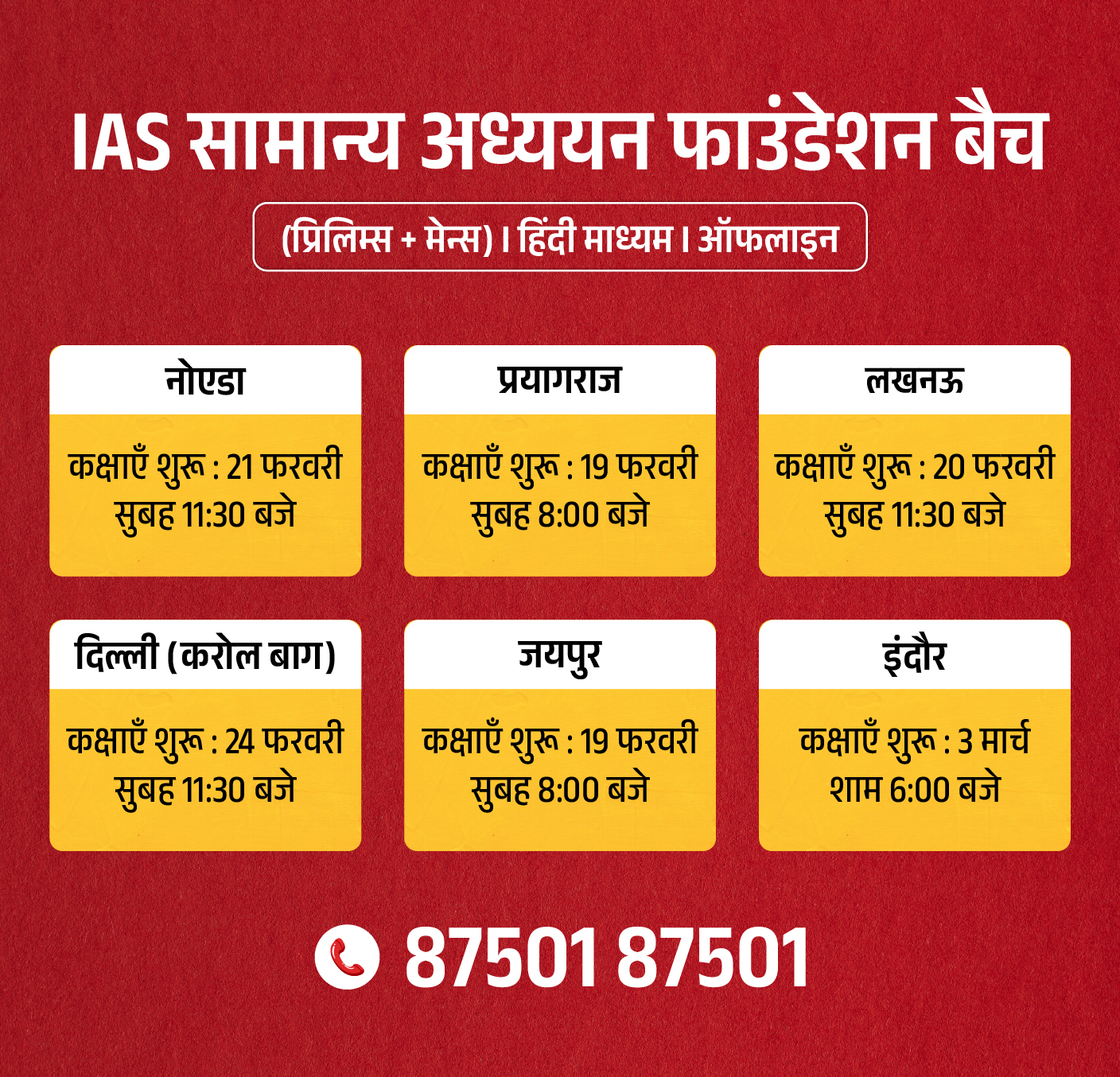
शासन व्यवस्था
मॉब लिंचिंग
प्रिलिम्स के लिये:भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, NCB, तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ मामला 2018 मेन्स के लिये:मॉब लिंचिंग और धार्मिक कट्टरवाद: चुनौतियाँ और आगे की राह |
स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स
चर्चा में क्यों?
सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवहार्यता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा हत्या) और गौ-रक्षा के नाम पर हिंसा के मामलों में मुआवजे के रूप में एक समान राशि तथा निगरानी के लिये राष्ट्रव्यापी निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया है।
- हालाँकि, इसने पुनः पुष्टि की कि उसके वर्ष 2018 के तहसीन पूनावाला दिशा-निर्देश संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सभी राज्यों के लिये बाध्यकारी हैं।
मॉब लिंचिंग क्या है?
- परिचय:
- मॉब लिंचिंग एक सामूहिक हिंसा है, जिसमें एक समूह कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए, कथित गलत कार्य के आधार पर व्यक्तियों को गैरकानूनी रूप से दंडित करता है।
- मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा हत्या) सामूहिक हिंसा का एक रूप है, जिसमें एक समूह द्वारा कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए कथित अपराधों के लिये लोगों को अवैध रूप से दंडित किया जाता है।
- गौ-रक्षा के नाम पर की जाने वाली हिंसा, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सद्भाव के लिये खतरा है, जो प्रायः संदेह से प्रेरित होती है।
- मॉब लिंचिंग के कारण:
- संस्कृति या पहचान के लिये कथित खतरा: लिंचिंग तब होती है जब किसी व्यक्ति या समूह को सांस्कृतिक, धार्मिक या पारंपरिक मूल्यों के लिये खतरा माना जाता है।
- सामान्य कारणों में अंतर्जातीय/अंतरधार्मिक संबंध, खान-पान की आदतें, या सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने वाले रीति-रिवाज शामिल हैं।
- फेक न्यूज़: फेक न्यूज़, जो अक्सर सोशल मीडिया और मौखिक रूप से फैलाई जाती हैं, मॉब लिंचिंग में योगदान दे सकती हैं।
- सामाजिक-राजनीतिक तनाव: भूमि विवाद, संसाधन प्रतिस्पर्द्धा और आर्थिक असमानताओं से उत्पन्न तनाव हिंसा में बदल सकता है, जिसका अक्सर राजनीतिक लाभ के लिये शोषण किया जाता है।
- सांप्रदायिक विभाजन: ऐतिहासिक धार्मिक, जातीय या सांप्रदायिक तनाव अक्सर लिंचिंग की घटनाओं के लिये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं।
- नैतिक सतर्कता: स्वघोषित संगठन सामाजिक मूल्यों के प्रति अपनी धारणा को कायम रखने के लिये हिंसा का प्रयोग करते हैं, विशेष रूप से उन लोगों को निशाना बनाते हैं जिनके बारे में उनका मानना है कि वे उनका उल्लंघन कर रहे हैं।
- संस्कृति या पहचान के लिये कथित खतरा: लिंचिंग तब होती है जब किसी व्यक्ति या समूह को सांस्कृतिक, धार्मिक या पारंपरिक मूल्यों के लिये खतरा माना जाता है।
भारत में मॉब लिंचिंग से संबंधित विधिक प्रावधान क्या हैं?
- भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023:
- धारा 103(2): मॉब लिंचिंग
- जब 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर नस्ल, जाति, समुदाय, लैंगिक हिंसा, जन्म स्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर हत्या करता है।
- सज़ा: मृत्युदंड या आजीवन कारावास और ज़ुर्माना।
- धारा 117(4): भीड़ द्वारा गंभीर चोट पहुँचाना
- जब 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर समान भेदभावपूर्ण आधार पर गंभीर चोट पहुँचाता है।
- सज़ा: 7 वर्ष तक का कारावास और ज़ुर्माना।
- धारा 103(2): मॉब लिंचिंग
- तहसीन पूनावाला मामला, 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश:
- सर्वोच्च न्यायालय ने मॉब लिंचिंग की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति या समूह कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता।
- न्यायालय ने चेतावनी दी कि अनियंत्रित लिंचिंग "नई सामान्य बात" बन सकती है और इस बात पर ज़ोर दिया कि सभ्य समाज में भीड़ द्वारा न्याय का कोई स्थान नहीं है।
- इसमें कहा गया कि नागरिकों की सुरक्षा करना तथा लक्षित हिंसा को रोकना राज्य का कर्त्तव्य है।
- इसने अमेरिकी कानूनी उदाहरणों का हवाला देते हुए इस बात पर बल दिया कि भीड़ द्वारा न्याय, विधि के शासन को कमज़ोर करता है।
- मॉब लिंचिंग के लिये सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश:
- उकसावे के खिलाफ सख्त कार्रवाई: घृणास्पद भाषण या फर्जी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ IPC की धारा 153A (BNS में धारा 196) के तहत (विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाने के लिये) स्वतः FIR दर्ज़ की जाएगी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने मॉब लिंचिंग की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति या समूह कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता।
- निवारक उपाय: राज्य प्रत्येक ज़िले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करेंगे। इसमें
- संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना और पुलिस गश्त बढाना, एवं
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को अभद्र भाषा तथा फर्जी खबरों पर अंकुश लगाना शामिल है।
- दंडात्मक और उपचारात्मक उपाय: प्रत्येक ज़िले में फास्ट-ट्रैक अदालतें 6 माह के भीतर मामलों का निपटारा करेंगी।
- भीड़ द्वारा हत्या जैसे अपराधों के लिये आजीवन कारावास सहित कठोर सज़ा का प्रावधान।
- लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई।
- पीड़ितों को मुआवज़ा: राज्यों को चोट की गंभीरता, आजीविका की हानि और चिकित्सा व्यय के आधार पर मुआवज़ा हेतु योजना विकसित करनी होगी।
- अधिकारियों की जवाबदेही: लिंचिंग को रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई।
- निगरानी और विधायी उपाय: राज्यों को मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
- संसद से राष्ट्रीय स्तर पर लिंचिंग विरोधी कानून बनाने का आग्रह किया गया (यह लंबित है), हालाँकि राजस्थान और मणिपुर ने राज्य स्तर पर कानून बना लिये हैं।
माॅब लिंचिंग को रोकने में क्या चुनौतियाँ हैं?
- विधिक खामियाँ और विधियों का अप्रभावी प्रवर्तन: भारत में लिंचिंग विरोधी कोई विशिष्ट कानून नहीं है जिसके कारण ऐसे अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई में बाधा आती है। हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने माॅब लिंचिंग को रोकने के लिये दिशा-निर्देश तय किये हैं लेकिन इनका प्रवर्तन कमज़ोर बना हुआ है।
- सांप्रदायिक भेदभाव और पक्षपात: लिंचिंग की घटनाओं से कमज़ोर समुदाय अधिक प्रभावित होते हैं। इससे सांप्रदायिक विभाजन के साथ व्यवस्थागत भेदभाव एवं पक्षपातपूर्ण कानून प्रवर्तन के बारे में चिंताएँ बढ़ती हैं।
- आँकड़ों की कमी और नीतिगत खामियाँ: NCRB ने वर्ष 2017 के बाद से माॅब लिंचिंग और हेट क्राइम पर अलग-अलग आँकड़े दर्ज करना बंद कर दिया, जिससे इस मुद्दे की सीमा का आकलन करना जटिल हो गया और इस तरह की हिंसा को रोकने के लिये प्रभावी उपाय तैयार करने में चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं।
- सोशल मीडिया और भ्रामक सूचना: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भ्रामक खबरों से हिंसा को बढ़ावा मिलता है, जिससे इनका विनियमन और जवाबदेहिता मुश्किल हो जाती है।
आगे की राह
- राष्ट्रीय कानून: एकरूपता और निवारण के क्रम में कठोर दंड एवं त्वरित सुनवाई के साथ एक समर्पित लिंचिंग विरोधी कानून आवश्यक है।
- मज़बूत कानून प्रवर्तन और न्यायपालिका: माॅब लिंचिंग को रोकने के साथ उसके संबंध में जवाबदेहिता सुनिश्चित करनी चाहिये।
- पीड़ितों के लिये त्वरित सुनवाई एवं न्याय सुनिश्चित करने के क्रम में विशेष जाँच दल (SIT) और फास्ट-ट्रैक न्यायालयों की सुविधा प्रदान करनी चाहिये।
- जन जागरूकता एवं मीडिया: सरकार एवं नागरिक समाज को जागरूकता तथा नैतिक पत्रकारिता के साथ फेक न्यूज़ पर अंकुश लगाकर माॅब लिंचिंग को रोकने में भागीदारी करनी चाहिये।
- प्रौद्योगिकी विनियमन एवं साइबर सुरक्षा: डिजिटल निगरानी को मज़बूत करना, हेट स्पीच पर अंकुश लगाना तथा डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देते हुए सोशल मीडिया को जवाबदेह बनाना आवश्यक है।
- सामुदायिक सहभागिता: सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने तथा अंतर-धार्मिक संवाद को बढ़ावा देने के साथ माॅब लिंचिंग पर अंकुश लगाने के लिये शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना चाहिये।
|
दृष्टि मेन्स प्रश्न: Q. भारत में मॉब लिंचिंग, विधि के शासन तथा सामाजिक सद्भाव के लिये खतरा है। इसके कारणों का विश्लेषण करने के साथ इस मुद्दे को हल करने हेतु विधिक एवं नीतिगत उपाय बताइये। |


कृषि
PMFBY की 9वीं वर्षगाँठ
प्रिलिम्स के लिये:प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), खरीफ, तिलहन फसलें, रबी, बागवानी फसलें, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS), MSP, FPO। मेन्स के लिये:प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की मुख्य विशेषताएँ, PMFBY से संबंधित चुनौतियाँ और आगे की राह। |
स्रोत: पी.आई.बी.
चर्चा में क्यों?
वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की 9वीं वर्षगाँठ है, जिसे अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को होने वाले फसल नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने के लिये वर्ष 2016 में शुरू किया गया था।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMFBY और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंज़ूरी दी है।
PMFBY क्या है?
- परिचय: PMFBY एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण फसल बर्बाद होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
- प्रमुख विशेषताएँ:
- पात्रता: अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदारों और किराएदार किसानों सहित सभी किसान कवरेज के लिये पात्र हैं।
- इसमें किसानों की भागीदारी स्वैच्छिक है और गैर-ऋणी किसानों की PMFBY के तहत कुल कवरेज में 55% हिस्सेदारी है।
- जोखिम कवरेज: PMFBY के तहत विभिन्न जोखिमों के लिये व्यापक कवरेज प्रदान किया गया है।
- प्राकृतिक आपदाएँ: बाढ़, सूखा, चक्रवात, ओलावृष्टि, भूस्खलन और बेमौसम बारिश।
- कीट एवं रोग: कीट संक्रमण और पौधों के रोग।
- कटाई के बाद की हानियाँ: इसके तहत कटाई के 14 दिनों के अंदर होने वाली हानियों को कवर किया गया है, मुख्यतः "कटी हुई" स्थितियों में संग्रहीत फसलों के लिये।
- समय पर बुवाई न होना: यदि प्रतिकूल मौसम के कारण बुवाई रोक दी जाती है तो किसान बीमा राशि के 25% तक क्षतिपूर्ति दावे के लिये पात्र होते हैं।
- वहनीय प्रीमियम: इसके तहत खरीफ फसलों के लिये 2%, रबी फसलों के लिये 1.5% और वार्षिक वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिये 5% की दर से वहनीय प्रीमियम है।
- सरकार पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिये संपूर्ण प्रीमियम का भुगतान करती है।
- प्रौद्योगिकी प्रगति:
- उपग्रह इमेजरी और ड्रोन: इस योजना में प्रौद्योगिकी के माध्यम से फसल क्षेत्र अनुमान, उपज संबंधी विवाद और फसल हानि आकलन किया जाता है।
- फसल कटाई प्रयोग (CCE): CCE-एग्री ऐप फसल उपज के आँकड़ों को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर सीधे अपलोड करने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे नुकसान के आकलन में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
- समय पर मुआवज़ा: PMFBY यह सुनिश्चित करती है कि फसल कटाई के दो माह के भीतर दावों का निपटान हो जाए, जिससे किसानों को कर्ज़ के जाल से बचने के लिये समय पर मुआवज़ा मिल सके।
- पात्रता: अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदारों और किराएदार किसानों सहित सभी किसान कवरेज के लिये पात्र हैं।
- वैश्विक स्तर: PMFBY अब 2023-24 में किसानों की संख्या और कवर किये गए हेक्टेयर भूमि के लिहाज से विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना बन गई है।
PMFBY और RWBCIS
- PMFBY किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों के कारण होने वाले नुकसान हेतु मुआवज़ा देने के लिये वास्तविक फसल नुकसान के आकलन पर निर्भर करती है। इसके विपरीत RWBCIS किसानों को वर्षा, तापमान, आर्द्रता और पवन की गति जैसे पूर्व निर्धारित मौसमी मापदंडों से विचलन के आधार पर मुआवज़ा प्रदान करती है।
- RWBCIS इन मौसमी मापदंडों का उपयोग फसल की उपज़ के लिये प्रॉक्सी के रूप में करती है, ताकि प्रत्यक्ष क्षेत्र-स्तरीय आकलन की आवश्यकता के बगैर, फसल के नुकसान का आकलन किया जा सके और उसकी आपूर्ति की जा सके।
PMFBY के कार्यान्वयन में क्या चुनौतियाँ हैं?
- विलंबित दावा निपटान: दावा निपटान प्रक्रिया धीमी है, इसमें पारदर्शिता का अभाव है, इससे क्षति की गणना और उपज हानि आकलन पर विवाद जारी रहता है।
- भौगोलिक असमानताएँ: गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में फसल बीमा दावों का बहुमत है, इसमें बिहार, असम और पूर्वोत्तर क्षेत्रों जैसे राज्यों की भागीदारी न्यूनतम है।
- प्रीमियम सब्सिडी से संबंधित समस्याएँ: सब्सिडी भुगतान के लिये लंबे इंतजार के कारण दावों का भुगतान 12-18 महीने तक नहीं हो पाता, जिससे योजना की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा है।
- फसल-पश्चात हानि की समस्याएँ: PMFBY केवल भौतिक क्षति की मात्रा को कवर करती है, यह सड़न या रंग उड़ने जैसी गुणात्मक हानि को कवर नहीं करती है।
- फसल कटाई के बाद नुकसान की भरपाई के लिये 14 दिन तक का समय दिया जाता है। यह छोटी सी समय-सीमा नुकसान की गणना और क्षतिपूर्ति को और अधिक कठिन बना देती है।
- आँकड़ों की कमी: खेत की कीमतों और उपज के आकलन पर विश्वसनीय आँकड़ों का अभाव, साथ ही बटाईदार किसानों के गलत भूमि रिकॉर्ड के कारण क्षति की गणना और योजना का कार्यान्वयन जटिल हो जाता है।
- बीमा और आपदा राहत पृथक्करण: एक प्रमुख मुद्दा बीमा को आपदा राहत से अलग करना है, क्योंकि बीमा वाणिज्यिक जोखिमों का प्रबंधन करता है, जबकि आपदा राहत एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है।
- यह विशेष रूप से MSP व्यवस्था के बाहर बागवानी उत्पादों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों के लिये चुनौतीपूर्ण है।
आगे की राह:
- किये गये दावे में सुधार: सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि बीमाकर्त्ता अपनी ज़िम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभा रहे हैं और केवल पुनर्बीमा कमीशन प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों का उपयोग नहीं कर रहे हैं।
- दावों का निष्पक्ष एवं समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिये एक निगरानी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिये।
- छोटे और सीमांत किसानों को संबोधित करना: समुदाय-आधारित बीमा मॉडल और FPO को प्रोत्साहित करने से छोटे और सीमांत किसानों को कवर किया जा सकता है, लेनदेन लागत कम हो सकती है, तथा विवादों को हल करने के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान किया जा सकता है।
- पहुँच को सुनिश्चित करना: निजी क्षेत्र, बैंक और बीमा कंपनियां एजेंटों और व्यापार संवाददाताओं (BC) का उपयोग करके पीएमएफबीवाई के बारे में जानकारी प्रसारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
- नए जोखिम शामिल करना: बीमा योजनाओं को व्यापक बनाने की आवश्यकता है ताकि जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान जैसे जोखिम भी शामिल किये जा सकें। किसान उन क्षेत्रों में दालों जैसी फसलों की खेती करने से बचते हैं जहाँ हाथी और नीलगाय खतरा उत्पन्न करते हैं।
|
दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये तथा योजना की कवरेज एवं दक्षता में सुधार के उपाय सुझाइये। |
UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न: 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016)
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) |