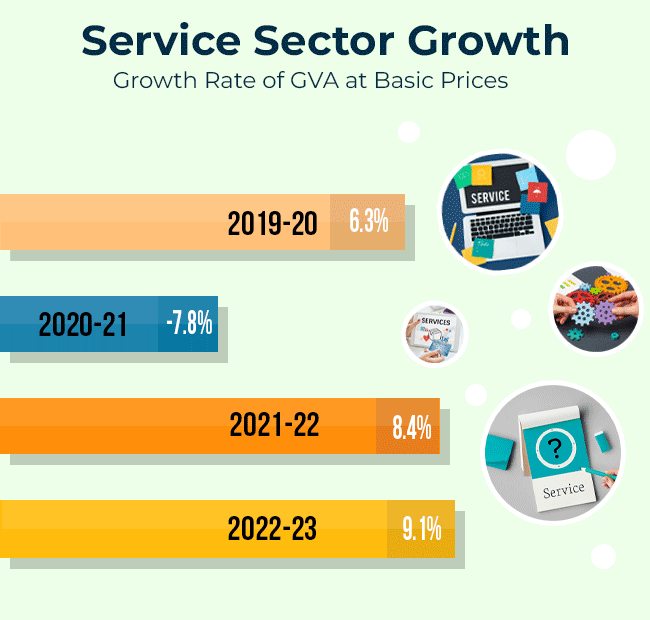भारतीय अर्थव्यवस्था
भारत की सर्विस सेक्टर अर्थव्यवस्था का भविष्य
- 05 Apr 2025
- 25 min read
यह एडिटोरियल 28/03/2025 को द हिंदू में प्रकाशित “Riding the new wave in services, industry” पर आधारित है। यह लेख भारत के सर्विस सेक्टर में वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) की परिवर्तनकारी भूमिका को सामने लाया गया है, उनके 65 बिलियन डॉलर के राजस्व एवं 1.9 मिलियन कर्मचारियों पर प्रकाश डाला गया है, जबकि क्षेत्रीय संकेंद्रण, राजकोषीय स्थिरता एवं AI के प्रभाव को संतुलित करने की आवश्यकता पर बल देता है।
प्रिलिम्स के लिये:सर्विस सेक्टर, नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क, AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बजट 2025-26, साइबर सुरक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020, दूरसंचार, कौशल भारत, BharatNet, डिजिटल इंडिया, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स मेन्स के लिये:भारत के सर्विस सेक्टर के प्रमुख विकास चालक, भारत के सर्विस सेक्टर से जुड़े प्रमुख मुद्दे। |
भारत वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) के साथ एक रणनीतिक दिशा में है जो अपने सर्विस सेक्टर परिदृश्य को बदल रहा है। लगभग 1,700 GCC में 1.9 मिलियन भारतीय कार्यरत हैं और 65 बिलियन डॉलर का राजस्व उत्पन्न करते हैं, विश्व भर के सभी GCC में लगभग आधी हिस्सेदारी भारत की है। यद्यपि विनिर्माण क्षेत्र तेज़ी से विशेष वैश्विक नेटवर्क पर निर्भर हो रहे हैं, सर्विस सेक्टर इन पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थाओं के माध्यम से परिचालन को सुदृढ़ कर रहे हैं। भारत का तकनीकी प्रतिभा पूल महत्त्वपूर्ण प्रतिस्पर्द्धी लाभ प्रदान करता है, हालाँकि नीति निर्माताओं को इस अवसर को अधिकतम करने के लिये क्षेत्रीय एकाग्रता, राजकोषीय स्थिरता और AI के प्रभाव को संतुलित करने की आवश्यकता है।
भारत के सर्विस सेक्टर के विकास के प्रमुख कारक क्या हैं?
- वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) और उच्च स्तरीय आउटसोर्सिंग का उदय: भारत वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) के लिये शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है, जो परिचालन नियंत्रण और लागत दक्षता चाहने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित कर रहा है।
- महामारी के बाद तृतीय पक्ष की आउटसोर्सिंग से लेकर इन-हाउस GCC की ओर बदलाव में तेज़ी आई है, जो डेटा सुरक्षा, एनालिटिक्स और IP-संवेदनशील सेवाओं की मांग से प्रेरित है।
- बंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर वित्तीय, तकनीकी एव्न्न स्वास्थ्य देखभाल GCC के लिये वैश्विक केंद्र बन गए हैं।
- वर्ष 2025 तक, भारत में 1,700 GCC होंगे, जो 1.9 मिलियन लोगों को रोज़गार देंगे तथा 65 बिलियन डॉलर के राजस्व का योगदान देंगे (इंडस वैली रिपोर्ट, 2025)।
- डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और AI-संचालित नवाचार का विस्तार: AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर केंद्र सरकार के प्रभावी प्रयासों ने भारत के डिजिटल सेवा परिदृश्य को अत्यधिक सक्रिय कर दिया है।
- फिनटेक से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक, सभी क्षेत्रों को AI-आधारित स्वचालन और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से नया रूप दिया जा रहा है।
- नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क और AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नवाचार क्षमता को बढ़ा रहे हैं।
- सरकार ने AI उत्कृष्टता केंद्रों के लिये 5 बिलियन रुपए देने की प्रतिबद्धता जताई है (केंद्रीय बजट 2024-25)।
- बढ़ता प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और नीति उदारीकरण: उदार FDI मानदंड, बढ़ता निवेशक विश्वास और संरचनात्मक नीति परिवर्तनों ने भारत को बीमा, दूरसंचार एवं वित्तीय सेवाओं जैसी सेवाओं में पूंजी के लिये एक आकर्षण का केंद्र बना दिया है।
- FDI सीमा बढ़ाने और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं ने वैश्विक भागीदारों के लिये प्रवेश आसान बना दिया है, जबकि नियामक सैंडबॉक्स फिनटेक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।
- अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान भारत के कुल 40.67 बिलियन डॉलर के FDI प्रवाह (DPIIT) में से सेवाओं को 7.22 बिलियन डॉलर का FDI प्राप्त हुआ।
- केंद्रीय बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई।
- उच्च मूल्य सेवा निर्यात में मज़बूत प्रदर्शन: भारत अब IT, परामर्श और वित्तीय सेवाओं में मज़बूती के साथ 7वाँ सबसे बड़ा वैश्विक सेवा निर्यातक है।
- विश्व भर में डिजिटल परिवर्तन की बढ़ती मांग ने भारतीय फर्मों को क्लाउड, साइबर सुरक्षा और उद्यम समाधान जैसे क्षेत्रों में विस्तार करने में मदद की है। भारत का विविध सेवा निर्यात आधार इसे क्षेत्र-विशिष्ट झटकों के प्रति समुत्थानशील बनाता है।
- वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी दोगुनी से अधिक होकर वर्ष 2023 में लगभग 4.3% तक पहुँच गई।
- दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और मनोरंजक सेवाओं के निर्यात में छठे स्थान पर है तथा अन्य व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में आठवें स्थान पर है।
- सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास और STEM शिक्षा को बढ़ावा: सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास प्रयासों को सर्विस सेक्टर की आवश्यकताओं के साथ जोड़ा है। स्किल इंडिया, PMKVY और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 जैसी योजनाएँ भविष्य के लिये तैयार प्रतिभाओं को बढ़ावा देती हैं।
- GCC के माध्यम से कौशल के साथ निजी क्षेत्र का एकीकरण कार्यबल की रोज़गार क्षमता को बढ़ाता है।
- भारत प्रतिवर्ष 1.5 मिलियन से अधिक इंजीनियर तैयार करता है, जो IT और फिनटेक प्रतिभा का एक प्रमुख स्रोत है।
- टियर 2 और टियर 3 शहरों में विस्तार: महानगरों में उच्च संतृप्ति के साथ, कंपनियाँ लागत लाभ और नए बाज़ार तक अभिगम के लिये बाह्य इलाकों, छोटे शहरों में विस्तार कर रही हैं।
- BharatNet और डिजिटल इंडिया जैसी सरकारी परियोजनाओं ने बैकएंड परिचालन एवं डिजिटल सेवाओं को वंचित क्षेत्रों में पहुँचाने में सक्षम बनाया है।
- इससे समावेशी विकास को भी बढ़ावा मिलता है और महानगरों पर प्रवास का दबाव कम होता है।
- उदाहरण के लिये, भारत का लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग क्षेत्र तेज़ी से विस्तार कर रहा है तथा देश में टियर 2 और 3 शहर प्रमुख केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं।
- BharatNet और डिजिटल इंडिया जैसी सरकारी परियोजनाओं ने बैकएंड परिचालन एवं डिजिटल सेवाओं को वंचित क्षेत्रों में पहुँचाने में सक्षम बनाया है।
- ग्रामीण भारत में घरेलू मांग में वृद्धि: बढ़ती आय, शहरीकरण और आकांक्षाओं ने स्वास्थ्य और शिक्षा से लेकर मनोरंजन एवं वित्तीय सेवाओं तक के लिये घरेलू बाज़ार का विस्तार किया है।
- यहाँ तक कि ग्रामीण भारत में भी सेवाओं की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो स्पष्ट संरचनात्मक बदलाव को दर्शाता है। घरेलू मांग में इस वृद्धि ने सेवाओं के मामले में भारत को निर्यात पर कम निर्भर बना दिया है।
- मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में शहरी-ग्रामीण अंतर सत्र 2011-12 में 84% से घटकर 2022-23 में 71% हो गया है, जो मुख्य रूप से सेवाओं पर खर्च में वृद्धि के कारण है।
- मनोरंजन, स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल शिक्षा जैसे क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में भारी वृद्धि देखी जा रही है।
भारत के सर्विस सेक्टर से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?
- कौशल और कार्यबल तत्परता अंतराल: भारत के सर्विस सेक्टर में AI, डेटा विज्ञान, फिनटेक और साइबर सुरक्षा में उच्च-स्तरीय कौशल की मांग बढ़ रही है लेकिन कार्यबल की आपूर्ति असमान बनी हुई है।
- यद्यपि हमारे यहाँ बड़ी संख्या में स्नातक हैं फिर भी उद्योग-अकादमिक संरेखण अभी भी कमज़ोर है जिसके कारण अल्परोज़गार की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
- विशिष्ट विशेषज्ञता की बढ़ती आवश्यकता (विशेष रूप से टियर 2/3 शहरों में) वर्तमान कौशल प्रयासों से कहीं अधिक है।
- उदाहरण के लिये, भारत में रोज़गार का संकट गहराता जा रहा है क्योंकि केवल 42.6% स्नातक ही रोज़गार के योग्य हैं, जिससे बढ़ते कौशल अंतराल पर चिंता बढ़ रही है।
- सेवा केंद्रों में शहरी बुनियादी अवसंरचना की बाधाएँ: प्रमुख सर्विस सेक्टर वाले शहरों में बुनियादी अवसंरचना की गंभीर समस्या (यातायात की भीड़ से लेकर जल की कमी और अचल संपत्ति की बढ़ती लागत तक) है।
- ये अक्षमताएँ व्यावसायिक लागतों को बढ़ाती हैं, उत्पादकता को कम करती हैं और कुशल श्रमिकों के लिये जीवन की गुणवत्ता को कम करती हैं। कुछ शहरी समूहों पर अत्यधिक निर्भरता दीर्घकालिक सर्विस सेक्टर के विकास के लिये धारणीय नहीं है।
- उदाहरण के लिये, बेंगलुरू (जो भारत में कार्यालय स्थल की मांग में शीर्ष पर है) शहरी बाढ़ के साथ जल और बिजली की कमी जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है।
- सेवा विकास में क्षेत्रीय असंतुलन: उच्च मूल्य सर्विस सेक्टर की अधिकांश गतिविधियाँ महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे कुछ समृद्ध राज्यों में केंद्रित हैं।
- बड़े श्रम स्रोत वाले राज्य- जैसे बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा अपर्याप्त कनेक्टिविटी, शिक्षा अंतराल और निवेश पारिस्थितिकी तंत्र की कमी के कारण सेवाओं के मामले में अविकसित बने हुए हैं।
- इससे स्थानिक असमानता बढ़ती है और राष्ट्रीय रोज़गार सृजन की संभावना सीमित होती है।
- वित्त वर्ष 2023 में कर्नाटक और महाराष्ट्र ने मिलकर भारत के कुल सर्विस सेक्टर के सकल राज्य मूल्यवर्द्धन में 25% से अधिक का योगदान दिया, जबकि 19 राज्यों का सामूहिक रूप से इस क्षेत्र में केवल 25% योगदान था।
- बड़े श्रम स्रोत वाले राज्य- जैसे बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा अपर्याप्त कनेक्टिविटी, शिक्षा अंतराल और निवेश पारिस्थितिकी तंत्र की कमी के कारण सेवाओं के मामले में अविकसित बने हुए हैं।
- उच्च निर्यात निर्भरता और भू-राजनीतिक जोखिम: भारत का सेवा निर्यात अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे बाज़ारों पर बहुत अधिक निर्भर है, जिससे यह क्षेत्र वैश्विक असंतुलन, संरक्षणवाद और वीजा प्रतिबंधों के प्रति संवेदनशील हो जाता है।
- आउटसोर्सिंग के रुझानों में बदलाव, मंदी के चक्र या व्यापार तनाव (जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हाल ही में टैरिफ मुद्दे) राजस्व, रोज़गार और निवेशक विश्वास को प्रभावित करते हैं।
- उदाहरण के लिये, भारत का लगभग 70% आईटी सेवा निर्यात अमेरिका को होता है, जो कि काफी निर्भरता को दर्शाता है।
- इसके अलावा, अमेरिकी प्रौद्योगिकी क्षेत्र इस समय बड़े पैमाने पर छंटनी से ग्रस्त है, जिसका भारतीय श्रमिकों पर काफी प्रभाव पड़ रहा है।
- MSME में उभरती प्रौद्योगिकियों का कम उपयोग: बड़ी सेवा कंपनियाँ तेज़ी से AI, स्वचालन और क्लाउड प्लेटफॉर्म को अपना रही हैं लेकिन MSME लागत बाधाओं, जागरूकता की कमी और सीमित डिजिटल बुनियादी अवसंरचनाके कारण इसमें पीछे हैं।
- इससे उत्पादकता का अंतर और गहरा होता है। समावेशी विकास के लिये छोटी फर्मों में तकनीक को अपनाना ज़रूरी है।
- ‘SME डिजिटल इनसाइट्स' अध्ययन के अनुसार, केवल 50% भारतीय MSME वित्त वर्ष 2024 में व्यवसाय विस्तार के लिये क्लाउड अपनाने को प्राथमिकता दे रहे हैं।
- इसके अलावा, केवल 6% MSME ही बिक्री के लिये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का सक्रिय रूप से लाभ उठाते हैं, जो इस क्षेत्र में डिजिटलीकरण की सीमितता को रेखांकित करता है।
- अवसंरचना विकास में खंडित सार्वजनिक-निजी सहयोग: सार्वजनिक अवसंरचना विस्तार (डिजिटल और भौतिक) की गति प्रायः निजी सर्विस सेक्टर की ज़रूरतों से कम बनी हुई है।
- कुछ साझेदारियों के बाद भी इसमें समन्वय अस्थायी बना हुआ है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और रसद सेवाओं में विकास सीमित होता है।
- उदाहरण के लिये, मुंबई तटीय सड़क परियोजना, जिसका उद्देश्य यातायात की भीड़ को कम करना और तटीय पहुँच में सुधार करना है, में भूमि अधिग्रहण के मुद्दों और नियामक बाधाओं के कारण बिलंब हो रहा है।
भारत अपने सर्विस सेक्टर को बढ़ाने के लिये क्या उपाय अपना सकता है?
- टियर-2 और टियर-3 सेवा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना: भारत को टियर-2 और टियर-3 शहरों में बुनियादी ढाँचे, कौशल समूहों और डिजिटल कनेक्टिविटी विकसित करके मेट्रो शहरों से परे अपने सर्विस सेक्टर के विकास को विकेंद्रीकृत करना चाहिये।
- इसके लिये स्मार्ट सिटी पहल, भारतनेट और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के बीच समन्वय की आवश्यकता है, ताकि GCC और उच्च कौशल सेवाओं के लिये अनुकूल परिस्थितियाँ बनाई जा सकें।
- रणनीतिक प्रोत्साहनों से इन क्षेत्रों में शिक्षा-तकनीक, स्वास्थ्य-तकनीक और परामर्श सेवाओं में निज़ी निवेश को आकर्षित किया जाना चाहिये।
- सार्वजनिक-निज़ी कौशल भागीदारी को सुदृढ़ करना: NEP- 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा को स्किल इंडिया के मॉड्यूलर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के लिये एक राष्ट्रीय कार्यात्मक ढाँचा सर्विस सेक्टर के कौशल अंतर को समाप्त कर सकता है। पाठ्यक्रम का डिज़ाइन और वितरण उद्योग की भागीदारी प्रशिक्षण को मांग-संचालित, भविष्य के लिये तैयार और रोज़गारयुक्त बना सकती है।
- सर्विस सेक्टर की उभरती मांगों को पूरा करने के लिये AI, फिनटेक, डिजिटल डिज़ाइन, कानूनी तकनीक और स्वास्थ्य तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
- विनियामक सैंडबॉक्स और एकीकृत अनुपालन प्लेटफॉर्म: फिनटेक, एड-टेक, गिग इकॉनमी और टेलीमेडिसिन में सेवा-उन्मुख स्टार्ट-अप को बिना किसी बाधा के बढ़ने के लिये एक सामान्य विनियामक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- भारत को प्रमुख सेवाओं (SEBI, RBI, IRDAI, आदि) में विनियामक सैंडबॉक्स को संस्थागत बनाना चाहिये और अंतर-राज्यीय नीति विखंडन को समाप्त करने, नवाचार और परिचालन मापनीयता को प्रोत्साहित करने के लिये एक अखिल भारतीय एकल-खिड़की अनुपालन पोर्टल विकसित करना चाहिये।
- रणनीतिक बाज़ार पहुँच के साथ सेवा निर्यात विविधीकरण को बढ़ावा देना: पारंपरिक निर्यात गंतव्यों पर निर्भरता को कम करने के लिये, भारत को IT, वित्तीय और शिक्षा सेवाओं के लिये अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया में उभरते बाज़ारों को सक्रिय रूप से लक्षित करना चाहिये।
- चैंपियन सर्विस सेक्टर योजना को भारत के FTA और व्यापार कूटनीतिक रणनीति के साथ जोड़ने से डिजिटल व्यापार विस्तार और सीमा पार सेवा वितरण के लिये अनुरूप समर्थन मिल सकता है।
- क्षेत्रीय परिवर्तन के लिये AI और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर: भारत को खुदरा, रसद, स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय सेवाओं में उत्पादकता बढ़ाने के लिये AI उत्कृष्टता केंद्र, ONDC (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स) और डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को एकीकृत करना चाहिये।
- इन प्लेटफार्मों को वास्तविक समय डेटा-साझाकरण कार्यात्मक ढाँचे और मज़बूत साइबर सुरक्षा प्रणालियों के साथ राज्यों में विस्तारित किया जाना चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लघु स्तरीय पैमाने और पहुँच के लिये DPI का लाभ उठा सकें।
- उच्च मूल्य सेवा शृंखलाओं में MSME का एकीकरण: क्लाउड प्लेटफॉर्म, स्वचालन उपकरण और साइबर सुरक्षा अवसंरचना तक विशेष प्रोत्साहन और रियायती पहुँच MSME को वैश्विक एवं घरेलू मूल्य शृंखलाओं में डिजिटल रूप से शामिल करने में मदद कर सकती है।
- डिजिटल MSME योजना को डिजिटल इंडिया सीड सपोर्ट और क्लस्टर-आधारित इनक्यूबेशन के साथ एकीकृत करने से सर्विस सेक्टर के भीतर डिजिटल डिवाइड को कम किया जा सकता है और छोटे अभिकर्त्ताओं के बीच लचीलापन उत्पन्न किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय सेवा प्रतिस्पर्द्धात्मकता परिषद का संस्थागतकरण: एक समर्पित अंतर-मंत्रालयी निकाय भारत के सर्विस सेक्टर के लिये थिंक-टैंक और निगरानी एजेंसी के रूप में कार्य कर सकता है, जो डेटा-संचालित नीतिगत जवाबदेही, नियामक समन्वय और रणनीतिक हस्तक्षेप सुनिश्चित कर सकता है।
- इस परिषद में निज़ी क्षेत्र, शिक्षा जगत और राज्यों के हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिये ताकि प्रवृत्तियों पर नज़र रखी जा सके, व्यवधानों का समाधान किया जा सके और नीतिगत लक्ष्यों को वास्तविक समय की क्षेत्रीय गतिशीलता के साथ संरेखित किया जा सके।
निष्कर्ष:
भारत का सर्विस सेक्टर एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है, जो वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) के तेज़ी से बढ़ने, डिजिटल बुनियादी अवसंरचना के विस्तार और बढ़ते विदेशी निवेश से प्रेरित है। नीति निर्माताओं को सेवा केंद्रों का विकेंद्रीकरण करके, कौशल पहलों को बढ़ाकर और MSME डिजिटल अपनाने को बढ़ावा देकर समावेशी विकास को बढ़ावा देना चाहिये। AI, विनियामक सुधारों और विविध निर्यात का लाभ उठाने वाली एक दूरदर्शी रणनीति की सेवाओं में निरंतर विकास और वैश्विक नेतृत्व सुनिश्चित करेगी।
|
दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न. भारत के सर्विस सेक्टर के प्रमुख विकास चालकों पर चर्चा कीजिये तथा वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बनाए रखने के लिये जिन चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिये, उनका विश्लेषण कीजिये। |
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. एस. एंड पी. 500 किससे संबंधित है? (2008) (a) सुपर कंप्यूटर उत्तर: (d) प्रश्न: 'आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक' में निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक योगदान किसका है? (2015) (a) कोयला उत्पादन उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न 1. "सुधारोत्तर अवधि में सकल-घरेलू-उत्पाद (जी.डी.पी.) की समग्र संवृद्धि में औद्योगिक संवृद्धि दर पिछड़ती गई है।" कारण बताइये। औद्योगिक-नीति में हाल में किये गए परिवर्तन औद्योगिक संवृद्धि दर को बढ़ाने में कहाँ तक सक्षम हैं? (2017) प्रश्न 2. सामान्यतः देश कृषि से उद्योग और बाद में सेवाओं को अंतरित होते हैं पर भारत सीधे ही कृषि से सेवाओं को अंतरित हो गया है। देश में उद्योग के मुकाबले सेवाओं की विशाल संवृद्धि के क्या कारण हैं? क्या भारत सशक्त औद्योगिक आधार के बिना एक विकसित देश बन सकता है? (2014) |