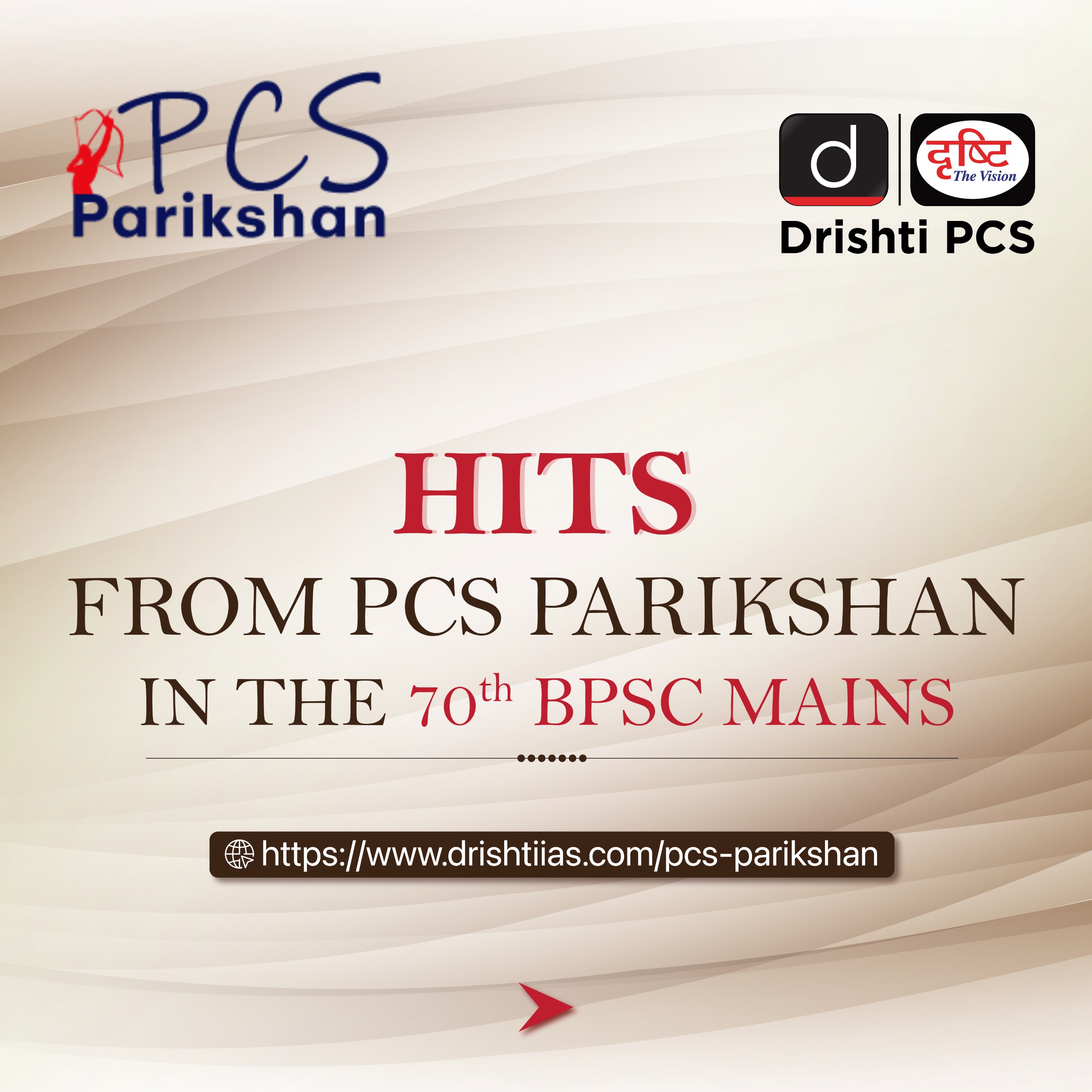जैव विविधता और पर्यावरण
इस्पात क्षेत्र का डीकार्बोनाइज़ेशन
यह एडिटोरियल 15/05/2023 को ‘हिंदू बिजनेस लाइन’ में प्रकाशित “Decarbonising the steel sector will pay off” लेख पर आधारित है। इसमें इस्पात क्षेत्र से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और इस्पात क्षेत्र को डीकार्बोनाइज़ करने के महत्त्व के साथ-साथ संबंधित चुनौतियों एवं प्रयासों के बारे में चर्चा की गई है।
प्रिलिम्स के लिये:भारत का इस्पात उद्योग, GHGs उत्सर्जन, राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017, यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM), हरित हाइड्रोजन मेन्स के लिये:भारत का इस्पात उद्योग और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, भारत के इस्पात क्षेत्र को डीकार्बोनाइज़ करने का महत्त्व, राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017, हरित हाइड्रोजन और इस्पात उत्पादन |
इस्पात (Steel) आधुनिक युग के प्रमुख स्तंभों में से एक है और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण इंजीनियरिंग एवं निर्माण सामग्रियों में शामिल है। लेकिन इस्पात उद्योग कार्बन डाइऑक्साइड के तीन सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। परिणामस्वरूप, विश्व भर के इस्पात क्षेत्र के खिलाड़ी पर्यावरणीय एवं आर्थिक, दोनों दृष्टिकोणों से अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिये लगातार एक डीकार्बोनाइज़ेशन चुनौती का सामना कर रहे हैं।
भारत वर्तमान में चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है। विभिन्न विश्लेषण वर्ष 2050 तक इस्पात की खपत में कई गुना वृद्धि होने की संभावना दिखाते हैं। बढ़ती घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग की पूर्ति के लिये भारत में इस्पात के उत्पादन में अगले कुछ दशकों में व्यापक वृद्धि होगी।
निम्न-कार्बन उत्सर्जन वाले भारत में देश के हरित भविष्य के लिये एक आवश्यक घटक के रूप में इस्पात क्षेत्र के डीकार्बोनाइज़ेशन की बड़ी भूमिका होगी।
भारत के इस्पात क्षेत्र का वर्तमान परिदृश्य
- उत्पादन परिदृश्य:
- इस्पात भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये एक प्रमुख क्षेत्र है (वित्त वर्ष 21-22 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 2% का योगदान)।
- भारत विश्व में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और तैयार इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
- राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 (National Steel Policy 2017) ने 120 मिलियन टन (MT) के वर्तमान वार्षिक उत्पादन स्तर से 2030 तक 300 मिलियन टन तक पहुँचने का लक्ष्य निर्धारिवर्षत किया था।
- अर्थव्यवस्था की वृद्धि के साथ भारत का कच्चा इस्पात उत्पादन वर्ष 2050 तक 435 मिलियन टन तक पहुँच सकता है।
- उत्सर्जन परिदृश्य: लौह एवं इस्पात उत्पादन से प्रत्यक्ष उत्सर्जन (खरीदी गई बिजली के उपयोग से होने वाले उत्सर्जन को छोड़कर) वर्ष 2018 में लगभग 270 मिलियन टन CO2 समतुल्य (MTCO2e) था, जिसमें कुल राष्ट्रीय ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 9% शामिल था।
- इस्पात प्रत्यक्ष औद्योगिक CO2 उत्सर्जन में लगभग एक-तिहाई भाग या भारत के कुल ऊर्जा अवसंरचना CO2 उत्सर्जन के 10% और देश के कुल उत्सर्जन के लगभग 11% का योगदान देता है।
इस्पात क्षेत्र के डीकार्बोनाइज़िंग का महत्त्व
- त्वरित संक्रमण में, अकेले कोकिंग कोयले पर कम खर्च से ही वर्ष 2050 तक लगभग 500 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बचत प्राप्त होगी।
- एक हरित इस्पात उद्योग भारत को एक वैश्विक हरित इस्पात निर्माण केंद्र बनने में सक्षम बना सकता है।
- इस्पात निर्माण के डीकार्बोनाइज़ेशन से कार, अवसंरचना और इमारतों जैसे संबद्ध उद्योगों का भी डीकार्बोनाइज़ेशन होगा।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरते नियामक परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य से भी इस्पात क्षेत्र को डीकार्बोनाइज़ करना महत्त्वपूर्ण है; यूरोपीय संघ (EU) के आगामी ‘कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म’ (CBAM) के कारण यूरोपीय संघ के लिये भारतीय इस्पात निर्यात, इस्पात क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज़ करने के किसी अतिरिक्त प्रयास के बिना ही, 58% तक गिर सकता है।
भारत के इस्पात क्षेत्र को डीकार्बोनाइज़ करने के लिये प्रमुख पहलें
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission) भारत के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिये इस्पात क्षेत्र को डीकार्बोनाइज़ करने में हरित हाइड्रोजन के लिये एक महत्त्वपूर्ण भूमिका को चिह्नित करता है।
- इस्पात मंत्रालय हरित इस्पात/’ग्रीन स्टील’ (जीवाश्म ईंधन का उपयोग किये बिना इस्पात विनिर्माण) को बढ़ावा देने के माध्यम से इस्पात उद्योग में CO2 को कम करने की मंशा रखता है।
- ऐसा कोयला-संचालित संयंत्रों के पारंपरिक कार्बन-गहन निर्माण मार्ग के बजाय हाइड्रोजन, कोयला गैसीकरण या बिजली जैसे निम्न-कार्बन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके किया जा सकता है।
- स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, 2019 (Steel Scrap Recycling Policy 2019) इस्पात निर्माण में कोयले की खपत को कम करने के लिये घरेलू स्तर पर उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाती है।
- ‘क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल’ (Clean Energy Ministerial) के बैनर तले ‘इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बोनाइज़ेशन इनिशिएटिव’ (Industrial Deep Decarbonisation Initiative) का सह-नेतृत्व करने के लिये भारत भी यू.के. से जुड़ा है। इससे इस्पात सहित विभिन्न निम्न-कार्बन औद्योगिक सामग्री की वैश्विक मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- जनवरी 2010 में MNRE द्वारा लॉन्च किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन (National Solar Mission- NSA) सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है और इस्पात उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करता है।
- हाल ही में सरकार ने कल्याणी ग्रुप के पहले ग्रीन स्टील ब्राण्ड ‘कल्याणी फेरेस्टा’ (Kalyani FeRRESTA) को लॉन्च किया।
इस्पात क्षेत्र को डीकार्बोनाइज़ करने की राह में चुनौतियाँ
- पारंपरिक तरीकों को हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित करने की चुनौतियाँ:
- इस्पात उत्पादन के दो बुनियादी मार्ग हैं: ब्लास्ट फर्नेस (BF) मार्ग, जहाँ कोक प्राथमिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (DRI) मार्ग, जहाँ ईंधन के रूप में कोयला या प्राकृतिक गैस प्रयुक्त होता है।
- भारत वर्तमान में BF और कोयला-आधारित DRI मार्गों के माध्यम से अपने लगभग 90% कच्चे इस्पात का उत्पादन करता है। जबकि हाइड्रोजन में DRI प्रक्रिया में प्रयुक्त कोयले या गैस को पूर्णतः प्रतिस्थापित करने की क्षमता है, BF मार्ग में कोक को प्रतिस्थापित कर सकने में इसकी सीमित भूमिका ही देखी जाती है।
- हाइड्रोजन आधारित इस्पात-निर्माण 1 डॉलर प्रति किग्रा से ऊपर हाइड्रोजन की कीमतों के लिये अप्रतिस्पर्द्धी बना हुआ है, विशेष रूप से उत्सर्जन के लिये कार्बन लागत के अभाव में।
- इस्पात उत्पादन के दो बुनियादी मार्ग हैं: ब्लास्ट फर्नेस (BF) मार्ग, जहाँ कोक प्राथमिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (DRI) मार्ग, जहाँ ईंधन के रूप में कोयला या प्राकृतिक गैस प्रयुक्त होता है।
- नेट-ज़ीरो प्रौद्योगिकियों को उन्नत करने में निहित चुनौतियाँ:
- लागत: वैश्विक अनुमान बताते हैं कि अपस्ट्रीम ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के साथ DRI इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिये निवेश 3.2 लाख रुपए प्रति टन तक पहुँच सकता है।
- इसके अतिरिक्त, ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत 300-400 रुपए प्रति किलोग्राम है जो ‘ग्रे हाइड्रोजन’ की कीमत (160-220 रुपए प्रति किलोग्राम) की तुलना में अधिक है।
- इसी प्रकार, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज (CCS) संयंत्र भी उच्च पूंजीगत लागत रखते हैं।
- सहायक अवसंरचना: हाइड्रोजन के भंडारण, उत्पादन और परिवहन के लिये सहायक नेटवर्क अपर्याप्त है।
- CCS के लिये, संभावित भूवैज्ञानिक भंडारण स्थलों की उपलब्धता और उनकी क्षमताओं के संबंध में डेटा की कमी है।
- CCS प्रौद्योगिकी को उन्नत करने में सीमित उपयोग के मामले भी एक चुनौती पेश करते हैं।
- लागत: वैश्विक अनुमान बताते हैं कि अपस्ट्रीम ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के साथ DRI इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिये निवेश 3.2 लाख रुपए प्रति टन तक पहुँच सकता है।
इस्पात क्षेत्र को डीकार्बोनाइज़ करने के लिये कौन-से कदम उठाए जा सकते हैं?
- CO2 मूल्य निर्धारण शुरू करना और हाइड्रोजन का तेज़ी से विकास करना:
- अगले कुछ वर्षों में CO2 मूल्य निर्धारण का आरंभ एवं अंशांकन निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों में निवेश को प्रोत्साहित करेगा और हाइड्रोजन-आधारित इस्पात निर्माण के अंगीकरण में तेज़ी लाएगा।
- यह इस्पात मूल्य शृंखला में अन्य हरित प्रौद्योगिकियों, जैसे कि हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली में निवेश को भी गति प्रदान करेगा।
- 50 डॉलर प्रति टन उत्सर्जन का कार्बन मूल्य वर्ष 2030 तक ग्रीन स्टील को प्रतिस्पर्द्धात्मक बना सकता है (यहाँ तक कि 2 डॉलर प्रति किलोग्राम के हाइड्रोजन मूल्य पर भी) और कोयला-आधारित से हाइड्रोजन-आधारित इस्पात निर्माण की ओर संक्रमण को उत्प्रेरित कर सकता है।
- अगले कुछ वर्षों में CO2 मूल्य निर्धारण का आरंभ एवं अंशांकन निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों में निवेश को प्रोत्साहित करेगा और हाइड्रोजन-आधारित इस्पात निर्माण के अंगीकरण में तेज़ी लाएगा।
- सामग्री दक्षता के लिये नीतियाँ:
- सभी मौजूदा वाणिज्यिक इस्पात निर्माण तकनीकों में से स्क्रैप-आधारित इस्पात निर्माण में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन होता है, लेकिन यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य होने और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिये गुणवत्तापूर्ण स्क्रैप के मूल्य एवं उपलब्धता पर निर्भर करता है।
- भारत स्क्रैप आयात पर निर्भर है, जो भविष्य में एक चुनौती बन जाएगा क्योंकि इस्पात निर्माण के लिये वैश्विक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण स्क्रैप की मांग बढ़ जाएगी।
- घरेलू स्क्रैप-आधारित इस्पात निर्माण को बढ़ाने के लिये स्क्रैप संग्रहण एवं पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को लागू करने की आवश्यकता होगी, ताकि निराकरण, संग्रहण एवं प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किये जा सकें।
- सभी मौजूदा वाणिज्यिक इस्पात निर्माण तकनीकों में से स्क्रैप-आधारित इस्पात निर्माण में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन होता है, लेकिन यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य होने और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिये गुणवत्तापूर्ण स्क्रैप के मूल्य एवं उपलब्धता पर निर्भर करता है।
- अंतिम-उपयोग (End-Use) में हरित इस्पात की खपत को प्रोत्साहित करना:
- सरकार हरित इस्पात के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। सार्वजनिक एवं निजी निर्माण और ऑटोमोटिव उपयोगों में सन्निहित कार्बन के लिये लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिये।
- यह घरेलू इस्पात निर्माताओं के लिये एक घरेलू हरित इस्पात बाज़ार के निर्माण का समर्थन करेगा, जो आरंभ में उन निर्यात बाज़ारों का दोहन कर सकते हैं जहाँ हरित इस्पात प्रीमियम स्थिति रखता है।
- CBAM जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियम निजी क्षेत्र को हरित इस्पात की ओर तेज़ी से आगे बढ़ने के लिये प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- ‘कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज’ (CCUS) में निवेश:
- CCUS वर्तमान में उत्सर्जन को कम करने के लिये एक महँगा लेकिन महत्त्वपूर्ण साधन है।
- इसे इस्पात उद्योग के लिये एक व्यवहार्य डीकार्बोनाइज़ेशन समाधान बनाने के लिये ओडिशा एवं झारखंड जैसे इस्पात उत्पादक केंद्रों में ‘हब’ के निर्माण के अलावा कैप्चर लागत को कम करने के लिये वृहत अनुसंधान एवं विकास प्रयासों की आवश्यकता है।
अभ्यास प्रश्न: ‘‘चूँकि वर्ष 2050 के लिये परिकल्पित भारत के अधिकांश का निर्माण होना अभी शेष है, ‘इस्पात उद्योग का त्वरित डीकार्बोनाइज़ेशन’ भारत के लिये आरंभ में ही इसका निर्माण कर लेने का एक स्पष्ट अवसर प्रदान करता है।’’ टिप्पणी करें।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न:प्रिलिम्स:1. ‘आठ मूल उद्योगों के सूचकांक (इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज)’ में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है? (a) कोयला उत्पादन उत्तर: b 2. भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? (a) शोरा उत्तर: (d) 3. निम्नलिखित में से कौन-से कुछ महत्त्वपूर्ण प्रदूषक हैं, भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किये जाते हैं? (2014)
नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 3 और 4 उत्तर: (d) 4. इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिये सामग्री हो सकता है?
नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये : (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. वर्तमान में लौह एवं इस्पात उद्योगों की कच्चे माल के स्रोत से दूर स्थिति का उदाहरणों सहित कारण बताइये। (2020) प्रश्न. विश्व में लौह एवं इस्पात उद्योग के स्थानिक प्रतिरूप में परिवर्तन का विवरण प्रस्तुत कीजिये। (2014) |