जैव विविधता और पर्यावरण
सी-वीड मूल्य शृंखला विकास पर नीति आयोग की रिपोर्ट
प्रिलिम्स के लिये:सी-वीड, NITI आयोग, लाल शैवाल, नीला शैवाल, भारत में प्रमुख सी-वीड बेड, भारत में वाणिज्यिक सी-वीड उत्पाद। मेन्स के लिये:सी-वीड का विस्तार और महत्त्व, भारत में सी-वीड की कृषि। |
स्रोत: NITI आयोग
चर्चा में क्यों?
हाल ही में NITI आयोग ने ‘स्ट्रेटेजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सी-वीड वैल्यू चेन’ शीर्षक से प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में भारत में सी-वीड के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये एक व्यापक रोडमैप तैयार किया है।
- इसमें सी-वीड उत्पादन बढ़ाने के लिये अनुसंधान, निवेश, प्रशिक्षण, अवसंरचना विकास और बाज़ार संवर्द्धन के लिये उपाय शामिल हैं, जिससे पर्यावरण, अर्थव्यवस्था एवं स्थानीय समुदायों को लाभ हो सकता है।
सी-वीड क्या हैं?
- सी-वीड के संदर्भ में:
- ये जड़, तने और पत्तियों से रहित आदिकालीन, गैर-पुष्पीय समुद्री शैवाल हैं जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
- बड़े सी-वीड गहन जल में अंतर्जलीय वन का निर्माण करते हैं जिन्हें केल्प वन के रूप में जाना जाता है, जो मत्स्य, घोंघे और सी-अर्चिन/जलसाही (एक छोटा समुद्री जीव जिसके शरीर पर गोल, काँटेदार कवच होता है) के लिये नर्सरी के रूप में कार्य करते हैं।
- सी-वीड की कुछ प्रजातियाँ हैं: गेलिडिएला एसेरोसा (Gelidiella acerosa), ग्रेसिलेरिया एडुलिस (Gracilaria edulis), ग्रेसिलेरिया क्रैसा (Gracilaria crassa), ग्रेसिलेरिया वेरुकोसा (Gracilaria verrucosa), सार्गासम एसपीपी (Sargassum spp.) और टर्बिनेरिया एसपीपी (Turbinaria spp.)
- इसे हरे (क्लोरोफाइटा), भूरे (फियोफाइटा) और लाल (रोडोफाइटा) समूहों में वर्गीकृत किया गया है।
- उत्पादन परिदृश्य:
- वैश्विक:
- वर्ष 2019 में वैश्विक सी-वीड उत्पादन (कृषि+संग्रह) लगभग 35.8 मिलियन टन था, जिसमें से वन्य प्रजाति संग्रह 1.1 मिलियन टन रहा।
- पूर्वी और दक्षिणपूर्वी एशिया क्षेत्र वैश्विक उत्पादन के 97.4% के साथ उत्पादन के परिदृश्य पर हावी हैं, जबकि अमेरिका तथा यूरोप मुख्य रूप से वन्य प्रजाति संग्रह पर निर्भर हैं। इंडोनेशिया सी-वीड का एक प्रमुख उत्पादक है।
- विश्व स्तर पर, कप्पाफाइकस अल्वारेज़ी (Kappaphycus alvarezii) और यूचेमा डेंटिकुलटम (Eucheuma denticulatum) प्रजातियाँ उत्पादन के माध्यम से कुल सी-वीड उत्पादन का 27.8% हिस्सा हैं।
- वर्ष 2022 से 2030 तक सी-वीड उद्योग के 2.3% की CAGR से बढ़ने का अनुमान है।
- भारत:
- भारत में मुख्य रूप से तमिलनाडु में 5,000 परिवार प्राकृतिक सागरीय संस्तरों से सालाना लगभग 33,345 टन (गीला भार) सी-वीड की पैदावार प्राप्त करते हैं।
- भारत का वार्षिक सी-वीड राजस्व (लगभग 200 करोड़ रुपए) वैश्विक उत्पादन में 1% से भी कम योगदान देता है।
- सरकार का लक्ष्य कृषि में सकल मूल्य वर्द्धन में संबद्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्ष 2018-19 के 7.28% से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 में 9% करना है।
- वैश्विक:
- आयात और निर्यात:
- वर्ष 2021 में, वैश्विक सी-वीड बाज़ार 9.9 बिलियन अमेरीकी डॉलर का था।
- प्रमुख व्यापारिक देशों में चीन, इंडोनेशिया, फिलीपींस, कोरिया गणराज्य और मलेशिया शामिल थे।
- कोरिया 30% से अधिक बाज़ार हिस्सेदारी के साथ सी-वीड निर्यात में अग्रणी है, जबकि चीन में सी-वीड-आधारित हाइड्रोकोलॉइड्स (विभिन्न प्रकार के सी-वीड से प्राप्त प्रगाढ़क और जेलिंग एजेंट) की समान हिस्सेदारी है।
- भारत में प्रमुख सी-वीड बेड:
- तमिलनाडु एवं गुजरात के तटों के साथ-साथ लक्षद्वीप तथा अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के आस-पास प्रचुर मात्रा में सी-वीड संसाधन पाए जाते हैं।
- मुंबई, रत्नागिरी, गोवा, तमिलनाडु में कारवार, वर्कला, विझिंजम और पुलिकट, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में चिल्का के आस-पास उल्लेखनीय सी-वीड बेड मौजूद हैं।
- संबंधित सरकारी पहल:
- सी-वीड मिशन: वर्ष 2021 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य मूल्य संवर्द्धन के लिये सी-वीड की कृषि और प्रसंस्करण का व्यवसायीकरण करना है। इसका उद्देश्य भारत के 7,500 किलोमीटर के समुद्र तट पर कृषि को बढ़ाना भी है।
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY): सरकार इस पहल के माध्यम से देश में सी-वीड की कृषि को भी बढ़ावा दे रही है।
- सी-वीड उत्पादों का व्यवसायीकरण: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)- केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (CMFRI) ने दो सी-वीड-आधारित न्यूट्रास्युटिकल उत्पादों, कैडलमिन TM इम्यूनलगिन एक्सट्रैक्ट (कैडलमिन TM IMe) और कैडलमिन TM एंटीहाइपरकोलेस्ट्रोलेमिक एक्सट्रैक्ट (कैडलमिन TM ACe) का सफलतापूर्वक व्यवसायीकरण किया है।
- पर्यावरण के अनुकूल 'हरित' तकनीक से विकसित इन उत्पादों का उद्देश्य एंटी-वायरल प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना और उच्च कोलेस्ट्रॉल या डिस्लिपिडेमिया (कोलेस्ट्रॉल का असंतुलन) से निपटना है।
- तमिलनाडु में बहुउद्देश्यीय सी-वीड पार्क
सी-वीड के उपयोग और लाभ क्या हैं?
- पोषण के लिये: सी-वीड कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटेशियम के साथ-साथ विटामिन A, B1, B12, C, D, E, नियासिन, फोलिक एसिड, पैंटोथेनिक एसिड एवं राइबोफ्लेविन का एक स्रोत है। इनमें चयापचय और समग्र स्वास्थ्य के लिये आवश्यक अमीनो एसिड भी होते हैं।
- औषधीय उद्देश्य: सी-वीड में औषधीय प्रभाव वाले सूजनरोधी और रोगाणुरोधी कारक होते हैं। कुछ सी-वीड में कैंसर से लड़ने वाले गुण होते हैं, जो घातक ट्यूमर एवं ल्यूकेमिया के खिलाफ संभावित रूप से प्रभावी होते हैं।
- निर्माण उपयोग: इनका उपयोग टूथपेस्ट और फलों की जेली जैसे उत्पादों में बाइंडिंग एजेंट (पायसीकारक) के रूप में और ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स तथा स्किनकेयर उत्पादों में सॉफ्टनर (इमोलिएंट) के रूप में किया जाता है।
- वाणिज्यिक मूल्य: वाणिज्यिक रूप से, सी-वीड बायोएक्टिव मेटाबोलाइट्स, खाद, चारा और सेल वॉल पॉलीसेकेराइड जैसे कि अगर, एल्गिन एवं कैरेजीनन के लिये मूल्यवान हैं।
- इनका उपयोग खाद्य, दवा, कॉस्मेटिक और खनन उद्योगों में एवं समुद्री रसायनों को निकालने के लिये कच्चे माल के रूप में किया जाता है।
- कृषि लाभ: यह कृषि उत्पादकता और पशु चारा योजक को बढ़ाने के लिये फसल बायोस्टिमुलेंट के रूप में भी कार्य करता है।
- सी-वीड की कृषि समुद्री उत्पादन को बढ़ाती है, मत्स्यन कृषकों की आय को बढ़ाती है और तटीय आजीविका में विविधता लाती है। इष्टतम परिस्थितियों में, एक हेक्टेयर (400 बाँस की राफ्ट) प्रतिवर्ष 13,28,000 रुपए तक कमा सकती है, जिसमें दो व्यक्तियों का परिवार 45 राफ्ट का प्रबंधन करता है, जिससे मूल्यवान आय के अवसर उत्पन्न होते हैं।
- जैव संकेतक: सी-वीड कृषि, औद्योगिक, जलीय कृषि और घरेलू अपशिष्ट से अतिरिक्त पोषक तत्त्वों को अवशोषित करते हैं, शैवाल के पनपने को रोकते हैं तथा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करते हैं।
- पर्यावरणीय लाभ: सी-वीड कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सहायता करते हैं। समुद्री कृषि सी-वीड की अनुमानित कार्बन अवशोषण दर प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर 57.64 मीट्रिक टन CO2 है, जबकि तालाब में उगाए गए सी-वीड प्रति हेक्टेयर 12.38 मीट्रिक टन CO2 अवशोषित करते हैं।
भारत में सी-वीड उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये नीति आयोग की सिफारिशें क्या हैं?
- कार्य आवंटन नियम, 1961 में संशोधन: वर्तमान में, सी-वीड को भारतीय समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1981 के तहत "मत्स्य" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसके वैश्विक उत्पादन को कार्य आवंटन नियम, 1961 द्वारा ट्रैक किया जाता है। बेहतर प्रबंधन के लिये सी-वीड मूल्य शृंखला विकास का कार्य मत्स्य विभाग को सौंपें।
- सी-वीड और उसके उत्पादों का निर्यात एवं प्रमाणन: सी-वीड के निर्यात एवं प्रमाणन की निगरानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत MPEDA को हस्तांतरित की जाएगी तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) FPO और SHG के माध्यम से बिक्री का कार्य संभालेगा।
- MPEDA द्वारा प्रोटोकॉल स्थापित करने तथा प्रमाणन का प्रबंधन करने वाली एक स्वतंत्र संस्था के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन सामंजस्य को लागू करना।
- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण: RBI को जलवायु परिवर्तन से निपटने में इसकी भूमिका को देखते हुए बैंकों के लिये प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) की सूची में सी-वीड से संबंधित ऋण को जोड़ने पर विचार करना चाहिये।
- बीमे के माध्यम से व्यापक जोखिम कवर: सी-वीड के उत्पादन में मौसम की घटनाओं से होने वाले जोखिमों से निपटने के लिये एक व्यापक बीमा योजना विकसित की जानी चाहिये। इस कार्यक्रम में फसल बीमा, किसान जीवन बीमा और पूंजीगत बुनियादी अवसरंचना को शामिल किया जाना चाहिये।
- वित्तीय सहायता: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-किसान) एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) योजनाओं का विस्तार सी-वीड किसानों को शामिल करने के लिये किया जाना चाहिये तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) को वित्तीय व कृषि आदान सहायता हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार करने चाहिये।
- इसके अतिरिक्त उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना में शामिल किया जाना चाहिये तथा समूह वित्तपोषण की सुविधा के लिये संयुक्त देयता समूहों (JLG) को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- निवेश एवं ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस:
- सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के निवेश को प्रोत्साहित करके तटीय सी-वीड क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना, स्टैंड-अप इंडिया एवं स्टार्टअप इंडिया जैसे सुधारों व पहलों का लाभ उठाना।
- क्लस्टर/सामूहिक विकास और विभिन्न हितधारकों के लिये पहुँच का समर्थन करने हेतु सी-वीड के उत्पादन हेतु जियो-टैग किये गए स्थलों के साथ एक गतिशील डेटा पोर्टल विकसित करना।
- e-NAM और राज्य कृषि मंडियों में सी-वीड एवं उसके उत्पादों को शामिल करना तथा बिक्री हस्तक्षेप हेतु PPP की खोज करना।
- डेटा-आधारित निर्णय लेने के लिये सी-वीड किसान सेवा मंच (SFSP) का विस्तार करना।
- मानसून के बाद गुणवत्तापूर्ण बीज सामग्री की तत्काल उपलब्धता के लिये समुद्री राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बीज बैंक स्थापित करना।
- प्राथमिक प्रसंस्करण के लिये क्लस्टर स्तर पर रसद और प्रसंस्करण केंद्र बनाना, जिसमें गोदाम, परिवहन तथा पैकेजिंग सुविधाएँ शामिल हों।
- कौशल विकास: कृषि एवं मात्स्यिकी से संबंधित विश्वविद्यालयों, MPEDA-RGCA तथा ICAR संस्थानों के माध्यम से सी-वीड के उत्पादन, पैदावार एवं इसके पश्चात् किये जाने वाले प्रबंधन से जुड़े प्रमाण-पत्र व डिप्लोमा पाठ्यक्रम उपलब्ध किये जाने चाहिये।
|
दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: सी-वीड क्या हैं और इसके क्या उपयोग हैं? भारत में इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये सरकार की क्या पहल हैं? |


शासन व्यवस्था
न्याय प्रणाली में DNA प्रोफाइलिंग
प्रिलिम्स के लिये:डी-ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA), DNA प्रोफाइलिंग, मोनोज़ायगोटिक ट्विन्स, भारतीय विधि आयोग, अनुच्छेद 20(3), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 मेन्स के लिये:DNA प्रोफाइलिंग और चुनौतियाँ, न्यायिक प्रणाली में उभरती प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग |
स्रोत: द हिंदू
चर्चा में क्यों?
जून 2024 में लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के तहत दोषसिद्धि को पलटने के मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के कारण कानूनी मामलों में डी-ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA) प्रोफाइलिंग की विश्वसनीयता पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है।
- न्यायालय ने दोषसिद्धि के लिये केवल DNA साक्ष्य पर निर्भर न होने के महत्त्व पर ज़ोर देने के साथ ही पुष्टि करने वाले साक्ष्य की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
DNA प्रोफाइलिंग क्या है?
- रिचय: DNA प्रोफाइलिंग या DNA फिंगरप्रिंटिंग में किसी व्यक्ति के DNA के विशिष्ट क्षेत्रों का विश्लेषण करके उसकी पहचान की जाती है। जबकि मानव DNA 99.9% समान है, शेष 0.1% में शॉर्ट टेंडम रिपीट (Short Tandem Repeats- STR) नामक अद्वितीय/विशिष्ट अनुक्रम होता है, जो फोरेंसिक जाँच के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- आनुवांशिक कोड के रूप में DNA: DNA यूकेरियोटिक कोशिकाओं (जंतु और पादप) के नाभिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं (बैक्टीरिया) के कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। इसकी संरचना एक डबल हेलिक्स के रूप में होती है।
- यह गुणसूत्रों के 23 युग्म में व्यवस्थित होता है, जो माता-पिता दोनों से समान रूप से वंशागत होते हैं, जो एडेनिन (A), गुआनिन (G), थाइमिन (T) और साइटोसिन (C) नामक चार न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रमों में आनुवंशिक सूचना को एनकोड करते हैं।
- DNA को विभिन्न जैविक पदार्थों जैसे रक्त, लार, वीर्य और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों से निकाला जा सकता है। DNA प्रोफाइल बनाने के लिये इन नमूनों को एकत्र किया जाता है और उनका विश्लेषण किया जाता है।
- शारीरिक संपर्क के दौरान पीछे छूटे (बचे) DNA, जिसे स्पर्श DNA/टच DNA के रूप में जाना जाता है, प्रायः कम मात्रा में होते हैं और संभावित संदूषण के कारण प्रोफाइलिंग के लिये आदर्श नहीं होते हैं।
- DNA प्रोफाइलिंग में विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है जिन्हें जेनेटिक मार्कर कहा जाता है, जिसमें मोनोज़ायगोटिक ट्विन्स (समान जुड़वाँ) को छोड़कर व्यक्तियों के बीच STR इनकी परिवर्तनशीलता के कारण अधिमान्य मार्कर होते हैं।
- DNA प्रोफाइलिंग की प्रक्रिया:
- पृथक्करण: एकत्रित जैविक नमूनों से DNA का निष्कर्षण।
- शुद्धिकरण और परिमाणीकरण: यह सुनिश्चित करना कि DNA संदूषकों से मुक्त है और इसकी सांद्रता का निर्धारण करना।
- प्रवर्द्धन: विश्लेषण के लिये पर्याप्त DNA उत्पन्न करने के लिये चयनित आनुवंशिक मार्करों का प्रतिकृतियन करना।
- विज़ुअलाइज़ेशन और जीनोटाइपिंग: DNA मार्करों के विशिष्ट अनुक्रमों की पहचान करना।
- सांख्यिकीय विश्लेषण एवं व्याख्या: DNA प्रोफाइल की तुलना करना और मिलान की संभावना की गणना करना।
- विशेष स्थितियाँ:
- खराब नमूनों के मामलों में, miniSTRs (छोटे DNA टुकड़े) का उपयोग किया जा सकता है क्योंकि वे पर्यावरणीय तनाव से बचने की अधिक संभावना रखते हैं। इसके अतिरिक्त, माइटोकॉन्ड्रियल DNA (mtDNA) मातृ वंश का पता लगाने के लिये उपयोगी है और इसका उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब नाभिकीय DNA अपर्याप्त होता है।
कानूनी कार्यवाहियों में DNA प्रोफाइलिंग का उपयोग कैसे किया जाता है?
- मिलान प्रक्रिया: फोरेंसिक मामलों में साक्ष्य से प्राप्त DNA प्रोफाइल की तुलना ज्ञात या संदर्भ नमूनों से की जाती है। इस तुलना के परिणाम तीन संभावित परिणाम दे सकते हैं:
- मिलान: DNA प्रोफाइल में कोई अंतर नहीं है, जो एक सामान्य स्रोत का संकेत देता है।
- बहिष्करण: प्रोफाइल अलग-अलग हैं, जो अलग-अलग स्रोतों का संकेत देते हैं।
- अनिर्णायक: डेटा स्पष्ट परिणाम प्रदान नहीं करता है।
- सांख्यिकीय समर्थन: यदि प्रोफाइल सुमेलित होती हैं तो भी यह निर्णायक रूप से पहचान साबित नहीं करता है; इसके बजाय विशेषज्ञ एक "यादृच्छिक घटना अनुपात" प्रदान करते हैं, जो यह दर्शाता है कि जनसंख्या में कितनी बार समान प्रोफाइल दिखाई दे सकते हैं।
- कानूनी व्याख्या: मद्रास उच्च न्यायालय और भारत का विधि आयोग ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि DNA मिलान निर्णायक रूप से पहचान साबित नहीं करता है।
- "यादृच्छिक घटना अनुपात" यह इंगित करता है कि जनसंख्या में एक विशेष DNA प्रोफाइल कितनी बार दिखाई दे सकती है, जो उचित संदेह से परे अपराध स्थापित करने के लिये पर्याप्त नहीं हो सकता है।
भारत में DNA प्रोफाइलिंग के संबंध में कानूनी प्रावधान क्या हैं?
- कानूनी ढाँचा:
- भारतीय संविधान: अनुच्छेद 20(3) व्यक्तियों को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिये मजबूर किये जाने से बचाता है तथा आत्म-दोषी ठहराए जाने के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है तथा अनाधिकृत हस्तक्षेप पर रोक लगाता है।
- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC): धारा 53 जाँच एजेंसी के अनुरोध पर संदिग्धों की DNA प्रोफाइलिंग को अधिकृत करती है। धारा 53A विशेष रूप से बलात्कार के संदिग्धों के लिये DNA प्रोफाइलिंग की अनुमति देती है।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 ने 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) को प्रतिस्थापित कर दिया।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872: धारा 45-51 न्यायालय में DNA साक्ष्य सहित विशेषज्ञ साक्ष्य की स्वीकार्यता से संबंधित हैं।
- भारतीय संविधान: अनुच्छेद 20(3) व्यक्तियों को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिये मजबूर किये जाने से बचाता है तथा आत्म-दोषी ठहराए जाने के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- न्यायिक उदाहरण:
- पट्टू राजन बनाम टी.एन. राज्य 2019: सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि DNA साक्ष्य का सत्यापनात्मक मूल्य मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों को दिये गए महत्त्व, चाहे वे विपरीत हों या पुष्टिकारक, के आधार पर भिन्न-भिन्न होता है।
- उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि DNA साक्ष्य, यद्यपि अधिकाधिक सटीक और विश्वसनीय होते जा रहे हैं, लेकिन वे अचूक नहीं हैं तथा ऐसे साक्ष्य के अभाव में किसी पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिये, विशेषकर तब जब अन्य ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद हों।
- शारदा बनाम धर्मपाल, 2003: सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किये बिना DNA प्रोफाइलिंग सहित चिकित्सा परीक्षाओं को अनिवार्य बनाने के वैवाहिक न्यायालयों के अधिकार को बरकरार रखा।
- दास @ अनु बनाम केरल राज्य, 2022: केरल उच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्म-दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अधिकार केवल साक्ष्य पर लागू होता है और आपराधिक मामले विशेषकर यौन अपराध में DNA नमूने लेना इस अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि CrPC की धारा 53A पुलिस को नमूने एकत्र करने के लिये आरोपी को चिकित्सक के पास भेजने का अधिकार देती है।
- पट्टू राजन बनाम टी.एन. राज्य 2019: सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि DNA साक्ष्य का सत्यापनात्मक मूल्य मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों को दिये गए महत्त्व, चाहे वे विपरीत हों या पुष्टिकारक, के आधार पर भिन्न-भिन्न होता है।
- विधि आयोग की सिफारिशें:
- भारतीय विधि आयोग की 271वीं रिपोर्ट (2017) में DNA प्रोफाइलिंग के लिये व्यापक कानून का प्रस्ताव दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप DNA प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019 तैयार हुआ। दुरुपयोग को रोकने और DNA प्रोफाइलिंग को केवल कानूनी उपयोग तक सीमित रखने हेतु एक अद्वितीय नियामक ढाँचे का आग्रह किया गया।
DNA प्रोफाइलिंग की सीमाएँ क्या हैं?
- पर्यावरणीय तनाव और नमूने का क्षरण: पर्यावरणीय कारकों के कारण DNA को नुकसान पहुँच सकता है, जिसके परिणामस्वरूप नमूने अधूरे या क्षीण हो सकते हैं।
- इन मामलों में miniSTRs और mtDNA विश्लेषण जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी उनमें सीमाएँ हैं।
- जटिलता और विश्वसनीयता: DNA प्रोफाइलिंग एक जटिल प्रक्रिया है जिसके लिये सटीक तकनीकों और स्थितियों की आवश्यकता होती है। संदूषण, अनुचित हैंडलिंग या परीक्षण में देरी जैसे मुद्दे परिणामों की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकते हैं।
- लागत: DNA विश्लेषण महंगा हो सकता है, जिससे कुछ मामलों में इसकी पहुँच सीमित हो सकती है।
- कानूनी व्याख्या: जबकि DNA साक्ष्य एक शक्तिशाली उपकरण है, इसे अचूक (हमेशा प्रभावी) के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये। न्यायालयों को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निर्णय सुनिश्चित करने के लिये अन्य पुष्टि या विरोधाभासी साक्ष्य के साथ DNA साक्ष्य पर विचार करना चाहिये।
- मौजूदा कानूनी ढाँचा DNA साक्ष्य को मान्यता देता है, लेकिन इसमें व्यापक विनियामक संरचना का अभाव है।
- DNA प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019 का उद्देश्य इन कमियों को दूर करना है। संसद में कई बार पेश किये गए DNA विधेयक को DNA प्रौद्योगिकी की सटीकता, व्यक्तिगत गोपनीयता के लिये संभावित खतरों और दुरुपयोग की संभावना के आधार पर विरोध का सामना करना पड़ा।
आगे की राह
- सटीकता और विश्वसनीयता बढ़ाना: DNA प्रोफाइलिंग तकनीकों को बेहतर बनाने और नमूने के क्षरण एवं संदूषण से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिये अनुसंधान तथा विकास में निवेश करना। प्रक्रियाओं को मानकीकृत करना और फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना।
- निष्पक्ष कानूनी व्यवहार सुनिश्चित करना: दोषसिद्धि में साक्ष्य की पुष्टि करने के महत्त्व पर ज़ोर देना। न्यायपूर्ण और निष्पक्ष परिणाम सुनिश्चित करने हेतु न्यायालय में DNA साक्ष्य की स्वीकार्यता और महत्त्व के लिये दिशा-निर्देश विकसित करना।
- DNA प्रौद्योगिकी विधेयक: DNA प्रौद्योगिकी विधेयक, 2019 का उद्देश्य दुरुपयोग को रोकने और DNA प्रोफाइलिंग का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिये एक विनियामक ढाँचा तैयार करना है। गोपनीयता संबंधी चिंताओं को दूर करने और मज़बूत सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिये इस विधेयक पर पुनः विचार करने तथा संभावित रूप से संशोधन करने की आवश्यकता है।
- कानूनी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता: जनता का विश्वास बनाए रखने के लिये DNA साक्ष्य को एकत्रित करने, उसका विश्लेषण करने और न्यायालय में प्रस्तुत करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
|
दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: दोषसिद्धि के लिये केवल DNA प्रोफाइलिंग पर निर्भर रहने से संभावित समस्याएँ क्या हैं और न्यायिक प्रक्रिया में न्याय सुनिश्चित करने हेतु इन मुद्दों को कैसे कम किया जा सकता है? |
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: DNA बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है?
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 प्रश्न: विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही नहीं है? (2019) (a) विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिये गए DNA के खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। उत्तर: (a) |
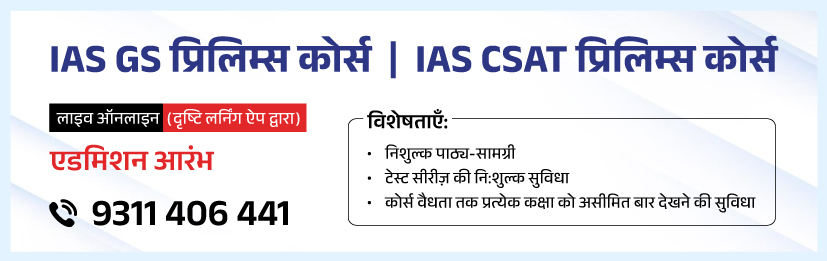
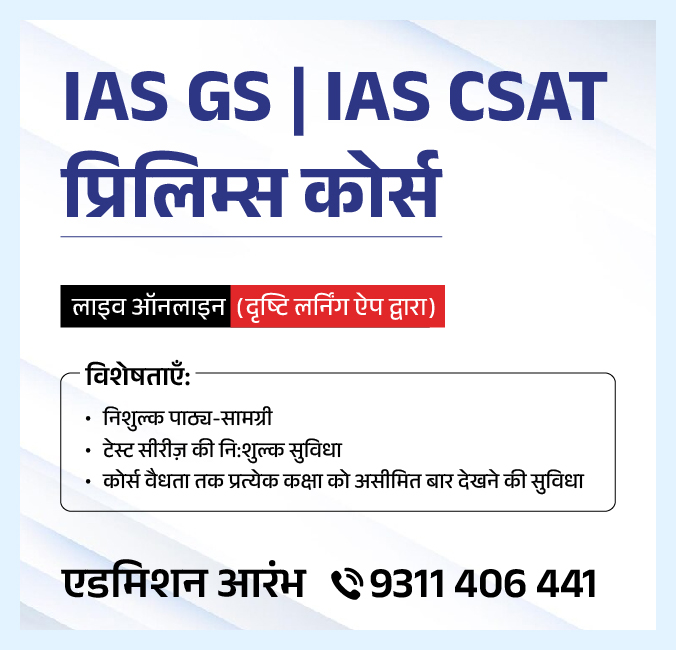
भारतीय राजव्यवस्था
बुद्धदेव भट्टाचार्य और साम्यवाद
प्रिलिम्स के लिये:मुख्यमंत्री, साम्यवाद, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), IT और IT-सक्षम सेवाएँ, पद्म भूषण पुरस्कार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), मेरठ षडयंत्र केस (1929-1933), बंगाल अकाल, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946, तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 मेन्स के लिये:भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव। |
स्रोत: द हिंदू
चर्चा में क्यों?
पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य (1944-2024) का हाल ही में कोलकाता में निधन हो गया।
- वह वर्ष 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे और साम्यवाद से जुड़े होने के बावजूद उनके शासन में औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया गया।
बुद्धदेव भट्टाचार्य कौन थे?
- परिचय:
- वे ज्योति बसु के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने वर्ष 2001 और 2006 में लगातार दो कार्यकालों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को सत्ता में पहुँचाया।
- वह वर्ष 2011 तक मुख्यमंत्री रहे जब तृणमूल कॉन्ग्रेस ने वाम मोर्चे के 34 वर्ष के शासन को समाप्त कर दिया।
- शासन और नीतियाँ:
- उनके कार्यकाल के दौरान, वाम मोर्चा सरकार ने साम्यवाद का पालन करने के बावजूद व्यापार के प्रति अपेक्षाकृत खुली नीति अपनाई।
- सिंगूर में टाटा नैनो प्लांट लगाने और नंदीग्राम में विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की योजना के पीछे भी उनका ही हाथ था। हालाँकि भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर स्थानीय राजनीतिक दलों के विरोध के बाद इस योजना को छोड़ दिया गया।
- उनके शासनकाल के दौरान पश्चिम बंगाल में IT और IT-सक्षम सेवाओं के क्षेत्र में निवेश हुआ।
- पुरस्कार: वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार देने की घोषणा की लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि मार्क्सवादी आमतौर पर सार्वजनिक सेवा के लिये पुरस्कार स्वीकार करने में अनिच्छुक होते हैं।
- मृत्यु: वे क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिज़ीज़ से पीड़ित थे और उनका शरीर चिकित्सा अनुसंधान के लिये NRS मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल, कोलकाता को दान कर दिया गया था।
साम्यवाद क्या है?
- परिचय:
- साम्यवाद कार्ल मार्क्स से जुड़ी एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है। यह एक वर्गहीन समाज की वकालत करता है जहाँ सभी संपत्ति और धन का सामूहिक स्वामित्व हो।
- मार्क्स ने वर्ष 1848 में अपनी रचना “कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र” में इन विचारों को लोकप्रिय बनाया।
- मार्क्स ने तर्क दिया कि पूंजीवाद असमानता और शोषण को जन्म देता है, जिससे श्रमिक वर्ग (सर्वहारा वर्ग) की कीमत पर कुछ धनी लोगों को लाभ होता है।
- उद्देश्य:
- मार्क्स ने एक ऐसे संसार की कल्पना की थी जहाँ श्रम स्वैच्छिक हो और धन सभी नागरिकों के बीच समान रूप से साझा किया जाए।
- मार्क्स ने प्रस्ताव दिया कि अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण वर्ग भेद को समाप्त कर देगा।
- साम्यवाद के प्रमुख उदाहरण सोवियत संघ और चीन थे। वर्ष 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया लेकिन चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में कुछ पूंजीवाद को शामिल करने के लिये बड़े पैमाने पर संशोधन किया है।
- साम्यवादी आर्थिक प्रणाली:
- साम्यवाद का लक्ष्य एक ऐसी प्रणाली स्थापित करना था, जिसमें वर्ग भेद समाप्त हो जाए और उत्पादन के साधनों पर जनता का स्वामित्व हो।
- इसकी विशेषता एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ संपत्ति का स्वामित्व राज्य के पास होता है और वस्तुओं का उत्पादन स्तर एवं कीमतें राज्य द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
- व्यक्ति शेयर या अचल संपत्ति जैसी निजी संपत्ति के मालिक नहीं हो सकते।
- इसका मुख्य लक्ष्य पूंजीवाद (निजी स्वामित्व द्वारा शासित एक आर्थिक प्रणाली) को खत्म करना है।
- मार्क्स पूंजीवाद से घृणा करते थे इसमें क्योंकि सर्वहारा वर्ग का शोषण किया जाता था और राजनीति में उसका अनुचित प्रतिनिधित्व किया जाता था।
भारत में साम्यवाद का इतिहास और प्रभाव क्या है?
- गठन: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) का गठन 17 अक्तूबर 1920 को ताशकंद में एम.एन. रॉय जैसे भारतीय क्रांतिकारियों के योगदान से हुआ था।
- दिसंबर 1925 में, कानपुर में एक खुले सम्मेलन में CPI की स्थापना हुई जिसका मुख्यालय बॉम्बे में था।
- स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका:
- साम्यवादी विचारों ने कॉन्ग्रेस को प्रभावित किया, जिससे वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मज़बूत रूख की ओर बढ़ गई, जो हल्के प्रतिरोध से अलग था।
- अंग्रेज़ों ने गिरफ़्तारियाँ करके और षड्यंत्र के मामले चलाकर प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिनमें सबसे उल्लेखनीय मेरठ षड्यंत्र मामला (वर्ष 1929-1933) था।
- वर्ष 1943 के बंगाल अकाल के दौरान कम्युनिस्टों ने राहत प्रयासों का आयोजन किया।
- जन संघर्ष: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में मज़दूर वर्ग के संघर्षों और किसान लामबंदी में उछाल देखा गया, जिसमें वर्ष 1946 में रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह भी शामिल था।
- तेभागा आंदोलन: बंगाल में बेहतर काश्तकारी या शेयरक्रॉपिंग अधिकारों की मांग को लेकर एक महत्त्वपूर्ण किसान आंदोलन, जिसमें हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रदर्शन किया गया।
- तेलंगाना आंदोलन (वर्ष 1946-1951): उन्होंने सामंती शोषण और निरंकुश शासन के खिलाफ युद्ध लड़ा, जिसके परिणामस्वरूप भूमि पुनर्वितरण हुआ।
- स्वतंत्रता के बाद (वर्ष 1947):
- पहली लोकसभा (वर्ष 1952-57) में विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) थी।
- वर्ष 1957 में, CPI ने केरल में राज्य चुनाव जीता। केरल स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था जिसने लोकतांत्रिक तरीके से कम्युनिस्ट सरकार का चुनाव किया।
- साम्यवाद आंदोलन में विभाजन: CPI के कुछ सदस्यों का मानना था कि कम्युनिस्टों को कॉन्ग्रेस पार्टी के भीतर वामपंथी समूह के साथ सहयोग करना चाहिये जो साम्राज्यवाद और सामंतवाद दोनों का विरोध करता था।
- इससे वर्ष 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में विभाजित हो गई।
- कॉन्ग्रेस के साथ सहयोग करने के मार्ग का विरोध करने वाले गुट ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), या CPI (M) का गठन किया, जबकि दूसरे गुट ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) नाम बरकरार रखा।
- वर्ष 1969 में माओत्से तुंग की तरह सशस्त्र संघर्ष की आवश्यकता पर विश्वास करते हुए, कम्युनिस्टों के एक अन्य समूह ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) या CPI (ML) का गठन किया।
माओवाद क्या है?
- परिचय:
- माओवाद चीन के माओ त्से तुंग द्वारा विकसित साम्यवाद का एक रूप है।
- यह सशस्त्र विद्रोह, जन-आंदोलन और सामरिक गठबंधनों के संयोजन के माध्यम से राज्य की सत्ता पर कब्ज़ा करने का एक सिद्धांत है।
- माओवादी अपने विद्रोह सिद्धांत के अन्य घटकों के रूप में राज्य संस्थाओं के खिलाफ अधिप्रचार और दुष्प्रचार का भी प्रयोग करते हैं।
- माओ ने इस प्रक्रिया को ‘दीर्घकालिक जनयुद्ध’ कहा, जहाँ सत्ता पर कब्ज़ा करने के लिये ‘सैन्य लाइन’ पर ज़ोर दिया जाता है।
- केंद्रीय विषय:
- माओवादी विचारधारा का केंद्रीय विषय राज्य की सत्ता पर कब्ज़ा करने के साधन के रूप में हिंसा और सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग है।
- माओवादी विद्रोह सिद्धांत के अनुसार 'हथियार रखना अपरिहार्य है'।
- माओवादी विचारधारा हिंसा का महिमामंडन करती है और पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PLGA) के कैडरों को उनके प्रभुत्व में आबादी के बीच आतंक उपन्न करने के लिये हिंसा के सबसे बुरे रूपों में विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है।
- माओवादी विचारधारा का केंद्रीय विषय राज्य की सत्ता पर कब्ज़ा करने के साधन के रूप में हिंसा और सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग है।
- भारत में माओवादियों का प्रभाव:
- भारत में सबसे बड़ा और सबसे हिंसक माओवादी संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (Maoist / माओवादी) है।
- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का गठन वर्ष 2004 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) पीपुल्स वार (पीपुल्स वार ग्रुप) और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया (MCCI) के विलय के माध्यम से हुआ था।
- CPI (माओवादी) और इसके सभी फ्रंट संगठन संरचनाओं को गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल किया गया है।
- फ्रंट संगठन मूल माओवादी पार्टी की शाखाएँ हैं, जो कानूनी दायित्व से बचने के लिये एक पृथक अस्तित्व का दावा करती हैं।
मार्क्सवाद और माओवाद के बीच क्या अंतर है?
- क्रांति का फोकस: दोनों ही सर्वहारा क्रांति, जो समाज को बदल देगी, के सिद्धांत पर केंद्रित हैं।
- मार्क्सवाद शहरी श्रमिकों पर ध्यान केंद्रित करता है जबकि माओवाद किसान या खेती करने वाली आबादी पर ध्यान केंद्रित करता है।
- औद्योगीकरण पर दृष्टिकोण: मार्क्सवाद एक आर्थिक रूप से सुदृढ़ राज्य में विश्वास करता है जो औद्योगिक है।
- माओवाद का एक व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण है जो कृषि को भी आवश्यक महत्त्व देता है।
- सामाजिक परिवर्तन की प्रेरक शक्ति: मार्क्सवाद के अनुसार सामाजिक परिवर्तन अर्थव्यवस्था द्वारा संचालित होता है।
- हालाँकि माओवाद 'मानव स्वभाव के लचीलापन' पर ज़ोर देता है। माओवाद इस बारे में उल्लेख करता है कि कैसे केवल इच्छाशक्ति का प्रयोग करके मानव स्वभाव को बदला जा सकता है।
- समाज पर अर्थव्यवस्था का प्रभाव: मार्क्सवाद का मानना था कि समाज में होने वाली हर चीज़ अर्थव्यवस्था से जुड़ी होती है।
- माओवाद का मानना था कि समाज में होने वाली हर चीज़ मानव इच्छा का परिणाम है।
निष्कर्ष
भारत में साम्यवाद का एक महत्त्वपूर्ण और जटिल इतिहास रहा है, जिसने राजनीतिक एवं सामाजिक दोनों परिदृश्यों को प्रभावित किया है। बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसे नेताओं ने राज्य की नीतियों को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेषकर पश्चिम बंगाल में जहाँ साम्यवाद दशकों तक हावी रहा। जबकि विचारधारा ने सामाजिक न्याय और श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा दिया, इसके कार्यान्वयन को अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, विशेषकर समानता एवं सांप्रदायिक सद्भाव के सिद्धांतों के साथ औद्योगिक विकास को संतुलित करने में।
|
दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. स्वतंत्रता से पहले और बाद के भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन की भूमिका पर चर्चा कीजिये। उन्होंने कमज़ोर वर्गों की चिंताओं को आवाज़ देकर भारतीय लोकतंत्र को मज़बूत करने में कैसे सहायता की? |
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिये: (2018)
निम्नलिखित में से कौन-सा उपर्युक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम है? (a) 4 – 1 – 2 – 3 उत्तर: (b) प्रश्न. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2019) व्यक्ति धारित पद 1. सर तेज बहादुर सप्रू : अध्यक्ष, अखिल भारतीय उदार संघ उपर्युक्त में से कौन-सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया और अपना सामाजिक आधार बढ़ाया। विवेचना कीजिये । (2020) प्रश्न. पिछली शताब्दी के तीसरे दशक से भारतीय स्वतंत्रता की स्वप्न दृष्टि के साथ सम्बद्ध हो गए नए उद्देश्यों के महत्त्व को उजागर कीजिये। (2017) प्रश्न. विश्व में घटित कौन-सी मुख्य राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों ने भारत में उपनिवेश-विरोधी (ऐंटी-कॉलोनियल) संघर्ष को प्रेरित किया? (2014) |






