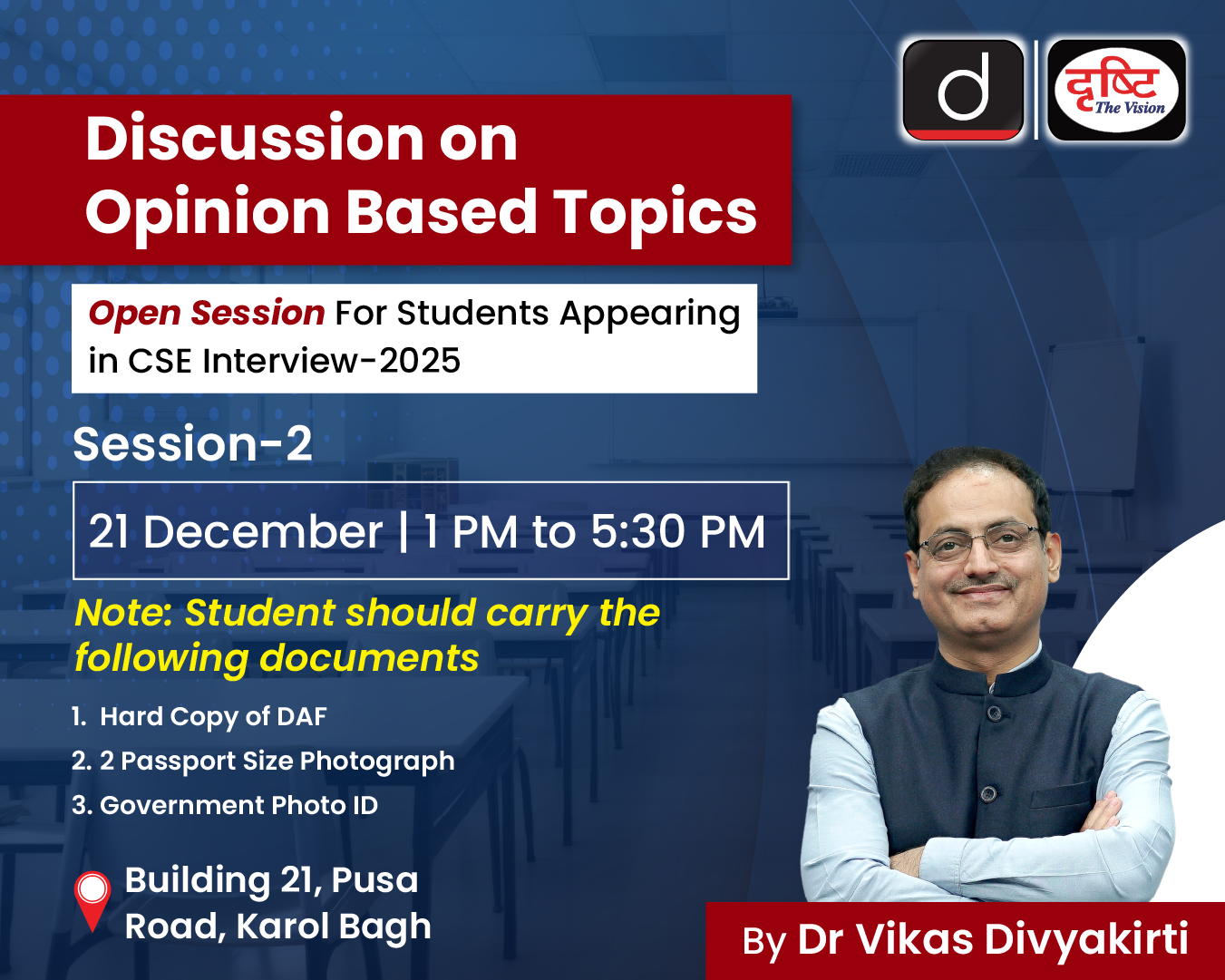आपदा प्रबंधन
हीटवेव एक अधिसूचित आपदा के रूप में
- 25 Jun 2024
- 89 min read
प्रिलिम्स के लिये:हीटवेव, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD), ग्लोबल वार्मिंग(वैश्विक तापन), नगरीय ऊष्मा द्वीप, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ग्रीनहाउस गैसें, एरोसोल, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये सेंडाई फ्रेमवर्क, जलवायु परिवर्तन के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना, प्रकृति-आधारित समाधान, पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी मेन्स के लिये:भारत में हीटवेव के लिये मानदंड, हीटवेव के प्रभावों को कम करने की रणनीतियाँ |
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
चर्चा में क्यों?
भारत में हाल ही में उत्पन्न हुई गर्मी की समस्या ने हीटवेव को केवल प्राकृतिक आपदा को आपदा प्रबंधन (DM) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अधिसूचित आपदाओं की सूची में जोड़ने से संबंधित बहस को फिर से जन्म दे दिया है।
हीट वेव्स क्या हैं?
- परिचय:
- हीटवेव भारत में ग्रीष्म ऋतु के दौरान होने वाली असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि है। हीटवेव आमतौर पर मार्च से जून के बीच चलती है और साथ ही कभी-कभी दुर्लभ मामलों में जुलाई तक चलती है।
- हीटवेव को परिभाषित करने के लिये IMD मानदंड:
|
मानदंड |
विवरण |
|
क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के आधार पर |
|
|
सामान्य अधिकतम तापमान से विचलन के आधार पर |
|
|
वास्तविक अधिकतम तापमान के आधार पर |
|
|
घोषणा का मानदंड |
|
हीटवेव के कारण क्या हैं?
- गर्म और शुष्क वायु का प्रचलन: गर्म और शुष्क वायु का एक बड़ा क्षेत्र गर्मी के रूप में कार्य करता है। फिर प्रचलित वायु इस गर्म वायु को अन्य क्षेत्रों में ले जाती हैं, जिससे तापमान में वृद्धि होती है।
- नमी का अभाव: वायु में नमी (Moisture) गर्मी को रोककर रखती है और उसे बाहर निकलने से रोकती है, जबकि शुष्क वायु सौर विकिरण को अधिक आसानी से सतह तक पहुँचने देती है तथा रात में न्यूनतम अवरोध के साथ वापस भेज देती है, जिसके परिणामस्वरूप दिन के तापमान में तेज़ी से वृद्धि होती है।
- बादल रहित आसमान: बादल एक ढाल की तरह काम करते हैं, जो सूर्य की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करते हैं और पृथ्वी की सतह को गर्म होने से रोकते हैं। साफ, बादल रहित आकाश अधिकतम सौर विकिरण को ज़मीन तक पहुँचने देता है, जिससे गर्मी बढ़ती है।
- बड़े आयाम वाला प्रतिचक्रवाती प्रवाह: प्रतिचक्रवात बड़े पैमाने पर वायुमंडलीय परिसंचरण प्रतिरूप हैं, जिनमें वायु का अवतलन शामिल है।
- यह अवतलित वायु रुद्धोष्म रूप से संपीड़ित होकर गर्म हो जाती है (बिना ऊष्मा प्राप्त किये गर्म हो जाती है), जिससे सतह पर तापमान बढ़ जाता है।
- भौगोलिक स्थित: उत्तर-पश्चिमी भारत जैसे शुष्क या अर्ध-शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में गर्मी की लहरें अधिक बार आती हैं। गर्मियों के महीनों के दौरान प्रचलित पश्चिमी वायुएँ गर्मी की लहरों को पूर्व और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं।
- जलवायु परिवर्तन: ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्मी की लहरों की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है। बढ़ता आधारभूत तापमान इन घटनाओं के घटित होने के लिये अधिक अनुकूल वातावरण तैयार करता है।
हीटवेव के प्रभाव क्या हैं?
- स्वास्थ्य पर: गर्म लहरों के कारण निर्जलीकरण, तापजन्य ऐंठन (heat cramps), तापजन्य थकावट (heat exhaustion) और तापघात (heat stroke) हो सकता है।
- लक्षणों में सूजन, बेहोशी, बुखार, थकान, कमज़ोरी, चक्कर आना और अत्यधिक पसीना आना शामिल हैं। हीट स्ट्रोक से शरीर का तापमान बढ़ सकता है, भ्रम, दौरे या कोमा हो सकता है और यह घातक भी हो सकता है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में गर्मी से संबंधित कारणों से 730 मौतें हुईं।
- जल संसाधन पर प्रभाव:
- हीटवेव भारत में पानी की कमी के मुद्दों को बढ़ा सकती है, जल निकायों को सुखा सकती है, कृषि और घरेलू उपयोग के लिये पानी की उपलब्धता कम कर सकती है तथा जल संसाधनों हेतु प्रतिस्पर्द्धा बढ़ा सकती है।
- इससे जल को लेकर टकराव उत्पन्न हो सकता है, सिंचाई के तरीके प्रभावित हो सकते हैं और पानी पर निर्भर उद्योगों पर असर पड़ सकता है।
- उदाहरण: दक्षिणी राज्यों के अधिकांश प्रमुख जलाशय अपनी क्षमता के केवल 25% या उससे भी कम तक भरे हुए हैं।
- हीटवेव भारत में पानी की कमी के मुद्दों को बढ़ा सकती है, जल निकायों को सुखा सकती है, कृषि और घरेलू उपयोग के लिये पानी की उपलब्धता कम कर सकती है तथा जल संसाधनों हेतु प्रतिस्पर्द्धा बढ़ा सकती है।
- ऊर्जा पर प्रभाव:
- हीटवेव कूलिंग उद्देश्यों के लिये बिजली की मांग को बढ़ा सकती है, जिससे पावर ग्रिड पर दबाव पड़ सकता है और संभावित ब्लैकआउट की स्थिति हो सकती है।
- यह आर्थिक गतिविधियों को बाधित कर सकता है, उत्पादकता और उन कमज़ोर आबादी को प्रभावित कर सकता है, जिनके पास हीटवेव के दौरान बिजली तक पहुँच नहीं हो।
- फसलें और पशुधन: फसलें और पशुधन: ताप तनाव कृषि के लिये एक बड़ी समस्या है, जो फसलों तथा पशुधन दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।
- फसलों में, उच्च तापमान ऊर्जा के लिये सूर्य के प्रकाश का उपयोग करने की उनकी क्षमता में बाधा डालता है, जिससे वृद्धि और समग्र उपज कम हो जाती है।
- पशुओं के लिये ताप तनाव विभिन्न शारीरिक कार्यों और व्यवहारों को बाधित करता है, जिसकी गंभीरता पशु की नस्ल तथा पर्यावरण पर निर्भर करती है।
- वनाग्नि: भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India- FSI) ने अनुमान लगाया है कि वन के अंतर्गत 21.4% क्षेत्र वनाग्नि के प्रति संवेदनशील है।
हीटवेव के लिये NDMA दिशा-निर्देश:
- धूप में बाहर जाने से बचें, विशेषकर दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच।
- जितना संभव हो सके, पर्याप्त मात्रा में पानी पियें।
- हल्के, हल्के रंग के, ढीले और छिद्रयुक्त सूती कपड़े पहनें। धूप में बाहर जाते समय सुरक्षा चश्मा, छाता/टोपी, जूते या चप्पल पहनें।
- शराब, चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड शीतल पेय से बचें, जो शरीर से पानी को कम करते हैं।
- उच्च प्रोटीन वाले भोजन से बचें और बासी भोजन न खाएँ।
- ORS, घर में बने पेय पदार्थ जैसे लस्सी, तोरानी (चावल का पानी), नींबू पानी, छाछ आदि का प्रयोग करें जो शरीर को पुनः जलयुक्त बनाने में मदद करते हैं।
- पशुओं को छाया में रखें और उन्हें पीने के लिये पर्याप्त पानी दें।
- अपने घर को ठंडा रखें, पर्दे, शटर या सनशेड का प्रयोग करें और रात में खिड़कियाँ खोलें।
- पंखे का प्रयोग करें, गीले कपड़े पहनें और बार-बार ठंडे पानी से नहाएँ।
अधिसूचित आपदा के रूप में ताप तरंगों से संबंधित आवश्यकताएँ और चुनौतियाँ क्या हैं?
- अधिसूचित आपदाएँ:
- आपदा प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न होने वाली विनाशकारी घटना को कहते हैं। इस घटना के परिणामस्वरूप जान-माल की भारी हानि, संपत्ति की क्षति, पर्यावरण का क्षरण या इन सबका संयोजन होता है।
- अधिसूचित आपदा वह होती है जिसे सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई हो तथा जिसे सामान्यतः आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 जैसे कानूनी ढाँचे में परिभाषित किया गया हो।
- वित्तीय सहायता: अधिसूचित आपदा घोषित होने से प्रभावित क्षेत्र आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत स्थापित दो निधियों, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (National Disaster Response Fund- NDRF) और राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (State Disaster Response Fund- SDRF) से वित्तीय सहायता के लिये पात्र हो जाता है।
- DM अधिनियम में हीटवेव्स को जोड़ने की चुनौती:
- वित्त आयोग की अनिच्छा: वित्त आयोग हीटवेव को अधिसूचित आपदा के रूप में शामिल करने के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है।
- 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को SDRF निधि का 10% तक "स्थानीय आपदाओं" जैसे बिजली गिरने या लू लगने के लिये उपयोग करने की अनुमति दी है, जिसकी अधिसूचना राज्य स्वयं दे सकते हैं।
- विशाल वित्तीय निहितार्थ: सरकार को अधिसूचित आपदा के कारण होने वाली हर जान के लिये मौद्रिक मुआवज़ा (4 लाख रुपए) देना होगा। गर्मी से संबंधित मौतों की बड़ी संख्या को देखते हुए यह एक बहुत बड़ा बोझ हो सकता है।
- मृत्यु का अनुमान: अधिकतर मामलों में, गर्मी प्रत्यक्ष रूप से लोगों की मृत्यु का कारण नहीं बनती। उनकी मृत्यु पहले से मौजूद दूसरी बीमारियों के कारण होती है जो अत्यधिक गर्मी के कारण और भी बदतर हो जाती हैं, जिससे मृत्यु के सटीक कारण का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
- आपदा निधि की संभावित समाप्ति: यद्यपि SDRF और NDRF के लिये वित्तीय आवंटन पर्याप्त है किंतु यदि हीटवेव तथा तड़ित (Lightning) जैसी अन्य स्थानीय आपदाओं को अधिसूचित सूची में जोड़ दिया जाए तो यह अपर्याप्त हो सकता है।
- वित्त आयोग की अनिच्छा: वित्त आयोग हीटवेव को अधिसूचित आपदा के रूप में शामिल करने के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है।
- हीटवेव को प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित करने की आवश्यकता:
- संसाधन का बेहतर आवंटन: हीटवेव की अधिसूचित करने से शमन रणनीतियों, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और बेहतर स्वास्थ्य सेवा तैयारियों के लिये समर्पित निधि तथा संसाधन उपलब्ध होंगे।
- प्रभावी कार्य योजनाएँ: यह राज्यों को हीटवेव के लिये व्यापक एक्शन प्लान विकसित करने के लिये प्रोत्साहित करेगा जिसमें जन जागरूकता, शीतलन केंद्र और सुभेद्य वर्ग की सहायता के लिये स्पष्ट प्रोटोकॉल की रूपरेखा होगी।
- बढ़ती तीव्रता और आवृत्ति: हीटवेव की स्थिति आम और गंभीर होती जा रही हैं। IMD की रिपोर्ट के अनुसार समग्र देश में "हीटवेव डेज़" में वृद्धि हुई है। 23 ऐसे राज्य हैं जो हीटवेव के प्रति सुभेद्य हैं।
हीट एक्शन प्लान क्या है?
- हीट एक्शन प्लान (HAP) सरकारों या संगठनों द्वारा विकसित एक व्यापक रणनीति है जिसका उद्देश्य अत्यधिक गर्मी से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना है।
- इसमें सुभेद्य वर्ग की रक्षा करना, सूचना और संसाधन उपलब्ध कराना तथा हीटवेव के दौरान प्रतिक्रियाओं का समन्वय करने के उपाय शामिल हैं।
- ये मानव हताहतों को कम करने के लिये अलर्ट और अंतर-विभागीय समन्वय सहित अल्पकालिक उपायों की रूपरेखा तैयार करते हैं। HAP में डेटा विश्लेषण के आधार पर भविष्य की हीटवेव का सामना करने के लिये तत्पर रहने के लिये शीतल छतों और अधिक वनस्पति जैसे बुनियादी ढाँचे के उन्नयन जैसी दीर्घकालिक रणनीतियाँ शामिल हैं।
- ओडिशा में वर्ष 1998 में हीटवेव के कारण 2,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई जिसके बाद राज्य ने वर्ष 1999 में पहली बार हीट एक्शन प्लान विकसित किया। इसके बाद वर्ष 2010 में भीषण हीटवेव की घटना के बाद वर्ष 2013 में अहमदाबाद द्वारा पहली शहर-स्तरीय एक्शन प्लान विकसित किया गया।
- NDMA और IMD HAP के विकास के लिये 23 राज्यों के साथ कार्य कर रहे हैं। HAP पर कोई केंद्रीकृत डाटाबेस उपलब्ध नहीं है किंतु राज्य और शहर स्तर पर लगभग 23 HAP मौजूद हैं तथा ओडिशा तथा महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों ने ज़िला स्तर पर HAP तैयार किये हैं।
|
दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: ऊष्ण तरंगों की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता के उत्तरदायी कारकों तथा उनके प्रभाव को कम करने के लिये राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर किये जा सकने वाले उपायों पर चर्चा कीजिये। |
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. वर्तमान में और निकट भविष्य में भारत की ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में संभावित सीमाएँ क्या हैं? (2010)
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न. संसार के शहरी निवास-स्थानों में ताप द्वीपों के बनने के कारण बताइये। (2013) |