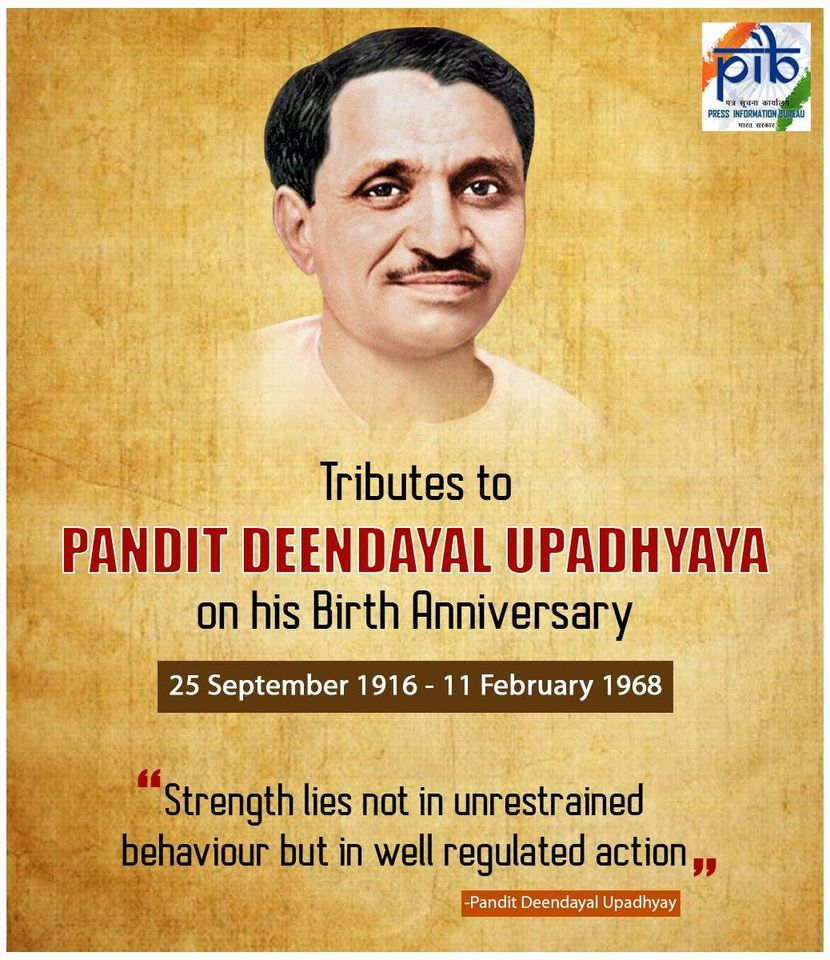प्रारंभिक परीक्षा
मृत्यु के बाद कोशिकीय कार्यक्षमता
स्रोत: इकोनाॅमिक टाइम्स
चर्चा में क्यों?
हालिया शोध में एक "तीसरी अवस्था" को प्रस्तावित किया गया है जिसमें जीवन और मृत्यु की पारंपरिक परिभाषाओं को चुनौती दी गई है, इसमें दर्शाया गया है कि कुछ कोशिकाएँ और ऊतक जीव की मृत्यु के बाद भी कार्य करना जारी रख सकते हैं, जिससे कोशिकीय क्षमताओं एवं जीव विज्ञान तथा चिकित्सा के लिये इसके निहितार्थों के बारे में नवीन प्रश्न उठते हैं।
प्रस्तावित 'तीसरी अवस्था' क्या है?
- परिचय: "तीसरी अवस्था" की अवधारणा ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है, जहाँ कोशिकाएँ और ऊतक ऐसी विशेषताएँ इंगित करते हैं जिससे जीवन एवं मृत्यु की पारंपरिक परिभाषाओं को चुनौती मिलती है। मृत्यु को जैविक कार्यों की पूर्ण समाप्ति के रूप में देखने के बजाय, इस शोध से संकेत मिलता है कि कुछ कोशिकाएँ जीव की मृत्यु के बाद भी कार्य और अनुकूलन करना जारी रख सकती हैं।
- मृत्यु के बाद कोशिकीय कार्यशीलता के उदाहरण:
- ज़ेनोबोट्स: मृत मेंढक भ्रूणों की त्वचा की कोशिकाओं में स्वतः ही नई बहुकोशिकीय संरचनाएँ बनती देखी गई हैं, जिन्हें ज़ेनोबोट्स के नाम से जाना जाता है।
- इन ज़ेनोबोट्स द्वारा अपने मूल जैविक कार्यों से परे व्यवहार प्रदर्शित किया गया तथा सिलिया (छोटे बाल जैसे उभार) का उपयोग नेविगेट करने एवं गति करने के लिये किया गया, जबकि जीवित मेंढक भ्रूणों में सिलिया का उपयोग म्यूकस को गति देने के लिये किया जाता है।
- ज़ेनोबोट्स में सेल्फ-रेप्लिकेशन हो सकता है, जिससे इनकी नवीन प्रतिकृति बन सकती हैं। यह प्रक्रिया परिचित रेप्लिकेशन विधियों से भिन्न है, जिसमें जीव के भीतर यह प्रक्रिया होती है।
- एन्थ्रोबॉट्स: अध्ययनों से पता चला है कि मानव फेफड़े की कोशिकाएँ स्वतः ही छोटे, बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण कर सकती हैं जिन्हें एन्थ्रोबॉट्स कहा जाता है।
- मानव श्वासनली (श्वसन तंत्र का एक भाग) कोशिकाओं से निर्मित ये जैव-रोबोट अद्वितीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जिससे वे गतिशील हो सकते हैं, स्वयं की मरम्मत कर सकते हैं तथा निकटवर्ती क्षतिग्रस्त न्यूरॉन कोशिकाओं को पुनर्स्थापित कर सकते हैं।
- तीसरी अवस्था के निहितार्थ: तीसरी अवस्था की धारणा जीवन और मृत्यु के पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित करती है तथा इससे सुझाव मिलता है कि जैविक प्रणालियाँ रैखिक जीवन चक्रों से बंधी हुई नहीं हो सकती हैं।
- मृत्यु के बाद कोशिकाओं की कार्यप्रणाली समझने से अंग संरक्षण और प्रत्यारोपण में सफलता मिल सकती है तथा दाता अंगों की व्यवहार्यता के साथ रोगी परिणामों में सुधार हो सकता है।
- ज़ेनोबोट्स: मृत मेंढक भ्रूणों की त्वचा की कोशिकाओं में स्वतः ही नई बहुकोशिकीय संरचनाएँ बनती देखी गई हैं, जिन्हें ज़ेनोबोट्स के नाम से जाना जाता है।
मृत्यु के बाद कोशिकाएँ किस प्रकार जीवित रहती हैं?
- कोशिकीय दीर्घायु: किसी जीव की मृत्यु के बाद विभिन्न कोशिकाओं की जीवित रहने की अवधि अलग-अलग होती है।
- श्वेत रक्त कोशिकाएँ: आमतौर पर मृत्यु के बाद 60 से 86 घंटों के अंदर नष्ट हो जाती हैं।
- कंकालीय मांसपेशी कोशिकाएँ: चूहों में इन्हें 14 दिनों तक पुनर्जीवित किया जा सकता है।
- फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएँ: भेड़ और बकरी की कोशिकाओं को मृत्यु के लगभग एक महीने बाद तक संवर्द्धित किया जा सकता है।
- प्रभावित करने वाले कारक: पर्यावरणीय परिस्थितियाँ (तापमान, ऑक्सीजन का स्तर), चयापचय गतिविधि, और क्रायोप्रिजर्वेशन (कम तापमान पर जैविक नमूनों को संग्रहीत करना) जैसी संरक्षण तकनीकें, मृत्यु के बाद कोशिकाओं और ऊतकों के अस्तित्व को प्रभावित करती हैं।
अधिक पढ़ें: हेफ्लिक सीमा
सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक, मानव शरीर में B कोशिकाओं और T कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है?(2022) (a) वे शरीर को पर्यावरणीय प्रत्यूर्जकों (एलर्जनों) से संरक्षित करती हैं। उत्तर: (d) |
प्रारंभिक परीक्षा
ब्रह्मांड में टेलीस्कोप
स्रोत: द हिंदू
चर्चा में क्यों?
चिली के अटाकामा रेगिस्तान में सेरो आर्माजोन्स पर्वत की चोटी पर एक एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप (ELT) का निर्माण कार्य चल रहा है।
टेलीस्कोप क्या हैं?
- परिचय: दूरबीन/टेलीस्कोप का उपयोग खगोलविद दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिये करते हैं।
- एपर्चर के आकार से यह निर्धारित होता है कि कितना प्रकाश एकत्र किया जा सकता है। एक छोटा परावर्तक दूरबीन (0.07 मीटर एपर्चर) मानव आँख की तुलना में 118.5 गुना अधिक प्रकाश एकत्र करता है।
- यह गलत धारणा है कि टेलीस्कोप को खगोलीय पिंडों को बड़ा दिखाने के लिये डिज़ाइन किया गया है। इसके बजाय इनका प्राथमिक कार्य आकाशीय पिंडों की स्पष्टता को बढ़ाना है, जिसे उनकी प्रकाश-एकत्रण क्षमता द्वारा मापा जाता है।
- दूरबीनों के प्रकार:
- परावर्तक दूरबीन: इसमें आने वाले प्रकाश को केंद्रित करने के लिये अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है जिससे वास्तविक, उल्टी और छोटी इमेज बनती हैं। अधिकांश आधुनिक दूरबीनें परावर्तक हैं, जिनमें इमेज को धुँधला होने से बचाने के लिये परवलयिक दर्पण होते हैं।
- अपवर्तक दूरबीन: अपवर्तक दूरबीन में दूर की वस्तुओं को बड़ा करके देखने के क्रम में प्रकाश को पुनर्निर्देशित करने हेतु लेंस एवं अपवर्तन का उपयोग किया जाता है।
- अपवर्तक दूरबीन में प्रैक्टिकेवल लेंस का अधिकतम आकार लगभग 1 मीटर होता है।
- विश्व का सबसे बड़ा अपवर्तक दूरबीन अमेरिका की यर्केस वेधशाला में है, जिसका लेंस 1.02 मीटर है।
- चमक मापना: अपारेंट मैग्नीटियूड द्वारा लघुगणकीय स्केल पर आकाशीय पिंडों की चमक को मापा जाता है।
- इसका निम्न मान अधिक चमकीली वस्तुओं का परिचायक है (उदाहरण के लिये सूर्य -26.78, शुक्र -4.92), जबकि उच्च मान, कम चमकीली वस्तुओं का परिचायक है (उदाहरण के लिये, एंड्रोमेडा आकाशगंगा +3.44)।
- दूरबीनों का रेज़ोल्यूशन: 20/20 दृष्टि वाली मानव आँख द्वारा 60 आर्कसेकेंड ( 1 आर्कसेकेंड = 1/3600 डिग्री ) जितने छोटे विवरण देखे जा सकते हैं।
- एक टॉय दूरबीन (जिसकी इष्टतम विभेदन क्षमता लगभग 1.47 आर्कसेकेण्ड होती है) द्वारा मानव आँख की तुलना में 40 गुना अधिक स्पष्टता से देखा जा सकता है।
- रेज़ोल्यूशन का आशय दूरबीनों द्वारा दो निकटवर्ती वस्तुओं के बीच सूक्ष्म विवरणों को पहचानने की क्षमता से है।
- सबसे बड़े और उन्नत दूरबीनों के उदाहरण:
- लार्ज बाईनोकुलर दूरबीन (LBT): यह अब तक की सबसे बड़ी दूरबीन है जिसमें 8.4 मीटर चौड़े दो दर्पण और 11.9 मीटर का प्रभावी संयुक्त एपर्चर है।
- यह अमेरिका के एरिजोना में माउंट ग्राहम अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला में है।
- एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप (ELT): इसका निर्माण यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के एक भाग के रूप में चिली के अटाकामा रेगिस्तान में सेरो आर्मजोन्स पर्वत के ऊपर किया जा रहा है।
- इसमें पाँच दर्पण हैं तथा इसका संयुक्त एपर्चर 39.3 मीटर है।
- सुबारू दूरबीन: यह 8.2 मीटर चौड़ी जापानी दूरबीन है जो हवाई के मौना की वेधशाला में स्थित है।
- लार्ज बाईनोकुलर दूरबीन (LBT): यह अब तक की सबसे बड़ी दूरबीन है जिसमें 8.4 मीटर चौड़े दो दर्पण और 11.9 मीटर का प्रभावी संयुक्त एपर्चर है।
- इंटरनेशनल लिक्विड-मिरर टेलीस्कोप: यह भारत और एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन है जो उत्तराखंड के देवस्थल में स्थित है। इसमें लिक्विड मरकरी की एक पतली परत से बना 4 मीटर व्यास का घूर्णित दर्पण है।
दूरबीनों को पहाड़ों पर ही क्यों स्थापित किया जाता है?
- पृथ्वी का वायुमंडल असंतुलित होने से तारों की रोशनी की स्पष्टता प्रभावित होती है तथा दूरबीन का रिज़ोल्यूशन कम हो जाता है।
- पहाड़ों जैसी ऊँची जगहों पर वायुमंडलीय असंतुलन कम होता है।
- हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसी अंतरिक्ष दूरबीनें इस प्रकार के असंतुलन से पूरी तरह बच जाती हैं जिससे जमीन पर स्थित दूरबीनों की तुलना में इनसे 10 गुना बेहतर रिज़ोल्यूशन मिलता है।
- हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने वायुमंडलीय उतार-चढ़ाव का विश्लेषण करने के लिये लेजर की मदद से कृत्रिम तारे निर्मित किये। एक उन्नत विधि (टोमोग्राफी) में स्पष्ट इमेज के लिये विचलन को समाप्त करने के क्रम में वायु सेगमेंट का परीक्षण किया जाता है।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिये: (2018)
उपर्युक्त में से एल्बर्ट आइंस्टीन के आपेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत का/के भविष्य कथन कौन सा/से है/हैं, जिसकी/जिनकी प्रायः समाचार माध्यमों में विवेचना होती है? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) प्रश्न. आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के संदर्भ में, हाल ही में समाचारों में रहे दक्षिण ध्रुव पर स्थित एक कण डिटेक्टर 'आइसक्यूब' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2015)
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) |
रैपिड फायर
रोबोटिक मल्टी-यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट
स्रोत: द हिंदू
हाल ही में भारतीय सेना ने अग्रिम (लड़ाकू) क्षेत्रों, विशेषकर उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में उपयोग के लिये 100 रोबोटिक मल्टी-यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट (MULE) को शामिल किया है।
- ये रोबोट -40 से +55 डिग्री सेल्सियस तक की कठोर जलवायु में काम करने, खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ने और 15 किलोग्राम का भार उठाने की क्षमता रखते हैं।
- इसके अलावा, उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में सहायता और परिवहन में सुधार के लिये लॉजिस्टिक्स ड्रोन का परीक्षण किया जा रहा है।
- रोबोटिक मल्टी-यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट एक सतत्, तीव्रता के साथ कार्य करने वाला ज़मीनी रोबोट है जिसे सभी मौसमों के लिये डिज़ाइन किया गया है, यह ऑब्जेक्ट की पहचान के लिये इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स और इन्फ्रारेड तकनीक से लैस है। यह नदियों के अंदर भी कार्य कर सकता है।
- इससे भारतीय सेना को मानव जीवन को जोखिम में डाले बिना निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने तथा अग्रिम पंक्ति के सैनिकों तक महत्त्वपूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
- MULE अभी भी उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में आपूर्ति वितरण के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, जो सेना के पशु परिवहन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं। सेना को उम्मीद है कि 2030 तक पशु परिवहन के उपयोग में 50-60% की कमी आएगी, हालाँकि यह कई सीमावर्ती क्षेत्रों के लिये आवश्यक है।
- चीन ने पहले ही अपने सैन्य अभियानों में रोबोट डॉग्स को शामिल कर लिया है, जो सैन्य क्षेत्रों में रोबोट की बढ़ती तैनाती और संभवतः एक नई हथियारों की दौड़ का संकेत है।
और पढ़ें: युद्ध क्षेत्र में रोबोट
रैपिड फायर
UAPA के तहत 14 दिन की समय-सीमा
स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत अभियोजन की मंजूरी देने के लिये 14 दिन की समय-सीमा अनिवार्य है , न कि विवेकाधीन।
- राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को इस समय-सीमा के तहत कार्य करना आवश्यक है।
- UAPA नियम 2008 में "करेगा (shall) " शब्द का प्रयोग किया गया है , जो निर्धारित 14 दिनों के अंदर मंजूरी प्रक्रिया को पूरा करने के स्पष्ट विधायी इरादे को दर्शाता है।
- इसमें स्वतंत्र समीक्षा (7 दिन) और सरकारी निर्णय (7 दिन) दोनों शामिल हैं।
- 14 दिन की समय-सीमा का पालन न करने पर गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं, जैसे आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना।
- यह निर्णय भावी रूप से लागू होगा, अर्थात यह पिछले मामलों को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन भविष्य में सभी मामलों में इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिये।
- इससे पहले बॉम्बे और झारखंड उच्च न्यायालयों ने 14 दिन की समय-सीमा को महज विवेकाधीन माना था।
- UAPA भारत सरकार के लिये आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है।
रैपिड फायर
भारत का मध्यस्थता अधिनियम
स्रोत: लाइव मिंट
मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के कार्यान्वयन में देरी से भारत का वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) ढाँचा प्रभावित हो रहा है।
- भारतीय मध्यस्थता परिषद के नियमों का मसौदा तैयार करने के लिये पीके मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली कार्य समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हालाँकि, सरकार ने अभी तक इन नियमों को अधिसूचित नहीं किया है।
- मध्यस्थता अधिनियम, 2023 का महत्त्व:
- न्यायिक कार्यभार में कमी: भारतीय न्यायालयों में लगभग 76.98 मिलियन सिविल विवाद मामले लंबित हैं। इनमें से वाणिज्यिक मुकदमों का हिस्सा 0.36% और मध्यस्थता का योगदान 0.77% है, जिन्हें मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के तहत निपटाया जा सकता है।
- पारिवारिक मामले: इससे "थर्ड जनरेशन कर्स (Third-Generation Curse)" को रोकने में मदद मिल सकती है , जहाँ विवादों के कारण 10% से भी कम पारिवारिक व्यवसाय तीसरी पीढ़ी से आगे तक संचालित रह पाते हैं।
- बैंकिंग: ऋण चूक और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) से संबंधित विवादों को सुलझाने में सहायक है।
- रियल एस्टेट क्षेत्र: परियोजना में देरी और क्रेता-डेवलपर अनुबंधों से संबंधित विवादों के त्वरित समाधान में सहायक है।
- वैश्विक मानकों के साथ तालमेल: इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मानकों के साथ समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी , जो सीमा-पार व्यापार विवादों को सुलझाने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
और पढ़ें: मध्यस्थता अधिनियम, 2023: न्यायपालिका का कार्यभार कम करना
रैपिड फायर
NRI कोटा और शिक्षा
स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स
हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार के उस निर्णय की निंदा की जिसमें उसने मेडिकल कॉलेजों में अनिवासी भारतीयों (NRI) कोटा (15%) को बढ़ाकर , उनके दूर के रिश्तेदारों जैसे चाचा, चाची और चचेरे भाई-बहनों को भी इसमें शामिल करने का निर्णय लिया था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने NRI कोटे के विस्तार को एक “धोखाधड़ी” बताया, जो योग्यता-आधारित प्रवेश को कमज़ोर करता है तथा इसे एक “पैसा कमाने की रणनीति” कहा, जो कम योग्य उम्मीदवारों को योग्यता के बजाय धन और संबंधों के आधार पर प्रवेश पाने की अनुमति प्रदान कर सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले, 2005 का संदर्भ दिया, जिसमें NRI कोटे के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था ।
- हालाँकि, NRI उम्मीदवारों की इसी प्रकार की व्यापक परिभाषा हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में भी अपनाई गई थी ।
- NRI कोटा NRI, PIO और OCI को प्रवेश पाने की अनुमति प्रदान करता है, अक्सर इसके लिये निवासियों को प्रवेश परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती है।
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTI) NRI छात्रों को तकनीकी संस्थानों में 5% तक प्रवेश की अनुमति प्रदान करता है, जबकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार यह सीमा मेडिकल संस्थानों में 15% है।
- NRI से तात्पर्य ऐसे भारतीय नागरिक से है जो एक वित्तीय वर्ष में 182 दिन भारत से बाहर रहता है ।
और पढ़ें: भारत के विदेशी नागरिकों के अधिकार
रैपिड फायर
अंत्योदय दिवस 2024
स्रोत: IE
25 सितंबर, 2024 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में अंत्योदय दिवस मनाया गया।
- यह दिवस उनके जीवन और योगदान की स्मृति तथा भारतीय राजनीति एवं समाज पर उनके प्रभाव को प्रमुखता से दर्शाने हेतु मनाया जाता है।
- योगदान: उन्होंने अंत्योदय पर ध्यान केंद्रित किया जिसका अर्थ है समाज में वंचित/उपेक्षित व्यक्ति का उत्थान और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना।
- उनका "एकात्म मानववाद" का दर्शन व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता तथा आत्मनिर्भरता पर केंद्रित था।
- वह भारतीय जनसंघ (BJS) के सह-संस्थापक थे, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) के रूप में विकसित हुआ।
- वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के भी एक प्रमुख विचारक थे।
- मान्यता: 25 सितंबर, 2014 से उनकी जयंती को राष्ट्र के प्रति उनके प्रयासों और योगदान को मान्यता देने के लिये अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- वर्ष 2015 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना-NRLM कर दिया गया।
- वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के मुगलसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। वर्ष 1968 में मुगलसराय के निकट ही उनकी मृत्यु हो गई थी।