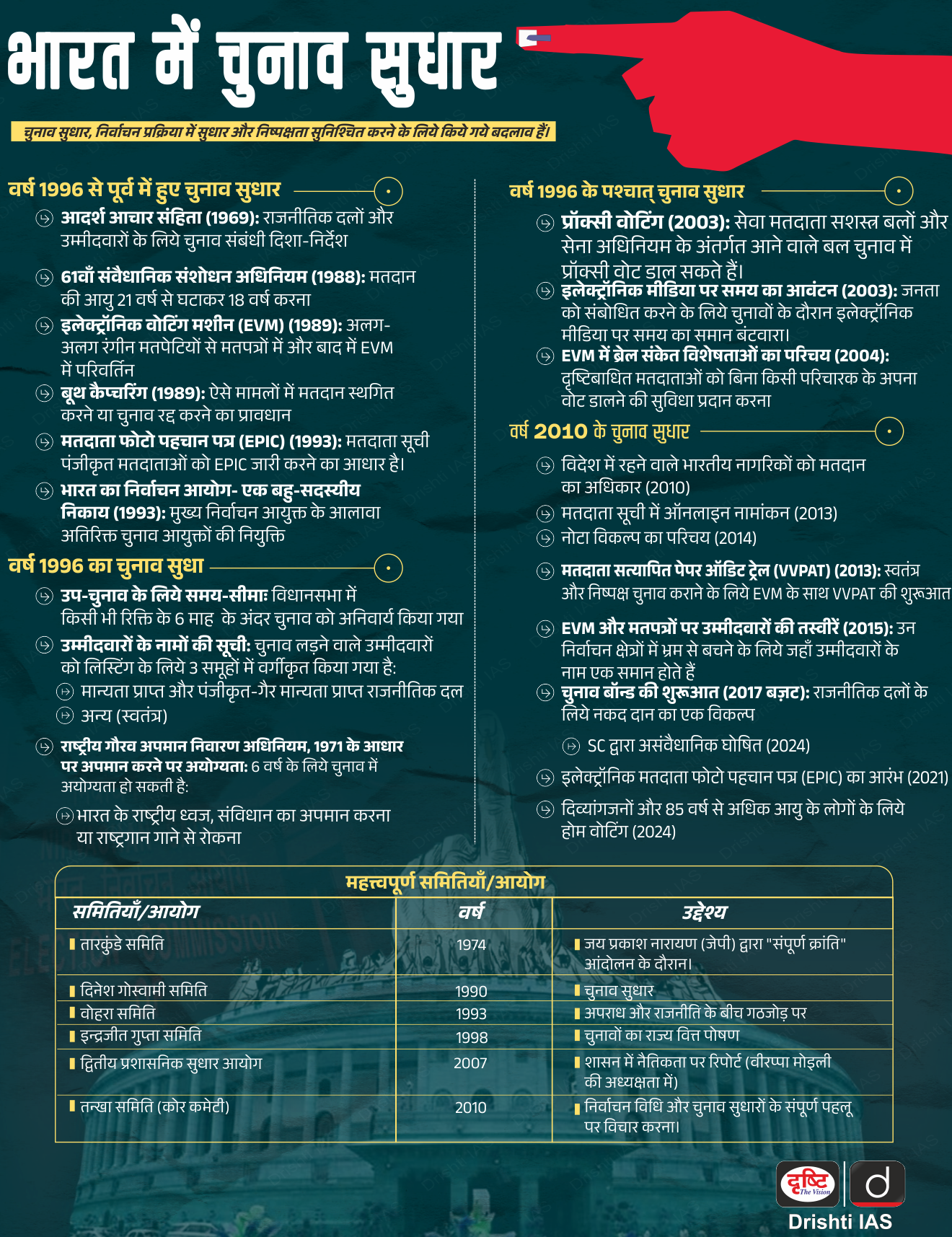प्रारंभिक परीक्षा
प्रोजेक्ट अस्मिता
स्रोत: द हिंदू
हाल ही में, आगामी पाँच वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करने के लिये अनुवाद और अकादमिक लेखन के माध्यम से भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री का संवर्द्धन (Augmenting Study Materials in Indian languages through Translation and Academic Writing- ASMITA) परियोजना शुरू की गई।
- यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के अनुरूप शिक्षा प्रणाली में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा की गई कई पहलों में से एक है।
प्रोजेक्ट अस्मिता क्या है?
- परिचय:
- इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा लॉन्च किया गया था।
- यह शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिये UGC और भारतीय भाषा समिति द्वारा किया गया संयुक्त प्रयास है।
- विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण तथा रखरखाव के लिये UGC की स्थापना वर्ष 1953 में की गई थी (वर्ष 1956 में सांविधिक संगठन बना)।
- भारतीय भाषा समिति वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार के लिये आधारभूत समिति है।
- इस परियोजना का नेतृत्व करने के लिये विभिन्न क्षेत्रों के सदस्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ 13 नोडल विश्वविद्यालयों की पहचान की गई है।
- UGC ने प्रत्येक निर्दिष्ट भाषा में पुस्तक-लेखन प्रक्रिया के लिये एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाई है।
- इस परियोजना का लक्ष्य पाँच वर्षों के भीतर 22 भाषाओं में 1,000 पुस्तकें तैयार करना है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार होंगी।
- इसके अतिरिक्त आयोग का लक्ष्य जून 2025 तक कला, विज्ञान और वाणिज्य स्ट्रीम पर आधारित 1,800 पाठ्यपुस्तकें तैयार करना है।
- प्रोजेक्ट अस्मिता के साथ शुरू की गई अन्य पहलें:
- बहुभाषा शब्दकोष:
- केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (Central Institute of Indian Languages) द्वारा भारतीय भाषा समिति के सहयोग से विकसित यह एक व्यापक बहुभाषी शब्दकोश संग्रह है।
- इससे आईटी, उद्योग, अनुसंधान और शिक्षा जैसे विभिन्न आधुनिक क्षेत्रों में भारतीय शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों का उपयोग करने में मदद मिलेगी।
- रीयल-टाइम अनुवाद वास्तुकला:
- राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम (National Educational Technology Forum) और भारतीय भाषा समिति द्वारा विकसित, इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में रीयल-टाइम अनुवाद को बढ़ाने के लिये एक रूपरेखा बनाना है।
- NETF की परिकल्पना एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई है, जिसे एक सोसायटी के रूप में शामिल किया गया है, जो NEP उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रौद्योगिकी की तैनाती, प्रेरण और उपयोग पर निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करेगा।
- राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम (National Educational Technology Forum) और भारतीय भाषा समिति द्वारा विकसित, इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में रीयल-टाइम अनुवाद को बढ़ाने के लिये एक रूपरेखा बनाना है।
- बहुभाषा शब्दकोष:
- उद्देश्य:
- इससे 22 अनुसूचित भाषाओं में शैक्षणिक संसाधनों का एक व्यापक पूल बनाने, भाषाई विभाजन को पाटने, सामाजिक सामंजस्य और एकता को बढ़ावा देने तथा देश के युवाओं को सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार वैश्विक नागरिकों में बदलने में मदद मिलेगी।
नोट:
- भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएँ शामिल हैं:
- असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।
और पढ़ें: राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत भाषाओं में चार भाषाओं को जोड़ा गया, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? (2008) (a) 90वाँ संविधान संशोधन उत्तर: (c) प्रश्न. निम्नलिखित में से किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? (2015) (a) उड़िया उत्तर: (a) |
प्रारंभिक परीक्षा
असम में विदेशी अधिकरण
स्रोत: द हिंदू
हाल ही में असम सरकार ने राज्य पुलिस की सीमा विंग से कहा कि वह वर्ष 2014 से पहले अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों के मामलों को विदेशी अधिकरणों (Foreigners Tribunal- FT) को अग्रेषित न करें।
- यह नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के अनुरूप था, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से उत्पीड़न के कारण प्रवास करने वाले हिंदु, सिख, ईसाई, पारसी, जैन तथा बौद्ध धर्म के व्यक्तियों के लिये नागरिकता का आवेदन करने का अवसर प्रदान करता है।
विदेशी अधिकरण (FT) से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं?
- परिचय:
- विदेशी अधिकरण (FT) अर्द्ध-न्यायिक निकाय होते हैं, जिनका गठन केंद्र सरकार द्वारा विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3 के अंतर्गत विदेशी विषयक (अधिकरण) आदेश, 1964 के माध्यम से किया गया है जिसका उद्देश्य किसी राज्य में स्थानीय प्राधिकारियों को किसी संदिग्ध विदेशी व्यक्ति को अधिकरण के पास भेजने की अनुमति प्रदान करना है।
- विदेशी विषयक (अधिकरण) आदेश (2019 संशोधन): मूल आदेश में वर्ष 2019 में किया गया संशोधन केवल यह रूपरेखा प्रदान करता है कि अधिकरण उन व्यक्तियों की अपीलों पर किस प्रकार निर्णय लेंगे जो NRC के लिये दायर अपने दावों और आक्षेपों के परिणाम से तुष्ट नहीं हैं।
- गृह मंत्रालय (MHA) ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ज़िला मजिस्ट्रेटों को अधिकरण स्थापित करने का अधिकार भी प्रदान किया है।
- ये सभी आदेश संपूर्ण देश में क्रियान्वित हैं और राज्य विशिष्ट नहीं हैं।
- हालाँकि इस आदेश के तहत विदेशी अधिकरण केवल असम में स्थापित किये गए हैं और देश के किसी अन्य राज्य में नहीं तथा इस प्रकार यह संशोधन वर्तमान में केवल असम के लिये प्रासंगिक प्रतीत होता है।
- इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों में "अवैध अप्रवासियों" के मामलों पर निर्णय विदेशियों विषयक अधिनियम के अनुसार लिया जाता है।
- मामलों के प्रकार: FT को दो प्रकार के मामले प्राप्त होते हैं:
- जिनके लिये सीमा पुलिस द्वारा “संदर्भ” दिया गया है।
- जिनके नाम मतदाता सूची में D [Doubtful (शंकास्पद)] मतदाता के रूप में दर्ज है।
- ‘D’ अथवा शंकास्पद मतदाताओं के मामलों को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा भी FT को भेजा जा सकता है।
- संरचना:
- प्रत्येक FT की अध्यक्षता न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और न्यायिक अनुभव वाले सिविल सेवकों में से चुने गए सदस्यों द्वारा की जाती है।
- न्यायाधीशों/अधिवक्ताओं को समय-समय पर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विदेशी अधिकरण अधिनियम, 1941 और विदेशी विषयक अधिकरण आदेश, 1964 के तहत FT के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है।
- प्रकार्य:
- 1964 के आदेश के अनुसार, FT के पास कुछ विशिष्ट मामलों में सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं जिनमें किसी व्यक्ति को बुलाए जाने और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने, शपथ पर उसका परीक्षण करने तथा किसी आवश्यक दस्तावेज़ को पेश करवाए जाने, जैसी शक्तियाँ शामिल हैं।
- अधिकरण को संबंधित प्राधिकारी से संदर्भ प्राप्त करने के 10 दिनों के भीतर विदेशी होने के अभियुक्त व्यक्ति को अंग्रेज़ी या राज्य की आधिकारिक भाषा में नोटिस देना आवश्यक है।
- FT को संदर्भ के 60 दिनों के भीतर मामले का निपटारा करना होता है।
- विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 9 के अनुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में किसी बात के होते हुए भी यह साबित करने का भार कि संबद्ध व्यक्ति विदेशी है या नहीं, उसी व्यक्ति पर होगा।
- यदि व्यक्ति नागरिकता का कोई सबूत देने में विफल रहता है तो FT उसे बाद में निर्वासन के लिये डिटेंशन सेंटर, जिसे अब ट्रांज़िट कैंप कहा जाता है, में भेज सकता है।
- विदेशी अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील:
- संबद्ध व्यक्ति द्वारा समीक्षा आवेदन आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर दायर किया जा सकता है और FT मामले का गुण-दोष के आधार पर निर्णय करेगा।
- FT द्वारा प्रतिकूल आदेश दिये जाने की स्थिति में उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है और उसके पश्चात् सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील दायर की जा सकती है।
अधिकरणों से संबंधित सांविधानिक प्रावधान
- इसे 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा शामिल किया गया था।
- अनुच्छेद 323-A प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है।
- अनुच्छेद 323-B अन्य मामलों के लिये अधिकरणों से संबंधित है।
असम की सीमा पुलिस की क्या भूमिका है?
- असम पुलिस सीमा संगठन की स्थापना वर्ष 1962 में पाकिस्तानी घुसपैठ की रोकथाम (PIP) योजना के तहत राज्य पुलिस की विशेष शाखा के एक हिस्से के रूप में की गई थी।
- इस संगठन को वर्ष 1974 में एक स्वतंत्र इकाई बना दिया गया।
- इस इकाई के सदस्यों को अवैध विदेशियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने तथा सीमा सुरक्षा बल के साथ भारत-बांग्लादेश सीमा पर गश्त करने का कार्य सौंपा गया है।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2009)
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. “केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसकी स्थापना केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा या उनके विरुद्ध शिकायतों एवं परिवादों के निवारण हेतु की गई थी, आजकल एक स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है।” व्याख्या कीजिये (2019) |
रैपिड फायर
जैविक उत्पादों हेतु पारस्परिक समझौता
स्रोत: पी.आई.बी.
हाल ही में भारत और ताइवान ने जैविक उत्पादों के लिये पारस्परिक मान्यता समझौते (Mutual Recognition Agreement- MRA) का कार्यान्वन किया।
- यह समझौता दोनों देशों के लिये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि यह जैविक उत्पादों के लिये पहला द्विपक्षीय समझौता है।
- MRA के लिये कार्यान्वयन अभिकरण भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority- APEDA) और ताइवान के कृषि मंत्रालय के तहत कृषि एवं खाद्य एजेंसी (AFA) हैं।
- पारस्परिक मान्यता से दोहरे प्रमाणन से बचने, अनुपालन लागत को कम करने, अनुपालन आवश्यकताओं को सरल बनाने और जैविक क्षेत्र में व्यापार के अवसरों को बढ़ाकर जैविक उत्पाद निर्यात को सुगम बनाया जा सकेगा।
- MRA प्रमुख भारतीय जैविक उत्पादों, जैसे चावल, प्रसंस्कृत खाद्य, हरी/काली और हर्बल चाय, औषधीय पौधों के उत्पादों आदि का ताइवान में निर्यात का मार्ग प्रशस्त करेगा।
भारत में जैविक उत्पादों हेतु योजनाएँ:
- इंडियन ऑर्गेनिक लोगो।
- पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया।
- राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP)।
और पढ़ें: भारत और ताइवान
रैपिड फायर
भारत-मलेशिया कृषि संबंध
स्रोत: पी.आई.बी.
हाल ही में भारत और मलेशिया ने कृषि में अपने द्विपक्षीय सहयोग को मज़बूत करने का निर्णय लिया है, जिसमें पाम ऑयल की खेती तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा।
- सहयोग के क्षेत्र: खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन- ऑयल पाम (NMEO-OP) को आगे बढ़ाने के लिये सहयोग पर चर्चा की गई। कृषि और संबद्ध उत्पादों के लिये बाज़ार पहुँच के मुद्दों पर चर्चा की गई।
- खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन- ऑयल पाम (NMEO-OP), वित्तीय वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम की खेती और कच्चे पाम तेल के उत्पादन को 11.20 लाख टन तक बढ़ाने के लिये वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया। यह 15 राज्यों में संचालित है, जिसका लक्ष्य 21.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है।
- ऑयल पाम मिशन का उद्देश्य किसानों को रोपण सामग्री, बायबैक आश्वासन और व्यवहार्यता अंतर भुगतान के माध्यम से वैश्विक मूल्य अस्थिरता से सुरक्षा प्रदान करके नए क्षेत्रों में ऑयल पाम को बढ़ावा देना है।
- भारत अपने खाद्य तेल का 57% आयात करता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर 20.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रभाव पड़ता है। भारत प्रत्येक वर्ष पाम तेल का आयात करता है, जो कुल खाद्य तेल आयात का लगभग 56% है।
- वर्तमान में लगभग 28 लाख हेक्टेयर के कुल संभावित क्षेत्र के मुकाबले, केवल 3.70 लाख हेक्टेयर में पाम तेल की खेती की जाती है।
- आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल प्रमुख तेल पाम उत्पादक राज्य हैं एवं कुल उत्पादन का 98% भाग उत्पादित करते हैं।
रैपिड फायर
EVM के माइक्रोकंट्रोलर्स का सत्यापन करेगा ECI
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India-ECI) ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) प्रणालियों की बर्न मेमोरी (या माइक्रोकंट्रोलर्स) के सत्यापन के लिये मानक संचालन प्रक्रिया ( Standard Operating Procedure- SOP) जारी की है।
- एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत निर्वाचन आयोग वाद, 2024 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद, निर्वाचन आयोग ने दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के लिखित अनुरोध पर विधानसभा तथा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 5% तक EVM और VVPAT माइक्रोकंट्रोलरों के सत्यापन की अनुमति दी है।
- प्रत्येक मशीन पर 1,400 वोट तक का मॉक पोल आयोजित किया जाएगा और यदि परिणाम VVPAT पर्चियों के साथ सुमेलित होते हैं, तो यह संकेत देगा कि बर्न मेमोरी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है तथा उन्हें सत्यापित माना जाएगा।
- हालाँकि विसंगतियों से निपटने की प्रक्रिया अभी भी अनिश्चित है।
- तकनीकी SOP इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाने वाली दो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (PSUs)- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा तैयार की गई थी।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM):
- इसमें 2 भाग होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट (CU) और एक बैलट यूनिट (BU)।
- बैलट यूनिट (BU) मतदाताओं को अपना वोट डालने की अनुमति देती है और उम्मीदवारों तथा उनसे संबंधित प्रतीकों को दर्शाती है, जबकि कंट्रोल यूनिट (CU) बैलट यूनिट का प्रबंधन करती है व डेटा को प्रोसेस करती है।
- पहली बार EVM का उपयोग वर्ष 1982 में केरल के पारवूर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में किया गया था।
और पढ़ें: सर्वोच्च न्यायालय ने EVM तथा VVPAT प्रणाली को सही ठहराया