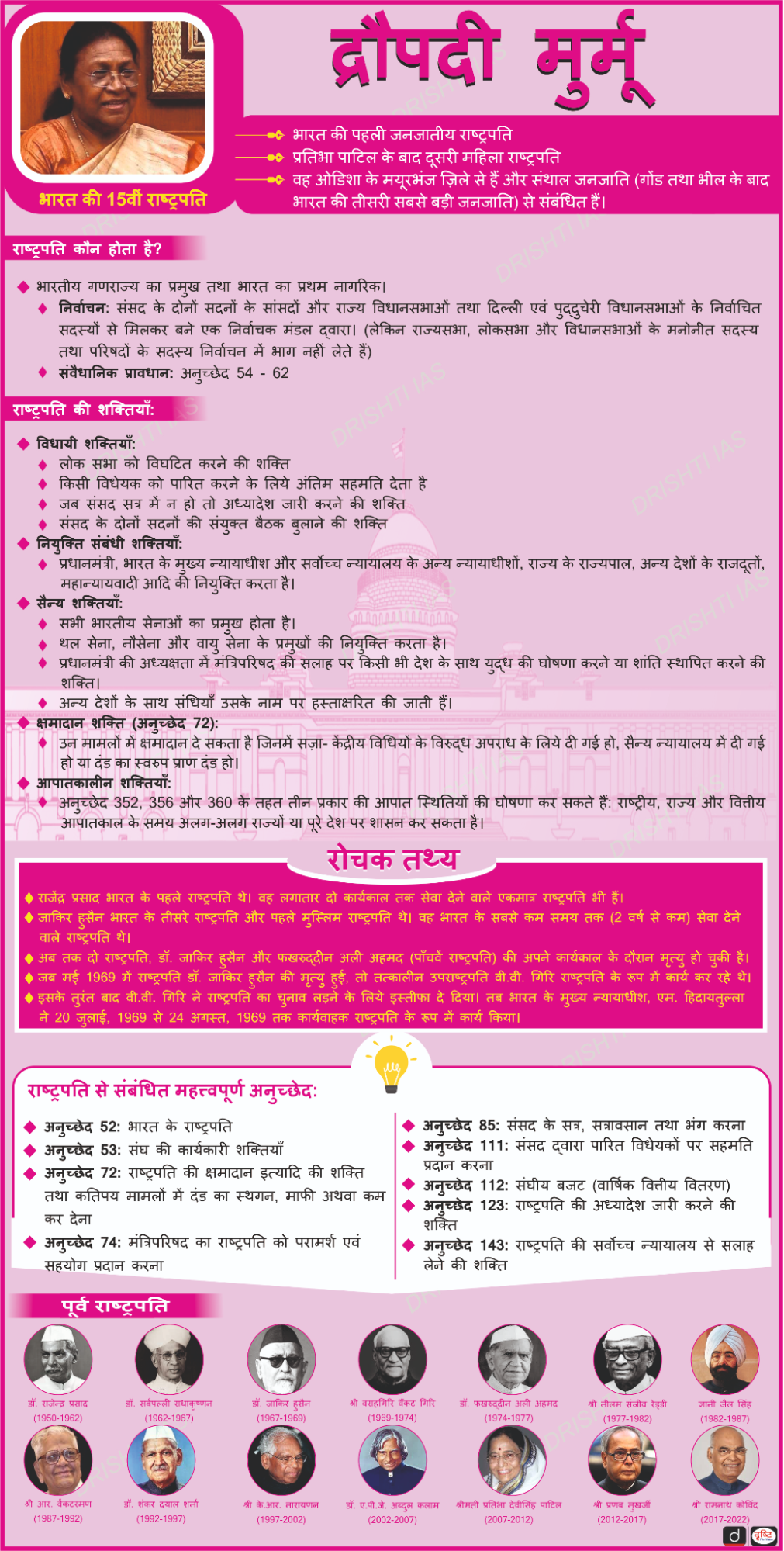भारतीय राजव्यवस्था
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति के निर्णय हेतु समय-सीमा का निर्धारण
- 14 Apr 2025
- 16 min read
प्रिलिम्स के लिये:भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति, राज्यपाल मेन्स के लिये:भारतीय संघवाद में राष्ट्रपति और राज्यपालों की भूमिका, राज्य विधेयकों और राष्ट्रपति की स्वीकृति के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियाँ |
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
चर्चा में क्यों?
भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल, 2023 में पहली बार संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने हेतु राष्ट्रपति के लिये 3 तीन माह की समय-सीमा का निर्धारण किया।
राज्य विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति की भूमिका पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या है?
- अनुच्छेद 201: इसमें कहा गया है कि "जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिये आरक्षित किया जाता है, तो राष्ट्रपति या तो विधेयक पर अनुमति देगा या उस पर अनुमति नहीं देगा।"
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति की मंज़ूरी के लिये कोई विशिष्ट समयसीमा नहीं दी गई है और इस तरह की देरी से विधायी प्रक्रियाओं में बाधा आ सकती है जिससे राज्य विधेयक "अनिश्चितकालीन तक स्थगित" हो सकते हैं।
- इसके द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि निष्क्रियता सत्ता के प्रयोग में मनमानी न करने के संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन है।
- समय-सीमा: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति अनिश्चितकाल तक विलंब करके "पूर्ण वीटो" का प्रयोग नहीं कर सकते। उन्हें तीन माह के अंदर निर्णय लेना होगा और किसी भी प्रकार के विलंब के बारे में उचित कारणों सहित राज्य को सूचित करना होगा।
- स्वीकृति रोकने का निर्णय ठोस एवं विशिष्ट आधारों पर होना चाहिये, यह निर्णय मनमाने ढंग से नहीं लिया जा सकता।
- यदि राष्ट्रपति निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही नहीं करते, तो राज्य निर्णय के लिये रिट याचिका दायर कर सकते हैं और कोर्ट से परमादेश (Mandamus) की मांग कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, यदि राज्यपाल किसी विधेयक को असंवैधानिकता के आधार पर आरक्षित करते हैं, तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेनी चाहिये।
- हालाँकि यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल, यदि किसी राज्य विधेयक को पुनः पारित कर दिया जाये, तो उसे स्वीकृति देना अनिवार्य होता है। परंतु राष्ट्रपति पर ऐसा कोई संवैधानिक बंधन नहीं है, जैसा कि अनुच्छेद 201 के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है।
- इसका कारण यह है कि अनुच्छेद 201 केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में लागू होता है, जब किसी राज्य विधान का राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है।
- संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में जारी कार्यालय ज्ञापनों (Office Memorandums) का उल्लेख किया, जिसमें राष्ट्रपति के पास आरक्षित राज्य विधेयकों पर निर्णय लेने हेतु तीन माह की समयसीमा निर्धारित की गई थी।
- न्यायालय ने सरकारिया आयोग (वर्ष 1988) और पुंछी आयोग (वर्ष 2010) की सिफारिशों का भी हवाला दिया, जिनमें दोनों ने आरक्षित विधेयकों पर समयबद्ध निर्णय लिये जाने की सिफारिश की थी।
राज्य विधेयक पारित करने में राज्यपाल की क्या भूमिका है?
और पढ़ें... राज्य विधेयकों में राज्यपालों की भूमिका
राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच संवैधानिक और कार्यात्मक अंतर क्या हैं?
|
कार्यक्षेत्र |
राष्ट्रपति |
राज्यपाल |
|
विधायी शक्तियाँ |
|
|
|
अध्यादेश बनाने की शक्ति |
|
|
|
क्षमादान की शक्ति |
|
|
|
आपातकालीन शक्तियाँ |
|
|
|
राजनयिक और सैन्य भूमिकाएँ |
|
|
|
विवेकाधीन शक्तियाँ |
|
|
राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय क्या हैं?
राष्ट्रपति:
- एस.आर.बोम्मई बनाम भारत संघ (1994): सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा के अधीन है और इसे मनमाने ढंग से नहीं लागू किया जा सकता है।
- केहर सिंह बनाम भारत संघ (1988): सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है।
- हालाँकि, प्रक्रियागत निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये इसकी समीक्षा की जा सकती है, जिसमें निर्णय के गुण-दोष के स्थान पर संवैधानिक सिद्धांतों और प्रक्रियागत आवश्यकताओं के पालन पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।
- केहर सिंह बनाम भारत संघ (1988): सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है।
- आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ (1970): सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अध्यादेश की आवश्यकता के संबंध में राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है और उसे चुनौती दी जा सकती है।
- इसने यह भी निर्णय दिया कि अध्यादेश भी संसद के अधिनियम के समान ही संवैधानिक सीमाओं के अधीन है तथा यह किसी भी मूल अधिकार या संविधान के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता।
राज्यपाल:
- एस.आर.बोम्मई बनाम भारत संघ (1994): सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति शासन के लिये राज्यपाल की सिफारिश न्यायिक समीक्षा के अधीन है और इसे मनमाने ढंग से लागू नहीं किया जा सकता।
- शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974): सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिये, सिवाय उन परिस्थितियों के जहाँ संविधान राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करने की अपेक्षा करता है।
- रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006): सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा के विघटन को असंवैधानिक घोषित किया तथा इस बात पर बल दिया कि राज्यपाल की शक्तियाँ निरपेक्ष नहीं हैं तथा उनका प्रयोग संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप ही किया जाना चाहिये।
- इस निर्णय ने कार्यकारी कार्यों की निगरानी में न्यायिक समीक्षा के महत्त्व को पुनः रेखांकित किया।
निष्कर्ष
अनुच्छेद 201 पर सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या राष्ट्रपति के लिये राज्य विधेयकों पर कार्रवाई करने हेतु तीन माह की स्पष्ट समयसीमा निर्धारित करती है, जिससे जवाबदेही बढ़ेगी और मनमाने विलंब की रोकथाम होगी। इस निर्णय से राज्यों को अनुचित विलंब पर आक्षेप करने का प्राधिकार प्रदान कर संघीय शासन का सुदृढ़ीकरण होगा। इससे विधायी प्रक्रिया में कार्यपालिका की शक्तियों के दुरुपयोग के खिलाफ पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
|
दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. राज्य विधेयकों में राष्ट्रपति की भूमिका पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के महत्त्व की विवेचना कीजिये। यह निर्णय गैर-स्वेच्छाचारिता के संवैधानिक सिद्धांत के साथ किस प्रकार सुमेलित होती है? |
और पढ़ें: राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. प्निम्नलिखित में से कौन-सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ हैं? (2014)
नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) प्रश्न. निम्नलिखित में कौन-सी लोकसभा की अनन्य शक्ति(याँ) है/हैं? (2020)
नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) 1 और 2 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग के लिये आवश्यक शर्तों की चर्चा कीजिये। राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों को विधायिका के समक्ष रखे बिना पुन: प्रख्यापित करने की वैधता पर चर्चा कीजिये। (2022) प्रश्न. यद्यपि परिसंघीय सिद्धांत हमारे संविधान में प्रबल है और वह सिद्धांत संविधान के आधारिक अभिलक्षणों में से एक है, परंतु यह भी इतना ही सत्य है कि भारतीय संविधान के अधीन परिसंघवाद (फैडरलिज्म) सशक्त केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। यह एक ऐसा लक्षण है जो प्रबल परिसंघवाद की संकल्पना के विरोध में है। चर्चा कीजिये। (2014) |