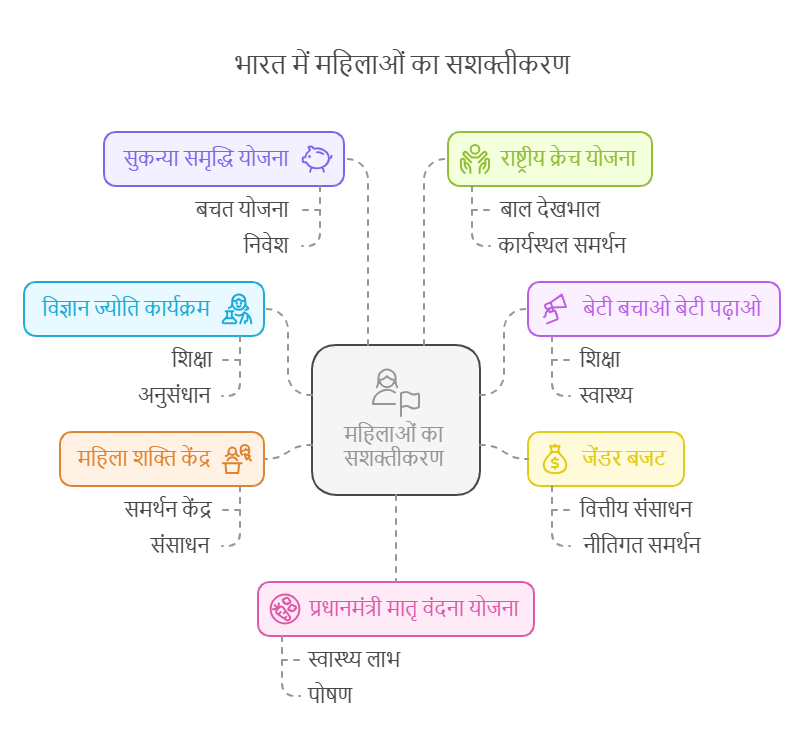सामाजिक न्याय
भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका
यह एडिटोरियल 10/05/2025 को बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित “Closing the gender gap: India still has miles to go in growth story” पर आधारित है। इस लेख में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में 41.7% की तीव्र वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया गया है, फिर भी अवैतनिक घरेलू काम, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक दृष्टिकोण में लगातार लैंगिक अंतराल बना हुआ है जो उनकी पूर्ण आर्थिक क्षमता में बाधा डालते हैं।
|
यद्यपि भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदारी में 6 वर्षों में 23.2% से 41.7% तक की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, फिर भी यह 77.2% की पुरुष दर और 50% के वैश्विक औसत से पीछे है। बढ़ती कार्यबल भागीदारी के बावजूद महिलाओं में असमान रूप से अवैतनिक घरेलू काम करना जारी है, जिससे दोहरा बोझ उत्पन्न होता है। हालाँकि महिला उद्यमिता और वित्तीय समावेशन बढ़ रहा है, फिर भी 18वीं लोकसभा में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व केवल 13.6% है। भारत को महिलाओं की पूरी आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने और राष्ट्रीय विकास को गति देने के लिये संरचनात्मक असमानताओं, सुरक्षा चिंताओं एवं सामाजिक धारणाओं को तत्काल दूर करने की आवश्यकता है।
भारत के आर्थिक परिवर्तन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं?
- शैक्षिक उन्नति और STEM समावेशन: महिलाओं के बीच बढ़ती शैक्षिक उपलब्धि कुशल क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण रही है।
- महिलाएँ तेज़ी से STEM क्षेत्रों में प्रवेश कर रही हैं, पारंपरिक रूढ़ियों को चुनौती दे रही हैं और उच्च वेतन वाली, नवाचार-संचालित नौकरियों तक पहुँच प्राप्त कर रही हैं।
- इससे आकांक्षाओं, कौशल निर्माण और कार्यबल तत्परता का एक अच्छा चक्र निर्मित हुआ है।
- डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्मों और छात्रवृत्तियों तक पहुँच ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अवसरों को लोकतांत्रिक बना दिया है।
- उदाहरण के लिये, उच्च शिक्षा में महिला नामांकन सत्र 2021-22 में बढ़कर 2.07 करोड़ हो गया, जो कुल नामांकन का लगभग 50% है।
- STEM छात्रों में महिलाओं की संख्या (AISHE, 2022) 42.57% है।
- महिला-नेतृत्व वाले विकास के लिये नीतिगत प्रयास: महिला कल्याण से महिला-नेतृत्व वाले विकास की ओर उद्देश्यपूर्ण किया गया बदलाव सभी मंत्रालयों की नीतियों में परिलक्षित होता है।
- पहलों को न केवल महिलाओं को शामिल करने के लिये डिज़ाइन किया गया है, बल्कि उन्हें नेता, उद्यमी और निर्णयकर्त्ता के रूप में सक्षम बनाने के लिये भी तैयार किया गया है। ये नीतियाँ ग्रामीण, जनजातीय और कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों को लक्षित करते हुए तेज़ी से अंतर-विभाजक बन रही हैं। अंतर-मंत्रालयी समन्वय ने प्रणालीगत चुनौतियों से अधिक सुसंगत तरीके से निपटना शुरू कर दिया है।
- उदाहरण के लिये, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10 करोड़ महिलाएँ 9 मिलियन SHG से जुड़ी हैं। स्टैंड-अप इंडिया ऋण का 84% महिलाओं को जाता है (PIB, 2024)।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-G के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है कि मकान का आवंटन महिला के नाम पर अथवा पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जाएगा।
- महिला उद्यमिता और स्टार्ट-अप संस्कृति का उदय: महिलाएँ नौकरी के अभ्यर्थियों से रोज़गार सृजक के रूप में परिवर्तित हो रही हैं तथा सक्रिय रूप से भारत के स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को आकार दे रही हैं।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म, वित्तीय समावेशन और मार्गदर्शन ने महिलाओं को अपने उद्यम को बढ़ाने में सक्षम बनाया है।
- महिला उद्यमियों की दृश्यता लैंगिक मानदंडों को चुनौती दे रही है और दूसरों को प्रेरित कर रही है। पारिस्थितिकी तंत्र अब अधिक लैंगिक जागरूक है, जो समावेशी नवाचार को बढ़ावा दे रहा है।
- उदाहरण के लिये, फाल्गुनी नायर की Nykaa, श्रद्धा शर्मा की YourStory और उपासना ताकू की MobiKwik इस प्रवृत्ति को दर्शाती हैं।
- SIDBI फंड का 10% से अधिक हिस्सा अब महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्ट-अप के लिये निर्धारित किया गया है (SIDBI, 2024)।
- वित्तीय और डिजिटल समावेशन: औपचारिक बैंकिंग और डिजिटल वित्तीय साधनों तक पहुँच ने महिलाओं को आर्थिक रूप से बहुत सशक्त बनाया है।
- वित्तीय नियंत्रण के साथ, महिलाएँ व्यवसाय और घरेलू निर्णय लेने में अधिक आत्मविश्वासी हैं। डिजिटल बैंकिंग, आधार-लिंक्ड सेवाओं और मोबाइल वॉलेट के उदय ने निर्भरता को कम किया है तथा आर्थिक एजेंसी में सुधार किया है। फिनटेक अर्थव्यवस्था में व्यापक भागीदारी का प्रवेश द्वार बन गया है।
- उदाहरण के लिये, 39.2% बैंक खाते और 39.7% जमा अब महिलाओं के पास हैं (MoSPI, 2024)। वर्ष 2021 और 2024 के दौरान महिलाओं के स्वामित्व वाले डीमैट खातों की संख्या तीन गुना हो गई। साथ ही, आर्थिक समावेशन को अब सामुदायिक प्रयास के रूप में देखा जाता है। बैंक सखियों के मॉडल ने $40 मिलियन (वर्ष 2020) के लेनदेन को संसाधित किया।
- कानूनी और संस्थागत सुधार: सुदृढ़ कानूनी समर्थन से कार्यस्थल सुरक्षा में सुधार हुआ है, कार्यबल को बनाए रखने को प्रोत्साहन मिला है तथा लिंग आधारित हिंसा की समस्या से निपटा गया है।
- फास्ट-ट्रैक कोर्ट, वन-स्टॉप सेंटर और कार्यस्थल कानून महिलाओं को संस्थागत आश्वासन देते हैं। यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा और मज़बूत मातृत्व लाभ ड्रॉपआउट को कम करते हैं।
- ये उपाय श्रम बल भागीदारी में दीर्घकालिक लैंगिक समानता के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- उदाहरण के लिये, 750 फास्ट ट्रैक कोर्ट, 802 वन स्टॉप सेंटर कार्यरत हैं; पुलिस स्टेशनों में 14,000 से अधिक महिला सहायता डेस्क हैं (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 2024)।
- तकनीकी प्रवेश और दूरस्थ कार्य के अवसर: डिजिटल परिवर्तन ने दूरस्थ कार्य को सक्षम किया है, जिससे महिलाओं को घरेलू जिम्मेदारियों के साथ पेशेवर भूमिकाओं को संतुलित करने में मदद मिली है।
- गिग इकॉनमी और प्लेटफॉर्म-आधारित नौकरियों ने लचीले रोज़गार के नए रास्ते खोले हैं। इससे पारंपरिक गतिशीलता और समय-संबंधी बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है।
- महिलाएँ अब अपने घरों से ही राष्ट्रीय और वैश्विक श्रम बाज़ार तक पहुँच बना सकती हैं।
- उदाहरण के लिये, कॉमन सर्विस सेंटर 67,000 महिला उद्यमियों द्वारा चलाए जा रहे हैं।
- बदलते सामाजिक मानदंड और रोल मॉडल: विविध क्षेत्रों में सफल महिलाओं की बढ़ती दृश्यता सामाजिक दृष्टिकोण को नया आकार दे रही है।
- न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं।
- रक्षा बलों से लेकर बोर्डरूम तक, महिला नेता युवा पीढ़ी को प्रेरित करती हैं और महत्त्वाकांक्षा को सामान्य बनाती हैं।
- उदाहरण के लिये, 15% भारतीय पायलट महिलाएँ हैं - वैश्विक औसत से तीन गुना। वर्ष 2023 में, कमांडर प्रेरणा देवस्थली भारतीय नौसेना के युद्धपोत की कमान संभालने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी बन गईं।
भारत में महिला सशक्तीकरण में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दे क्या हैं?
- महिला श्रम बल में लगातार कम भागीदारी: हाल के सुधारों के बावजूद, भारत की LFPR वैश्विक औसत 50% से कम बनी हुई है।
- सामाजिक मानदंड, लचीली नौकरियों की कमी और देखभाल की जिम्मेदारियाँ महिलाओं की सक्रिय आर्थिक भागीदारी को प्रतिबंधित करती हैं।
- कई महिलाएँ विवाह या बच्चे के जन्म के बाद नौकरी छोड़ देती हैं तथा अनुकूल कार्य वातावरण के अभाव के कारण पुनः प्रवेश कठिन बना रहता है।
- उदाहरण के लिये, महिला LFPR 23.3% (सत्र 2017-18) से बढ़कर 41.7% (सत्र 2023-24) हो गई, लेकिन अभी भी यह 77.2% पर पुरुषों से पीछे है और वैश्विक महिला औसत 50% से नीचे है (MoSPI, 2024; विश्व बैंक)।
- अवैतनिक देखभाल कार्य और घरेलू बोझ: महिलाएँ अनुपातहीन रूप से अवैतनिक घरेलू कार्य करती हैं, जो आधिकारिक आर्थिक मापदंडों में अदृश्य रहता है।
- यह दोहरा बोझ शिक्षा, कौशल विकास या औपचारिक रोज़गार के लिये समय को सीमित करता है। घरेलू जिम्मेदारियों को अभी भी महिलाओं का कर्त्तव्य माना जाता है जो लैंगिक भूमिकाओं को सुदृढ़ करता है।
- घरेलू कार्यों में पुरुषों की भागीदारी अत्यंत कम बनी हुई है, जो धीमी सामाजिक परिवर्तन का संकेत है।
- उदाहरण के लिये, टाइम यूज़ सर्वे से पता चलता है कि महिलाएँ अवैतनिक घरेलू सेवाओं पर प्रतिदिन 236 मिनट खर्च करती हैं, जबकि पुरुष 24 मिनट प्रतिदिन खर्च करते हैं।
- लिंग आधारित वेतन अंतर और अनौपचारिकता: जब महिलाएँ काम करती हैं, तब भी उन्हें वेतन असमानताओं का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से अनौपचारिक और ग्रामीण क्षेत्रों में।
- बहुत से लोग कम वेतन वाले, असुरक्षित, अनौपचारिक कामों में लगे हुए हैं, जिनमें सामाजिक सुरक्षा नहीं है। वेतन में अंतर के कारण लंबे समय तक कार्यबल में बने रहना मुश्किल हो जाता है और महिलाओं के कौशल को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन कम हो जाता है।
- उदाहरण के लिये, शहरी क्षेत्रों में पुरुष महिलाओं की तुलना में 29.4% अधिक कमाते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में वे 51.3% अधिक कमाते हैं। लगभग 81% महिलाएँ अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करती हैं (NSSO, 2023)।
- लिंग आधारित हिंसा और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: सार्वजनिक और निजी स्थानों पर सुरक्षा संबंधी भय महिलाओं की गतिशीलता, रोज़गार एवं शिक्षा के अवसरों को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करता है।
- NFHS-5 (सत्र 2019-2021) सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती है कि 18-49 वर्ष की आयु की 29.3% विवाहित महिलाओं ने पति द्वारा हिंसा का अनुभव किया है।
- लिंग-आधारित हिंसा (GBV) मनोवैज्ञानिक और आर्थिक अशक्तता का कारण बनती है।
- त्वरित न्याय का अभाव, कानूनों का अकुशल क्रियान्वयन तथा कम रिपोर्टिंग से स्थिति और बदतर हो जाती है।
- उदाहरण के लिये, भारत में हर घंटे महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के 51 मामले दर्ज होते हैं; वर्ष 2022 में 4.4 लाख से अधिक मामले: NCRB रिपोर्ट।
- राजनीतिक और नेतृत्वकारी भूमिकाओं में अल्प प्रतिनिधित्व: ज़मीनी स्तर पर संख्यात्मक लाभ के बावजूद, उच्च स्तरों पर निर्णय लेने में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी अल्प है।
- महिलाओं को न केवल ग्लास सीलिंग (अदृश्य बाधाएँ जो महिलाओं को शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचने से रोकती हैं) का सामना करना पड़ता है, बल्कि ग्लास क्लिफ के उदाहरणों का भी सामना करना पड़ता है, जहाँ संकट के समय में उन्हें नेतृत्व की भूमिका में नियुक्त किये जाने की अधिक संभावना होती है, जिससे सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है।
- संसद में महिलाओं की कमी (महिला आरक्षण विधेयक का क्रियान्वयन अगले परिसीमन तक लंबित है) और कॉर्पोरेट बोर्ड लिंग-संवेदनशील नीति निर्माण को कम करते हैं। पंचायतों में आरक्षण अभी तक राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर आनुपातिक संख्या में तब्दील नहीं हुआ है।
- उदाहरण के लिये, 18वीं लोकसभा के केवल 13.6% सदस्य महिलाएँ हैं। इसके अलावा, निफ्टी-500 कंपनियों के निदेशकों में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 17.6% है।
- डिजिटल डिवाइड और तकनीक-पहुँच असमानता: यद्यपि डिजिटल साक्षरता बढ़ रही है, महिलाओं की डिजिटल उपकरणों तक पहुँच, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, सीमित है।
- विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में फोन, इंटरनेट और डिजिटल वित्त तक लैंगिक पहुँच उन्हें शिक्षा, नौकरी या उद्यमिता के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने से रोकती है।
- यह अपवर्जन के चक्र को और सुदृढ़ करता है। उदाहरण के लिये, ग्रामीण क्षेत्रों की केवल 33% महिलाएँ ही इंटरनेट का उपयोग करती हैं, जबकि पुरुषों में यह प्रतिशत 57% है। मोबाइल फोन का स्वामित्व अभी भी महिलाओं के पास लगभग 54% है (NFHS-5, 2021)।
- कार्यस्थल पर अपर्याप्त बुनियादी अवसंरचना और सहायता: लिंग-संवेदनशील बुनियादी अवसंरचना (जैसे: स्वच्छता, क्रेच, परिवहन) का अभाव महिलाओं को कार्यबल में शामिल होने या बने रहने से हतोत्साहित करता है।
- इसके अलावा, भारत में 37% संगठन अभी भी मातृत्व अवकाश का लाभ प्रदान नहीं करते हैं और केवल 17.5% ही शिशु देखभाल सुविधाएँ प्रदान करते हैं।
- पर्याप्त मातृत्व लाभ, सवेतन छुट्टी या लचीले काम के घंटों के बिना, महिलाओं को काम और जीवन के बीच संतुलन बनाना मुश्किल लगता है। कई महिलाएँ देखभाल करने वाली भूमिकाओं के कारण नौकरी छोड़ देती हैं।
- उदाहरण के लिये, अकुशल नीतियों के कारण 4 में से 1 कामकाज़ी महिला को बच्चों की देखभाल और कॅरियर के बीच चयन करना पड़ा।
आर्थिक विकास में महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?
- स्थानीय आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ कौशल को एकीकृत करना: कौशल भारत, PMKVY और SANKALP के तहत महिलाओं के कौशल कार्यक्रमों को स्थानीय आर्थिक मांगों तथा ग्रीन जॉब्स, स्वास्थ्य सेवा एवं डिजिटल सेवाओं जैसे उभरते क्षेत्रों के साथ संरेखित किया जाना चाहिये।
- यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि कौशल विकास से वास्तविक, संधारणीय आर्थिक अवसर प्राप्त होंगे।
- प्रशिक्षण मांग आधारित होना चाहिये तथा उसे प्लेसमेंट सेल, SHG फेडरेशन (जैसे: केरल का कुदुम्बश्री) और उद्यमिता केंद्रों जैसे प्रशिक्षण-पश्चात संपर्कों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिये।
- प्रारंभिक अनुभव के लिये माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिये। ज़िला कौशल समितियों के तहत ज़िला-स्तरीय जेंडर-स्मार्ट कौशल योजनाएँ बनाई जानी चाहिये।
- एकीकृत वित्त मॉडल के माध्यम से महिला उद्यम को बढ़ावा देना: नैनो और सूक्ष्म उद्यमों को समर्थन देने के लिये एकीकृत ऋण पहुँच मॉडल के तहत MUDRA ऋण, स्टैंड-अप इंडिया और महिला उद्यमिता कोष को जोड़ा जाना चाहिये।
- GeM जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से महिला उद्यमियों को व्यवसाय विकास सेवाओं, डिजिटल ऑनबोर्डिंग और बाज़ार संपर्कों के साथ सहायता प्रदान किया जाना चाहिये।
- स्वयं सहायता समूहों को स्थानीय महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिये इनक्यूबेटर में परिवर्तित किया जा सकता है।
- क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिये संयुक्त देयता और सहकर्मी सलाह मॉडल पेश किया जाना चाहिये। यह महिलाओं के लिये एक व्यवहार्य आजीविका विकल्प के रूप में उद्यमिता को मुख्यधारा में लाएगा।
- बाल देखभाल और देखभाल अर्थव्यवस्था समर्थन को संस्थागत बनाना: सामर्थ्य और ICDS के तहत एक राष्ट्रीय क्रेच ग्रिड विकसित किया जाना चाहिये, कामकाज़ी माताओं को समर्थन देने के लिये आँगनवाड़ियों एवं कार्यस्थल-आधारित क्रेच को एकीकृत किया जाना चाहिये।
- इससे देखभाल संबंधी कार्य का पुनर्वितरण होगा और कार्यबल में महिलाओं की उपस्थिति सुनिश्चित होगी।
- नियोक्ता-प्रायोजित बाल देखभाल सुविधाएँ बनाने के लिये PPP मॉडल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- औपचारिक कौशल और वेतन तंत्र के माध्यम से देखभाल कर्मियों को मान्यता दी जानी चाहिये और उन्हें पेशेवर बनाया जाना चाहिये।
- पोर्टेबल देखभाल लाभ कार्यढाँचे के माध्यम से अनौपचारिक क्षेत्र में सशुल्क मातृत्व अवकाश का विस्तार किया जाना चाहिये।
- बुनियादी अवसंरचना और डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र परियोजनाओं में महिलाओं को मुख्यधारा में लाना: स्वच्छता, परिवहन, जल, आवास के लिये बुनियादी अवसंरचना के निर्माण में लिंग-उत्तरदायी बजट को अनिवार्य किया जाना चाहिये ताकि महिलाओं के लिये सार्वजनिक बुनियादी अवसंरचना की उपयोगिता में सुधार हो सके।
- स्मार्ट सिटी और AMRUT परियोजनाओं में जेंडर ऑडिट एवं मोबिलिटी मैपिंग को संस्थागत बनाया जाना चाहिये। इससे बुनियादी अवसंरचना अधिक समावेशी और सशक्त बनेगा।
- महिलाओं के डिजिटल सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय अवसंरचना और ग्रामीण इंटरनेट परियोजनाओं में डिजिटल साक्षरता एवं PMGDISHA को शामिल किया जाना चाहिये।
- सामुदायिक भागीदारी मंचों के माध्यम से बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं की योजना बनाने और निगरानी में महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिये।
- अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं के लिये औपचारिकीकरण और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना: महिलाओं के नेतृत्व वाले अनौपचारिक उद्यमों को औपचारिक कार्यढाँचे के तहत लाने के लिये लिंग-स्मार्ट उद्यम पंजीकरण अभियान बनाया जाना चाहिये।
- इससे अनौपचारिक महिला श्रमिकों की दृश्यता, सुरक्षा और उत्पादकता बढ़ती है।
- सरलीकृत दस्तावेज़ीकरण और मोबाइल-सक्षम नामांकन के साथ e-SHRAM, ESIC और NPS कवरेज का विस्तार किया जाना चाहिये।
- मूल्य संवर्द्धन और आपूर्ति शृंखलाओं को औपचारिक बनाने के लिये एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP) के अंतर्गत महिला-विशिष्ट क्लस्टरों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- शासन और निर्णय-निर्माण में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सशक्त करना: सरकारी बोर्डों, स्थानीय योजना समितियों, MSME संवर्द्धन परिषदों और सहकारी समितियों में लिंग कोटा अनिवार्य किया जाना चाहिये।
- पंचायत प्रोत्साहनों को आर्थिक एवं योजना भूमिकाओं में महिलाओं के समावेशन से जोड़ने की आवश्यकता है।
- शासन के सभी स्तरों पर जेंडर बजट और नियोजन पर क्षमता निर्माण को संस्थागत बनाया जाना चाहिये। नेतृत्व में महिलाएँ अधिक लैंगिक-संवेदनशील नीतियाँ और संसाधन आवंटन सुनिश्चित करती हैं।
- निजी क्षेत्र में लिंग-संवेदनशील कार्य मानदंडों का विस्तार करना: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और ESG कार्यढाँचे के तहत पितृत्व अवकाश और जेंडर ऑडिट प्रकटीकरण को अनिवार्य किया जाना चाहिये।
- ये मानदंड, दिखावे से आगे बढ़कर, लिंग-समावेशी मानव संसाधन प्रथाओं को मुख्यधारा में लाने में मदद कर सकते हैं।
- निजी कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये कि वे महिलाओं के लिये कॅरियर ब्रेक के बाद वापसी कार्यक्रम और पुनः कौशल विकास के विकल्प तैयार करें।
- कंपनियों को सार्वजनिक खरीद प्राथमिकताओं से जुड़ा एक जेंडर इक्विटी इंडेक्स पेश करना चाहिये। सभी क्षेत्रों में फ्लेक्सी-टाइम, घर से काम करने और ऑन-साइट चाइल्डकेयर सुविधाओं के अंगीकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- एकीकृत महिला डिजिटल पहचान और लाभ मंच विकसित करना: आधार से जुड़ा तथा API-सक्षम मंच महिला डिजिटल सशक्तीकरण स्टैक बनाया जाना चाहिये जो कल्याण, ऋण, कौशल एवं बीमा तक पहुँच को एकीकृत करता है।
- इस स्टैक का उपयोग प्रगति को ट्रैक करने, लीकेज को कम करने और कस्टम एडवाइस प्रदान करने के लिये किया जाना चाहिये। इसे एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम और डिजिटल इंडिया पहलों में शामिल किया जाना चाहिये।
- महिलाओं के नेतृत्व वाली CSC के माध्यम से सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी के लिये फिनटेक के साथ साझेदारी की जानी चाहिये।
- लिंग-केंद्रित स्थानीय विकास योजनाओं के माध्यम से योजना का विकेंद्रीकरण: ग्राम पंचायत, ब्लॉक और ज़िला स्तर पर लिंग कार्य योजनाओं को संस्थागत बनाना, महिला सभाओं और SHG नेटवर्क से प्राप्त इनपुट को एकीकृत किया जाना चाहिये।
- इन योजनाओं को महिलाओं के साथ मिलकर बनाया जाना चाहिये तथा वार्षिक विकास योजना चक्रों एवं वित्तपोषण में शामिल किया जाना चाहिये।
- प्राथमिकता अंतराल की पहचान करने के लिये MoSPI के टाइम यूज़ सर्वे, NFHS और SECC से डेटा का उपयोग किया जाना चाहिये। विकेंद्रीकृत, डेटा-संचालित लिंग नियोजन संदर्भ-विशिष्ट और प्रभावी हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है।
निष्कर्ष:
जैसा कि प्रसिद्ध संस्कृत कहावत है: "राष्ट्रस्य श्रवः नारी अस्ति, नारी राष्ट्रस्य अक्षि अस्ति !" अर्थात् महिला वह कान है जिसके माध्यम से राष्ट्र सुनता है, वह नेत्र है जिसके माध्यम से वह देखता है। भारत के जनांकिक लाभांश का सही मायने में दोहन करने के लिये, महिला सशक्तीकरण को आकांक्षा से कार्यान्वयन की ओर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। महिलाओं की समानता को बढ़ावा देने से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में $28 ट्रिलियन की वृद्धि हो सकती है, जिसमें भारत में संभावित रूप से वर्ष 2025 तक $770 बिलियन की वृद्धि देखी जा सकती है। लैंगिक समानता वाली अर्थव्यवस्था न केवल समावेशी विकास को बल्कि राष्ट्रीय विकास को भी गति देती है। ये प्रयास सीधे SDG 5 (लैंगिक समानता) और SDG 8 (उत्कृष्ट श्रम और आर्थिक विकास) के साथ संरेखित हैं।
|
दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. "भारत का विकास परिदृश्य महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के बिना अधूरी रहेगा।" चर्चा कीजिये। |
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न 1. निम्नलिखित में से कौन, विश्व के देशों के लिये 'सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक (ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स)' का श्रेणीकरण प्रदान करता है? (2017) (a) विश्व आर्थिक मंच उत्तर: (a) मेन्सप्रश्न 1. "महिला सशक्तीकरण जनसंख्या संवृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है।" चर्चा कीजिये। (2019) प्रश्न 2. भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के समारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा कीजिये। (2015) प्रश्न 3. "महिला संगठनों को लिंग-भेद से मुक्त करने के लिये पुरुषों की सदस्यता को बढ़ावा मिलना चाहिये।" टिप्पणी कीजिये। (2013) प्रश्न 4. ‘देखभाल अर्थव्यवस्था’ और ‘मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था’ के बीच अंतर कीजिये। महिला सशक्तीकरण के द्वारा देऽभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में कैसे लाया जा सकता है? (2023) |