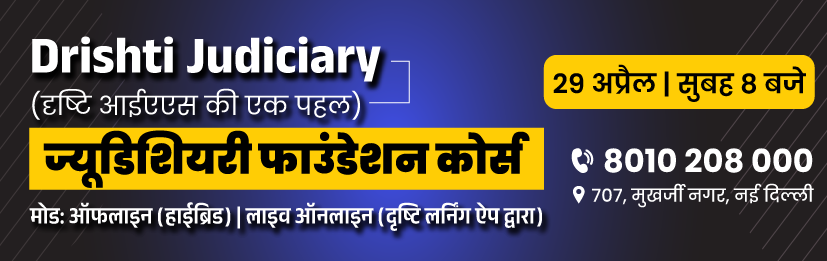शासन व्यवस्था
नई सैटेलाइट-आधारित टोल संग्रहण प्रणाली
प्रिलिम्स के लिये:गगन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, फास्टैग मेन्स के लिये:सैटेलाइट-आधारित नेविगेशन सिस्टम, बुनियादी ढाँचे का महत्त्व |
स्रोत: द हिंदू
चर्चा में क्यों?
हाल ही में भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने संसद में घोषणा की कि सरकार 2024 चुनाव के लिये आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने से पहले वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (GNSS) पर आधारित एक नई राजमार्ग टोल संग्रह प्रणाली शुरू करने की योजना बना रही है।
नई प्रस्तावित राजमार्ग टोलिंग प्रणाली क्या है?
- मुख्य विशेषताएँ:
- प्रस्तावित राजमार्ग टोलिंग प्रणाली सटीक स्थान ट्रैकिंग के लिये भारतीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली GAGAN (GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन) सहित GNSS का उपयोग करती है।
- GNSS एक शब्द है जिसका उपयोग अमेरिका के ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम (GPS) सहित किसी भी उपग्रह-आधारित नेविगेशन सिस्टम को संदर्भित करने के लिए किया जाता है।
- यह अकेले GPS की तुलना में विश्व स्तर पर उपयोगकर्त्ताओं को अधिक सटीक स्थान और नेविगेशन जानकारी प्रदान करने के लिये उपग्रहों के एक बड़े समूह का उपयोग करता है।
- कार्यान्वयन में वाहनों को ऑन-बोर्ड यूनिट (OBU) या ट्रैकिंग डिवाइस के साथ फिट करना शामिल है, जो स्थान निर्धारित करने के लिये उपग्रहों के साथ संचार करता है।
- राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्देशांक डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का उपयोग करके लॉग किये जाते हैं, जिससे सॉफ्टवेयर यात्रा की गई दूरी के आधार पर टोल दरों की गणना कर सकता है।
- टोल राशि की कटौती OBU से जुड़े/संबद्ध डिजिटल वॉलेट से की जाती है जिससे निर्बाध और नकदी रहित लेन-देन सुनिश्चित होता है।
- इसके प्रवर्तन उपायों में अनुपालन की निगरानी और चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिये राजमार्गों पर CCTV कैमरों से सुसज्जित गैन्ट्री (Gantry) शामिल है।
- यह नवीन प्रणाली संभवतः वर्तमान में मौजूदा FASTag-आधारित टोल संग्रह के साथ संचालित की जाएगी। सभी वाहनों के लिये OBU अनिवार्य करने के संबंध में निर्णय करना अभी बाकी है।
- प्रस्तावित राजमार्ग टोलिंग प्रणाली सटीक स्थान ट्रैकिंग के लिये भारतीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली GAGAN (GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन) सहित GNSS का उपयोग करती है।
- लाभ:
- सुचारु यातायात प्रवाह: टोल प्लाज़ा को समाप्त करने से यातायात की भीड़, विशेषकर पीक आवर्स के दौरान, में काफी कमी आने की उम्मीद है।
- यात्रा समय: निर्बाध टोल संग्रह से यात्रा का समय कम हो जाएगा और साथ ही राजमार्ग नेटवर्क अधिक कुशल हो जाएगा।
- उचित बिलिंग: इस प्रणाली का लक्ष्य उपयोगकर्त्ताओं को केवल यात्रा की गई वास्तविक दूरी के लिये टोल का भुगतान करने का लाभ प्रदान करना है जो उपयोग आधारित भुगतान (Pay-As-You-Use Model) करने के मॉडल को बढ़ावा देता है।
- चुनौतियाँ:
- भुगतान वसूली: आवश्यकता से कम राशि वाले डिजिटल वॉलेट वाले अथवा सिस्टम से छेड़छाड़ करने वाले उपयोगकर्त्ताओं से टोल वसूलना एक चिंता का विषय बना हुआ है।
- प्रवर्तन अवसंरचना: प्रवर्तन उद्देश्यों के लिये स्वचालित रूप से नंबर-प्लेट पहचान (ANPR) कैमरों का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करने के लिये महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के विकास की आवश्यकता है।
- निजता संबंधी चिंताएँ: डेटा सुरक्षा और उपयोगकर्त्ता गोपनीयता को प्रभावी ढंग से संबोधित करने की आवश्यकता है।
फास्टैग:
- FASTag एक उपकरण है जो वाहन के चलते समय सीधे टोल भुगतान करने के लिये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग करता है।
- फास्टैग (RFID टैग) वाहन की विंडस्क्रीन पर चिपकाया जाता है और ग्राहक को फास्टैग से जुड़े खाते से सीधे टोल भुगतान करने में सक्षम बनाता है।
- इसका संचालन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की देखरेख में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।
गगन
- GPS सहायता प्राप्त GEO संवर्धित नेविगेशन (GAGAN) भारत में सैटेलाइट-आधारित नेविगेशन सेवाओं के लिये भारत सरकार की एक पहल है।
- इसका उद्देश्य संदर्भ संकेतों के माध्यम से वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (global navigation satellite system - GNSS) रिसीवरों की सटीकता को बढ़ाना है।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगन को एक सैटेलाइट बेस्ड ऑग्मेंटेशन सिस्टम के रूप में विकसित करने के लिये सहयोग किया है।
- GAGAN का लक्ष्य भारतीय हवाई क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र में विमान को सटीक लैंडिंग में सहायता करने के लिये एक नेविगेशन प्रणाली प्रदान करना है और नागरिक संचालन के लिये जीवन की सुरक्षा के लिये लागू है। GAGAN अन्य अंतर्राष्ट्रीय SBAS प्रणालियों के साथ अंतःक्रियाशील है।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपनी उपग्रह मार्गनिर्देशन (नैविगेशन) प्रणाली है? (2023) (a) ऑस्ट्रेलिया उत्तर: (d) प्रश्न. भारतीय क्षेत्रीय-संचालन उपग्रह प्रणाली (इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम/IRNSS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न. भारतीय प्रादेशिक नौपरिवहन उपग्रह प्रणाली (आई.आर.एन.एस.एस.) की आवश्यकता क्यों है? यह नौपरिवहन में किस प्रकार सहायक है? (2018) |
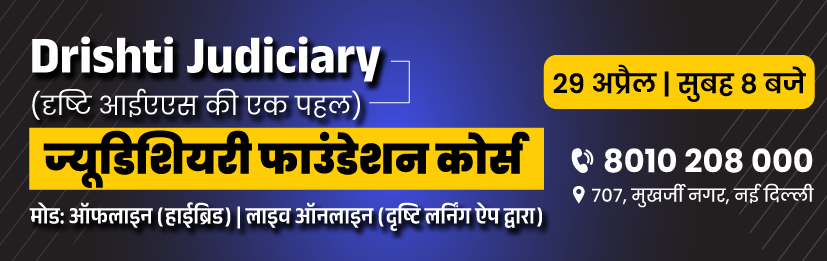

भारतीय अर्थव्यवस्था
विनियामकीय सैंडबॉक्स के लिये व्यापक रूपरेखा
प्रिलिम्स के लिये:भारतीय रिज़र्व बैंक, विनियामकीय सैंडबॉक्स, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023, फिनटेक मेन्स के लिये:नए वित्तीय नवाचारों के जोखिमों के आकलन में विनियामकीय सैंडबॉक्स का महत्त्व। |
स्रोत: बिज़नेस स्टैण्डर्ड
चर्चा में क्यों?
हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियामकीय सैंडबॉक्स के विभिन्न चरणों को पूरा करने की समय-सीमा को पिछले 7 महीनों से बढ़ाकर 9 महीने कर दिया है।
- विनियामकीय सैंडबॉक्स के लिये अद्यतन ढाँचे में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सैंडबॉक्स संस्थाओं की भी आवश्यकता होती है।
विनियामकीय सैंडबॉक्स (RS) क्या है?
- पृष्ठभूमि:
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने फिनटेक के विस्तृत पहलुओं के साथ उसके निहितार्थों की निगरानी करने एवं रिपोर्ट करने हेतु वर्ष 2016 में एक अंतर-नियामक कार्य समूह की स्थापना की, ताकि नियामक ढाँचे की समीक्षा की जा सके और साथ ही तेज़ी से विकसित हो रहे फिनटेक परिदृश्य की गतिशीलता पर प्रतिक्रिया दी जा सके।
- रिपोर्ट में एक अच्छी तरह से परिभाषित स्थान और अवधि के भीतर एक विनियामकीय सैंडबॉक्स के लिये एक उपयुक्त ढाँचे को प्रस्तुत करने की सिफारिश की गई है, जहाँ वित्तीय क्षेत्र नियामक दक्षता बढ़ाने, जोखिमों का प्रबंधन करने तथा उपभोक्ताओं के लिये नए अवसर सृजित करने हेतु आवश्यक नियामक मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
- परिचय:
- विनियामकीय सैंडबॉक्स एक नियंत्रित नियामक वातावरण में नए उत्पादों अथवा सेवाओं के प्रत्यक्ष रूप से हुए परीक्षण को संदर्भित करता है जिसके लिये नियामक परीक्षण के सीमित उद्देश्य हेतु कुछ नियामक छूट की अनुमति दे भी सकते हैं और नहीं भी।
- विनियामकीय सैंडबॉक्स एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है जो अधिक गतिशील, साक्ष्य-आधारित नियामक वातावरण को सक्षम बनाता है जो उभरती प्रौद्योगिकियों से सीखते हुए उनके साथ-साथ विकसित होता है।
- यह विनियामक, वित्तीय सेवा प्रदाताओं और ग्राहकों को उनके जोखिमों की निगरानी तथा नियंत्रण करते हुए नए वित्तीय नवाचारों के लाभों एवं जोखिमों पर साक्ष्य एकत्र करने के लिये क्षेत्र परीक्षण करने में सक्षम बनाता है।
- उद्देश्य:
- विनियामकीय सैंडबॉक्स का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं में उत्तरदायी नवाचार को बढ़ावा देकर दक्षता को प्रोत्साहन प्रदान करना और उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाना है।
- यह विनियामक को संबद्ध पारितंत्र के साथ जुड़ने और नवाचार-सक्षम अथवा नवाचार-उत्तरदायी नियमों को विकसित करने के लिये एक संरचित अवसर प्रदान कर सकता है जो प्रासंगिक, अल्प लागत वाले वित्तीय उत्पादों की डिलीवरी की सुविधा प्रदान करता है।
- लक्षित आवेदक:
- विनियामकीय सैंडबॉक्स में प्रवेश के लिये लक्षित आवेदकों में फिनटेक, बैंक और वित्तीय सेवा व्यवसायों के साथ साझेदारी करने वाली अथवा उन्हें सहायता प्रदान करने वाली कंपनियाँ शामिल हैं।
भारत में विनियामकीय सैंडबॉक्स का अंगीकरण:
- फिनटेक फोकस: भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2019 में पहला विनियामकीय सैंडबॉक्स कार्यक्रम प्रस्तुत किया।
- यह RBI की देखरेख में नियंत्रित वातावरण में नवीन वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के लाइव परीक्षण की सुविधा प्रदान करता है।
- विषयगत कॉहोर्ट्स: RBI सैंडबॉक्स विषयगत कॉहोर्ट्स के आधार पर संचालित होता है। प्रत्येक कॉहोर्ट खुदरा भुगतान, सीमा पारीय लेन-देन अथवा MSME ऋण जैसे विशिष्ट क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है।
- विनियामकीय सैंडबॉक्स से संबंधित प्रमुख घटक:
- विनियामकीय सैंडबॉक्स कॉहोर्ट्स: वित्तीय समावेशन, भुगतान और ऋण, डिजिटल KYC आदि पर ध्यान केंद्रित करने वाले विषयगत कॉहोर्ट्स पर आधारित।
- विनियामक छूट: RBI द्वारा कुछ छूट प्रदान की जा सकती हैं जिनमें चलनिधि आवश्यकताएँ, बोर्ड संरचना, वैधानिक प्रतिबंध आदि शामिल हैं।
- विनियामकीय सैंडबॉक्स परीक्षण से अपवर्जन: सांकेतिक नकारात्मक सूची में क्रेडिट रजिस्ट्री, क्रिप्टोकरेंसी, प्रारंभिक सिक्का प्रस्ताव/पेशकश (Initial Coin Offerings) आदि शामिल हैं।
- विनियामकीय सैंडबॉक्स से संबंधित प्रमुख घटक:
- टेलीकॉम सैंडबॉक्स: सरकार ने "मिलेनियम स्पेक्ट्रम रेगुलेटरी सैंडबॉक्स" पहल शुरू की। इसमें एक स्पेक्ट्रम रेगुलेटरी सैंडबॉक्स (SRS) और वायरलेस टेस्ट जोन (WiTe ज़ोन) शामिल हैं।
- इन पहलों का उद्देश्य दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिये नियमों को सरल बनाना और तकनीकी प्रगति के लिये नए स्पेक्ट्रम बैंड की खोज करना है।
विनियामकीय सैंडबॉक्स से संबंधित लाभ और चुनौतियाँ क्या हैं?
- लाभ:
- विनियामक अंतर्दृष्टि: नियामक उभरती प्रौद्योगिकियों के लाभों और जोखिमों तथा उनके निहितार्थ पर प्रत्यक्ष अनुभवजन्य साक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वे संभावित नियामक परिवर्तनों पर विचारशील दृष्टिकोण अपना सकें।
- वित्तीय प्रदाताओं के लिये समझ: मौजूदा वित्तीय सेवा प्रदाता अपनी समझ में सुधार कर सकते हैं कि नई वित्तीय प्रौद्योगिकियाँ कैसे काम कर सकती हैं, संभावित रूप से उन्हें अपनी व्यावसायिक योजनाओं के साथ ऐसी नई प्रौद्योगिकियों को उचित रूप से एकीकृत करने में मदद मिल सकती है।
- लागत प्रभावी व्यवहार्यता परीक्षण: RS के उपयोगकर्त्ताओं के पास बड़े और अधिक महँगे रोल-आउट की आवश्यकता के बिना उत्पाद की व्यवहार्यता का परीक्षण करने की क्षमता है।
- वित्तीय समावेशन क्षमता: फिनटेक ऐसे समाधान प्रदान करते हैं जो संभावित रूप से महत्त्वपूर्ण तरीके से वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ा सकते हैं।
- नवप्रवर्तन के लिये महत्त्वपूर्ण क्षेत्र: जिन क्षेत्रों को संभावित रूप से RS से बल मिल सकता है उनमें माइक्रोफाइनेंस, संभावित रूप से नवीन लघु बचत, प्रेषण, मोबाइल बैंकिंग और अन्य डिजिटल भुगतान शामिल हैं।
- चुनौतियाँ:
- लचीलापन और समय की कमी: नवप्रवर्तकों को सैंडबॉक्स प्रक्रिया के दौरान लचीलेपन और समय के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे संभावित रूप से अनुकूलन तथा त्वरित पुनरावृत्ति करने की उनकी क्षमता प्रभावित हो सकती है।
- केस-दर-केस प्राधिकरण: व्यक्तिगत आधार पर अनुकूलित प्राधिकरण और नियामक छूट हासिल करना एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, जिसमें अक्सर व्यक्तिपरक मूल्यांकन शामिल होता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रयोग में देरी हो सकती है।
- कानूनी छूट पर सीमाएँ: RBI या उसका नियामक सैंडबॉक्स कानूनी छूट की पेशकश नहीं कर सकता है, जो प्रयोग करते समय कानूनी जोखिमों को कम करने की चाह रखने वाले नवप्रवर्तकों को सीमित कर सकता है।
- सैंडबॉक्स के बाद विनियामक स्वीकृतियाँ: सफल सैंडबॉक्स परीक्षण के बाद भी, प्रयोगकर्त्ताओं को अपने उत्पाद, सेवाओं या प्रौद्योगिकी को व्यापक अनुप्रयोग के लिये अनुमति देने से पहले नियामक अनुमोदन की आवश्यकता हो सकती है, जिससे संभावित रूप से बाज़ार में आने का समय बढ़ सकता है।
आगे की राह
- नवप्रवर्तकों पर समय और प्रशासनिक बोझ को कम करने के लिये सैंडबॉक्स प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की दिशा में काम करें। इसमें आवेदन प्रक्रियाओं को सरल बनाना और भागीदारी के लिये स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करना शामिल हो सकता है।
- निर्णय लेने के लिये स्पष्ट मानदंड प्रदान करके और यह सुनिश्चित करके कि निर्णय लगातार तथा निष्पक्ष रूप से किये जाएँ, मामले-दर-मामले प्राधिकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाएँ।
- सैंडबॉक्स में भाग लेने वाले नवप्रवर्तकों के लिये व्यापक शिक्षा और सहायता प्रदान करें, जिसमें नियामक आवश्यकताओं तथा संभावित कानूनी मुद्दों पर मार्गदर्शन शामिल है।
- प्रयोग के दौरान उत्पन्न होने वाले कानूनी मुद्दों, जैसे उपभोक्ता हानि, के समाधान के लिये रूपरेखा विकसित करने हेतु कानूनी विशेषज्ञों के साथ सहयोग करें। इसमें नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिये सुरक्षा उपायों को लागू करना शामिल हो सकता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिये कि सफल प्रयोग तेज़ी से व्यापक अनुप्रयोग के लिये आगे बढ़ सकें, सैंडबॉक्स परीक्षण के बाद विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करें। इसमें सिद्ध नवाचारों हेतु फास्ट-ट्रैक अनुमोदन तंत्र स्थापित करना शामिल हो सकता है।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)प्रिलिम्स:प्रश्न. भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2010)
उपर्युक्त में से किसे भारत में "वित्तीय समावेशन" प्राप्त करने के लिये उठाया गया कदम माना जा सकता है? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) |

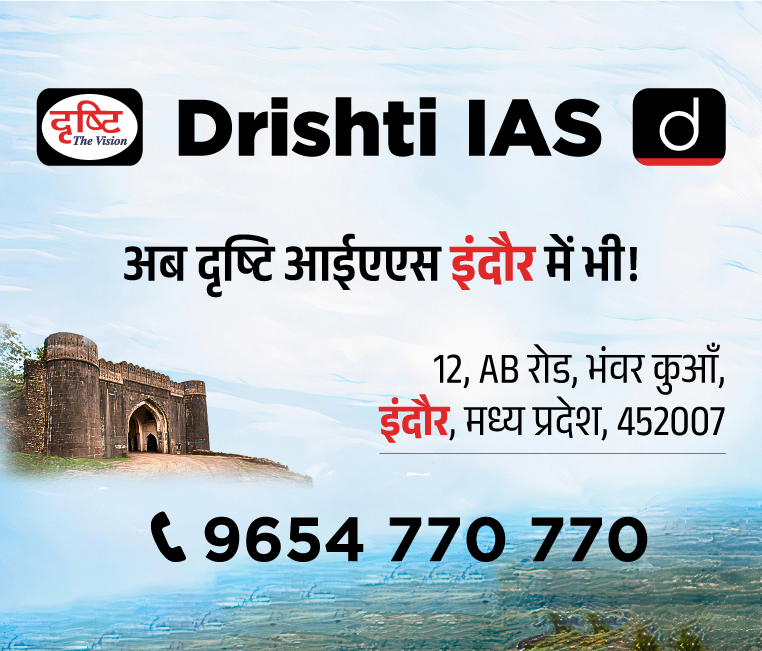
सामाजिक न्याय
गिग श्रमिकों से संबंधित चुनौतियाँ
प्रिलिम्स के लिये:गिग श्रमिकों से संबंधित चुनौतियाँ, गिग श्रमिक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020), वेतन संहिता, 2019 मेन्स के लिये:गिग श्रमिकों से संबंधित चुनौतियाँ, गिग श्रमिकों के लिये चुनौतियाँ और समाधान, भारत में गिग अर्थव्यवस्था और उठाए जाने वाले कदम |
स्रोत:द हिंदू
चर्चा में क्यों?
हाल ही में पीपल्स एसोसिएशन इन ग्रासरूट्स एक्शन एंड मूवमेंट्स और इंडियन फेडरेशन ऑफ एप-आधारित ट्रांसपोर्ट वर्कर्स द्वारा एक अध्ययन किया गया जो भारत में एप-आधारित कैब तथा डिलीवरी ड्राइवरों/व्यक्तियों जैसे गिग श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।
अध्ययन से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं?
- दीर्घ कार्यावधि:
- लगभग एक तिहाई एप-आधारित कैब ड्राइवर दिन में 14 घंटे से अधिक कार्य करते हैं, 83% से अधिक ड्राइवर 10 घंटे से अधिक कार्य करते हैं और 60% ड्राइवर 12 घंटे से अधिक कार्य करते हैं।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 60% से अधिक ड्राइवर दिन में 14 घंटे से अधिक कार्य करते हैं। काम के घंटों को लेकर ये असमानताएँ कार्य स्थिति पर और अधिक प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।
- कम वेतन:
- 43% से अधिक गिग श्रमिक सभी लागतों की कटौती के बाद प्रतिदिन 500 रुपए अथवा 15,000 रुपए से कम आय अर्जित करते हैं।
- इसके अतिरिक्त 34% एप-आधारित डिलीवरी करने वाले श्रमिक प्रति माह 10,000 रुपए से कम आय अर्जित करते हैं। ये आय असमानताएँ मौजूदा सामाजिक असमानताओं में योगदान करती हैं।
- आर्थिक तंगी:
- 72% कैब ड्राइवर और 76% डिलीवरी श्रमिकों को व्यय का प्रबंधन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, 68% कैब ड्राइवरों का कुल व्यय उनकी आय से अधिक हो जाता है जिससे संभावित रूप से ऋण जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- असंतोषजनक प्रतिपूर्ति:
- अध्ययन के अनुसार 80% से अधिक एप-आधारित कैब ड्राइवर कंपनियों द्वारा दिये जाने वाले किराए से असंतुष्ट थे जबकि 73% से अधिक एप-आधारित डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों ने उनकी दरों पर असंतोष व्यक्त किया।
- अध्ययन के अनुसार नियोक्ता द्वारा ड्राइवरों की प्रति सवारी पर लिया जाने वाला कमीशन दर 31-40% है जबकि कंपनियों द्वारा आधिकारिक तौर पर दावा किया गया आँकड़ा 20% है।
- कार्य की स्थिति:
- कार्यावधि के कारण ड्राइवर शारीरिक रूप से थक जाते हैं और विशेष रूप से कुछ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों की 'दरवाज़े पर 10 मिनट की डिलीवरी' नीति के कारण सड़क यातायात दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।
- कई ड्राइवर और डिलीवरी बॉय नियमित छुट्टी लेने के लिये संघर्ष करते हैं, जिनमें से 37% से कम ड्राइवर यूनियन से संबंधित हैं।
- प्लेटफॉर्म से संबंधित मुद्दे:
- श्रमिकों को आईडी निष्क्रियकरण और ग्राहक दुर्व्यवहार जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- ड्राइवरों और डिलीवरी बॉय का एक महत्त्वपूर्ण बहुमत ग्राहक व्यवहार से नकारात्मक प्रभावों की रिपोर्ट करता है।
- अनुशंसाएँ:
- रिपोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिये नियमों की सिफारिश की कि कंपनियाँ गिग श्रमिकों को कंपनियों द्वारा कम भुगतान या शोषण से बचाने के लिये निष्पक्ष और पारदर्शी भुगतान संरचनाएँ स्थापित करें।
- प्लेटफॉर्म श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का भुगतान आय में एक निश्चित घटक की गारंटी देने में मदद करेगा।
- श्रमिकों की ID को ब्लॉक करने के मामलों में, ऐसी प्रथाओं की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये और श्रमिकों की ID को अनिश्चित काल के लिये ब्लॉक नहीं किया जा सकता है।
- प्लेटफ़ॉर्म को श्रमिकों की मांगों का जवाब देना चाहिये, जैसे कि प्रति लेन-देन कमीशन शुल्क कम करना या श्रमिकों को अपने गैसोलीन बिलों के लिये अलग से भुगतान करने की आवश्यकता, जो ईंधन की कीमतों के साथ बढ़ रहे हैं और आय अपर्याप्तता की बढ़ती चिंताओं को संबोधित करना चाहिये।
- यह अध्ययन एप-आधारित श्रमिकों के लिये मज़बूत सामाजिक सुरक्षा और श्रमिकों की निगरानी के लिये प्लेटफॉर्मों द्वारा उपयोग किये जाने वाले एल्गोरिदम तथा तंत्र की निष्पक्षता पर सरकारी निगरानी की सिफारिश करता है।
गिग वर्कर कौन हैं?
- गिग वर्कर्स:
- गिग वर्कर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अस्थायी, लचीले आधार पर काम करते हैं, अक्सर कई ग्राहकों या कंपनियों के लिये कार्य करते हैं या सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- वे पारंपरिक कर्मचारियों के बजाय आम तौर पर स्वतंत्र ठेकेदार होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे कब, कहाँ और कैसे काम करते हैं, इस पर उनका अधिक नियंत्रण होता है।
- गिग इकोनॉमी:
- एक मुक्त बाज़ार प्रणाली जिसमें अस्थायी पद सामान्य होते हैं और संगठन अल्पकालिक कार्यों के लिये स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध करते हैं।
गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना क्यों आवश्यक है?
- आर्थिक सुरक्षा:
- 'केवल मांग-आधारित' प्रकृति के परिणामस्वरूप रोज़गार की सुरक्षा की कमी होती है और आय की निरंतरता से जुड़ी अनिश्चितता होती है, जिससे बेरोज़गारी बीमा, विकलांगता कवरेज़ तथा सेवानिवृत्ति बचत कार्यक्रमों जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना और भी उचित हो जाता है।
- अधिक उत्पादक कार्यबल:
- नियोक्ता-प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा और अन्य स्वास्थ्य देखभाल लाभों तक पहुँच का अभाव गिग वर्कर्स को अप्रत्याशित चिकित्सा खर्चों के प्रति संवेदनशील बनाता है। उनके स्वास्थ्य एवं कल्याण को प्राथमिकता देने से एक स्वस्थ और अधिक उत्पादक कार्यबल का निर्माण हो सकेगा।
- अवसरों की समता:
- पारंपरिक रोज़गार सुरक्षा से अपवर्जन असमानता पैदा करती है, जहाँ गिग वर्कर्स को शोषणकारी कार्य दशाओं और अपर्याप्त मुआवज़े का सामना करना पड़ता है। सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने से एकसमान अवसर का निर्माण होगा।
- दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा:
- नियोक्ता-प्रायोजित सेवानिवृत्ति योजनाओं के बिना गिग वर्कर्स अपने भविष्य के लिये पर्याप्त बचत कर सकने में अक्षम हो सकते हैं। गिग वर्कर्स को सेवानिवृत्ति के लिये बचत करने में सक्षम बनाने से उनके लिये भविष्य की वित्तीय कठिनाई और सार्वजनिक सहायता कार्यक्रमों पर निर्भर होने का जोखिम कम होगा।
गिग कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की राह की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?
- वर्गीकरण और अतिरिक्त लचीलापन:
- स्वरोज़गार और निर्भर-रोज़गार के बीच की धुंधली सीमाएँ तथा कई फर्मों के लिये कार्य कर सकने या अपनी इच्छा से नौकरी छोड़ सकने की स्वतंत्रता, गिग वर्कर्स के प्रति कंपनी दायित्वों की सीमा निर्धारित करना कठिन बना देती है।
- गिग इकोनॉमी को इसके लचीलेपन के लिये जाना जाता है, जहाँ कामगारों को यह तय करने की अनुमति मिलती है कि वे कब, कहाँ और कितना कार्य करें।
- इस लचीलेपन को समायोजित कर सकने और गिग वर्कर्स की विविध आवश्यकताओं को पूरा कर सकने वाले सामाजिक सुरक्षा लाभों को डिज़ाइन करना एक जटिल कार्य है।
- गिग इकोनॉमी को इसके लचीलेपन के लिये जाना जाता है, जहाँ कामगारों को यह तय करने की अनुमति मिलती है कि वे कब, कहाँ और कितना कार्य करें।
- स्वरोज़गार और निर्भर-रोज़गार के बीच की धुंधली सीमाएँ तथा कई फर्मों के लिये कार्य कर सकने या अपनी इच्छा से नौकरी छोड़ सकने की स्वतंत्रता, गिग वर्कर्स के प्रति कंपनी दायित्वों की सीमा निर्धारित करना कठिन बना देती है।
- वित्तपोषण और लागत वितरण:
- पारंपरिक सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ नियोक्ता और कर्मचारी के योगदान पर निर्भर करती हैं, जहाँ नियोक्ता आमतौर पर लागत के एक उल्लेखनीय भाग का वहन करते हैं।
- गिग इकॉनमी, जहाँ कर्मचारी प्रायः स्व-नियोजित होते हैं, के लिये एक उपयुक्त वित्तपोषण तंत्र की पहचान करना जटिल हो जाता है।
- पारंपरिक सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ नियोक्ता और कर्मचारी के योगदान पर निर्भर करती हैं, जहाँ नियोक्ता आमतौर पर लागत के एक उल्लेखनीय भाग का वहन करते हैं।
- समन्वय एवं डेटा साझाकरण:
- विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिये गिग वर्कर्स के आय अर्जन, योगदान एवं पात्रता का सटीक आकलन करने के लिये गिग प्लेटफॉर्म, सरकारी एजेंसियों तथा वित्तीय संस्थानों के बीच कुशल डेटा साझाकरण और समन्वयन आवश्यक है।
- लेकिन गिग वर्कर्स प्रायः कई प्लेटफॉर्म या क्लाइंट्स के लिये कार्य करते हैं, जिससे इस संदर्भ में समन्वय करना और उचित कवरेज सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिये गिग वर्कर्स के आय अर्जन, योगदान एवं पात्रता का सटीक आकलन करने के लिये गिग प्लेटफॉर्म, सरकारी एजेंसियों तथा वित्तीय संस्थानों के बीच कुशल डेटा साझाकरण और समन्वयन आवश्यक है।
- शिक्षा और जागरूकता:
- कई गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा लाभों के संबंध में अपने अधिकारों और पात्रता से अनभिज्ञ भी हो सकते हैं।
- इनकी जागरूकता बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा, पात्रता मानदंड एवं आवेदन प्रक्रिया के महत्त्व के बारे में शिक्षित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
- कई गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा लाभों के संबंध में अपने अधिकारों और पात्रता से अनभिज्ञ भी हो सकते हैं।
गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किया जा सकता है?
- सामाजिक सुरक्षा पर संहिता कार्यान्वयन, 2020:
- हालाँकि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में गिग श्रमिकों के लिये प्रावधान शामिल हैं, नियम अभी तक राज्यों द्वारा तैयार नहीं किये गए हैं और साथ ही बोर्ड की स्थापना के संदर्भ में बहुत कुछ नहीं हुआ है। अतः सरकार को इन पर शीघ्रता से कार्य करना चाहिये।
- अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों को अपनाना:
- यूके ने गिग श्रमिकों को "श्रमिक" के रूप में वर्गीकृत करके एक मॉडल स्थापित किया है, जो कर्मचारियों और स्व-रोज़गार के बीच की एक श्रेणी है।
- इससे उन्हें न्यूनतम वेतन, सवैतनिक छुट्टियाँ, सेवानिवृत्ति लाभ योजनाएँ और स्वास्थ्य बीमा प्राप्त होता है।
- इसी प्रकार इंडोनेशिया में वे दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा एवं मृत्यु बीमा के होते हैं।
- यूके ने गिग श्रमिकों को "श्रमिक" के रूप में वर्गीकृत करके एक मॉडल स्थापित किया है, जो कर्मचारियों और स्व-रोज़गार के बीच की एक श्रेणी है।
- नियोक्ता उत्तरदायित्वों का विस्तार:
- गिग श्रमिकों हेतु मज़बूत समर्थन उन गिग कंपनियों से आना चाहिये जो स्वयं इस जटिल एवं कम लागत वाली कार्य व्यवस्था से लाभान्वित होती हैं।
- गिग श्रमिकों को स्व-रोज़गार अथवा स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में वर्गीकृत करने की प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता है।
- कंपनियों को नियमित कर्मचारी के समान लाभ दिया जाना चाहिये।
- गिग श्रमिकों हेतु मज़बूत समर्थन उन गिग कंपनियों से आना चाहिये जो स्वयं इस जटिल एवं कम लागत वाली कार्य व्यवस्था से लाभान्वित होती हैं।
- सरकारी समर्थन:
- सरकार को शिक्षा, वित्तीय सलाहकार, कानूनी, चिकित्सा अथवा ग्राहक प्रबंधन क्षेत्रों जैसे उच्च कौशल वाले गिग कार्यों में व्यवस्थित रूप से निर्यात बढ़ाने में निवेश करना चाहिये; भारतीय गिग श्रमिकों हेतु वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच को आसान बनाकर।
- साथ ही सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की ज़िम्मेदारी साझा करने हेतु निष्पक्ष एवं पारदर्शी तंत्र स्थापित करने के लिये सरकारों, गिग प्लेटफॉर्मों एवं श्रमिक संगठनों के बीच सहयोग की आवश्यकता होगी।
गिग श्रमिकों से संबंधित सरकार की पहल:
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में 'गिग इकॉनमी' पर एक अलग खंड शामिल है और साथ ही गिग नियोक्ताओं पर सरकार के नेतृत्व वाले बोर्ड द्वारा प्रबंधित सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान करने का दायित्व भी दिया गया है।
- वेतन संहिता, 2019 गिग श्रमिकों सहित संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन एवं आधारभूत वेतन प्रदान करता है।
निष्कर्ष
एप-आधारित श्रमिकों की कार्य स्थितियों, वित्तीय सुरक्षा एवं समग्र कल्याण में सुधार हेतु व्यापक उपायों की आवश्यकता है, उनके अधिकारों तथा सुरक्षा की वकालत करते हुए गिग अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को मान्यता दी जाए।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. भारत में महिलाओं के सशक्तीकरण की प्रक्रिया में 'गिग इकॉनमी' की भूमिका का परीक्षण कीजिये। (2021) |

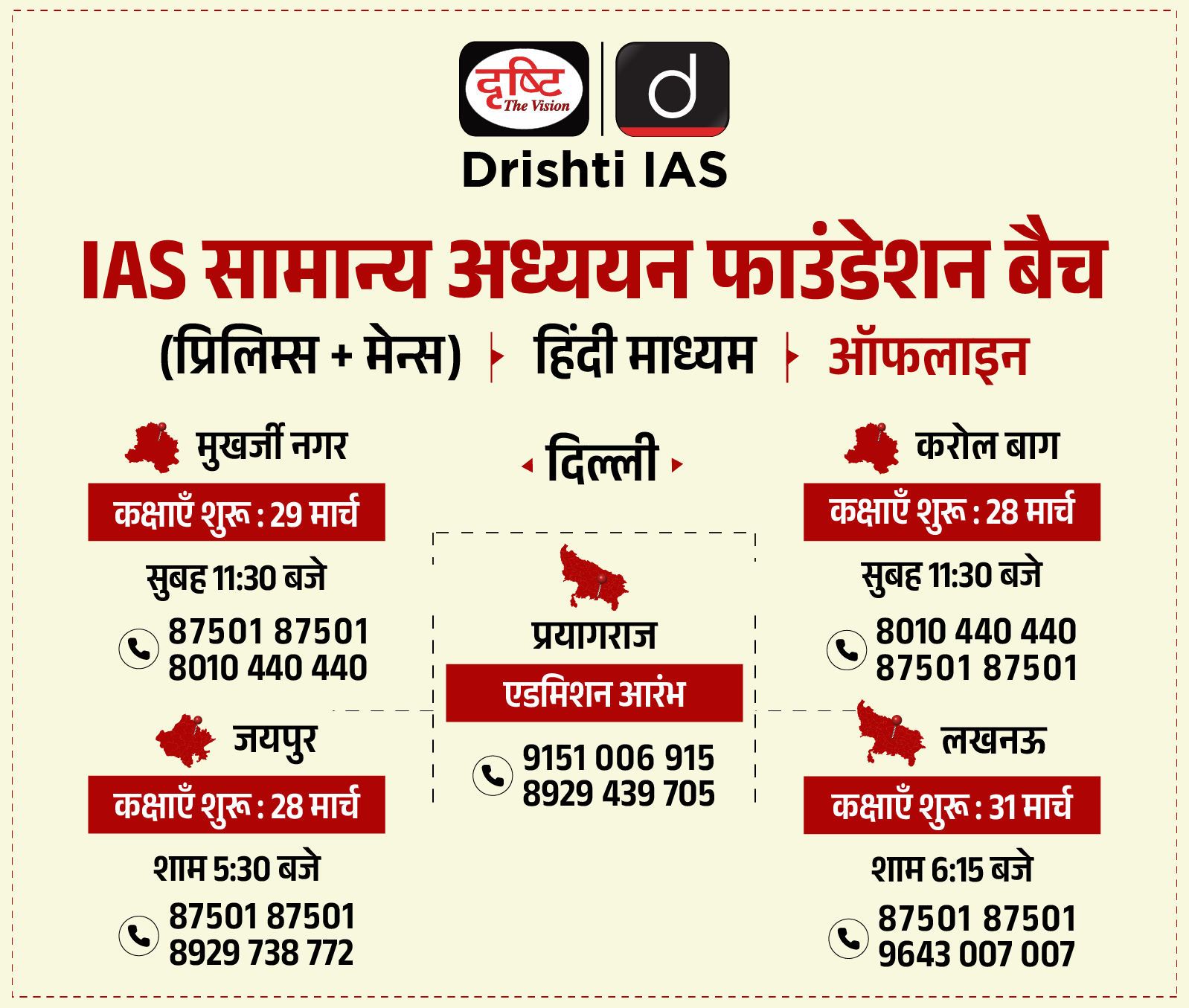
सामाजिक न्याय
लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी
प्रिलिम्स के लिये:सतत् विकास लक्ष्य, लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी, बाल मृत्यु अनुमान के लिये संयुक्त राष्ट्र अंतर-एजेंसी समूह, पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर (U5MR)। मेन्स के लिये:लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी,भारत में मृत-जन्म तथा बाल मृत्यु दर से संबंधित मुद्दे। |
स्रोत: डाउन टू अर्थ
चर्चा में क्यों?
हाल ही में बाल मृत्यु दर अनुमान के लिये संयुक्त राष्ट्र अंतर-एजेंसी समूह द्वारा “लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की वार्षिक संख्या वर्ष 2000 के अनुमान से आधे से अधिक कम (9.9 मिलियन से 4.9 मिलियन तक) हो गई है।
रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं?
- बाल मृत्यु दर में ऐतिहासिक कमी:
- वर्ष 2022 में पाँच वर्ष से कम आयु में होने वाली मौतों की वार्षिक संख्या घटकर 4.9 मिलियन हो गई, जो बाल मृत्यु दर को कम करने के वैश्विक प्रयास में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।
- यह वर्ष 2000 के बाद से वैश्विक स्तर पर पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर (U5MR) में आधे से अधिक की गिरावट के साथ जुड़ा हुआ है।
- सरकारों, संगठनों, स्थानीय समुदायों, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों एवं परिवारों सहित विभिन्न हितधारकों की निरंतर प्रतिबद्धता के कारण, पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में गिरावट लगातार बनी हुई है।
- मृत्यु दर का लगातार उच्च होना:
- प्रगति के बावजूद बच्चों, किशोरों एवं युवाओं के बीच वार्षिक मृत्यु दर अस्वीकार्य रूप से अधिक बनी हुई है।
- वर्ष 2022 में जीवन के पहले महीने के दौरान पाँच वर्ष से कम उम्र के 2.3 मिलियन बच्चों की मृत्यु हो गई तथा 1 से 59 महीने की उम्र के बीच अतिरिक्त 2.6 मिलियन बच्चों की मृत्यु हो गई।
- इसके अतिरिक्त 5 से 24 वर्ष की आयु के 2.1 मिलियन बच्चों, किशोरों तथा युवाओं की भी मृत्यु हुई।
- बड़ी संख्या में जीवन की हानि:
- वर्ष 2000 से वर्ष 2022 के बीच विश्व के 221 मिलियन बच्चों, किशोरों तथा युवाओं की मृत्यु हुई, जिसकी तुलना नाइजीरिया की लगभग पूरी आबादी से की जा सकती है।
- नवजात शिशुओं की मृत्यु (जन्म के 28 दिनों के भीतर शिशु की मृत्यु) के कारण पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु 72 मिलियन थी और 1-59 महीने की आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या 91 मिलियन थी।
- नवजात अवधि में पाँच साल से कम उम्र की मृत्यु की प्रवृत्ति 2000 में 41% से बढ़कर वर्ष 2022 में 47% हो गई है।
- वर्ष 2000 से वर्ष 2022 के बीच विश्व के 221 मिलियन बच्चों, किशोरों तथा युवाओं की मृत्यु हुई, जिसकी तुलना नाइजीरिया की लगभग पूरी आबादी से की जा सकती है।
- उत्तरजीविता की संभावनाओं में असमानता:
- बच्चों को भौगोलिक स्थिति, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और चाहे वे नाज़ुक या संघर्ष-प्रभावित सेटिंग्स में रहते हों, जैसे कारकों के आधार पर जीवित रहने की असमान संभावनाओं का सामना करना पड़ता है।
- ये असमानताएँ बच्चों की कमज़ोर आबादी के बीच लगातार और गहरी असमानताओं को उजागर करती हैं।
- क्षेत्रीय असमानताएँ:
- जबकि बाल मृत्यु दर की वैश्विक दर में गिरावट आ रही है, महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानताएँ हैं।
- वर्ष 2030 से पहले 5 वर्ष से कम उम्र के 35 मिलियन बच्चे अपनी जान गँवा देंगे और उप-सहारा अफ्रीका में सबसे अधिक मौतें होंगी।
- देश संयुक्त राष्ट्र-अनिवार्य सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goal - SDG) लक्ष्यों को समय पर पूरा नहीं करेंगे।
- हालाँकि यदि प्रत्येक देश ने पाँच साल से कम उम्र की बच्चों की रोकी जा सकने वाली मौतों को समाप्त करने के SDG-5 दृष्टिकोण को महसूस किया और समय पर प्रासंगिक मृत्यु दर लक्ष्यों को पूरा किया, तो 9 मिलियन से अधिक बच्चे पाँच वर्ष की आयु तक जीवित रहेंगे।
- मौजूदा रुझानों के तहत 59 देश पाँच मृत्यु दर लक्ष्य के तहत सतत् विकास लक्ष्य से चूक जाएँगे और 64 देश नवजात मृत्यु दर लक्ष्य से चूक जाएँगे।
- जबकि बाल मृत्यु दर की वैश्विक दर में गिरावट आ रही है, महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानताएँ हैं।
- अनुशंसाएँ:
- कई निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों ने पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में वैश्विक गिरावट से बेहतर प्रदर्शन किया है, कुछ मामलों में 2000 के बाद से उनकी दरों में दो तिहाई से अधिक की कमी आई है।
- जब मातृ, नवजात शिशु और बाल स्वास्थ्य तथा उत्तरजीविता में निवेश किया जाता है तो ये प्रेरक परिणाम उच्च रिटर्न दर्शाते हैं।
- वे इस बात का महत्त्वपूर्ण प्रमाण भी प्रदान करते हैं कि यदि संसाधन की कमी वाली स्थितियों में भी सतत् और रणनीतिक कार्रवाई की जाती है, तो पाँच साल से कम उम्र की मृत्यु दर के स्तर तथा रुझान में बदलाव आएगा एवं जीवन बचाया जाएगा।
- कई निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों ने पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में वैश्विक गिरावट से बेहतर प्रदर्शन किया है, कुछ मामलों में 2000 के बाद से उनकी दरों में दो तिहाई से अधिक की कमी आई है।
बाल मृत्यु दर को रोकने हेतु क्या किया जा सकता है?
- परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुँच: व्यापक परिवार नियोजन सेवाएँ प्रदान करने से अनपेक्षित गर्भधारण को रोकने में मदद मिल सकती है, जिससे समय से पहले जन्म और मृत जन्म के जोखिम को कम किया जा सकता है।
- प्रसवपूर्व सेवाओं में सुधार: गर्भवती महिलाओं के लिये नियमित स्वास्थ्य और पोषण जाँच सहित प्रसवपूर्व देखभाल सेवाओं को बढ़ाने से स्वस्थ गर्भधारण में योगदान हो सकता है तथा समय से पहले जन्म एवं मृत जन्म की संभावना कम हो सकती है।
- गर्भवती माताओं के लिये आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण तक पहुँच सुनिश्चित करने से मातृ और भ्रूण के स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है।
- जोखिम कारकों की पहचान और प्रबंधन: समय से पहले जन्म तथा मृत जन्म से जुड़े जोखिम कारकों की पहचान एवं प्रबंधन के लिये प्रभावी स्क्रीनिंग कार्यक्रम लागू करने से प्रतिकूल परिणामों को कम करने में मदद मिल सकती है।
- इसमें गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप, मधुमेह और संक्रमण जैसी स्थितियों का प्रबंधन शामिल है।
- डेटा रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग में सुधार: समय से पहले जन्म तथा मृत जन्म को सटीक रूप से रिकॉर्ड करने एवं रिपोर्ट करने के लिये डेटा संग्रह प्रणालियों को बढ़ाना समस्या की भयावहता को समझने व लक्षित हस्तक्षेपों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- प्रसवकालीन मृत्यु दर की रिपोर्ट करने के लिये रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण जैसे मानकीकृत वर्गीकरण प्रणालियों को अपनाने से डेटा की गुणवत्ता और तुलनीयता में सुधार हो सकता है।
- निगरानी दिशा-निर्देश लागू करना: मातृ और प्रसवकालीन मृत्यु निगरानी दिशा-निर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने से प्रवृत्तियों, जोखिम कारकों तथा हस्तक्षेप के अवसरों की पहचान करने में मदद मिल सकती है।
- इसमें नीति और अभ्यास को सूचित करने के लिये मातृ तथा प्रसवकालीन मौतों की समय पर रिपोर्टिंग तथा विश्लेषण शामिल है।
महिलाओं के पोषण और बाल मृत्यु दर को रोकने हेतु भारत की पहल क्या हैं?
- पोषण अभियान: भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक "कुपोषण मुक्त भारत" सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय पोषण मिशन (NNM) या पोषण अभियान प्रारंभ किया है।
- इसके अलावा पोषण अभियान, मिशन सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0 की प्रभावशीलता तथा दक्षता को बढ़ाने के लिये, सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों हेतु बजट 2021-2022 में एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम की घोषणा की गई थी।
- शासन में सुधार के लिये पोषण ट्रैकर के अंतर्गत पोषण गुणवत्ता में सुधार और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण, वितरण को सुदृढ़ करने तथा प्रौद्योगिकी के इष्टतम प्रयोग के लिये उपाय किये गए हैं।
- एनीमिया मुक्त भारत अभियान: वर्ष 2018 में शुरू किये गए इस मिशन का लक्ष्य एनीमिया की वार्षिक गिरावट दर में सुधार करते हुए इसमें एक से तीन प्रतिशत अंक की वृद्धि करना है।
- मिशन शक्ति: 'मिशन शक्ति' में महिलाओं की सुरक्षा और महिला सशक्तीकरण के लिये क्रमशः दो उप-योजनाएँ 'संबल' तथा 'सामर्थ्य' शामिल हैं।
- वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन (181-WHL), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी अदालत जैसी योजनाएँ 'संबल' उप-योजना का हिस्सा हैं।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पालना, शक्ति सदन, सखी निवास और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये हब के घटक 'सामर्थ्य' उप-योजना का हिस्सा हैं।
- एकीकृत बाल विकास सेवा योजना: इसे वर्ष 1975 में शुरू किया गया था और इस योजना का उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा उनकी माताओं को भोजन, प्रीस्कूल शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच एवं रेफरल सेवाएँ प्रदान करना है।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-से 'राष्ट्रीय पोषण मिशन (नेशनल न्यूट्रिशन मिशन)' के उद्देश्य हैं? (2017)
नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न. क्या लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुश्चक्र को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनेंस) प्रदान करके तोड़ा जा सकता है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिये। (2021) |