हरियाणा Switch to English
हरियाणा वन जनगणना
चर्चा में क्यों?
पहली राज्य-व्यापी वृक्ष गणना के अनुसार, हरियाणा में निर्दिष्ट वनों के बाहर लगभग 4.1 करोड़ पेड़ हैं, जिनमें नीम, शीशम, पीपल, बरगद और नीलगिरी सबसे सामान्य प्रजातियाँ हैं।
मुख्य बिंदु:
- राज्य में हरित आवरण प्रबंधन के संबंध में सुविज्ञ निर्णय लेने में अधिकारियों की सहायता के लिये लगभग 150 सर्वेक्षक, टैक्सोनोमिस्ट और तकनीकी कर्मचारी 13 महीने की अवधि के लिये परियोजना में लगे हुए थे।
- यह वन क्षेत्रों के बाहर प्रत्येक ज़िले में वृक्षों की संख्या पर डेटा प्रदान करता है। वृक्षों की सबसे अधिक संख्या यमुनानगर, अंबाला, सिरसा, भिवानी और हिसार में पाई गई।
- फरीदाबाद की गिनती सबसे कम थी, इसके बाद कुरुक्षेत्र, पलवल, गुड़गाँव और रोहतक थे।
- अपने कुल क्षेत्रफल का केवल 6.7% हिस्सा कवर करने वाले हरियाणा में भारत में सबसे कम वन और वृक्ष क्षेत्र है। राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य प्रत्येक राज्य के लिये 20% कवरेज का है।
- हरियाणा के 22 ज़िलों में से 21 में 20% से कम वन और वृक्ष आवरण है।
- करनाल 1.8% के साथ सबसे निचले स्थान पर है, पंचकुला 47.4% के साथ सूची में शीर्ष पर है और गुड़गाँव 12.9% के साथ छठे स्थान पर है।
- भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में वृक्ष आवरण में भी तेज़ी से गिरावट देखी जा रही है, वर्ष 2019 से 2020 तक वृक्ष आवरण (वन क्षेत्र को छोड़कर) में 140 वर्ग किमी. की कमी आई है।
- वन विभाग के अधिकारी जनगणना डेटा का उपयोग करके संरक्षण प्रयासों को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं।
- वे इस तर्क का समर्थन कर रहे हैं कि सरकार कम-से-कम 25% पंचायत और सामान्य भूमि वृक्षारोपण के लिये निर्धारित करे, संस्थानों को अपने क्षेत्र का 33% वृक्ष कवर के तहत रखना चाहिये तथा शहरी स्थानीय निकायों को हैदराबाद की पहल से प्रेरणा लेते हुए शहरों में हरित स्थान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
- उच्च गुणवत्ता वाले पौधों के महत्त्व पर ज़ोर देते हुए, अधिकारियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वृक्षों के अस्तित्व और विकास को सुनिश्चित करने हेतु उनका उपयोग करना महत्त्वपूर्ण है।
राष्ट्रीय वन नीति
- भारत के वन वर्तमान में राष्ट्रीय वन नीति, 1988 द्वारा शासित होते हैं
- इसके केंद्र में पर्यावरण संतुलन और आजीविका है।
- मुख्य विशेषताएँ और लक्ष्य:
- पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण और बहाली के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखना
- प्राकृतिक विरासत का संरक्षण (मौजूदा)।
- नदियों, झीलों और जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा के कटाव तथा अनाच्छादन की जाँच करना।
- राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों और तटीय इलाकों में रेत के टीलों के विस्तार की जाँच करना।
- वनीकरण और सामाजिक वानिकी के माध्यम से वन/वृक्ष आवरण में पर्याप्त वृद्धि करना।
- ग्रामीण और जनजातीय जनसंख्या की ईंधन, लकड़ी, चारा, लघु वन उपज, मृदा तथा इमारती लकड़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कदम उठाना।
- राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वनों की उत्पादकता बढ़ाना।
- वन उपज के कुशल उपयोग और लकड़ी के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- कार्य के अवसरों का सृजन, महिलाओं की भागीदारी।
भारतीय वन सर्वेक्षण
- भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI), देहरादून वर्ष 1987 से वन आवरण का द्विवार्षिक (प्रत्येक दो वर्ष में एक बार) आकलन कर रहा है और निष्कर्ष भारत राज्य वन रिपोर्ट (ISFR) में प्रकाशित किये जाते हैं।
- ISFR 2021 के नवीनतम आकलन के अनुसार, भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है।
- विशेष रूप से, यह ISFR 2019 मूल्यांकन की तुलना में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्शाता है जो वन संरक्षण प्रयासों में सकारात्मक प्रगति का संकेत देता है।
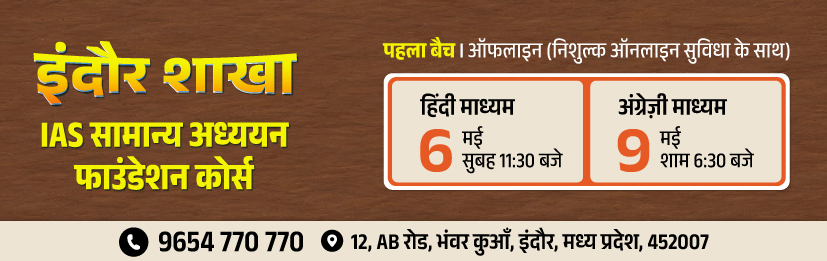
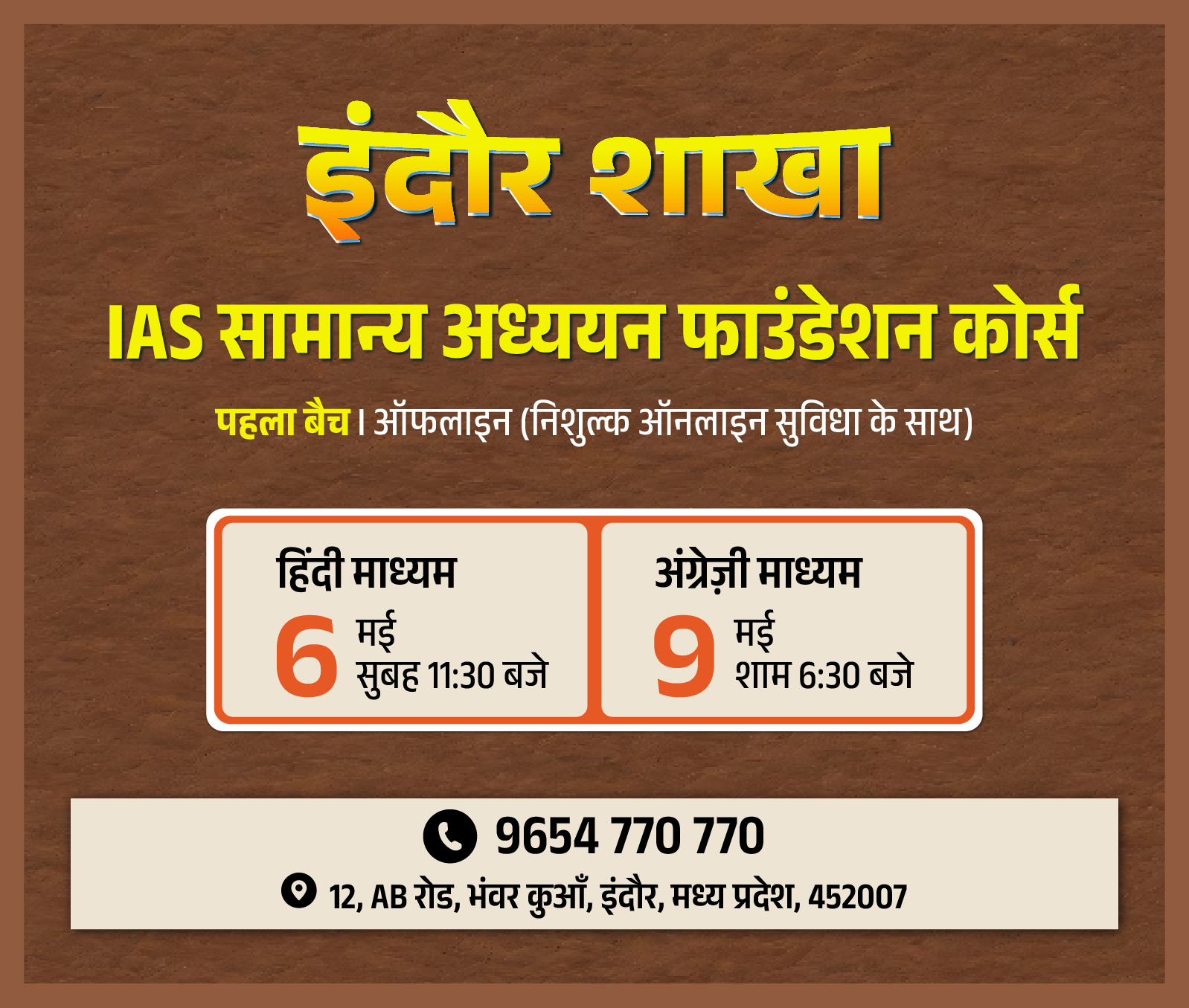
हरियाणा Switch to English
भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (AFI)
चर्चा में क्यों?
भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय अंतर-ज़िला जूनियर एथलेटिक्स मीट के लिये टीमें भेजने में विफल रहने पर पूरे देश के 16 ज़िला संघों की मान्यता रद्द कर दी है।
मुख्य बिंदु:
- असंबद्ध ज़िले (राज्य/केंद्रशासित प्रदेश संघ के नाम के साथ): पंचकुला (हरियाणा), बडगाम, रामबन एवं शोपियाँ (सभी जम्मू-कश्मीर), लोहरदगा (झाकड़ी), कल्पेनी (लक्षद्वीप), पूर्वी जैंतिया हिल्स, पूर्वी खासी हिल्स एवं री-भोई ( सभी मेघालय), हरदा व नीमच (दोनों MP), फिरोज़पुर और फाजिल्का (दोनों पंजाब), झालावाड़ (राजस्थान), कृष्णागिरी (TN), पुरबा मेदिनीपुर (WB)।
- AFI संविधान के अनुसार, निलंबित ज़िलों को हटा दिया जाएगा और नए संघ बनाए जाएंगे।
- राज्य संघों को AFI के परामर्श से उचित कार्रवाई करने और नई ज़िला इकाइयाँ बनाने के लिये कहा गया है।
भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (AFI)
- यह भारत में एथलेटिक्स के संचालन और प्रबंधन के लिये सर्वोच्च संस्था है।
- यह एक गैर-सरकारी और गैर-लाभकारी स्वायत्त निकाय है।
- यह विश्व एथलेटिक्स, एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन (AAA) और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन से संबद्ध है।
- इसे पहले एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया (AAFI) कहा जाता था।
- AFI की लगभग 32 संबद्ध राज्य इकाइयाँ और संस्थागत इकाइयाँ हैं।
- AFI की लगभग 32 संबद्ध राज्य इकाइयाँ और संस्थागत इकाइयाँ हैं।
- यह वर्ष 1946 में अस्तित्त्व में आया और यह महासंघ राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन करता है, भारतीय एथलेटिक्स राष्ट्रीय शिविरार्थियों को प्रशिक्षित करता है, ओलंपिक, एशियाई खेलों, CWG, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई चैंपियनशिप तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैठकें, विभिन्न आयु वर्गों के लिये राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित करता है।
- AFI खेल को बढ़ावा देने, इसे जनता के बीच लोकप्रिय बनाने और एथलीट व खेल के आगे विकास के लिये एथलेटिक्स को व्यावसायिक रूप से आकर्षक बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय चैंपियनशिप व विभिन्न बैठकें आयोजित करता है।
- महासंघ अपनी राज्य इकाइयों की गतिविधियों की देखरेख और सहायता भी करता है, विशेष कोचिंग शिविरों की योजना बनाता है तथा स्थापित करता है। यह प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देता है और भारत में एथलेटिक्स के विकास कार्यक्रमों तथा ज़मीनी स्तर पर प्रचार के लिये पहल करता है।
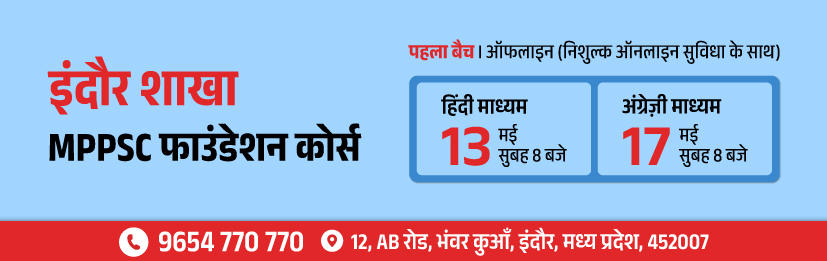

उत्तर प्रदेश Switch to English
GI टैग में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर
चर्चा में क्यों?
छह नए उत्पादों के साथ, उत्तर प्रदेश ने भारत में सर्वाधिक 75 भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication - GI) टैग वाले उत्पादों वाले राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है।
मुख्य बिंदु:
- इसमें काशी की प्रसिद्ध 'तिरंगी बर्फी' शामिल है, जो एक तिरंगे रंग की मिठाई है जिसका व्यापार भारत छोड़ो आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा एक बयान देने के लिये किया गया था।
- उत्तर प्रदेश में प्रमाणन प्राप्त करने वाले अन्य उत्पादों में बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, लखीमपुर खीरी थारू कढ़ाई, बरेली बेंत एवं बाँस शिल्प, बरेली ज़रदोज़ी शिल्प और पिलखुवा हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल शामिल हैं।
- इन छह नई वस्तुओं को शामिल करने के साथ उत्तर प्रदेश सबसे अधिक GI-टैग उत्पादों के साथ भारत का अग्रणी राज्य बना हुआ है।
- 58 GI उत्पादों के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है।
भौगोलिक संकेतक (GI) टैग
- परिचय:
- भौगोलिक संकेत (GI) टैग, एक ऐसा नाम या चिह्न है जिसका उपयोग उन विशेष उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं।
- GI टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्त्ताओं या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही लोकप्रिय उत्पाद के नाम का उपयोग करने की अनुमति है।
- यह उत्पाद को दूसरों द्वारा नकल या अनुकरण किये जाने से भी बचाता है।
- एक पंजीकृत GI टैग 10 वर्षों के लिये वैध होता है।
- GI पंजीकरण की देखरेख वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा की जाती है।
- विधिक ढाँचा तथा दायित्व:
- वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण तथा बेहतर संरक्षण प्रदान करने का प्रयास करता है।
- यह बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार-संबंधित पहलुओं (TRIPS) पर WTO समझौते द्वारा विनियमित एवं निर्देशित है।
- इसके अतिरिक्त बौद्धिक संपदा के अभिन्न घटकों के रूप में औद्योगिक संपत्ति और भौगोलिक संकेतों की सुरक्षा के महत्त्व को पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1(2) एवं 10 में स्वीकार किया गया, साथ ही इस पर अधिक बल दिया गया है।


उत्तर प्रदेश Switch to English
अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना
चर्चा में क्यों?
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (Indian Institute of Astrophysics- IIA) ने अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
मुख्य बिंदु:
- सूर्य तिलक परियोजना के तहत चैत्र मास में श्री राम नवमी के अवसर पर दोपहर 12 बजे श्री राम लला के माथे पर सूर्य की रोशनी लाई गई।
- IIA टीम ने सूर्य की स्थिति, ऑप्टिकल/प्रकाशिकी सिस्टम के डिज़ाइन व इष्टतम उपयोग की गणना की और साइट पर एकीकरण व संरेखण का प्रदर्शन किया।
- IIA टीम ने 19 वर्षों के एक चक्र के लिये श्री राम नवमी के कैलेंडर दिनों की पहचान हेतु गणना का नेतृत्व किया, इसके बाद इसकी पुनरावृत्ति, राम नवमी की कैलेंडर तिथियों पर आकाश में स्थिति का अनुमान लगाया।
- टीम ने मंदिर के शीर्ष से मूर्ति के माथे तक सूरज की रोशनी लाने के लिये एक ऑप्टो-मैकेनिकल प्रणाली के डिज़ाइन का भी नेतृत्व किया, सिस्टम में दर्पण और लेंस के आकार, आकृति तथा स्थान का निर्धारण लगाया ताकि लगभग 6 मिनट तक मूर्ति पर पर्याप्त रोशनी पड़ सके।
- डिवाइस का निर्माण ऑप्टिका, बैंगलोर द्वारा किया गया है और साइट पर ऑप्टो-मैकेनिकल सिस्टम का कार्यान्वयन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद- केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (CSIR-CBRI) द्वारा किया जा रहा है।
भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (Indian Institute of Astrophysics- IIA)
- IIA पूर्णतः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित भारत का एक प्रमुख शोध संस्थान है जो खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और संबंधित क्षेत्रों के अध्ययन के लिये समर्पित है
- इसमें कई ओब्ज़र्वेशन सुविधाएँ हैं, जिनमें तमिलनाडु के कवलूर में वेणु बप्पू वेधशाला, कर्नाटक में गौरीबिदानूर रेडियो वेधशाला और लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर में हनले वेधशाला शामिल हैं।


मध्य प्रदेश Switch to English
अश्वगंधा
चर्चा में क्यों?
अश्वगंधा की लोकप्रियता भारत और विदेश दोनों में बढ़ रही है। यह एक सदाबहार झाड़ी है जो भारत, अफ्रीका और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में पाई जाती है।
मुख्य बिंदु:
- अश्वगंधा (Withania somnifera) एक औषधीय जड़ी बूटी है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली औषधि के रूप में प्रतिष्ठित है।
- इसे एडाप्टोजेन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि यह शरीर में तनाव को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है।
- अश्वगंधा मस्तिष्क की कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है और रक्त शर्करा को कम करता है, साथ ही चिंता तथा अवसाद के लक्षणों से लड़ने में मदद करता है।
- अश्वगंधा ने तीव्र और दीर्घकालिक रुमेटाइड आर्थराइटिस यानी संधिशोथ/गठिया जो व्यक्ति के जोड़ों में विकृति व विकलांगता पैदा करती है, दोनों के उपचार में नैदानिक सफलता दिखाई है।
- रुमेटीइड गठिया (RA) एक ऑटोइम्यून रोग है जो आपके पूरे शरीर में जोड़ों के दर्द और क्षति का कारण बन सकती है।
- ऑटोइम्यून रोग एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अचेतन अवस्था में शरीर को प्रभावित करती है।
- अपने विशाल जैव यौगिकों के साथ सख्त और सूखा प्रतिरोधी प्रजाति होने के कारण, इसके उपयोग को हमेशा महत्त्व दिया जाता है तथा भारत के कई हिस्सों में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश में, इसका एकाधिकार बना हुआ है।
- यह उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शुष्क भागों में उगता है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश देश के प्रमुख अश्वगंधा उत्पादक राज्य हैं।
- मध्य प्रदेश में इसकी कृषि 5000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की जाती है।
- भारत में अश्वगंधा जड़ों का अनुमानित उत्पादन 1500 टन से अधिक है और वार्षिक आवश्यकता लगभग 7000 टन है, जिससे इसकी कृषि में वृद्धि तथा अधिक उत्पादन की आवश्यकता है।


उत्तराखंड Switch to English
उत्तराखंड में जलविद्युत परियोजना का पुनर्निर्माण
चर्चा में क्यों?
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने उत्तराखंड में हिमालय की ऊपरी गंगा क्षेत्र में एक जलविद्युत परियोजना के पुनर्निर्माण के लिये पर्यावरणीय मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो वर्ष 2013 में बड़े पैमाने पर हुए फ्लैश फ्लड के दौरान लगभग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी, जिसमें 6,000 से अधिक लोग मारे गए थे।
मुख्य बिंदु:
- नदी घाटी और जलविद्युत परियोजनाओं के लिये मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने फाटा ब्यूंग जलविद्युत परियोजना (76 मेगावाट) को संदर्भ की शर्तों (Terms of Reference- ToR) के अनुदान को मंज़ूरी दे दी।
- फाटा ब्यूंग परियोजना ने मंदाकिनी नदी के प्रवाह को अवरुद्ध करके वर्ष 2013 में बादल फटने (Cloudburst) और फ्लैश फ्लड से होने वाली क्षति को और भी बढ़ा दिया।
मंदाकिनी नदी
- यह उत्तराखंड में अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी है।
- यह नदी रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग क्षेत्रों के बीच लगभग 81 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है तथा चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है।
- मंदाकिनी सोनप्रयाग में सोनगंगा नदी में विलीन हो जाती है और उखीमठ में मध्यमहेश्वर मंदिर के पास से बहती है।
- अपने मार्ग के अंत में यह अलकनंदा में गिरती है, जो गंगा में मिल जाती है।



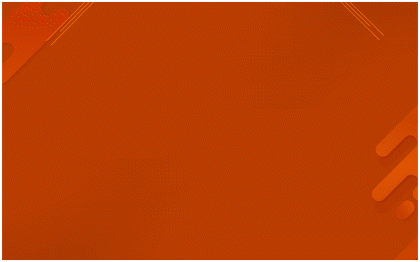


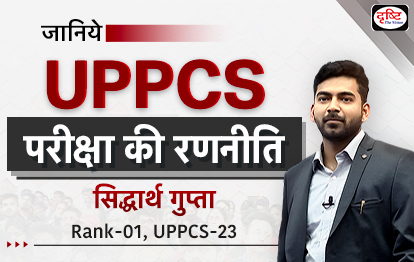
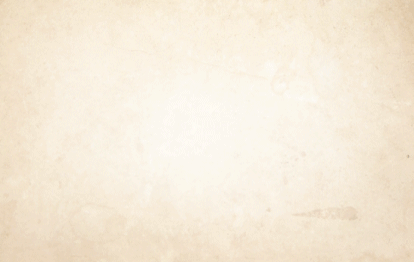
.jpg)
.jpg)
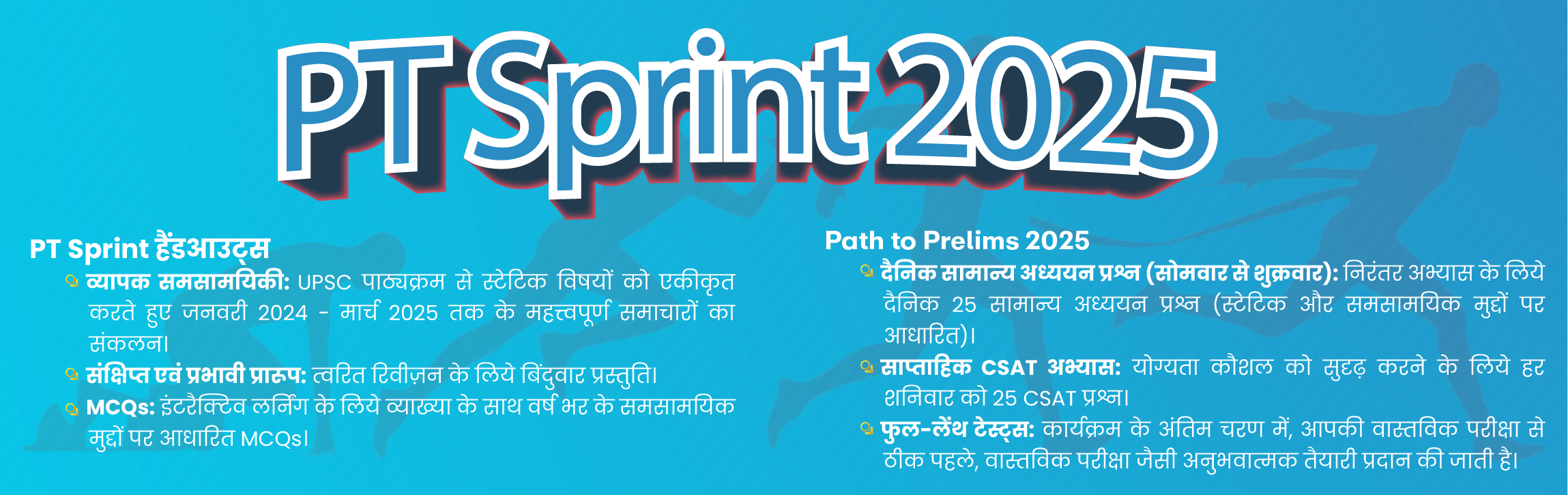
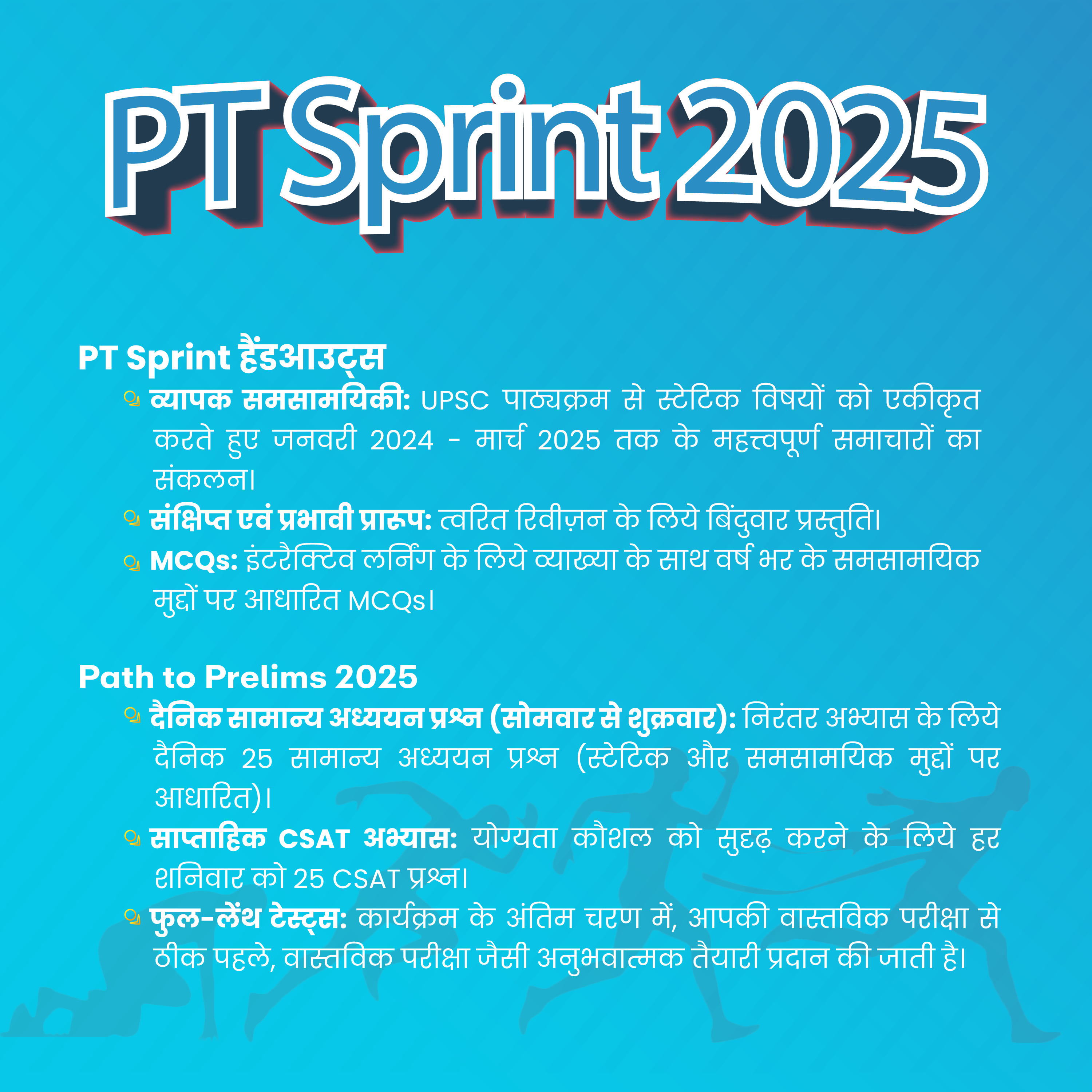

%201.jpeg)
.jpg)


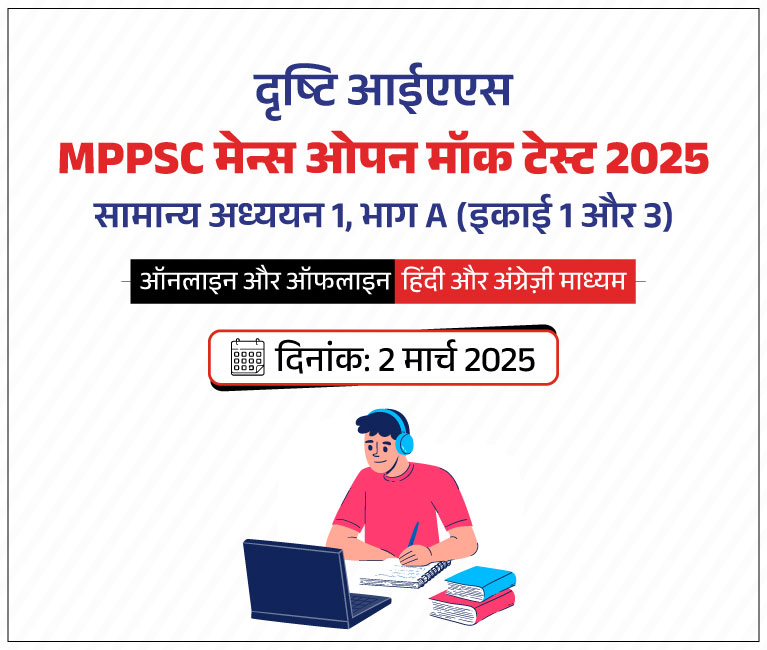
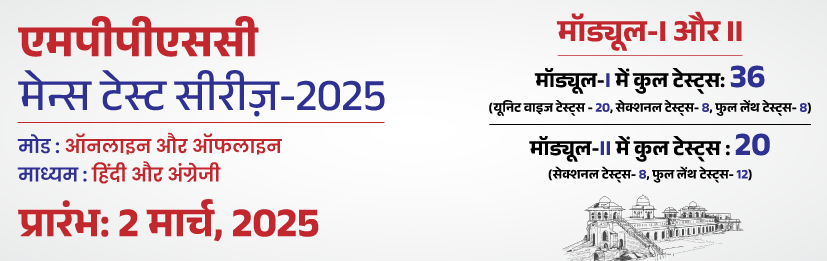

%20MPPCS%202025%20Desktop%20H.jpg)
%20MPPCS%202025%20Mobile%20H%20(1).jpg)

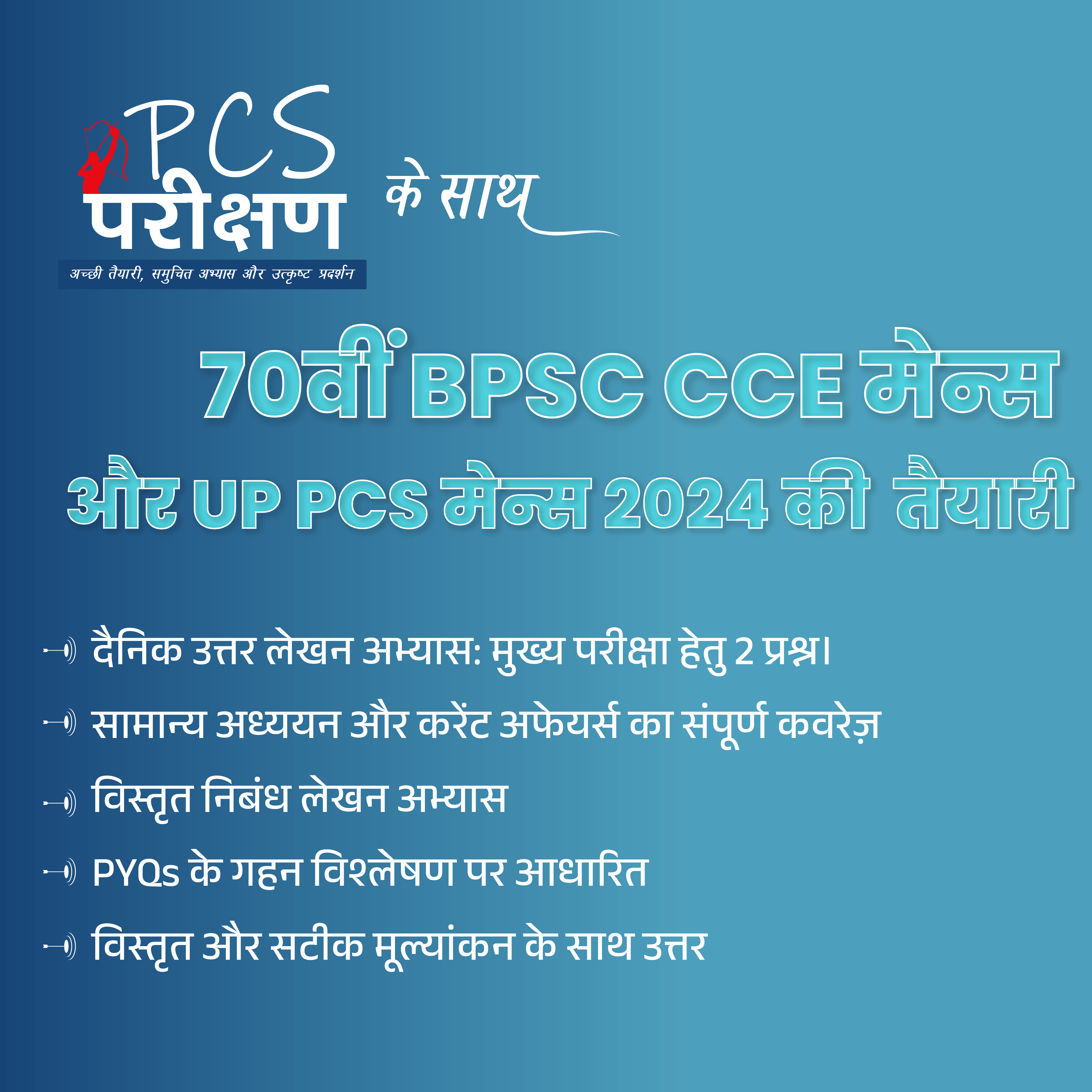


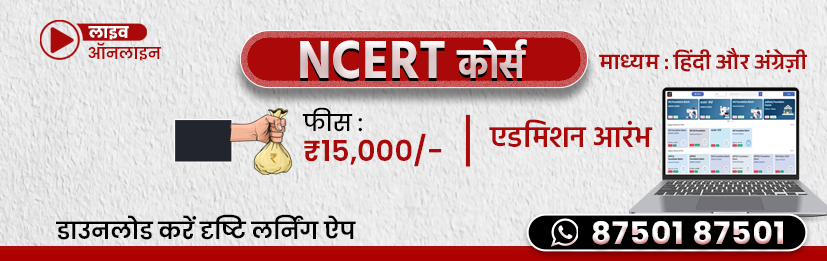
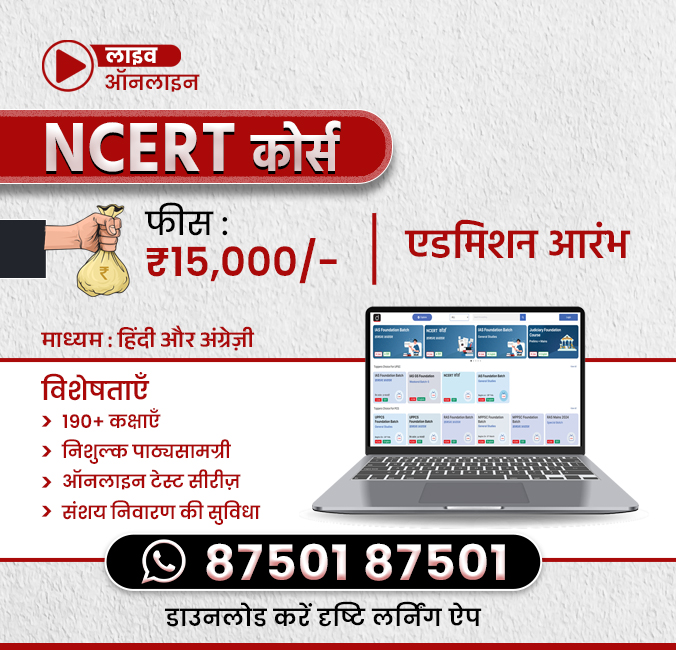

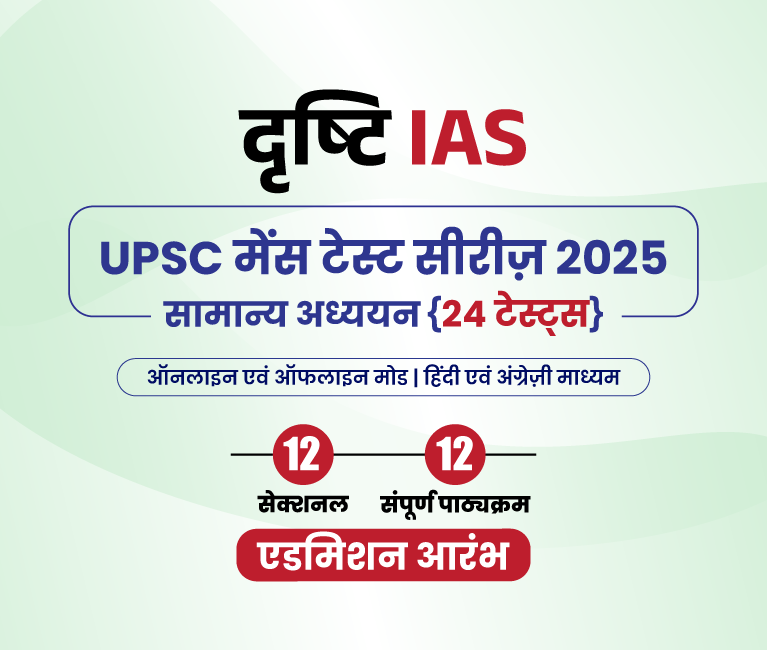
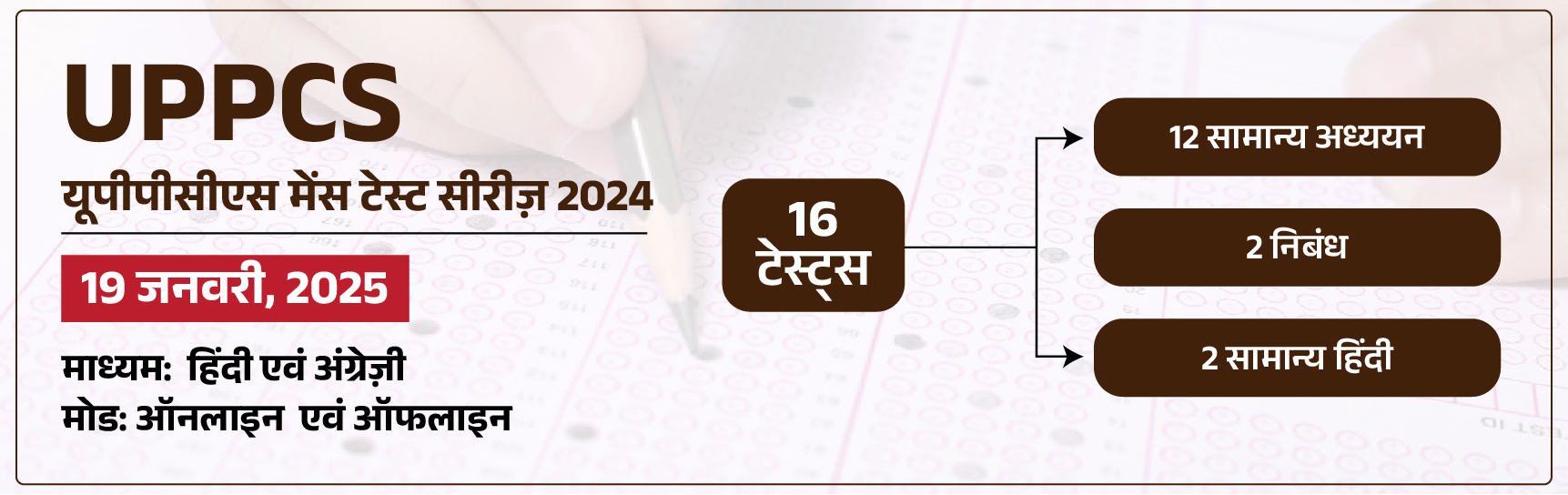
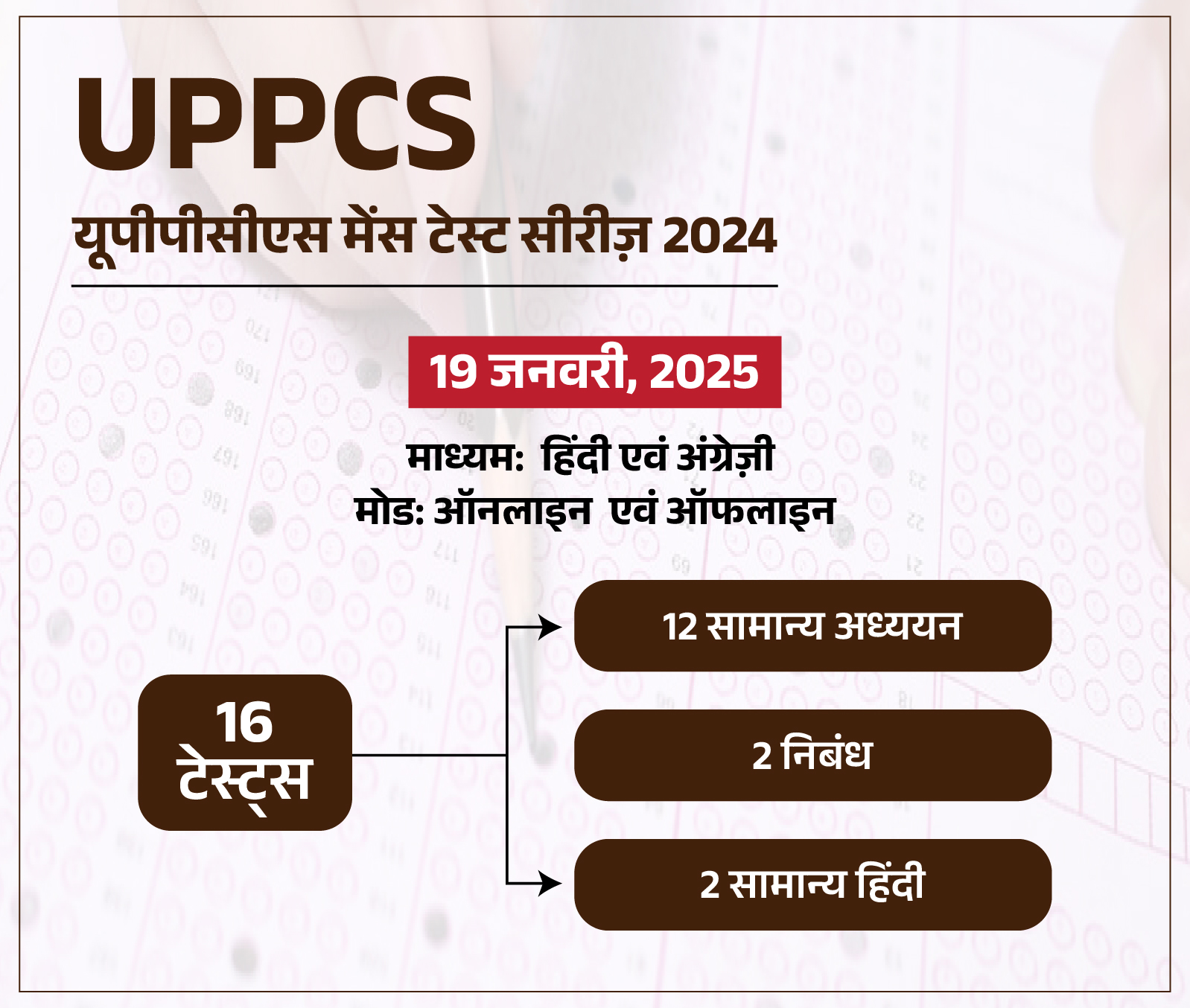



 PCS परीक्षण
PCS परीक्षण


