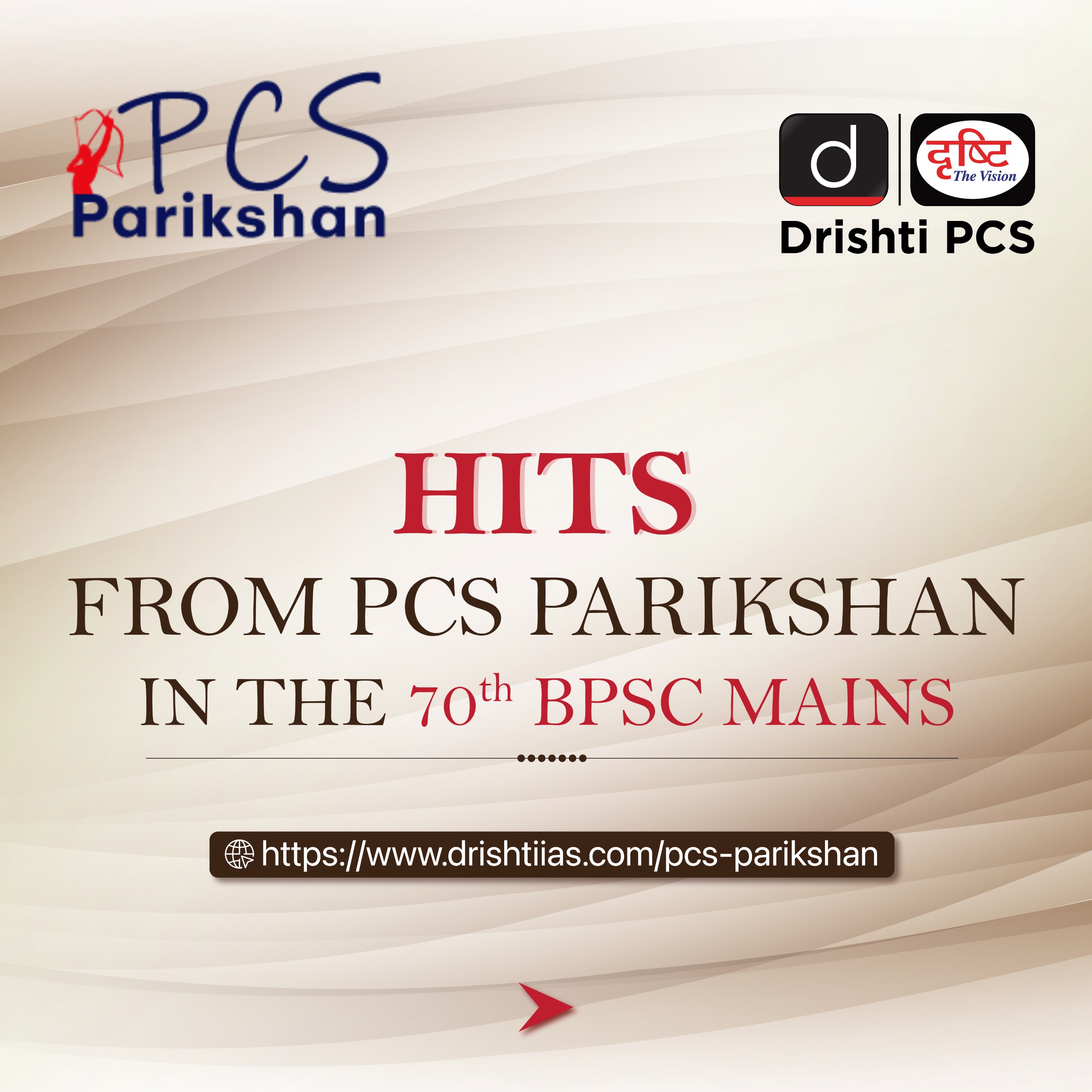भारतीय अर्थव्यवस्था
भारत का आर्थिक विकास परिदृश्य
यह एडिटोरियल 31/05/2024 को ‘इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित “India’s economy: From stable to positive” लेख पर आधारित है। इसमें भारत के बारे में S&P Global के अनुमान में सुधार की चर्चा की गई है, जहाँ अब इसकी भविष्य की संभावनाओं को ‘स्थिर’ के बजाय ‘सकारात्मक’ के रूप में अद्यतन किया गया है, जो भारत की नीति स्थिरता, आर्थिक सुधारों और अवसंरचना में निवेश के प्रति विश्वास को परिलक्षित करता है।
प्रिलिम्स के लिये:भारत की आर्थिक वृद्धि, विश्व आर्थिक परिदृश्य, भारतीय रिज़र्व बैंक, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, खुदरा मुद्रास्फीति, मेक इन इंडिया कार्यक्रम, उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ, भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, लाल सागर संकट, राजकोषीय घाटा, गिनी गुणांक, ई-कॉमर्स मेन्स के लिये:भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक, भारत की आर्थिक वृद्धि में वर्तमान प्रमुख चुनौतियाँ |
भारत के आर्थिक विकास प्रक्षेप वक्र ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि प्रसिद्ध रेटिंग एजेंसी S&P Global ने देश के लिये अपने अनुमान को ‘स्थिर’ (stable) से संशोधित कर ‘सकारात्मक’ (positive) कर दिया है। एजेंसी के आकलन में यह सुधार परिलक्षित करता है कि भारत की नीति स्थिरता, गहन आर्थिक सुधार और सुदृढ़ अवसंरचना निवेश देश की दीर्घकालिक विकास संभावनाओं को जारी बनाए रखेंगे।
निकट भविष्य के विकास में सार्वजनिक निवेश और उपभोक्ता संवेग के प्रमुख चालक होने के साथ, वर्ष 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति के लिये और सतत आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिये भारत के प्रक्षेपवक्र को आकार देने के लिये लक्षित आर्थिक नीतियों की आवश्यकता है।
भारत के बारे में हाल के आर्थिक विकास अनुमान:
- IMF का अनुमान (विश्व आर्थिक परिदृश्य, अप्रैल 2024): IMF ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिये भारत के जीडीपी विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया है, जो जनवरी 2024 के अनुमान से 0.3 प्रतिशत अंक अधिक है।
- वित्त वर्ष 2025-26 के लिये IMF ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है।
- संयुक्त राष्ट्र का अनुमान (विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएँ, 2024 के मध्य में): भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में 6.9% और वर्ष 2025 में 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है।
- जनवरी 2024 में 6.2% वृद्धि के अनुमान को संशोधित करते हुए वर्ष 2024 के लिये 6.9% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक: भारतीय रिज़र्व बैंक को उम्मीद है कि वर्ष 2024-25 में भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 7% की दर से बढ़ेगा।
- वर्ष 2024 की जून तिमाही के लिये जीडीपी वृद्धि 7.2% आँकी गई है जो सितंबर तिमाही में कुछ घटकर 6.8% होने की उम्मीद है
भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक:
- मज़बूत घरेलू मांग: बढ़ती आय और बढ़ते मध्यम वर्ग द्वारा संचालित मज़बूत निजी उपभोग वृद्धि। डेलॉइट (Deloitte) के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में निजी उपभोग व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 3.5% की वृद्धि हुई।
- इसके अलावा, लग्ज़री एवं प्रीमियम वस्तुओं और सेवाओं की मांग बुनियादी वस्तुओं की मांग की तुलना में तेज़ी से बढ़ रही है।
- मज़बूत निवेश गतिविधि: वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में निजी निवेश में पिछले वर्ष की तुलना में 10.6% की वृद्धि हुई, जो निजी पूंजीगत व्यय चक्र में मज़बूत पुनरुद्धार का संकेत है।
- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (National Monetization Pipeline) जैसी पहलों का उद्देश्य ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों का मूल्य बढ़ाना और निजी निवेश आकर्षित करना है।
- IMF का सुझाव है कि विदेशी निवेश को उदार बनाने तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिये किये गए सुधारों से विकास को और अधिक बढ़ावा मिल सकता है।
- इसके अलावा, सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय (capex) के रूप में वर्गीकृत बजटीय व्यय वर्ष 2024-25 में लगभग 11 ट्रिलियन रुपए तक बढ़ने का अनुमान है, जो वर्ष 2014-15 के स्तर से लगभग 4.5 गुना है।
- मुद्रास्फीति में कमी: मुद्रास्फीति घट रही है, जहाँ अप्रैल 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.83% दर्ज की गई।
- इससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिये एक स्थिर वातावरण उपलब्ध हो रहा है तथा व्यय एवं निवेश को प्रोत्साहन मिल रहा है।
- विनिर्माण क्षेत्र का पुनरुद्धार: ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम और PLI योजनाओं जैसी पहलों से प्रेरित होकर विनिर्माण क्षेत्र में वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में पिछले वर्ष की तुलना में 11.6% की वृद्धि हुई।
- ‘आत्मनिर्भर भारत’ पर सरकार का ज़ोर घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा दे रहा है।
- सेवा क्षेत्र की प्रत्यास्थता: सेवा क्षेत्र (जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महत्त्वपूर्ण योगदान करता है) में वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में पिछले वर्ष की तुलना में 7% की वृद्धि हुई।
- डिजिटल समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग से प्रेरित आईटी और आईटी-सक्षम सेवा क्षेत्र में वृद्धि जारी है।
- कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील के साथ, पर्यटन, आतिथ्य एवं मनोरंजन जैसी संपर्क-गहन सेवाओं में मज़बूत सुधार देखा गया है।
- भारत में यात्रा बाज़ार वित्तीय वर्ष 2027 तक 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।
- वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति प्रत्यास्थता: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, भू-राजनीतिक तनावों (रूस-यूक्रेन युद्ध), आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान (लाल सागर संकट) और अमेरिका जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सख्त वित्तीय दशाओं के बावजूद, भारत की घरेलू मांग अपेक्षाकृत प्रत्यास्थी बनी हुई है।
- वर्ष 2023 में विश्व खाद्य मूल्यों में वर्ष 2022 के उच्चतम स्तर से व्यापक कमी आई। हालाँकि दिसंबर 2023 में भारत की खाद्य मुद्रास्फीति 9.5% के उच्च स्तर पर बनी रही, जबकि वैश्विक अपस्फीति -10.1% रही थी।
- बाह्य आघातों से इस रोधन से भारत के विकास को बनाए रखने में मदद मिली है, जबकि कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ गिरावट या मंदी का सामना कर रही हैं।
- आपूर्ति शृंखला विविधीकरण: वैश्विक आपूर्ति शृंखला में व्यवधानों के बीच भारत विनिर्माण निवेश के लिये एक आकर्षक वैकल्पिक गंतव्य के रूप में उभरा है (विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में)।
- भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) जैसे व्यापार समझौतों ने इस आपूर्ति शृंखला विविधीकरण को सुगम बनाया है।
भारत की आर्थिक वृद्धि के लिये विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ:
- रोज़गार संबंधी चुनौतियाँ: पिछले दशक में स्थिर सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के बावजूद, पर्याप्त रोज़गार सृजन की कमी (रोज़गारहीन विकास की स्थिति) सरकार के समक्ष एक प्रमुख नीतिगत चुनौती बनी हुई है।
- CMIE के उपभोक्ता पिरामिड घरेलू सर्वेक्षण (Consumer Pyramids Household Survey) के अनुसार, अप्रैल 2024 में भारत में बेरोज़गारी दर 8.1% थी।
- निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता संबंधी चुनौतियाँ: नीतिगत प्रोत्साहनों के बावजूद, वित्त वर्ष 24 में भारत के निर्यात में 3% की कमी आई।
- अप्रैल 2024 के दौरान वस्तु व्यापार घाटा 19.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर आकलित किया गया, जो अप्रैल 2023 के दौरान 14.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था।
- संभावित राजकोषीय घाटा जोखिम (Fiscal Slippage Risks): S&P Global के अनुसार, सामान्य सरकारी राजकोषीय घाटा, जिसमें भले ही गिरावट आ रही है, वित्त वर्ष 28 तक सकल घरेलू उत्पाद का 6.8% रहने का अनुमान है।
- राजकोषीय समेकन पथ से कोई भी विचलन भारत की क्रेडिट रेटिंग और उधार लागत को प्रभावित कर सकता है।
- कौशल असंगति और श्रम गुणवत्ता: भारत को उपलब्ध कार्यबल और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच कौशल असंगति (Skill Mismatch) का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उत्पादकता और रोज़गार सृजन में बाधा आ रही है।
- एक नए अध्ययन से पता चला है कि नौकरियों के लिये आवेदन करने वाले भारतीय स्नातकों में से केवल 45% ही रोज़गार-योग्य (employable) हैं जिनके पास उद्योग की तेज़ी से बदलती मांगों को पूरा कर सकने का कौशल है।
- आय असमानता: भारत में अमीर और गरीब के बीच की खाई अभी भी बहुत बड़ी है। आय असमानता का एक मापक गिनी गुणांक (Gini coefficient) वर्ष 2022-23 में 0.4197 रहा।
- भारत में धन असमानता छह दशक के उच्चतम स्तर पर है, जहाँ शीर्ष 1% लोगों के पास देश का 40.1% धन है।
- इसका अर्थ यह है कि जनसंख्या के एक बड़े हिस्से के पास सीमित व्यय योग्य आय है, जिससे समग्र उपभोग वृद्धि में बाधा उत्पन्न हो रही है।
- अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व: भारत के कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, जहाँ मज़दूरी कम है, सामाजिक सुरक्षा लाभ न्यूनतम हैं और उत्पादकता लाभ सीमित है।
- रोज़गार हिस्सेदारी के संदर्भ में, असंगठित क्षेत्र में 83% कार्यबल कार्यरत है जबकि संगठित क्षेत्र में 17% कार्यबल कार्यरत है (IMF के अनुसार)।
- यह अनौपचारिकता आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है क्योंकि यह कर राजस्व को सीमित करती है और अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण को बाधित करती है।
- अवसंरचना संबंधी बाधाएँ: हाल के प्रयासों के बावजूद, भारत में बिजली, परिवहन और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में अवसंरचना की कमी बनी हुई है।
- नीति आयोग का अनुमान है कि भारत को अपनी विकास गति को बनाए रखने के लिये वर्ष 2040 तक अवसंरचना पर 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की आवश्यकता होगी।
आर्थिक विकास में तेज़ी लाने के लिये भारत कौन-से उपाय कर सकता है?
- विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करना: भारत को विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि कृषि से संक्रमित करने वाले कार्यबल को रोज़गार के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।
- कृषि श्रमिकों को नियोजित करने और उन्हें कौशल प्रदान करने के लिये उद्योगों को लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रोत्साहन प्रदान करने के माध्यम से इसे सुगम बनाया जा सकता है। इससे सुचारु संक्रमण सुनिश्चित होगा और समग्र उत्पादकता में वृद्धि होगी।
- इसके अतिरिक्त, किसानों के लिये आय के अवसरों का विस्तार करने के लिये खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- कृषि श्रमिकों को नियोजित करने और उन्हें कौशल प्रदान करने के लिये उद्योगों को लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रोत्साहन प्रदान करने के माध्यम से इसे सुगम बनाया जा सकता है। इससे सुचारु संक्रमण सुनिश्चित होगा और समग्र उत्पादकता में वृद्धि होगी।
- ‘गिग इकॉनमी स्किलिंग’: गिग इकॉनमी के लिये प्रासंगिक लक्षित माइक्रो-स्किलिंग कार्यक्रम विकसित करने के लिये ‘उबर’ एवं ‘मीशो’ जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के साथ साझेदारी की जाए।
- इससे युवाओं को तत्काल रोज़गार अवसरों के लिये आवश्यक कौशल से लैस किया जाता है।
- फ्रीलांस कार्य के लिये एक राष्ट्रीय ऑनलाइन बाज़ार का सृजन किया जाए, जो कौशल-प्राप्त व्यक्तियों को भारत भर के व्यवसायों से जोड़े। यह उद्यमियों को भी सशक्त बनाएगा और लचीली कार्य व्यवस्था की सुविधा प्रदान करेगा।
- EPZs 2.0: संवहनीयता एवं प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए नवयुगीन निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (Export Processing Zones- EPZs) की स्थापना की जाए। हरित प्रौद्योगिकी और उच्च-मूल्य विनिर्माण कंपनियों को आकर्षित करने के लिये कर छूट एवं सुव्यवस्थित विनियमन प्रदान किया जाए।
- ई-कॉमर्स निर्यात के लिये लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) को सक्षम बनाने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाए।
- स्मार्ट कराधान और संशोधित PPP: मौजूदा कराधान प्रणालियों की खामियों को दूर करने और कर आधार को व्यापक बनाने के लिये स्मार्ट कराधान (Smart Taxation) लागू करने हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जाए।
- अभिनव कर संग्रहण समाधानों के लिये फिनटेक कंपनियों के साथ साझेदारी स्थापित की जाए।
- जोखिम-साझाकरण और प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए PPP की एक नई पीढ़ी का विकास किया जाए।
- इससे अवसंरचना परियोजनाओं के लिये निजी पूंजी आकर्षित होगी और निवेश का समुचित लाभ प्राप्त होगा।
- उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहकार्यता: उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित करने के लिये विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच मज़बूत सहकार्यता को बढ़ावा दिया जाए।
- माइक्रो-क्रेडेंशियल्स और स्टैकेबल सर्टिफिकेशन की एक प्रणाली शुरू की जाए जो विशिष्ट कौशल को मान्यता प्रदान करे।
- इससे व्यक्तियों को निरंतर कौशल उन्नयन करने तथा बदलती नौकरी की मांग के अनुरूप ढलने का अवसर मिलेगा।
- भारत आयरलैंड की बाज़ार-संचालित उद्योग-अकादमी साझेदारियों से प्रेरणा ग्रहण कर सकता है, जिसने वहाँ के कार्यबल को उभरती प्रौद्योगिकियों के लिये प्रभावी रूप से तैयार किया है।
- माइक्रो-क्रेडेंशियल्स और स्टैकेबल सर्टिफिकेशन की एक प्रणाली शुरू की जाए जो विशिष्ट कौशल को मान्यता प्रदान करे।
- औपचारिकीकरण के लिये प्रोत्साहन: औपचारिक क्षेत्र में संक्रमण करने वाले अनौपचारिक व्यवसायों को कर छूट और ऋण तक आसान पहुँच प्रदान करना। इससे औपचारिकीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा और कर राजस्व में वृद्धि होगी।
- वित्तीय समावेशन का विस्तार करने के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना, अनौपचारिक श्रमिकों के लिये बैंक खातों, सूक्ष्म ऋणों और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों तक पहुँच प्रदान करना।
- हरित अवसंरचना बॉण्ड: नवीकरणीय ऊर्जा और सार्वजनिक परिवहन जैसी सतत अवसंरचना परियोजनाओं के लिये निजी पूंजी आकर्षित करने हेतु हरित अवसंरचना बॉण्ड (Green Infrastructure Bonds) जारी किये जाएँ।
- गंभीर अवसंरचना अंतराल की पहचान करने और परियोजना विकास के लिये संसाधन आवंटन को इष्टतम करने के लिये ‘बिग डेटा एनालिटिक्स’ और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग किया जाए।
अभ्यास प्रश्न: हाल के आर्थिक आकलनों में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये निरंतर वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इस सकारात्मक अनुमान या अवेक्षण को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारकों की चर्चा कीजिये।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. 'आठ मूल उद्योगों के सूचकांक (इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज़)' में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है? (2015) (a) कोयला उत्पादन उत्तर: (b) प्रश्न. निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP में वृद्धि आर्थिक विकास की ऊँची स्तर का संकेत नहीं करती, यदि: (2018) (a) औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ-साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। उत्तर: (c) प्रश्न. किसी दिये गए वर्ष में भारत के कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएँ अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं क्योंकि: (2019) (a) गरीबी की दर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. "सुधार के बाद की अवधि में औद्योगिक विकास दर सकल-घरेलू-उत्पाद (जीडीपी) की समग्र वृद्धि से पीछे रह गई है" कारण बताइये। औद्योगिक नीति में हालिया बदलाव औद्योगिक विकास दर को बढ़ाने में कहाँ तक सक्षम हैं? (2017) प्रश्न. आमतौर पर देश कृषि से उद्योग और फिर बाद में सेवाओं की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, लेकिन भारत सीधे कृषि से सेवाओं की ओर स्थानांतरित हो गया। देश में उद्योग की तुलना में सेवाओं की भारी वृद्धि के क्या कारण हैं? क्या मज़बूत औद्योगिक आधार के बिना भारत एक विकसित देश बन सकता है? (2014) |