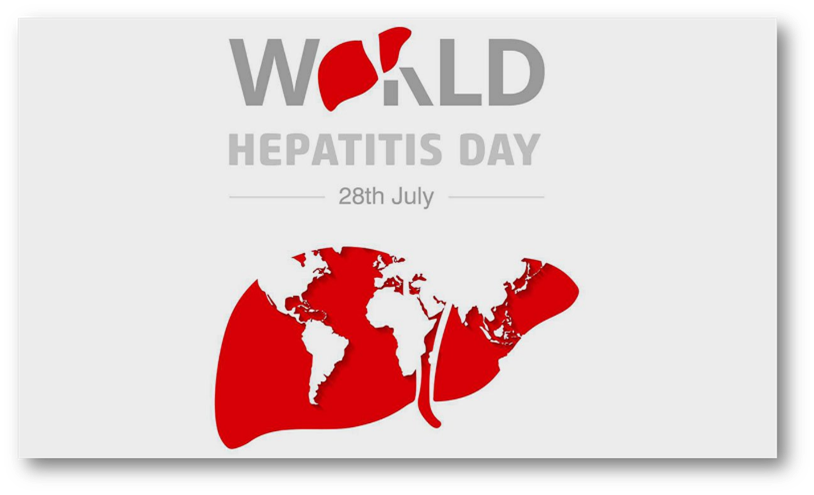शासन व्यवस्था
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
प्रिलिम्स के लिये:ठोस अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, सरकार की पहल मेन्स के लिये:ठोस अपशिष्ट प्रबंधन चुनौतियाँ, अपशिष्ट प्रबंधन में असंगठित क्षेत्र की भूमिका, अपशिष्ट प्रबंधन में असंगठित क्षेत्र के लिये चुनौतियाँ, संबंधित सरकार की पहल |
चर्चा में क्यों?
बढ़ती आबादी और तीव्र शहरीकरण के कारण भारतीय शहरों में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (Municipal Solid Waste-MSW) के उत्पादन में व्यापक वृद्धि हुई है।
- यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि संगठित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की भागीदारी शहरों में कम है, क्योंकि अपर्याप्त धन, कम क्षेत्रीय विकास और स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन व्यवसायों के बारे में जानकारी की कमी है।
- इसलिये भारत सहित कई विकासशील देशों में अपशिष्ट संग्रह और वस्तु पुनर्चक्रण गतिविधियाँ मुख्य रूप से असंगठित अपशिष्ट क्षेत्र द्वारा की जाती हैं।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में असंगठित क्षेत्र की भूमिका:
- परिचय:
- असंगठित अपशिष्ट संग्रहकर्त्ताओं में ऐसे व्यक्ति, संघ या कचरा-व्यापारी शामिल हैं जो पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों की छँटाई, बिक्री और खरीद में शामिल हैं।
- कचरा बीनने वाला व्यक्ति असंगठित रूप से अपशिष्ट उत्पादन के स्रोत से पुन: प्रयोज्य और पुनर्चक्रण योग्य ठोस अपशिष्ट के संग्रह तथा पुनर्प्राप्ति में लगा हुआ है, जो सीधे या बिचौलियों के माध्यम से पुनर्चक्रणकर्त्ताओं को अपशिष्ट की बिक्री करता है।
- यह अनुमान है कि असंगठित अपशिष्ट अर्थव्यवस्था दुनिया भर में लगभग 0.5% - 2% शहरी आबादी को रोज़गार देती है।
- असंगठित अपशिष्ट संग्रहकर्त्ताओं में ऐसे व्यक्ति, संघ या कचरा-व्यापारी शामिल हैं जो पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों की छँटाई, बिक्री और खरीद में शामिल हैं।
- चुनौतियाँ:
- न्यूनतम आय वाले रोज़गार:
- असंगठित क्षेत्र को अक्सर आधिकारिक तौर पर अनुमोदित, मान्यता प्राप्त और स्वीकार नहीं किया जाता है, जबकि वे पुनर्चक्रण मूल्य शृंखला में अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करने, छाँटने, प्रसंस्करण, भंडारण और व्यापार करके शहरों के अपशिष्ट पुनर्चक्रण प्रथाओं में योगदान करते हैं।
- स्वास्थ्य चुनौतियाँ:
- असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग अपशिष्ट के ढेर के पास रहतें हैं एवं अस्वच्छ तथा अस्वस्थ परिस्थितियों में काम करतें हैं।
- श्रमिकों के पास पीने के जल या सार्वजनिक शौचालय तक पहुँच नहीं है।
- उनके पास दस्ताने, गमबूट और एप्रन जैसे उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPI) नहीं हैं।
- निम्न स्तर का जीवनयापन और काम करने की स्थिति के कारण उनमें कुपोषण, एनीमिया और तपेदिक आम हैं।
- सामाजिक उपचार:
- उन्हें समाज में गंदे और अवांछित तत्त्वों के रूप में माना जाता है, साथ ही उन्हें शोषक सामाजिक व्यवहार से निपटना पड़ता है।
- असंगठित अपशिष्ट-श्रमिकों के विभिन्न स्तरों की मज़दूरी और रहने की स्थिति बहुत भिन्न होती है।
- अन्य:
- इस क्षेत्र में बाल श्रम काफी प्रचलित है और जीवन प्रत्याशा कम है।
- अपशिष्ट बीनने वाले किसी भी श्रम कानून के दायरे में नहीं आते हैं।
- नतीजतन उन्हें सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा बीमा योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है।
- न्यूनतम आय वाले रोज़गार:
ठोस अपशिष्ट
- परिचय:
- ठोस अपशिष्ट में ठोस या अर्द्ध-ठोस घरेलू अपशिष्ट, स्वच्छता अपशिष्ट, वाणिज्यिक अपशिष्ट, संस्थागत अपशिष्ट, खानपान और बाज़ार अपशिष्ट एवं अन्य गैर-आवासीय अपशिष्ट, सड़क पर झाड़ू लगाना, सतही नालियों से हटाया या एकत्र किया गया गाद, बागवानी अपशिष्ट, कृषि तथा डेयरी अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट को छोड़कर उपचारित जैव चिकित्सा अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, रेडियो-सक्रिय अपशिष्ट आदि शामिल हैं।
- भारत की स्थिति:
- अकेले शहरी भारत में प्रतिदिन लगभग 15 मिलियन टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है।
- अनुमान है कि देश में सालाना लगभग 62 मिलियन टन अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें से 5.6 मिलियन प्लास्टिक अपशिष्ट और 0.17 मिलियन बायोमेडिकल कचरा है।
- इसके अलावा खतरनाक अपशिष्ट उत्पादन प्रतिवर्ष 7.90 मिलियन टन है और 15 लाख टन ई-अपशिष्ट है।
- अपशिष्ट की मात्रा वर्ष 2031 तक 165 मिलियन टन और वर्ष 2050 तक 436 मिलियन टन तक पहुँचने का अनुमान है।
- अपशिष्ट प्रबंधन में चुनौतियाँ:
- भारत में बढ़ते शहरीकरण के परिणामस्वरूप अति-उपभोक्तावाद की स्थिति है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक अपशिष्ट उत्पादन होता है।
- जैविक खेती और खाद बनाना भारतीय किसान के लिये आर्थिक रूप से आकर्षक नहीं है, क्योंकि रासायनिक कीटनाशकों पर भारी सब्सिडी दी जाती है तथा खाद का विपणन कुशलता से नहीं किया जाता है।
- नगर निगमों/शहरी स्थानीय निकायों के पास वित्तीय संसाधनों की कमी के परिणामस्वरूप ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन और प्रबंधन की खराब स्थिति है।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की मुख्य विशेषताएँ
- कचरे को निम्नलिखित प्रकार से तीन श्रेणियों में अलग करने की जिम्मेदारी इसके उत्पादक की है:
- गीला (बायोडिग्रेडेबल) ।
- सूखा (प्लास्टिक, कागज़, धातु, लकड़ी आदि) ।
- घरेलू खतरनाक अपशिष्ट (डायपर, नैपकिन, खाली कंटेनर आदि) तथा अलग किये गए कचरे को अधिकृत कचरा बीनने वालों या कचरा संग्रहकर्ता या स्थानीय निकायों को सौंपना।
- अपशिष्ट उत्पादकों को करना होगा भुगतान:
- कचरा संग्रहणकर्त्ताओं को 'उपयोगकर्त्ता शुल्क'।
- लिटरिंग और नॉन-सेग्रीगेशन के लिये 'स्पॉट फाइन'।
- डायपर, सैनिटरी पैड जैसे इस्तेमाल किये गए सैनिटरी अपशिष्ट को निर्माताओं या इन उत्पादों के ब्रांड मालिकों द्वारा प्रदान किये गए पाउच में या उपयुक्त रैपिंग सामग्री में सुरक्षित रूप से लपेटा जाना चाहिये और इसे सूखे अपशिष्ट/गैर-जैव-अवक्रमणीय अपशिष्ट के लिये कूड़ादान (Bin) में रखा जाना चाहिये।
- स्वच्छ भारत में साझेदारी की अवधारणा पेश की गई है।
- थोक और संस्थागत उत्पादक, बाज़ार संघों, कार्यक्रम आयोजकों, होटल और रेस्तराँ को स्थानीय निकायों के साथ साझेदारी में अपशिष्ट को अलग करने, व्यवस्थित करने तथा प्रबंधन के लिये सीधे ज़िम्मेदार बनाया गया है।
- टिन, काँच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि जैसे डिस्पोज़ेबल उत्पादों के निर्माता या ब्रांड मालिक जो ऐसे उत्पादों को बाज़ार में पेश करते हैं,अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना हेतु स्थानीय अधिकारियों आवश्यक वित्तीय प्रदान करेंगे।
- बायो-डिग्रेडेबल अपशिष्ट को जहाँ तक संभव हो परिसर के भीतर कंपोस्टिंग या बायो-मीथेनेशन के माध्यम से संसाधित, उपचारित तथा निपटाया जाना चाहिये।
- अवशिष्ट कचरा स्थानीय प्राधिकरण के निर्देशानुसार कचरा संग्रहकर्त्ता या एजेंसी को दिया जाएगा।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये सरकार की पहल:
- वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल:
- वेस्ट टू वेल्थ मिशन प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (PMSTIAC) के नौ वैज्ञानिक मिशनों में से एक है।
- इसका उद्देश्य ऊर्जा उत्पन्न करने, सामग्रियों का पुनर्चक्रण करने और कचरे के उपचार हेतु प्रौद्योगिकियों की पहचान, विकास और तैनाती करना है।
- राष्ट्रीय जल मिशन:
- इसका उद्देश्य एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से जल का संरक्षण करना, अपव्यय को कम करना तथा राज्यों के बाहर भीतर जल का अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना है।
- अपशिष्ट से ऊर्जा:
- एक अपशिष्ट-से-ऊर्जा या ऊर्जा-से-अपशिष्ट संयंत्र औद्योगिक प्रसंस्करण के लिये नगरपालिका एवं औद्योगिक ठोस अपशिष्ट को बिजली और/या गर्मी में परिवर्तित करता है।
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) नियम, 2016:
- यह प्लास्टिक कचरे के उत्पादन को कम करने, प्लास्टिक कचरे को फैलने से रोकने और अन्य उपायों के बीच स्रोत पर कचरे का अलग भंडारण सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाने पर ज़ोर देता है।
- यह प्लास्टिक कचरे के उत्पादन को कम करने, प्लास्टिक कचरे को फैलने से रोकने और अन्य उपायों के बीच स्रोत पर कचरे का अलग भंडारण सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाने पर ज़ोर देता है।
आगे की राह
- असंगठित श्रमिक:
- दशकों से कचरा बीनने वाले या ‘रैग-पिकर्स’ (Rag-Pickers) खतरनाक एवं अस्वच्छ परिस्थितियों में कार्य करते हुए हमारी फेंकी हुई चीज़ों से अपनी आजीविका प्राप्त करते रहे हैं।
- इसमें पानी, स्वच्छता एवं स्वच्छ जीवन और स्वास्थ्य बीमा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के व्यावसायिक खतरों को कम करने के लिये संग्रह, पृथक्करण तथा PPE की छँटाई हेतु अनिवार्य पहचान पत्र तक पहुँच से संबंधित बुनियादी प्रावधान शामिल होने चाहिये।
- कचरा बीनने वालों को शहर में निर्दिष्ट संग्रह और संघनन स्टेशनों (स्थानांतरण स्टेशन, सामग्री वसूली सुविधाओं) का उपयोग करने की अनुमति देकर औपचारिक रूप से पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं के पृथक्करण के लिये किया जाना चाहिये।
- दशकों से कचरा बीनने वाले या ‘रैग-पिकर्स’ (Rag-Pickers) खतरनाक एवं अस्वच्छ परिस्थितियों में कार्य करते हुए हमारी फेंकी हुई चीज़ों से अपनी आजीविका प्राप्त करते रहे हैं।
- भागीदारी:
- सरकार को कचरा बीनने वाले संगठनों के साथ साझेदारी स्थापित करनी चाहिये, जिसका उल्लेख SWM 2016 नियमों में भी किया गया है।
- कचरा बीनने वालों की पहचान करने, उन्हें संगठित करने, प्रशिक्षित करने और उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता है।
- सरकार को कचरा बीनने वाले संगठनों के साथ साझेदारी स्थापित करनी चाहिये, जिसका उल्लेख SWM 2016 नियमों में भी किया गया है।
- कचरे को आर्थिक अवसर के रूप में देखना:
- ऊर्जा उत्पादन:
- अपशिष्ट का गैसीकरण: बायोगैस संयंत्रों के लिये कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाने वाला ठोस अपशिष्ट।
- पुनर्चक्रण सामग्रियाँ:
- पृथक्करण के चरण में पुनर्चक्रण एक अच्छा आर्थिक अवसर प्रस्तुत करता है।
- भारत द्वारा अपनाए गए चक्रीय अर्थव्यवस्था से 40 लाख करोड़ रुपए (अनुमानित) का वार्षिक लाभ हो सकता है।
- पृथक्करण के चरण में पुनर्चक्रण एक अच्छा आर्थिक अवसर प्रस्तुत करता है।
- आवश्यक संसाधनों की प्राप्ति:
- ई-कचरे के प्रसंस्करण से तांबा, सोना, एल्युमिनियम आदि कीमती धातुओं का निष्कर्षण संभव हो सकता है।
- ऊर्जा उत्पादन:
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (पीवाईक्यू)प्रश्न. भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है? (2019) (a) अपशिष्ट उत्पादक को पाँच कोटियों में अपशिष्ट अलग-अलग करने होंगे। उत्तर: (c) व्याख्या:
प्रश्न. निरंतर उत्पन्न किये जा रहे और फेंके गए ठोस कचरे की विशाल मात्रा का निस्तारण करने में क्या-क्या बाधाएँ हैं? हम अपने रहने योग्य परिवेश में जमा होते जा रहे जहरीले अपशिष्टों को सुरक्षित रूप से किस प्रकार हटा सकते हैं? (2018 मुख्य परीक्षा) |
स्रोत: डाउन टू अर्थ


शासन व्यवस्था
फ्रीबी कल्चर
प्रिलिम्स के लिये:तर्कहीन फ्रीबीज़, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM), वित्त आयोग। मेन्स के लिये:फ्रीबीज़ और अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव। |
चर्चा में क्यों?
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या चुनाव अभियानों के दौरान तर्कहीन फ्रीबीज़ (मुफ्त उपहार) वितरित करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य है।
- इसने तर्कहीन चुनावी फ्रीबीज़ पर अंकुश लगाने में वित्त आयोग की विशेषज्ञता का उपयोग करने का भी उल्लेख किया है।
- भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, क्या ऐसी नीतियाँ आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं या राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव एक ऐसा प्रश्न है जिस पर राज्य के मतदाताओं को विचार करना और निर्णय लेना है।
फ्रीबीज़:
राजनीतिक दल लोगों के वोट को सुरक्षित करने के लिये मुफ्त बिजली/पानी की आपूर्त्ति, बेरोज़गारों, दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों और महिलाओं को भत्ता, साथ-साथ गैजेट जैसे- लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि की पेशकश करने का वादा करते हैं।
राज्यों को कर्जमाफी या मुफ्त बिजली, साइकिल, लैपटॉप, टीवी सेट आदि के रूप में मुफ्त उपहार देने की आदत हो गई है।
- लोकलुभावन वादों या चुनावों को ध्यान में रखकर किये जाने वाले ऐसे कुछ खर्चों पर निश्चय ही प्रश्न उठाए जा सकते हैं।
- लेकिन यह देखते हुए कि पिछले 30 वर्षों से देश में असमानता बढ़ रही है, सब्सिडी के रूप में आम आबादी को किसी प्रकार की राहत प्रदान करना अनुचित नहीं माना जा सकता, बल्कि वास्तव में अर्थव्यवस्था के विकास पथ पर बने रहने के लिये यह आवश्यक है।
फ्रीबीज़ की आवश्यकता:
- विकास को सुगम बनाना: ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि कुछ व्यय, परिव्यय के समग्र लाभ के रूप में होते हैं जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रोज़गार गारंटी योजनाएँ, शिक्षा के लिये समर्थन और विशेष रूप से महामारी के दौरान स्वास्थ्य सुविधा के लिये किया गया परिव्यय।
- अल्प विकसित राज्यों को मदद: गरीबी से पीड़ित आबादी के एक बड़े हिस्से के साथ तुलनात्मक रूप से निम्न स्तर के विकास वाले राज्यों को इस तरह की निःशुल्क सुविधाएँ जरूरत/मांग परआधारित होती हैं और इस क्रम में उनका उत्थान करने के लिये उन्हें सब्सिडी प्रदान करना अपरिहार्य हो जाता है।
- अपेक्षाओं की पूर्ति: भारत जैसे देश में जहाँ राज्यों में विकास का एक निश्चित स्तर होता है (अथवा नहीं होता है), चुनाव के अवसर पर किये गए लोकलुभावन वायदे से जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति की जाती है।
फ्रीबीज़ की कमियाँ:
- समष्टि अर्थव्यवस्था के लिये अस्थिर: फ्रीबीज़ समष्टि अर्थव्यवस्था की स्थिरता के बुनियादी ढाँचे को कमजोर करते हैं, फ्रीबीज़ की राजनीति व्यय प्राथमिकताओं को विकृत करती है और यह परिव्यय किसी-न-किसी रूप में सब्सिडी पर केंद्रित रहता है।
- राज्यों की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव: निःशुल्क उपहार देने से अंततः सरकारी खजाने पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और भारत के अधिकांश राज्यों में मज़बूत वित्तीय व्यवस्था नहीं है, अक्सर राजस्व के मामले में संसाधन बहुत सीमित होते हैं।
- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ: चुनाव से पहले सार्वजनिक धन से तर्कहीन मुफ्त का वादा मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करता है, सभी को समान अवसर की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करता है, तथा चुनाव प्रक्रिया की शुचिता को नष्ट करता है।
- पर्यावरण से दूर: जब मुफ्त बिज़ली दी जाएगी, तो इससे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होगा और अक्षय ऊर्जा प्रणाली से ध्यान भी विचलित हो जाएगा।
आगे की राह
- मुफ्त के आर्थिक प्रभावों को समझना: यह इस बारे में नहीं है कि फ्रीबीज़ कितने सस्ते हैं बल्कि लंबे समय में अर्थव्यवस्था, जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक सामंजस्य के लिये ये कितने महंगे हैं।.
- इसके बजाय हमें लोकतंत्र और सशक्त संघवाद के माध्यम से दक्षता के लिये प्रयास करना चाहिये जहाँ राज्य अपने अधिकार का उपयोग नवीन विचारों और सामान्य समस्याओं के समाधान के लिये कर सकें तथा जिनका अन्य राज्य अनुकरण कर सकते हैं।
- सब्सिडी और मुफ्त में अंतर: आर्थिक अर्थों में मुफ्त के प्रभावों को समझने और इसे करदाता के पैसे से जोड़ने की ज़रूरत है।
- सब्सिडी और मुफ्त में अंतर करना भी आवश्यक है क्योंकि सब्सिडी के उचित और विशेष रूप से लक्षित लाभ हैं जो मांगों से उत्पन्न होते हैं।
- सब्सिडी और मुफ्त में अंतर करना भी आवश्यक है क्योंकि सब्सिडी के उचित और विशेष रूप से लक्षित लाभ हैं जो मांगों से उत्पन्न होते हैं।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्षों के प्रश्न:प्रश्न. सरकार द्वारा की जाने वाली निम्नलिखित कार्रवाइयों पर विचार कीजिये: (2010)
उपर्युक्त कार्यों में से किसे/किन्हें "राजकोषीय प्रोत्साहन" पैकेज का हिस्सा माना जा सकता है? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) व्याख्या:
प्रश्न: किस तरह से मूल्य सब्सिडी को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) में बदलने से भारत में सब्सिडी का परिदृश्य बदल सकता है? चर्चा कीजिये। (2015, मुख्य परीक्षा) |
स्रोत: द हिंदू
शासन व्यवस्था
विश्व हेपेटाइटिस दिवस
प्रिलिम्स के लिये:हेपेटाइटिस दिवस, हेपेटोट्रोपिक वायरस, अन्य रोग, हेपेटाइटिस बी मेन्स के लिये:वैश्विक और भारतीय स्तर पर हेपेटाइटिस की व्यापकता, हेपेटाइटिस से निपटने में चुनौतियाँ और वैश्विक लक्ष्य कैसे प्राप्त करें |
चर्चा में क्यों?
वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है।
- वर्ष 2022 की थीम "ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोज़र टू यू’' (Bringing hepatitis care closer to you) है।
- इसका उद्देश्य हेपेटाइटिस देखभाल को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और समुदायों तक पहुँचाने की आवश्यकता को रेखांकित करना है, ताकि उपचार और देखभाल की बेहतर सुविधाएँ सुनिश्चित की जा सकें।
हेपेटाइटिस:
- परिचय:
- हेपेटाइटिस शब्द यकृत की किसी भी सूजन को संदर्भित करता है- किसी भी कारण से यकृत कोशिकाओं में होने वाली जलन या सूजन।
- यह तीव्र भी हो सकता है (यकृत की सूजन जिस बीमारी की वजह से होती है उनमें पीलिया, बुखार, उल्टी आदि शामिल हैं) यकृत की सूजन छह महीने से अधिक समय तक भी रहती है, लेकिन अनिवार्य रूप से इसका कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है।
- कारण:
- आमतौर पर यह A, B, C, D और E सहित "हेपेटोट्रोपिक" (यकृत निर्देशित) वायरस के एक समूह के कारण होता है।
- अन्य वायरस भी इसका कारण हो सकते हैं, जैसे कि वैरिकाला वायरस जो चिकन पॉक्स का कारण बनता है ।
- SARS-CoV-2, Covid-19 पैदा करने वाला वायरस भी यकृत को नुकसान पहुँचा सकता है।
- अन्य कारणों में ड्रग्स और अल्कोहल का दुरुपयोग, यकृत में वसा का निर्माण (फैटी लीवर हेपेटाइटिस) या एक ऑटोइम्यून प्रक्रिया शामिल है जिसमें एक व्यक्ति का शरीर एंटीबॉडी बनाता है जो यकृत (ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस) पर हमला करता है।
- हेपेटाइटिस एकमात्र संचारी रोग है जिसकी मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है।
- उपचार:
- हेपेटाइटिस A और E स्व-सीमित रोग (self-limiting diseases) हैं (अर्थात् अपने आप दूर हो जाते हैं) और इसके लिये किसी विशिष्ट एंटीवायरल दवाओं की आवश्यकता नहीं होती है।
- हेपेटाइटिस B और C के लिये प्रभावी दवाएँ उपलब्ध हैं।
- वैश्विक परिदृश्य:
- लगभग 354 मिलियन लोग हेपेटाइटिस B और C से पीड़ित हैं।
- दक्षिण-पूर्व एशिया में हेपेटाइटिस के वैश्विक रुग्णता बोझ का 20% है।
- सभी हेपेटाइटिस से संबंधित मौतों में से लगभग 95% सिरोसिस तथा हेपेटाइटिस B और C वायरस की वजह से होने वाले यकृत कैंसर के कारण होती हैं।
- भारतीय परिदृश्य:
- वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस वायरस A और E के कारण होता है, जो अभी भी भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है।
- भारत में हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और अनुमानित 40 मिलियन पुराने HVB संक्रमित लोगों के लिये "मध्यवर्ती से उच्च स्थानिकता" है, जो अनुमानित वैश्विक भार का लगभग 11% है।
- भारत में क्रोनिक HBV संक्रमण का प्रसार लगभग 3-4% जनसंख्या पर है।
- चुनौतियाँ:
- स्वास्थ्य सेवाओं तक अक्सर समुदायों की पहुँच नहीं होती है क्योंकि वे आमतौर पर केंद्रीकृत/विशेषीकृत अस्पतालों में उच्च कीमत पर उपलब्ध होती हैं जिन्हें सभी द्वारा वहन नहीं किया जा सकता है।
- देर से निदान या उचित उपचार की कमी के कारण लोगों की मौत हो जाती है। ऐसें में प्रारंभिक निदान, रोकथाम और सफल उपचार दोनों ही मामलों में आवश्यक है।
- दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में हेपेटाइटिस वाले लगभग 10% लोग ही अपनी स्थिति के प्रति सजग हैं और उनमें से केवल 5% लोग इलाज करवा रहे हैं।
- हेपेटाइटिस सी से ग्रसित अनुमानित 10.5 मिलियन लोगों में से केवल 7% ही अपनी स्थिति के प्रति सजग हैं, जिनमें से लगभग पाँच में से एक का इलाज चल रहा है।
हेपेटाइटिस हेतु वैश्विक लक्ष्य:
- परिचय:
- वैश्विक लक्ष्य 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में वायरल हेपेटाइटिस को खत्म करना है।
- लक्ष्य की प्राप्ति:
- वर्ष 2025 तक हमें हेपेटाइटिस बी और सी के नए संक्रमणों को 50% तक एवं यकृत कैंसर से होने वाली मौतों को 40% तक कम करना होगा, साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिये कि हेपेटाइटिस बी और सीपीड़ित 60% लोगों का निदान किया जाए और उनमें से आधे लोगों को उचित उपचार मिले।
- क्षेत्र के सभी देशों में राजनीतिक प्रतिबद्धता बढ़ाने की आवश्यकता है और:
- हेपेटाइटिस के लिये निरंतर घरेलू वित्तपोषण सुनिश्चित करना।
- कीमतों को और कम करके दवाओं एवं निदान तक पहुँच में सुधार करना।
- जागरूकता प्रसार के लिये संचार रणनीतियों का विकास करना।
- HIV में विभेदित और जन-केंद्रित सेवा वितरण विकल्पों का अधिकतम उपयोग के लिये सेवा वितरण में सुधार करना तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण के अनुरूप लोगों की ज़रूरतों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार सेवाएँ प्रदान करना।
- परिधीय स्वास्थ्य सुविधाओं, समुदाय-आधारित क्षेत्रों और अस्पताल से परे स्थानों पर हेपेटाइटिस देखभाल का विकेंद्रीकरण रोगियों को उनके घरों के करीब इलाज़ की सुविधा प्रदान करेगा।
- WHO द्वारा वायरल हेपेटाइटिस, एचआईवी और यौन संचारित संक्रमण (STI) के निदान हेतु वर्ष 2022-2026 के लिये एकीकृत क्षेत्रीय कार्ययोजना विकसित की जा रही है।
- यह क्षेत्र के लिये उपलब्ध सीमित संसाधनों का प्रभावी और कुशल उपयोग सुनिश्चित करेगा तथा देशों को रोग-विशिष्ट दृष्टिकोण के बजाय व्यक्ति-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिये मार्गदर्शन करेगा।
आगे की राह
- स्वच्छ भोजन और उचित व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ-साथ साफ पानी एवं स्वच्छता हमें हेपेटाइटिस A और E से बचा सकती है।
- हेपेटाइटिस B और C को रोकने के उपायों में जन्म की खुराक सहित हेपेटाइटिस B टीकाकरण के साथ-साथ सुरक्षित रक्त, सुरक्षित सेक्स और सुरक्षित सुई के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- नई और शक्तिशाली एंटीवायरल दवाओं के साथ-साथ हेपेटाइटिस B को रोकने के लिये सुरक्षित और प्रभावी टीके मौज़ूद हैं जिनका उपयोग क्रोनिक हेपेटाइटिस B के प्रबंधन और हेपेटाइटिस C के अधिकांश मामलों के इलाज में किया जा सकता है।
- प्रारंभिक निदान और जागरूकता अभियानों के साथ इन हस्तक्षेपों में वैश्विक स्तर पर वर्ष 2030 तक निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में 4.5 मिलियन समय पूर्व होने वाली मौतों को रोकने की क्षमता है।
- प्रारंभिक निदान और जागरूकता अभियानों के साथ इन हस्तक्षेपों में वैश्विक स्तर पर वर्ष 2030 तक निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में 4.5 मिलियन समय पूर्व होने वाली मौतों को रोकने की क्षमता है।
नोट:
- हेपेटाइटिस बी को भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के तहत शामिल किया गया है। जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा टाइप बी (Hib), खसरा, रूबेला, जापानी इंसेफेलाइटिस (JE), रोटावायरस डायरिया के कारण ग्यारह (हेपेटाइटिस B को छोड़कर) वैक्सीन-रोकथाम योग्य बीमारियों यानी तपेदिक, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, निमोनिया और मेनिनजाइटिस के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण प्रदान करता है।
- बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और थाईलैंड विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में हेपेटाइटिस बी को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने वाले पहले चार देश बन गए हैं।
- हाल ही में 'COBAS 6800' नामक एक स्वचालित कोरोनावायरस परीक्षण उपकरण लॉन्च किया गया था जो वायरल हेपेटाइटिस B और C का भी पता लगा सकता है।
- यह ध्यान दिया जा सकता है कि केवल चार बीमारियों जैसे HIV-एड्स (1 दिसंबर), टीबी (24 मार्च), मलेरिया (25 अप्रैल), हेपेटाइटिस के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) आधिकारिक तौर पर रोग-विशिष्ट वैश्विक जागरूकता दिवसों का समर्थन करता है।
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्न (पीवाईक्यू)प्रश्न. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही नहीं है? (a) यकृतशोध B विषाणु HIV की तरह ही संचरित होता है। उत्तर: (b) व्याख्या:
अतः विकल्प (b) सही उत्तर है। |
स्रोत : द हिंदू


शासन व्यवस्था
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021
प्रिलिम्स के लिये:डोपिंग, नाडा, वाडा। मेन्स के लिये:राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021 के प्रावधान और संबंधित मुद्दे। |
चर्चा में क्यों?
हाल ही में लोकसभा ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021 पारित किया, जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) के लिये वैधानिक ढाँचा तैयार करने का प्रयास करता है।
- केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा इसे पहली बार दिसंबर, 2021 में लोकसभा में पेश किया गया था।
- यह विधेयक खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करेगा क्योंकि यह उन्हें अपना पक्ष रखने के लिये पर्याप्त जगह प्रदान करेगा, खासकर जब वे डोपिंग रोधी आरोपों का सामना कर रहे हों।
विधेयक की मुख्य विशेषताएँ:
- डोपिंग का निषेध:
- विधेयक एथलीटों, एथलीट सपोर्ट कर्मियों और अन्य व्यक्तियों को खेल में डोपिंग में शामिल होने से रोकता है।
- उल्लंघन के परिणाम:
- डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के परिणामस्वरूप खिलाडी को अयोग्य ठहराया जा सकता है, जिसमें पदक, अंक और पुरस्कार की जब्ती, निर्धारित अवधि के लिये किसी प्रतियोगिता या कार्यक्रम में भाग लेने की अयोग्यता, वित्तीय प्रतिबंध आदि शामिल हैं।
- राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी हेतु वैधानिक समर्थन:
- विधेयक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी को वैधानिक निकाय के रूप में गठित करने का प्रावधान करता है।
- इसकी अध्यक्षता केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक करेगा। एजेंसी के कार्यों में शामिल हैं:
- डोपिंग रोधी गतिविधियों की योजना बनाना, उन्हें लागू करना और उनकी निगरानी करना।
- डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन की जाँच।
- डोपिंग रोधी अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- खेल में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड (National Board for Anti-Doping in Sports):
- डोपिंग रोधी विनियमन और डोपिंग रोधी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर सरकार को सिफारिशें करने के लिये विधेयक खेल क्षेत्र में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड की स्थापना करता है।
- बोर्ड एजेंसी की गतिविधियों की निगरानी करेगा और उसे निर्देश जारी करेगा।
- डोप परीक्षण प्रयोगशालाएँ:
- मौजूदा राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को प्रमुख डोप परीक्षण प्रयोगशाला माना जाएगा।
- केंद्र सरकार और अधिक राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित कर सकती है।
विधेयक का महत्त्व:
- डोपिंग से लड़ने में एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने के अलावा विधेयक एथलीटों को समयबद्ध न्याय प्राप्त करने का प्रयास करता है।
- यह खेलों के लिये अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने हेतु भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने का भी एक प्रयास है।
- यह विधेयक डोपिंग रोधी निर्णय के लिये एक मज़बूत, स्वतंत्र तंत्र स्थापित करने में मदद करेगा।
- यह विधेयक नाडा और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (NDTL) के कामकाज को कानूनी मान्यता देगा।
विधेयक से संबद्ध मुद्दे:
- महानिदेशक की योग्यता विधेयक में निर्दिष्ट नहीं हैं और नियमों के माध्यम से अधिसूचित करने के लिए छोड़ दी गई हैं।
- केंद्र सरकार दुर्व्यवहार या अक्षमता या "ऐसे अन्य आधार" पर महानिदेशक को पद से हटा सकती है।
- इन प्रावधानों को केंद्र सरकार के विवेक पर छोड़ने से महानिदेशक की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।
- यह विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अधिदेश के विरुद्ध भी है कि ऐसे निकायों को अपने संचालन में स्वतंत्र होना चाहिये।
- बिल के तहत बोर्ड के पास अनुशासन पैनल और अपील पैनल के सदस्यों को उन आधारों पर हटाने का अधिकार है जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किये जाएगे और बिल में निर्दिष्ट नहीं हैं।
- इसके अलावा उन्हें सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता नहीं है। यह इन पैनलों के स्वतंत्र कामकाज को प्रभावित कर सकता है।
डोपिंग और संबंधित एजेंसियाँ:
- परिचय:
- प्रदर्शन बढ़ाने के लिये खिलाडियों द्वारा कुछ निषिद्ध पदार्थों का सेवन।
- राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA):
- राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) को भारत में डोप मुक्त खेलों के लिये एक जनादेश के साथ 24 नवंबर, 2005 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया था।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA) कोड के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों को लागू करना, डोप नियंत्रण कार्यक्रम को विनियमित करना, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा डोपिंग एवं इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
- नाडा के पास इसके लिये आवश्यक अधिकार और ज़िम्मेदारी है:
- डोपिंग नियंत्रण में योजना, समन्वय, कार्यान्वयन, निगरानी और सुधार की वकालत करना;
- अन्य प्रासंगिक राष्ट्रीय संगठनों, एजेंसियों और अन्य डोपिंग रोधी संगठनों आदि के साथ सहयोग करना।
- वाडा:
- नवंबर 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के तहत विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA) की स्थापना की गई थी।
- खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (2005) द्वारा WADA को मान्यता दी गई है।
- WADA की प्राथमिक भूमिका सभी खेलों और देशों में एंटी-डोपिंग नियमों को विकसित करना, सामंजस्य तथा समन्वय स्थापित करना है।
- यह विश्व डोपिंग रोधी संहिता (वाडा कोड) और उसके मानकों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने, डोपिंग की घटनाओं की जाँच करने, डोपिंग पर शोध करने, खिलाड़ियों व संबंधित कर्मियों को डोपिंग रोधी नियमों के बारे में शिक्षित करने का कार्य करता है।
स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस


शासन व्यवस्था
मानव-पशु संघर्ष
प्रिलिम्स के लिये:मानव-पशु संघर्ष, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972। मेन्स के लिये:मानव-पशु संघर्ष और उसके प्रभाव। |
चर्चा में क्यों?
हाल ही में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने लोकसभा में जानकारी दी कि मानव- वन्यजीव संघर्षों की घटनाओं में वृद्धि हुई है।
मानव- वन्यजीव संघर्ष
- परिचय:
- मानव-वन्यजीव संघर्ष (HWC) उन संघर्षों को संदर्भित करता है जब वन्यजीवों की उपस्थिति या व्यवहार मानव हितों या ज़रूरतों के लिये वास्तव में या प्रत्यक्ष रूप से खतरों का कारण बनता है जिसके कारण लोगों, जानवरों, संसाधनों तथा आवास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- कारण:
- प्राकृतिक वास का नुकसान।
- जंगली जानवरों की आबादी में वृद्धि।
- जंगली जानवरों को खेत की ओर आकर्षित करने वाले फसल पैटर्न बदलना।
- वन क्षेत्र से जंगली जानवरों का भोजन और चारे के लिये मानव-प्रधान भू-भागों में आना-जाना।
- वनोपज के अवैध संग्रहण के लिये मनुष्यों का वनों की ओर आना-जाना।
- आक्रामक विदेशी प्रजातियों आदि की वृद्धि के कारण आवास का क्षरण।
- प्रभाव:
- जान गँवाना।
- जानवर और इंसान दोनों को चोट लगना।
- फसलों और कृषि भूमि को नुकसान।
- जानवरों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि।
- संबंधित डेटा:
- 2018-19 और 2020-21 के बीच देश भर में बिजली के करंट से 222 हाथियों की मौत हो गई।
- इसके अलावा वर्ष 2019 और 2021 के बीच अवैध शिकार के चलते 29 बाघ मारे गए, जबकि 197 बाघों की मौत की जाँच की जा रही है।
- जानवरों के साथ मानव के संघर्ष के दौरान हाथियों ने तीन वर्षों में 1,579 मनुष्यों को मार डाला– वर्ष 2019-20 में 585, 2020-21 में 461 और 2021-22 में 533।
- 332 मौतों के साथ ओडिशा सबसे ऊपर है, इसके बाद 291 के साथ झारखंड और 240 के साथ पश्चिम बंगाल है।
- जबकि वर्ष 2019 से 2021 के बीच बाघों ने रिज़र्व में 125 इंसानों को मार डाला।
- इनमें से लगभग आधी मौतें महाराष्ट्र में हुईं है।
संघर्ष से निपटने के लिये की गई पहल:
- मानव-वन्यजीव संघर्ष (HWC) के प्रबंधन के लिये सलाह: यह राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (SC-NBWL) की स्थायी समिति द्वारा जारी किया गया है।
- ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना: परामर्श में वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसार समस्याग्रस्त जंगली जानवरों से निपटने के लिये ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने की परिकल्पना की गई है।
- बीमा प्रदान करना: HWC के कारण फसल क्षति के लिये मुआवज़े हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऐड-ऑन कवरेज का उपयोग करना।
- चारा बढ़ाना: वन क्षेत्रों के भीतर चारे और जल स्रोतों को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है।
- सक्रिय उपाय करना: स्थानीय/राज्य स्तर पर अंतर-विभागीय समितियों को निर्धारित करना, पूर्व चेतावनी प्रणाली को अपनाना, बाधाओं का निर्माण, टोल-फ्री हॉटलाइन नंबरों के साथ समर्पित सर्कल-वार नियंत्रण कक्ष, हॉटस्पॉट की पहचान आदि।
- तत्काल राहत प्रदान करना: पीड़ित/परिवार को घटना के 24 घंटे के भीतर अंतरिम राहत के रूप में अनुग्रह राशि के एक हिस्से का भुगतान।
आगे की राह
- मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिये सबसे व्यापक तरीके शमन के रूप में खोजे जाते हैं या वन्यजीवों को उच्च घनत्व मानव आबादी या कृषि वाले क्षेत्रों से बाहर रखना है।
- जनता के बीच शिक्षा और जागरूकता के प्रसार की आवश्यकता है ताकि उन्हें मानव-पशु संघर्ष के बारे में जागरूक किया जा सके, जिससे संघर्ष को रोकने के लिये दीर्घकालिक स्थायी समाधान विकसित होगा।
- यह सुनिश्चित करना कि मनुष्यों और जानवरों के पास जीवन-निर्वाह के लिये पर्याप्त जगह है यह मानव-वन्यजीव संघर्ष समाधान का आधार है।
- जंगली भूमि और प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना महत्त्वपूर्ण है, लेकिन जंगली और शहरी क्षेत्रों के बीच बफर ज़ोन बनाना भी महत्त्वपूर्ण है।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न:प्रश्न. वाणिज्य में प्राणिजात और वनस्पति-जात के व्यापार-संबंधी विश्लेषण (TRAFFIC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: 1- TRAFFIC, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के अंतर्गत एक ब्यूरो है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: B व्याख्या:
|
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस


शासन व्यवस्था
स्टार्टअप्स
प्रिलिम्स के लिये:स्टार्टअप्स, स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन (NIDHI), युवा और महत्त्वाकांक्षी इनोवेटर्स तथा स्टार्टअप्स (PRAYAS), अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा देना और स्टार्टअप्स का विकास करना। मेन्स के लिये:स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और उसका महत्त्व। |
चर्चा में क्यों?
सरकार के विभिन्न सुधारों और पहलों से भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी आई है।
स्टार्टअप्स:
- परिचय:
- स्टार्टअप शब्द एक कंपनी के संचालन के पहले चरण को संदर्भित करता है। स्टार्टअप एक या एक से अधिक उद्यमियों द्वारा स्थापित किये जाते हैं जो एक ऐसे उत्पाद या सेवा का विकास करना चाहते हैं जिसकी बाज़ार में मांग है।
- ये कंपनियाँ आमतौर पर उच्च लागत और सीमित राजस्व के साथ शुरू होती हैं, यही वजह है कि वे उद्यम पूंजीपतियों जैसे विभिन्न स्रोतों से पूंजी की मांग करती हैं।
- भारत में स्टार्टअप्स की वृद्धि :
- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) ने स्टार्टअप को मान्यता दी है जो 56 विविध क्षेत्रों से संबंधित हैं।
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एनालिटिक्स आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित क्षेत्रों में 4,500 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता प्रदान की गई है।
- इस दिशा में निरंतर सरकारी प्रयासों के परिणामस्वरूप मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या वर्ष 2016 के 471 से बढ़कर वर्ष 2022 में 72,993 हो गई है।
- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) ने स्टार्टअप को मान्यता दी है जो 56 विविध क्षेत्रों से संबंधित हैं।
स्टार्टअप-इंडिया योजना का भारत के स्टार्टअप्स के विकास में योगदान:
स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार द्वारा शुरू किये गए विभिन्न कार्यक्रमों ने स्टार्टअप्स के विकास को सुगम बनाया है:
- स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान: इसमें सरलीकरण, मार्गदर्शन, वित्तीय समर्थन, प्रोत्साहन और उद्योग शिक्षाविद, साझेदारी एवं इनक्यूबेशन जैसे क्षेत्रों में विस्तारित 19 घटक शामिल हैं।
- कार्य योजना ने देश में एक जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिये परिकल्पित सरकारी सहायता, योजनाओं और प्रोत्साहनों की नींव रखी।
- स्टार्टअप इंडिया हब: यह भारत में उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के सभी हितधारकों के लिये एक-दूसरे को खोजने, जोड़ने और संलग्न करने हेतु अपनी तरह का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है।
- ऑनलाइन हब स्टार्टअप, निवेशक, फंड, सलाहकार, शैक्षणिक संस्थान, इनक्यूबेटर, एक्सेलेरेटर, कॉर्पोरेट, सरकारी निकायों को मेज़बानी प्रदान करता हैै।
- 3 साल के लिए आयकर छूट: 1 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद निगमित स्टार्टअप्स के निगमन के बाद से 10 वर्षों में से लगातार 3 वर्षों की अवधि के लिये आयकर से छूट दी गई है।
- स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS): इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स को अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाज़ार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- भारतीय स्टार्टअप के लिये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार पहुँच: स्टार्टअप इंडिया ने 15 से अधिक साझेदार देशों (ब्राजील, स्वीडन, रूस, पुर्तगाल, यूके, फिनलैंड, नीदरलैंड, सिंगापुर, इज़रायल, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, क्रोएशिया, कतर और संयुक्त अरब अमीरात) के साथ परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने में सहायता हेतु स्टार्टअप के लिये सॉफ्ट लैंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किये हैं।,
स्टार्टअप्स को हैंडहोल्डिंग प्रदान करने वाले अन्य कारक:
- सरकारी योजनाएँ :
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने सफल स्टार्टअप में विचारों और नवाचारों (ज्ञान-आधारित एवं प्रौद्योगिकी-संचालित) को पोषित करने के लिये नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन (NIDHI) नामक एक अम्ब्रेला कार्यक्रम शुरू किया था।
- स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये युवा और महत्त्वाकांक्षी इनोवेटर्स एवं स्टार्टअप्स (PRAYAS) कार्यक्रम को बढ़ावा देना और उसे तेज़ी से शुरू किया गया था।
- जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा:
- जैव प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिये जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी फर्मों को बढ़ावा देता है तथा उनका पोषण करता है।
- रक्षा क्षेत्र:
- रक्षा उत्पादन विभाग ने उद्योगों, R&D संस्थानों और शिक्षाविदों को शामिल करके तथा उन्हें R&D के लिये अनुदान प्रदान कर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, रक्षा एवं एयरोस्पेस में नवाचार तथा प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिये रक्षा उत्कृष्टता के लिये नवाचार (iDEX) कार्यक्रम शुरू किया।
- अटल नवाचार मिशन (AIM):
- अटल नवाचार मिशन के तहत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप को इनक्यूबेट करने के लिये अटल इनक्यूबेशन सेंटर (AIC) की स्थापना की है।
- इसने राष्ट्रीय महत्त्व और सामाजिक प्रासंगिकता की क्षेत्रीय चुनौतियों को हल करने वाले प्रौद्योगिकी-आधारित नवाचारों के साथ स्टार्टअप्स को सीधे सहायता देने के लिये अटल न्यू इंडिया चैलेंज (ANIC) कार्यक्रम भी शुरू किया है।
- विदेशी मुद्रा प्रवाह की भूमिका:
- भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में विशेष रूप से प्रमुख तकनीकी कंपनियों जैसे फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से विदेशी मुद्रा का प्रवाह घरेलू बाज़ार की अपार संभावनाओं का संकेत देता है।
- प्रौद्योगिकी की भूमिका:
- नए तकनीकी उपकरणों के साथ स्टार्टअप समुदाय व्यापक बाज़ार अंतराल को समाप्त करने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा, रोबोटिक्स आदि जैसे नए युग की तकनीकों का लाभ उठा रहा है।
आगे की राह
- स्टार्टअप्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि कई उद्यमी अपने परिवार और सामाजिक वातावरण द्वारा अपने शौक को पूरा करने से हतोत्साहित होते रहते हैं तथा नौकरी एवं जीवन शैली का चयन (जो अधिक स्थिरता प्रदान करने के लिये देखा जाता है) करने के लिये दबाव में होते हैं।
- अवसर की इच्छा रखने वाले को अधिक पुरस्कृत किया जाना चाहिये और असफलता को नकारात्मक रूप से नहीं देखा जाना चाहिये।
- इसके अलावा पूर्वाग्रहों को तोड़ना बढ़ती विविधता की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है, जो सफल होने के लिये आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।
- देश के निर्माताओं, जोखिम उठाने वाली कंपनियों और फंडिंग एजेंसियों को घरेलू पूंजी की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये अनुकूल माहौल बनाने की ज़रूरत है।
- नवाचार को प्रोत्साहित करने और उभरते व्यापार मॉडल को समर्थन देने वाले उपयुक्त नियमों को तैयार कर नियामकों को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
- नवाचार को प्रोत्साहित करने और उभरते व्यापार मॉडल को समर्थन देने वाले उपयुक्त नियमों को तैयार कर नियामकों को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न:प्रश्न. उद्यम पूंजी से क्या तात्पर्य है? (2014) (a) उद्योगों को उपलब्ध कराई गई अल्पकालीन पूंजी उत्तर: (b) व्याख्या:
|
स्रोत: पी.आई.बी.


भारतीय राजव्यवस्था
PMLA तथा सर्वोच्च न्यायालय
प्रिलिम्स के लिये:विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999, FEMA, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 FEOA, विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 COFEPOSA, ED, सर्वोच्च न्यायालय मेन्स के लिये:मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा, काले धन का महत्त्व, ईडी की शक्तियाँ न्यायिक समीक्षा |
चर्चा में क्यों?
हाल ही में एक याचिका कि सुनवाई में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
- न्यायालय ने रेखांकित किया कि आरोपी/अपराधी की बेगुनाही के सिद्धांत को एक मानव अधिकार के रूप में माना जाता है, लेकिन इस अवधारणा को संसद/विधायिका द्वारा बनाए गए कानून द्वारा बाधित किया जा सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:
- प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR):
- प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ECIR) की तुलना प्राथमिकी से नहीं की जा सकती।
- प्रत्येक मामले में संबंधित व्यक्ति को ECIR की आपूर्ति अनिवार्य नहीं है और "यह पर्याप्त है यदि प्रवर्तन निदेशालय (ED), गिरफ्तारी के समय, ऐसी गिरफ्तारी के आधार का खुलासा करता है"।
- ECIR ईडी का एक आंतरिक दस्तावेज़ है और यह तथ्य कि अनुसूचित अपराध के संबंध में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, ईडी अधिकारियों के जाँच/परीक्षण शुरू करने के मामले में दखल नहीं करता है।
- प्रत्येक मामले में संबंधित व्यक्ति को ECIR की आपूर्ति अनिवार्य नहीं है और "यह पर्याप्त है यदि प्रवर्तन निदेशालय (ED), गिरफ्तारी के समय, ऐसी गिरफ्तारी के आधार का खुलासा करता है"।
- प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ECIR) की तुलना प्राथमिकी से नहीं की जा सकती।
- PMLA अधिनियम की धारा 3:
- PMLA अधिनियम 2002 की धारा 3 की व्यापक पहुँच है और यह दर्शाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि के संबंध में एक स्वतंत्र अपराध है जो एक अनुसूचित अपराध से संबंधित या उसके संबंध में आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त किया गया था।
- निर्णय ने यह भी स्पष्ट किया कि:
- धारा 3 के तहत अपराध "एक अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप संपत्ति के अवैध लाभ पर निर्भर है"।
- वर्ष 2002 के अधिनियम के तहत प्राधिकरण किसी भी व्यक्ति पर काल्पनिक आधार पर या इस धारणा के आधार पर मुकदमा नहीं चला सकते हैं कि अपराध हुआ है लेकिन यह पुलिस के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत नहीं है और सक्षम मंच के समक्ष आपराधिक शिकायत जाँच लंबित है।
- धारा 3 के तहत अपराध "एक अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप संपत्ति के अवैध लाभ पर निर्भर है"।
- प्रवर्तन निदेशालय (ED):
- पीठ ने अधिनियम की धारा 5 (अपराध की किसी भी आय की अस्थायी कुर्की का आदेश) के तहत ED की शक्ति को बरकरार रखा।
- न्यायालय ने कहा कि धारा 5 व्यक्ति के हितों को सुरक्षित करने के लिये एक संतुलन व्यवस्था प्रदान करती है और यह भी सुनिश्चित करती है कि अपराध अधिनियम, 2002 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से निपटने के लिये उपलब्ध रहे।
- इसने इस तर्क को खारिज कर दिया कि ED अधिकारी पुलिस अधिकारी हैं और इसलिये अधिनियम की धारा 50 के तहत उनके द्वारा दर्ज बयान संविधान के अनुच्छेद 20 (3) से प्रभावित होगा, जिसमें कहा गया है कि अपराध का आरोपी कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ गवाह बनने के लिये मज़बूर नहीं किया जाएगा।
- पीठ ने अधिनियम की धारा 5 (अपराध की किसी भी आय की अस्थायी कुर्की का आदेश) के तहत ED की शक्ति को बरकरार रखा।
धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002
- यह आपराधिक कानून है जो धन शोधन/मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित मामलों से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करने के लिए बनाया गया है।
- यह मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिये भारत द्वारा स्थापित कानूनी ढाँचे का मूल है।
- इस अधिनियम के प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों (RBI सहित), म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं।
- PMLA (संशोधन) अधिमियम, 2012:
- इसमें 'रिपोर्टिंग इकाई' की अवधारणा शामिल है जिसमें बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान, मध्यस्थ आदि शामिल होंगे।
- PMLA, 2002 में 5 लाख रुपए तक का ज़ुर्माना लगाने का प्रावधान था, लेकिन संशोधन अधिनियम में इस ऊपरी सीमा को हटा दिया गया है।
- इसमें गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति की संपत्ति की अस्थायी कुर्की और ज़ब्ती का प्रावधान किया गया है।
प्रवर्तन निदेशालय:
- संगठनात्मक इतिहास:
- प्रवर्तन निदेशालय या ED एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन है जो आर्थिक अपराधों की जाँच और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के लिये अनिवार्य है।
- इस निदेशालय की उत्पत्ति 1 मई, 1956 को हुई, जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (फेरा '47) के तहत विनिमय नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिये आर्थिक मामलों के विभाग में एक 'प्रवर्तन इकाई' का गठन किया गया।
- समय बीतने के साथ, FERA'1947 कानून को FERA’1973 कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 04 साल की अवधि (1973-1977) के लिये निदेशालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में रहा। पुनः आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत के साथ, FERA’1973 (जो एक नियामक कानून था) निरस्त कर दिया गया और इसके स्थान पर 1 जून, 2000 से एक नया कानून-विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) लागू किया गया।
- हाल ही में विदेशों में शरण लेने वाले आर्थिक अपराधियों से संबंधित मामलों की संख्या में वृद्धि के साथ सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA) पारित किया है और ED को इसे लागू करने का जिम्मा सौंपा गया है।
- कार्य:
- मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम, 2002 (PMLA):
- इसके तहत धन शोधन के अपराधों की जाँच करना, संपत्ति की कुर्की और जब्ती की कार्रवाई करना और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाना हैं।
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA):
- इसके तहत निदेशालय नामित अधिकारियों द्वारा फेमा के उल्लंघन के दोषियों की जाँच की जाती है और इसमें शामिल राशि का तीन गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
- भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA):
- इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों को दंडित करना है जो भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर कानून की प्रक्रिया से बचने के उपाय खोजते हैं।
- COFEPOSA के तहत प्रायोजक एजेंसी:
- FEMA के उल्लंघन के संबंध में विदेशी मुद्रा और संरक्षण गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (COFEPOSA) के तहत निवारक निरोध के प्रायोजक मामले देखना।
- FEMA के उल्लंघन के संबंध में विदेशी मुद्रा और संरक्षण गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (COFEPOSA) के तहत निवारक निरोध के प्रायोजक मामले देखना।
- मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम, 2002 (PMLA):
विगत वर्ष के प्रश्न(PYQs)प्रारंभिक परीक्षा:भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन-सा एक मदसमूह सम्मिलित है? (2013) (a) विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, विशेष आहरण अधिकार (SDR) तथा विदेशों से ऋण उत्तर:B व्याख्या:
अतः विकल्प B सही है। प्रश्न. चर्चा कीजिये कि उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण धन शोधन में कैसे योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर धन शोधन की समस्या से निपटने के लिये विस्तृत उपाय सुझाइए। (2021, मुख्य परीक्षा) प्रश्न. दुनिया के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उत्पादक राज्यों के साथ भारत की निकटता ने उसकी आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों जैसे- बंदूक रखना , मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिये। इसे रोकने के लिये क्या उपाय किये जाने चाहिये? (2018, मुख्य परीक्षा) |
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस