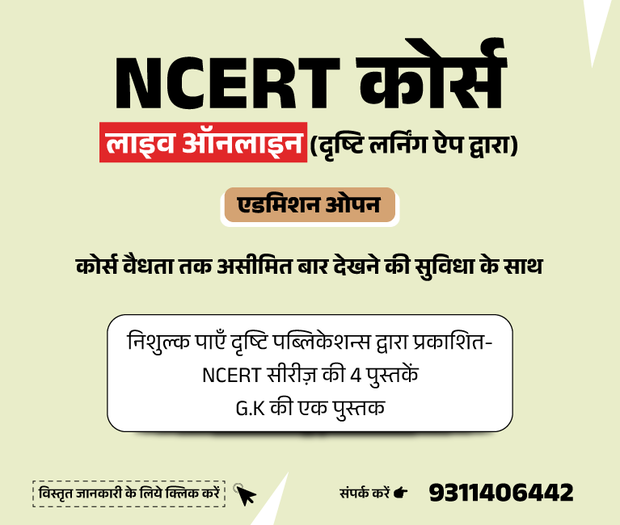अंतर्राष्ट्रीय संबंध
भूटान के राजा भारत दौरे पर
प्रिलिम्स के लिये:चूखा जलविद्युत परियोजना, भारत-भूटान सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट, STEM-आधारित पहल, भारत इंटरफेस फॉर मनी। मेन्स के लिये:भारत-भूटान संबंध। |
चर्चा में क्यों?
भूटान के राजा ने भारत का दौरा किया और भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की, जहाँ दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग एवं राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय हितों के मुद्दों पर चर्चा की।
प्रमुख बिंदु
- भूटान की विकास योजनाएँ:
- भूटान की परिवर्तन पहल और सुधार प्रक्रिया एवं भूटान की विकास महत्त्वाकांक्षाओं हेतु भारत का समर्थन, विशेष रूप से वर्ष 2024 में शुरू होने वाली 13वीं पंचवर्षीय योजना इस चर्चा का मुख्य विषय था।
- भूटान की वर्ष 2023 में सबसे अल्प विकसित देशों की सूची से निकलने की उम्मीद है, साथ ही इसका अगले दस वर्षों में 12,000 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय के साथ एक विकसित देश बनने का लक्ष्य है।
- ऋण सुविधा और वित्तीय सहायता:
- संस्थागत क्षमता निर्माण और सुधारों हेतु वित्तीय सहायता पर चर्चा करने के अलावा, भारत भूटान को तीसरी अतिरिक्त स्टैंडबाय क्रेडिट सुविधा देने पर भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने भारत-भूटान उपग्रह के हालिया लॉन्च सहित जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा परियोजनाओं के साथ-साथ अंतरिक्ष सहयोग सहित ऊर्जा सहयोग के बारे में भी बात की है।
- जलविद्युत परियोजना के लिये पावर टैरिफ:
- भारत सरकार ने चूखा जलविद्युत परियोजना हेतु विद्युत शुल्क बढ़ाने के लिये भूटान की लंबे समय से लंबित मांग पर सहमति व्यक्त की है, जिसका परिचालन वर्ष 1986 में भारत की मदद से शुरू किया था।
- इसके अलावा भारत ने वर्ष 2008 में ऑस्ट्रियाई समर्थित बसोचू जलविद्युत परियोजना से विद्युत खरीदने के बारे में चर्चा करने के लिये सहमति जताई है।
- संकोश जलविद्युत परियोजना:
- दोनों देश पर्यावरण और लागत संबंधी चिंताओं के कारण दशकों से लंबित जलाशय आधारित 2,500 मेगावाट संकोश जलविद्युत परियोजना पर बातचीत में तेज़ी लाने का भी प्रयास करेंगे।
- एकीकृत चेक पोस्ट:
- भारत जयगाँव में भारत-भूटान सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट स्थापित करने और प्रस्तावित कोकराझार-गेलेफू रेल लिंक परियोजना में तेज़ी लाने की संभावनाओं पर भी विचार कर रहा है।
- रेल और हवाई मार्ग लिंक:
- भारत के साथ सीमा के पास भूटान गेलेफू में अपने दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कर रहा है। रेल लिंक परियोजना दक्षिणी भूटानी शहर को अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने का एक केंद्र बनाने में मदद करेगी।
- डिजिटल अवसंरचना:
- सहयोग के पारंपरिक क्षेत्रों से परे नए क्षेत्रों में सहयोग पर भी चर्चा की गई, जैसे नई STEM-आधारित पहल, तीसरे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे जैसे डिजिटल अवसंरचना की स्थापना, भारत के राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के साथ भूटान के ड्रुकरेन (DrukRen) का एकीकरण (ई-लर्निंग के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण सहयोग), ई-लर्निंग पर भूटान के प्रयासों की पूरक ई-लाइब्रेरी परियोजना।
- वित्तीय सहयोग:
- वित्तीय सहयोग अथवा एकीकरण के तहत RuPay परियोजना का पहला चरण शुरू किया गया था।
- भारत का भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM) भी जुलाई 2021 में लॉन्च किया गया था।
- दोनों पक्ष भूटान में BHIM ऐप के कार्यान्वयन की भी समीक्षा करेंगे।
भारत-भूटान संबंध:
- शांति एवं मित्रता की भारत-भूटान संधि, 1949:
- यह संधि अन्य बातों के अलावा, स्थायी शांति एवं मित्रता, मुक्त व्यापार और वाणिज्य तथा एक दूसरे के नागरिकों हेतु समान न्याय प्रदान करती है।
- वर्ष 2007 में संधि पर फिर से बातचीत की गई तथा भूटान की संप्रभुता को प्रोत्साहित करने के लिये प्रावधानों को शामिल किया गया, जिससे विदेश नीति पर भारत का मार्गदर्शन प्राप्त करने की आवश्यकता समाप्त हो गई।
- बहुपक्षीय भागीदारी:
- दोनों बहुपक्षीय मंचों को साझा करते हैं जैसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC), ‘बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल’ (BBIN), तथा बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC) आदि।
- जलविद्युत सहयोग:
- यह जलविद्युत सहयोग वर्ष 2006 के जल विद्युत क्षेत्र में सहयोग समझौते के अंतर्गत है। इस समझौते के एक प्रोटोकॉल के तहत, भारत वर्ष 2020 तक न्यूनतम 10,000 मेगावाट जलविद्युत के विकास तथा उसी से अधिशेष विद्युत के आयात में भूटान की सहायता करने हेतु सहमत हुआ है।
- भूटान में कुल 2136 मेगावाट की चार जलविद्युत परियोजनाएँ (HEPs) - चूखा, कुरिछु, ताला और मंगदेछू पहले से ही संचालित हैं तथा भारत को विद्युत की आपूर्ति कर रही हैं।
- अंतर-सरकारी मोड में दो HEPs नामत: पुनात्सांगछू-I, पुनात्सांगछू-II कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं
- व्यापार:
- दोनों देशों के बीच व्यापार भारत- भूटान व्यापार और पारगमन समझौते, 1972 द्वारा संचालित होता है जिसे अंतिम बार नवंबर 2016 में नवीनीकृत किया गया था।
- नवंबर 2021 में भारत सरकार ने भारत के साथ भूटान के द्विपक्षीय तथा पारगमन व्यापार के लिये सात नए व्यापार मार्गों को खोलने की औपचारिक घोषणा की।
- इन नए मार्गों से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने तथा दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ने की उम्मीद है।
- इसके अलावा भूटान से भारत में 12 कृषि उत्पादों के औपचारिक निर्यात की अनुमति प्रदान करने हेतु नई बाज़ार पहुँच प्रदान की गई है, जिससे देश के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- आर्थिक सहायता:
- भारत, भूटान का प्रमुख विकास भागीदार है। वर्ष 1961 में भूटान की पहली पंचवर्षीय योजना (FYP) के शुभारंभ के बाद से, भारत भूटान की FYPs को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। भारत ने भूटान की 12वीं FYP (वर्ष 2018-23) के लिये 4500 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।
- शैक्षिक एवं सांस्कृतिक सहयोग:
- बड़ी संख्या में भूटानी छात्र भारत में अध्ययन करते हैं। भारत सरकार भूटानी छात्रों को कई प्रकार की छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती है।
आगे की राह
- भारत-भूटान संबंधों के संदर्भ में पर्यावरणीय स्थिरता के महत्त्व को कम करके नहीं आँका जा सकता है। भारत और भूटान दोनों ही प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न हैं और यह अनिवार्य है कि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिये इन संसाधनों को संरक्षित और सुरक्षित करने हेतु मिलकर कार्य करें।
- इसलिये यह महत्त्वपूर्ण है कि भारत और भूटान अपने द्विपक्षीय संबंधों में पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता देना जारी रखें और सतत् विकास को बढ़ावा देने तथा प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने के अपने साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करें।
स्रोत: द हिंदू


जैव विविधता और पर्यावरण
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और जलवायु परिवर्तन
प्रिलिम्स के लिये:UNFCCC, UNGA, पेरिस समझौता, UNCLOS, NDC, ग्लोबल वार्मिंग, ICJ मेन्स के लिये:अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और जलवायु परिवर्तन। |
चर्चा में क्यों?
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (UNFCCC) के आधार पर जलवायु परिवर्तन के प्रति देशों के दायित्त्वों पर एक प्रस्ताव पारित करके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) से अपनी राय देने का निर्देश दिया है।
- इस प्रस्ताव को विश्व के सबसे छोटे देशों में से एक, प्रशांत के वानुअतु द्वीप द्वारा आगे बढ़ाया गया था, एक द्वीप जो वर्ष 2015 में चक्रवात पाम के प्रभाव से तबाह हो गया था, माना जाता है कि यह जलवायु परिवर्तन से प्रेरित था जिसने इसकी 95% फसलों को नष्ट दिया और इसकी दो-तिहाई आबादी को प्रभावित किया।
प्रस्ताव:
- UNGA ने ICJ से दो प्रश्नों के उत्तर पूछे:
- वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिये जलवायु प्रणाली की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत राज्यों के क्या दायित्त्व हैं?
- राज्यों के लिये इन दायित्त्वों के अंतर्गत कानूनी कर्तव्य क्या हैं, जहाँ उन्होंने अपने कृत्यों और लापरवाहियों से जलवायु प्रणाली को महत्त्वपूर्ण नुकसान पहुँचाया है, विशेष रूप से छोटे द्वीप, विकासशील राज्यों (SIDS) और उन लोगों के लिये जिन्हें क्षति हुई है।
- यह प्रस्ताव पेरिस जलवायु समझौते और संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS) जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को संदर्भित करता है।
- ICJ को अपनी राय देने में करीब 18 महीने लगेंगे।
भारत की स्थिति:
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है, लेकिन यह सामान्यतः जलवायु न्याय और ग्लोबल वार्मिंग के लिये जवाबदेही का समर्थन करता है।
- भारत सरकार ने इसके निहितार्थ और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का आकलन करने के लिये कानूनी अधिकारियों को संकल्प भेजा है।
- भारत ने अपनी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) प्रतिबद्धताओं को अद्यतन किया है और 2030 तक नवीकरणीय स्रोतों से अपनी आधी बिजली प्राप्त करने की योजना बनाई है, लेकिन इसने मसौदा प्रस्ताव को सह-प्रायोजित नहीं किया।
- भारत संकल्प के प्रति अमेरिका और चीन जैसी प्रमुख शक्तियों की प्रतिक्रिया को अद्यतन संसूचित रूप से देख रहा है, क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिये उनका समर्थन महत्त्वपूर्ण है।
- भारत ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि ICJ प्रक्रिया केवल जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित कर सकती है और किसी एक देश को लक्षित नहीं कर सकती है। भारत ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि "टॉप-टू-बॉटम" आधार पर राय थोपने के किसी भी प्रयास का विरोध किया जाएगा।
क्या ICJ की राय बाध्यकारी है?
- ICJ की सलाह निर्णय के रूप में कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होगी, लेकिन यह कानूनी महत्त्व और नैतिक अधिकार रखती है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानूनों पर महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण प्रदान कर सकता है, साथ ही COP प्रक्रिया में जलवायु वित्त, जलवायु न्याय, नुकसान तथा क्षति निधि से संबंधित मुद्दों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकता है।
- अतीत में ICJ की सलाहकारी राय का फिलीस्तीनी संघर्ष और चागोस द्वीपों पर यूनाइटेड किंगडम एवं मॉरीशस के बीच विवाद जैसे मामलों में पालन किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय:
- वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में ‘संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय' पर हस्ताक्षर किये गए, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन (Earth Summit), रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है।
- भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है, जिसने जलवायु परिवर्तन (UNFCCC), जैवविविधता (जैविक विविधता पर सम्मेलन) और भूमि (संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय) पर तीनों रियो सम्मेलनों की मेज़बानी की है।
- UNFCCC 21 मार्च, 1994 से लागू हुआ और 197 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई।
- यह वर्ष 2015 के पेरिस समझौते की मूल संधि (Parent Treaty) है। UNFCCC वर्ष 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol) की मूल संधि भी है।
- UNFCCC सचिवालय (यूएन क्लाइमेट चेंज) संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो जलवायु परिवर्तन के खतरे पर वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करती है। यह बॉन (जर्मनी) में स्थित है।
- इसका उद्देश्य वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को एक स्तर पर स्थिर करना है, जिससे एक समय-सीमा के भीतर खतरनाक नतीजों को रोका जा सके ताकि पारिस्थितिक तंत्र को स्वाभाविक रूप से अनुकूलित कर सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. “मोमेंटम फॉर चेंज: क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ” यह पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी? (2018) (a) जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल उत्तर: (c) व्याख्या:
अतः विकल्प (c) सही है। मेन्स:प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC) के सी.ओ.पी. के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ क्या हैं? (2021) |
स्रोत: द हिंदू


जैव विविधता और पर्यावरण
भारत में सौर फोटोवोल्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु चुनौतियाँ तथा समाधान
प्रिलिम्स के लिये:फोटोवोल्टिक अपशिष्ट और इसके उदाहरण, संबंधित पहलें मेन्स के लिये:भारत और विश्व के अन्य हिस्सों में सौर अपशिष्ट का प्रबंधन, सौर अपशिष्ट से उत्पन्न चुनौतियाँ, सुझाव और संबंधित पहल। |
चर्चा में क्यों?
भारतीय नीति निर्माताओं द्वारा चक्रीय अर्थव्यवस्था की तरफ संक्रमण के प्रयासों के बावजूद वर्तमान में सौर फोटोवोल्टिक (Solar Photovoltaic- PV) उद्योग में अपशिष्ट प्रबंधन हेतु स्पष्ट निर्देशों का अभाव है।
फोटोवोल्टिक अपशिष्ट (PV Waste):
- परिचय:
- फोटोवोल्टिक अपशिष्ट सौर पैनलों द्वारा छोड़े गए इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट से उत्पन्न होता है। उन्हें देश में स्क्रैप के रूप में बेचा जाता है।
- अनुमान है कि अगले दशक तक यह कम-से-कम चार-पाँच गुना बढ़ सकता है। अतः भारत को सौर अपशिष्ट से निपटने हेतु व्यापक नियमों का मसौदा तैयार करने पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
- सौर PV की संरचना:
- भारत के सौर PV प्रतिष्ठानों में क्रिस्टलीय सिलिकॉन (c-Si) प्रौद्योगिकी का प्रभुत्त्व है। विशिष्ट PV पैनल c-Si मॉड्यूल (93%) और कैडमियम टेल्यूराइड थिन-फिल्म मॉड्यूल (7%) से बना होता है।
- c-Si मॉड्यूल में मुख्य रूप से ग्लास शीट, एल्यूमीनियम फ्रेम, एन्कैप्सुलेंट, बैक शीट, ताँबे के तार और सिलिकॉन वेफर्स होते हैं। c-Si मॉड्यूल बनाने हेतु चाँदी, टिन एवं सीसा का उपयोग किया जाता है। थिन-फिल्म मॉड्यूल ग्लास, एनकैप्सुलेंट तथा कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स से बना होता है।
- भारत के सौर PV प्रतिष्ठानों में क्रिस्टलीय सिलिकॉन (c-Si) प्रौद्योगिकी का प्रभुत्त्व है। विशिष्ट PV पैनल c-Si मॉड्यूल (93%) और कैडमियम टेल्यूराइड थिन-फिल्म मॉड्यूल (7%) से बना होता है।
- PV अपशिष्ट में भारत की स्थिति:
- विश्व स्तर पर भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा सौर PV स्थापित करने वाला देश है। नवंबर 2022 में स्थापित सौर क्षमता लगभग 62GW थी। इससे बड़ी मात्रा में सौर PV अपशिष्ट निकलता है।
- अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी की वर्ष 2016 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत वर्ष 2030 तक 50,000-3,25,000 टन PV अपशिष्ट और 2050 तक चार मिलियन टन से अधिक अपशिष्ट उत्पन्न कर सकता है।
अपशिष्ट की पुनर्प्राप्ति या पुनर्चक्रण:
- जब PV पैनल समाप्त होने वाला होता है, तो कुछ फ्रेम को हटा दिया जाता है और स्क्रैप के रूप में बेच दिया जाता है, साथ ही जंक्शनों एवं केबलों को ई-अपशिष्ट नियमों के अनुसार पुनर्नवीनीकरण किया जाता है।
- कांच के टुकड़े को आंशिक रूप से पुनर्नवीकृत किया जाता है, जबकि सीमेंट भट्टियों में मॉड्यूल को जलाकर सिलिकॉन और चाँदी को निष्कर्षित किया जा सकता है। हालाँकि कुल सामग्री का लगभग 50% पुनर्प्राप्त किया जा सकता है और केवल लगभग 20% अपशिष्ट सामान्य रूप से पुनर्प्राप्त किया जाता है, बाकी को अनौपचारिक रूप से उपचारित किया जाता है।
- PV अपशिष्टों के इस बढ़ते अनौपचारिक प्रबंधन ने भराव क्षेत्रों में अपशिष्टों को निक्षेपित कर दिया है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ रहा है। एनकैप्सुलेंट के दहन से वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड भी उत्सर्जित होता है।
भारत में PV अपशिष्ट के प्रबंधन में चुनौतियाँ
- PV अपशिष्ट का अनौपचारिक प्रबंधन:
- PV पैनलों के कुछ हिस्सों को निष्कर्षित और पुनर्चक्रित किये जाने के बावजूद, अपशिष्ट का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा अनौपचारिक रूप से संसाधित किया जाता है, जिससे भरावक्षेत्रों में अपशिष्टों का संचय होता है और आसपास के क्षेत्र प्रदूषित होते हैं।
- पुनर्चक्रित PV अपशिष्ट के पुन: उपयोग के लिये सीमित बाज़ार:
- वर्तमान में पुनर्चक्रित PV अपशिष्ट का पुन: उपयोग करने के लिये भारत में उपयुक्त प्रोत्साहनों और योजनाओं की कमी के कारण बाज़ार बहुत छोटा है जिससे निवेश में कठिनाई उत्पन्न होती हैं।
- अपशिष्ट संचय और उपचार में होने वाले वित्तीय नुकसान से बचने के लिये केंद्रीय बीमा या नियामक निकाय की कमी।
- वर्तमान में पुनर्चक्रित PV अपशिष्ट का पुन: उपयोग करने के लिये भारत में उपयुक्त प्रोत्साहनों और योजनाओं की कमी के कारण बाज़ार बहुत छोटा है जिससे निवेश में कठिनाई उत्पन्न होती हैं।
- PV अपशिष्ट उपचार के लिये विशिष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव:
- केवल PV अपशिष्टों को अन्य ई-अपशिष्टों के साथ जोड़ने से भ्रम उत्पन्न हो सकता है और ई-अपशिष्ट दिशा-निर्देशों के दायरे में विशिष्ट प्रावधानों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।
- भ्रम से बचने के लिये ई-अपशिष्ट दिशा-निर्देशों के भीतर PV अपशिष्ट उपचार के लिये विशिष्ट प्रावधानों की आवश्यकता है।
- केवल PV अपशिष्टों को अन्य ई-अपशिष्टों के साथ जोड़ने से भ्रम उत्पन्न हो सकता है और ई-अपशिष्ट दिशा-निर्देशों के दायरे में विशिष्ट प्रावधानों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।
- खतरनाक अपशिष्ट वर्गीकरण:
- PV मॉड्यूल और उनके घटकों से उत्पन्न अपशिष्टों को भारत में 'खतरनाक अपशिष्ट' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- PV अपशिष्टों के प्रबंधन के बारे में जागरूकता अभियान और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित करने से लोगों को खतरनाक अपशिष्टों को ठीक से प्रबंधित करने के महत्त्व को समझने में मदद मिल सकती है। यह अधिक लोगों को उचित अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान प्रथाओं में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करेगा।
- सीमित स्थानीय सौर PV-पैनल निर्माण:
- भारत को घरेलू अनुसंधान एवं विकास प्रयासों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि एकल मॉड्यूल प्रकार के आधार पर कुछ प्राकृतिक संसाधनों को समान रूप से समाप्त कर देगा और महत्त्वपूर्ण सामग्रियों के पुनर्चक्रण और उनकी पुनर्प्राप्ति हेतु स्थानीय क्षमता को अवरुद्ध कर देगा। PV अपशिष्ट पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियों के घरेलू विकास को उचित अवसंरचनात्मक सुविधाओं और पर्याप्त पूंजी माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
भारत द्वारा की गई पहलें:
- मसौदा EPR अधिसूचना: प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021
- ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016
- ई-कचरा (प्रबंधन) संशोधन नियम, 2018
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
अन्य देशों द्वारा की गई पहलें:
- यूरोपीय संघ:
- यूरोपीय संघ का अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (Waste Electrical and Electronic Equipment- WEEE) निर्देश पहली बार अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित उपकरण स्थापित करने वाले विनिर्माताओं अथवा वितरकों पर अपशिष्ट के निपटान का उत्तरदायित्त्व निर्धारित करता है।
- WEEE के निर्देश के अनुसार, उत्पादों के जीवन चक्र में मॉड्यूल को एकत्रित करना, संभालना और निपटान करना पूरी तरह से PV उत्पादकों की ज़िम्मेदारी है।
- यूरोपीय संघ का अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (Waste Electrical and Electronic Equipment- WEEE) निर्देश पहली बार अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित उपकरण स्थापित करने वाले विनिर्माताओं अथवा वितरकों पर अपशिष्ट के निपटान का उत्तरदायित्त्व निर्धारित करता है।
- ब्रिटेन:
- ब्रिटेन में उद्योग-प्रबंधित "टेक-बैक और रीसाइक्लिंग योजना" भी कार्यरत है, जिसमे सभी PV उत्पादकों को आवासीय सौर बाज़ार (बिज़नेस-टू-कंज्यूमर) और गैर-आवासीय बाज़ार के लिये उपयोग किये जाने वाले उत्पादों से संबंधित डेटा को पंजीकृत और एकत्रित करने की आवश्यकता होती है।
- अमेरिका:
- हालाँकि अमेरिका में पुनर्चक्रण के संबंध में कोई संघीय कानून अथवा नियम नहीं हैं, परंतु ऐसे कुछ राज्य हैं, जिन्होंने ‘एंड ऑफ लाइफ’ PV मॉड्यूल प्रबंधन के लिये नीति निर्माण की दिशा में कुछ कदम उठाए हैं।
- वाशिंगटन और कैलिफोर्निया ने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्त्व (Extended Producer Responsibility- EPR) नियम लागू किये हैं।वाशिंगटन में PV मॉड्यूल के निर्माताओं को अब उपभोक्ता लागत के बिना राज्य में बेचे गए PV मॉड्यूल के निपटान, पुन: उपयोग अथवा पुनर्चक्रण के लिये भुगतान करना होगा।
- ऑस्ट्रेलिया:
- ऑस्ट्रेलिया की संघीय सरकार ने चिंता को ध्यान में रखते हुए PV प्रणाली के लिये एक उद्योग-आधारित उत्पाद प्रबंधन योजना को विकसित करने और लागू करने हेतु राष्ट्रीय उत्पाद प्रबंधन निवेश कोष के हिस्से के रूप में 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान की घोषणा की है।
- जापान और दक्षिणी कोरिया:
- जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश पहले ही PV अपशिष्ट की समस्या को दूर करने के लिये समर्पित कानून लाने के लिये संकल्पित हैं।
भारत द्वारा कार्रवाई की आवश्यकता:
- अगले 20 वर्षों में भारत में बड़ी मात्रा में PV अपशिष्ट उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिससे वर्ष 2050 तक यह विश्व भर में शीर्ष पाँच प्रमुख फोटोवोल्टिक अपशिष्ट उत्पादकों में से एक बन जाएगा।
- इसलिये भारत को इस नई चुनौती के लिये तैयार करने हेतु स्पष्ट नीति निर्देशों, अच्छी तरह से स्थापित रीसाइक्लिंग रणनीतियों तथा अधिक सहयोग को स्थापित करने की आवश्यकता है। PV अपशिष्ट प्रबंधन में अंतराल को संबोधित करके भारत सतत् विकास को बढ़ावा देते हुए एक चक्रीय अर्थव्यवस्था एवं प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिये गए कथनों पर विचार कीजिये: (वर्ष 2018)
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: D व्याख्या:
प्रश्न. पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन की तुलना में सूर्य के प्रकाश से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लाभों का वर्णन कीजिये। इस उद्देश्य के लिये हमारी सरकार द्वारा क्या पहल की गई हैं? (मुख्य परीक्षा-2015) |
स्रोत: द हिंदू


अंतर्राष्ट्रीय संबंध
चीन, जापान द्वारा सैन्य हॉटलाइन की स्थापना
प्रिलिम्स के लिये:सेनकाकू द्वीप, दियाओयू द्वीप, पूर्वी चीन सागर मेन्स के लिये:क्षेत्रीय विवादों का भू-राजनीति पर प्रभाव |
चर्चा में क्यों?
हाल ही में चीन और जापान ने विवादित द्वीपों (सेनकाकू द्वीप) पर समुद्री, हवाई घटनाओं का प्रबंधन करने के लिये सैन्य हॉटलाइन (विशिष्ट उद्देश्य के लिये स्थापित एक प्रत्यक्ष फोनलाइन) स्थापित की है।
- जापान के नियंत्रण वाले पूर्वी चीन सागर के निर्जन द्वीपों पर चीन और जापान के बीच लंबे समय से विवाद है और इन पर चीन द्वारा दावा किया जाता है।
हॉटलाइन की स्थापना का कारण:
- यह कदम विवादित जल क्षेत्र में इन देशों की आक्रामक गश्त के कारण उत्पन्न होने वाली घटनाओं के प्रबंधन और नियंत्रण हेतु उठाया गया था।
- यह हॉटलाइन चीन और जापान के रक्षा विभागों के बीच संचार को समृद्ध करने के साथ समुद्री और हवाई संकटों के प्रबंधन और नियंत्रण के लिये दोनों पक्षों की क्षमताओं को मज़बूत करेगी और क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगी।
सेनकाकू द्वीप विवाद:
- परिचय:
- सेनकाकू द्वीप विवाद आठ निर्जन द्वीपों संबंधी एक क्षेत्रीय विवाद है, इस द्वीपसमूह को जापान में सेनकाकू द्वीपसमूह, चीन में दियाओयू द्वीपसमूह और हॉन्गकॉन्ग में तियायुतई द्वीपसमूह के नाम से जाना जाता है।
- जापान और चीन दोनों इन द्वीपों पर स्वामित्व का दावा करते हैं।
- अवस्थिति:
- ये आठ निर्जन द्वीप पूर्वी चीन सागर में स्थित हैं। इनका कुल क्षेत्रफल लगभग 7 वर्ग किलोमीटर है और ये ताइवान के उत्तर-पूर्व में स्थित हैं।
- सामरिक महत्त्व:
- ये द्वीप रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण शिपिंग लेन के करीब हैं जो समृद्ध मत्स्यन का अवसर प्रदान करते हैं और माना जाता है कि इसमें समृद्ध तेल भंडार हैं।
- जापान का दावा:
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जापान ने सैन फ्रांसिस्को की संधि, 1951 के तहत ताइवान सहित कई क्षेत्रों एवं द्वीपों पर अपना दावा छोड़ दिया था।
- लेकिन संधि के तहत नानसी शोटो द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रस्टीशिप के अधीन आ गए और फिर वर्ष 1971 में जापान को वापस कर दिये गए।
- जापान का कहना है कि सेनकाकू द्वीप नानसी शोटो द्वीप समूह का हिस्सा है और इसलिये उस पर भी जापान का अधिकार है।
- इसके अलावा चीन ने सैन फ्रांसिस्को संधि पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
- केवल 1970 के दशक के बाद से, जब क्षेत्र में तेल संसाधनों का मुद्दा उभरा, चीनी और ताइवान के अधिकारियों ने अपने दावों पर ज़ोर देना शुरू कर दिया।
- चीन का दावा:
- ये द्वीप प्राचीन काल से इसके क्षेत्र का हिस्सा रहे हैं जो ताइवान प्रांत द्वारा प्रशासित महत्त्वपूर्ण मत्स्यन मैदान के रूप में कार्य करते हैं।
- जब सैन फ्रांसिस्को की संधि में ताइवान को वापस कर दिया गया था तो चीन ने कहा था कि इसके हिस्से के रूप में द्वीपों को भी वापस कर दिया जाना चाहिये था।
- ताइवान का दावा:
- ताइवान इन द्वीपों पर दावा करता है, लेकिन किसी भी संघर्ष से बचने के लिये जापान के साथ समझौते किये हैं क्योंकि जापान एवं ताइवान के बीच घनिष्ठ रक्षा संबंध है।
- वर्तमान विवाद के बावजूद, जापान एवं ताइवान के मध्य घनिष्ठ रक्षा संबंध बबने हुए हैं।
अन्य हालिया द्वीप विवाद:
- कुरील द्वीप: उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है।
- रूस और जापान के बीच विवाद है।
- चागोस द्वीपसमूह: उत्तरी हिंद महासागर में स्थित है।
- ब्रिटेन और मॉरीशस के बीच विवाद है।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स :Q.निम्नलिखित कथनों में कौन-सा एक, कभी-कभी समाचारों में उल्लिखित सेनकाकू द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? (a) आमतौर पर यह माना जाता है कि वे दक्षिणी चीन सागर के आसपास किसी देश द्वारा निर्मित कृत्रिम द्वीप हैं। उत्तर: (b) व्याख्या:
|
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस


कृषि
ओपन-सोर्स सीड्स मूवमेंट
प्रिलिम्स के लिये:IPR, ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर, WTO, TRIPS, हरित क्रांति। मेन्स के लिये:ओपन-सोर्स सीड्स मूवमेंट। |
चर्चा में क्यों?
प्रजनन और बीज क्षेत्र में क्रमशः सार्वजनिक क्षेत्र के घटते एवं निजी क्षेत्र के बढ़ते वर्चस्व के साथ, ओपन-सोर्स सीड्स की अवधारणा तेज़ी से प्रासंगिक हो रही है।
- वर्ष 1999 में पहली बार कनाडाई पौधा-प्रजनक टी.ई. माइकल्स द्वारा ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर के सिद्धांतों के आधार पर 'ओपन-सोर्स सीड्स' का सुझाव दिया गया था।
- किसान सदियों से बिना किसी विशेष अधिकार या बौद्धिक संपदा अधिकार का दावा किये, बीजों (Seeds) को साझा करते हुए नवाचार करते रहे हैं, उसी तरह जैसे प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर पर साझा एवं नवाचार करते हैं।
ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (OSS):
- OSS एक सॉफ्टवेयर है जिसका स्रोत कोड किसी को भी खुले स्रोत लाइसेंस के तहत देखने, संशोधित करने और वितरित करने हेतु सभी के लिये उपलब्ध होता है। यह लाइसेंस आमतौर पर उपयोगकर्त्ताओं को स्रोत कोड तक पहुँचने और संशोधित करने की अनुमति देता है, साथ ही उपयोग या वितरण पर किसी भी प्रतिबंध के बिना सॉफ़्टवेयर को पुनर्वितरित करने की अनुमति होती है।
- OSS की अवधारणा वर्ष 1980 के दशक में उत्पन्न हुई, लेकिन फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन (FSF) तथा ओपन सोर्स इनिशिएटिव (OSI) के प्रयासों से वर्ष 1990 के दशक में इसे व्यापक मान्यता और लोकप्रियता मिली।
- OSS के लाभों में विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सॉफ्टवेयर को अनुकूलित करने की क्षमता, स्वामित्त्व की कम लागत और स्रोत कोड की बढ़ी हुई पारदर्शिता के कारण अधिक सुरक्षा की संभावना शामिल है। इसके अलावा OSS डेवलपर्स को मौजूदा सॉफ्टवेयर पर निर्माण करने एवं इसे बेहतर बनाने की अनुमति देकर नवाचार को बढ़ावा दे सकता है।
पादप प्रजनकों के अधिकार:
- वाणिज्यिक बीज उद्योग का विकास, वैज्ञानिक पादप-प्रजनन और संकर बीजों के आगमन से कई देशों में पादप प्रजनकों के अधिकार (PBR) की स्थापना हुई।
- PBR पद्धति के तहत, पौध प्रजनकों और नई किस्मों के विकासकर्त्ताओं को बीजों पर रॉयल्टी वसूलने तथा कानूनी रूप से PBR लागू करने का विशेष अधिकार है।
- इसने किसानों द्वारा बीजों के पुन: प्रयोग के अधिकारों को सीमित कर दिया और उनकी नवाचार करने की क्षमता को सीमित कर दिया।
- वर्ष 1994 में विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना तथा व्यापार संबंधित IPR समझौते (TRIPS) ने पादप किस्मों पर वैश्विक IPR व्यवस्था लागू की।
- ट्रिप्स के लिये देशों को पौधों की किस्मों हेतु IP संरक्षण का कम-से-कम एक प्रतिरूप प्रदान करने की आवश्यकता थी, जिसने नवाचार करने की स्वतंत्रता के बारे में चिंताओं को उज़ागर किया।
- हरित क्रांति का नेतृत्त्व सार्वजनिक क्षेत्र के प्रजनन संगठनों ने किया था और बीजों को 'ओपन पोलीनेटेड किस्मों' या उचित मूल्य वाले संकरों के रूप में उपलब्ध कराया गया था, जिसमें किसानों की उत्पादन, पुन: उपयोग एवं साझा करने की क्षमता पर कोई सीमा नहीं थी।
- लेकिन कृषि में आनुवंशिक क्रांति का नेतृत्त्व निजी क्षेत्र ने किया, जिसमें बीजों को ज़्यादातर संकर के रूप में उपलब्ध कराया गया और IPR द्वारा संरक्षित किया गया।
कृषि में IP संरक्षण
- कृषि में IPR संरक्षण के दो रूप हैं: पादप-प्रजनकों के अधिकार और पेटेंट।
- साथ में वे IP-संरक्षित किस्मों से जर्मप्लाज़्म (Germplasm) का उपयोग करके किसानों के अधिकारों और नई किस्मों को विकसित करने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हैं।
- इस प्रकार उन्होंने बीज क्षेत्र को और समेकित किया है और IPR द्वारा कवर की गई पौधों की किस्मों की संख्या में वृद्धि की है।
ओपन सोर्स सीड्स
- आवश्यकता:
- आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों की उच्च कीमतों और IP दावों ने भारत में बीटी कपास के बीजों पर राज्य के हस्तक्षेप सहित कई समस्याओं को जन्म दिया। जैसे-जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रजनन में गिरावट आई और बीज क्षेत्र में निजी क्षेत्र का वर्चस्व बढ़ने लगा, विकल्पों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी।
- यह तब है जब ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर की सफलता ने एक समाधान को प्रेरित किया।
- ओपन-सोर्स मॉडल:
- वर्ष 2002 में वैज्ञानिकों द्वारा बीजों और पौधों की किस्मों के लिये एक ओपन-सोर्स मॉडल प्रस्तावित किया गया था, जिसे "बायोलाइनक्स मॉडल" का नाम दिया गया था, और यह विद्वानों और नागरिक-समाज के सदस्यों के लिये इस दिशा में कार्य करने का आधार बना।
- जैक क्लोपेनबर्ग ने वर्ष 2012 में विस्कॉन्सिन में ओपन सोर्स सीड्स इनिशिएटिव (OSSI) लॉन्च किया।
- इसका उपयोग किसान आधारित बीज संरक्षण और वितरण प्रणाली में किया जा सकता है। भारत में पारंपरिक किस्मों को संरक्षण और साझा करने के लिये कई पहलें हैं।
- इसका उपयोग किसानो के नेतृत्त्व वाली प्लांट ब्रीडिंग अभ्यासों को बढ़ावा देने के लिये भी किया जा सकता है।
- पारंपरिक किस्मों में अक्सर एकरूपता और गुणवत्ता की कमी होती है। ओपन सोर्स सिद्धांत परीक्षण, सुधार और अपनाए जाने की सुविधा के साथ इन दोनो चुनौतियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं - ये सभी अंततः भारत की खाद्य सुरक्षा और जलवायु सुनम्यता के लिये फायदेमंद होंगे।
भारत की पहलें:
- हैदराबाद स्थित सतत् कृषि केंद्र (CSA) जो अपना बीज नेटवर्क का एक हिस्सा है, ने एक मॉडल का निर्माण किया जिसे CSA और बीज सामग्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बीच एक अनुबंध में शामिल किया गया था। थ्री फार्मर प्रोडूसर आर्गेनाईजेशन (FPO) के माध्यम से इस रणनीति का उपयोग करने की कोशिश की जा रही है।
- विश्व भर में ओपन-सोर्स मॉडल का उपयोग करने वाली बीज फर्मों की संख्या और इसके तहत उपलब्ध कराई गई फसल किस्मों और बीजों की संख्या कम है, लेकिन इसमें वृद्धि होने की पूरी संभावना है। भारत द्वारा अभी इसका परीक्षण करना और इसे व्यापक रूप से अपनाया जाना शेष है।
- पौधा किस्म एवं किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत यदि किसान कुछ शर्तों को पूरा करते हैं तो यह कुछ किस्मों को 'किसान किस्मों (Farmer Varieties)' के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं।
- हालाँकि यह अधिनियम के तहत व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु संरक्षित किस्मों के प्रजनन और व्यापार के पात्र नहीं होते हैं।
आगे की राह:
- ओपन-सोर्स दृष्टिकोण का उपयोग करने से किसानों को जर्मप्लाज़्म और बीजों पर अधिक अधिकार प्राप्त होने के साथ नवाचार को सुगम बनाने में मदद मिलेगी।
- इसलिये इस दृष्टिकोण का परीक्षण करने की आवश्यकता है और तीनों FPO इसका नेतृत्व कर सकते हैं।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 3 उत्तर: (c)
अतः विकल्प (C) सही उत्तर है। |
स्रोत: द हिंदू
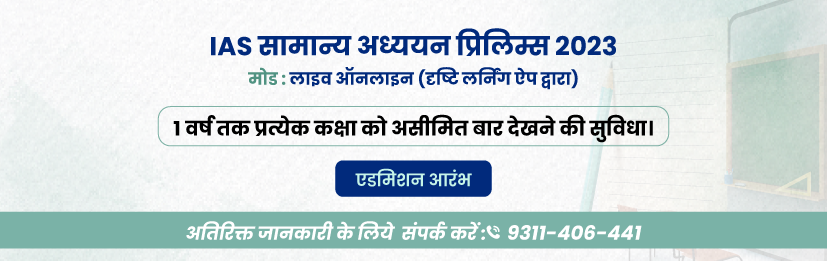

जैव विविधता और पर्यावरण
मेगाफौना बायस हैम्पर्स कार्निवोर संरक्षण प्रयास
प्रिलिम्स के लिये:मांसाहारी, प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर रिज़र्व, केन-बेतवा रिवर इंटर-लिंकिंग प्रोजेक्ट, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972), भारतीय तेंदुआ, भारतीय जैविक विविधता अधिनियम (2002)। मेन्स के लिये:भारत में वन्यजीव संरक्षण में चुनौतियाँ, भारत में माँसाहारियों का संरक्षण और प्रबंधन, भारत में जैव विविधता संरक्षण, संरक्षण प्रयासों में पारिस्थितिक डेटा की भूमिका, मानव- पशु संघर्ष। |
चर्चा में क्यों?
भारत का मांसाहारी अनुसंधान बड़ी और अधिक लोकप्रिय प्रजातियों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे छोटे और कम प्रसिद्ध माँसाहारियों की जानकारी में कमी आ रही है। जानकारी का यह अंतर देश में संरक्षण के प्रयासों में बाधा बन रहा है।
संरक्षण के लिये मांसाहारी जीव क्यों महत्वपूर्ण हैं?
- पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए मांसाहारी खाद्य शृंखला पर हावी हैं। उनके महत्त्व के बावजूद, मांसाहारी विश्व में सबसे अधिक संकट वाले स्तनधारियों में से हैं।
- इसलिये विश्व स्तर पर मांसाहारी आबादी के अध्ययन, सुरक्षा और प्रबंधन में पर्याप्त अनुसंधान और संरक्षण संसाधनों का निवेश किया जाता है।
भारत में मांसाहारी जीवों की संरक्षण स्थिति
- भारत दुनिया की 23% मांसाहारी आबादी का आवास है, जो 60 प्रजातियों से संबंधित हैं।
- हालाँकि वर्ष 1947 से प्रकाशित अध्ययनों की समीक्षा से पता चलता है कि देश में उनकी संरक्षण स्थिति और नीतियों पर करिश्माई/चमत्कारी प्रजातियों पर 70 वर्षों के शोध का प्रभाव संतोषजनक नहीं रहा है।
- जंगली बिल्ली वर्ग, विशेष रूप से बाघ, देश में मांसाहारी समूह पर हावी है। अन्य शीर्ष मांसाहारी, जिन पर पर्याप्त शोध ध्यान केंद्रित किया गया है उनमें भारतीय तेंदुआ, सुनहरा सियार, ढोल और जंगली बिल्ली शामिल हैं।
- हालाँकि छोटे और कम करिश्माई/चमत्कारी मांसाहारियों पर अध्ययन की गुणवत्ता आमतौर पर खराब रही है।
भारत में मांसाहारी जीवों पर अनुसंधान का प्रभाव:
- बाघों पर वैज्ञानिक अनुसंधान के कारण वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। जिससे देश भर में 50 स्थानों पर बाघ अभयारण्यों की स्थापना में मदद मिली।
- अनुसंधान होने से बाघों के आवास क्षेत्र में राजमार्गों के निर्माण या विस्तार के संबंध में साक्ष्य प्रदान हुए हैं, जैसे कि बांदीपुर टाइगर रिज़र्व, कान्हा-पेंच बाघ गलियारा और भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य में हुए विकास।
- अनुसंधान डेटा के आधार पर महत्वाकांक्षी केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का विरोध किया गया है जिससे मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिज़र्व के मुख्य क्षेत्र के एक बड़े हिस्से के जलमग्न होने की संभावना है।
- भारतीय तेंदुए पर अनुसंधान के परिणामस्वरूप मानव-तेंदुआ संघर्ष को रोकने हेतु राष्ट्रीय दिशा-निर्देश तैयार किये गए हैं।
- देश में बाघ को मांसाहारी जीव के रूप में प्रमुख माना जाता है। भारतीय तेंदुआ, ढोल और जंगली बिल्ली अन्य प्रमुख ऐसे मांसाहारी जीव हैं, जिन पर पर्याप्त शोध किया गया है।
- लेकिन छोटे स्तर के माँसाहारियों पर सीमित अध्ययन हुआ है।
छोटे स्तर के मांसाहारी जीवों पर शोध क्यों महत्त्वपूर्ण है?
- इससे माँसाहारियों और उनके पारिस्थितिकी के अन्य समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच महत्त्वपूर्ण संबंध को समझने में मदद मिलेगी।
- जंगली बिल्ली को मांसाहारी कृंतक आबादी को नियंत्रित करने, बीजों को प्रसारित करने और वन पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी कार्यों हेतु जाना जाता है।
- सिवेट को भी बीजों को प्रसारित करने और वन पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिये जाना जाता है।
नोट:
- करिस्मैटिक मेगाफौना (Charismatic Megafauna) शब्द का उपयोग जीवों की प्रमुख प्रजातियों का वर्णन करने के लिये किया जाता है, जैसे कि हाथी, बाघ, शेर और पांडा। इन जानवरों का प्रायः इनके सांस्कृतिक और सौंदर्य संबंधी महत्त्व के कारण इनके संरक्षण पर अधिक महत्त्व दिया जाता है।
भारत में मांसाहारी अनुसंधान एवं संरक्षण में चुनौतियाँ:
- आर्द्रभूमि संरक्षण को कम प्राथमिकता दी जाती है एवं चरागाह पारिस्थितिक तंत्र, जो स्याहगोश/कैरॅकेल जैसी गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों को शरण देते हैं, को भी अनुसंधान एवं संरक्षण में दरकिनार कर दिया जाता है।
- प्राकृतिक इतिहास के अध्ययन में गिरावट तथा इस तरह के अध्ययनों को प्रकाशित करने वाली पत्रिकाओं में समानांतर कमी से प्रजातियों की पारिस्थितिकी को समझने हेतु बुनियादी कदम है।
- नीतियाँ अक्सर राजनीतिक प्रभावों और गलत प्राथमिकताओं से संचालित होती हैं तथा वैज्ञानिक सिफारिशों की अवहेलना की जाती है।
- मांसाहारी सीमित अंतःविषय अध्ययन एवं सामाजिक-पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील नीतियों के विकास में बाधा डालते हैं।
- गैर-सरकारी एजेंसियों और स्वतंत्र शोधकर्त्ताओं को लाभ पहुँचाने हेतु नौकरशाही की बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है।
भारत में मांसाहारी संरक्षण में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा सकते हैं?
- छोटे और कम प्रभावकारी माँसाहारियों पर शोध के लिये धन में वृद्धि, ताकि उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके और भारत की संरक्षण नीतियों में उनके कमज़ोर और खतरे वाले आवासों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।
- सामाजिक-पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील समुदायों को शामिल करके नीतियों को प्रोत्साहित करने हेतु एक सहयोगी और रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ अंतःविषय अनुसंधान।
- भारतीय जैवविविधता अधिनियम (2002) के तहत जैव विविधता विरासत स्थलों या भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972) के तहत सामुदायिक कोष जैसे ढाँचे व स्थानीय नेतृत्त्व को बढ़ावा तथा अंततः मांसाहारी अनुसंधान का लोकतंत्रीकरण करके सामाजिक-पारिस्थितिक प्रणालियों के रखरखाव की सुविधा प्रदान करना।
स्रोत: डाउन टू अर्थ