राजस्थान Switch to English
नए शैक्षणिक सत्र में गरीब बच्चों के प्रवेश को प्राथमिकता
चर्चा में क्यों?
राजस्थान सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र के लिये शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों में वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश को प्राथमिकता पर लिया है।
मुख्य बिंदु:
- सूत्रों के अनुसार, राज्य के 31,857 निजी स्कूलों में प्रवेश के लिये 3.08 लाख से अधिक बच्चों ने आवेदन किया था।
- निजी स्कूलों में 25% सीटें समाज के कमज़ोर वर्ग के छात्रों से भरी जाएंगी।
- प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाओं और कक्षा 1 में RTE प्रवेश हेतु दो श्रेणियों के लिये आयु सीमा तय करते हुए एक प्रावधान किया है।
- तीन से चार वर्ष की आयु के बच्चों को प्री-प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश दिया जाता है और छह से सात वर्ष के बीच के बच्चे कक्षा 1 में प्रवेश पाने के पात्र होते हैं।
- राज्य में बड़ी संख्या में निजी स्कूलों ने प्री-प्राइमरी कक्षाओं में छात्रों के प्रवेश को लेकर चिंता व्यक्त की है क्योंकि इस श्रेणी को वर्ष 2023-24 में सरकार द्वारा किसी छात्र को कक्षा 1 में पदोन्नत होने तक तीन वर्ष की फीस के भुगतान के लिये किसी स्पष्ट दिशा-निर्देश के बिना जोड़ा गया था।
शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 के तहत वर्ष 2009 में बच्चों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया तथा इसे अनुच्छेद 21-A के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया गया।
- RTE अधिनियम का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है।
- धारा 12 (1) (C) में कहा गया है कि गैर-अल्पसंख्यक निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल आर्थिक रूप से कमज़ोर और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिये प्रवेश स्तर ग्रेड में कम- से-कम 25% सीटें आरक्षित करें।
- यह गैर-प्रवेशित बच्चे को आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश देने का भी प्रावधान करता है।
- यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय एवं अन्य ज़िम्मेदारियों को साझा करने के बारे में भी जानकारी देता है।
- भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र व राज्य दोनों इस विषय पर कानून बना सकते हैं।
- यह छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR), भवन और बुनियादी ढाँचा, स्कूल-कार्य दिवस, शिक्षकों के लिये कार्यावधि से संबंधित मानदंडों तथा मानकों का प्रावधान करता है।
- इस अधिनियम में गैर-शैक्षणिक कार्यों जैसे- स्थानीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभाओं और संसद के चुनावों तथा आपदा राहत के अलावा अन्य कार्यों में शिक्षकों की तैनाती का प्रावधान करता है।
- यह अपेक्षित प्रविष्टि और शैक्षणिक योग्यता के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
- यह निम्नलिखित का निषेध करता है:
- शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न।
- बच्चों के प्रवेश के लिये स्क्रीनिंग प्रक्रिया।
- प्रति व्यक्ति शुल्क।
- शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन।
- बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय।
- यह बच्चे को उसके अनुकूल और बाल केंद्रित शिक्षा अधिगम के माध्यम से भय, आघात एवं दुश्चिंता से मुक्त बनाने पर केंद्रित है।


राजस्थान Switch to English
सेमल वृक्ष
चर्चा में क्यों?
दक्षिण राजस्थान में सेमल वृक्षों की संख्या में कमी आ रही है जिससे क्षेत्र के वनों और लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
मुख्य बिंदु:
- दक्षिणी राजस्थान में भील और गरासिया आदि स्थानों पर सेमल बड़ी मात्रा में काटा जाता है तथा उदयपुर में बेचा जाता है।
- यह कटाई राजस्थान वन अधिनियम, 1953 से लेकर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 तक कई कानूनों का उल्लंघन करती है।
- सेमल एक अभिन्न प्रजाति है जो वन पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ रखती है। शैल-मधुमक्खियाँ इसकी शाखाओं पर घोंसला बनाती हैं क्योंकि वृक्ष के प्ररोह में उगे नोंक (Spike) इसके शिकारी स्लॉथ बियर से बचाव करती हैं।
- जनजातीय समुदायों के सदस्य मानसून के दौरान भोजन के लिये वृक्ष की लाल जड़ का सेवन करते हैं। बुक्कुलैट्रिक्स क्रेटरेक्मा (Bucculatrix crateracma) कीट के लार्वा इसकी पत्तियों को खाते हैं।
- गोल्डन-क्राउन्ड गौरैया अपने घोंसलों की परत इनके बीजों की सफेद रुई से बुनती है।
- डिस्डेर्कस बग, इंडियन क्रेस्टेड साही, हनुमान लंगूर और कुछ अन्य प्रजातियाँ इसके फूलों के रस का आनंद लेती हैं।
- क्षेत्र की गरासिया जनजाति भी मानती है कि वे सेमल वृक्ष के वंशज हैं। कथोडी जनजाति इसकी लकड़ी का उपयोग संगीत वाद्ययंत्र बनाने के लिये करती है जबकि भील इसका उपयोग बर्तन बनाने के लिये करते हैं।
सेमल वृक्ष (Semal Tree)
- रेशम कपास के वृक्ष और बॉम्बेक्स सेइबा के नाम से भी जाना जाने वाला सेमल वृक्ष भारत का स्थानीय तथा तेज़ी से बढ़ने वाला वृक्ष है।
- यह अपने विशिष्ट, नुकीले लाल फूलों और इसके रोयेंदार बीज की फली के लिये जाना जाता है जिसमें कपास जैसा पदार्थ होता है जिसका उपयोग कभी तकिये तथा गद्दे भरने के लिये किया जाता था।
- यह वृक्ष अपने सजावटी मूल्य के लिये बहुमूल्य है और प्रायः उद्यान एवं बगीचों में उगाया जाता है।
इंडियन क्रेस्टेड साही (Indian Crested Porcupine)
- वैज्ञानिक नाम: हिस्ट्रिक्स इंडिका (Hystrix indica)
- भौगोलिक सीमा: यह पूरे दक्षिण-पूर्व और मध्य एशिया एवं मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, जिसमें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इज़रायल, ईरान तथा सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं।
- व्यवहार:
- रात्रिचर जीव जो प्रत्येक रात लगभग 7 घंटे भोजन की तलाश में बिताते हैं।
- प्राकृतिक गुफाओं या खोदे गए बिलों में रहते हैं।
- शिकारियों में बड़ी बिल्लियाँ, भेड़िये, लकड़बग्घा और मनुष्य शामिल हैं।
- संरक्षण की स्थिति:
- IUCN स्थिति: कम चिंतनीय (LC)
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972: अनुसूची IV

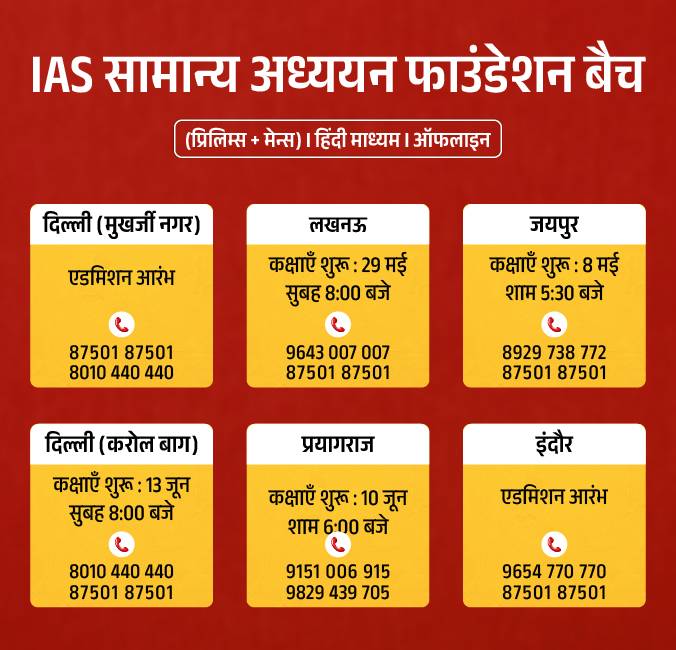
उत्तराखंड Switch to English
शंभू नदी
चर्चा में क्यों?
उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले के कुँवारी गाँव में शंभू नदी पर एक बार फिर लगभग 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक मानव निर्मित झील का निर्माण किया गया है, जिससे स्थानीय लोग आसन्न त्रासदी को लेकर चिंतित हैं।
मुख्य बिंदु:
- झील का यह पुनरुद्धार वर्ष 2022 और 2023 की पिछली घटनाओं की याद दिलाता है जब भू-स्खलन के कारण नदी के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाली तुलनीय संरचनाओं के कारण बहाव में संभावित बाढ़ को रोकने के लिये त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई की गई थी।
- शंभू नदी बागेश्वर से निकलती है और चमोली ज़िले में पिंडर नदी में मिल जाती है।
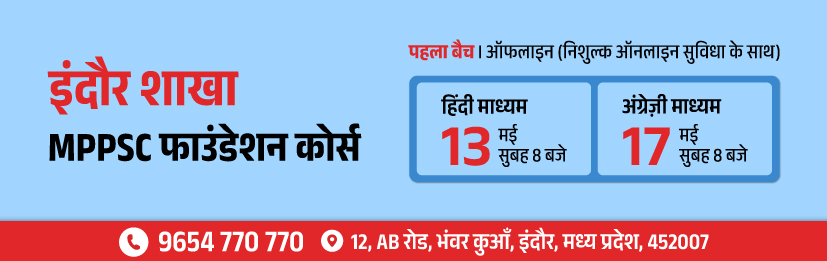

उत्तराखंड Switch to English
अपर्याप्त सिद्ध हुईं पाइन नीडल ऊर्जा परियोजनाएँ
चर्चा में क्यों?
विद्युत उत्पन्न करने के लिये बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पाइन नीडल का प्रयोग करने हेतु उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UREDA) द्वारा स्थापित जैव-ऊर्जा परियोजनाएँ "असफल" रही हैं, अधिकारियों का कहना है कि इनका प्रयोग करने के लिये उपयुक्त तकनीक अभी तक मौजूद नहीं है।
मुख्य बिंदु:
- राज्य के अधिकारियों ने जलवायु परिवर्तन से प्रेरित अनावृष्टि और पाइन नीडल (चीड़ की तीक्ष्ण, नुकीली पत्तियाँ) व कृषि अपशिष्ट जैसे कार्बनिक पदार्थों के बढ़ते भंडार जैसे कारकों के संयोजन के कारण होने वाली वार्षिक वनाग्नि के जोखिम को कम करने का प्रायः प्रयास किया है।
- अप्रैल और मई 2024 में कम वर्षा के कारण सूखे चीड़ के जमा हो जाने से क्षेत्र के वनों में लगी आग से संबंधित याचिकाओं के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार की आलोचना की थी।
- वर्ष 2021 में, राज्य सरकार ने विद्युत उत्पादन के लिये ईंधन के रूप में पाइन नीडल का प्रयोग करके ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित करने की एक योजना की घोषणा की।
- प्रारंभिक प्रस्ताव में तीन चरणों (कुल मिलाकर लगभग 150 मेगावाट) में 10 किलोवाट से 250 किलोवाट तक की कई इकाइयों को स्थापित करना शामिल था।
- 58 इकाइयों की स्थापना की आशंका के बावजूद, अब तक केवल छह 250 किलोवाट इकाइयाँ (कुल क्षमता 750 किलोवाट) स्थापित की गई हैं।
- वर्ष 2023 में, उत्तराखंड सरकार ने कहा कि पाइन नीडल परियोजनाओं से उत्पन्न विद्युत की कमी के कारण वह अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्रय को पूरा करने में असमर्थ थी।
- उत्तराखंड में पाइन नीडल की प्रचुरता एक मूल्यवान संसाधन प्रदान करती है।
- आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि राज्य के वन क्षेत्र का लगभग 16.36%, जो लगभग 3,99,329 हेक्टेयर है, में अधिकांश हिस्सा चिड़ पाइन (Pinus Roxburghii) वनों का है।
- अनुमानतः प्रत्येक वर्ष 15 लाख टन से अधिक पाइन नीडल का उत्पादन होता है।
- यदि इस अनुमानित राशि का 40% भी, अन्य कृषि अपशिष्टों के साथ, उपयोग किया जा सकता है, तो यह राज्य को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत मदद करेगा, साथ ही रोज़गार के अवसर का सृजन करेगा और आजीविका का समर्थन करेगा।
चिर पाइन (Pinus Roxburghii)
- पाइनस रॉक्सबर्गी (Pinus Roxburghi), जिसे आमतौर पर चिर पाइन के नाम से जाना जाता है, हिमालय क्षेत्र के स्थानीय देवदार-वृक्ष की एक प्रजाति है। यह एक महत्त्वपूर्ण काष्ठ प्रजाति है और इसका व्यापक रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये उपयोग किया जाता है।
- यह भारतीय उपमहाद्वीप, विशेष रूप से भारत, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में का मूल वृक्ष है।
- यह एक सदाबहार शंकुवृक्ष/ शंकुधारी वृक्ष है जो 30-50 मीटर की ऊँचाई तक वृद्धि कर सकता है।
- पाइनस रॉक्सबर्गी की छाल मोटी और परतदार होती है, जिसका रंग लाल-भूरा होता है।
- पत्तियाँ सुई जैसी नुकीली होती हैं, जो तीन के बंडलों में व्यवस्थित होती हैं और 20-30 सेमी. तक लंबी हो सकती हैं।
- इस वृक्ष पर कोन/शंकु लगते हैं जिनमें द्विकोषीय लघु बीजाणुधानियाँ (Microsporangia) अथवा बीजांडी शल्क होते हैं।
- संरक्षण की स्थिति:
- IUCN स्थिति: कम चिंतनीय (LC)
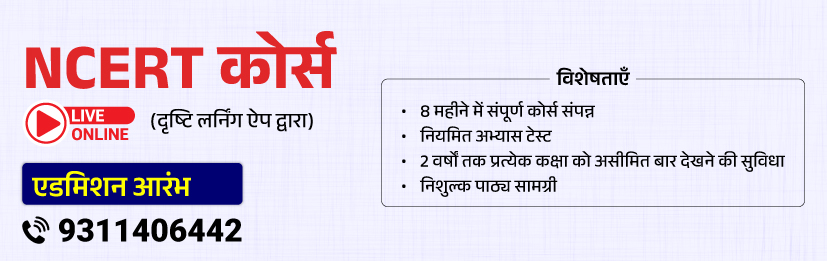
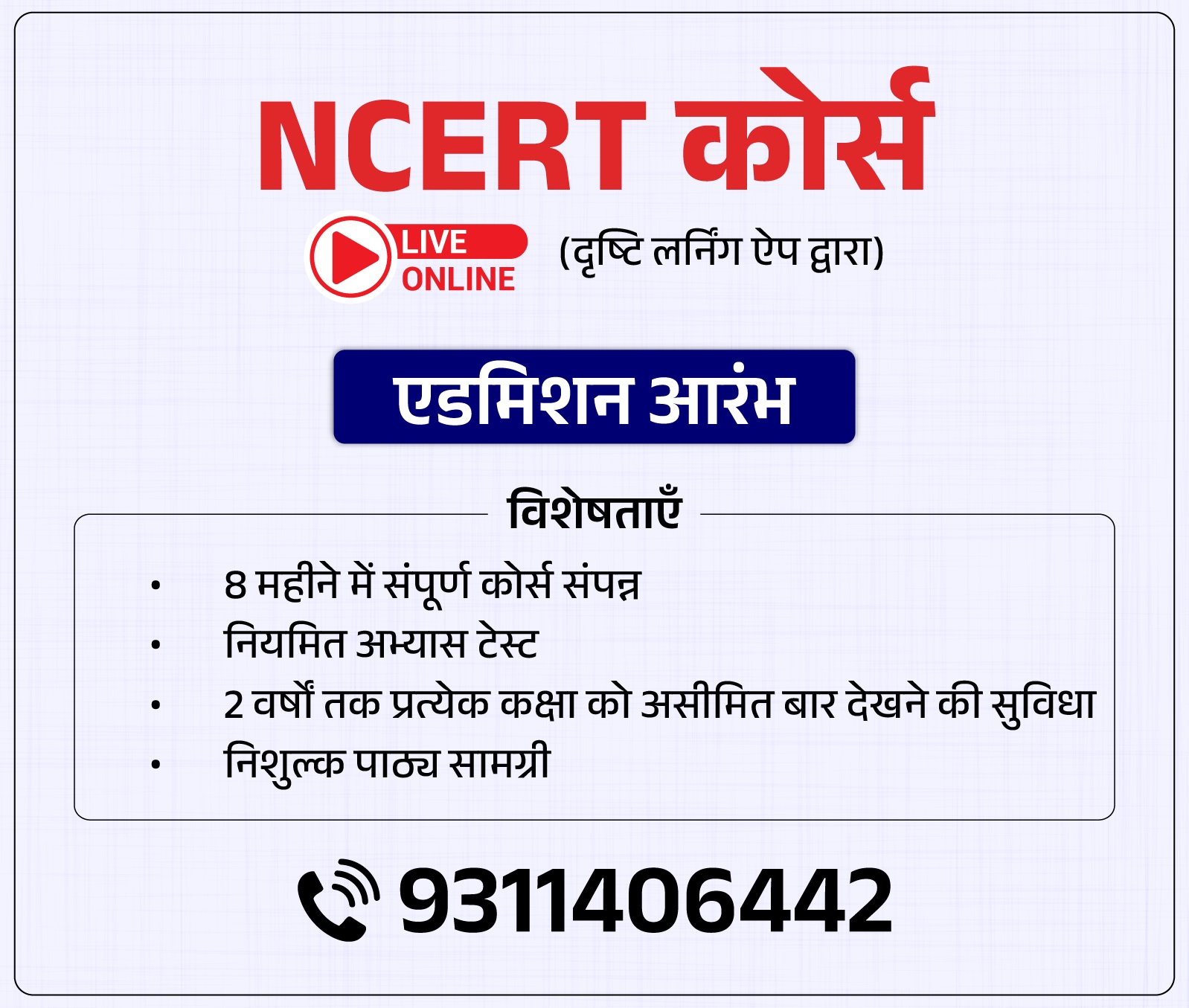
उत्तर प्रदेश Switch to English
वायु प्रदूषण से मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र पर संकट: IIT कानपुर
चर्चा में क्यों?
बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर के प्रमुख वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से लिखे गए अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण सुंदरबन के लिये एक बहुत बड़ा संकट है।
मुख्य बिंदु:
- अध्ययन का शीर्षक है “Acidity and oxidative potential of atmospheric aerosols over a remote mangrove ecosystem during the advection of anthropogenic plumes” अर्थात् "मानवजनित पिच्छक (Plumes) के संवहनीय तरंगो के कारण दूरस्थ मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र पर वायुमंडलीय एरोसोल की अम्लता और ऑक्सीकारक संभावना"।
- अध्ययन में पाया गया कि मुख्य रूप से ब्लैक कार्बन या सोत/कालिख कणों से समृद्ध भारी मात्रा में प्रदूषक, न केवल कोलकाता महानगर बल्कि पूरे भारत में गंगा के मैदानी क्षेत्र से भी आ रहे हैं, जो सुंदरबन की वायु गुणवत्ता को काफी खराब कर रहे हैं, जिससे इसके पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ रहा है।
- अध्ययन के लेखकों ने सुंदरबन की वायु गुणवत्ता और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र में गिरावट को रोकने के लिये 10-सूत्रीय सिफारिशें सुझाई हैं।
- सिफारिशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, पवन ऊर्जा का उपयोग, विद्युत परिवहन, सब्सिडी वाली LPG, विनियमित पर्यटन, डीज़ल जनरेटर पर प्रतिबंध, विषाक्त शिपमेंट पर प्रतिबंध, प्रदूषक कारखानों को बंद करना, ईंट भट्टों और भूमि उपयोग का विनियमन तथा तटीय नियमों को मज़बूत करना शामिल है।
सुंदरबन (Sundarban)
- सुंदरबन विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों का अग्रणी है, जो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है
- मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भूमि तथा समुद्र के बीच एक विशिष्ट पर्यावरण होता है।
मैंग्रोव (Mangroves)
- मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देशों के तटों के साथ अंतर-ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादप समूह हैं।
- मैंग्रोव वन कई पारिस्थितिक कार्य में महत्त्वपूर्ण हैं जैसे: काष्ठ वृक्षों के उत्पादन में, फिन-फिश और शेलफिश के लिये पोषण तथा अंडे देने के क्षेत्र के रूप में, पक्षियों एवं अन्य बहुमूल्य जीवों को आवास प्रदान करने में; समुद्र तट की सुरक्षा व तलछट के संचयन में।
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में, पश्चिम बंगाल में कुल मैंग्रोव कवर क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है, इसके बाद गुजरात तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं।
- भारत राज्य वन रिपोर्ट देश में मैंग्रोव और उनकी स्थितियों के बारे में डेटा देती है।

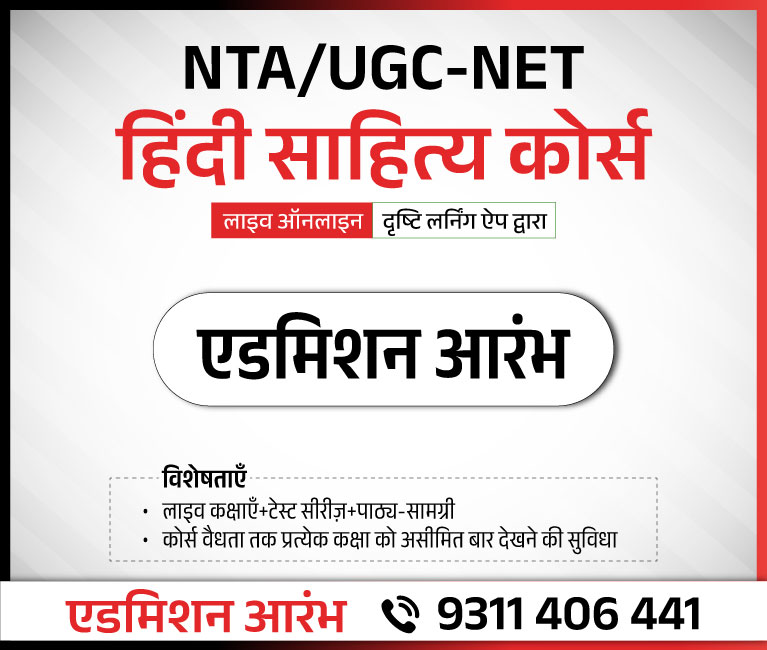
झारखंड Switch to English
सिंहभूम में सबसे अधिक मतदान दर्ज
चर्चा में क्यों?
झारखंड में पहले चरण के मतदान में सिंहभूम में सबसे अधिक 63.14% मतदान हुआ।
मुख्य बिंदु:
- सिंहभूम के बाद 62.82% के साथ खूँटी, 62.60% के साथ लोहरदगा और 59.99% के साथ पलामू का स्थान रहा।
- रेंगदाहातु, मुरमुरा, तेनसारा और सियांबा में गहन माओवादी विरोधी अभियान तथा CRPF शिविरों की स्थापना के साथ-साथ मतदान केंद्र स्थापित किये गए थे।
- माओवाद विरोधी अभियानों की प्रभावशीलता स्पष्ट है क्योंकि कई गाँवों में दो दशकों में पहली बार स्थानीय मतदान केंद्र बने हैं, जिससे उच्च मतदान हुआ।
- स्थिति में सुधार के बावजूद पश्चिमी सिंहभूम देश के सबसे अधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ज़िलों में से एक बना हुआ है। यहाँ वर्ष 2023 में 46 माओवादी-संबंधी घटनाएँ भी दर्ज की गईं, जिनमें 22 मौतें हुईं।
- माओवाद माओ त्से तुंग द्वारा विकसित साम्यवाद का एक रूप है। यह सशस्त्र विद्रोह, जन लामबंदी और रणनीतिक गठबंधनों के संयोजन के माध्यम से राज्य की सत्ता पर कब्ज़ा करने का एक सिद्धांत है।
वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism- LWE)
- वामपंथी उग्रवाद, जिसे वामपंथी आतंकवाद या कट्टरपंथी वामपंथी आंदोलनों के रूप में भी जाना जाता है, उन राजनीतिक विचारधाराओं और समूहों को संदर्भित करता है जो क्रांतिकारी तरीकों के माध्यम से महत्त्वपूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन का समर्थन करते हैं।
- LWE समूह अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिये सरकारी संस्थानों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों या निजी संपत्ति को निशाना बनाने जैसे कदम उठाते हैं।
- भारत में वामपंथी उग्रवादी आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1967 के पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी (Naxalbari) के उदय के साथ हुई।
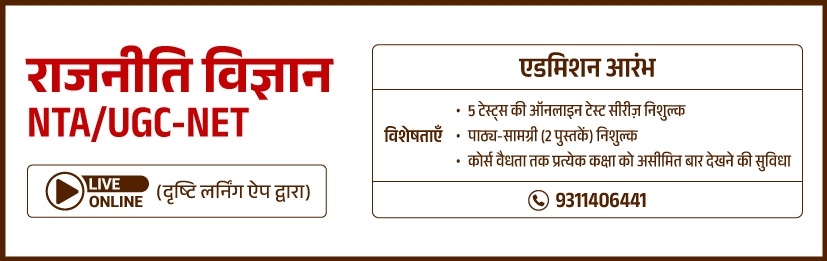
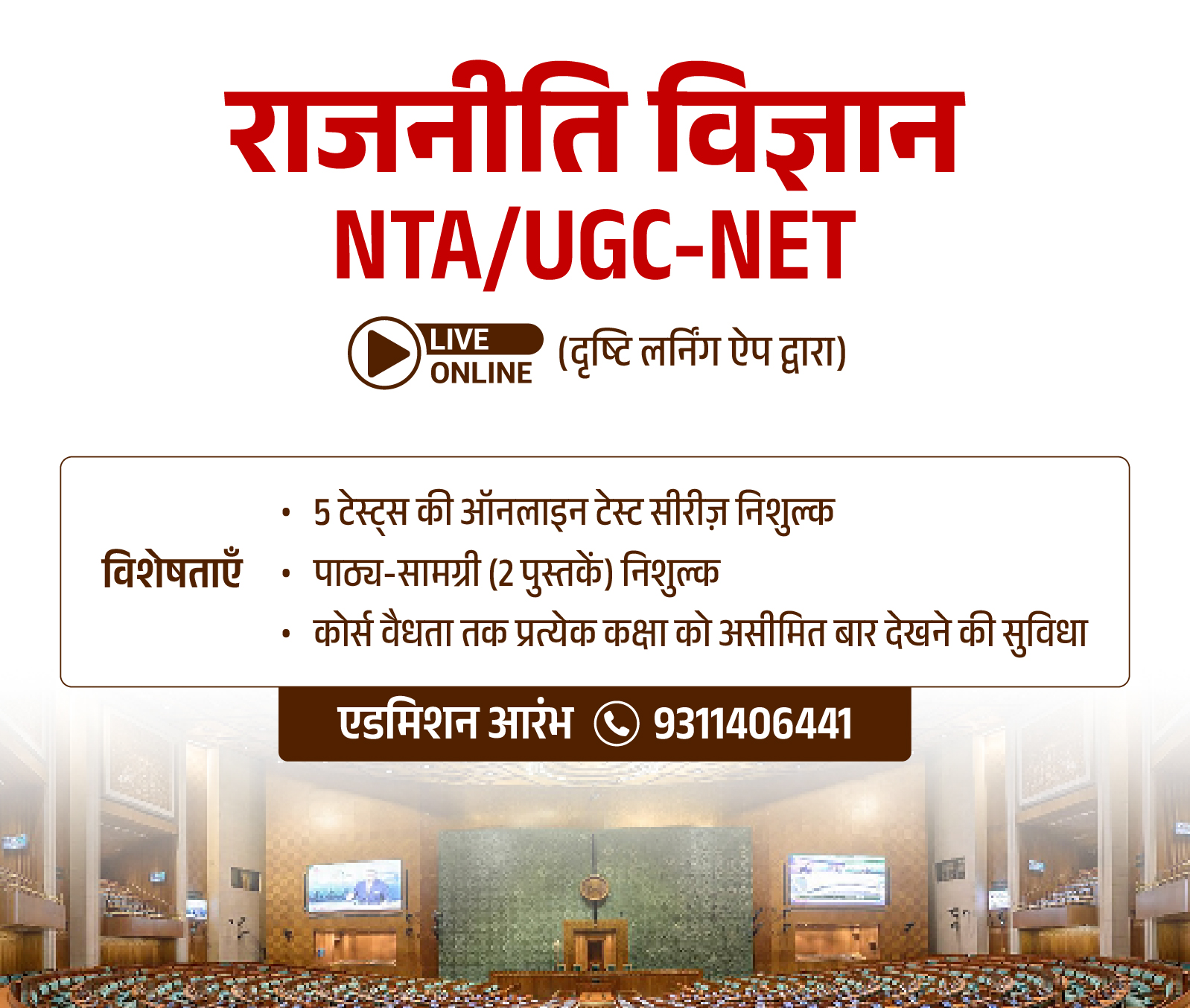

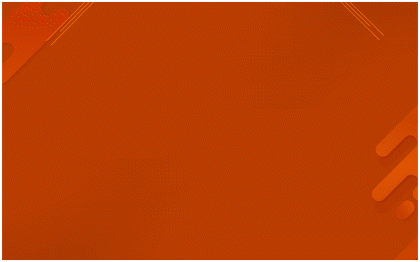


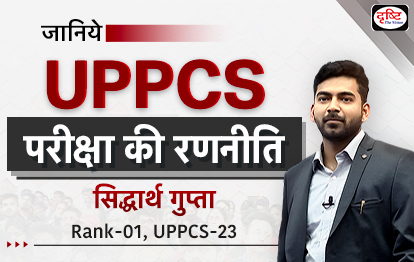
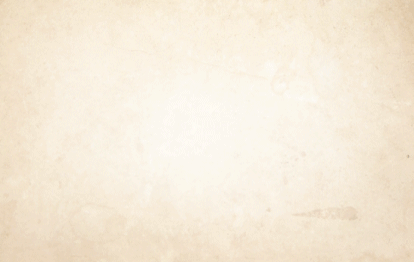

.jpg)
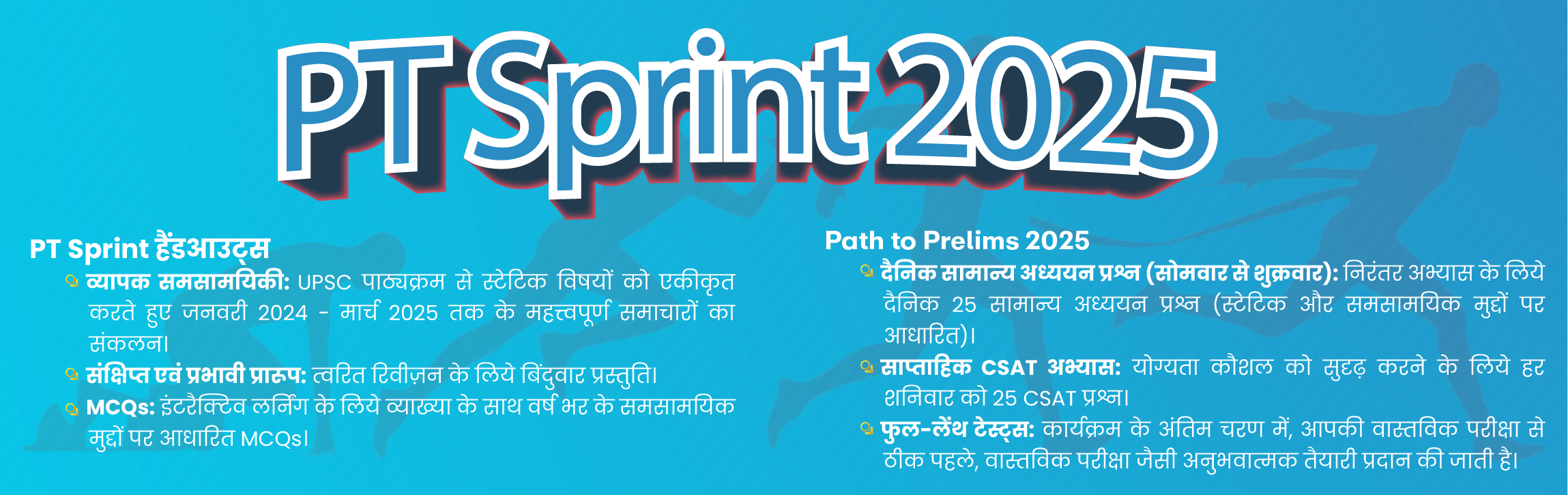
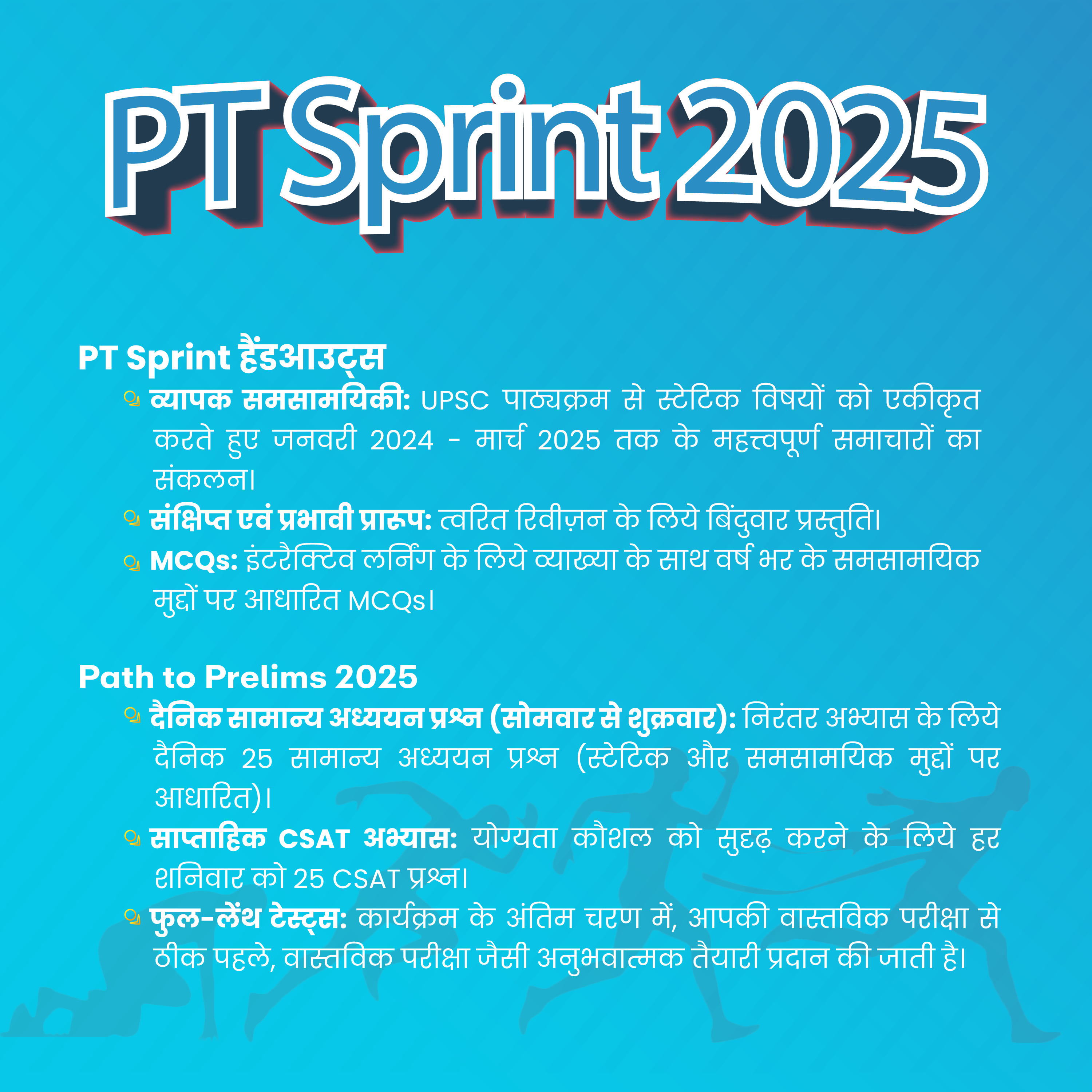

%201.jpeg)
.jpg)


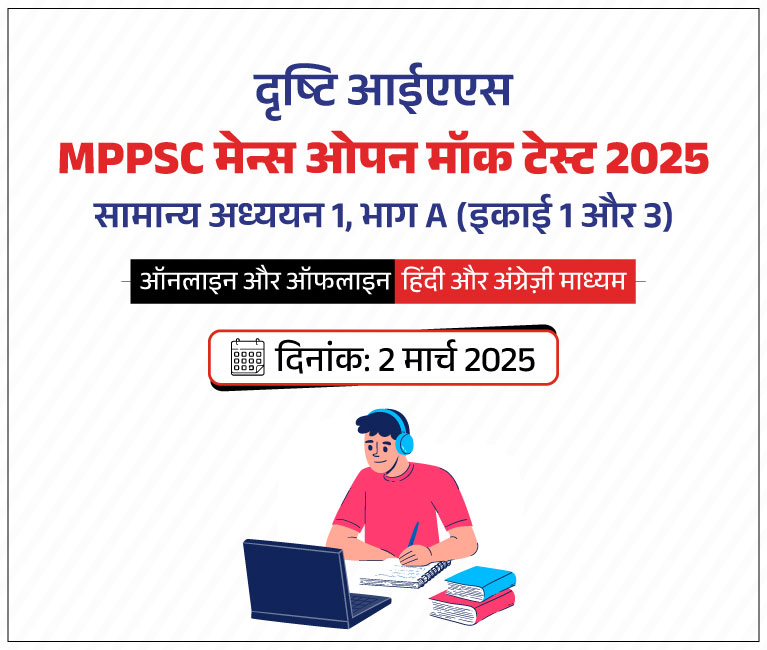
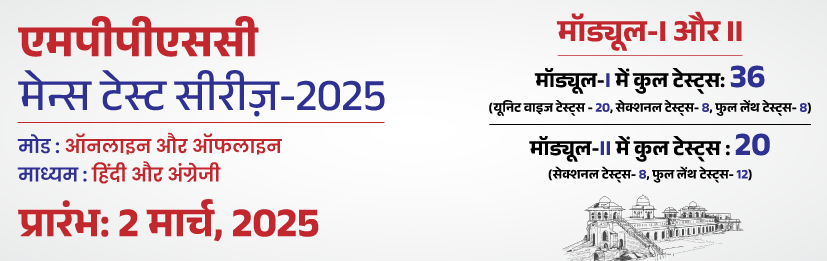

%20MPPCS%202025%20Desktop%20H.jpg)
%20MPPCS%202025%20Mobile%20H%20(1).jpg)

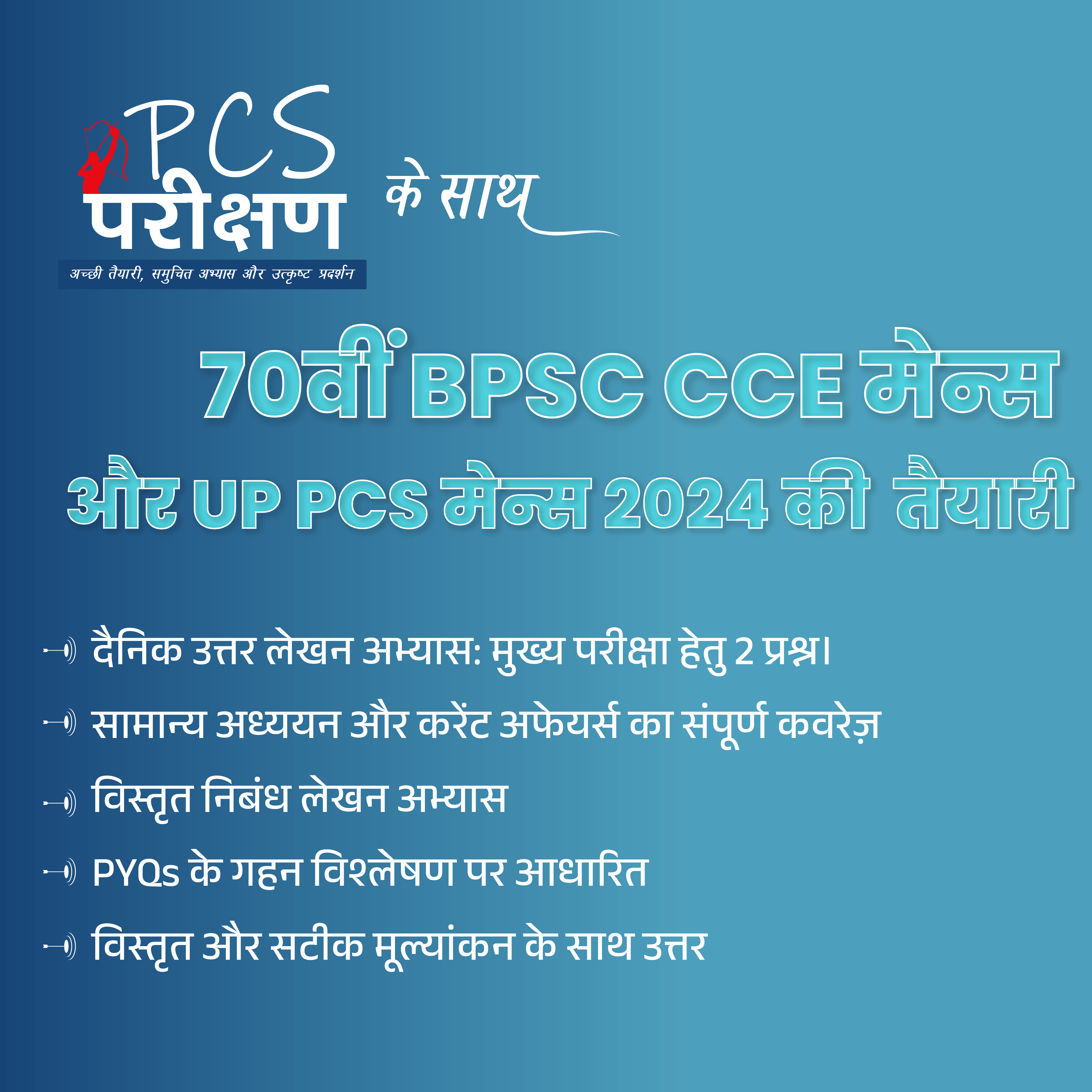


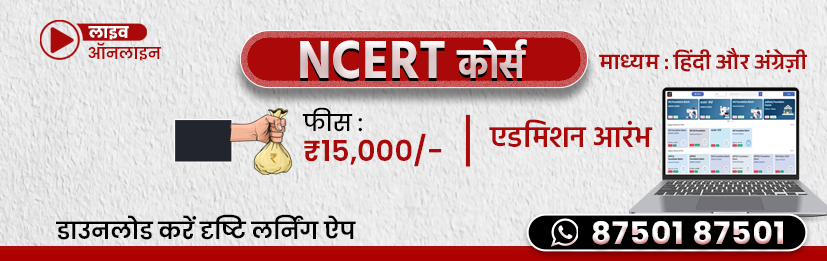
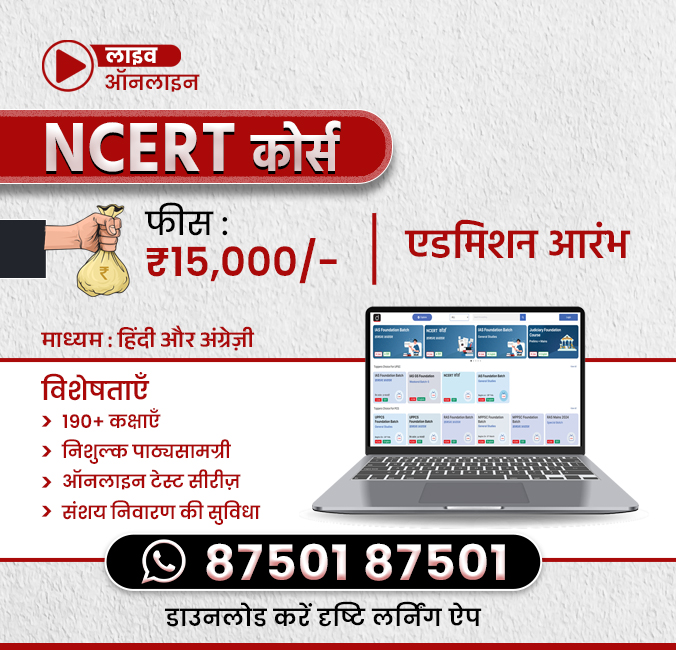

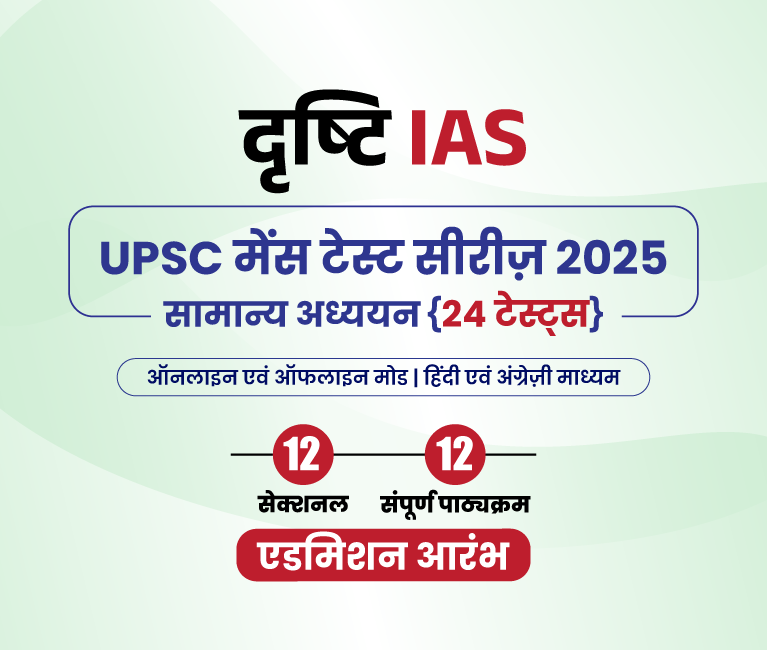
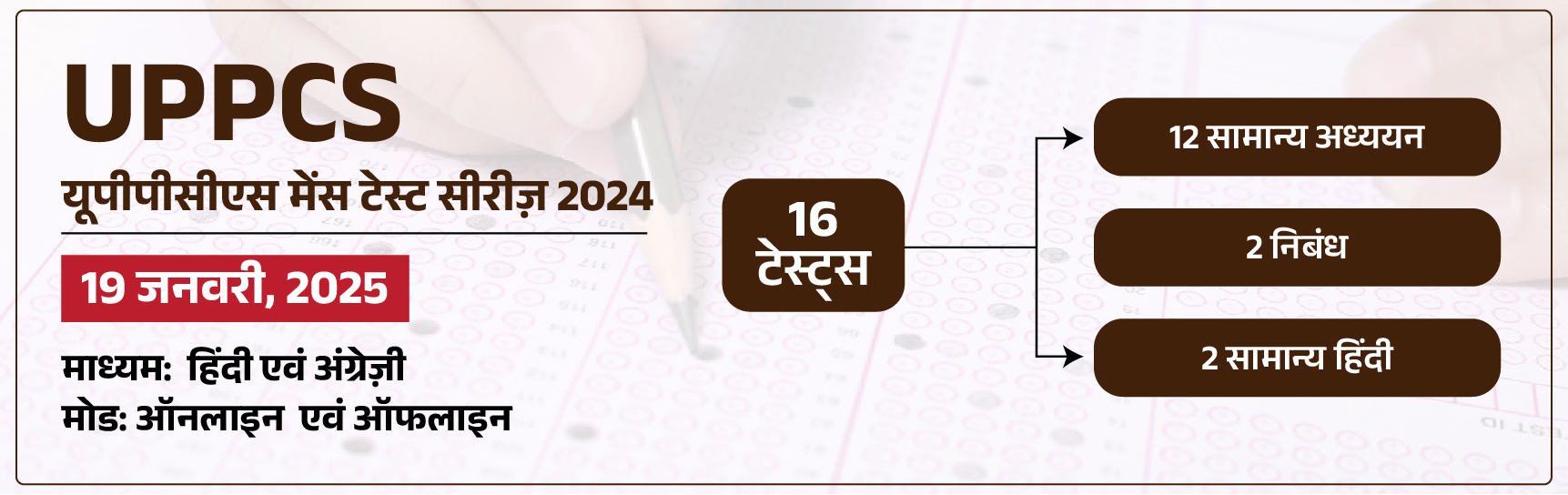
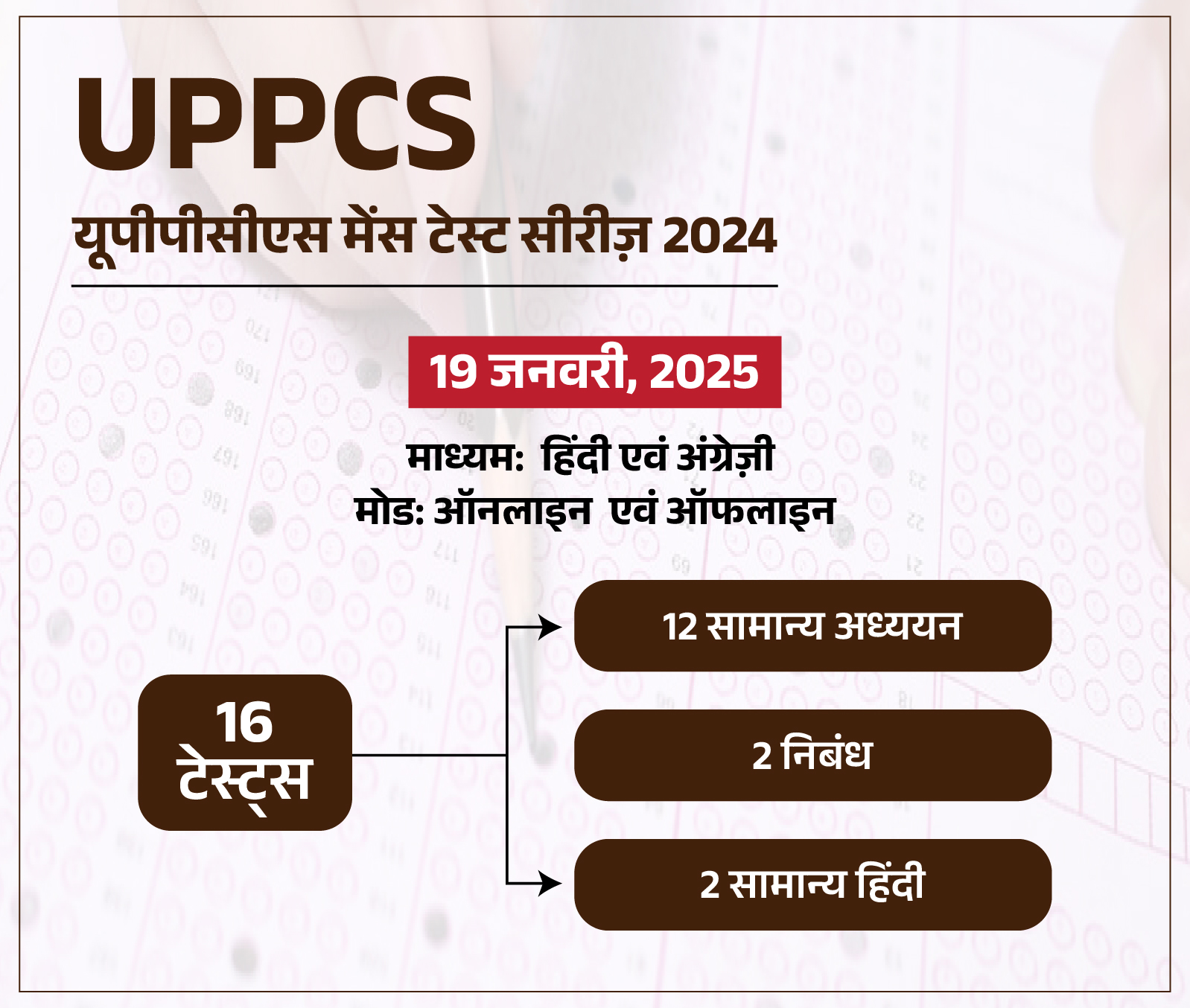



 PCS परीक्षण
PCS परीक्षण





