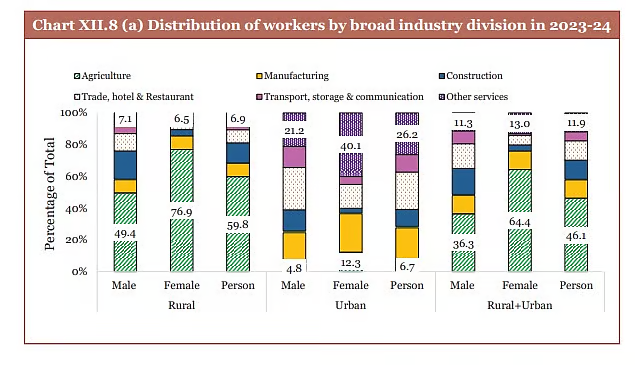विनिर्माण कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती अनौपचारिकता | 17 Apr 2025
प्रिलिम्स के लिये:अनौपचारिक क्षेत्र, औपचारिक क्षेत्र, कौशल भारत मिशन, डिजिटल साक्षरता अभियान, GDP, कौशल भारत मिशन मेन्स के लिये:भारत में विनिर्माण क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी की स्थिति, महिला श्रम भागीदारी से संबंधित चुनौतियाँ, महिला श्रम बल भागीदारी बढ़ाने के लिये प्रमुख पहल। |
स्रोत: द हिंदू
चर्चा में क्यों?
भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 17% का योगदान देने वाला विनिर्माण क्षेत्र, विकसित भारत के दृष्टिकोण के तहत आर्थिक विकास के लिये एक प्रमुख चालक माना जाता है। हालाँकि, इस क्षेत्र में, विशेष रूप से औपचारिक रोज़गार में, महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है, जो गहरी संरचनात्मक और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को दर्शाता है।
भारत पर्याप्त औपचारिक रोज़गार सृजित करने में क्यों संघर्ष करता है?
भारत में विनिर्माण क्षेत्र में महिलाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?
- औपचारिक क्षेत्र: औपचारिक विनिर्माण में महिलाओं की हिस्सेदारी वर्ष 2015-16 में 20.9% से घटकर वर्ष 2022-23 में 18.9% हो गई है, जिसमें 8.34 मिलियन औपचारिक श्रमिकों में से केवल 1.57 मिलियन महिलाएँ हैं।
- तमिलनाडु में सबसे अधिक (41%) महिलाएँ कार्यरत हैं, इसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात का स्थान है, जहाँ कुल मिलाकर औपचारिक विनिर्माण में लगभग 75% महिलाएँ कार्यरत हैं।
- बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में लैंगिक असमानता बहुत अधिक है (6% से भी कम महिलाएँ), और यहाँ तक कि गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे औद्योगिक राज्यों में भी (15% से भी कम महिलाएँ)।
- इसके विपरीत, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत बेहतर है।
- महिलाएँ ज्यादातर वस्त्र, परिधान और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत हैं, जो महिला रोज़गार का 60% है।
- तंबाकू एकमात्र औपचारिक विनिर्माण उद्योग है जहाँ पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएँ कार्यरत हैं।
- अनौपचारिक क्षेत्र: अनौपचारिक विनिर्माण कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 43% है, लेकिन वे अधिकतर कम वेतन वाली, कम कौशल वाली नौकरियों में कार्यरत हैं, जिनमें उन्हें नौकरी की सुरक्षा या लाभ नहीं मिलता।
- प्रमुख क्षेत्रों में वस्त्र और तंबाकू शामिल हैं, जहाँ अनौपचारिक तंबाकू कार्यबल में 90% से अधिक महिलाएँ हैं।
- हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में लैंगिक अंतराल अभी भी उच्च है।
- तेलंगाना, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में लैंगिक अंतराल नकारात्मक है, जो दर्शाता है कि अनौपचारिक विनिर्माण में पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएँ काम करती हैं।
भारत में महिला श्रम बल भागीदारी में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?
और पढ़ें: महिलाओं की कम भागीदारी के मुख्य कारण
नोट
- सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना है।
- यह बुनियादी ढाँचे और FDI को बढ़ावा देने के लिये मेक इन इंडिया, प्रमुख क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिये उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI) और वस्त्र क्षेत्र में महिलाओं को कौशल प्रदान करने के लिये समर्थ जैसी योजनाओं के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देता है।
- स्किल इंडिया योजना व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती है, जबकि मुद्रा योजना जबकि मुद्रा योजना विनिर्माण में महिला उद्यमियों को संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करती है।
औपचारिक विनिर्माण क्षेत्र में महिला श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाने हेतु क्या उपाय किये जा सकते हैं?
- शिक्षा और कौशल विकास: विनिर्माण क्षेत्र में केवल 30% महिलाओं ने माध्यमिक शिक्षा पूरी की है (जबकि पुरुषों में यह आँकड़ा 47% है), तथा केवल 6% के पास औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण है।
- इस अंतराल को कम करने हेतु, कौशल भारत मिशन और इसी प्रकार की पहलों में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार किया जाना चाहिये और साथ ही कुशल, बेहतर वेतन वाली नौकरियों तक उनकी पहुँच में सुधार करने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी क्षेत्रों में लक्षित कौशल उन्नयन किया जाना चाहिये।
- क्षेत्रीय विविधीकरण: औपचारिक विनिर्माण में महिलाएँ वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण (60%) जैसे सीमित क्षेत्रों तक ही केंद्रित हैं।
- लक्षित प्रशिक्षण और प्रोत्साहन के माध्यम से ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति का विविधीकरण करना, भागीदारी और अवसरों में सुधार लाने की कुंजी है।
- सुरक्षित कार्य वातावरण का निर्माण: छात्रावास, परिवहन और बाल देखभाल सुविधाओं के माध्यम से सुरक्षित और समावेशी कार्यस्थलों का निर्माण करने से राज्यों में विनिर्माण क्षेत्र में महिलाओं के प्रवेश और प्रतिधारण को बढ़ावा मिल सकता है।
- नीतिगत हस्तक्षेप: मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम और कारखाना अधिनियम जैसे अधिनियमों का सुदृढ़ीकरण करने से कार्य स्थितियों और लैंगिक समानता में सुधार हो सकता है।
- विनिर्माण क्षेत्र में महिलाओं की अधिक संख्या में नियुक्ति को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार और उद्योग को मातृत्व लाभ की लागत साझा करनी चाहिये, जिससे नियोक्ताओं पर वित्तीय बोझ कम हो जाएगा।
निष्कर्ष:
भारत के विनिर्माण क्षेत्र में महिलाएँ मुख्य रूप से अल्प वेतन वाली, अपर्याप्त परिस्थितियों वाली अनौपचारिक नौकरियों में कार्यरत हैं। इस अंतराल को कम करने हेतु, महिलाओं की शिक्षा, कौशल और कार्यस्थल सुरक्षा का वर्द्धन करना आवश्यक है और साथ ही अनौपचारिक से औपचारिक रोज़गार में उनकी सहभागिता को बढ़ावा देना भी आवश्यक है। समावेशी और सहायक परिवेश स्थापित करने से महिलाएँ सशक्त होंगी और देश के "विकसित भारत" बनने के लक्ष्य को पूरा करने में सहायता मिलेगी।
|
दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत के विनिर्माण क्षेत्र में महिलाओं के समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ हैं तथा उनकी भागीदारी और अवसर बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं? |
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP में वृद्धि आर्थिक विकास की ऊँची स्तर का संकेत नहीं करती, यदि: (2018) (a) औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ-साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। उत्तर: (c) प्रश्न. प्रच्छन्न बेरोज़गारी का आमतौर पर अर्थ होता है- (2013) (a) बड़ी संख्या में लोग बेरोज़गार रहते हैं उत्तर:(c) मेन्स:प्रश्न. भारत में सबसे ज्यादा बेरोज़गारी प्रकृति में संरचनात्मक है। भारत में बेरोज़गारी की गणना के लिये अपनाई गई पद्धतियों का परीक्षण कीजिये और सुधार के सुझाव दीजिये। (2023) प्रश्न. "भारत में बनाइये' कार्यक्रम की सफलता, 'कौशल भारत' कार्यक्रम और आमूल श्रम सुधारों की सफलता पर निर्भर करती है।" तर्कसम्मत दलीलों के साथ चर्चा कीजिये। (2015) प्रश्न. "जिस समय हम भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिविडेंड) को शान से प्रदर्शित करते हैं, उस समय हम रोज़गार-योग्यता की पतनशील दरों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं।" क्या हम ऐसा करने में कोई चूक कर रहे हैं? भारत को जिन जॉबों की बेसबरी से दरकार है, वे जॉब कहाँ से आएँगे? स्पष्ट कीजिये। (2014) |