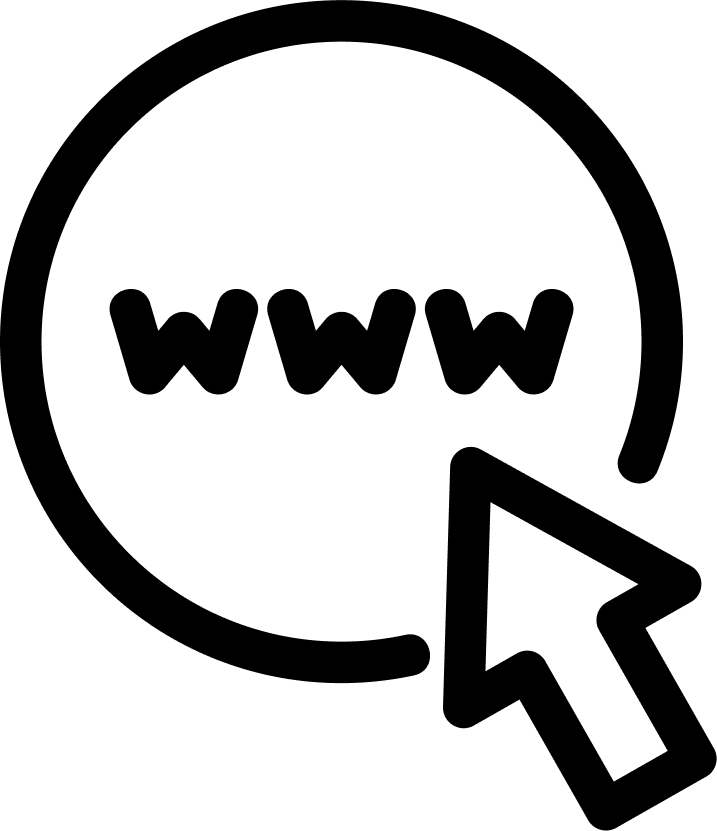भारतीय राजव्यवस्था
नागरिक स्वतंत्रता में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका
यह एडिटोरियल 13/08/2024 को ‘द हिंदू’ में प्रकाशित “The top court as custodian of liberties” लेख पर आधारित है। इसमें हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत देने के निर्णय की चर्चा की गई है जहाँ न्यायालय ने स्वतंत्रता को संवैधानिकता का अंतर्निहित अंग बताया और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने तथा समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। यह निर्णय आपराधिक न्याय प्रणाली में देरी की समस्या और कड़े कानूनों के समस्याग्रस्त उपयोग की आलोचना करता है तथा पुष्टि करता है कि जमानत को अपवाद के बजाय नियम की तरह देखा जाना चाहिये।
प्रिलिम्स के लिये:सर्वोच्च न्यायालय, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), मूल अधिकार के रूप में निजता का अधिकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A, मूल अधिकार, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम, ई-न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना। मेन्स के लिये:मूल अधिकारों एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में न्यायपालिका का महत्त्व। |
9 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई (speedy trial) एक मूल अधिकार है और बिना सुनवाई के लंबे समय तक कारावास, यहाँ तक कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) जैसे कड़े कानूनों के तहत भी, इस अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय का यह निर्णय, जो इस बात पर बल देता है कि ‘स्वतंत्रता संवैधानिकता का एक अंतर्निहित अंग है’, इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि जमानत को अपवाद के बजाय नियम के रूप में देखा जाना चाहिये (यानी यह एक मानक अभ्यास हो, न कि कोई दुर्लभ या असाधारण अभ्यास)। यह अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार के रूप में निष्पक्ष एवं समय पर सुनवाई सुनिश्चित करने की न्यायालय की प्रतिबद्धता को परिलक्षित करता है।
न्यायालय ने अपने निर्णय में न केवल जमानत के इस मामले विशेष को संबोधित किया, बल्कि आपराधिक न्याय प्रणाली में, विशेष रूप से PMLA जैसे कड़े कानूनों के तहत, अंतर्निहित विलंबन एवं अक्षमताओं के बारे में व्याप्त व्यापक चिंताओं पर भी मत व्यक्त किया। न्यायालय ने अत्यधिक देरी और ऐसे कानूनों के समस्याग्रस्त अनुप्रयोग को उजागर कर न्याय के प्रशासन के तरीके पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया, जहाँ उसका उद्देश्य प्रक्रियात्मक अतिक्रमण (procedural excesses) के विरुद्ध नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करना हो।
यह निर्णय न्याय को अक्षुण्ण रखने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में न्यायालय की महत्त्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है, जहाँ एक ऐसी न्याय प्रणाली की ओर बदलाव का आग्रह करता है जो व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करती हो और प्रणालीगत अकुशलताओं से निपटती हो।
सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में प्रतिष्ठित है, लेकिन हाल के वर्षों में इसे अधिकाधिक संवीक्षा का सामना करना पड़ा है। समकालीन राजनीतिक एवं संवैधानिक टिप्पणीकारों ने इसके कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं पर चिंता जताई है और इसकी स्वतंत्रता, निरंतरता एवं प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
- वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अंगीकृत किया। इसके तुरंत बाद ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन सत्र 28 जनवरी 1950 को आयोजित हुआ।
- भारतीय संविधान के भाग V (संघ) और अध्याय 6 (संघीय न्यायपालिका) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का उपबंध किया गया है।
- संविधान के भाग V में शामिल अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित हैं।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और, जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक, सात से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा।
- वर्तमान में शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को मोटे तौर पर मूल अधिकार क्षेत्र, अपीलीय अधिकार क्षेत्र और सलाहकार अधिकार क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय के पास अन्य कई शक्तियाँ भी हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अधिकारपूर्ण (authoritative) होते हैं और भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं।
- न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, जो उसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने, संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को बाधित करने या संविधान द्वारा गारंटीकृत मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले विधायी एवं कार्यकारी कृत्यों को अमान्य घोषित करने में सक्षम बनाती है। इस प्रकार, भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत में नागरिक स्वतंत्रता का संरक्षक या ‘गारंटर’ है।
कौन-से प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय को नागरिक स्वतंत्रता का संरक्षक बनाते हैं?
- संवैधानिक प्रावधान:
- अनुच्छेद 13: यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कोई भी विधि जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है या उन्हें छीनती है, उसे शून्य माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय यह तय कर सकता है कि कोई विधि असंवैधानिक है या नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।
- अनुच्छेद 32: यह अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिये सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। यह सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का रक्षक बनाता है।
- अनुच्छेद 136: यह प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिये विशेष अनुमति देने की विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है, जिसमें नागरिक स्वतंत्रता से संबंधित मामले भी शामिल हैं।
- विशेष अनुमति याचिका(SLP): यह सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी जाती एक याचिका है जिसमें महत्त्वपूर्ण विधिक मुद्दों पर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील करने की अनुमति मांगी जाती है।
- अनुच्छेद 142: यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को नागरिक स्वतंत्रता और मूल अधिकारों की सुरक्षा सहित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिये आवश्यक कोई भी आदेश या डिक्री पारित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- अन्य साधन:
- रिट: ये उच्चतर न्यायालयों द्वारा मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने या सार्वजनिक प्राधिकारों को निर्देश देने के लिये जारी विधिक आदेश हैं। नागरिक स्वतंत्रता को लागू करने के लिये बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार-पृच्छा रिट उपलब्ध हैं।
- जनहित याचिका (PIL): ये आम लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबोधित करने और व्यापक सामाजिक सरोकार के मामलों पर न्याय सुनिश्चित करने के लिये दायर की गई याचिकाएँ हैं।
- न्यायिक समीक्षा: यह विधियों और सरकारी कृत्यों की संवैधानिकता का आकलन करने की न्यायालयों की शक्ति है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे संविधान के अनुरूप हैं।
- विभिन्न सिद्धांत:
- मूल ढाँचा सिद्धांत (Basic Structure Doctrine): यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित एक सिद्धांत है जो बलपूर्वक स्थापित करता है कि संविधान की कुछ मूल विशेषताओं को संशोधनों द्वारा बदला या नष्ट नहीं किया जा सकता है।
- यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि संविधान में संशोधन से उसके आवश्यक ढाँचे, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और विधि के शासन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिये। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले (1973) में इसे औपचारिक रूप प्रदान किया गया था।
- विच्छेदनीयता का सिद्धांत (Doctrine of Severability): इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी विधि का कोई भाग असंवैधानिक पाया जाता है तो उस भाग को शेष विधि से अलग किया जा सकता है, जो तभी वैध रहेगा जब वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके।
- यह विधि के केवल असंवैधानिक हिस्सों को अमान्य करने में मदद करता है तथा शेष विधि को सुरक्षित बनाए रखता है।
- आच्छादन का सिद्धांत (Doctrine of Eclipse): इस सिद्धांत के अनुसार, यदि कोई विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वह उल्लंघन की सीमा तक शून्य या ‘आच्छादित’ हो जाती है, लेकिन पूरी तरह से शून्य एवं निरस्त नहीं होती है। यह तब तक निष्क्रिय बनी रहती है जब तक यह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, लेकिन यदि असंगतता को दूर कर दिया जाए तो इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है।
- यह सिद्धांत यह प्रावधान करता है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों को पूरी तरह से अवैध घोषित नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें तब तक निलंबित कर दिया जाएगा जब तक कि वे संविधान के अनुरूप नहीं हो जाते।
- मूलभूत सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत (Doctrine of Substantive Due Process): यह सिद्धांत केवल प्रक्रियात्मक निष्पक्षता से आगे बढ़कर मूल अधिकारों (fundamental rights) के रूप में कुछ मूलभूत अधिकारों (substantive rights) के संरक्षण को शामिल करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि विधियाँ मूल अधिकारों के मूल सार का उल्लंघन न करें।
- यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली विधियाँ न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित हों।
- छद्मता का सिद्धांत (Doctrine of Colorable Legislation): छद्मता का सिद्धांत एक विधिक सिद्धांत है जो सरकार को अपने विधायी अधिकार का असंवैधानिक तरीके से उपयोग करने से रोकता है। इसे ‘संविधान के साथ धोखाधड़ी’ (Fraud on the Constitution) के रूप में भी जाना जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो कार्य प्रत्यक्षतः नहीं किये जा सकते, उन्हें अप्रत्यक्षतः भी नहीं किया जा सकता।
ऐसे कौन-से उदाहरण हैं जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में कार्य किया है?
- दिल्ली आबकारी नीति मामला (2024):
- इस हालिया निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि शीघ्र सुनवाई का अधिकार (right to a speedy trial) अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार है।
- करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य (1994) मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा शीघ्र सुनवाई के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया था।
- इस निर्णय में इस बात पर बल दिया गया कि बिना सुनवाई के लंबे समय तक कारावास में रखना नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, विशेष रूप से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) जैसे कड़े कानूनों के संदर्भ में।
- इस हालिया निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि शीघ्र सुनवाई का अधिकार (right to a speedy trial) अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार है।
- अर्नब गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य (2020):
- निर्णय में स्वतंत्रता और शीघ्र सुनवाई के अधिकार को रेखांकित किया गया तथा इस बात पर बल दिया गया कि मनमाने या अतिक्रमणकारी विधिक कानूनी उपायों के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरा नहीं पहुँचाया जा सकता।
- इसने इस संवैधानिक सिद्धांत को दोहराया कि जमानत मानक या आदर्श स्थिति है और कारावास में बनाए रखना अपवाद है। यह सिद्धांत न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर द्वारा वर्ष 1977 में व्यक्त किया गया था।
- यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष एवं शीघ्र सुनवाई के अधिकार के अनुरूप है।
- नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018):
- सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को निरस्त करते हुए सहमतिपूर्ण समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया।
- इस ऐतिहासिक निर्णय ने LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों की पुष्टि की तथा भेदभावपूर्ण कानूनों के विरुद्ध व्यक्तिगत गरिमा एवं निजता को बनाए रखने के प्रति न्यायालय की प्रतिबद्धता को उजागर किया।
- न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017):
- सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के तहत मूल अधिकार माना।
- निर्णय में इस बात पर बल दिया गया कि निजता किसी व्यक्ति की गरिमा का अभिन्न अंग है और इसे राज्य की मनमानी कार्रवाइयों से संरक्षित किया जाना चाहिये, ताकि भारत में नागरिक स्वतंत्रता का दायरा बढ़ सके।
- श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015):
- सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को रद्द कर दिया, जो आपत्तिजनक या धमकीपूर्ण ऑनलाइन सामग्री को अपराध मानती थी।
- न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है।
- ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2014):
- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संज्ञेय अपराधों की शिकायत मिलने पर पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी (FIR)) दर्ज करने के लिये बाध्य है।
- इस निर्णय ने शिकायतों का कानून प्रवर्तन द्वारा समाधान किये जाने के व्यक्तियों के अधिकार को सुदृढ़ किया, ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो और नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा हो।
- लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013):
- न्यायालय ने घोषणा की कि यदि कोई विधि-निर्माता या सदन सदस्य दो वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराध के लिये दोषी पाया जाता है तो उसे (अपील के लंबित रहने के बावजूद) दोषसिद्धि के तुरंत बाद पद पर बने रहने के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- यह निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों की विश्वसनीयता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था।
- गौरव जैन बनाम भारत संघ (1997):
- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने वेश्यावृत्ति के संदर्भ में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को संबोधित किया।
- न्यायालय ने कहा कि देह व्यापार में संलग्न महिलाओं को अपराधी के बजाय सामाजिक-आर्थिक कठिनाइयों के पीड़ित के रूप में देखा जाना चाहिये तथा उन्हें और उनके बच्चों को गरिमा, सुरक्षा एवं बिना किसी कलंक के समाज में पुनः एकीकृत होने का अवसर मिलना चाहिये।
- मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978):
- इस मामले ने अनुच्छेद 21 के दायरे को बढ़ाया, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह अधिकार केवल अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है।
- निर्णय में इस बात पर बल दिया गया कि किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने वाला कोई भी कानून निष्पक्ष, न्यायसंगत एवं उचित होना चाहिये; इस प्रकार, प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ किया गया।
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973):
- इस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘मूल ढाँचा सिद्धांत’ की स्थापना की और कहा कि नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षण सहित संविधान की कुछ मूल विशेषताओं को संशोधनों द्वारा बदला नहीं जा सकता।
- न्यायालय ने कहा कि संविधान में निहित मूल अधिकार उसकी मूल संरचना अंग हैं, जिन्हें संरक्षित किया जाना चाहिये।
- ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950):
- इस आरंभिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निवारक निरोध (preventive detention) के मुद्दे पर विचार किया। हालाँकि इस निर्णय ने आरंभ में निवारक निरोध कानूनों की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन इसने बाद के निर्णयों के लिये एक मंच तैयार किया जहाँ मूल अधिकारों के साथ बेहतर तालमेल के लिये ऐसे कानूनों के दायरे को संबोधित एवं सीमित किया गया।
- रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950):
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मद्रास में एक समाचार पत्र के प्रवेश एवं प्रसार पर प्रतिबंध लगाने वाला सरकारी आदेश संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है और माना कि प्रेस की स्वतंत्रता वाक् एवं अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य के अधिकार का एक अनिवार्य अंग है।
- इसमें इस बात पर बल दिया गया कि राज्य प्रेस पर मनमाने प्रतिबंध नहीं लगा सकता; इस प्रकार, नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा को मज़बूत किया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सरकार की शक्ति को सीमित किया।
सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकरण से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ
- निर्णयों का क्रियान्वयन:
- आलोचकों ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के क्रियान्वयन एवं प्रवर्तन के बारे में चिंता जताई है। कुछ मामलों में, न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, उसके आदेशों का क्रियान्वयन सुस्त या अपर्याप्त रहा है।
- संवैधानिक विशेषज्ञों का तर्क है कि सुदृढ़ कार्यान्वयन ढाँचे के बिना न्यायालय के निर्णयों का प्रभाव कम हो सकता है, जिससे वादियों में निराशा पैदा होगी और विधि का शासन कमज़ोर होगा।
- इसके अलावा, नागरिक स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समर्थित विभिन्न सिद्धांतों के अनुप्रयोग में एकरूपता मौजूद नहीं है ।
- विभिन्न पीठों में सैद्धांतिक एकरूपता के अभाव के कारण कानूनी परिणामों में भ्रम और अप्रत्याशितता उत्पन्न होती है।
- मामले में देरी और लंबितता:
- सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दा लंबित मामलों के विशाल बोझ का है, जिसके कारण न्याय मिलने में व्यापक देरी हो रही है।
- राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार, भारतीय न्यायालयों में लगभग 4.4 करोड़ मामले लंबित पड़े हैं, जिनमें से 1 करोड़ से अधिक मामले सिविल मुक़दमे हैं।
- न्यायनिर्णयन में देरी से न केवल न्यायपालिका में लोगों का विश्वास कम होता है, बल्कि वादियों के जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विभिन्न पीठों में सैद्धांतिक एकरूपता की कमी से कानूनी परिणामों में भ्रम और अनिश्चितता पैदा होती है।
- सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दा लंबित मामलों के विशाल बोझ का है, जिसके कारण न्याय मिलने में व्यापक देरी हो रही है।
- ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ का मुद्दा:
- न्यायाधीशों सहित विभिन्न आलोचकों ने ‘मास्टर ऑफ द रोस्टर’ की अवधारणा की आलोचना की है, जो मुख्य न्यायाधीश को पीठों के गठन और मामलों के आवंटन का विशेष अधिकार प्रदान करती है। उनका तर्क है कि इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिये कि मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों पर श्रेष्ठ स्थिति रखता है।
- उनका मानना है कि रोस्टर प्रबंधन को निर्देशित करने वाली पारंपरिक परंपराओं की अनदेखी की गई है, जिसके परिणामस्वरूप मुख्य न्यायाधीश द्वारा चुनिंदा और संभावित रूप से पक्षपातपूर्ण मामलों का आवंटन किया गया है।
- न्यायिक अतिक्रमण और सक्रियता:
- सर्वोच्च न्यायालय की सबसे अधिक आलोचनाओं में से एक इसके न्यायिक अतिक्रमण और सक्रियता (Judicial Overreach and Activism) के लिये की जाती रही है।
- आलोचकों का तर्क है कि न्यायालय ने कई बार विधायिका एवं कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है, जिससे सरकार की तीनों शाखाओं के बीच शक्ति संतुलन बिगड़ गया है।
- इस तरह की सक्रियता से शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत (principle of separation of powers) के कमज़ोर पड़ने का खतरा है और न्यायिक सत्तावाद (judicial authoritarianism) के आरोप लग सकते हैं।
- नियुक्तियाँ एवं पारदर्शिता संबंधी मुद्दे:
- सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी आलोचना का केंद्र बिंदु रही है। नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से बनाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम को वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया।
- पारदर्शिता एवं संपूर्णता का अभाव तथा न्यायाधीशों की उपयुक्तता के आकलन के लिये स्पष्ट मानकों का अभाव ‘कॉलेजियम’ की ईमानदारी के प्रति भरोसे को कम करती है।
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता:
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारत में एक मूल सिद्धांत है, जिसकी गारंटी संविधान द्वारा अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 124(2) जैसे प्रावधानों के माध्यम से दी गई है, जिसका उद्देश्य न्यायिक कार्यों को कार्यपालिका के प्रभाव से स्वतंत्र रखना है।
- इन सुरक्षा उपायों के बावजूद, न्यायिक नियुक्तियाँ, प्रक्रियागत देरी और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियाँ इस स्वतंत्रता के लिये खतरा पैदा करती हैं।
न्यायिक आचरण के ‘बैंगलोर सिद्धांत’
- न्यायिक आचरण के बैंगलोर सिद्धांतों (Bangalore Principles of Judicial Conduct) का उद्देश्य न्यायाधीशों के लिये नैतिक मानक निर्धारित करना है।
- वे न्यायिक व्यवहार को विनियमित करने के लिये एक रूपरेखा प्रदान करते हैं और न्यायिक नैतिकता बनाए रखने पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
- ये सिद्धांत छह प्रमुख मूल्यों को चिह्नित करते हैं: स्वतंत्रता (independence), निष्पक्षता (impartiality), अखंडता/सत्यनिष्ठा (integrity), औचित्य (propriety), समानता (equality) और योग्यता एवं कर्मठता (competence and diligence)।
- स्वतंत्रता: न्यायाधीशों को बाह्य दबावों या प्रभावों से मुक्त होकर निर्णय लेना चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके निर्णय पूरी तरह विधि पर आधारित हों।
- निष्पक्षता: न्यायाधीशों को पूर्वाग्रहरहित एवं निष्पक्ष होना चाहिये, सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार करना चाहिये और साक्ष्य एवं विधिक सिद्धांतों के आधार पर मामलों का निर्णय करना चाहिये।
- अखंडता: न्यायाधीशों को ईमानदारी एवं नैतिकता से कार्य करना चाहिये तथा सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता के उच्च मानकों को बनाए रखना चाहिये।
- औचित्य: न्यायाधीशों को न्यायालय के अंदर और बाहर अपने पद की गरिमा के अनुरूप आचरण करना चाहिये।
- समानता: न्यायाधीशों को सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिये, यह सुनिश्चित करना चाहिये कि किसी के साथ अनुचित भेदभाव न हो तथा न्याय निष्पक्ष रूप से हो।
- योग्यता एवं कर्मठता: न्यायाधीशों के पास आवश्यक विधिक विशेषज्ञता होनी चाहिये और उन्हें मामलों को सावधानीपूर्वक एवं गहनता से निपटाना चाहिये, ताकि समयबद्ध और सुविचारित निर्णय सुनिश्चित हो सके।
- ये सिद्धांत इन मूल्यों को परिभाषित करते हैं और प्रत्येक मूल्य का प्रभावी ढंग से पालन करने के लिये न्यायाधीशों से अपेक्षित आचरण का विवरण प्रदान करते हैं।
आगे की राह
- कार्यान्वयन ढाँचे को सुदृढ़ करना:
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के कार्यान्वयन के लिये स्पष्ट, प्रवर्तनीय दिशानिर्देश विकसित किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्देशों पर शीघ्र एवं प्रभावी ढंग से कार्रवाई हो।
- आदेशों के निष्पादन पर नज़र रखने और गैर-अनुपालन के मुद्दों को हल करने के लिये निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए।
- लंबित मामलों को कम करना:
- सुनवाई प्रक्रिया में तेज़ी लाने और लंबित मामलों को कम करने के लिये न्यायाधीशों एवं न्यायालय के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जाए।
- प्रक्रियाओं को सरल बनाने और दक्षता बढ़ाने के लिये ई-फाइलिंग एवं केस प्रबंधन प्रणालियों जैसे प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों को लागू किया जाए।
- उदाहरण के लिये, भारत सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग कर न्याय तक पहुँच में सुधार लाने के उद्देश्य से ज़िला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिये देश में ई-कोर्ट एकीकृत मिशन मोड परियोजना शुरू की गई है।
- सिद्धांतगत एकरूपता सुनिश्चित करना:
- निर्णयों में भिन्नता को कम करने के लिये क्रॉस-बेंच संवाद को बढ़ावा देकर और न्यायिक दृष्टिकोण को मानकीकृत करक विधिक सिद्धांतों के एकरूप या सार्वभौमिक अनुप्रयोग को बढ़ावा दिया जाए।
- उदाहरण के लिये, सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय (जहाँ निष्पक्ष एवं समयबद्ध सुनवाई के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार के रूप में देखा गया है) की भावना को अन्य लंबित मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिये लागू किया जाना चाहिये।
- न्यायिक निर्णयों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिये व्यापक दिशानिर्देशों के विकास को प्रोत्साहित किया जाए।
- निर्णयों में भिन्नता को कम करने के लिये क्रॉस-बेंच संवाद को बढ़ावा देकर और न्यायिक दृष्टिकोण को मानकीकृत करक विधिक सिद्धांतों के एकरूप या सार्वभौमिक अनुप्रयोग को बढ़ावा दिया जाए।
- न्यायिक अतिक्रमण को संबोधित करना:
- विधायी और कार्यकारी मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं को स्पष्ट कर शक्तियों के पृथक्करण को सुदृढ़ किया जाए।
- न्यायिक संयम को बढ़ावा दिया जाए तथा अतिक्रमण के आरोपों से बचने और सरकारी शाखाओं के बीच संतुलन बनाए रखने के लिये संवैधानिक सीमाओं के पालन पर बल दिया जाए।
- नियुक्तियों और पारदर्शिता में सुधार:
- न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिये ‘कॉलेजियम प्रणाली’ को संशोधित किया जाए।
- न्यायिक उम्मीदवारों के मूल्यांकन के लिये स्पष्ट मानक स्थापित करने तथा अधिक पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक सुधारों पर विचार किया जाए।
- न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करना:
- न्यायिक स्वतंत्रता के लिये विद्यमान खतरों का समाधान कर संवैधानिक सुरक्षा उपायों को अक्षुण्ण बनाए रखा जाए, जिसमें नियुक्तियों, प्रक्रियागत देरी और भ्रष्टाचार से संबंधित चिंताओं का समाधान करना भी शामिल है।
- न्यायिक प्रणाली की स्वतंत्रता और अखंडता को सुदृढ़ करने के लिये न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच जारी संवाद को प्रोत्साहित किया जाए।
निष्कर्ष
न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रायः लोकतांत्रिक राजनीति की आधारशिला माना जाता है। भारत में यह सिद्धांत संविधान में निहित है, जिसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप से स्वतंत्रता की गारंटी देने वाले उपबंध किये गए हैं।
हालाँकि, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को पिछले कुछ वर्षों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कथित तौर पर कार्यकारी अतिक्रमण और न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने के प्रयासों के कई उदाहरण सामने आए हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, भारतीय न्यायपालिका ने संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिये अपने साहस एवं प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। मूल अधिकारों, चुनावी सुधारों और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर ऐतिहासिक निर्णयों ने संवैधानिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में इसकी स्थिति को सुदृढ़ किया है।
अभ्यास प्रश्न: सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण के रूप में भारत का सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक मूल्यों और नागरिक स्वतंत्रता को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पर प्रकाश डालते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न. भारत में उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2017) |