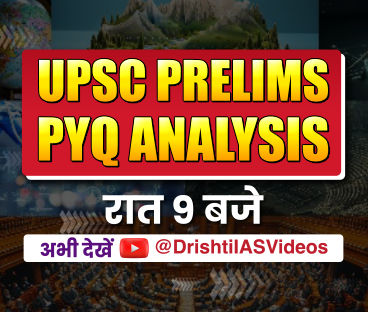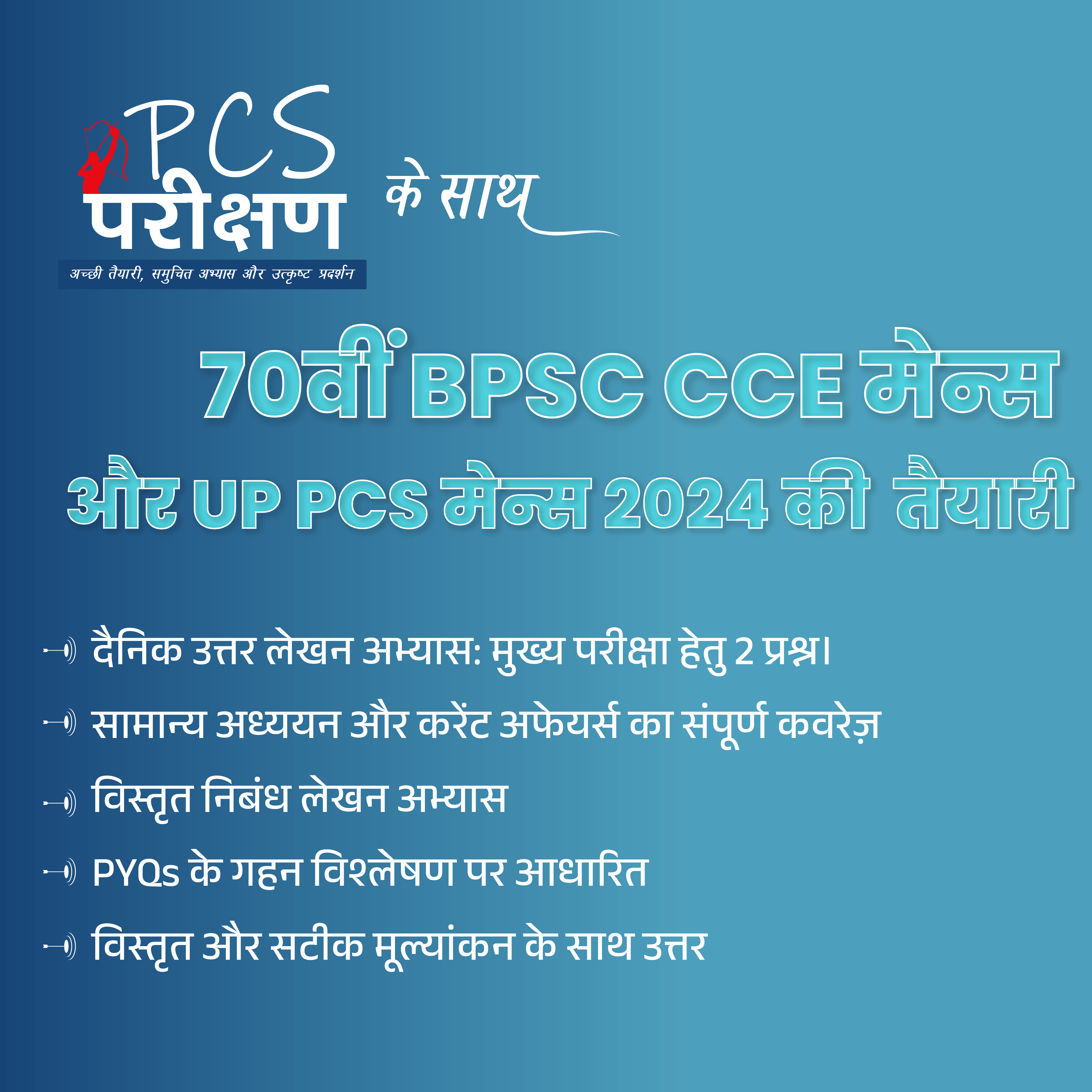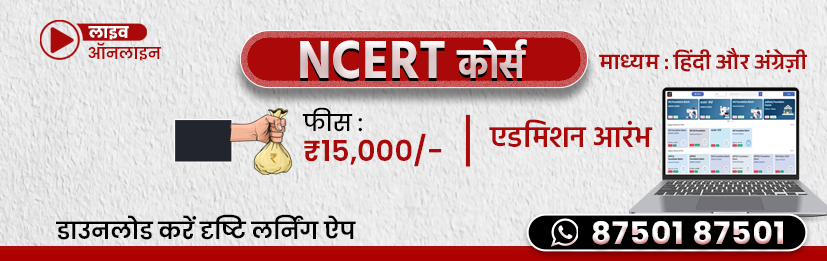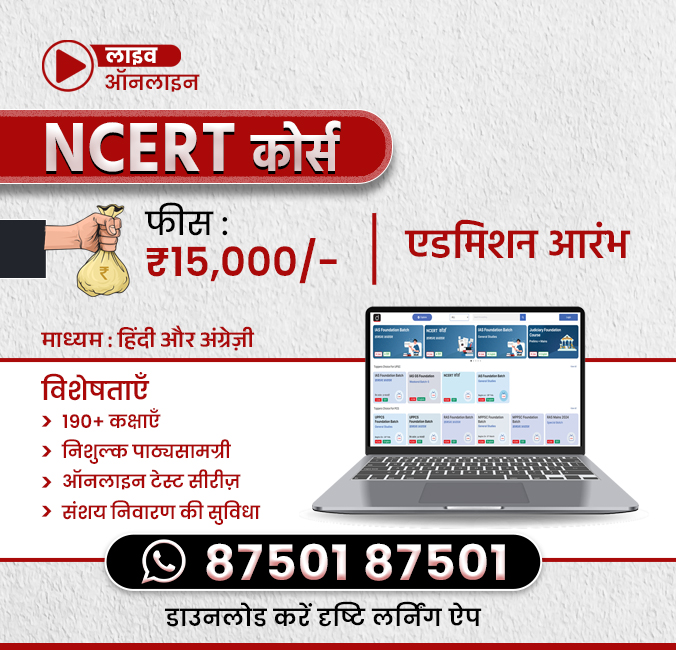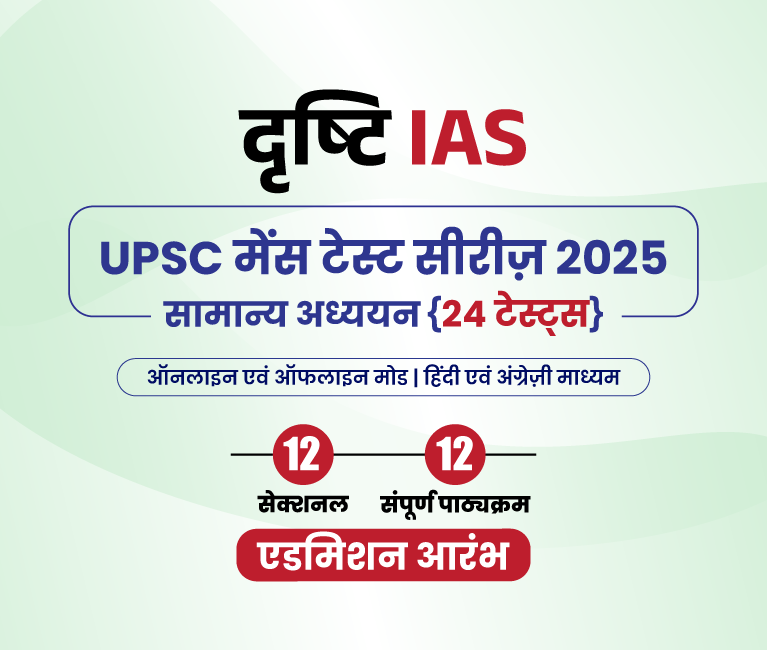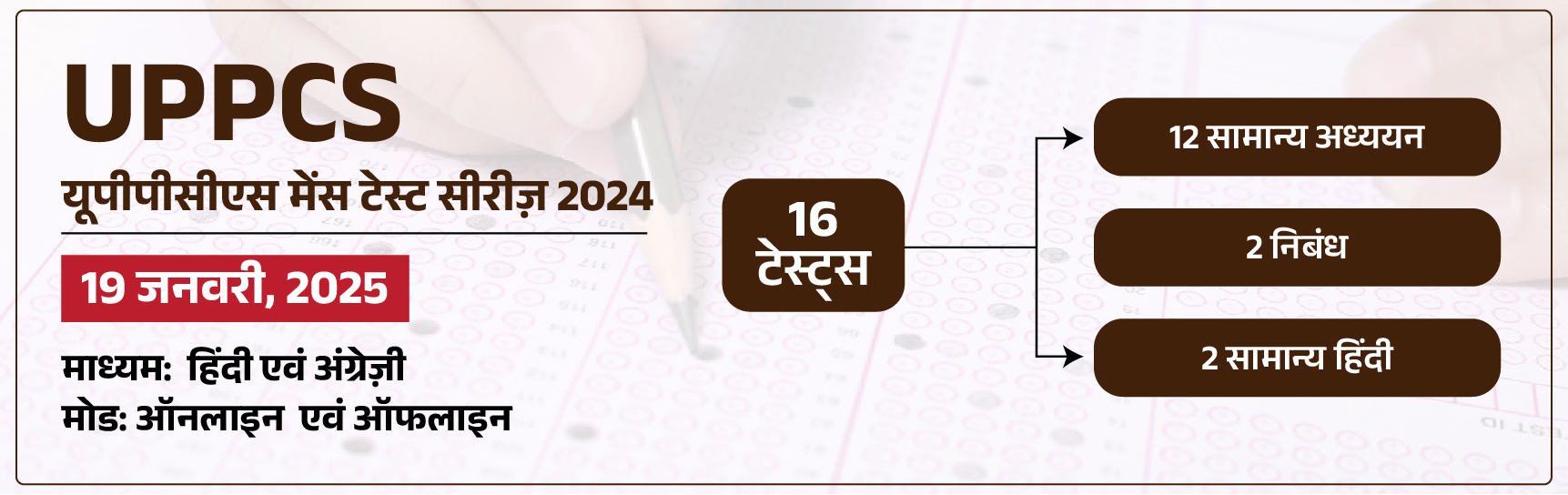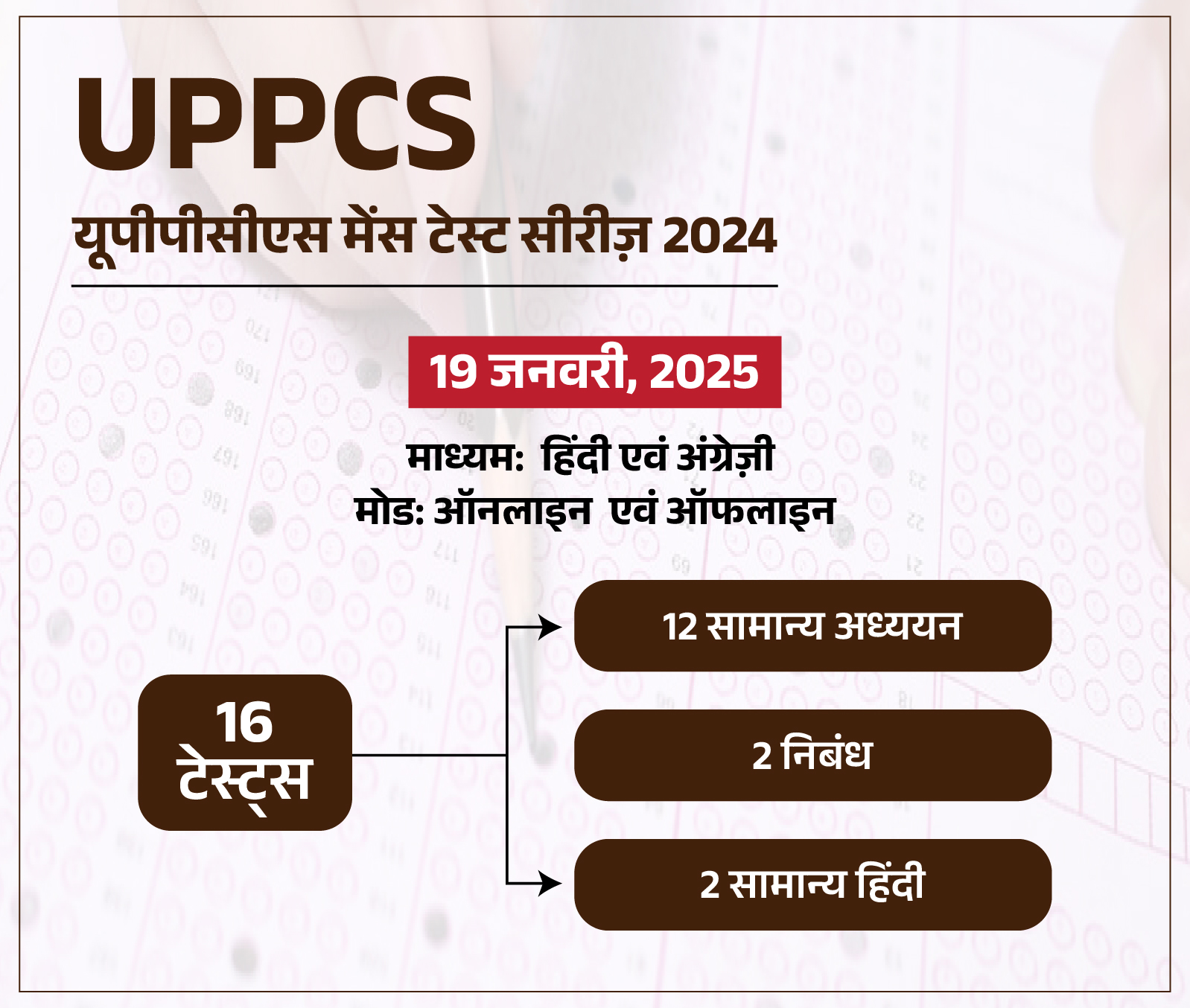उत्तर प्रदेश Switch to English
गरीबी उन्मूलन लक्ष्य
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तीन साल के भीतर राज्य में गरीबी उन्मूलन की योजना की घोषणा की है। उन्होंने सभी के लिये आवास, पानी और रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
मुख्य बिंदु
- गरीबी के बारे में:
- गरीबी एक ऐसी स्थिति या अवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिये वित्तीय संसाधन और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। गरीबी का मतलब है कि रोजगार से आय का स्तर इतना कम है कि बुनियादी मानवीय ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं।
- विश्व बैंक के अनुसार, गरीबी का अर्थ है खुशहाली में कमी और इसमें कई आयाम शामिल हैं। इसमें कम आय और गरिमा के साथ जीने के लिये आवश्यक बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने में असमर्थता शामिल है। गरीबी में स्वास्थ्य और शिक्षा का निम्न स्तर, स्वच्छ जल और स्वच्छता तक खराब पहुँच, अपर्याप्त शारीरिक सुरक्षा, आवाज़ की कमी और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिये अपर्याप्त क्षमता और अवसर भी शामिल हैं।
- वर्ष 2018 में, दुनिया के लगभग 8% श्रमिक और उनके परिवार प्रति व्यक्ति प्रति दिन 1.90 अमेरिकी डॉलर (अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा) से कम पर जीवन यापन कर रहे थे।
- गरीबी के प्रकार:
- पूर्ण गरीबी: ऐसी स्थिति जिसमें घरेलू आय बुनियादी जीवन स्तर (भोजन, आश्रय, आवास) को बनाए रखने के लिये आवश्यक स्तर से कम हो। यह स्थिति विभिन्न देशों के बीच और समय के साथ तुलना करना संभव बनाती है।
- इसे पहली बार वर्ष 1990 में पेश किया गया था, "एक डॉलर प्रतिदिन" गरीबी रेखा ने दुनिया के सबसे गरीब देशों के मानकों के अनुसार पूर्ण गरीबी को मापा। अक्तूबर 2015 में, विश्व बैंक ने इसे $1.90 प्रतिदिन पर निर्धारित कर दिया।
- सापेक्ष गरीबी: इसे सामाजिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया जाता है, अर्थात आसपास रहने वाली आबादी के आर्थिक मानकों की तुलना में जीवन स्तर। इसलिये यह आय असमानता का एक उपाय है।
- आमतौर पर सापेक्ष गरीबी को जनसंख्या के उस प्रतिशत के रूप में मापा जाता है, जिसकी आय औसत आय के एक निश्चित अनुपात से कम होती है।
- पूर्ण गरीबी: ऐसी स्थिति जिसमें घरेलू आय बुनियादी जीवन स्तर (भोजन, आश्रय, आवास) को बनाए रखने के लिये आवश्यक स्तर से कम हो। यह स्थिति विभिन्न देशों के बीच और समय के साथ तुलना करना संभव बनाती है।
- भारत में गरीबी का अनुमान
- भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग के टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा एकत्र आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा की गणना के माध्यम से किया जाता है।
- अलघ समिति (1979) ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक वयस्क के लिये क्रमशः 2400 और 2100 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा निर्धारित की।
- इसके बाद विभिन्न समितियाँ; लकड़ावाला समिति (1993), तेंदुलकर समिति (2009), रंगराजन समिति (2012) ने गरीबी का आकलन किया।
- रंगराजन समिति की रिपोर्ट (2014) के अनुसार, गरीबी रेखा का अनुमान शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के रूप में लगाया गया है।
उत्तर प्रदेश Switch to English
ओडीओपी 2.0 नीति
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये ODOP (One District One Product) की एक कार्ययोजना तैयार की है।
- इस योजना को ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और गुणवत्ता सुधार जैसे नए आयामों से जोड़ा जाएगा, जिससे इसकी पहुँच और प्रभावशीलता और भी अधिक बढ़ सके।
मुख्य बिंदु
- योजना के बारे में:
- ओडीओपी योजना को अब राज्यव्यापी स्वरोज़गार, कौशल विकास, और उद्यमिता के रूप में विस्तारित किया जाएगा ।
- वर्ष 2025-26 के लिये विभिन्न श्रेणियों में बजट आवंटन किया गया है, जिससे योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।
- वित्तपोषण, कौशल उन्नयन, और टूलकिट वितरण के लिये अलग से योजना तैयार की गई है।
- पहले चरण के सफल उद्यमियों को अब द्वितीय ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे उनके व्यवसाय को अगले स्तर पर पहुँचाया जा सकेगा।
- हर ज़िले को लक्ष्य दिया जाएगा और वर्ष 2024-25 में लंबित फाइलों को नवीनीकरण कर बैंकों को भेजा जाएगा।
- योजना के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य का 20% स्वीकृति और वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।
- ओडीओपी 2.0 के अंतर्गत वर्तमान योजनाओं का सरलीकरण किया जाएगा और नई परियोजनाओं को मंजूरी दी जाएगी।
- उन्नाव, बिजनौर और गोंडा में निर्माणाधीन सीएफसी (Common Facility Center) परियोजनाओं का संचालन किया जाएगा।
- डिजिटल ई-पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाएगा और उन्हें मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों से जोड़ा जाएगा।
- सेक्टोरल विशेषज्ञों की मदद से ओडीओपी उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
- एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP)
- यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 ज़िलों में लागू किया गया है और इसे न केवल राष्ट्रीय, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना प्राप्त हुई है।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2018 में इस मिशन का शुभारंभ किया गया था।
|
उत्तर प्रदेश में ODOP उत्पादों की सूची |
||
|
क्रमांक |
ज़िला |
उत्पाद |
|
1. |
आगरा |
चमड़ा उत्पाद एवं स्टोन/मार्बल से निर्मित सभी हस्तशिल्प उत्पाद |
|
2. |
अमरोहा |
वाद्य यंत्र (ढोलक) एवं रेडीमेड गारमेंट्स |
|
3. |
बागपत |
होम फर्नीशिंग |
|
4. |
बरेली |
ज़री-ज़रदोज़ी एवं बाँस के उत्पाद/सुनारी उद्योग |
|
5. |
गोरखपुर |
टेराकोटा एवं रेडीमेड गार्मेंट्स |
|
6. |
लखनऊ |
चिकनकारी एवं ज़री ज़रदोज़ी |
|
7. |
महोबा |
गौरा पत्थर |
|
8. |
मिर्ज़ापुर |
कालीन एवं मेटल उद्योग |
|
9. |
सिद्धार्थनगर |
काला नमक चावल |
|
10. |
वाराणसी |
बनारसी रेशम साड़ी |
उत्तर प्रदेश Switch to English
यूपी पुलिस पोर्टल को मिला स्कॉच पुरस्कार
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश पुलिस की तकनीकी सेवा इकाई द्वारा विकसित जाँच, अभियोजन एवं दोषसिद्धि पोर्टल को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
मुख्य बिंदु
- पोर्टल के बारे में:
- यह पुरस्कार पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में दिया गया है।
- जाँच, अभियोजन एवं दोषसिद्धि पोर्टल उत्तर प्रदेश पुलिस की तकनीकी सेवा इकाई द्वारा विकसित किया गया है।
- यह पोर्टल माफिया, पोक्सो (POCSO), बलात्कार और अन्य जघन्य अपराधों से संबंधित मामलों में जाँच प्रक्रिया की निगरानी करता है।
- इसके माध्यम से समय पर चार्जशीट दाखिल करने और न्यायिक प्रक्रिया को तेज़ करने का कार्य किया जाता है।
- अब तक इस पोर्टल के जरिये 85,000 लोगों को दोषसिद्धि घोषित किया गया और 40,000 से अधिक पाँच वर्ष पुराने मामलों का निपटारा किया गया।
- स्कॉच पुरस्कार
- वर्ष 2003 में स्कॉच समूह द्वारा स्थापित किया गया था। यह एक स्वतंत्र नागरिक सम्मान है, जिसे उन व्यक्तियों, परियोजनाओं और संस्थानों को प्रदान किया जाता है, जो भारत के सतत विकास में उल्लेखनीय योगदान देते हैं।
- यह पुरस्कार विशेष रूप से शासन, वित्त, प्रौद्योगिकी और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने के लिये प्रदान किया जाता है।
POCSO अधिनियम:
- परिचय:
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम 14 नवंबर, 2012 को लागू हुआ, जो वर्ष 1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के भारत के अनुसमर्थन के परिणामस्वरूप अधिनियमित किया गया था।
- इस विशेष कानून का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण और यौन उत्पीड़न के अपराधों को संबोधित करना है, जिन्हें या तो विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया या पर्याप्त रूप से दंड का प्रावधान नहीं किया गया है।
- यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है। अधिनियम अपराध की गंभीरता के अनुसार सज़ा का प्रावधान करता है।
- बच्चों के साथ होने वाले ऐसे अपराधों को रोकने के उद्देश्य से बच्चों के यौन शोषण के मामलों में मृत्युदंड सहित अधिक कठोर दंड का प्रावधान करने की दिशा में वर्ष 2019 में अधिनियम की समीक्षा तथा इसमें संशोधन किया गया।
- भारत सरकार ने POCSO नियम, 2020 को भी अधिसूचित कर दिया है।

.jpg)
.jpg)
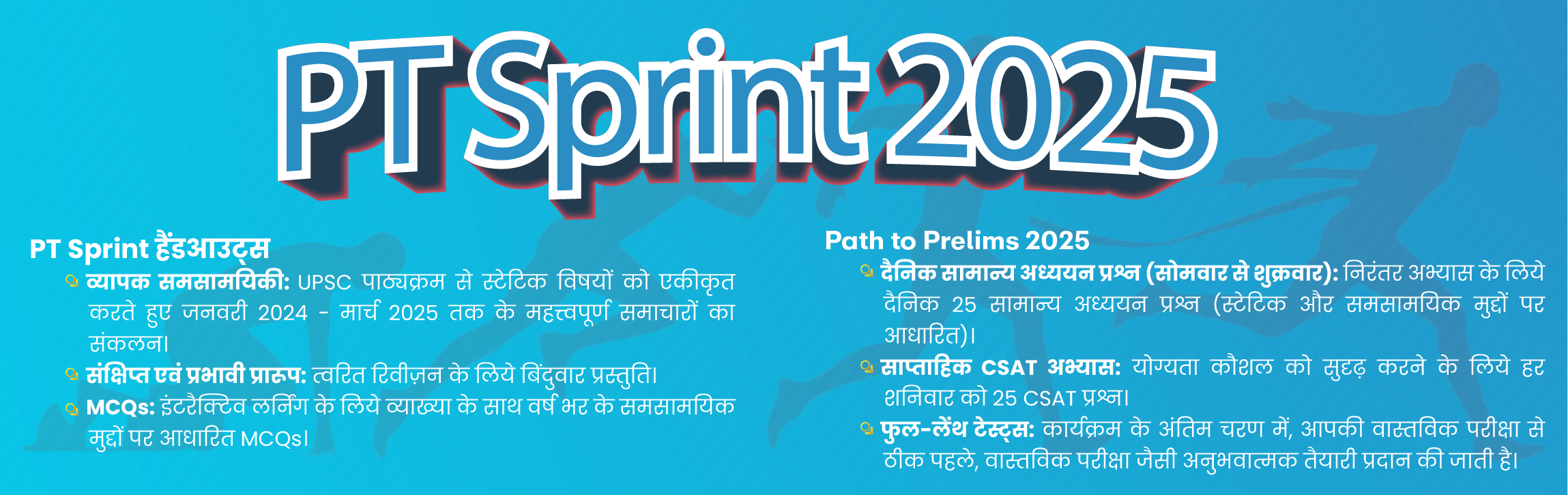
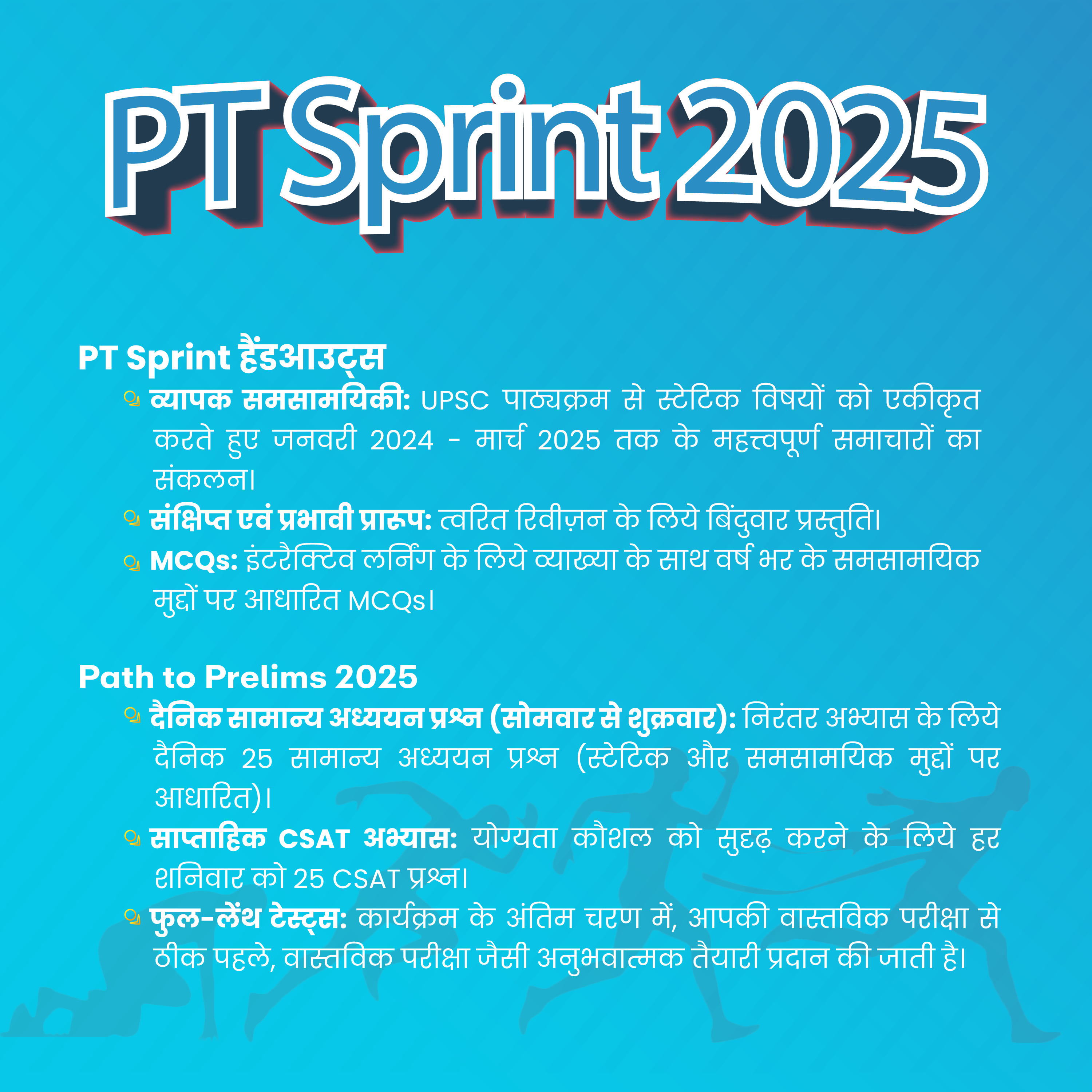
.jpg)


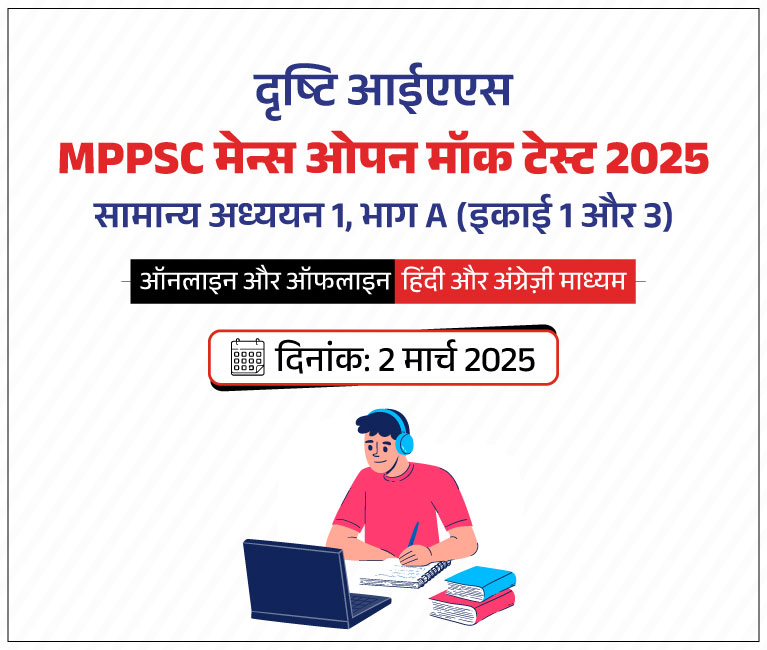
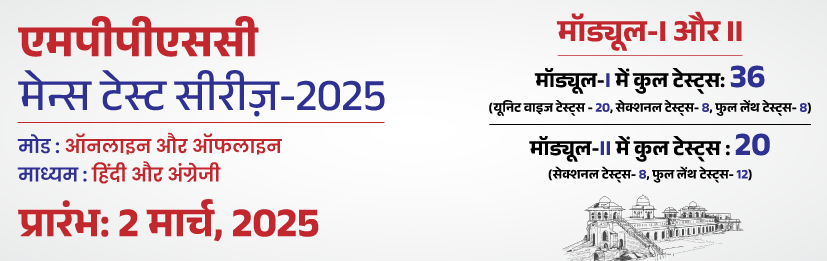

%20MPPCS%202025%20Desktop%20H.jpg)
%20MPPCS%202025%20Mobile%20H%20(1).jpg)