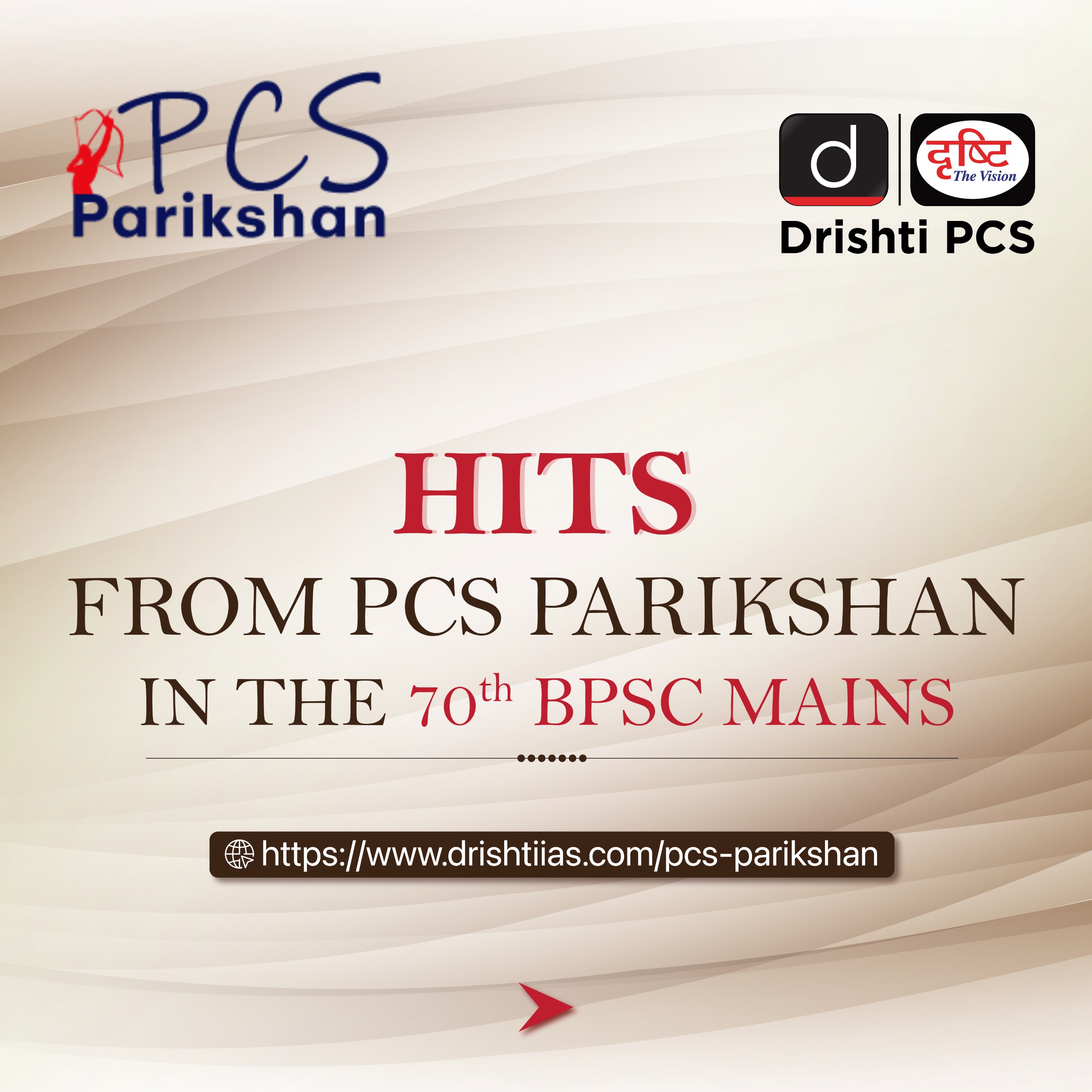भारतीय राजव्यवस्था
चुनाव के संरक्षक निकाय को मज़बूत करना
यह एडिटोरियल 28/11/2022 को ‘इकोनॉमिक टाइम्स’ में प्रकाशित “Is Election Commission becoming a victim of judiciary-government crossfire over appointments?” लेख पर आधारित है। इसमें भारत निर्वाचन आयोग और उससे संबद्ध मुद्दों के बारे में चर्चा की गई है।
भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India- ECI) एक स्वायत्त और स्थायी संवैधानिक निकाय है जो भारत के संघ और राज्यों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराने के लिये उत्तरदायी है।
संविधान भारत निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानमंडलों, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के निर्वाचन के निर्देशन, अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति सौंपता है। ECI राज्यों में शहरी निकायों (जैसे नगर पालिकाओं) और पंचायतों के चुनावों से संबद्ध नहीं है। ECI निकट अतीत में भारत में चुनावों के संरक्षक निकाय के रूप में अपनी स्वतंत्रता और विश्वसनीयता को लेकर, विशेष रूप से मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner- CEC) की नियुक्ति के संबंध में, कई विवादों से प्रभावित रहा है जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
भारत निर्वाचन आयोग का संघटन:
- मूल रूप से आयोग में केवल एक निर्वाचन आयुक्त होता था लेकिन ‘निर्वाचन आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989’ के बाद इसे एक बहु-सदस्यीय निकाय बना दिया गया।
- आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) का होता है।
- उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं।
निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ और ज़िम्मेदारियाँ:
- निर्वाचन के संबंध में आयोग के कार्यों और शक्तियों को तीन श्रेणियों (प्रशासनिक, सलाहकारी एवं अर्द्ध-न्यायिक) में विभाजित किया गया है। इन शक्तियों में शामिल हैं:
- देश भर में निर्वाचन क्षेत्रों की क्षेत्रीय सीमाओं का निर्धारण करना।
- मतदाता सूची तैयार करना और इन्हें समय-समय पर संशोधित करना तथा सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना।
- निर्वाचन के कार्यक्रमों एवं तिथियों को अधिसूचित करना और नामांकन पत्रों की जाँच करना।
- विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना तथा उन्हें निर्वाचन चिह्न आवंटित करना।
- आयोग के पास संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के मामले में सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी है।
- आवश्यकतानुसार किसी निर्वाचन क्षेत्र में उप-चुनाव (Bye-Elections) आयोजित कराने के लिये भी वह ज़िम्मेदार है।
- यह चुनाव के समय राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिये आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct- MCC)लागू करता है ताकि कोई भी अनुचित व्यवहार में लिप्त न हो या सत्ता में बैठे लोगों द्वारा शक्तियों का मनमाना दुरुपयोग न हो।
निर्वाचन आयोग से संबद्ध हाल के मुद्दे:
- CEC का संक्षिप्त कार्यकाल: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में टिप्पणी की कि ‘‘वर्ष 2004 से किसी भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने छह साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है’’ और इस संक्षिप्त कार्यकाल के कारण CEC कोई विशेष भूमिका निभाने में असमर्थ रहा है।
- संविधान में विस्तृत प्रावधान का अभाव: संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान तो करता है, लेकिन इस संबंध में वह केवल इस आशय के एक कानून के अधिनियमन की परिकल्पना करता है और इन नियुक्तियों के लिये कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है।
- नियुक्ति पर कार्यपालिका का प्रभाव: निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति वर्तमान सरकार द्वारा की जाती है और इसलिये वे संभावित रूप से सरकार के प्रति कृतज्ञ होते हैं या उन्हें ऐसा लग सकता कि उन्हें सरकार के प्रति एक विशिष्ट स्तर की निष्ठा का प्रदर्शन करना है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि यद्यपि एक निर्वाचन आयुक्त कुशल, सक्षम, पूर्ण ईमानदार और उत्कृष्ट सेवा रिकॉर्ड से लैस हो सकता है, लेकिन उसका एक व्यक्तिगत राजनीतिक झुकाव भी हो सकता है, जो संस्था की तटस्थता से समझौते की स्थिति बन सकती है।
- इसके साथ ही, संविधान ने सेवानिवृत्त होने वाले निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से संबद्ध किये जाने को अवरुद्ध नहीं किया है, इसलिये वे सरकार से अच्छे संबंध बनाए रखने को प्रवृत्त हो सकते हैं।
- वित्त के लिये केंद्र पर निर्भरता: ECI को एक स्वतंत्र निकाय बनाने के लिये अभिकल्पित विभिन्न प्रावधानों के बावजूद अभी भी इसके वित्त का नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है। निर्वाचन आयोग का व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं रखा गया है।
- स्वतंत्र कर्मचारियों की कमी: चूँकि ECI के पास स्वयं के कार्मचारी नहीं होते, इसलिये जब भी चुनाव आयोजित होते हैं तो उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता है।
- इस परिदृश्य में प्रशासनिक कर्मचारी सामान्य प्रशासन के साथ-साथ चुनावी प्रशासन के लिये भी ज़िम्मेदार होते हैं, जो आयोग की निष्पक्षता और प्रभावशीलता के लिये अनुकूल स्थिति नहीं है।
- आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के लिये सांविधिक समर्थन का अभाव: आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के लिये और निर्वाचन संबंधी अन्य निर्णयों के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के पास उपलब्ध शक्तियों के दायरे एवं प्रकृति के बारे में स्पष्टता नहीं है।
- आंतरिक-पार्टी लोकतंत्र को विनियमित करने की सीमित शक्ति: राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनावों के संबंध में ECI की शक्ति एवं भूमिका सलाह देने तक सीमित है और उसके पास राजनीतिक दल के अंदर लोकतंत्र को लागू करने या उनके वित्त को विनियमित करने का कोई अधिकार नहीं है।
आगे की राह:
- निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की पुनर्कल्पना: न्यायमूर्ति तारकुंडे समिति (1975), दिनेश गोस्वामी समिति (1990), विधि आयोग (2015) जैसी विभिन्न समितियों ने अनुशंसा की है कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सलाह पर की जानी चाहिये जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अनुशंसा की थी ऐसे कॉलेजियम में केंद्रीय विधि मंत्री और राज्यसभा के उपसभापति को भी शामिल किया जाना चाहिये।
- अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2015) मामले में भी ECI के लिये एक कॉलेजियम प्रणाली की आवश्यकता जताई गई थी।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अनुशंसा की थी ऐसे कॉलेजियम में केंद्रीय विधि मंत्री और राज्यसभा के उपसभापति को भी शामिल किया जाना चाहिये।
- आयुक्तों की समकक्षता: कार्यालय से निष्कासन के मामलों में ECI के सभी सदस्यों को समान संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिये। निर्वाचन आयुक्तों की पुनर्नियुक्ति पर अंकुश हो और एक समर्पित निर्वाचन प्रबंधन संवर्ग और कार्मिक प्रणाली का निर्माण किया जाना चाहिये।
- आदर्श आचार संहिता का समर्थन: ECI द्वारा प्रवर्तित आदर्श आचार संहिता के लिये सांविधिक समर्थन प्रदान करना आवश्यक है, विशेष रूप से जब सोशल मीडिया के चुनाव-संबंधी राजनीतिकरण की बात आती है।
- चुनाव सुधार पर विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट: रिपोर्ट में अनुशंसा की गई है कि लोकसभा/राज्यसभा सचिवालय की तरह भारत निर्वाचन आयोग के लिये भी एक स्वतंत्र और स्थायी सचिवालय प्रदान करने के लिये अनुच्छेद 324 में संशोधन किया जाना चाहिये।
- इसके अलावा, राज्य निर्वाचन आयोगों के लिये भी समान प्रावधान करने चाहिये ताकि चुनावों में उनकी स्वायत्तता और निष्पक्षता की भी गारंटी सुनिश्चित हो सके।
अभ्यास प्रश्न: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) भारत में चुनावी लोकतंत्र का आधार है, लेकिन हाल में इसकी संस्थागत विश्वसनीयता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं। टिप्पणी कीजिये।
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs)प्रिलिम्सप्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) मेन्सप्र. आदर्श आचार संहिता के विकास के आलोक में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (2022) |