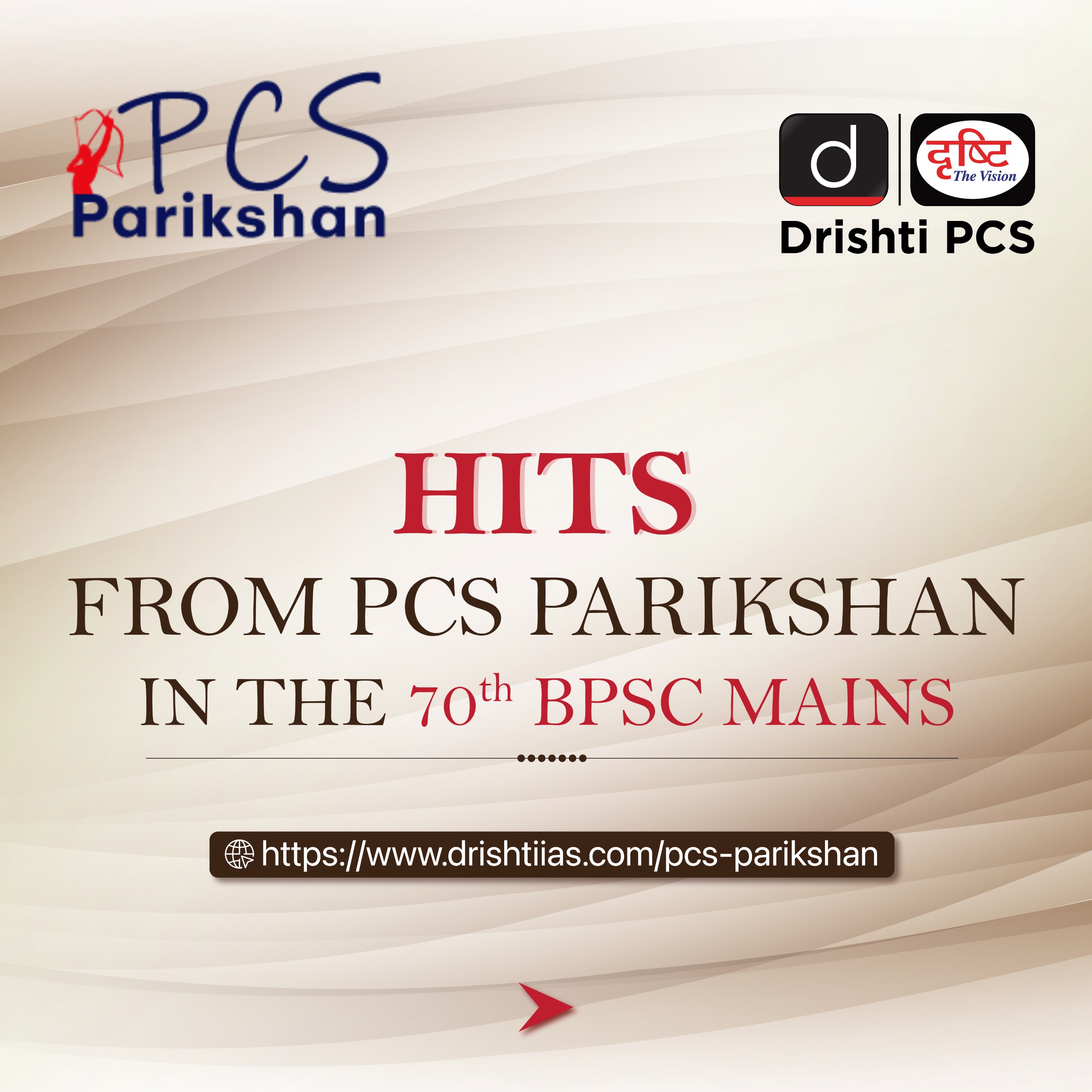अंतर्राष्ट्रीय संबंध
गुटनिरपेक्षता से बहुपक्षीयता की तरफ
यह एडिटोरियल 02/08/2022 को ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ में प्रकाशित “Decoding India’s new multi-alignment plan” लेख पर आधारित है। इसमें गुटनिरपेक्षता से बहुपक्षीयता की ओर भारत के बढ़ते कदम और ‘इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर’ के संबंध में चर्चा की गई है।
संदर्भ
भारतीय स्वतंत्रता के बाद के आरंभिक दो दशकों में जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शीत युद्ध (US-USSR) के गहन प्रभाव में थी और उसकी दशा-दिशा तय कर रही थी, भारत की विदेश नीति वृहत रूप से ‘गुटनिरपेक्षता की नीति’ से प्रेरित थी जो बाद में वर्ष 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non Alignment Movement- NAM) के रूप में एक पूर्ण आंदोलन और विचार मंच बनकर उभरी।
- लेकिन आज भारत गुटनिरपेक्षता के बजाय एक बहुपक्षीयता या बहु-संरेखण (Multi-alignment) की राह पर कुशलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है जहाँ एक ओर वह चीन या रूस के नेतृत्व वाले ब्रिक्स (BRICS) और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का सदस्य है तो दूसरी ओर अमेरिका के नेतृत्व वाले चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (Quad) में जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ शामिल है।
- बहु-संलग्नता की इस व्यवहार्यता को समझने के लिये हमें पहले इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हुए गुटनिरपेक्षता के दृष्टिकोण पर विचार करना होगा।
भारत में गुटनिरपेक्षता का इतिहास
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) का आरंभ औपनिवेशिक व्यवस्था के पतन और अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका एवं विश्व के अन्य क्षेत्रों के लोगों के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ था जब शीत युद्ध भी अपने चरम पर था।
- वर्ष 1960 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के पंद्रहवें साधारण सत्र में गुटनिरपेक्ष देशों के आंदोलन का जन्म हुआ जिसके परिणामस्वरूप 17 नए अफ्रीकी और एशियाई सदस्य देशों को प्रवेश मिला।
- तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ‘गुटनिरपेक्षता’ या शीत युद्ध में संलग्न दो महाशक्तियों से ‘तीसरी दुनिया’ की एकसमान दूरी की अवधारणा को भी बढ़ावा दिया। इन अवधारणाओं पर आगे बढ़ते हुए वर्ष 1955 में ‘बांडुंग सम्मेलन’ (Bandung Conference) का आयोजन किया गया।
- गुटनिरपेक्ष देशों के प्राथमिक उद्देश्य आत्मनिर्णय, राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा राज्यों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन करने तथा बहुपक्षीय सैन्य समझौतों के गैर-अनुपालन पर केंद्रित थे।
- तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ‘गुटनिरपेक्षता’ या शीत युद्ध में संलग्न दो महाशक्तियों से ‘तीसरी दुनिया’ की एकसमान दूरी की अवधारणा को भी बढ़ावा दिया। इन अवधारणाओं पर आगे बढ़ते हुए वर्ष 1955 में ‘बांडुंग सम्मेलन’ (Bandung Conference) का आयोजन किया गया।
- 1980 के दशक के अंत तक पहुँचते समाजवादी ब्लॉक के पतन के साथ इस आंदोलन को वृहत चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। दो विरोधी गुटों के बीच संघर्ष (जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अस्तित्व, नाम और मूल भावना का कारण था) के अंत के साथ ही माना जाने लगा कि अब इस आंदोलन के अंत का आरंभ भी हो चुका है।
भारत का नया बहुपक्षीय दृष्टिकोण क्या है?
- बहु-संरेखण: यह समानांतर संबंधों की एक शृंखला है जो बहुपक्षीय साझेदारी को सुदृढ़ करती है और सुरक्षा, आर्थिक समता और आतंकवाद जैसे अस्तित्वकारी खतरों के उन्मूलन के लिये समूह के बीच एक साझा दृष्टिकोण की तलाश करती है। नीचे कुछ समूहों/मंचों के विवरण हैं जहाँ भारत का बहुपक्षीय या बहु-संरेखीय दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से नज़र आता है:
- इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC): यह 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जिसमें सड़क, रेल और समुद्री मार्ग शामिल हैं। यह सेंट पीटर्सबर्ग (रूस) को मुंबई से जोड़ता है।
- इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत को यूरेशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में रूस, ईरान और मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ सहयोग करने के लिये एक मंच प्रदान करता है।
- INSTC के पूर्णतः कार्यान्वित होने पर स्वेज नहर के डीप-सी मार्ग की तुलना में माल ढुलाई लागत में 30% और यात्रा के समय में 40% की कमी आने की उम्मीद है।
- ब्रिक्स: ब्रिक्स (BRICS) विश्व की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं—ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिये संक्षिप्त शब्द है। यह समूह एक सुनियोजित तंत्र के माध्यम से लोगों के आपसी संपर्क में वृद्धि सहित आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग का लक्ष्य रखता है।
- न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की सह-स्थापना में भारत की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही थी। यह एक नई बहुपक्षीय पहल है जो विश्व बैंक को प्रतिस्पर्द्धा दे सकती है।
- शंघाई सहयोग संगठन (SCO): SCO एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है।
- सदस्यता: कज़ाखस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान।
- ईरान और बेलारूस इसके दो नए सदस्य होंगे।
- SCO के माध्यम से चीन और रूस पश्चिम का, विशेष रूप से नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) के विस्तार का मुक़ाबला करना चाहते हैं।
- सदस्यता: कज़ाखस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान।
- चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (Quadrilateral Security Dialogue- Quad): यह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक संवाद मंच है जो ‘मुक्त, खुले और समृद्ध’ हिंद-प्रशांत क्षेत्र को समर्थन देने और चीन के प्रभाव को नियंत्रित रखने का साझा उद्देश्य रखता है।
- इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC): यह 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जिसमें सड़क, रेल और समुद्री मार्ग शामिल हैं। यह सेंट पीटर्सबर्ग (रूस) को मुंबई से जोड़ता है।
भारत की वर्तमान विदेश नीति
- सम्मान: प्रत्येक देश की संप्रभुता का सम्मान
- संवाद: सभी देशों के साथ वृहत संलग्नता।
- सुरक्षा: भारत एक ज़िम्मेदार शक्ति है, यह आक्रामकता या विदेश नीति में दुस्साहसिकता आजमाने की कोई भावना नहीं रखता है
- समृद्धि: साझा समृद्धि
- संस्कृति और सभ्यता: सांस्कृतिक मूल्यों की प्रेरक अभिगम्यता एक ऐसे दर्शन में निहित है जो ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ में विश्वास करता है।
भारत की विदेश नीति के लिये समकालीन चुनौतियाँ
- रूस-चीन धुरी का उभार: रूस की अपनी परिधि क्षेत्र के मामलों में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा, क्रीमिया के विलय के बाद उस पर लगाए गए प्रतिबंधों ने उसे चीन के साथ घनिष्ठ संबंधों की ओर धकेल दिया है जो निश्चित रूप से भारत में उसकी रुचि को कम कर सकता है।
- भारत का आत्मारोपित अलगाव: वर्तमान में भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) जैसे बहु-देशीय निकायों से अलग-थलग बना हुआ है। इसके अलावा, भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) से बाहर रहने का विकल्प चुना है।
- वैश्विक शक्ति बनने की भारत की महत्वाकांक्षा के साथ यह आत्मारोपित अलगाव (Self-Imposed Isolation) संगत नहीं है।
- पड़ोसी देशों के साथ कमज़ोर होते संबंध: भारतीय विदेश नीति के लिये एक अधिक चिंताजनक विषय पड़ोसी देशों के साथ कमज़ोर होते संबंध हैं। इसे श्रीलंका एवं पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में चीन की ‘चेक बुक डिप्लोमेसी’, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के मुद्दे पर बांग्लादेश के साथ तनाव और नेपाल के साथ सीमा विवाद जैसे उदाहरणों में देखा जा सकता है।
- इस परिदृश्य में भारत देश के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सुरक्षा पर भारी निवेश करने के लिये विवश है।
आगे की राह
- पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करना: भारत को बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधार की दिशा में साहसिक प्रयास करने चाहिये।
- इस संदर्भ में भारत पड़ोसी देशों के प्रति अपनी ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति के तहत ‘वैक्सीन डिप्लोमेसी’ (जिसके तहत वर्ष 2021 में पड़ोसी देशों को मुफ़्त में या मामूली कीमत पर वैक्सीन की आपूर्ति की गई थी) जैसी अन्य कूटनीतिक नीतियों को आगे बढ़ा सकता है।
- भू-राजनीति से परे जाकर देखना: सीमापारीय डिजिटल दिग्गजों की नियामक निगरानी, बिग डेटा प्रबंधन, व्यापार संबंधी मुद्दों और आपदा राहत जैसे विषयों को संबोधित करने के लिये भू-राजनीतिक सीमाओं के पारंपरिक दृष्टिकोण से परे जाकर भारत की विदेश नीति एजेंडे के फोकस का विस्तार करना अनिवार्य है।
- वर्ष 2023 में G20: वर्ष 2023 में G20 की भारत द्वारा अध्यक्षता उसे भू-राजनीतिक हितों के साथ भू-आर्थिक विषयों को संलग्न करने का अवसर देगी। अभी तक भारत ने एक वैश्विक शक्ति बनने की महत्त्वाकांक्षा रखने वाली एक उभरती हुई शक्ति होने की भूमिका निभाई है। वर्ष 2023 का G20 शिखर सम्मेलन भारत को विश्व के लिये महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर स्पष्ट और सक्रिय होने की अनुमति देगा।
निष्कर्ष
- इस प्रकार, एक ऐसा बहु-संरेखीय दृष्टिकोण जो गुटनिरपेक्षता के कुछ प्रमुख मूल्यों को संरक्षित रखता हो, भारत के हितों के और ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ की ओर आगे बढ़ने के उसके दृष्टिकोण के अनुकूल होगा।
अभ्यास प्रश्न: ‘‘भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता से बहुपक्षीयता या बहु-संरेखीय दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित हो रही है।’’ टिप्पणी कीजिये।
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs)प्रश्न 1: भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? (2009) (a) डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन उत्तर: (c) प्रश्न 2: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: (2016)
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) |