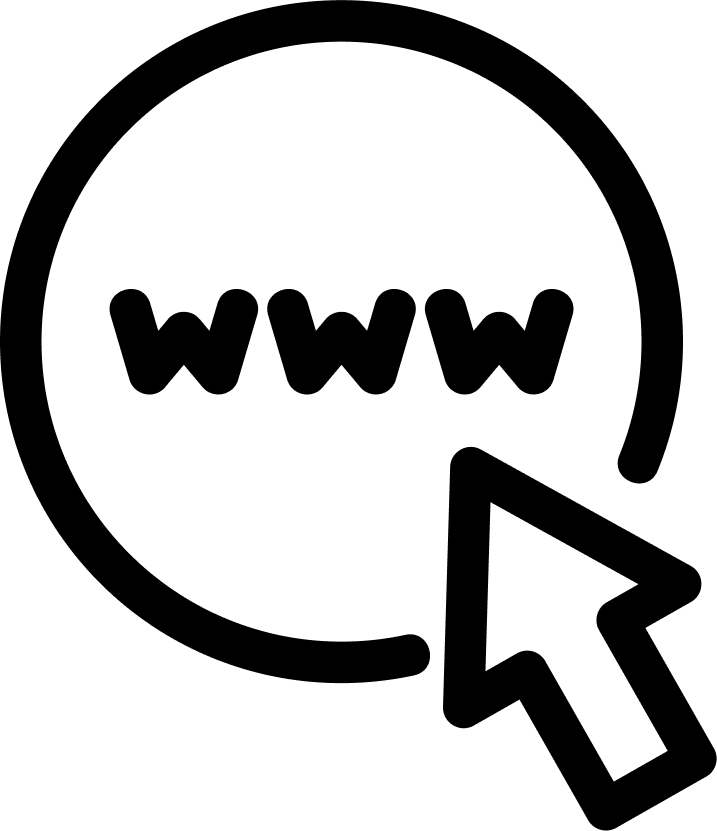सामाजिक न्याय
सामाजिक उपेक्षा मानसिक रोगियों को दोहरा आघात पहुँचाती है!
- 03 Jun 2017
- 11 min read
2007 में आई फिल्म तारे ज़मीन पर एक ऐसे लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है जो डिस्लेक्सिया से ग्रस्त है। उसे पढ़ने-लिखने में समस्याएँ आती हैं लेकिन उसके माता-पिता या अध्यापक उसकी इस बीमारी को समझ नहीं पाते, फलस्वरूप उसके साथ उद्दण्ड बालक की तरह व्यवहार किया जाता है और उसे घर से दूर बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है। वास्तव में इस फिल्म ने समाज में विद्यमान उस गंभीर सामाजिक समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया जिसमें मानसिक रोग से ग्रस्त लोगों के साथ समाज किस प्रकार से जाने-अनजाने में भेदभावपूर्ण और दमनात्मक व्यवहार करता है।
एक मनुष्य के लिये "आरोग्यमं परमं भाग्यं" "स्वास्थयं सर्वाथ साधनम्" जैसे मूल्य विशेष महत्त्व रखते हैं। कोई भी व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की विकृति से ग्रस्त नहीं होना चाहता, बल्कि वह एक स्वस्थ, स्थिर एवं खुशहाल जीवन व्यतीत करना चाहता है, किन्तु यह सभी व्यक्तियों के साथ हमेशा-हमेशा के लिये संभव नहीं हो पाता। कभी-कभी जन्म से इन्सान कुछ अनुवांशिक कारणों से रोगग्रस्त रहता है या कभी कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ जीवन को विचलित कर देती हैं। आज के इस आपाधापी भरे भौतिक जीवन में, जिसमें व्यक्ति चैन शुकून या प्रकृति सहज जीवन से दूर होता जा रहा है, समाज में मानसिक बीमारियों की व्यापकता बढ़ती ही जा ही है। ये मानसिक बीमारियाँ ही हैं जो कभी-कभी इतना गंभीर रूप ले लेती हैं कि इन्सान आत्महत्या जैसी दुष्प्रवृत्तियों तक का शिकार हो जाता है, वास्तव में यह आत्महत्या भी स्वयं में एक मानसिक रोग है।
इसी प्रकार फिर चाहे मंदबुद्धि जैसी स्थिति हो या सिज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक बिमारी हो, मानसिक रोग स्वयं में ही रोगी को गहरा आघात पहुँचाते हैं, उसके खुशहाल जीवन में विष घोलने का काम करते हैं। इसीलिये मानव समाज का यह सामुदायिक दायित्व बनता है कि वह इस प्रकार से ग्रस्त लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति रखे, प्रेमपूर्वक व्यवहार करे, साथ ही गरिमापूर्ण जीवन जीने में यथाशक्ति योगदान देता रहे। लेकिन जब समाज अपने दायित्वों से विमुख होकर, मानसिक रोगियों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार करता है तो यह न केवल मानसिक रोगियों को दोहरा आघात पहुँचाता है, बल्कि उनके गरिमापूर्ण जीवन के संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार का भी दमन करता है।
समानता एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार वास्तव में व्यक्ति का नैसिर्गक अधिकार है जिसे लोकतांत्रिक शासन पद्धति में मूल अधिकार के रूप में संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता) एवं अनुच्छेद 21 (गरमिापूर्ण जीवन) के रूप में परिभाषित किया गया है।
अब मूल प्रश्न यह है कि सिर्फ इसलिये कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की मानसिक बीमारी से ग्रस्त है जैसे पागलपन या उसमें सोचने-समझने, विचार करने की उतनी सामर्थ्य नहीं है जितनी सामान्य लोगों में होती है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उसके साथ दोयम दर्ज़े का व्यवहार किया जाए और उसके समानता के अधिकार का हनन किया जाए; यह मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इस प्रकार का उपेक्षापूर्ण व्यवहार समाज के प्रत्येक स्तर पर देखा जा सकता है। खुद उसके अपने परिवार में ही उसके साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाता है, उसे समझने एवं मदद करने की बजाय उद्दण्ड मानकर उसकी उपेक्षा या तिरिस्कार करने की प्रवृत्ति रोगी पर अतिरिक्त दबाव डालती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर जितने अधिकार एक स्वस्थ एवं सामान्य मनुष्य के हैं, उतने ही उतने ही उसके क्यों नहीं? फिर बात चाहे सिनेमा की हो या मीडिया की, कला की हो या साहित्य की; कही पर भी समानता का नामों निशान नज़र नहीं आता।
अगर सिनेमा की बात करें तो खामोशी, तारे ज़मीन पर और गुज़ारिश जैसी चंद फिल्में ही बनी हैं जिनमें इस विषय पर रोशनी डालने की कोशिश की गई है। समाज में आदिकाल से व्याप्त एक गंभीर समस्या पर, समाज को सोचने और अपने भेदभाव पूर्ण व्यवहार को बदलने के लिये विवश कर देने जैसी एक गंभीर किस्म की सिनेमाई प्रस्तुती की आवश्यकता है, क्योंकि सिनेमा की पहुँच की व्यापकता ही दर्शक मन पर गंभीर एवं स्थिर प्रभाव के इस कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकती है। बिल्कुल यही बात हमारी मीडिया के संदर्भ में भी लागू होती है। तालठोंक हल्ला-बोल जैसे ना जाने क्या-क्या उत्तेजक और अनुपयोगी विषयों के साथ व्यर्थ की चर्चा करते मीडिया जगत का ध्यान कभी भी गंभीरता पूर्वक समाज के इस वंचित वर्ग की ओर नहीं गया।
यदि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया ऐसे मानिसक रोग ग्रस्त लोगों की समस्याओं संवेदनशील ढंग से उठाएँ, उस पर चर्चा करें; समाज को, सिविल सोसाईटी को, राजनीतिक सत्ता से जुड़े लोगों को, विधिवेत्ताओं, शिक्षक, चिकित्सक, स्थानीय प्रशासन से जुड़े लोगों को एक गंभीर संदेश दें; उन्हें इस चर्चा में भागीदार बनाएँ और इन सभी व्यवस्थाओं को वंचित वर्ग के कल्याण के प्रति ध्यान आकृष्ट करने के लिये प्रेरित करें तो निश्चित की समाज का उपेक्षावादी रवैया कमज़ोर होगा और संवेदनशीलता में वृद्धि होगी।
समाज की यह संवदेनशीलता ही वास्तव में मानसिक रोगी की रामबाण औषधि है। समाज में हमारे समक्ष अनेक ऐसे उदाहरण गुज़रते हैं जिनमें निःशक्त व्यक्ति भी अपनों के प्रोत्साहन से सफलता की बुलंदियों को छू लेता है। इसलिये आवश्यकता है तो इस उपेक्षित किन्तु महत्त्वपूर्ण मसले को आम मीडिया द्वारा प्रमुखता से रखने की।
शिक्षा और साहित्य जैसे दो आधारभूत स्तंभ भी इसी पहल का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि आज की शिक्षा व्यवस्था में ऐसी विषयवस्तु एवं पाठ्य संरचना का सर्वत्र अभाव है जिससे व्यक्ति में स्वयं ही निराशा-अवसाद जैसे मानसिक विकारों से लड़ने के सामर्थ्य का विकास संभव हो।
साथ-ही-साथ, इस बात की भी नितांत कमी नज़र आती है कि बचपन से ही बच्चों को किस प्रकार से विशिष्ट मानसिक रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता का पाठ पढ़ाया जाए? शिक्षा व्यवस्था में इस तत्त्व की कमी ने समाज में सामाजिक उपेक्षावादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया है, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस आभाव ने ऐसे समाज के निर्माण को प्रोत्साहित किया है जो मानसिक व्याधि ग्रस्त वंचित वर्ग को समाज का हिस्सा मानने को तैयार ही नहीं है, वे इन्हें इसी अवहेलना का अधिकारी मानते हैं।
वास्तव में शिक्षा ही इस विकराल समस्या के समाधान में रामबाण सिद्ध हो सकती है। यही वह माध्यम है जो इस वंचित वर्ग के कल्याण की बात को साहित्य में स्थान दिलाएगा और बौद्धिक जगत में इस अपवंचना को विर्मश का केन्द्र बनाकर इनका समाधान सुझाने को प्रेरित करेगा।
भारतीय समाज में तो गांधी, बुद्ध, महावीर, विवेकानंद जैसे अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने नर सेवा को ही नारायण सेवा मानकर, इसे अपने जीवन में उतारकर, सामाजिक उपेक्षा के शिकार लोगों को प्रोत्साहित किया है। भारतीय संविधान के भाग-3 और 4 में इनके कल्याण की बात स्वीकार कर एक प्रजातांत्रिक और समानतावादी समाज निर्माण की बात की गई हैं। इसी के तहत 1987 में मानसिक स्वास्थ अधिनियम भी बनाया गया, जिसमें हाल में ही संशोधन के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि इसे और सशक्त बनाया जा सके। इसी तरह, मूल कर्तव्यों में भी लोगों से अपेक्षा की गई है कि वे सभी नागरिकों की समानता का सम्मान करें।
मानसिक व्याधियों से ग्रस्त लोगों की समस्याओं का दीर्घकालिक एवं बहुआयामी समाधान जनसहभागिता के माध्यम से ही संभव है। समाज के विभिन्न वर्गों को यह समझना होगा कि विकृतिग्रस्त कुछ लोगों से सहानुभूति एवं प्रेम एक ऐसे समाज के निर्माण की बुनियाद होगी जहाँ कोई व्यक्ति अवसाद की वजह से आत्महत्या की ओर प्रेरित नहीं होगा, साथ ही इससे सामाजिक समरसता की स्थापना में भी मदद मिलेगी क्योंकि मानसिक रोगी भी आखिर है तो इन्सान ही; इस संदर्भ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की कुछ पंक्तियाँ बेहद उपयुक्त प्रतीत होती हैं-
"सब स्वच्छंद यहाँ पर जन्में और मृत्यु सब पाएंगे,
फिर यह कैसा बंधन जिसमें मानव पशु से हो जाएँगे।"