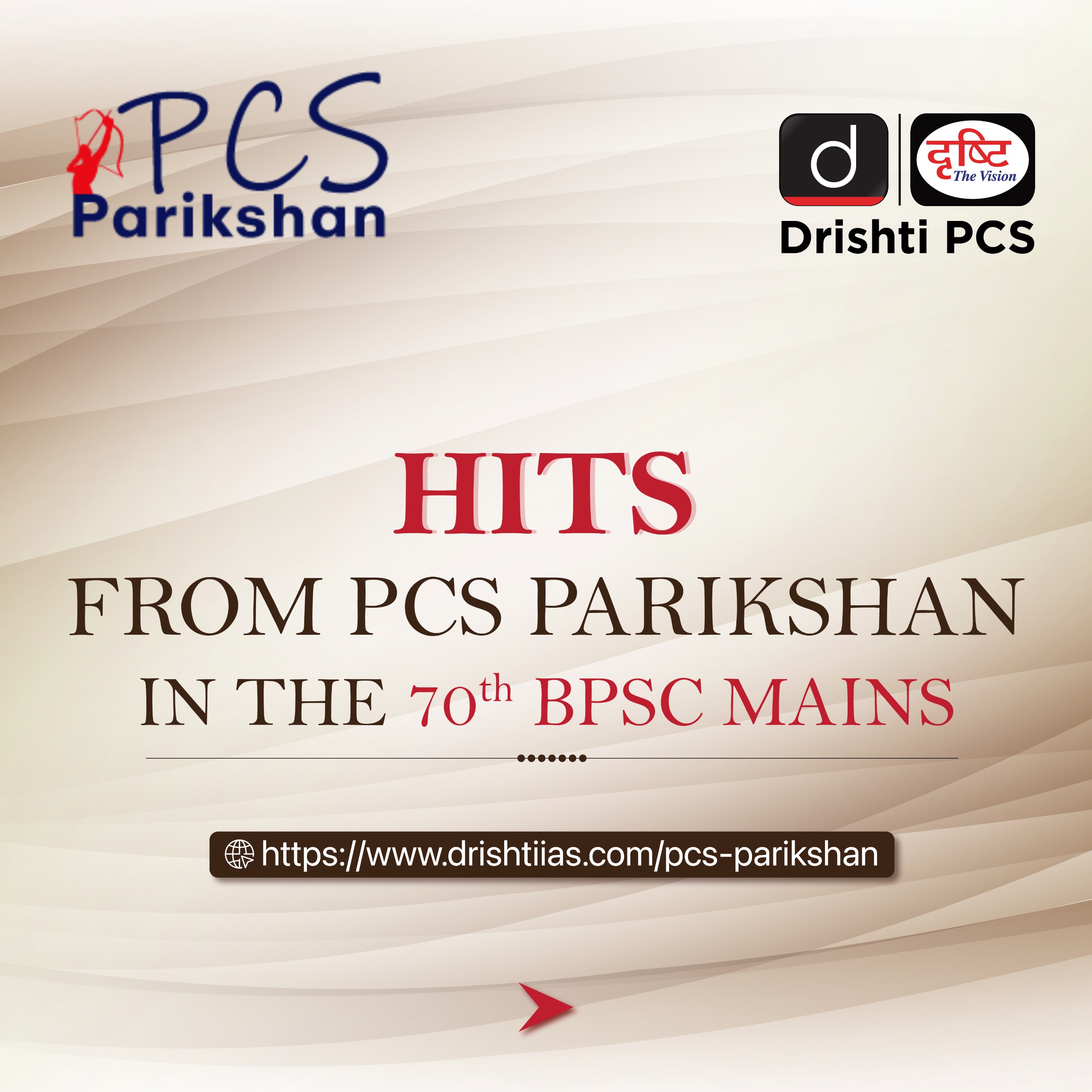सामाजिक न्याय
अंबेडकर और पूना समझौता
इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण किया गया है। इस लेख में अंबेडकर और पूना समझौते से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। आवश्यकतानुसार, यथास्थान टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल किये गए हैं।
संदर्भ
प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को पूरे देश में स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख उन्नायक, शिल्पकार और स्वतंत्र भारत के प्रमुख संविधान निर्माता डा. भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती का हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया जाता है।
इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य भारत के युवाओं को उन विचारों से अवगत करना है जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को संविधान रूपी नींव पर स्थापित किया। डा. अंबेडकर का योगदान केवल संविधान निर्माण तक ही नहीं सीमित था बल्कि सामाजिक व राजनैतिक स्तर पर भी उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। समाज में निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को सामाजिक स्तर पर बराबरी का दर्जा दिलाया तो वहीँ राजनैतिक स्तर पर दलितों, शोषितों व महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्रदान करने हेतु विधि का निर्माण कर उसे संहिताबद्ध किया।
कुछ विद्वानों का ऐसा मानना था कि महात्मा गांधी व अंबेडकर की विचारधारा सर्वथा एक-दूसरे से भिन्न थी, परंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है। भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी के प्रशंसक ही नहीं बल्कि अनुगामी भी थे। निश्चित ही दोनों के बीच कुछ विषयों पर मतभेद थे परंतु उनका उद्देश्य मानव मात्र का कल्याण करना ही था। इसका एक ज्वलंत उदाहरण छुआछूत के विषय में देखा जा सकता है- छुआछूत के विषय पर दोनों का ही मानना था कि यह समाज में एक कोढ़ की भांति है, परंतु दोनों ही विद्वान छुआछूत को दूर करने के भिन्न-भिन्न मार्ग के समर्थक थे।
इस आलेख में डा. भीमराव रामजी अंबेडकर के सामाजिक, राजनीतिक व जातिगत विचारों पर अध्ययन करने के साथ ही आधुनिक भारत के निर्माण में उनकी भूमिका और महात्मा गाँधी के साथ उनके विचारों की भिन्नता व वैचारिक मतैक्यता पर भी विमर्श किया जाएगा।
पृष्ठभूमि
- भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रांत (वर्तमान मध्यप्रदेश) के महू नामक तहसील में हुआ था।
- डा. अंबेडकर के पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे जबकि इनकी माता भीमाबाई सकपाल एक गृहिणी थी।
- इनका जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। छुआछूत के विषय ने अंबेडकर के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला।
- अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा बॉम्बे के एल्फिंस्टन स्कूल से हुई। इसके बाद बॉम्बे विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की तत्पश्चात उच्चतर शिक्षा कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्राप्त की।
- डा. अंबेडकर जीवन भर दलितों व शोषितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे। वे ऐसा समतामूलक समाज स्थापित करना चाहते थे जिसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव का कोई स्थान न हो। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में बाबासाहेब भीमराव रामजी अंबेडकर ने अंतिम सांस ली।
छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष
- डा. अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध संगठित प्रयास करते हुए वर्ष 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही अछूत वर्ग के कल्याण की दिशा में कार्य करना था।
- दलित अधिकारों की रक्षा के लिये उन्होंने मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी प्रभावशाली पत्रिकाएँ निकालीं।
- द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध के दौरान 1 जनवरी 1818 को हुई भीमा कोरेगाँव की लड़ाई के दौरान मारे गये भारतीय महार सैनिकों के सम्मान में अंबेडकर ने 1 जनवरी 1927 को कोरेगाँव विजय स्मारक पर एक समारोह आयोजित किया। यहाँ महार समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर खुदवाये गये तथा कोरेगाँव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया गया।
- वर्ष 1927 में डॉ॰ अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरम्भ करने का निर्णय किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जलूसों के द्वारा, पेयजल के सार्वजनिक स्रोत समाज के सभी वर्गों के लिये खुलवाने के साथ ही अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिये संघर्ष किया।
- 20 मार्च 1927 को डॉ॰ अंबेडकर की अगुवाई में महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड नामक स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीने और उस पानी का उपयोग करने का अधिकार दिलाने के लिये एक सत्याग्रह किया गया, जिसे महाड सत्याग्रह के नाम से जाना गया।
- 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने हजारों अनुयायियों के साथ मिलकर मनुस्मृति की प्रतियों को जला दिया।
असमानता दूर करने के लिये अंबेडकर के सुझाव
- राजनीतिक प्रतिनिधित्व- डॉ. अंबेडकर मानते थे कि समाज के विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों का सरकार के विभिन्न अंगों में प्रतिनिधित्व होना चाहिये। उनके अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों को अपना प्रतिनिधित्व ख़ुद करना चाहिये क्योंकि सिर्फ़ ‘मुद्दे का रखा जाना’ मायने नहीं रखता बल्कि उस मुद्दे का प्रतिनिधित्व स्वयं करना मायने रखता है।
- सहकारी खेती- स्वतंत्रता के पहले भारत की ज़्यादातर आबादी ग्रामीण थी, जहाँ आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि थी। परंतु कृषि की ज़मीनों पर ज़मींदारों और कुछ उच्च जातियों का क़ब्ज़ा था। शेष ज़्यादातर जातियाँ भूमिहीन थीं और मज़दूरी का कार्य करती थीं। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करके भूमि सुधार लागू कर सहकारी खेती कराए जाने का वचन दिया परंतु राजनीतिक कारणों से स्वतंत्रता के बाद इसे लागू नहीं किया जा सका।
- सेपरेट सेटलमेंट- स्वतंत्रता से पूर्व गाँव की व्यवस्था जजमानी प्रथा से चलती थी, जिसमें एक जाति दूसरी जाति पर निर्भर होती थी। इस निर्भरता की वजह से ही सवर्ण जातियाँ दलित जातियों का विभिन्न प्रकार से शोषण करती थी। इस तरह के शोषण से निकलने के लिये ही अंबेडकर ने सेपरेट सेटलमेंट की मांग की।
- पे-बैक टू सोसायटी- अंबेडकर सरकार की सीमाओं से परिचित थे , जिसकी वजह से ही उन्होंने अपने समाज के नौकरीपेशा लोगों से कहा था कि शोषितों और वंचितों को ऊपर उठाने के लिये वे आर्थिक रूप से मदद करें, जिसे पे-बैक टू सोसायटी कहा गया।
पूना समझौता
24 सितंबर 1932 को डॉ॰ अंबेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता किया गया। इसे पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार-
- दलित वर्ग के लिये पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदू वर्ग के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गये।
- प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिये 147 सीटें आवंटित की गई जबकि सांप्रदायिक पंचाट में उन्हें 71 सीटें प्रदान करने का वचन दिया गया था।
- मद्रास में 30, बंगाल में 30 मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में 20-20, बिहार एवं उड़ीसा में 18 बम्बई एवं सिंध में 15, पंजाब में 8 तथा असम में 7 स्थान दलितों के लिये सुरक्षित किये गए।
- साथ ही यह वादा भी किया गया कि गैर-मुस्लिमों निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित सीटों का एक निश्चित प्रतिशत दलित वर्गों के लिये आरक्षित कर दिया जाएगा।
- केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिये संयुक्त निर्वाचन की प्रक्रिया तथा प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने की व्यवस्था को मान्यता दी गई।
- दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई।
- कांग्रेस ने स्वीकार किया कि दलित वर्गों को प्रशासनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा।
- अंबेडकर के नेतृत्व में दलित वर्गों ने संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया।
- वंचित वर्गों के लिये केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों में मताधिकार लोथियन समिति की रिपोर्ट में निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा।
- केंद्रीय विधानमंडल में, ब्रिटिश भारत के सामान्य निर्वाचक वर्ग के लिये प्रदत्त 18 प्रतिशत सीटें दलित वर्गों के लिये आरक्षित होंगी।
- किसी को भी स्थानीय निकाय के किसी चुनाव या लोक सेवाओं में नियुक्ति के संदर्भ में मात्र दलित वर्ग से संबद्ध होने के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।
पूना समझौते का दलितों पर प्रभाव
- पूना समझौते ने दलितों को राजनीतिक हथियार बना दिया। संयुक्त निर्वाचन में वास्तविक दलितों को हराकर हिंदू जाति के संगठनों का एजेंट बना दिया और केवल उन दलितों की चुनावी जीत को पक्का किया जो इन संगठनों के एजेंट या हथियार थे।
- पूना समझौते ने दलितों के राजनीतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक अवनयन को बढ़ावा दिया और इस प्रकार ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था से लड़ने वाले दलितों के वास्तविक एवं स्वतंत्र नेतृत्व को बर्बाद कर दिया।
- इसने हिंदू से पृथक एवं अलग दलित अस्तित्व को स्वीकार न करके उसे हिंदू सामाजिक व्यवस्था के एक हिस्से के रूप में रखा।
- इस समझौते ने समानता-स्वतंत्रता-बंधुत्व-न्याय पर आधारित ‘आदर्श समाज’ के सामने बाधा खड़ी की।
- दलित वर्ग को एक पृथक एवं भिन्न तत्व न मानकर इसने दलित एवं अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं सुरक्षा संबंधी रक्षोपायों को भारत के संविधान में स्पष्ट करने से रोक दिया।
- सांप्रदायिक निर्णय द्वारा भारतीयों को विभाजित करने तथा पूना समझौते के द्वारा हिंदुओं से दलितों को पृथक करने की व्यवस्थाओं ने गांधी जी को आहत कर दिया। गांधी जी ने पूना समझौते के प्रावधानों को पूरी तरह पालन किये जाने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के उद्देश्य से गांधी जी ने अन्य कार्यों को छोड़कर पूर्णरूपेण ‘अश्पृश्यता निवारण अभियान’ में जुट गए।
वर्ण-व्यवस्था पर गांधी व अंबेडकर के मतभेद
गांधी और अंबेडकर दोनों तात्कालिक सामाजिक स्थितियों व परिवेश से असंतुष्ट थे। दोनों समाज का नव निर्माण करना चाहते थे, परंतु इस संदर्भ में समस्या के कारण, स्वरुप व निदान के प्रति दोनों का दृष्टिकोण एवं कार्य-पद्धति अलग-अलग थी।
- गांधी जी वर्ण-व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि वर्ण-व्यवस्था समाज के लिये उपयोगी है, इससे श्रम-विभाजन एवं विशेषीकरण को बढ़ावा मिलता है। वहीँ अंबेडकर वर्ण-व्यवस्था के कट्टर आलोचक थे। अंबेडकर के अनुसार, वर्ण-व्यवस्था अवैज्ञानिक, अमानवीय, अलोकतांत्रिक, अनैतिक, अन्यायपूर्ण एवं शोषणकारी सामाजिक योजना है।
- गांधी जी का मानना था कि छुआछूत का वर्ण-व्यवस्था से सीधा संबंध नहीं है। छुआछूत वर्ण-व्यवस्था की अनिवार्य विकृति न होकर वाह्य विकृति है, अतः छुआछूत समाप्त करने हेतु वर्ण-व्यवस्था में रचनात्मक सुधार की आवश्यकता है। वहीँ अंबेडकर के अनुसार, अश्पृश्यता या छुआछूत वर्ण-व्यवस्था का अनिवार्य परिणाम है। अतः बिना वर्ण-व्यवस्था का उन्मूलन किये छुआछूत को दूर नहीं किया जा सकता है।
- गांधी जी छुआछूत को दूर करने के लिये आदर्शवादी व दीर्घकालिक उपायों की बात करते थे जबकि अंबेडकर छुआछूत को दूर करने के लिये व्यावहारिक, त्वरित एवं ठोस उपायों पर बल देते थे।
- गांधी जी ने सवर्ण हिंदुओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन कर अछूतों के प्रति भेदभाव को दूर करने के प्रयासों के हिमायती थे वहीँ अंबेडकर यह मानते थे कि हिंदू धर्म के अंतर्गत अछूतों का उद्धार नहीं हो सकता अतः धर्मान्तरण द्वारा ही दलितों का उद्धार संभव है।
- गांधी जी के अनुसार हिंदू धर्मशास्त्र अश्पृश्यता का समर्थन नहीं करते जबकि अंबेडकर का मानना था कि हिंदू धर्मशास्त्र में ही अश्पृश्यता के बीज विद्यमान हैं।
प्रश्न- पूना समझौते के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए वर्ण-व्यवस्था पर गांधी व अंबेडकर के मतभेदों का वर्णन कीजिये।