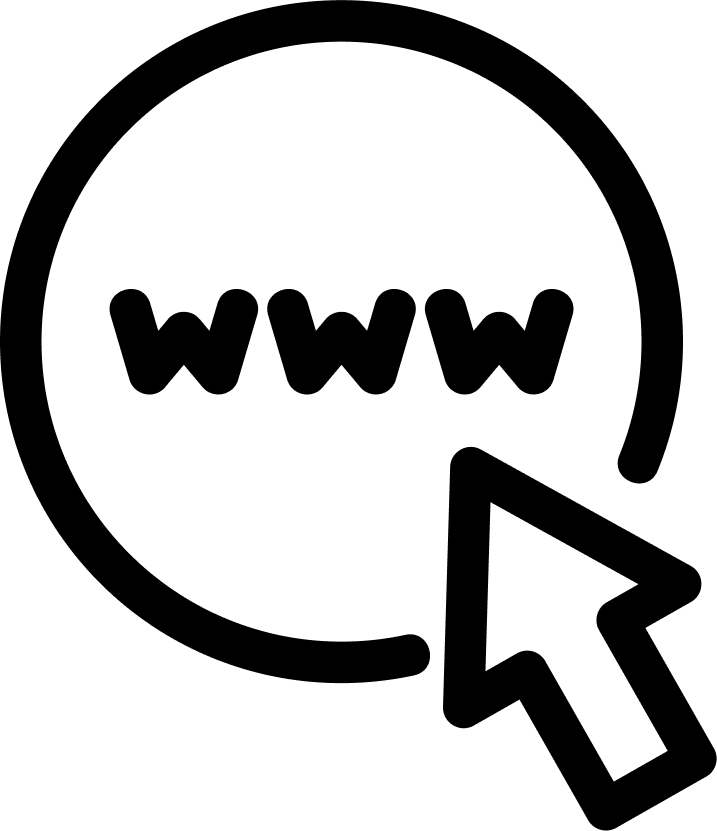शक्ति का केंद्र कौन: अमेरिका या चीन?
- 01 Aug, 2024 | रहीस सिंह
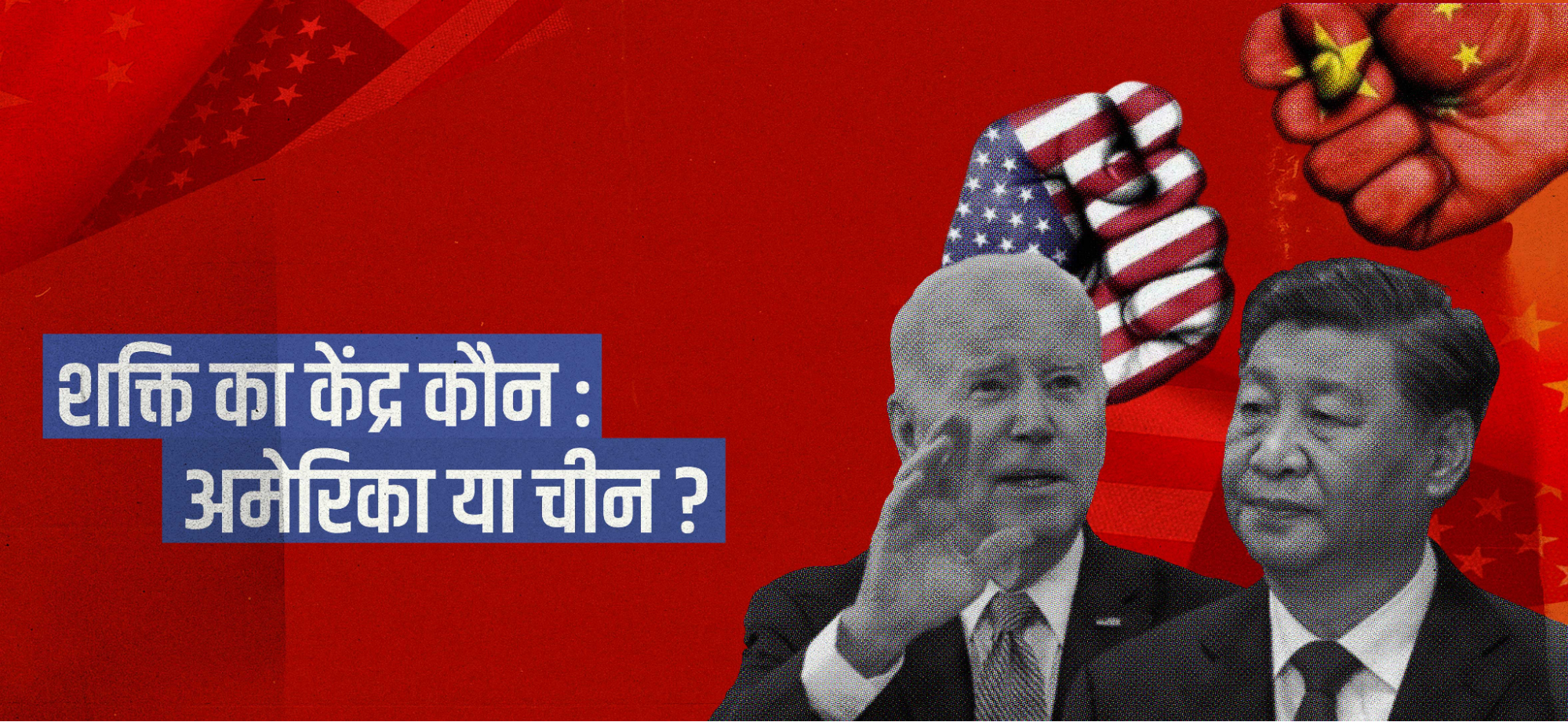
अमेरिका के राजनीतिक अर्थशास्त्री लेस्टर थोरो ने अपनी पुस्तक ‘दि फ्यूचर ऑफ कैपिटलिज़्म’ में लिखा है कि विश्व व्यापार व्यवस्था के नियम-कायदे हमेशा वर्चस्वशील अर्थव्यवस्थाओं ने तय किये हैं और लागू कराए हैं। 19वीं सदी में ग्रेट ब्रिटेन ने यह भूमिका निभायी और 20वीं सदी में संयुक्त राज्य अमेरिका ने। परंतु 21वीं सदी में आर्थिक प्रबंधन के नियम-कायदों की रूपरेखा बनाने, संगठित करने और उन्हें लागू कराने वाली कोई भी वर्चस्वपूर्ण शक्ति नहीं रहेगी। उन्होंने यह भी कहा था कि अमेरिका के प्रभाव में संचालित एकध्रुवीय व्यवस्था के दिन लद चुके हैं और एक बहुध्रुवीय संसार उभर कर विश्व रंगमंच पर आ चुका है। उनकी यह बात कितनी सही है, इस पर अध्ययन किया जा रहा है। निष्कर्ष भी आएंगे लेकिन जो बदलाव दिख रहे हैं, वे इस ओर इशारा करते हैं कि अमेरिका अब दुनिया का नेता नहीं रह गया। दूसरा यह कि अमेरिकी खेमे के देश बहुत हद तक अब चीन की ओर देख रहे हैं। तीसरा, अमेरिका जितना अकेला पड़ता जा रहा है उतना ही अधिक चीन दुनिया के देशों को आकर्षित करने में सफल हो रहा है। ऐसे में एक सवाल यह उठता है कि इस बदलाव को किस तरह से देखा जाए? दूसरा यह कि अभी कुछ समय पहले तक ट्रस्ट डेफिसिट के शिकार बताए जा रहे चीन के चक्कर फ्रांस, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, इज़रायल सहित दुनिया के तमाम देशों के नेता क्यों काट रहे हैं? इनकी वाशिंगटन से बढ़ती दूरियों और बीज़िंग से बढ़ती निकटता के निहितार्थ क्या हैं? यह अमेरिकी नेतृत्व की अनिश्चितता और शी जिनपिंग के शक्तिशाली होने का संकेत है अथवा अमेरिकी जियो-पॉलिटिक्स पर भारी पड़ती चीनी जियो-पॉलिटिक्स का परिणाम या इससे भी कुछ अलग? ऐसे में भारत के हिस्से में अवसर आएंगे अथवा नए प्रकार के दायित्व, यह भी विचार करने योग्य पक्ष है।
विश्वव्यवथा में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अभी इस निष्कर्ष तक पहुँच जाना शायद जल्दबाज़ी होगी कि इसका नेतृत्व कौन करेगा-वाशिंगटन, बीज़िंग अथवा कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच? हालाँकि, इस परिवर्तन की शुरुआत सही अर्थों में वर्ष 2008 से ही हो गई थी जब अमेरिका में लीमैन ब्रदर्स का पतन हुआ था और अमेरिका एक ऐसे वित्तीय संकट से गुज़रा जिसका प्रभाव अभी तक खत्म नहीं हो पाया है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लगे इस धक्के का प्रभाव इतना अधिक था कि इसके बाद के वर्षों में पूरा यूरोप आर्थिक संकट की चपेट में आ गया। इसने यह दर्शाया कि विश्व बैंक के अर्थशास्त्रियों की तरफ से जो घोषणा की गयी थी, वह पूरी तरह से सही नहीं थी। ध्यातव्य है कि इससे पहले विश्व बैंक के अर्थशास्त्रियों ने घोषणा की थी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अब ‘डि-कपल’ हो चुकी है। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी एक अर्थव्यवस्था को झटके लगने से अन्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इससे दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाएँ प्रभावित हुईं और अभी भी हो रही हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिये यह एक टर्निंग प्वाइंट सिद्ध हुआ। यही वह टर्निंग प्वाइंट था जिसने एक क्षण में यह सुनिश्चित कर दिया था कि अमेरिका अब विश्व शक्ति (वर्ल्ड पॉवर) अथवा सेंटर ऑफ ग्लोबल पावर (विश्व शक्ति का केंद्र) नहीं रहा। इसने यह भी संकेत दे दिया था कि विश्व में शक्ति के अन्य केंद्र उभर चुके हैं जो अकेले अथवा संगठित होकर भविष्य में दुनिया का सामूहिक नेतृत्व कर सकते हैं। यहीं से चीन की एक नई यात्रा आरंभ हुई थी और भारत ने भी एक नया इतिहास लिखने की कोशिश शुरू की।
वर्ष 2008 से वर्ष 2023 के बीच वैश्विक राजनीति में कई प्रकार के उतार-चढ़ाव आए, जिनमें कभी लगा कि अमेरिका अभी भी चुनौतीविहीन है, अत: उसकी जगह दुनिया की कोई दूसरी ताकत नहीं ले सकती, परंतु कभी यह लगा कि अमेरिका शक्ति का प्रदर्शन बेहद रणनीतिक तरीके से कर रहा है ताकि उसकी साख और ज़मीन बची रहे। कभी ऐसा भी प्रतीत हुआ कि चीन आक्रामकता के साथ अमेरिका को पीछे धकेलने की कोशिश में कामयाब हो रहा है। उसकी आर्थिक संस्थाएँ तथा वैश्विक पहलें और मध्य-पूर्व व यूरेशिया की उभरती परिस्थितियों में उसकी भूमिका ने उसकी योग्यता और प्रभाव को प्रमाणित भी किया। हालाँकि, चीन की अर्थव्यवस्था में भी बुलबुलों का प्रभाव है और वह लोकतंत्र की बजाय तानाशाही पर चल रहा है जिसमें आक्रामकता है तथा दूसरे देशों की संप्रभुताओं के प्रति अनादर का भाव है। वह शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को भी स्वीकार नहीं कर पा रहा है, इसलिये दुनिया के देश उसके साथ लंबे समय तक अपने आपको सहज रख पाएंगे, ऐसा अनुमान करना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल अमेरिका की तुलना में चीन को रणनीतिक बढ़त हासिल करते हुए देखा जा सकता है। ऐसा इसलिये कहा जा सकता है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के उदय का एक कारण मानकर चीन को कठघरे में खड़ा किया जाता रहा है। वायरस जनित इस वैश्विक महामारी ने दुनिया को बुरी तरह से प्रभावित किया और संपूर्ण मानवता को संकट में डाल दिया। इससे व्यापक पैमाने पर मानव हानि हुई और अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं। इस वायरस के उद्गम को लेकर निकाले गए कुछ निष्कर्ष चीन की वुहान वायरोलॉजी लैब तक पहुँच गए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसे ‘वुहान वायरस’ का नाम भी दे दिया। इसके बाद कुछ समय के लिये ऐसा लगा कि चीन विश्वास के संकट (ट्रस्ट डेफिसिट) का शिकार हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप वह विश्व बाज़ार में अपनी साख खो देगा। यदि ऐसा हुआ तो उसके लिये दुनिया के बाज़ार संकुचित होंगे और निर्यात घटेंगे जिससे उसकी अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी। अर्थव्यवस्था के धराशायी होते ही चीन की सैन्य और कूटनीतिक शक्ति के प्रभावित होने की संभावनाएँ बढ़ेंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि छोटे-छोटे झटके लगने के बाद स्थितियाँ इसके ठीक उलट दिखने लगीं। आज जिस तरह से दुनिया के तमाम देशों के राजनीतिक प्रतिनिधि बीज़िंग के चक्कर लगाते हुए दिख रहे हैं, उससे कुछ समय के लिये ही सही परंतु ऐसा लगने लगा है कि दुनिया अब अमेरिका की तरफ नहीं बल्कि चीन की ओर देख रही है। क्या वास्तव में ऐसा ही है? क्या वास्तव में चीन विश्व राजनीति के केंद्र में आ चुका है?
वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को करीब से देखें तो इसमें दो विशेषताएँ दिखेंगी, पहली यह कि इसमें अनिश्चितता का तत्त्व अधिक है और दूसरी यह कि अब वैश्विक शक्ति के केंद्र में केवल अमेरिका नहीं है। यद्यपि दुनिया दो ध्रुवों में अभी भी नहीं बँटी है क्योंकि वर्तमान वैश्विक नेतृत्व में नई दिल्ली, मॉस्को, लंदन, पेरिस, बर्लिन, टोक्यो, कैनबरा आदि की किसी भी स्तर पर अनदेखी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जी-20 से लेकर जी-7, क्वाड, शंघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स, आसियान, जैसे संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की गतिशीलता के साथ-साथ दशा और दिशा भी सुनिश्चित करते हैं। हाँ, वाशिंगटन, बीज़िंग और मॉस्को के बीच बनते-बिगड़ते समीकरण, संतुलन (इक्विलिब्रियम) दुनिया को अपेक्षाकृत थोड़ा अधिक प्रभावित कर रहे हैं जबकि नई दिल्ली, टोक्यो, कैनबरा आदि की भूमिका शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ-साथ शांतिपूर्ण विकास में कहीं अधिक निर्णायक साबित हो रही है। विगत कुछ वर्षों को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि बीज़िंग-मास्को बॉण्डिंग अधिक मज़बूत हुई है। यही कारण है कि पश्चिमी दुनिया की लीडरशिप अथवा उसके थिंक टैंक्स भले ही मॉस्को को महत्त्व न दें, लेकिन बीज़िंग-मॉस्को को कहीं अधिक प्रभाव वाली बॉण्डिंग के रूप में देख रहे हैं। इसकी तुलना में वाशिंगटन अपेक्षाकृत एकाकी पड़ता दिख रहा है। ऐसा क्यों है? आखिर इसकी वजह क्या है कि अमेरिका के मित्र देश ही नहीं बल्कि स्वयं अमेरिका कभी-कभी बीज़िंग की तरफ देखता हुआ प्रतीत होता है? इसके प्रमाण के तौर पर एंटनी ब्लिंकन की चीन यात्रा को ले सकते हैं। उससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की बीज़िंग यात्रा संपन्न हुई, यूरोपीय कमीशन के चेयरमैन ने भी चीन की यात्रा की। चीन की मध्यस्थता द्वारा ईरान और सऊदी अरब का निकट आना, यह भी एक करिश्माई उदाहरण हो सकता है।
अब तक जिन तथ्यों को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जा रहा था उनके अनुसार सऊदी अरब सुन्नी दुनिया (सुन्नी वर्ल्ड) का नेतृत्व करने का दावा कर रहा था और ईरान शिया दुनिया (शीते वर्ल्ड) का। सामान्यतया यह माना जा रहा था कि इन दोनों के बीच मित्रता संभव नहीं है क्योंकि ये दोनों विपरीत ध्रुव हैं, लेकिन चीन ने इसे मिथक साबित कर दिया। सवाल यह उठता है कि ऐसा कैसे संभव हुआ? क्या यह मान लिया जाए कि पिछले एक दशक में इस क्षेत्र को ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में अमेरिका की कूटनीतिक अनिश्चितता चीन के लिये मार्ग प्रशस्त होने का कारण है। अब यदि मध्य-पूर्व में चीनी पैठ सुनिश्चित हो चुकी है तो फिर अमेरिका के लिये क्या कोई क्षेत्र बचा है अथवा नहीं? या फिर अमेरिका का रणनीतिक रुख फिलहाल मध्य-पूर्व से यूरेशिया की तरफ हो चुका है? लेकिन यदि यह वास्तव में अमेरिकी डिप्लोमैटिक शिफ्ट है तो क्या यह अमेरिका के लिये लाभदायक साबित होगा, विशेषकर उस परिस्थिति में जब यूरोपीय देश डिप्लोमैटिक ही नहीं इकोनॉमिक डेफिसिट का शिकार हो रहे हैं। उसका एक कारण तो अमेरिका ही है। यदि अमेरिका और उसके सहयोगी, रूस पर आर्थिक प्रतिबंध न थोपते तो यूरोपीय जनता और अर्थव्यवस्था को शायद मुश्किलों का सामना करना नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा हुआ। इसके लिये सबसे अधिक दोषी अमेरिका ही है।
पहले इस्लामी देशों को देखें, जो शीतयुद्ध के दौर से ही या तो अमेरिकी खेमे में चले गए थे अथवा उनका अमेरिका की तरफ झुकाव था। अब ये देश इधर चीन की ओर झुकाव प्रदर्शित करते दिख रहे हैं जबकि चीन ‘हुई’ और ‘उइगर’ समुदाय के खिलाफ मुहिम चला रहा है। पिछली कुछ घटनाएँ अथवा पहलें चीन और इस्लामी दुनिया के बीच नज़दीकियाँ बढ़ाती दिख रही हैं। ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ इस्लामी कोऑपरेशन (ओआईसी) की बैठक में न केवल चीन को आमंत्रित किया गया बल्कि चीन के प्रति समर्थन भी व्यक्त किया गया, जिसे लेकर विदेश मंत्री वांग ई ने संयुक्त राष्ट्र में चीन का समर्थन करने को लेकर इस्लामी दुनिया का शुक्रिया अदा किया था। ऐसा इसलिये हुआ कि इस्लामी दुनिया स्वयं ऐसे मूल्यों के साथ व्यवस्थाओं का संचालन कर रही है जो आधुनिक विश्व का प्रतिनिधित्व नहीं करते। दूसरे शब्दों में कहें तो इस्लामी दुनिया को भी चीन की तरह लोकतंत्र से डर लगता है। वे नहीं चाहते कि उनके देशों को या उन्हें लोकतंत्र की कोई हवा लगे और अरब स्प्रिंग जैसी पुनरावृत्ति से उन्हें दो-चार करना पड़ जाए। तो क्या ये देश और इनका राजनीतिक नेतृत्व अपने अस्तित्व पर फिर से एक संकट गहराता हुआ देखे, ठीक उसी प्रकार जैसे ट्यूनीशिया में बेन अली को दिखा था, मिस्र में होस्नी मुबारक के समक्ष आया था और लीबिया में गद्दाफी के सामने। सभी जानते हैं कि उनके इतिहास का अंत कैसा था। इसका मतलब यह हुआ कि अर्दोगान से लेकर मोहम्मद बिन सलमान तक और शहबाज से लेकर अयातुल्लाह खमैनी तक कोई भी यह नहीं चाहता, अरब स्प्रिंग जैसी किसी घटना से इनका सामना हो।
यह भी हो सकता है कि चीन ने जो ऋण जाल बिछाया है यह उसका असर हो। जैसा कि ओआईसी की बैठक में चीनी विदेश मंत्री वांग ई ने वादा किया था कि बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (बीआरआई) के तहत चीन मुस्लिम देशों में 400 अरब डॉलर का निवेश करेगा। निवेश की इतनी बड़ी धनराशि उनमें चीनी प्रेम पैदा करने के लिये फिलहाल पर्याप्त है। शायद यह भी कारण है कि इस्लामी दुनिया चीन में मसीहाई देखने लगी। फिर चीन चाहे शिंजियांग में अलगाववाद और चरमपंथ के नाम पर उइगरों का खात्मा करे अथवा युआन प्रांत में ‘हुई’ लोगों का, इस्लामी दुनिया पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिये और पड़ भी नहीं रहा। दरअसल, यह बात उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है जितनी यह कि ये सभी देश अमेरिकी खेमे के देश थे जो अब चीन के साथ खड़े दिख रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? संभवत: यह कि उन्हें चीन में अपना भविष्य दिख रहा है और अमेरिका के साथ खड़े होने पर अनिश्चितता अथवा विश्वासघात; अथवा इसका कारण कुछ और है। पाकिस्तान, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, मलेशिया, तुर्की, कतर, मिस्र और अफगानिस्तान जैसे देशों में उइगर मुसलमानों को गिरफ्तार कर पुन: चीन भेजने के पीछे का वास्तविक पक्ष क्या है? क्या इसका यह अनुमान लगाया जा सकता है कि चीन इतना ताकतवर हो चुका है कि इस्लामी दुनिया चीन से डरने लगी है अथवा यह कि इन्हें बीज़िंग पसंद आ रहा है और आगे का रास्ता ये उसके साथ चलकर तय करना चाहते हैं? फिलहाल ये दोनों ही कारण पर्याप्त नज़र नहीं आते। इसके पीछे दो वजहें हो सकती हैं; इनमें पहली है-चीन की ऋण कूटनीति (डेट डिप्लोमैसी) दरअसल, चीन पिछले कुछ वर्षों से खुले ऋण की खिड़की (विश्व बैंक को इसी नाम से जाना जाता रहा है) की तरह कार्य कर रहा है। हालाँकि, इसके पीछे उसकी मंशा उदारता की नहीं है बल्कि वह इन देशों की अर्थव्यवस्था अथवा उनके कुछ घटकों को अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना चाहता है। यही नहीं चीन बहुत से देशों को अपने ऋण जाल में फँसाने में कामयाब भी हो चुका है तथा दूसरा कारण है- ऊर्जा कूटनीति। उल्लेखनीय है कि चीन ऊर्जा की मांग के लिये सबसे बड़ा बाज़ार है। ऐसे में चीन से अलग जाना इस्लामी दुनिया के उन देशों के लिये संभव नहीं है जो तेल उत्पादक हैं।
अब अमेरिका की बात करें जो दिखावे के लिये चीन से कई मोर्चे पर युद्ध लड़ रहा है लेकिन द्विपक्षीय व्यापार पर उतनी तीव्र कैंची चलती हुई नहीं दिखी, जैसा कि इन युद्धों का परिणाम होना चाहिये था। आखिर वाशिंगटन-बीज़िंग के इस लव-हेट गेम का निहितार्थ क्या है? वैसे तो अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा है जो पहले मुद्रा युद्ध (करेंसी वॉर) के रूप में चला था, लेकिन अब व्यापार युद्ध (ट्रेड वॉर) के रूप में चल रहा है, लेकिन असल में महाशक्तियाँ कभी आपस में लड़ीं नहीं बल्कि केवल दुनिया को गुमराह ही किया। इसलिये इन दोनों के मामले में भी परदे के पीछे क्या है, यह एक कौतूहल है। अमेरिका ने पिछले कुछ वर्षों में चीन पर आंशिक रूप से प्रतिबंध भी लगाए और व्यापार युद्ध की शुरुआत की, लेकिन चीन ने उसके समक्ष घुटने नहीं टेके। यही नहीं, अमेरिका ने वुहान वायरस थियरी भी चलाई लेकिन चीन फिर भी नहीं झुका। हाँ, कुछ आरंभिक झटके उसे अवश्य लगे लेकिन बाद में ‘न्यू नॉर्मल’ प्रभाव के तहत उसने संतुलन साध लिया और फिर परंपरागत रास्ते पर चल पड़ा। यहाँ तक कि यूरोप के कई देश अपने कूटनीतिक व राजनीतिक प्रतिनिधियों और राष्ट्राध्यक्षों को बीज़िंग भेजकर एक नया इतिहास लिखने की तैयारी में रहे। शायद इसे ही देखते हुए अमेरिका ने भी अपने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को भी चीन भेजने का निर्णय लिया। उल्लेखनीय है कि जिस समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका-यात्रा शुरू हो रही थी, उसी समय अमेरिकी विदेश मंत्री का बीज़िंग दौरा संपन्न हो रहा था। क्या ब्लिंकन का यह दौरा अमेरिका के ऊपर चीन के जासूसी बैलून वाले विवाद का पटाक्षेप करने के लिये हुआ अथवा उस दरार को पाटने के लिये जो पिछले कई वर्षों से अमेरिका और चीन के रिश्तों में पड़ी दिख रही है और निरंतर गहरी होती जा रही है। दुनिया के कुछ थिंक टैंक्स भले ही यह तर्क गढ़ रहे हों कि ब्लिंकन की यह यात्रा दो महाशक्तियों के बीच बिगड़ते संबंधों से दुनिया भर में पैदा हो रही चिंताओं से प्रेरित थी, लेकिन सच यह नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर ब्लिंकन के चीन से लौटते ही राष्ट्रपति बाइडन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह कदापि न कहते। इसका मतलब तो यही हुआ कि ब्लिंकन के दौरे से भी कुछ बात नहीं बनी। यही नहीं, ब्लिंकन की इस यात्रा को रणनीतिक चूक के लिये उत्तरदायी मानना चाहिये, क्योंकि वे इस यात्रा के दौरान ‘वन चाइना पॉलिसी’ के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता को फिर से दुहरा कर चले आए, जबकि अमेरिका ताइवान के साथ खड़े होने का दिखावा कर रहा है। इससे अमेरिका के प्रति दुनिया का विश्वास कमज़ोर होगा, विशेषकर उन देशों का जो चीनी आक्रामकता के विरुद्ध संरक्षण पाने के लिये अमेरिका की ओर देख रहे हैं।
हालाँकि, इस बीच यह तर्क अवश्य दिया जा सकता है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और चीन दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है और चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 700 अरब डॉलर का है और दोनों की ही अर्थव्यवस्था बहुत हद तक एक दूसरे से जुड़ी हुई है अथवा अन्योन्याश्रित है, इसलिये उनके बीच बेहतर संबंधों का होना वैश्विक अर्थव्यवस्था के हित में है। लेकिन यह बात पूरी तरह से सही नहीं है।
बहरहाल, चीन तथा अमेरिका के संबंधों की पृष्ठभूमि में जाएँ तो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन वर्ष 1972 में चीन गए थे। इनसे ठीक पहले वर्ष 1971 के जुलाई में तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने चीन की एक गुप्त यात्रा की थी। किसिंजर की यह यात्रा बेहद महत्त्वपूर्ण थी, क्योंकि इसके ठीक बाद संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना’ को मान्यता दे दी गई थी। यानी, चीन ने वैश्विक स्तर पर विधिक हैसियत (लेजिटीमेसी) प्राप्त कर ली थी। इसके बाद ही अमेरिका और चीन के बीच ऐतिहासिक संबंधों का नया अध्याय शुरू हुआ था। अब ब्लिंकन की बीज़िंग की वो यात्रा किस तरह का अध्याय शुरू करेगी और उन देशों को क्या संदेश देगी जो चीन की आक्रामकता का शिकार हैं और अमेरिका की तरफ एक आशा से देख रहे हैं, इसका जवाब शायद अमेरिका के पास नहीं होगा। यह अमेरिका के प्रति भरोसा कम होने का एक बड़ा कारण है। ऐसे दौर में भारत को भी थोड़ा और सक्रिय व सशक्त होकर विश्वव्यवस्था के निर्माण के लिये आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी।
लेखक अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं।