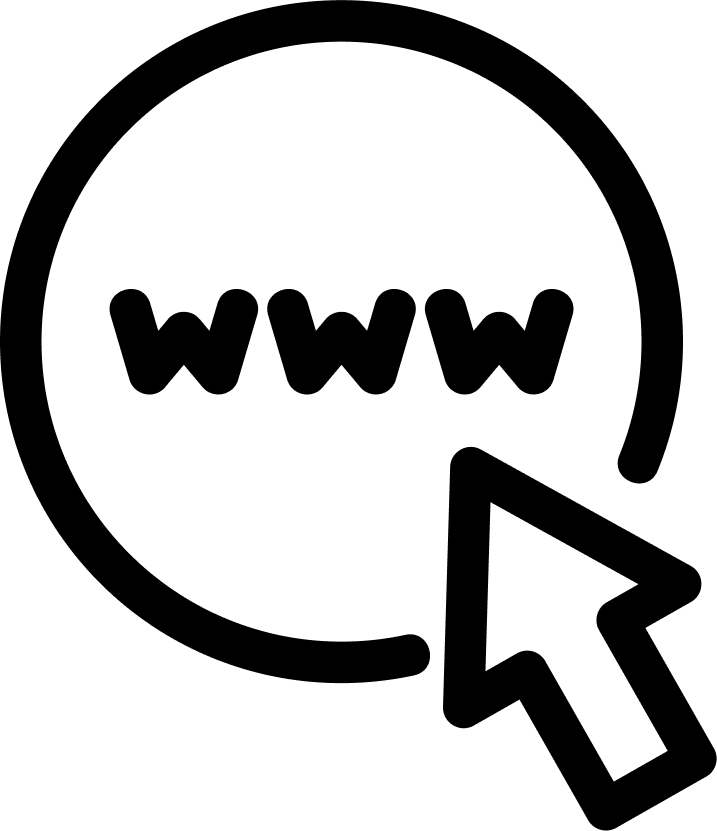विश्वव्यवस्था को किधर ले जा रहे नाटो-मॉस्को-बीजिंग!
- 20 Aug, 2024 | रहीस सिंह
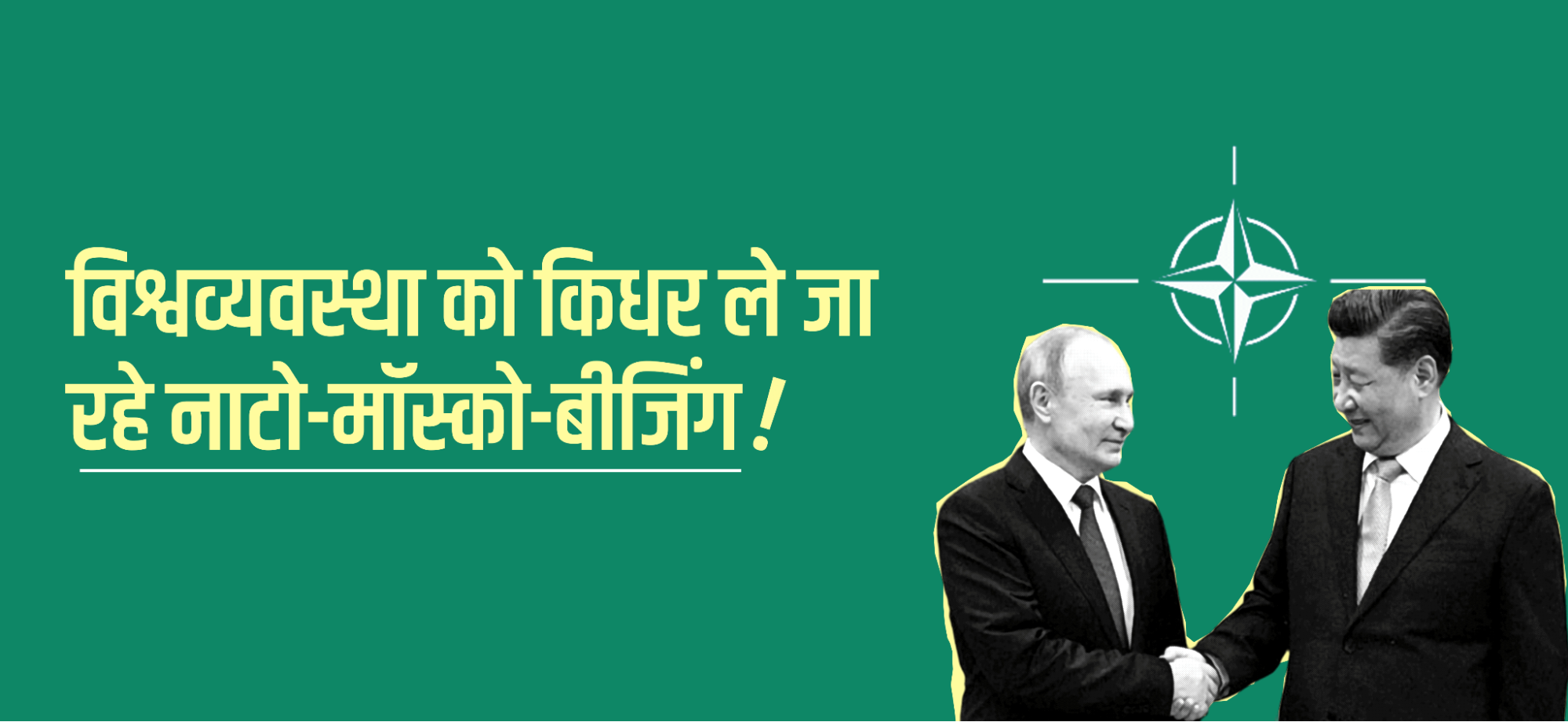
पिछले वर्ष अप्रैल के पहले सप्ताह में नार्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइज़ेशन यानी नाटो में 31वें सदस्य देश के रूप में फिनलैंड को शामिल किया गया। कुछ ही समय बाद स्वीडन भी संगठन का 32वां सदस्य देश बना। फिनलैंड को शामिल करने की वास्तविक वजह उसकी 1340 किलोमीटर की सीमा रेखा का रूस से लगा होना है। उसके बाद से नाटो इसे अपनी विजय के रूप में देखने और पेश करने की कोशिश कर रहा। उसे लगता है कि इससे रूस के साथ चल रहे यूक्रेन युद्ध में उसे रणनीतिक लाभांश (Strategic Dividend) हासिल हो जाएगा क्योंकि फिनलैंड के नाटो में शामिल हो जाने के बाद नाटो की रूस के साथ साझा सीमा की लंबाई दो गुनी हो गई। रूस के यूक्रेन के प्रति नज़रिये को देखते समय नाटो की मंशा को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिये है कि यूरेशिया तथा पूर्वी यूरोप के संदर्भ में बात होते समय रूस की क्रीमिया से लेकर कीव तक पर कार्रवाई की चर्चा तो होती है लेकिन नाटो की रणनीति को कमोबेश छोड़ दिया जाता है अथवा उसे सही मानकर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। विश्वव्यवस्था के किसी भी पक्ष के आकलन का यह तरीका उचित नहीं है, हालाँकि अपनाया यही जाता रहा है। इस संदर्भ में कुछ प्रश्न यहाँ पर महत्त्वपूर्ण प्रतीत होते हैं जिसका विश्लेषण करना आवश्यक है। पहला- क्या नाटो सही राह पर चल रहा है? दूसरा- आज यदि दुनिया शीतयुद्ध के जैसे वातावरण को फिर से महसूस कर रही है या संघर्षों के नए दौर को देख रही है तो इसके लिये दोषी कौन है? क्या ऐसा नहीं लगता कि दुनिया को बार-बार नए शीतयुद्ध के मुहाने तक खींचकर लाने का काम नाटो ही करता है? कारण यह है कि नाटो की उत्पत्ति शीतयुद्धयुगीन है इसलिये उसके रहने तक शीतयुद्ध के अवशेषों का बने रहना भी स्वाभाविक है। तीसरा- क्या नाटो वैचारिक तथा नीतियों की दृष्टि से और पारस्परिक लाभ की दृष्टि से एकता की कसौटी पर खरा उतर पा रहा है या उसकी तथाकथित एकजुटता सिर्फ रूस के खिलाफ ही दिख रही है? अंतिम प्रश्न यह है कि क्या नाटो चीन के मामले में भी ऐसी ही एकजुटता का परिचय दे पा रहा है?
इस संपूर्ण घटनाक्रम का बारीकी से विश्लेषण करें तो यही स्पष्ट होता है कि फिनलैंड को लेकर नाटो जो संदेश देना चाहता था, वह दे नहीं पाया। उलटे सदस्य देश उलझन में दिखे। उनकी यह उलझन बताती है कि उनके सभी सदस्य देश किसी एक बिंदु पर सहमत नहीं हैं। इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला उदहारण- जर्मन विदेश मंत्री की ताइवान यात्रा संबंधी रही। दूसरा उदाहरण- फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों और यूरोपियन कमीशन के चेयरपर्सन की बीजिंग यात्रा का और तीसरा उदाहरण फ्रांस में चीनी राजदूत का दिया गया वह बयान है जिसमें उसने क्रीमिया को रूस का ऐतिहासिक हिस्सा माना, न कि यूक्रेन का। उल्लेखनीय है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने अपनी बीजिंग यात्रा के दौरान यूरोप को चीन-ताइवान के मुद्दे से दूर रहने की सलाह दी थी। मैक्रों का यह संदेश यूरोपीय कमीशन के निर्णय से भिन्न था और जर्मन पहल के विपरीत भी। इससे कुछ तो संदेश जाता ही है। संदेश यही कि चीन-ताइवान पर न केवल जर्मनी और फ्रांस की दिशाएँ अलग-अलग हैं बल्कि यूरोपीय एकता भी प्रतीकात्मक मात्र नज़र आ रही है। ऐसे में नाटो में फिनलैंड के शामिल होने के जश्न के मायने क्या होने चाहिये, यह भी स्पष्ट नहीं रहा। इसमें यदि चीन के राजदूत का पेरिस में दिया हुआ बयान जोड़ दिया जाए तो यूरोप की एकता का सिद्धांत पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। पेरिस में चीन के राजदूत लू शाये ने एक न्यूज़ चैनल द्वारा क्रीमिया पर पूछे गए सवाल के उत्तर में कहा कि ऐतिहासिक रूप से क्रीमिया रूस का हिस्सा था और सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव ने इसे यूक्रेन को दे दिया था।
रूस ने वर्ष 2014 में इसे यूक्रेन से छीन लिया और बाद में उसका विलय कर लिया। चीनी राजदूत ने यह भी कहा कि सोवियत संघ के पतन के बाद उभरे देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे देशों के लिये संप्रभु राष्ट्र के तौर पर उनकी स्थिति की पुष्टि करने वाला कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं है। अब नाटो देश बताएँ कि वे चीन के साथ अभी भी संबंध बहाल रखना चाहेंगे या फिर अपने आपको अलग कर लेंगे? अथवा कोई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेंगे?
इस दिशा में आगे बढ़ने से पहले यह विचार बार-बार आता है कि क्या यूरोपीय एकता के मानदंड देश और क्षेत्र सापेक्ष हैं? उसके उद्देश्य और उसकी मंशा भी अलग-अलग हैं अर्थात् किसी छोटे देश के लिये अलग, रूस के लिये कुछ और अलग तथा चीन के लिये पूरी तरह से भिन्न। यह एक प्रश्न अब तक शेष है। यही कि बर्लिन की दीवार के गिरने और सोवियत संघ के बिखर जाने के पश्चात वैश्वीकरण के नाम पर अमेरिकी नेतृत्व में बाज़ारवादी पूंजीवाद के थोपे जाने के बाद भी क्या नाटो की प्रासंगिकता शेष थी? क्या नाटो के बने रहने तक शीतयुद्ध को पूरी तरह से समाप्त माना जाना तकनीकी रूप से उचित था? यदि नहीं तो फिर नाटो बना क्यों रहा? यह वही नाटो समूह है जो सोवियत संघ के पतन के बाद ‘इतिहास के अंत’ का प्रचार-प्रसार कर रहा था। इससे उसकी मंशा का साफ पता लग जाता है कि इसका उद्देश्य एकध्रुवीय विश्व का निर्माण था। हालाँकि एकध्रुवीय विश्व का सपना अब सपना ही रह गया है। कारण यह कि नाटो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे विश्व उसे स्वाभाविक नेता या सुरक्षात्मक ढाल के रूप में स्वीकार कर ले। इसका शोर कुछ विशेष अवसरों पर ही सुनाई दिया और इसकी कार्रवाइयाँ कुछ खास देशों के लिये कुछ चुने हुए देशों के खिलाफ ही संपन्न हुईं।
रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच नाटो का शोर भी सुनाई देता रहता है। इसका बारीक विश्लेषण यह है कि वास्तविक युद्ध तो नाटो और रूस के बीच ही हो रहा है, यूक्रेन तो केवल युद्ध का मैदान भर है। नाटो ऐसे समय पर अपने होने का अहसास कराता रहता है। लेकिन एक बात समझने की ज़रूरत है- क्या आज के समय में अंतिम रूप से कोई लड़ाई जीतने में नाटो सक्षम है? क्या ऐसे परिणाम विगत दो दशकों में देखे गए हैं? इस सदी की पहली लड़ाई नाटो ने अपगानिस्तान में लड़ी। उसका अंतिम परिणाम सभी के सामने है। अफगानिस्तान का तो पतन हो गया लेकिन तालिबान फिर सत्ता पर काबिज़ हो गया। यूक्रेन में लंबा खिंचता युद्ध भी कुछ इसी तरह के संकेत दे रहा है। इसकी एक झलक नाटो प्रमुख के एक बयान में देखी जा सकती है जो करीब तीन माह पहले का है। उन्होंने इस युद्ध को लंबा खिंचता देखकर इस बात का ज़िक्र किया था कि यूक्रेन में जारी जंग अब चिंता का विषय बन गई है। अगर यह बंद नहीं हुआ तो फिर दुनिया के हालात भयानक होंगे। सवाल यह उठता है कि क्या नाटो देश इसके बाद भी किसी उचित दिशा और सार्थक परिणामों की ओर बढ़ेंगे?
वर्ष 1949 में अस्तित्व में आया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइज़ेशन (नाटो) एक सैन्य गठबंधन (मिलिट्री अलायंस) के तौर पर काम करता है और किसी भी सैन्य गठबंधन से शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती। कारण यह है कि ऐसे गठबंधनों की शांति की प्रस्तावना युद्ध से शुरू होती है और युद्ध का अंत या तो युद्ध होता है अथवा ध्वंस, शांति नहीं। इस बात की पुष्टि तो यूक्रेन युद्ध से भी हो गई है कि किस प्रकार से नाटो (अथवा सदस्य देशों) की तरफ से युद्ध के बीच लाखों डॉलर वाले एयर डिफेंस सिस्टम सहित पर्याप्त सैन्य एवं युद्धक सामग्री यूक्रेन को उपलब्ध कराई गई। हम यह नहीं कह सकते कि यह अनुचित है लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि इससे शांति कभी नहीं आ सकती।
अगर लगभग तीन दशक पीछे जाकर विश्वव्यवस्था में आए बदलावों का संक्षिप्त आकलन किया जाए तो इस निष्कर्ष पर पहुँचना आसान हो जाएगा कि आज के इस संघर्ष का मूल कारण क्या है और क्या इस पर कभी कोई विराम लगेगा भी या नहीं? इस बात से सभी परिचित ही होंगे कि नाटो शीतयुद्ध की पृष्ठभूमि में निर्णायक कड़ी था। इसका लक्ष्य मूलत: यूरोप में सोवियत विस्तार को रोकना था। लेकिन इसके काउंटर में सोवियत संघ ने वारसा पैक्ट के तहत मध्य और पूर्वी यूरोप के समाजवादी गणराज्यों का राजनीतिक-सैनिक गठबंधन बना लिया। इसके बाद दोनों के बीच करीब साढ़े तीन दशक तक संघर्ष चलता रहा, जब तक कि वर्ष 1991 में सोवियत संघ बिखर नहीं गया। सोवियत संघ के बिखरते ही वारसा पैक्ट भी समाप्त हो गया लेकिन वारसा पैक्ट से जुड़ देशों को नाटो में जगह दे दी गई। आज भी नाटो को मूल चरित्र वही है जो वर्ष 1991 से पहले था। इन तीन दशकों में दुनिया कितनी बदल गई लेकिन नाटो आज भी वहीं खड़ा दिख रहा है। यह रूस के अस्तित्व पर तब भी सीधी चोट थी और आज भी है। रूस निरंतर नाटो को कठघरे में खड़ा करता रहा और यह आरोप लगाता रहा कि पूर्वी यूरोप के देशों को नाटो की स्वीकृति मिलना उसकी सुरक्षा के लिये खतरा है। यूक्रेन भी नाटो की सदस्यता हासिल करने की कतार में था, रूस का विरोध भी स्वाभाविक था। उसके विरोध को नज़रअंदाज़ करने का परिणाम हुआ वर्ष 2014 में क्रीमिया पर हमला। वर्ष 2014 में ही पहले क्रीमिया को रूस से अलग किया गया, फिर जनमत कराकर क्रीमिया को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कराया गया। और अंतत: इसका रूस में विलय कर लिया गया। क्रीमिया अब रूसी टाइम ज़ोन का हिस्सा है और यह रूस के लिये काला सागर (Black Sea) में रणनीतिक संतुलन स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है। ध्यान रहे कि उस समय रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था- सोवियत संघ के पतन के बाद रूसी जनता दुनिया के सबसे विभाजित समुदायों में शामिल हो गई। लाखों लोगों ने सोने से पहले एक देश देखा और दूसरे देश में आँखें खोलीं, जहाँ वे अल्पसंख्यकों में गिने जाने लगे। पिछले दस साल से यूक्रेन में चल रहे राजनीतिक संकट ने वहाँ निवास कर रहे रूसी मूल के लोगों को तबाह कर दिया। पुतिन कितना सही थे यह कहना मुश्किल है लेकिन पूरी तरह से गलत नहीं थे यह कहना तर्कसंगत होगा।
सामान्यतया रूस को भले ही गलत मान लिया गया हो लेकिन एकतरफा निष्कर्ष निकाला जाना भी उचित नहीं है। इसमें कई पेंच थे। पहला यह कि यूक्रेन में लगातार दक्षिणपंथी ताकतों को समर्थन क्यों दिया गया जबकि उसकी गतिविधियाँ रूस विरोधी थीं। ऐसा किसी एक दिन या एक वर्ष में नहीं हो गया बल्कि यह सोवियत विघटन के बाद से ही रणनीतिक रूप से चल रहा था। वहाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ पाँव पसारने लगी थीं जिनका उद्देश्य नए संघर्षों को जन्म देकर अपने हितों को पूरा करना था। यूूक्रेन में दक्षिणपंथी और नव-नाज़ीवादी (Neo-Nazism) अपना प्रभाव रणनीतिक तौर पर बढ़ाते दिख रहे हैं। पश्चिमी ताकतें रूस को कमज़ोर करने के लिये नव-नाज़ीवादियों को लगातार समर्थन दे रही थीं, जो अभी भी जारी है। इसमें यदि भाषायी अतिवाद को जोड़ दें तो बात और भी स्पष्ट हो जाएगी अर्थात भाषायी आधार पर राष्ट्र को निर्धारित करने वाले अतिवादी सक्रिय हैं। राइट सेक्टर, स्वोबोदा (स्वतंत्रता) तथा राष्ट्रवादी स्टेपान बांडेरा, जैसे संगठन पूरी तरह से रूस विरोधी और नाज़ी समर्थक रहे हैं। ये पश्चिमी संरक्षण में रूस के लिये निरंतर चुनौती बनते जा रहे थे।
आर्थिक टकराव को भी यहाँ नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। करीब एक दशक पहले के यूरेशियन कस्टम यूनियन और यूरोपियन यूनियन के बीच टकराव भी एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। उल्लेखनीय है कि संघ की स्थापना नवंबर 2011 में हुई जिसमें रूस, कज़ाकिस्तान और बेलारूस शामिल थे। इस संघ का प्रमुख लक्ष्य है- मुक्त व्यापार, कस्टम और वाणिज्यिक आदान-प्रदान से सदस्य देशों को लाभ पहुँचाना। इसके बाद किर्गिस्तान और ताज़िकिस्तान ने भी इसमें शामिल होने की मंशा व्यक्त की और वर्ष 2013 में यूक्रेन ने भी अपनी सदस्यता के लिये आवेदन किया। इस बीच जनवरी 2012 में संघ ने यूरेशियाई आयोग की शुरुआत भी कर दी। हालाँकि जार्जिया, आर्मीनिया आदि देशों ने भी पहले इसमें शामिल होने की इच्छा जताई लेकिन बाद में वे मुकर गए। सवाल यह उठता है कि आखिर इन देशों के मुकरने के पीछे कारण क्या था? इसकी भी पड़ताल होनी चाहिये।
फिलहाल नाटो में फिनलैंड को शामिल कर यह संदेश देने की कोशिश हुई है कि नाटो फौज में अतिरिक्त 2,80,000 सिपाहियों के आने से मॉस्को को और ज़्यादा डरना शुरू कर देना चाहिये। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा हुआ? बल्कि उसी समय क्रेमलिन में शी जिनपिंग की उपस्थिति ने कुछ और ही संदेश दिया। परिणाम यह हुआ कि दुनिया इसके बाद ब्रुसेल्स की तरफ कम और मॉस्को-बीजिंग की तरफ ज़्यादा उत्सुकता से देखने लगी। इसने इस बात की पुष्टि कर दी कि पिछले एक वर्ष दो माह से जो टकराव मॉस्को और कीव के बीच चल रहा है वह सही मायने में मॉस्को-बीजिंग बनाम अमेरिका और पश्चिम है। यूक्रेन तो केवल युद्ध का मैदान भर है।
वास्तविक तो यही है कि चाहे वह ब्रुसेल्स हो या मॉस्को, वहाँ संपन्न होने वाली प्रत्येक गतिविधि इंडो-पेसिफिक को प्रभावित करेगी ही करेगी। कारण यह है कि अर्थव्यवस्था भले ही डि-कपल्ड हो रही हो लेकिन जियो-स्ट्रैटेजी और जियो-फिज़िक्स के छोर एक-दूसरे से इतने मिलते हैं कि अलग-अलग पहचान करना मुश्किल है। यहाँ तक कि दोस्त-दुश्मन के बीच खिंची हुई लकीरें भी अस्पष्ट-सी लगने लगती हैं। ऐसे में यह देखने की आवश्यकता है कि यदि मॉस्को-बीजिंग और पश्चिम के बीच टकराव यूक्रेन से बाहर निकलकर कुछ अन्य क्षेत्रों तक पहुँचता है, तो लक्ष्य कौन होगा? बीजिंग या मॉस्को अथवा पेरिस या लंदन तो नहीं ही होंगे। फिर कीव जैसा कोई दूसरा होगा। फिलहाल तो कीव के बाद सबसे आगे ताइपेई दिख रहा है।
ध्यातव्य है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के इस दौर में ब्रुसेल्स में बैठकर फिनलैंड के नाटो में शामिल होने का जश्न मनाना और सदस्य देशों पर जीडीपी का 2 प्रतिशत रक्षा खर्च करने का दबाव बनाना, कहाँ तक प्रासंगिक है। किसी की चिंता यूरोप में ऊर्जा संकट, लड़खड़ा रही सप्लाई लाइन, कोविड-19 के खिलाफ अधूरी लड़ाई, बेरोज़गारी और महँगाई को लेकर क्यों नहीं दिख रही। आखिर नाटो देश कैसी विश्व व्यवस्था चाहते हैं? आज जर्मनी, इटली, तुर्किये, फ्रांस, ब्रिटेन आदि की अर्थव्यवस्थाएँ अत्यधिक दबाव में हैं जिसकी वजह से यूरोपीय एकता दरकती हुई दिख रही है। लेकिन कोशिशें एकता को पुख्ता करने की बजाय युद्ध की हो रही हैं।
अंतिम बात यह है कि वुहान वायरस थ्योरी के उभार और चीन की ज़ीरो कोविड नीति की असफलता के बावजूद भी यूरोपीय देश चीन पर विश्वास को लेकर भ्रम की स्थिति में रहे लेकिन किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाए। इसके विपरीत वे विश्वास की कमी से जूझते चीन के लिये ऐसे लूपहोल छोड़ते रहे जिनसे होते हुए उनकी बाज़ारों तक ही नहीं उनके घरों तक चीनी माल की सप्लाई लाइंस पहुँचती रहीं। इसी की झलक है कि ब्रुसेल्स में बैठकर नाटो सदस्य चीन पर ध्यान केंद्रित किये हैं जबकि उसी संगठन के कुछ देश ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स में जिनपिंग के गले मिल रहे हैं तो कुछ जिनपिंग के महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ‘बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव’ का हिस्सा बनने में गर्व की अनुभूति कर रहे हैं जबकि सभी को पता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन की जियो-इकोनॉमिक्स और जियो-पॉलिटिक्स का एक ऐसा उपोत्पाद है जो आने वाले समय में विश्वव्यवस्था को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा।
अप्रैल की शुरुआत में ही यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला फोन डेय लायन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों तीन दिन की बीजिंग यात्रा पर थे। बीजिंग से लौटने के बाद मैक्रों ने एक फ्रांसीसी अखबार से बातचीत में कहा कि ताइवान के मुद्दे पर यूरोपीय संघ को किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिये। ब्लॉक से उनका तात्पर्य अमेरिका और चीन से था। इसका मतलब साफ है अमेरिका अब यूरोप में दूसरे विश्वयुद्ध के ठीक बाद वाली स्थिति में नहीं है। अन्यथा चीन के मुद्दे पर यूरोप के सुर इतने विभाजित नहीं दिखते। यदि यूरोप में अमेरिका को लेकर इतना रूखापन है तो फिर नाटो के विस्तार का अर्थ क्या है? क्या फ्रांस जैसा देश अमेरिका को यह बताना चाह रहा है कि बीते दो दशकों में चीन, यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्थाओं के लिये इंजन साबित हुआ है, जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था डि-कपल्ड होकर अपने ही बोझ के नीचे दब चुकी है। अब यदि यूरोप चीनी अर्थव्यवस्था के साथ बेहतर बॉण्डिंग में (कपल्ड) है तो वह शी जिनपिंग की रूस के साथ ‘नो-लिमिट्स फ्रेंडशिप’ को किस तरह देखना चाहेगा। ऐसा लगता है कि चीन-रूस की ‘नो लिमिट्स’ वाली मित्रता को जानने के बाद भी यूरोप चीन के लिये ‘रेड लाइन’ खींचने की स्थिति में नहीं है।
फिलहाल रूसी विरोध ने अमेरिका और यूरोप को वहाँ लाकर खड़ा कर दिया है जिसे सीमित अर्थों में ही लेकिन एक नए शीतयुद्ध का प्रस्थान बिंदु कहा जा सकता है। यहाँ प्रश्न यह है कि इसके लिये दोषी कौन है? केवल मॉस्को अथवा वाशिंगटन, पेरिस, बर्लिन और लंदन भी?
लेखक अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं।