युद्ध: महिलायें और बच्चे
- 01 Mar, 2024 | डॉ अंकित पाठक

रोमन दार्शनिक और विधिवेत्ता सिसरो ने इतिहासकारों के बारे में कहा था-
“इतिहासकार का पहला नियम है- कभी झूठ कहने की हिम्मत न करना और दूसरा नियम है- जो सच है, उसे किसी भी कीमत पर कह देना”। सिसरो अपने इस कथन में इतिहासकारों क चेतना की, उनके समाज के प्रति और आने वाली पीढ़ियों के प्रति उत्तरदायित्व की और उनके नैतिक साहस को आवाज दे रहे थे। सिसरो के इतिहासकार जैसी ही चेतना से लैस युद्धों पर कई अहम पुस्तकें लिखने वाली हमारे समय की मशहूर इतिहास मार्गरेट मैकमिलन ने अपने शोध से यह स्थापित किया कि 'युद्ध ने महिलाओं के जीवन की दिशाएँ बदल दीं और कई मायनों में उन्हें पहले से बेहतर भूमिकाएँ दीं। बदले में उन्होंने भी दिखा दिया कि वे न केवल पुरुषोचित समझे जाने वाले कार्यों को करने में सक्षम हैं, बल्कि बौद्धिक रूप से किसी भी परिस्थिति का सामना करने को तत्पर हैं'।
यहाँ मैकमिलन प्रथम विश्वयुद्ध के दरमियान बदली स्त्रियों की ज़िंदगी की चर्चा कर रही हैं। प्रथम विश्वयुद्ध ने दुनिया में लाखों को जख्म दिए लेकिन उन्हीं जख्मों की पीड़ा से खुला 'स्त्रियों की मुक्ति' का द्वार। बीसवीं सदी के वैश्विक युद्धों ने आत्महीनता के बोझ से लदी-फदी नजर आने वाली स्त्री को आत्मविश्वास से लबरेज कर दिया। युद्धों पर लिखने वाले कतिपय अन्य इतिहासकारों का भी मानना है कि प्रथम विश्वयुद्ध ने महिलाओं के जीवन में सर्वथा एक नवीन धारा का सूत्रपात किया। इसकी अनुगूँज सबसे पहले यूरोप के देशों में सुनाई और दिखाई दी और उसके बाद दुनिया के अन्य हिस्सों में भी। लेकिन इस अनुगूँज में केवल महिलाओं के द्वारा जो कुछ हासिल किया गया था सिर्फ वही नहीं था बल्कि उनकी कुर्बानियाँ और उनके द्वारा खोए गए वे तमाम रिश्ते थे, जिन्हें पिता, बेटा, पति, भाई या दोस्त के नाम से जानते हैं। इस ब्लॉग में युद्ध के दौरान महिलाओं की स्थिति, उनके द्वारा निर्वहन की गई भूमिकाओं के विश्लेषण के साथ ही युद्ध में बच्चों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को भी शामिल किया गया है।
सार्वजनिक जीवन और महिलायें
यूरोप में छठीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही पब्लिक स्फीयर (सार्वजनिक क्षेत्र) और प्राइवेट स्फीयर (निजी क्षेत्र) का द्विविभाजन बना दिया गया था। इस दौर में सार्वजनिक क्षेत्र केवल पुरुषों और वह भी महज नागरिकों तक लिए सीमित था। सार्वजनिक क्षेत्र में राज-काज और सेना से सबंधित कार्य समझे जाते थे। यानी घर की चहारदीवारी के बाहर होने वाले आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप। जबकि निजी क्षेत्र में रसोई, परिवार, बच्चे आदि की देखरेख एवं पालन पोषण यानी चहारदीवारी के भीतर से जुड़े कार्य आते हैं। अरस्तू तक आते-आते यानी चौथी सदी ईसा पूर्व में नागरिकता की धारणा भी बेहद संकीर्ण हो गई थी, कुल आबादी का महज बीस फीसदी ही नागरिक की हैसियत ग्रहण कर पाते थे, बच्चे, महिलायें, बूढ़े, अपाहिज, पागल, दिवालिया और दास आदि को अरस्तू नागरिकता से दूर रखता है। जिन पाबंदियों से प्लेटो ने महिलाओं को मुक्ति दिलाई थी अरस्तू महिलाओं के लिए ईसा पूर्व चौथी सदी में उन्हीं पाबंदियों को थोप देता है। अरस्तू महिलाओं को राज काज के काबिल नहीं मानता। वह कहता है कि पति को पत्नी पर राजनीतिक नियंत्रण रखना चाहिए, महिलाओं को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। यहाँ यह स्थापित हो रहा था कि स्त्रियाँ अपने जीवन के बारे में स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती, और राज्य के भविष्य के बारे में तो उनमें विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता है ही नहीं। सार्वजनिक और निजी दायरे का यह द्विविभाजन पाश्चात्य चिंतन परंपरा में हॉब्स और रूसो जैसे उदारवादियों तक भी बना हुआ था। दोनों स्त्रियों को उनकी यौनिकता के कारण ही निजी क्षेत्र तक समेट देते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र को उनके लिए निषिद्ध करार देते हैं।
चौथी सदी ईस्वी में जब ईसाई धर्म का प्रभुव राज्य पर बढ़ना शुरू हो जाता है और रोमन साम्राज्य ने ईसाईयत को अपना राजकीय धर्म बना लिया तब से धर्म की सत्ता से मनुष्य नियंत्रित होने लगा और इसमें भी सबसे अधिक जकड़न में स्त्रियों की ज़िंदगी आई। उनके जीवन की यह जकड़न पुनर्जागरण, आधुनिकता और और विशेषकर उदारवादी क्रांतियों (इंग्लैंड की क्रांति-1688, अमेरिका की क्रांति-1777 और फ्रांस की क्रांति-1789) के बाद भी नहीं टूटी, उन्हें लंबे समय तक मूलभूत नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा। और यह भी सभी महिलाओं के नहीं कहा जा सकता, संयुक्त राज्य अमेरिका में तो अश्वेत महिलाओं को अपने नागरिक अधिकारों के लिए अलग से एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। रोजा पार्क्स नामक अश्वेत महिला का नाम अश्वेत महिला अधिकारों का हासिल था। यह सार्वजनिक क्षेत्र में दूसरी श्वेत महिलाओं के समान ही अपने अधिकारों की दावेदारी का आंदोलन था। ऐसे ही आंदोलन पूरी दुनिया में आज भी जारी है, महिलायें आज भी अपने लिए सार्वजनिक जीवन में अधिक से अधिक स्पेस की तलाश कर रही हैं। कहीं कहीं यह राज्य के प्रयास से संभव हो रहा है तो कहीं कहीं उनके आंदोलनों की बदौलत पर कहीं कहीं यह जाने अनजाने में ही सही पर युद्धों की बदौलत भी संभव हो रहा है भले ही इनमें वह अपना बहुत कुछ गवां भी रही हैं।
आँकड़ें क्या कहते हैं?
एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई, 1914 में सरकारी संस्थानों, फैक्ट्रियों में काम करने वाली स्त्रियों की संख्या महज 2 हजार थी, जबकि नवंबर, 1918 तक यह संख्या बढ़कर 2 लाख 47 हजार हो गई। महिलायें ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, सिविल सेवा से लेकर कृषि कार्यों तक में संलग्न थीं। ऐसा भी नहीं था युद्धों के दौरान महिलाओं ने अपनी जानें नहीं गवाईं पर उनकी कुर्बानी ने ही उनकी मुक्ति के द्वार खोल दिए, चूंकि प्रथम विश्व युद्ध के जमाने में महिलायें लगभग देशों की सेनाओं में शामिल नहीं होती थीं इसीलिए युद्धों के दौरान प्रत्यक्ष हताहत होने वालों की संख्या में महिलाओं की संख्या कम थीं लेकिन उनकी एक बड़ी संख्या कतिपय क्षेत्रों में बड़े जोखिम के कार्य कर रहीं थी जिनमें घायल सैनिकों की तीमारदारी जैसे मानवीय कार्यों से लेकर फैक्ट्रियों में कोयला ढोने जैसे भारी भरकम कामों तक शामिल थे।
प्रथम विश्वयुद्ध में वे महिलायें जो नजीर बनीं
इंग्लैंड के एक काउंटी शहर वारविकशायर की रहने वाली डोरोथी लॉरेंस का ख्वाब युद्ध पत्रकार बनना था, पर जब उनका ये ख्वाब हकीकत में न बदल सका तो उन्होंने पुरुष के भेष में सेना में अपनी जगह बना ली, बाद में जब पकड़ी गईं तो उन्हें दुश्मन का जासूस घोषित कर दिया गया, उन्हें युद्ध के दौरान अपने अनुभवों को साझा करने की इजाजत नहीं दी गई। युद्धोपरांत डोरोथी ने तमाम इतिहासकारों को युद्ध क्षेत्र के आँखों देखे दृश्यों का वर्णन किया।
डोरोथी लारेंस पुरुष सैनिक के भेष में
इस क्रम में यार्कशायर की फ्लोरा संडेस का नाम अहम है जो आधिकारिक रूप से प्रथम विश्वयुद्ध के युद्ध सैनिकों की फेहरिस्त में शामिल होने वाली अकेली महिला थीं। फ्लोरा संडेस को सर्बियन आर्मी में अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला के नाम से भी जाना जाता है। फ्लोरा, लेडीज नर्सिंग येओमनरी (Yeomanry) से नर्सिंग की ट्रेनिंग लेकर पहली स्वयंसेवक नर्स बनीं। अगस्त, 1914 के आसपास फ्लोरा घायल लोगों की मदद करते करते सर्बियन रेड क्रॉस की सदस्य बन गई। बाद में फ्लोरा को सर्बियन रेजीमेंट में सार्जेंट मेजर का पद मिलने वाला था लेकिन ऐन वक्त पर चोटिल हो जाने के कारण वो सेना में और अधिक समय तक नहीं रह सकीं पर सेना और देश के प्रति अपनी सेवा देने के लिए वे आजीवन सर्बियन आर्मी फंड और हॉस्पिटल से जुड़ी रहीं।
इसी तरह एक नाम दक्षिणी रोमानिया की रहने वाली एकाटेरिना तेओदोरोइउ ने रोमानियन आर्मी को बतौर नर्स जॉइन किया था लेकिन जल्द ही वे सिपाही बन गईं और युद्ध में शहीद होकर उन्हें मिलिट्री वर्च्यु मेडल (Military Virtue Medal) से नवाजा गया। इस फेहरिस्त में एक नाम पेन्सिलवेनिया की रहने वाली लोरेट्टा पी. वाल्श का भी है जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स नेवी जॉइन की और चार साल बाद उन्हें ‘ऐक्टिव ड्यूटी नेवी वीमेन’ का खिताब दिया गया। यूनाइटेड स्टेट की ही मरीन कॉर्प्स रिजर्व से जुडने वाली तीन सौ से अधिक महिलाओं में पहला नाम ओपा एम. जोनसन का है जिन्होंने शुरुआत में मिलिट्री नर्स के रूप में काम करना शुरू किया और बाद में मरीन रिजर्व का हिस्सा बन गईं।
युद्ध के बाहर महिलाओं ने क्या कुछ हासिल किया?
साल 1918 में ब्रिटेन की संसद ने ‘रेप्रिज़ेन्टेशन ऑफ पीपुल ऐक्ट’ के जरिए इंग्लैंड और आयरलैंड की महिलाओं को जो एक निश्चित संपत्ति रखती थी, को मताधिकार का अधिकार दे दिया परंतु यहाँ महिलाओं के मताधिकार की आयु 30 वर्ष थी जबकि इसी समय में पुरुषों के मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी। यानी राजनीतिक अधिकार हासिल तो हुआ पर गैर बराबरी अभी भी बनी रही। महज मतदान का अधिकार दिए जाने से उसके जमीन पर चरितार्थ हो जाने में एक लंबा वक्त बाकी था, पर इसने शहरी उच्च और मध्यवर्गीय महिलाओं के राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सेदारी के दरवाजे सीमित स्तर पर खोल दिए। यहाँ महिलाओं को चुनने का अधिकार तो दिया गया पर अभी भी चुने जाने का अधिकार उनके पास नहीं था।
साल 1919 में लैंगिक आधार पर स्त्रियों के साथ असमान व्यवहार करने और उन्हें सार्वजनिक कार्य न करने देने को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। इन कानूनों से यह माना जा रहा था कि स्त्रियों की स्थिति में काफी सकारात्मक बदलाव आएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फ्रांस जैसे देश में ‘स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व’ जैसा नारा लगा था वहाँ भी महिलाओं को मताधिकार के लिए द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद तक इंतजार करना पड़ा। यहाँ अभी भी हम दुनियाभर की अश्वेता महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, उन्हें तो पचास के दशक से संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुए नागरिक अधिकार आंदोलन तक का इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद से अश्वेत महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में दावेदारी श्वेत महिलाओं की तरह मिलनी शुरू हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश संसद ने एक चौंकाने वाला अधिनियम पारित किया जिसका शीर्षक था- ‘रेस्टोरेशन ऑफ प्री वार प्रैक्टिस ऐक्ट’, इसके जरिए ब्रिटिश सरकार ने महिलाओं द्वारा युद्ध के समय में ली गई भूमिकाओं को पुनः पुरुषों के हक में छोड़ देने का दबाव बनाया, यानी फिर से महिलाओं को उनके निजी दायरे में सीमित करने की कानूनी कवायद की जाने लगी, जिसे आंशिक स्तर पर सफलता भी मिली पर इसी बीच महिलाओं का आंदोलन भी जोर पकड़ने लगा था जिससे अब महिलाओं को बहुत दिनों तक उनके अधिकारों से वंचित रख पाना मुमकिन न था। उदाहरणस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही ब्रिटेन का उपनिवेश रहे भारत में भी महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग सरोजिनी नायडू, बेगम रसूल और एनी बेसेंट ने मोटेंग्यू-चेम्सफोर्ड सिफारिशों के ठीक पहले कर दी थी।
युद्ध की कोख से जन्मा महिला शांति आंदोलन
भले ही युद्ध ने महिलाओं के लिए मुक्ति के द्वार खोले हों लेकिन महिलायें युद्ध की आकांक्षी कभी नहीं रहीं। उन्होंने सांगठनिक रूप से शांति के क्षेत्र में कार्य किए। साल 1915 में अमेरिकी शांतिवादी और नारीवादी संगठन महिला शांति संगठन (Women’s Peace Party -WPP) की स्थापना हुई जिसका कालांतर में नाम बदलकर शांति एवं स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध महिला अंतर्राष्ट्रीय लीग (Women’s International League for Peace and Freedom- WILPF) कर दिया गया। इस संगठन की स्थापना के तीन महीने बाद ही नीदरलैंड के हेग में विश्वयुद्ध समाप्त करने में मध्यस्थता करने के मकसद से महिलाओं के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता जेन एडम्स ने की। यह सम्मेलन अपने आप में महिला आंदोलन के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसमें कुल 12 देशों के 150 महिला संगठनों के लगभग 1150 महिला प्रतिनिधियों ने शिरकत की। यह उस दौर में नामुमकिन सा था जब देशों के बीच युद्ध जारी हों और तमाम यात्रा प्रतिबंध लगे हों। इस सम्मेलन का विरोध और इसे असफल बनाने की कोशिश उस दौर की तमाम सरकारों ने की थी जिसमें स्वयं अमेरिका और ब्रिटेन की सरकार थी। ब्रिटिश मीडिया ने तो इस सम्मेलन का उपहास इसे ‘उन्मादी महिलाओं का बोझ’ कहकर उड़ाया था।
जेन एडम्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने का विरोध किया। इस पर उन्हें पुरुषों की वीरता को कुंठित करने का वाला कहा गया लेकिन एडम्स ने दलील दी कि ‘सैनिक प्राकृतिक रूप से हत्यारे नहीं होते, बल्कि यह तो यंत्रीकृत ढंग से युद्ध आतंक के शिकार बनाए जाते हैं’। उस समय तो एडम्स को हाशिये पर कर दिया गया क्योंकि चारों तरह युद्ध समर्थक ही अपनी झंडा बुलंद किए हुए थे पर साल 1931 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया और खुद अमेरिकी सरकार ने उन्हें शांति के लिए किए गए उनके कार्यों पर सम्मानित किया। अपनी अंतिम सांस तक युद्ध का विरोध करने वाली एडम्स को यह यकीन था कि ‘युद्ध में अपने बच्चों को मरने से केवल एक माँ ही बचा सकती है’। उन्होंने दुनियाभर की मांओं को इस शांति आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया। उनके अनुसार ‘महिलायें युद्ध का विरोध इसलिए नहीं करती कि उनमें संघर्ष की शक्ति नहीं होती, बल्कि महिलाओं का एक बड़ा प्रतिशत संघर्ष के प्रत्येक क्षण को जुनून की तरह थामकर रखता है। उनके विरोध का आधार केवल और केवल एक होता है और वह है- ‘शांति’...’।
जेन एडम्स: महिला शांति सम्मेलन में नारीवादी महिलाकर्मियों के साथ
युद्ध की भयावहता और बच्चे
महिलाओं के लिए युद्ध जहां आत्महंता और आत्ममुक्ति दोनों रूपों में हैं तो बच्चों के लिए युद्ध केवल हंता के रूप में हैं। हालिया आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग दो साल से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध में लगभग 700 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है और लगभग 15 लाख बच्चे बेघर हो चुके हैं। जून, 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में युद्ध के विस्थापित बच्चों की तादाद 3.7 करोड़ थी जो साल 2024 तक बढ़कर 4 करोड़ तक हो गई है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के बावजूद भी राज्य और गैर राज्य अभिकर्ता प्रायः युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हैं जिनमें बच्चों को लेकर किए गए अपराध भी शामिल होते हैं। 16 दिसंबर, 2014 को पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुए आतंकी हमले में मारे गए 132 बच्चों को कौन भूल सकता है? और उधर सीरियाई आर्मी द्वारा भी सारिन नामक गैस के इस्तेमाल से राज्य अभिकर्ता भी इस तरह के मानवता विरोधी हमलों में शामिल हैं। सीरियाई गृहयुद्ध में असद सरकार और इस्लामिक स्टेट के बीच छिड़ी जंग का खामियाजा वहाँ की आम आबादी को कैसे भुगतना पड़ा, और खासकर बच्चों को भुगतना पड़ा उसका अंदाजा एलेन कुर्दी की समुंदर किनारे औंधें मुंह गिरे हुए उस तस्वीर से लगाई जा सकती है, जिससे मानवता शर्मशार हो गई, जिस तस्वीर को दुनिया में युद्ध विरोधी तस्वीरों की फेहरिस्त में शामिल किया गया और युद्ध खत्म करने तथा आतंकवाद के खात्मे आदि के लिए सोचने पर सत्ताधारियों को मजबूर किया। यहाँ कवि आलोक धन्वा की एक लंबी कविता ‘पतंग’ की कुछ पंक्तियाँ कौंधती हैं-
चिड़ियाँ बहुत दिनों तक जीवित रह सकती हैं
अगर आप उन्हें मारना बंद कर दें
बच्चे बहुत दिनों तक जीवित रह सकते हैं
अगर आप उन्हें मारना बंद कर दें
भूख से, महामारी से, बाढ़ से, गोलियों से मारते हैं आप उन्हें
बच्चों को मारने वाले आप लोग
एक दिन पूरे संसार से बाहर निकाल दिए जाएंगे
बच्चों को मारने वाले शासकों सावधान!
एक दिन आपको बर्फ में फेंक दिया जाएगा
जहां आप लोग गलते हुए मरेंगे
और आपकी बंदूकें भी बर्फ में गल जाएंगी
सीरिया का तीन वर्षीय बालक एलेन कुर्दी जिसकी मृत्यु युद्ध जनित विस्थापन के कारण हुई।
 |
डॉ अंकित पाठकडॉ अंकित पाठक मूलत: सुल्तानपुर जिले के हैं। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में परास्नातक और शोध किया है। वर्तमान में ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेज ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इनके पास उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापन, लेखन और शोध का दस से अधिक वर्षों का अनुभव है। राजनीति विज्ञान, इतिहास, सिनेमा और साहित्य में इनकी गहरी रुचि है। |







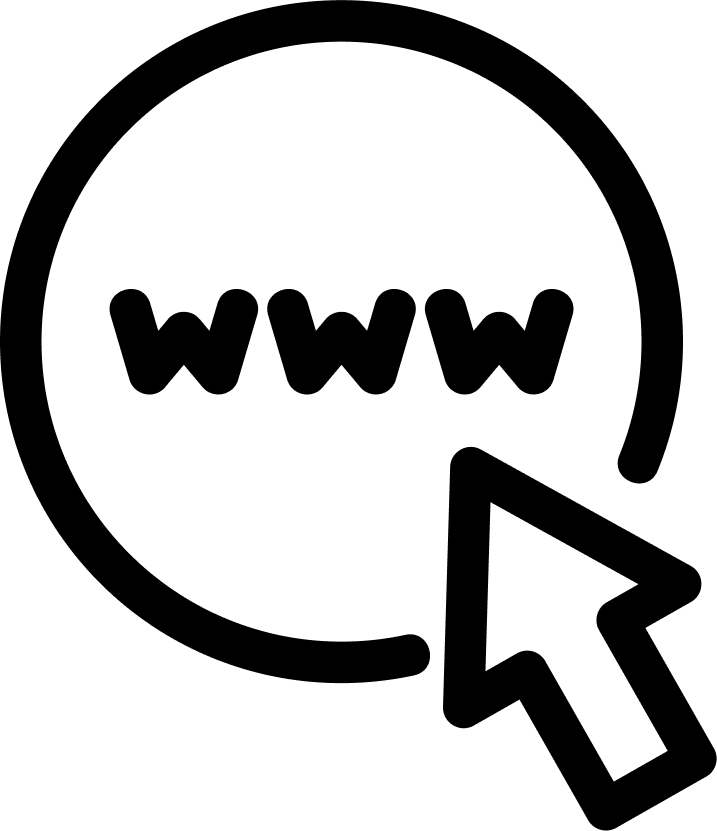
-min.jpg)