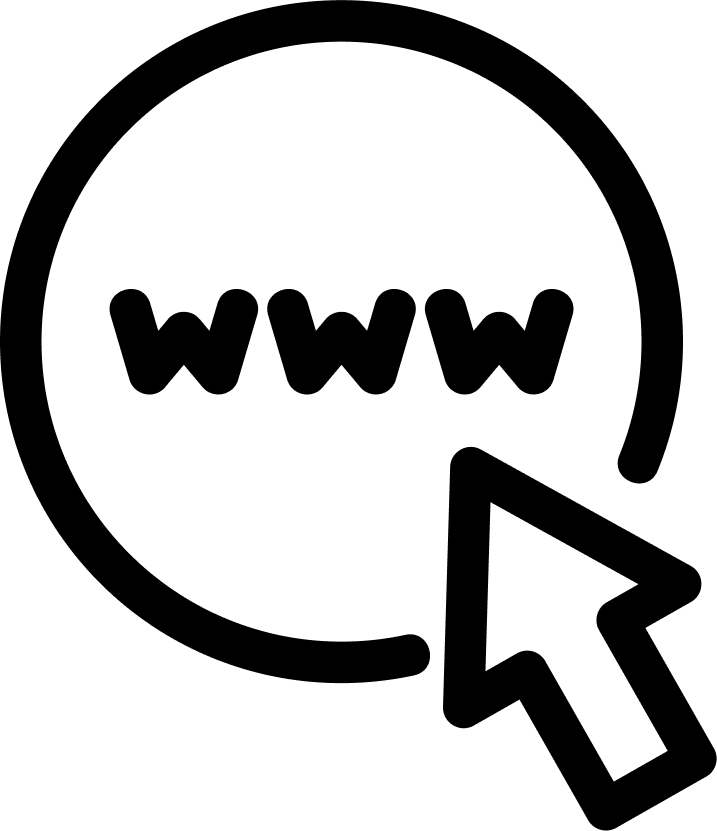पितृसत्ता की व्यवस्था नजर में बहुत कम आने के बावजूद विषमता की सबसे प्रभावी संरचना है
- 08 Mar, 2021 | सन्नी कुमार

“पढ़िये गीता
बनिये सीता
फिर इन सबमें लगा पलीता
किसी मूर्ख की हो परिणीता
निज घर-बार बसाइये
होंय कँटीली
आँखें गीली
लकड़ी सीली, तबियत ढीली
घर की सबसे बड़ी पतीली
भर कर भात पसाइये।”
कवि ‘रघुवीर सहाय’ मात्र दस पंक्तियों की अपनी इस कविता में उस व्यवस्था की पूरी सच्चाई उकेर देते हैं जहाँ भेदभावमूलक और निरर्थक जीवन की तहें इतने सलीके से सजाई गई होती हैं कि वो उचित और स्वाभाविक लगती हैं। इतना ही स्वाभाविक कि रोज व्यतीत हो रहे इस जीवन के विरुद्ध समाज कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। अरे! प्रतिक्रिया क्यों? वह तो चौंकता भी नहीं। सभ्यताई विकास और सांस्कृतिक निर्मिति की पूरी संरचना ही इस रूप में संचालित होती रही है जिसका लक्ष्य स्त्रियों को ‘कमतर मनुष्य’ के रूप में तैयार करना है। इस पूरी व्यवस्था को प्रसिद्ध नारीवादी चिंतक ‘सिमोन द बोउवार’ ने एक वाक्य में सूत्रबद्ध कर दिया है- “स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है।” आखिर वह कौन-सी व्यवस्था है जो स्त्री को स्त्री बना देती है? यह व्यवस्था है- पितृसत्ता।
पितृसत्ता का सामान्य अर्थ एक पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था से है अर्थात् सामाजिक हैसियत का ऐसा पदानुक्रम जहाँ पुरुष शीर्ष पर है और महिला तल पर। यहाँ इस बात को और स्पष्टता से कह देने की आवश्यकता है कि भेदभाव की यह कोई लैंगिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह एक विशुद्ध सांस्कृतिक परिघटना है। लिंग आधारित जैवकीय अंतर तो प्राकृतिक हैं किंतु इस आधार पर दो अलग सामाजिक संसार बना देना एक मानवीय कृत्य है। इस अलग और भेदभावपूर्ण संसार की रचना ही पितृसत्ता के मूल में है। पितृसत्ता विचारों के रूप में गढ़ी जाती है और व्यवहारों के माध्यम से मूर्त होती है। विचार के रूप में पितृसत्ता के बीज धार्मिक ग्रंथों से लेकर राजनीतिक सिद्धांतों तक में देखे जा सकते हैं। प्लेटो, अरस्तू, देकार्त जैसे विचारकों ने स्त्री को परिवार, प्रजनन तथा मातृत्व के साथ जोड़कर उसके अस्तित्व को पराश्रित तथा विस्तार को संकुचित कर दिया। जर्मन दार्शनिक हीगल ने तो स्त्री-पुरुष की दो अलग दुनिया का ही निर्माण कर डाला जिसमें महिलाओं के लिये ‘प्राइवेट स्फीयर’ तथा पुरुषों के लिये ‘पब्लिक स्फीयर’ निश्चित किया। स्वाभाविक रूप से यहाँ महिलाओं के सार्वजनिक जीवन के लिये कोई स्थान नहीं था। रूसो जैसे चिंतक स्त्री को बौद्धिक गतिविधि के योग्य नहीं मानते थे। रूसो ने सदाचार और सद्गुणों को भी स्त्री और पुरुष दोनों के लिये अलग-अलग निर्धारित किया। जैविक तात्त्विकवाद के दर्शन ने तो पुरुष को जन्मना श्रेष्ठ व योग्य तथा स्त्री को जन्मना सामान्य माना। कुल मिलाकर कहने का भाव यह है कि पितृसत्ता का विचार भेदभाव को जायज मानने की बुनियाद पर टिका है, और यही विचार सामाजिक व्यवहारों के रूप में प्रत्यक्ष होता है। आखिरकार यह विचार किस प्रकार प्रत्यक्ष होकर विषमता की प्रभावी संरचना निर्मित करता है, इससे पहले यह देख लेना अधिक उचित होगा कि आखिर इतनी प्रभावशाली संरचना आसानी से नजर क्यों नहीं आती?
इस संदर्भ में मुख्यतः दो पक्षों का उल्लेख किया जा सकता है। एक तो पितृसत्ता सामाजिक जीवन में इस तरह घुल-मिल गई है कि भेदभाव की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। और स्पष्टता से कहा जाए तो पितृसत्तावादी भाव से संचालित व्यवहार इतने रूढ़ हो गए हैं कि जब तक विशिष्ट रूप से इस ओर ध्यान न दिया जाए, भेदभाव का एहसास नहीं होता। उदाहरण के लिये लड़कों व लड़कियों के लिये अलग-अलग समाजीकरण की प्रक्रिया को अपनाना- जहाँ लड़कियों को अधिकांशतः घरेलू सीमा के भीतर गुड़िया जैसे खिलौने के साथ खेलने के लिये प्रोत्साहित करना तो लड़कों को इस दायरे के बाहर क्रिकेट या फुटबॉल जैसे खेलों के लिये छूट देना। एक ओर घर की कोमल दुनिया के अनुरूप विनम्र स्वभाव की सीख है तो दूसरी ओर बाहर की दुनिया से होड़ लेने की आक्रामक ट्रेनिंग। यही प्रक्रिया आगे बढ़कर एक खास ढंग से जीवन बरतने की ओर बढ़ जाती है जहाँ लड़कियों से पारिवारिक मूल्यों के अनुकूल व्यवहार करने, विनम्र व लज्जाशील होने, घरेलू आवश्यकताओं को प्राथमिक मानने और सबसे बढ़कर अपनी पवित्रता कायम रखने की न केवल अपेक्षा की जाती है बल्कि उन्हें इसी तरह तैयार किया जाता है, लड़कों को इन बंदिशों से विस्तृत छूट दे दी जाती है। इस प्रकार लड़कियों के जीवन को इस प्रकार तराशा जाता है कि वे पितृसत्तावादी संस्कृति के अनुकूल हो जाती हैं। व्यवस्था के प्रति यह महासमर्पण यहीं से शुरू हो जाता है। समाजीकरण की यह प्रक्रिया अलग-अलग रूपों में इस तरह घटती है कि लड़कियों के व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाती है। जाहिर सी बात है कि जब स्त्री के कमतर होने की बात को लड़कियों के व्यक्तित्व का हिस्सा बना दिया जाता है और इस असंगति को सामाजिक आदर्श के रूप में स्थापित कर दिया जाता है तब इस ‘विषमता की पहचान’ कठिन ही होगी। यहीं अब पितृसत्ता के कम नजर आने के दूसरे पक्ष को देखें तो वह दरअसल पहले बिंदु का ही विस्तार है। दरअसल, मानव-जीवन के इर्द-गिर्द संस्कृति का ताना-बाना इतनी कठोरता से बुना गया होता है कि उसका प्रतिकार आसान नहीं होता। सबसे बढ़कर संस्कृति के तत्त्व सीधे-सीधे विरोध के रूप में नहीं आते हैं बल्कि यह कहना चाहिये कि वे जीवन को एक आदर्श ढाँचे में ढालने के रूप में आते हैं। इसलिये इसे सहज ही अपना लिया जाता है। और चूँकि ‘स्त्री बना दी जाती है’ के जिस रूपक का प्रयोग बोउवार ने किया है वो संस्कृति के दायरे में ही पूरी होती है, इसलिये शोषित स्त्रियाँ इसका प्रतिकार करने की बजाय इसे स्वीकार कर लेती हैं। स्त्रियों का अपने शोषण के प्रति यह ‘अनुकूलन’ भी पितृसत्ता की दृश्यता को कम कर देता है क्योंकि यहाँ पीड़ित/शोषित की सहमति भी शामिल हो जाती है। प्रसिद्ध चिंतक ‘ग्राम्शी’ इस प्रक्रिया को ‘सांस्कृतिक आधिपत्यवाद’ के रूप में चिह्नित करते हैं जहाँ संस्कृति के माध्यम से वर्चस्व कायम रखा जाता है और शोषितों को वर्चस्व के अधीन रहने के लिये तैयार किया जाता है। इस प्रकार स्त्रियाँ धीरे-धीरे इस व्यवस्था के अनुरूप ढलने लग जाती हैं। इस पूरी परिघटना को शिक्षाविद् कृष्ण कुमार इस रूप में चित्रित करते हैं- “ऐसे अनुभवों को झेलने के सतत् प्रयास में अपनी गरिमापूर्ण अस्मिता को, जो अभी तक तिल-तिल करके छीली गई थी, अंततः बलि चढ़ा देती हैं। वे आतंक को आत्मा में उतार लेती हैं।”
अब अगर इस पहलू पर विचार करें कि पितृसत्ता से निर्देशित विषमता किन रूपों में दृश्य होती है तो यह कहा जा सकता है कि इसकी व्याप्ति जीवन के सभी अंगों में है। परिवार के स्तर पर देखें तो जेंडर आधारित यह विभेद जन्म के पूर्व से ही शुरू हो जाता है। पुत्र की चाहत रखने वाला परिवार गर्भ में भ्रूण जाँच कराने तक से नहीं चूकता है। पारिवारिक स्नेह से लेकर पोषण तक और शिक्षा से लेकर संपत्ति के बँटवारे तक भेदभाव की एक पूरी कहानी है। इसके अलावा, सामाजिक मूल्यों की जकड़न स्त्रियों को घरेलू दायित्वों के निर्वहन तक सीमित रखने की भरपूर कोशिश करती है। इसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में देखें तो वहाँ भी महिलाओं की भागीदारी अत्यंत सीमित दिखती है। दिलचस्प बात है कि जिस कौशल में महिलाओं को घरेलू दायरों में निपुण माना जाता है, व्यावसायिक रूप से वहाँ भी उनका प्रतिनिधित्व गौण है।
इसे ‘माँ के हाथ से बने खाने’ के रूपक से समझा जा सकता है। निजी दायरे में यह बात न जाने कितनी बार कही जाती होगी कि जो स्वाद माँ के हाथों से बने खाने में है वो कहीं नहीं। अब अगर यह बात ठीक है कि माँ यानी स्त्री अच्छा खाना बनाती है तो फिर अधिकतर रेस्तरां के रसोइये पुरुष क्यों होते हैं? और अगर यह बात गलत है तो आखिर किस उद्देश्य की पूर्ति के लिये इस वाक्य को दोहराया जाता है? दोनों ही अर्थों के भेदभाव की धारणा को समझा जा सकता है। दरअसल यह महिलाओं को आर्थिक भागीदारी वाले क्षेत्र से वंचित रखने की परियोजना का एक हिस्सा है। आर्थिक गतिविधि के जिस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अधिक है, थोड़ी सूक्ष्मता से देखें तो वो भी दरअसल ‘घरेलू क्षेत्र’ का ही विस्तार है। उदाहरण के लिये अधिकांश महिला श्रमबल प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका, नर्सिंग, खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग, एयर होस्टेस, रिसेप्सनिस्ट इत्यादि जैसे क्षेत्रें में ही खप रहा है, जो मूलतः लालन-पालन के घरेलू दायित्वों का ही व्यावसायिक विस्तार है। इतना ही नहीं, अपवादों को छोड़ दिया जाए तो निर्णय लेने वाले पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग शून्य है।
वस्तुतः विषमता की यह स्थिति संस्कृति से लेकर बाजार तक दोहरे रूप में व्याप्त है। संस्कृति स्त्रियों की भूमिका ज्यादातर इस मामले से निर्धारित कर देती है कि वे अपनी उपस्थिति से पुरुषों को ‘पूर्णता’ प्रदान करें। इस प्रकार स्त्रियों का अपना कोई स्वतंत्र जीवन नहीं बचता। कला के लोकप्रिय माध्यमों, यथा- सिनेमा में भी इस सांसारिक चेतना का प्रदर्शन देखा जा सकता है जहाँ नायिका का पात्र केंद्रीय नहीं होता और उसका सारा महत्त्व नायक के पात्र को मजबूती देना होता है। दूसरी तरफ बाजार सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने का दावा तो करता है लेकिन इसकी आड़ में महिला शरीर का वस्तुकरण कर बैठता है। इसके अलावा सामाजिक निषेधों के प्रतिकार के नाम पर उन सभी बुराइयों को अपनाने के लिये प्रेरित करता है जो अंततः स्त्रियों के खिलाफ ही जाती हैं। इन प्रसंगों और उदाहरणों की एक अंतहीन शृंखला है।
राहत की बात यही है कि धीरे-धीरे ही सही, समाज विषमता की पहचान करने लगा है। और एक बार जब मर्ज की पहचान होने लगी है तो इसका समाधान भी होगा, ऐसी आशा रखना उचित ही है। अंत में पुनः कवि ‘रघुवीर सहाय’ को याद करना होगाः
“बच्चा गोद में लिये
चलती बस में
चढ़ती स्त्री
और मुझमें कुछ दूर घिसटता जाता हुआ।”
 |
[सन्नी कुमार] |