पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन और भारत की ऊर्जा रणनीति
- 29 Apr, 2025
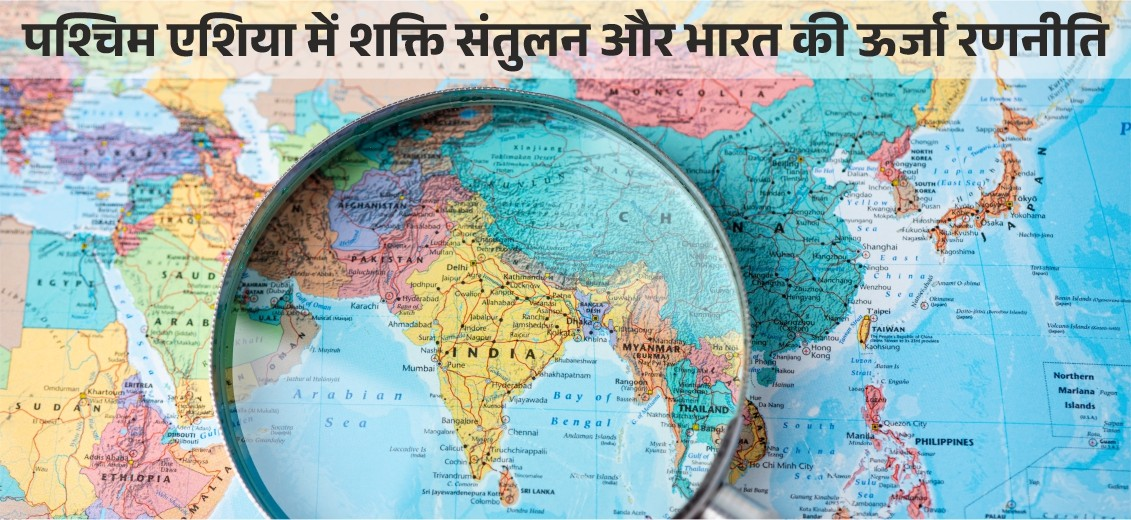
तेहरान की परमाणु गतिविधियों पर ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तीसरे दौर की बातचीत के साथ ही पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन ने नई करवट ले ली है। यह वार्ता क्षेत्र में एक और संघर्ष को टालने में सक्षम है। यह बातचीत भारत के दृष्टिकोण से बेहद महत्त्वपूर्ण है क्योंकि ईरान, भारत की ऊर्जा ज़रूरतें पूरा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के समय 2018 में ईरान के साथ पिछले परमाणु समझौते को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह एक त्रुटिपूर्ण समझौता था। अमेरिकी और ईरानी विशेषज्ञों के अनुसार, तीसरे दौर की वार्ता में ईरानी परमाणु सुविधाओं पर संभावित इज़रायली हमले की आशंका को कम करने और ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिये प्रयास किये गए । यह अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाकर और ईरान को विदेशी निवेश के लिये खोलकर ईरान के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को भी बदल सकता है। इसमें ईरान की परमाणु सुविधाओं की निगरानी उसके यूरेनियम संवर्द्धन और यूरेनियम के उसके भंडार के साथ भविष्य की रणनीति और प्रतिबंध की बात शामिल है। वार्ता का उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकना भी है, क्योंकि यह समझौता ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच व्यापक संघर्ष को टाल सकता है। ईरान यूरेनियम को लगभग 60% शुद्धता तक समृद्ध कर रहा है, जो हथियार बनाने के लिये आवश्यक स्तर से थोड़ा कम है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार अगर वह हथियार बनाना चाहे तो उसके पास पर्याप्त यूरेनियम है, जबकि ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये है।
वास्तव में ऊर्जा किसी भी अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा है। तेल और गैस का ईंधन के रूप में प्रयोग करने की खोज ने इसकी दक्षता और परिवहन में आसानी के कारण ऊर्जा परिदृश्य में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इसने तेल को विश्व के प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में स्थापित कर दिया। औद्योगीकरण की बढ़ती गति और विश्व युद्धों ने ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित करने की दौड़ को तेज़ कर दिया, जिससे ऊर्जा सुरक्षा वैश्विक राजनीति में एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व बन गई। बढ़ती वैश्विक मांगों और सीमित आपूर्ति के कारण तेल का रणनीतिक महत्त्व नई ऊँचाइयों पर आ गया । ऊर्जा की पर्याप्त और सस्ती उपलब्धता सुनिश्चित करना दुनिया भर में राष्ट्रीय रणनीति का एक महत्त्वपूर्ण पहलू बन गया। पश्चिम एशियाई संदर्भ में, यह परिवर्तन विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र की स्थिति प्रमुख तेल और गैस भंडार वाले क्षेत्र की है। तेल और प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडारों का घर अब पश्चिम एशिया है। इसी कारण से पश्चिम एशियाई अर्थव्यवस्थाएँ ऊर्जा-आधारित निर्यात राजस्व पर बहुत अधिक निर्भर हैं। यह स्थिति उनके शासन और सामाजिक संरचनाओं को गहराई से प्रभावित करती हैं।
तेल और प्राकृतिक गैस की दुर्लभ प्रकृति के विपरीत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रचुर मात्रा में हैं। यह तथ्य पश्चिम एशियाई देश के तेल और गैस भंडारों की वैश्विक प्रासंगिकता को कम करता है और क्षेत्रीय स्थिरता को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। तेल गैस आधारित ऊर्जा से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर आना ही ऊर्जा संक्रमण है। इस संक्रमण की धीमी और अनिश्चित गति के बावजूद, ऊर्जा संसाधनों का रणनीतिक महत्त्व और तेल तथा गैस की ऐतिहासिक भू-राजनीति, पश्चिम एशियाई की भू-राजनीति और स्थिरता पर संक्रमण के प्रभाव के बारे में खासी चिंताएँ उत्पन्न करती हैं। पश्चिम एशिया क्षेत्र दुनिया के लगभग 30% तेल का उत्पादन और वैश्विक तेल भंडार का 48% हिस्सा रखता है। इस क्षेत्र के प्रमुख तेल उत्पादकों में सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, कुवैत, कतर और ओमान हैं।
पिछले कुछ वर्षों में, पश्चिम एशिया में बाहरी देशों का हस्तक्षेप बढ़ा है, जिससे अधिकांश पश्चिम एशियाई देशों की यूरोप एवं अमेरिका पर निर्भरता बढ़ गई है। आंशिक रूप से अपनी रणनीतिक स्थिति से प्रेरित होने के बावजूद, अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिये राजनीति और आधिपत्य के लिये पश्चिम एशियाई तेल के महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता। हालाँकि, शेल गैस की खोज ने पश्चिम एशियाई तेल पर अमेरिकी निर्भरता को कम कर दिया है, जिससे अमेरिकी प्रशासन को अधिक रणनीतिक और कूटनीतिक लचीलापन मिल गया है। हाल ही में, अमेरिकी प्रशासन ने पश्चिम एशिया से हटकर चीन की ओर बढ़ते हुए रणनीतिक प्राथमिकताओं में परिवर्तन का संकेत दिया है।
इधर चीन तेज़ी से पश्चिम एशियाई तेल का एक प्रमुख आयातक बन रहा है। उसने पश्चिम एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को गहरा किया है, यहाँ तक कि पेट्रो-डॉलर वर्चस्व को चुनौती देने के लिये "पेट्रो-युआन" व्यवस्था का प्रस्ताव भी रखा है। दूसरी ओर सऊदी अरब जैसे पश्चिम एशियाई देश अमेरिकी छत्र से दूर अपने रणनीतिक गठबंधनों में विविधता लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें चीन एक आकर्षक विकल्प प्रस्तुत कर रहा है। चीन एवं पश्चिम एशियाई देशों के बीच संबंध जितने घनिष्ठ होंगे, पश्चिम एशियाई क्षेत्र में अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता की संभावना उतनी ही अधिक होगी, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता की पहले से ही नाज़ुक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भारत जैसे रणनीतिक स्वायत्तता का प्रयोग करने वाले और ऊर्जा संक्रमण की दृष्टि से आर्थिक और राजनीतिक ताकत रखने वाले देशों का उदय भी क्षेत्र में स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।
पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन को परिभाषित करने, अंतर-क्षेत्रीय संबंधों, निर्भरताओं और कमज़ोरियों को आकार देने में तेल की महत्त्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। निकट भविष्य में वैश्विक राजनीति में तेल का महत्त्व कम होने की संभावना नहीं है, लेकिन ऊर्जा संक्रमण इसके प्रभाव को अवश्य कम कर सकता है। स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले कारकों की ओर ध्यान केंद्रित करने में यह परिवर्तन संभावित रूप से ऐसे कारकों को नियंत्रित करने वाले देशों के प्रभाव को बढ़ा सकता है। पश्चिम एशिया में यह संक्रमण कमज़ोरियों, निर्भरताओं और गठबंधनों के नवीन संरूपण पेश कर सकता है, जिससे भू-राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप मिल सकता है।
पश्चिम एशिया में नवीकरणीय ऊर्जा की ओर परिवर्तन राजनीतिक एवं आर्थिक विविधीकरण के महत्त्व को रेखांकित करता है। जैसे-जैसे यह क्षेत्र तेल गैस आधारित अर्थव्यवस्था से दूर होता जाएगा, राजस्व और उद्योगों के नए स्रोत उभरेंगे। रणनीतिक वर्चस्व प्रदान करने वाली प्रौद्योगिकी एक केंद्र बिंदु बन जाएगी, जो पश्चिम एशियाई देशों को अनुसंधान और नवाचार में निवेश करने के लिये प्रोत्साहित करेगी। पर निवेश को बनाए रखने के लिये स्थिरता, सुरक्षा और सामाजिक चीज़ों को सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण होगा। पश्चिम एशिया में राजनीतिक विविधीकरण, सुचारू आर्थिक संक्रमण और सामाजिक परिवर्तनों को सुगम बना सकता है। इससे शक्ति और इसकी गतिशीलता को संतुलित करने में सहायता मिलेगी।
हम सब जानते हैं कि वर्ष 2018 में भारत ने पहली बार “वन सन-वन वर्ल्ड-वन ग्रिड” (ओएसओडब्लूओजी) पहल का प्रस्ताव रखा था, जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण हेतु एक सामान्य ग्रिड के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रिड को जोड़ना था। 2021 में इस विचार के साथ साझेदारी में कोप 26 में ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव (जीजीआई) का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य ऊर्जा-समृद्ध स्थानों को महाद्वीपीय ग्रिड से जोड़ने के लिये बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना है, जिससे अक्षय ऊर्जा का निर्बाध हस्तांतरण सुनिश्चित हो सके।
पिछले कुछ वर्षों में खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) आर्थिक रूप से सबसे प्रभावशाली संगठनों में से एक बन कर उभरी है। इसके सभी छह सदस्य-देश - बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई की महत्त्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएँ हैं और इनमें स्वच्छ और हरित ऊर्जा की काफी अधिक संभावना है। इनमें अक्षय ऊर्जा दोहन प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है। पश्चिम एशियाई देशों के लिये हरित ऊर्जा से संचालित क्षेत्रीय बिजली ग्रिड विकसित करना और क्षेत्र के अन्य देशों को ऊर्जा की आपूर्ति करना अभी दूर की कौड़ी पर है पर ओएसओडब्लूओजी और जीजीआई के माध्यम से तथा ऑस्ट्रेलिया की केबल उपयोग प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर ये पश्चिम एशियाई देश, अफ्रीकी और यूरोपीय महाद्वीप के देशों को स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रदान करने के लिये बुनियादी ढाँचे का विकास कर सकते हैं। चूंकि उनके पास पहले से ही जीसीसी के माध्यम से एक सहयोगी व्यवस्था है, इसलिये क्षेत्रीय बिजली ग्रिड और समुद्र के नीचे केबल के माध्यम से अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति में अग्रणी बन कर इसका लाभ उठाने से उनकी क्षेत्रीय भू-राजनीतिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
यह बात बेहद स्पष्ट हो चुकी है कि जलवायु संकट के प्रभावों से कोई भी देश अछूता नहीं है, जिसमें समुद्र का बढ़ता स्तर, बढ़ता तापमान, सूखा, खाद्य असुरक्षा और जबरन विस्थापन शामिल हैं। जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करने की आवश्यकता सर्वोपरि है, जिससे ऊर्जा परिवर्तन अपरिहार्य हो जाता है। बढ़ती आबादी और बढ़ती ऊर्जा मांगों के साथ एक क्रमिक ऊर्जा परिवर्तन आवश्यक है। हालाँकि, वैश्विक बिजली वितरण और भू-राजनीतिक यथास्थिति पर इसके प्रभाव को अनदेखा नहीं किया जा सकता।
तेल उत्पादक पश्चिम एशियाई देशों के लिये तेल आधारित ऊर्जा से स्वच्छ और हरित ऊर्जा स्रोतों की ओर ऊर्जा संक्रमण, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को अस्थिर करने की क्षमता रखता है तो वहीं दूसरी ओर यह कदम ऊर्जा संसाधनों पर भौतिक संघर्षों की संभावना को कम कर सकता है। इतना ही नहीं, यह उपागम यहाँ की राजनीतिक और आर्थिक जटिलताओं को और कठिन बना सकता है, जिससे यहाँ पर चला आ रहा क्षेत्रीय तनाव पहले से कहीं अधिक बढ़ भी सकता है। जलवायु प्रौद्योगिकी और महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में चीन का प्रभुत्व निस्संदेह इन देशों के चीन के साथ संबंधों को प्रभावित करेगा। अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता के बीच पश्चिम एशियाई देशों की यह गतिशीलता अमेरिका को इस क्षेत्र के प्रति अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करने के लिये प्रेरित कर सकती है, जिससे तनाव में वृद्धि हो सकती है।
पश्चिम एशिया में तेल और गैस उत्पादक देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता, परमाणु ऊर्जा का उपयोग और क्षेत्रीय ग्रिडों के संभावित उपयोग जैसे अंतर-क्षेत्रीय कारक भी क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करेंगे। पश्चिम एशियाई देशों के लिये इस जटिलता से निपटने के लिये भारत को विशेष ध्यान देना होगा। इसका एक कारण यह भी है कि यह क्षेत्र भारतीय निर्यात व्यापार के लिये बेहतर जगह है और दूसरा यह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय श्रमिक भी बसे हुए हैं। इसलिये सबसे महत्त्वपूर्ण रणनीति के तहत एक दूरदर्शी और व्यापक आर्थिक और राजनीतिक विविधीकरण रणनीति विकसित करने पर ध्यान देना होगा। पश्चिम एशिया में चीन की चहलकदमी, भारत के दूरगामी लक्ष्यों पर अधिक खराब असर डाल सकती है। पर भारत-मध्य, पूर्व-यूरोप, आर्थिक गलियारा और आई2यू2 जैसी पहल, हितों और चिंताओं को संतुलित करने में मदद कर सकती हैं, जिससे पश्चिम एशिया के तेल गैस वाले क्षेत्रों के लिये घरेलू लाभ और अवसर प्रदान किये जा सकते हैं। विदित हो कि भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा परियोजना वैश्विक अवसंरचना और निवेश साझेदारी का हिस्सा है। यह निम्न और मध्यम आय वाले देशों की विशाल बुनियादी ढाँचे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये एक मूल्य-संचालित, उच्च-प्रभावी तथा पारदर्शी बुनियादी ढाँचा साझेदारी है। इस प्रस्तावित योजना में रेलमार्ग, शिप-टू-रेल नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग शामिल होंगे, जो दो गलियारों तक फैले होंगे। पहला या पूर्वी गलियारा - भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ता है, जबकि दूसरा उत्तरी गलियारा - खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है। इसी तरह आई2यू2 चार देशों—भारत, इज़रायल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गठित एक नया समूह है। इसे ‘आर्थिक सहयोग के लिये अंतर्राष्ट्रीय मंच’ का नाम दिया गया है। यह मध्य-पूर्व और एशिया में आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के विस्तार पर केंद्रित है, जिसके अंतर्गत व्यापार, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला, ऊर्जा सहयोग और अन्य महत्त्वपूर्ण साझा हितों पर समन्वय करना शामिल है। चार देशों का यह समूह आधारभूत संरचना, प्रौद्योगिकी और समुद्री सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समर्थन और सहयोग को बढ़ावा देगा।
ईरान, पश्चिम एशिया का महत्त्वपूर्ण देश है। अमेरिका और ईरान ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में ओमान के साथ मस्कट और रोम में दो दौर की वार्ता की है। अमेरिका एवं ईरान के मध्य इस बातचीत के बाद भी तनाव कम नहीं है। ईरान ने अपनी परमाणु गतिविधियों को तेज़ कर रखा है हालाँकि उसने अभी तक परमाणु बम बनाने का फैसला नहीं किया है, लेकिन अधिकांश आकलन इस बात से सहमत हैं कि ईरान के पास कुछ ही दिनों के भीतर ऐसा करने की क्षमता है। साथ ही ईरान का क्षेत्रीय प्रभाव स्थानीय इज़रायली हमलों और सीरिया के असद शासन के पतन जैसे अन्य क्षेत्रीय बदलावों के परिणामस्वरूप कम हो गया है। इज़रायल ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमले के लिये दबाव बना रहा है, लेकिन अमेरिकी दबाव के कारण ऐसा नहीं हो सका है। अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई है और साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में बमवर्षक विमानों को भेजा है। इन सभी का उद्देश्य ईरान को यह संकेत देना है कि अमेरिकी खतरों को गंभीरता से लिया जाना चाहिये। लेकिन अमेरिका और इज़रायल की संयुक्त सैन्य शक्ति के बावजूद, ईरान पर कोई भी हमला क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिये विनाशकारी होगा। ईरान की परमाणु सुविधाएँ बिखरी हुई और भूमिगत हैं, जिससे उन्हें नष्ट करना बेहद मुश्किल है। हाल ही में हुई शुरुआत ने इस मुद्दे को हमेशा के लिये हल करने के अवसर की एक दुर्लभ खिड़की खोली है। कूटनीति को सफल बनाने के लिये, अमेरिका को एक ज़िम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में कार्य करना चाहिये, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के शस्त्रीकरण को रोकने के लिये प्रतिबद्ध है, न कि एक पक्षपातपूर्ण संरक्षक के रूप में, जो इज़रायल की ओर से ईरान को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने अपने हिस्से के लिये संकेत दिया है कि वह प्रतिबंधों और धमकियों को हटाने के बदले में अपनी परमाणु गतिविधियों को कम करने के लिये तैयार है। इन सबके बीच भारत को आशा रखनी होगी कि यह वार्ता सफल हो और उसका ऊर्जा संकट कम हो सके। अगर पश्चिम एशिया में शांति के प्रयास सफल होते हैं तो भारत के लिये ऊर्जा कूटनीति के लिये नए अवसर भी बनेंगे।




