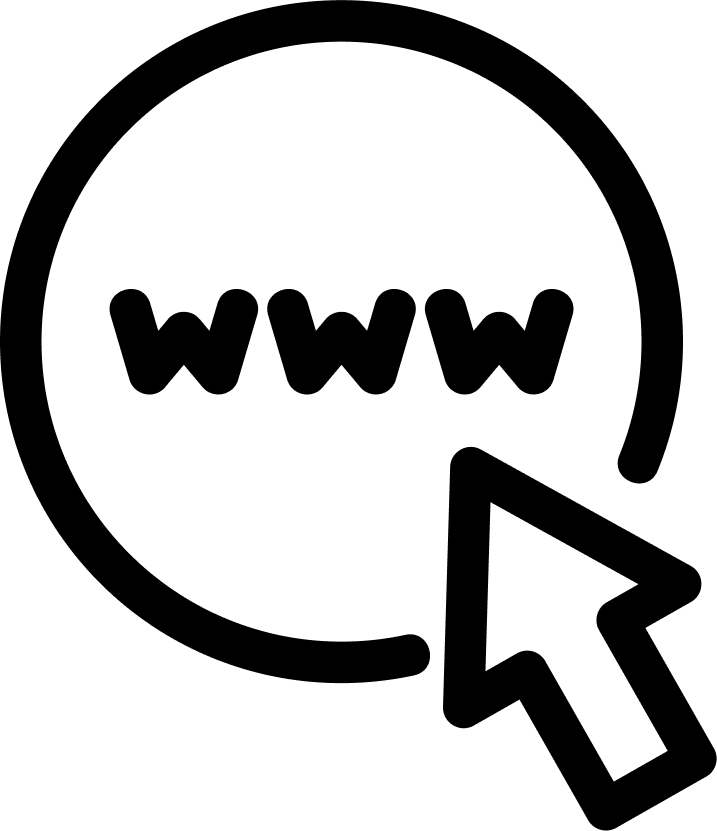कुबेरनाथ राय : भारतीय चिंतन धारा के प्रमुख हस्ताक्षर
- 03 Jan, 2022 | डॉ. मनोज कुमार राय

भारतीय साहित्य के महाप्राज्ञ शिखर पुरुष श्री कुबेरनाथ राय का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के मतसा गाँव में 26 मार्च 1933 को हुआ था। (स्कूल रजिस्टर में 1935 अंकित है) प्रारम्भिक शिक्षा मतसा-मलसा से, इंटरमीडिएट क्वींस कालेज, वाराणसी तथा उच्च शिक्षा क्रमशः काहिविवि और कोलकाता विश्वविद्यालय,कोलकाता से प्राप्त की। रोजी-रोटी के लिए असम के नलबारी जिला के एक कालेज में अंग्रेज़ी के अध्यापक बने । 27 वर्ष की अध्यापकीय जीवन के बाद के बाद जीवन-सेवा के अंतिम दशक में अपने गृह जनपद के एक कालेज में प्राचार्य होकर लौटे और सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर ही 5 जून 1996 को दिवंगत हो गए ।
कुबेरनाथ राय के मन में ‘लेखक बनने का शौक पहले [बचपन] से ही था। परंतु तब वे संपादकों को बताते नहीं थे कि वे विद्यार्थी हैं।’ श्री राय के शब्दों में - “सन 1962 में प्रो हुमायूँ कबीर की इतिहास संबंधी ऊलजलूल मान्यताओं पर मेरे एक तर्कपूर्ण और क्रोधपूर्ण निबंध को पढ़कर पं. श्रीनारायन चतुर्वेदी ने मुझे घसीट कर मैदान में खड़ा कर दिया और हाथ में धनुष-बाण पकड़ा दिया । अब मैं अपने राष्ट्रीय और साहित्यिक उत्तरदायित्व के प्रति सजग था।” सरस्वती की कृपा कुछ इस तरह हुई कि उन्होने “निश्चय किया..कि एक दिन पूज्य पिताजी जब सोये रहेंगे, उनके सिरहाने से ..फटी दीमक लगी किताब निकाल लाऊँगा और आग लगाकर फूँक दूंगा। ..तब हिन्दू धर्म के लिए एक नई पोथी लिखनी पड़ेगी ..उस नई किताब को मैं लिखूंगा, और जो-जो मन में आयेगा, सो लिखूंगा। आखिर मेरी बात भी तो कभी आनी चाहिए, कि आजीवन मैं ‘हाँ,कहारी हाँ’ का ठेका ही पीछे से भरता रहूँगा।” इस प्रकार उनकी कल्पना की नई पोथी की ‘रस-आखेटक’ साधना ‘प्रिया नीलकंठी’ से शुरू होकर ‘गंधमादन’के शिखर पर जा पहुँची । धर्म-युद्ध के शीर्ष पर ‘विषाद योग’ से गुजरना स्वाभाविक है। तब वीरासन को साधते हुए भीतर बैठे रामत्व का उन्होने ‘पर्णमुकुट’ बनाया। ‘कामधेनु’ की रस्सी को ‘महाकवि की तर्जनी’ में लपेटा और ‘निषाद-बांसुरी’ पर ‘त्रेता का वृहत्साम’ का राग छेड़ते हुए ‘उत्तरकुरु’ की ओर बढ़ चले। रास्ते में ‘किरात नदी में चंद्रमधु’ के उस पार जाने के लिए ‘मन पवन की नौका’ पर सवार हो गए। भीतर बैठा राग-पुरुष ‘मराल’‘पत्र मणिपुतुल के नाम’ का गांधी-मंत्र जपते हुए ‘चिन्मय भारत’ से ‘दृष्टि अभिसार’ करने लगा। रस का छक कर पान करने के बाद ‘कंथामणि’ को हृदय से लगाए ‘आगम की नाव’ में सवार हो गए । घोर निशीथ में उनका पथ-प्रदर्शक बना ‘अंधकार में अग्निशिखा’ और वे पहुँच गए अपने सर्वप्रिय घाट ‘रामायण महातीर्थम’ पर जहाँ उनकी ‘वाणी का क्षीर सागर’से ‘महाजागरण का शलाका पुरुष’ का स्फोट हुआ।
कुबेरनाथ राय का युगबोध
श्री राय एक सजग लेखक हैं। वे युगीन विसंगितयों से वाकिफ हैं। वर्तमान से वह बहुत संतुष्ट नहीं है-“वर्तमान को लेकर कब कौन सुखी रहा है।” लेकिन अपने इस क्रोध और शिकायत को साहित्य का माध्यम देने के वे समर्थक हैं । श्री राय ने जीवन की केवल उन्हीं प्रवृत्तियों और नीतियों का समर्थन किया है जो बहुजन हिताय है । सच तो यह है कि उन्होंने सत्य और लोकमंगल में से भी लोकमंगल को वरीयता दी है। यदि सत्य जनहितकारी नहीं है, तो उन्हें स्वीकार नहीं है । उदाहरणतः वे आधुनिक उच्च तकनीक और बड़े-बड़े उद्योगों के महत्व को स्वीकारते हुए भी लघु उद्योगों को वरीयता देते हैं क्योंकि वर्तमान जनबहुल भारत में अधिक उत्पादन की बजाय अधिक जन हितकारी है- ‘अधिक लोगों द्वारा उत्पादन’। लघु उद्योगों द्वारा अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे । अतः बेरोजगारी से पीड़ित भारतवर्ष में लघु उद्योग ही हितकारी हैं-“एक गरीब आदमी, सबसे छोटा मंदिर बनाकर, सबसे बड़ा बनाने वाले अमीर आदमी से कम मेधावी नहीं है।” यहाँ वे महात्मा गांधी मार्ग पर चलते हुए दिखते हैं। वे राजनीति के वर्तमान स्वरूप से इसलिए क्षुब्ध हैं क्योंकि उसमें सत्य और जनहित की सर्वदा उपेक्षा होती है। वे शील-सापेक्ष राजनीति के पक्षधर हैं, शीलहीन राजनीति के नहीं । उन्हें वर्तमान बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों से इसलिए शिकायत है क्योंकि वे वृहत्तर जनमंगल के दायित्व से शून्य ‘पवनी-पजहर’ बनने में रुचि रखता है। उन्हें नए साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही लगती है कि वह पाठक को कोई मूल्यबोध नहीं दे पाता । वे मार्क्सवादी, अस्तित्ववादी, नव्य मार्क्सवादी दर्शनों के विरूद्ध इसीलिए हैं कि ये मानव को कोई आशा,उत्साह और जिजीविषा देने की बजाय संशय,निराशा और कुंठा प्रदान करते हैं । वे वर्तमान पुरोहित-तन्त्र के इसलिए विरुद्ध हैं क्योंकि इन्होंने अपने स्वार्थ के कारण धर्म को विकृत किया है और लोगों की आस्थाओं को भ्रष्ट किया है । वे विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों और प्रोफेसरों से इसलिए निराश हैं क्योंकि सभी अपनी स्वार्थ-साधना में संलिप्त हैं। उन्होंने विद्या और दायित्व की बजाय सुख-साधन को जीवन का लक्ष्य बना लिया है । उन्हें सरकारी अधिकारियों से यही शिकायत है कि वे काम के नाम पर शून्य, और दाम के नाम पर सदा अतृप्त बने रहते हैं। इसलिए आनंद कुमारस्वामी द्वारा एक सदी पूर्व दिये गए जंतर ‘कि देश की महत्वपूर्ण ताकतों को अस्थायी राजनीतिक संघर्ष में बर्बाद न करते [हुए]’ साहित्य,कला, शिल्प, कुटीर उद्योग, शिक्षा, संगीत, स्वदेशी, स्वच्छता-सरलता जैसे रचनात्मक पहलुओं को अपने निबंधों में भरपूर जगह दिया। क्योंकि वे भी यह मानते हैं कि राष्ट्रों का निर्माण कवि और कलाकार द्वारा होता है न कि व्यापारी और राजनीतिज्ञों द्वारा।
कुबेरनाथ राय और भारतीयता की धारणा
श्री राय का जन्म गंगा तटवर्ती गाँव में हुआ था। उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 27 वर्ष) अध्यापन करते हुए ब्रह्मपुत्र के किनारे नलबारी (असम) में बिता और अंत में जीवन के आखिरी दस वर्ष भी उसी गंगा की छाया में बीता जहाँ बचपन गुजरा था। इसलिए ‘गंगातीरी लोकजीवन और संस्कृति न केवल उनकी आत्मीयता की भाजन है; बल्कि उनके समूचे लेखन के देशज संस्कार की कारक और सर्जन का आधार भी है।’ उनके लेखन में जो ‘सांस्कृतिक चेतना या मूल्य चेतना सक्रिय है, उसका संबंध भारत से है। भारत, जो सनातन है,सहस्त्रशीर्षा है,महातीर्थ है। उनका समूचा लेखन इसी भारत से एकाकार होने, उसके भीतर के हाहाकार और आर्त्तनाद को आत्मसात करने तथा समष्टिगत अनुभवों से तदाकारता की कोशिश है।’ श्री राय ने सम्पूर्ण विश्व को दो भागों में बांटा है-भारतीय और अभारतीय। भारतीय संस्कृति या भारतीयता को वे एक ‘अति प्रश्न’ (चरम प्रश्न) के रूप में देखते हैं और उसकी परिभाषा या सुनिश्चित लक्ष्य-निरूपण असंभव मानते हुए ‘भारतीयता के प्रत्यभिज्ञान अर्थात भारत की सही आइडेंटिटी के पुनराविष्कार’ की ‘पहचान’ की कोशिश करते हैं और यह कोशिश उनके लेखन में इतिहास-नृतत्व-पुरातत्व-मिथक-भाषाशास्त्र-साहित्य-मूल्यबोध आदि की विमिश्र पद्धति से की गई है। सच तो यह है कि श्री राय का सम्पूर्ण लेखन हमें भारत के ‘चिन्मय’ और ‘मनोमय’ संस्करण से जोड़ता है और उनकी दृष्टि में ऐसे ‘भारत से जुड़ने का तात्पर्य ही होता है मनुष्य,पृथ्वी और ईश्वर से जुड़ना।’
निर्मल वर्मा अपने एक लेख में लिखते हैं-“दुनिया की शायद ही कोई ऐसी संस्कृति हो, जीवित या मृत जो कोई कहानी न कहती हो। इतिहास की धूल में उसकी कुछ कड़ियाँ छिप जाती हैं, कुछ अंश हमेशा के लिए दब जाते हैं। कोई नहीं जानता,पूरी कहानी क्या है,वह कहाँ से शुरू होती है,किस दिशा में बहती है?” श्री राय इस चिंता से बखूबी वाकिफ हैं। वे अपने निबंधों में संस्कृति के उन विस्मृत अंतरालों को युगनद्ध करते हुए अपनी अद्भुत कहन-शैली में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं , “प्रजागर पर्व तुम्हारी नियति है। तुम्हारे जागरण के लिए ही मैं कहानी सुना रही हूँ..तू सुनता जा और हुंकारी भरता हुआ रात भर जागता रह ।” और कहानी आगे बढ़ चलती है कभी नदी के माध्यम से तो कभी पशु-पक्षी के सहारे। लेकिन कहानी में ‘हाँ,कहारी हाँ’ का ठेका बनना उन्हें पसंद नहीं। वे तो एक नई कहानी की किताब लिखने के लिए आतुर हैं जिसमें इतिहास-भूगोल-दर्शन-भाषा की चतुरंगिणी भी साथ-साथ चलती रहती है- “बौद्धों के दिग्विजय का अश्व काशी-वृंदावन में प्रवेश नहीं पा सका।” इतिहास और भूगोल दोनों आकर मिलते हैं गंगा की घाटी में और वहीं धरती का सबसे उदार एवं पावन सत्य रचते हैं जिसे भारतीयता या ‘चिन्मय भारत’ कहा जाता है भारतीयता की सर्वोच्च गाथा ‘रामकथा’ की भूमि यही है और यह नदी ही राम के पूर्वजों की दृष्टि में ‘रघुकुल देवि देवता’ रही है । वस्तुत: अयोध्या-नैमिषाराण्य-वाराणसी’ की भूमि ही भारतवर्ष की सांस्कृतिक कुक्षि है।” लेकिन वे भारतीयता की निर्मिति को केवल ‘वाक-विलास’ अथवा ‘लिखने के लिए लिखना’ तक सीमित नहीं रखते हैं। वे अपने दायित्व को समझते हैं। इसलिए वे बेलौस होकर कहते हैं -“यह ‘भारतीयता’ किसी एक की बपौती नहीं अपितु संयुक्त उत्तराधिकार है। और इस उत्तराधिकार के रचयिता सिर्फ आर्य ही नहीं रहे हैं। वस्तुत: आर्यों के नेतृत्व में इस संयुक्त उत्तराधिकार की रचना द्राविड़-निषाद-किरात ने की है। ग्राम-संस्कृति और कृषि-सभ्यता का बीजारोपण और विकास निषाद द्वारा हुआ है । नगर सभ्यता,कलाशिल्प,ध्यान-धारणा,भक्तियोग के पीछे द्राविड़ मन है। अरण्यक शिल्प और कला-संस्कारों में किरातों का योगदान है। भारतीय ब्रह्मा चतुरानन हैं जिनके चार मुख हैं: आर्य-द्राविड़-किरात-निषाद।” बीसवीं सदी के छठे-सातवें दशक में जब वह अपने राष्ट्रीय-साहित्यिक दायित्व को समझते हुए ‘एक किनारे जम ही रहे थे’, उसी समय उन्हें चतुर्दिक जम्बुक-स्वर (क्षेत्रीय जीवन दृष्टि) की प्रतिध्वनि भी सुनाई देती है -“जब-जब अंधकार छा जाता है,तो जम्बुक वेला का आगमन होता है। तब चारो ओर से जम्बुक-स्वर उठना स्वाभाविक है।” वे इन स्वरों से गहरे चिंतित हैं-“आज सारा देश मोहरात्रि से पराजित और अवसन्न है। आलोक के बिन्दु एक के बाद एक बुझते जा रहें हैं। भय से अधिक हताशा का वातावरण है।” लेकिन श्री राय आशावादी हैं-“मैं एक नए श्रीकृष्ण जन्म की प्रतीक्षा कर रहा हूँ । मैं देव शिशु के अवतरण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे ज्ञात है कि अवतरण होगा, पर इस बार रूप नहीं,भाव का अवतरण होगा,इस बार अवतरण की शैली सामूहिक होगी।”
कुबेरनाथ का कला-विवेक
विषय का सूक्ष्म-संवेद्य निरीक्षण और वर्णन कौशल श्री राय के निबंधों की एक खास विशेषता है। प्रकृति,लोक और मिथकों की व्याख्या का कला-विवेक उन्हें अपने समकालीनों में विशिष्ट बनाते हुए टैगोर,जयशंकर प्रसाद,निराला के [ऐतिहासिक मन] और प्रेमचंद की [अनुभूतिगत ईमानदारी] पंक्ति में खड़ा कर देता है। प्रकृति-पुरुष के निबिड़ संयोग का वर्णन देखने लायक है-‘‘फिर आता है आषाढ़ जिसकी राशि है मिथुन- बैलों के जोड़े खेत में, पुरुष-नारी के जोड़े खेत में, धरती-आकाश का जोड़ा सृष्टि में, मेघ और दामिनी का जोड़ा हवा में - सर्वत्र जोड़ से जोड़ मिल गया है। अब हवाओं का स्वर और स्पर्श कुछ और ही है। लगता है धरती और आकाश का व्रत कंकण आज टूटा है, और वर-वधू को पहली बार स्नान जल पड़ा है। प्रत्येक हृदय सीपी के होंठों की तरह खुला है। पहली बूँद छन्न से वाष्प बनकर उड़ जाती है, मोती नहीं बन पाती। मोती बनने के लिए बूँद को भीतर-भीतर पलना होगा, भाव को भीतर-भीतर बनाना होगा।’’ उनके किसी भी निबंध संग्रह में ऐसे उदाहरण पृष्ठ-पृष्ठ देखे जा सकते हैं। श्री राय के लिए निबंध लेखन ‘आत्म धर्म के पालन’ जैसा है। उनकी दृष्टि में साहित्य व्यक्ति की तुष्टि या मौज शौक के लिए नहीं,समूह की तुष्टि-पुष्टि और शील-संरक्षण के लिए रचा जाता है। उनका उद्देश्य अपने पाठकों को रसबोध कराने के साथ उनकी मानसिक ऋद्धि और बौद्धिक क्षितिज का विस्तार करना रहा है। अपने इस उद्देश्य को, मनुष्य की मनुष्यता के प्रति अपनी बुनियादी प्रतिबद्धता को, अपने लेखन में उन्होंने अनेकशः दुहराया है। इस प्रतिबद्धता के मूल में उनकी यह निर्भ्रांत समझ है- “मनुष्य की सार्थकता उसकी 'देह' में नहीं, उसके 'चित्त' में है। उसके चित्त-गुण को, उसकी सोचने-समझने और अनुभव करने की क्षमता को विस्तीर्ण करते चलना ही 'मानविकी' के शास्त्रों का, विशेषतः साहित्य का, मूलधर्म है।” इसलिए वे अपने पाठकों को अपनी विशिष्ट शैली,भाषा और कथन-भंगिमा के ब्याज से बहुत कुछ देना चाहते हैं। इसके लिए एक विशिष्ट भाषा की दरकार होगी। श्री राय इस बारे में सचेत हैं। वे लिखते हैं -“मैं गाँव-गाँव, नदी-नदी, वन-वन घूम रहा हूँ । मुझे दरकार है भाषा की। मुझे धातु जैसी ठन-ठन गोपाल टकसाली भाषा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए नदी जैसी निर्मल झिरमिर भाषा, मुझे चाहिए हवा जैसी अरूप भाषा। मुझे चाहिए उड़ते डैनों जैसी साहसी भाषा, मुझे चाहिए काक-चक्षु जैसी सजग भाषा, मुझे चाहिए गोली खाकर चट्टान पर गिरे गुर्राते हुए शेर जैसी भाषा, मुझे चाहिए भागते हुए चकित भीत मृग जैसी ताल-प्रमाण झंप लेती हुई भाषा, मुझे चाहिए वृषभ के हुंकार जैसी गर्वोन्नत भाषा, मुझे चाहिए भैंसे की हँकड़ती डकार जैसी भाषा, मुझे चाहिए शरदकालीन ज्योत्सना में जंबुकों के मंत्र पाठ जैसी बिफरती हुई भाषा, मुझे चाहिए सूर के भ्रमरगीत, गोसाई जी के अयोध्याकाण्ड, और कबीर की ‘साखी’ जैसी भाषा, मुझे चाहिए गंगा-जमुना-सरस्वती जैसी त्रिगुणात्मक भाषा, मुझे चाहिए कंठलग्न यज्ञोपवीत की प्रतीक हविर्भुजा सावित्री जैसी भाषा।”
भारतीय मुहावरे और भारतीय संस्कारों से निर्मित विशिष्ट वर्णमाला के बल पर श्री राय ने ललित निबंध को जो विस्तार दिया है वह अद्भुत है। उनसे असल परिचय प्राप्त करने के लिए उनके ‘निबंध-कांतार’ में अनुप्रवेश ही एक आवश्यक शर्त है- वह भी तर्जनी-ओष्ठ एकाग्रता और सावधानी के साथ। मेरा मानना है कि कोई भी पाठक यदि ‘भारत-भारतीयता’ की निर्मिति और उसके आयामों से परिचित होना चाहता है तो उसे आचार्य कुबेरनाथ रोड पर कुछ कदम जरूर चलना चाहिए।
 |
डॉ. मनोज कुमार राय (लेखक गांधी व शांति अध्ययन विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के अध्यक्ष हैं) |