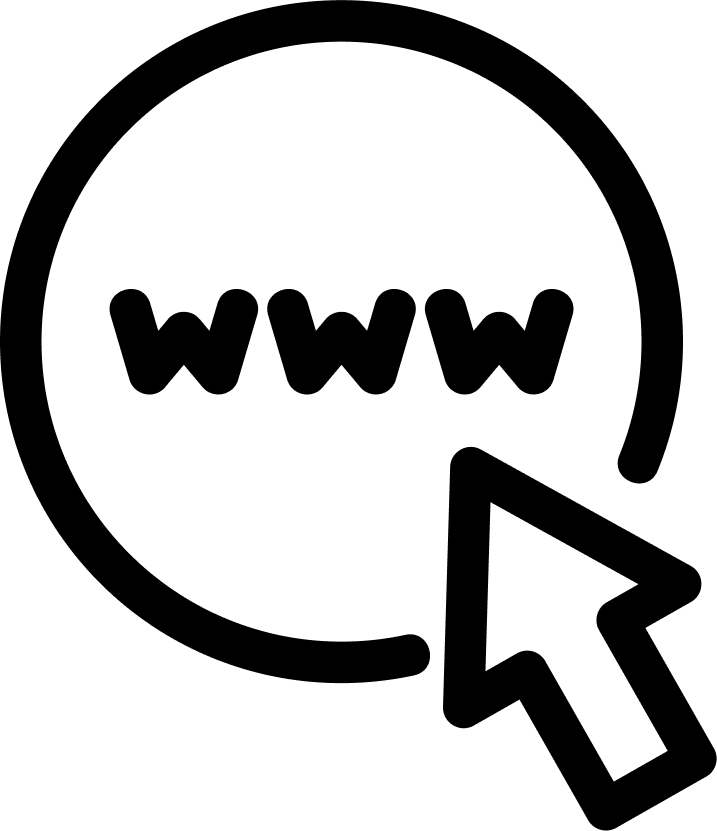आदिम संस्कृति के संरक्षण की कवायद
- 16 Nov, 2019 | अरविंद कुमार यादव

पिछले कुछ वर्षों में पर्यटन के क्षेत्र में ट्राइब टूरिज़्म का तेज़ी से विकास हुआ है। परिभाषा की बात करें तो, ट्राइब टूरिज़्म में लोग दूरदराज के जंगलों में रहने वाले वहाँ के मूल निवासियों को देखने तथा उनकी भाषा, संस्कृति आदि को समझने जाते हैं। माना जाता है कि इस प्रकार की यात्रा से उन क्षेत्रों में रह रहे निवासियों को भी आर्थिक लाभ हो तथा बाहरी समाज से उनका संपर्क बढ़ेगा। परंतु वास्तविकता में ट्राइब टूरिज़्म पर जाने वाले पर्यटक किसी एंथ्रोपोलॉजी के शोध के लिये नहीं जाते बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन तथा रोमांच होता है। हमें इन लोगों को देखना अच्छा लगता है जो हमसे रंग रूप या शारीरिक बनावट में भिन्न हों। कुछ लोगों को इन मूल निवासियों को देखकर दयाभाव भी आता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये असभ्य या गरीब हैं तथा उन्हें इन लोगों की मदद करनी चाहिये। इसलिये वे कभी कभार इन्हें पैसे, खाना, कपड़े आदि वस्तुएँ दे देते हैं। लेकिन इस प्रकार की अंतर्क्रिया से जहाँ एक वर्ग का मनोरंजन मात्र होता है वहीं ऐसा देखा गया है कि इन मूल निवासियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बढ़ते पर्यटन से इनके जंगल, ज़मीनें तथा प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। इसके अलावा बाहरी संपर्क तथा बदलते खान-पान से इनमें अनेक प्रकार की बीमारियाँ भी पनप रही हैं।
भारत में भी ईको टूरिज़्म या ट्राइब टूरिज़्म का काफी विकास हुआ है तथा इसके लिये अंडमान एवं निकोबार लोगों की पहली प्राथमिकता है। पर्यटक वहाँ रहने वाली कुछ जातियों जैसे- जारवा, ओंगे आदि के क्षेत्रों में भ्रमण के लिये जाते हैं। ये लोग सदियों से अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहते आए हैं। अंडमान एवं निकोबार में कुछ ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्र भी हैं जहाँ पर्यटकों को जाने की मनाही है। इसके बावजूद भी लोग ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाते हैं तथा वे वहाँ के निवासियों की हिंसा का शिकार होते हैं।
जॉन एलेन चाऊ
ऐसी ही एक घटना पिछले वर्ष सामने आई जिसमें एक 27 वर्षीय अमेरिकी इसाई मिशनरी जॉन एलन चाऊ की अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी सेंटिनल द्वीप के निवासियों द्वारा हत्या कर दी गई। हालाँकि यह खबर कुछ दिनों तक सुर्खियों में बनी रही लेकिन उसके बाद चाऊ के परिवार द्वारा किसी भी प्रकार का केस दर्ज न किये जाने तथा स्वयं को जोखिम में डालने के उसके निर्णय से मामला रफा-दफा हो गया। बाद में अदालत ने उन मछुआरों को भी बरी कर दिया जिन्होंने वहाँ तक पहुँचने में उसकी मदद की थी। अपनी इस जोखिम भरी यात्रा का ज़िम्मेदार चाऊ स्वयं ही था और उसे यह निश्चित तौर पर पता था कि वहाँ जाना मतलब मौत को गले लगाने के समान है। लेकिन जूनून था क्योंकि साहसिक काम करने निकले थे और वह था धर्म का प्रचार करना तथा इन मूल निवासियों को सभ्य बनाना। चाऊ ने अपने नोट्स में लिखा था कि इन लोगों ने एक बार उसे घायल करके समुद्र के किनारे छोड़ दिया था लेकिन सभ्य बनाने के उसके जूनून की वजह से वो दुबारा गया और इस बार नहीं बचा।
इस लेख के प्रारंभ से तथा उक्त घटना का वर्णन करते समय मैंने ‘मूल निवासी’ शब्द का प्रयोग किया है जबकि इन लोगों के लिये प्रायः आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आदिवासी शब्द का अर्थ भी यही है कि ऐसे लोग जो आदिकाल से किसी स्थान के वासी हों। लेकिन नए शब्द के प्रयोग का मेरा औचित्य मात्र यह है कि वर्तमान में आदिवासी शब्द का आशय प्रायः ऐसे लोगों के समूह से लिया जाता है जो आदिम अवस्था में रहते हों, जिनका आवास, खान-पान, पहनावा आदि आधुनिक इंसानों से कमतर हो, जो असभ्य और बर्बर हों।
लेकिन मेरा मानना है कि ये लोग अपने मूल स्थानों में उस समय से रहते आए हैं जिस समय से पहले का हमें इतिहास भी स्पष्ट रूप से नहीं पता है इसलिये इन्हें मूल निवासी कहना ज़्यादा उचित होगा। रही बात खान-पान की, तो काँटा-छुरी और सफेद कवर वाले टेबल पर शैम्पेन के साथ बैठकर खाना खाने वालों को ये लोग असभ्य लगते हैं। इनके घर-घास फूस के होते हैं इसलिये ये एयर कंडीशनर का प्रयोग नहीं करते और पहनावे के नाम पर किचन में एप्रेन या बाहर ओवरकोट की जगह ये नंगे रहते हैं या शायद कभी-कभार पत्तियाँ लपेटे हुए, इसलिये ये असभ्य हैं। ये भी तो हो सकता है कि इनके पूर्वजों ने आदम और ईव की तरह स्वर्ग के बगीचे के सेब न खाए हों इसलिये इनमें लालच या शर्म जैसी भावना ना पनपी हो और इन्होंने निर्वस्त्र रहना ही पसंद किया हो।
उत्तरी सेंटिनल द्वीप के निवासियों के बारे में मानना है कि ये लोग करीब साठ हज़ार वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। इसी समय के दौरान सिंधु, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं का उदय व अंत हुआ। एक लघु हिम-युग भी आया, फिर भी ये जीवित हैं। वर्ष 2004 की जिस सुनामी ने पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया को प्रभावित किया उसका इन लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि ये असभ्य हैं।
खैर अब बात आती है इनको सभ्य बनाने की ज़िम्मेदारी की, इस प्रक्रिया में ईसाई मिशनरी सबसे आगे रहते हैं क्योंकि उनकी धारणा ये है कि वे दुनिया के सबसे आधुनिक और सभ्य लोग हैं। उनका धर्म सबसे प्रभावी है और उसको मानने वाले स्वयं ही सभ्य हो जाते हैं। इतिहास में दुनिया भर में उन्होंने इसका प्रयोग किया, कई जगह पर वे सफल भी रहे और कई जगह पर असफल। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि स्थानों पर उन्हें सफलता मिली लेकिन भारत, चीन तथा मध्य-पूर्व में वे तकरीबन असफल ही रहें। जब वे लोग इन जगहों पर गए तो पहले तो उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को खाने-पीने की चीज़ें दी और फिर बदले में इनकी आज़ादी छीन ली। इनकी ज़मीनें, घर, खेत जला दिये। बहुत से लोगों को मार दिया गया और जो बचे उन्हें गुलाम बना दिया। उसके बाद मिशनरी आए, उन्होंने कहा ईसाई धर्म स्वीकार कर लो, हम तुम्हें सभ्य बना देंगे। फिर शुरू हुआ सभ्य बनाने का महान कार्य।
इन्हें अस्पताल दिये गए, इनको कपड़े पहनाए गए, इनके बच्चों को स्कूल भेजा गया, नए तौर-तरीके सिखाए गए, भोजन और दवाईयाँ दी गई और बदले में इनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया गया। यहाँ सोना, कोयला और तेल आदि खनिजों की खोज में इनकी बसी-बसाई सभ्यता को नष्ट कर दिया गया। इसे ही उस समय के लोगों ने सभ्य होना कहा। यह बर्ताव अमेरिका में रेड इन्डियंस, ऑस्ट्रेलिया में अबोरिजिनल्स और अफ्रीकी निग्रोस के साथ किया गया।
अमेरिकी रेड इंडियन
15वीं शताब्दी में उत्तरी अमेरिका में यूरोप से, खासकर ब्रिटिश और फ्रेंच मूल के लोग भारी तादाद में पहुँच रहे थे। उन लोगों ने यहाँ के मूल निवासियों, जिन्हें वे रेड इन्डियंस कहते थे, के तौर-तरीके के बारे में कहा कि ये लोग मुद्रा के बारे में नहीं जानते। इनकी अपनी कोई निजी संपत्ति या ज़मीन नहीं होती और पूरा कबीला सार्वजनिक तौर से खेती-बड़ी करता था। उत्पादन को पूरे कबीले में बाँटा जाता था। ये लोग दस्तकारी के कामों में अत्यंत निपुण थे। इन्हें सोना चाँदी जैसी बहुमूल्य धातुओं का ज्ञान नहीं था। जब पहली बार यूरोप के लोग यहाँ पहुँचे तो मूल निवासियों ने उनका स्वागत किया। रेड इन्डियंस ने उन्हें तम्बाकू दिया और बदले में उन्हें शराब मिली। शुरुआती रुझान तो ठीक थे लेकिन बाद में बाहरी लोगों ने इनकी ज़मीनों को घेरना शुरू किया, छोटे-छोटे शहर बसाने शुरू किये और बदले में इन लोगों को इन्हीं की ज़मीनों से बेदखल करने लगे। उसके बाद इनको गुलाम बनाया गया और जो बचे वे जान बचाकर पश्चिमी अमेरिका के रेगिस्तानी इलाके में जाकर बस गए।
ऑस्ट्रेलियाई अबोरिजिनल्स
ठीक इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, जिन्हें वे अबोरिजिनल्स कहते हैं, के साथ हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ ऑस्ट्रेलिया का विशाल भूखण्ड लगा। उन्होंने ब्रिटेन की जेलों में बंद कैदियों को इस बात पर आज़ाद होने दिया कि वो चाहें तो ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ और वापस न आएँ। तब वहाँ बड़ी संख्या में अंग्रेज़ कैदी पहुँचे और ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों का इतना नरसंहार हुआ कि तकरीबन इनकी दो-तिहाई आबादी समाप्त हो गई। वहाँ अनेकों खदान, बड़े-बड़े कारखाने तथा बागानों की स्थापना हुई जहाँ इन कैदियों को काम पर लगाया गया और इस प्रकार आधुनिक ऑस्ट्रेलिया तैयार हुआ। कहा जाता है कि ये लोग कई भाषाओं के जानकार थे तथा प्रकृति के प्रति इनका गहरा लगाव था।
हालाँकि ये सब इतिहास की बातें हैं, आज का समाज और उसकी सोच भले ही वैसी नहीं है। ये कहें कि अब वे इन मूल निवासियों का आर्थिक शोषण नहीं करेंगे या इनको गुलाम नहीं बनाया जाएगा लेकिन ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब भी आधुनिक मानव जाति का इन लोगों के साथ मेल-मिलाप बढ़ा है, तब कुछ नई प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं। उदाहरण के तौर पर, 1970 के दशक में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासियों जैसे- जारवा, ओंगे या निकोबारी से बाहरी लोगों द्वारा जब पहली बार मिलने की कोशिश की गई तब वे भी बिलकुल सेंटीलीज़ की तरह ही आधुनिक समाज से अलग लेकिन स्वाभाव से थोड़े नरम थे। सरकार ने इनके लिये कई मदद के काम किये जैसे- इनको मलेरिया, कुपोषण व अन्य बीमारियों से बचाव के लिये दवाईयाँ दी गईं, टीके लगाए गए। इनके रहने के लिये आरक्षित स्थानों पर पक्के घर बनाए गए। इसके अलावा इनके बच्चों के लिये स्कूल खोले गए और इनके परिवारों को जीवन-यापन के लिये भत्ता भी दिया गया। इन सुविधाओं के कारण अपने पारंपरिक जीवन को छोड़कर इस नए आरामपूर्ण जीवन में, न केवल इनके कौशल में कमी आई है बल्कि भोजन व दिनचर्या में आए बदलावों से इन्हें नई प्रकार की बीमारियों तथा संक्रमण ने भी घेरा है। इससे इनके रीति-रिवाज़ों, भोजन, रहन-सहन, स्वास्थ्य व भाषा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
एक खबर के मुताबिक जारवा जाति की एकमात्र वृद्ध महिला, जो कि ‘हो’ नामक छः हज़ार साल पुरानी एक विशेष भाषा जानती थी तथा उसके माध्यम से वो पशु-पक्षियों की भाषा बोल व समझ सकती थी, वर्ष 2017 में इस महिला की मृत्यु के बाद यह भाषा ही समाप्त हो गई।
कुछ इसी तरह की समस्याएँ दुनिया के अन्य मूल निवासियों के साथ भी सामने आती रहती हैं, जैसे- पापुआ न्यू गिनी, जावा, सुमात्रा तथा अफ्रीका के लोगों के साथ। इनके साथ समस्या न सिर्फ स्वास्थ्य की है बल्कि इनके जीवन का सांस्कृतिक और सामाजिक ढाँचा भी बदला है। कई हिस्सों में आधुनिक मानव से इनके अंतर्संबंधों ने हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया है। इन घटनाओं की कीमत इन इलाकों में रह रहे एनजीओ, मिशनरी या रेड क्रॉस जैसे संगठन के लोगों को चुकानी पड़ती है।
मधुमाला चट्टोपाध्याय सेंटिलीज़ के साथ
कई एंथ्रोपोलोजिस्ट, जिन्होंने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासियों से मुलाकात की है या इन पर शोध कर चुके हैं, का मानना है कि इन सुदूर क्षेत्रों में बसे निवासियों का मूल उद्गम तकरीबन साठ हज़ार साल पुराना है तथा ये मुख्यतः अफ्रीका की नीग्रो प्रजाति से संबंधित हैं। अपनी पुरातन परंपरा व रहन-सहन को बनाए रखने के कारण ये उस वातावरण में अनुकूलित हो चुके हैं जिसके कारण ये इतने लंबे समय से वहाँ रह रहे हैं। मधुमाला चट्टोपाध्याय जो कि वर्तमान में भारत सरकार के सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय में वरिष्ठ शोध अधिकारी हैं, वह पहली व्यक्ति है जिन्होंने सेंटीलीज़ लोगों से 4 जनवरी, 1991 को मित्रतापूर्वक मुलाकात की थी। उस वक़्त वे एंथ्रोपोलॉजीकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक शोध छात्रा थीं। वे अंडमान के मूल निवासियों पर कई शोध पत्र लिख चुकी हैं। उनका मानना है कि ये लोग बाहरी दुनिया के साथ किसी भी प्रकार के संपर्क में नहीं आना चाहते तथा ये प्रकृति, पशु-पक्षी, मौसम आदि का खासा ज्ञान रखते हैं एवं उनकी पूजा करते हैं। ये सदियों से सौहार्दपूर्वक उस परिवेश में रहते आए हैं इसलिये इन्हें इनकी अवस्था पर छोड़ देना चाहिये। साथ ही उनका यह भी मानना है कि हमें किसी प्राकृतिक आपदा के समय ही इनकी मदद के आगे आना चाहिये अन्यथा नहीं।
अरविंद कुमार यादव एक शांत स्वभाव, खोजी प्रकृति, चुनौतियाँ स्वीकार करने वाले, ज़िंदादिल व्यक्ति हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी इस स्वतंत्र लेखक को किताबें पढ़ना और नए लोगों से मिलना पसंद है।