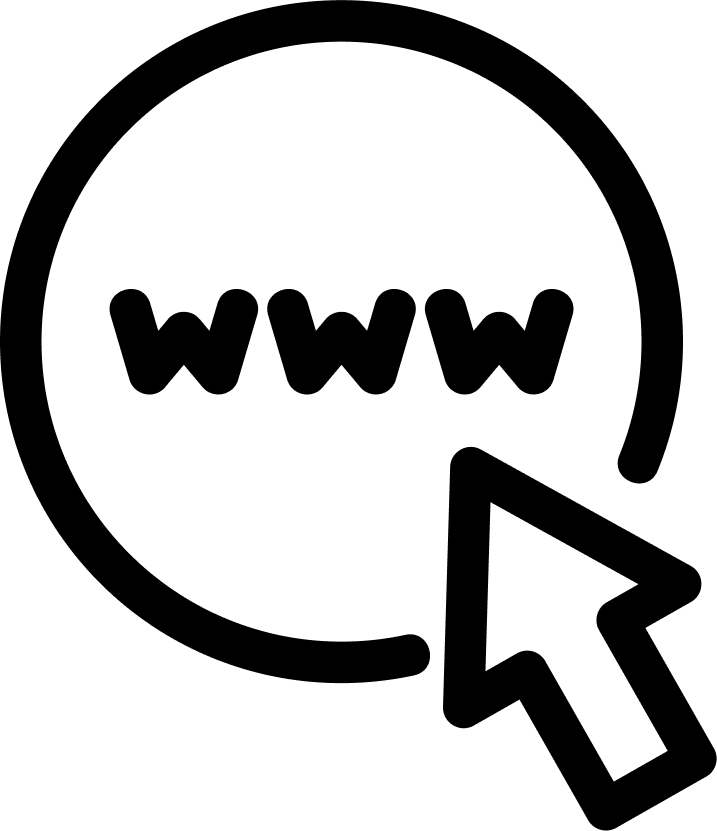डर को जीतना ही ज्ञान की शुरुआत है
- 05 Feb, 2020 | हिमांशु सिंह

संभावित अनिष्ट की आशंका जिसे रोका या नियंत्रित नहीं किया जा सकता, डर है। डर के तमाम रूप और गुण हैं, पर डर का व्यक्तिनिष्ठ होना उसकी प्रमुख विशेषता है। यानी, हर व्यक्ति के पास अपने निजी डर और उसके अपने संस्करण हैं, काफी कुछ प्रेम की तरह।
अधिकांश व्यक्ति जब अपने अनुभवों के आधार पर अपने भविष्य की रूपरेखा बनाते हैं तो वो अनजाने में ही अपने डरों से संचालित हो रहे होते हैं। इस प्रकार डर हमारे जीवन में दिशानिर्धारक की महत्त्वपूर्ण भूमिका में होता है। असल बात तो ये है कि मानव समाज ही नहीं, संपूर्ण जीव-जगत डर की मौजूदगी के चलते ही गतिमान है। यहाँ एक आवश्यक प्रश्न यह उठता है कि यदि डर हमारे अनुभवों को स्वरूप दे रहा है तो डर को ज्ञान से भिन्न क्यों समझा जाए?
दरअसल डर की संकल्पना प्रत्यक्षत: हानि और अप्रत्यक्षत: लाभ से जुड़ी हुई है, यानी डर का आदि-अंत प्राय: भौतिक परिस्थितियों के मध्य ही विस्तारित रहता है, जबकि ज्ञान अपने मुक्त स्वरूप में निर्बंधित नहीं किया जा सकता।
डर के आवरण में छिपे लाभ-हानि के चिंतन से मुक्ति का प्रयास सभ्यता की शुरुआत से ही जारी है। इस चिंतन का उद्देश्य समय-समय पर सभ्यता को डर, अर्थात् लाभ-हानि के मकड़जाल में पूरी तरह से उलझने से बचाना था। समझने की बात है कि अगर हर व्यक्ति के चिंतन का प्रथम और अंतिम उद्देश्य हानि की न्यूनता एवं लाभ की अधिकता ही हो जाएगी तो सभ्यता के विकास की गति चाहे बढ़ती जाए पर उसका दायरा सीमित और मूल्य जड़ हो जाएंगे। बड़ी बात नहीं है ऐसी परिस्थितियों में स्वयं उस व्यक्ति समेत सब कुछ सिर्फ और-सिर्फ साधन बनकर रह जाएगा। यह व्यवस्था अमानव तैयार करेगी महामानव नहीं। यही अमानव ही एक दिन विश्व के अंत का कारण बनेंगे।
वस्तुत: ये डर व्यक्ति साथ लेकर नहीं जन्मता है। ब्राज़ील के पाउलो कोइलो, ‘द अल्केमिस्ट’ जैसी शानदार किताब के लेखक, कहते हैं कि व्यक्ति मूलत: दो प्रकार के डर साथ लेकर पैदा होता है। पहला, गिरने का डर और दूसरा, तेज़ आवाज़ का डर तथा ये दोनों डर हमारा मन नहीं, बल्कि हमारा तंत्रिका तंत्र महसूस करता है। इनके अतिरिक्त व्यक्ति अपने सभी डर जीवन के अपने अनुभवों के साथ ही अर्जित करता है। वस्तुत: मृत्यु का डर भी जन्मजात नहीं होता।
विचारणीय है कि अंधेरे में हम अकेले होने की वजह से नहीं बल्कि अकेले न होने की आंशका से डरते हैं। जीवन के शुरुआती चरणों में हमारा परिचय जिस क्रम से डर के जिस संस्करण से होता है, उसी क्रम और अनुपात में हम उस डर से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन के तमाम अनुभव दरअसल अलग-अलग तरह के डर और उनके प्रभावों के अनुमानों का संकलन हैं।
संभव है, डर से जन्मी दशाओं के चिंतन की इसी अवस्था अथवा निष्कर्ष पर आकर गीता में जीवन, शरीर, संबंध, धन इत्यादि लाभों को गौण बताया गया हो। क्या सच में असंभव है कि नए अनुभवों का लालच देकर जोखिम उठाने और बहादुर बनने की सीख देते समय पाउलो कोइलो का ‘बी ब्रेव, टेक रिस्क, नथिंग कैन सब्स्टीट्यूट एक्पीरियंस’ कहना, मानव को हानि से डरा हुआ स्वार्थी अमानव बनने से रोकने का एक प्रयास भर हो बिल्कुल संभव है।
भय और ज्ञान के संबंधों पर प्राचीनकाल से ही हमारे विचारकों ने पर्याप्त विमर्श और चिंतन किया है। हमारी ज्ञान परंपरा में भी इस बात के तमाम प्रमाण हैं कि हर तरह के भय के विरुद्ध हमारा ज्ञान प्रमुख हथियार रहा है। इसे समझने के लिये हम आत्मा का उदाहरण लेते हैं। एक अर्थ में, आत्मा की संकल्पना दरअसल मृत्यु के भय को कम करने का ही एक सफल उपाय है। मृत्यु से हम सभी परिचित हैं, जानते हैं कि शरीर का अंत तय है। ऐसे में हमारी आत्मा के अमर होने का ज्ञान हमें मृत्यु के भय से राहत देता है। ये महज़ संयोग नहीं है कि आत्मा को मुख्य रूप से वही सहूलियतें मिली हुई हैं, जिनकी हम अपने लिये कल्पना या इच्छा करते हैं। मसलन उसका अजर होना, अमर होना, आग से न जलना या ऐसे ही तमाम गुण।
डर के संदर्भ में लाभ-हानि संबंधी विश्लेषण में एक अनूठी बात यह भी है कि हमारी परंपरा में हर बीती हुई बात को ‘घटना’ कहने का रिवाज़ है। संस्कृति ने अपने दर्शन और विचारों को अपनी भाषा में गूँथ दिया है। जाहिर है कि भाषा संस्कृति की ज़ुबान बोलेगी, फिर भी विचारणीय है कि घटनाएँ घटती क्यों हैं? जुड़ती क्यों नहीं? शायद सब कुछ पूर्व निर्धारित होने की धारणा के चलते ऐसा कहा जाता हो। फिर तो जो हो चुका है, होने को है, उसका बहीखाता ज़रूर होता होगा कि अभी ये बचा है घटने को, घट जाएगा समय आने पर। हमारे भीतर हमारे इर्द-गिर्द या हमसे बहुत दूर जो कुछ भी है, सब कुछ घटा ही तो है। यहाँ समझ ये नहीं आता कि घटने के बाद क्षरण क्यों होता है फिर शायद क्षरण की विभिन्न प्रक्रियाएँ और चरण ही असल मनोरंजन है उस बहीखाते वाले का। आखिर क्षरण भी घटने की ही सूक्ष्म और चरणबद्ध प्रक्रिया ही तो है न
कहा जाता है कि कविताएँ रची नहीं जाती हैं, वो तो पहले से मौजूद होती हैं, रचनाकार बस उन्हें उजागर करते हैं। बात सिर्फ कविता, कहानी, संगीत या किसी अन्य कला तक सीमित होती तो क्या बात थी। साहित्य, भावनाएँ, प्राकृतिक गतिविधियाँ, नक्षत्रों की दशा, सफलता, असफलता, जीवन, मृत्यु; सब कुछ तो पहले से ही मौजूद रहता होगा फिर तो, और इसका रजिस्टर रखा रहता होगा किसी सुलेमानी बस्ते में। ये बस्ता किसकी पीठ पर रहता होगा? खैर, मजेदार बात तो यह है कि सब कुछ घटते जाने के बावजूद हम हमेशा जोड़ने की फिराक में रहते हैं। अगर एक बार मुस्कुराते हुए स्वत: ही घटने की इस प्रक्रिया में शामिल हो जाया जाए तो संभव है कि घटनाओं के सुलेमानी बस्ते वाले मुनीम से हमारी बनने लगे, दोस्ती हो जाए उससे कि हमने उसका काम आसान कर दिया। तब शायद हम घटने को लेकर भी उतना ही सहज हो जाएँ, जितना जुड़ने को लेकर हम रहते हैं और शायद ये भी समझ पाएँ कि जुड़ते वक्त भी दरअसल हम घटते ही हैं और तब शायद इस समझ के साथ ही जुड़ने-घटने के तमाम वहम और सुकून हमारे किसी काम के न बचें। यही तो मुक्ति है न मोक्ष यही तो है शायद
मुक्ति का गूढ़ अर्थ वास्तव में लाभ-हानि के विचारों से मुक्ति ही है। इसी को ज्ञान प्राप्ति की दशा भी कहा जाता है। पाश्चात्य परंपरा में डर की व्याख्या सफलता के मार्ग की प्रमुख बाधा के रूप में की गई है। उनके जीवन दर्शन में डर से संबंधित कथनों का विश्लेषण करने पर मसला भारतीय दर्शन से ज़्यादा अलग नहीं जान पड़ता। हर बार जब पाउलो कोइलो कहते हैं कि ‘जीवन को अलविदा कह पाने में सक्षम वीर ही जीवन की नई शुरुआत कर पाते हैं।’ तब-तब यह भरोसा और भी दृढ़ हो जाता है कि हानि के डर को पराजित किये बिना हम असल नफे तक नहीं पहुँच सकते हैं और असल नफा कुछ और नहीं ज्ञान प्राप्ति ही है।
 |
[हिमांशु सिंह] |